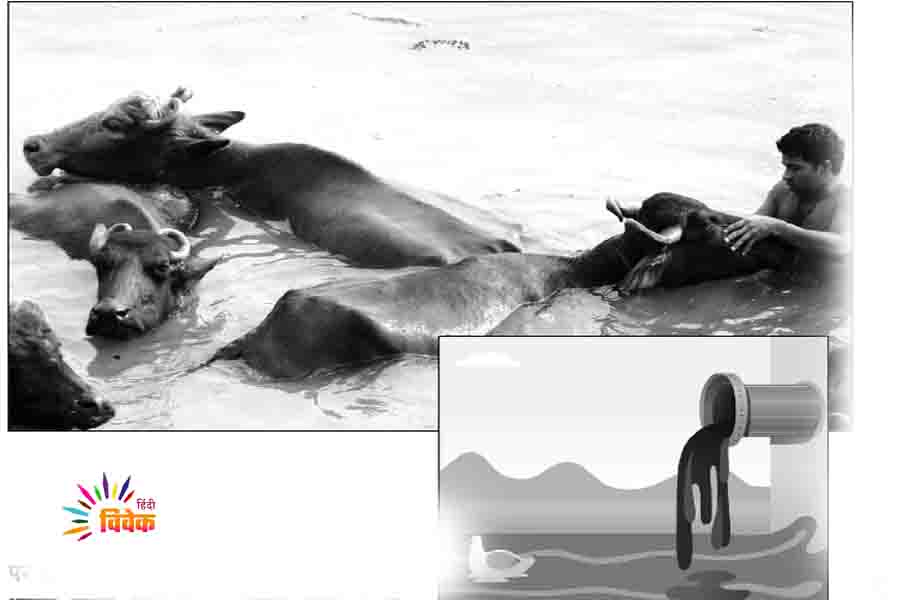बढते तापमान के परिणामस्वरूप बढ़ती शुष्कता, बढ़ते बाष्पीकरण से जमीन पर होनेवाले दुष्परिणामों को रोका जा सकता है। इसके लिए जमीन पर योजनाबध्द तरीके से भरपूर घास और वृॄक्षों का ऐसा आवरण बनाना होगा जो तेजी से बरसने वाले पानी को सही ढंग से सोख सके। वर्तमान में चरागाहों की उपयोगिता की ओर आवश्यक ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इस संदर्भ में सामाजिक जागृति करनी होगी। चरागाहों का विकास एवं सुरक्षा एक महत्त्वपूर्ण उपक्रम होना चाहिए। जल प्रबंध को पूरक के रूप में इसे जलागम क्षेत्रों में प्राथमिकता से चलाना चाहिए।
19 वीं सदी के मध्य से ही विश्वभर में जलवायु को सावधानी से नोट किया जाने लगा। सीमित मात्रा में जानकारी का आदानप्रदान भी आरंभ हुआ। इससे वैश्विक जलवायु में सालदरसाल कैसे बदलाव आता है तथा एक ही समय विश्वभर में किस प्रकार भिन्नभिन्न स्थिति होती है, इसके प्रति कौतूहल एवं अध्ययन में भी वृद्धि होने लगी। सालदरसाल होनेवाले ये बदलाव किन कारणों से होते हैं इसकी खोज भी आरंभ हुई। संभावना यह व्यक्त की गई कि सूरज के बदलते दागों के कारण ये परिवर्तन होते होंगे। एक अनुमान यह भी था कि प्रागऐतिहासिक हिमवर्ष, अतिबारिश के वर्ष एवं अल्पबारिश के वर्ष की लगातार प्रदीर्घ कालचक्रीय पद्धति से जलवायु में परिवर्तन आता है। 1940 के पश्चात् इन पृथ्वीबाह्य प्रभावों से होनेवाले चक्रीय परिवर्तनों के अलावा पृथ्वी के ऊपर ही नये विज्ञान युग के कारण तथा उसमें से निर्माण हुई नयी उद्योग व्यवस्थाओं से और साथ ही बदलती जीवनशैली के फलस्वरूप पृथ्वी के वायुमंडल पर मानवी व्यवस्थाओं का भी लक्षणीय प्रभाव की संभावनाएं व्यक्त की जाने लगीं।
विशेषज्ञों की यह राय बनी कि औद्योगिक इकाइयों से तथा ईंधनों पर आधारित यातायात व्यवस्था से जो जहरीली गैसे बड़ी मात्रा में निकलती हैं उसका पृथ्वी की जलवायु पर असर होता है। वैज्ञानिकों के इस संबंध में भिन्नभिन्न निरीक्षण और निष्कर्ष थे। उनमें तालमेल न था। इसलिऐ राष्ट्रसंघ के विज्ञान कार्यक्रम के अंतर्गत आयपीसीसी नाम से एक समिति अध्ययन करने के लिए गठित की गई। उस समिति ने समय-समय पर संकलित अध्ययनों के आधार पर रिपोर्ट प्रकाशित की। उसमें आरंभ में ऐसे परिवर्तनों की संभाव्यता व्यक्त की गई। अंत में सन 2007 की रिपोर्ट में इसे स्पष्ट किया गया कि पिछले 100 से अधिक वर्षों से मानवी व्यवस्था ने हवा में कार्बन डाइआक्साइड़ जैसे अनेक घटक अतिरिक्त मात्रा हवा में छोड़े हैं जिसका कुल परिणाम पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ने में निश्चित रूप से हो रहा है। सूर्य से पृथ्वी पर आने वाली उष्णता पहले जितनी ही हो लेकिन पृथ्वी से परावर्तित होने वाली उष्णता इन अनिष्ट वायु घटकों से प्रतिबंधित होती है और सूक्ष्म रूप में भी क्यों न हो लेकिन इस वायुमंडल में बंदिस्त होती है और उसके फलस्वरूप पृथ्वी का औसतन तापमान पिछले सौ वर्षों मे 0.74 अंश सेंटीग्रेड बढ़ा है तथा अगले दो दशकों में वह प्रति दशक में 0.2 अंश सेंटिग्रेड तक बढ़ते जाने के आसार दिखाई दे रहे हैं।
इसके परिणामस्वरूप उत्तर-दक्षिण दोनों ध्रुवों पर अथवा आल्प और हिमालय में भी बर्फ का अतिरिक्त पिघलना दिखाई देने लगा है। ग्लेशियर सिमटते जा रहे हैं। पृथ्वी के दो तिहाई पृष्ठ भाग पर फैले हुए सागर का बाष्पीकरण बढ़ रहा है। इन सभी बातों का वायुमंडल पर असर हुआ है और सौ साल पहले का जलीय चक्र बदल गया है। नई जलचक्रीय प्रक्रिया का उदय हो रहा है।
परिणामस्वरूप बारिश तथा तूफानों की तीव्रता बढ़ती दिखाई दे रही है। सर्द इलाकों में भी गरमी का मौसम ज्यादा तीव्र हुआ है। वह असहनीय होने से मानवहानि का खतरा दिखाई दे रहा है। भारत के संदर्भ में अगर देखें, तो हिमालय के ऊपर के हिमनद अब अधिक मात्रा में छीजते जा रहे हैं और उससे गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु आदि नदियों को बर्फ पिघलने से गरमी के मौसम में मिलनेवाला पानी घटने का खतरा दिखाई दे रहा है। बढते बाष्पीकरण से पृथ्वी से हवा में लौटनेवाला बारिश के बाद का पानी बढ़कर भूजल में रूपांतर होने की प्रक्रिया किसी हद तक क्षीण होनेवाली है। बारिश की तीव्रता बढ़ी, तो भी बारिश के दो मौसमों में होनेवाली दूरी का ख्याल कर आगामी जलप्रबंध का ब्यौरा नये सिरे से निश्चित करना आज जरूरी देख रहा है।
एक ओर अनिष्ट वायु आदि पर रोक लगाने हेतु ‘क्योटो प्रोटोकॉल’ जैसे अंतरराष्ट्रीय प्रतिज्ञापत्र का महत्त्व एवं अनुपालन आदि की ओर विश्व का ध्यान बढ़ता जा रहा होगा, फिर भी उससे साध्य होने वाला वायुमंडल में संभाव्य सुधार यह कम से कम दो-तीन दशकों तक वास्तव में अनुभव किया जाएगा ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। उससे पानी के नियोजन में कम से कम अगले तीन दशकों की अवधि में जल चक्र में हो रहे परिवर्तन होते ही रहेंगे। या यों कहिए कि किसी हद तक बढ़ेंगे, ऐसा मानते हुए ही भविष्य की जलप्रबंध नीतियां तय करना उचित होगा। उदाहरणार्थ बारिश की तीव्रता बढ़ेगी, परंतु दो बारिशों के बीच का अंतराल भी बढ़ेगा। ऐसी स्थिति को निपटने की दृष्टि से कृषि तालाबों की उपयोगिता महत्वपूर्ण होगी। दूसरी ओर बारिश की बढ़ती तीव्रता के कारण, जहां-जहां भूपृष्ठीय संचय करने हेतु छोटे बडे बांधों का निर्माण किया गया है, वहां बाढ़ की समस्या पर ज्यादा ध्यान देना होगा। बड़े बांधों में दरवाजे लगाकर किसी हद तक बाढ़ का नियंत्रण संभव होता है। लेकिन जहां दरवाजे नहीं लगे हैं वहां बाढ़ की बढ़ती तीव्रता का मुकाबला कर सकें, इस दृष्टि से उनके नहरों का अधिक विस्तार करना जरूरी होगा।
बढ़ते तापमान के परिणामस्वरूप बढती शुष्कता, बढ़ता बाष्पीकरण आदि के जमीन में पानी के सोखे जाने पर होनेवाले दुष्परिणामों को रोकने के लिए तेजी से बरसने वाले पानी को सही ढंग से सोखा जा सके, ऐसा घास से भरापूरा तथा वृक्षीय आवरण आदि की नियोजनबद्ध वृद्धि करनी होगी। वर्तमान परिस्थिति में भी जलचक्रीय संदर्भ में चरागाहों उपयोगिता की ओर आवश्यक जितना ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इस संदर्भ में सामाजिक जागृति में वृद्धि कर चरागाहों के विकास एवं सुरक्षा को एक महत्वपूर्ण उपक्रम के रूप में जलप्रबंध को पूरक के रूप में जलागम क्षेत्रों में प्राथमिकता से चलाना होगा। जो बस्तियां, खेती जमीन, गृहनिर्माण आदि जो नदियों के तटों के समीप हैं, उन्हें बाढ़ से पहुंचनेवाले खतरे आगामी काल में बारम्बार-होने की संभावना है। उसके फलस्वरूप जिन्हें दस वर्षोंं में कभी एक बार बाढ़ के खतरे का सामना करना था, उन्हें तो अब तीन या पांच वर्षों के बाद ही उन कठिनाइयों में से गुजरना पड़ेगा। इसलिए ऐसी व्यवस्थाओं की बडे पैमाने पर पुनर्रचना शुरू करनी होगी। विशेष रूप से जिन शहरों का विस्तार नदी के तटों पर हुआ है- उदाहरण पंढरपुर, नांदेड, पैठण, चिपलुण, महाड आदि उन सभी की नगररचना का तथा सुरक्षा का सावधानी से पुनरावलोकन करते हुए आवश्यक पुनर्रचना बाढ़ की बारंबारता के संदर्भ में सही ढंग से करना आवश्यक होगा।
बढ़ते तापमान के कारण समुद्र का स्तर कहां और कितना ऊपर उठनेवाला है, इसके बारे में विभिन्न प्रकार के अनुमान महत्त्वपूर्ण महासागरों के संबंध में वैज्ञानिक पुष्टि के साथ व्यक्त किये जा रहे हैं। खासकर चीन जैसे प्रशांत महासागर की बगल में प्रदीर्घ लंबा तटवर्ती इलाके वाले देश ने उस इलाके पर कहां-कहां और कितना सागर का स्तर अगले पचास बरसों में ऊपर उठेगा इस संदर्भ में वैज्ञानिक अनुमान बना लिये हैं तथा तटवर्ती गांवों को सतर्क कर अपनी पुनर्रचना करा लेने को प्रोत्साहित किया है। उसका अनुकरण लंबे तटवर्ती इलाके वाले सभी देशों को तुरन्त करना ही जरूरी होगा। विशेष रूप से टापुओं पर बसी आबादी के लिए सागर के स्तर में होनेवाले ये परिवर्तन ज्यादा खतरनाक हैं, तभी तो इन टापुओं पर चलनेवाले मानवी क्रियाकलापों का मूलभूत पुनर्विचार आवश्यक है।
वैज्ञानिकों का अनुमान है कि विभिन्न क्षेत्रों में होनेवाली बारिश के कुल सालाना परिणामों में भी शायद महत्त्वपूर्ण परिवर्तन होंगे। वैसे तो भारत जैसे उष्ण कटिबंधीय देशों में वर्षा की कुल मात्रा बढ़ने की संभावना दिखाई दे रही है, लेकिन बारिश का मौसम शुरू होना और समाप्त होना इसमें भी कुछ परिवर्तन होंगे ऐसा लगता है। उस कारण पारंपरिक ऋतुचक्र की तथा उस पर आधारित कृषिप्रणाली की जो कार्यव्यवस्था स्थायी बनी हुई है, उसमें कुछ परिवर्तन करना जरूरी होगा।
इसलिए भारतीय संदर्भ में संभाव्य परिवर्तनों का पता करा लेनेवाला ब्यौरेवार अध्ययन आगामी एक-दो बरसों में अगर हम कर सकें और उसे प्रकाशित करें, तो उस पर विभिन्न क्षेत्रों में चर्चा हो सकती है। उसके द्वारा समाज का यथोचित प्रबोधन होगा और उसके लिए आवश्यक परिवर्तनों का स्वीकार करने की मानसिकता बनेगी। पानी, खेती, जलवायु आदि विषयों के संदर्भ में वैज्ञानिक एवं ऐच्छिक काम करनेवाले कितने ही संगठन भारत में हैं। उन्हें इस दिशा में प्रवृत्त कर उन्हीं के द्वारा यह मार्गदर्शनात्मक विश्लेषण शीघ्र ही समाज के समक्ष लाना निहायत जरूरी है।
नियोजन तटवर्ती क्षेत्र का
बढ़ते तापमान से समुद्र का स्तर कहां और कितना ऊपर उठनेवाला है, इसे लेकर महत्त्वपूर्ण महासागरों के लिए भिन्न-भिन्न अनुमान वैज्ञानिक प्रमाणों द्वारा व्यक्त किये जा रहे हैं। इस सदी के अंत तक सागर के स्तर में आधे मीटर से भी अधिक वृद्धि कई जगहों पर होने का खतरा है। ध्रुवीय प्रदेशों की बर्फ पिघलने से सागर में जा मिलनेवाले ठंडे पानी के प्रवाह के दबाव के परिणामस्वरूप आज तक के प्रस्थापित सागरीय उष्ण प्रवाह या ठंडे प्रवाह के प्रचालन में बड़ा परिवर्तन अपेक्षित है। एक ओर हवा के बढ़ते तापमान से सागर के पानी का तापमान बढ़ता जानेवाला है, तो दूसरी ओर उसमें घुसने वाले ठंडे पानी के प्रवाह बड़े तेज होंगे। उसका परिणाम तटवर्ती क्षेत्र की जलवायु पर होनेवाला है। हवा में अतिरिक्त मात्रा में छोड़े जा रहे अन्य घटकों के कारण हवा का तापमान निश्चित रूप में बढ़ रहा है। इस तथ्य पर वैज्ञानिक सहमत हों, तो भी इस तापमान वृद्धि के सागर के पानी पर एवं जमीन पर जो विभिन्न प्रकार के परिणाम होने जा रहे हैं, उनका अध्ययन अब तक पर्याप्त मात्रा में न होने से उस संबंध में आज भी पूरी स्पष्टता नहीं है। ऐसे संभाव्य परिणामों पर स्थानीय संदर्भ में सही ढंग से ध्यान देना, यह वहां के सामाजिक स्थैर्य की दृष्टि से निहायत जरूरी लगता है। इसीलिए उस संदर्भ में काफी विशाल अनुसंधान की, स्थानीय गणना की तथा विश्लेषण की योजना और अधिक मात्रा में करना जरूरी है।
भारत में विश्वविद्यालयीन अनुसंधान व्यवस्था अभी तक उस दिशा में पर्याप्त मात्रा में कार्यरत हुई नहीं है। उस कारण स्थानीय जलप्रबंध की ब्योरेवार पुनर्रचना के लिए और कुछ समय प्रतीक्षा करनी होगी, ऐसा दिखाई देता है। फिर भी जिन प्रदेशों में बाढ़ के, उष्ण हवा के झोंकों के या तेज बारिश के दुष्परिणाम पहले से ही जांचे जा रहे हैं, उनकी भविष्य की जरूरतों का एवं तदनुसार आवश्यक उचित रचनाओं का विचार ठोस रूप में क्यों न हो, पर समय पर ही होना चाहिए। तब जाकर तुरन्त करने योग्य कुछ उपाय समय पर ही करना संभव होगा। इसके अलावा नये स्थानीय अनुसंधान द्वारा किस बिंदु पर ज्यादा प्रकाश डालना जरूरी है, इसकी कुछ कल्पना आ सके। उस दिशा में जिन देशों ने उचित समय पर ही ब्यौरेवार अध्ययन आरंभ किया है, उनमें चीन एक है। चीन में प्रशांत के किनारे पर प्रदीर्घ तटवर्ती क्षेत्र है। उस तटवर्ती क्षेत्र में अगले पचास बरसों में सागर का स्तर कहां कितना ऊपर उठेगा इस संबंध में वैज्ञानिक अनुमान चीन ने बनवा लिये हैं तथा तटवर्ती इलाके के गांवों को सतर्क कर उसके आधार पर अपनी पुनर्रचना कराने प्रवृत्त किया है। इन सभी प्रयासों का अनुकरण लम्बे तटवर्ती इलाके वाले सभी देशों को तुरन्त करना आवश्यक है।
खासकर टापुओं पर बसी हुई आबादी के लिए सागर के स्तर में होनेवाले परिवर्तन ज्यादा खतरनाक हैं। ऐसे टापुओं पर जीवन-व्यवहारों का मूलगामी पुनर्विचार आवश्यक है। मुंबई महानगर इस संदर्भ में काफी संवेदनक्षम होगा। इसलिए वहां ऐसा अध्ययन तुरन्त होना चाहिए। भारत के पूर्व की ओर के प्रदेशों में वर्षा की बदलते स्वरूप में कौन से परिवर्तन होने की संभावना है, इसका कुछ अध्ययन हाल ही में हुआ है। वैसे ही महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर होना चाहिए।
मुंबई महानगर का विस्तार और सागर तट की निकटता के कारण सागर के स्तर में होनेवाली संभाव्य वृद्धि का आघात मुंबई पर होने का खतरा है। विशेष रूप से मुंबई द्वीप पर नदियों के मुहाने की खाडियां में ज्वार के समय अंदर आनेवाला पानी और ठीक उसी समय बारिश हो रही हो तो खाड़ी की पिछली ओर वाले नदी के प्रवाह में होनेवाला उभार बढ़नेवाला होगा। इस संभाव्यता का ख्याल कर मुंबई की नागरी, औद्योगिक तथा यातायात व्यवस्था का तुरन्त पुनर्नियोजन होना लाभदायक होगा। इस दृष्टि से मुंबई के भू-पृष्ठ के बीस-बीस सेंटिमीटर ऊंचाई पर की ऊंचाई दिखानेवाले नक्शे तुरन्त उपलब्ध होना जरूरी है। सन 2005 में मुंबई में जो प्रलय हुआ, उसने यह आवश्यकता पहले की अधोरेखित की है। इस संदर्भ में मुंबई के वर्तमान हवाई अड्डे की सुरक्षा को लेकर पुनर्विचार जल्द से जल्द होना लाभदायक साबित होगा।