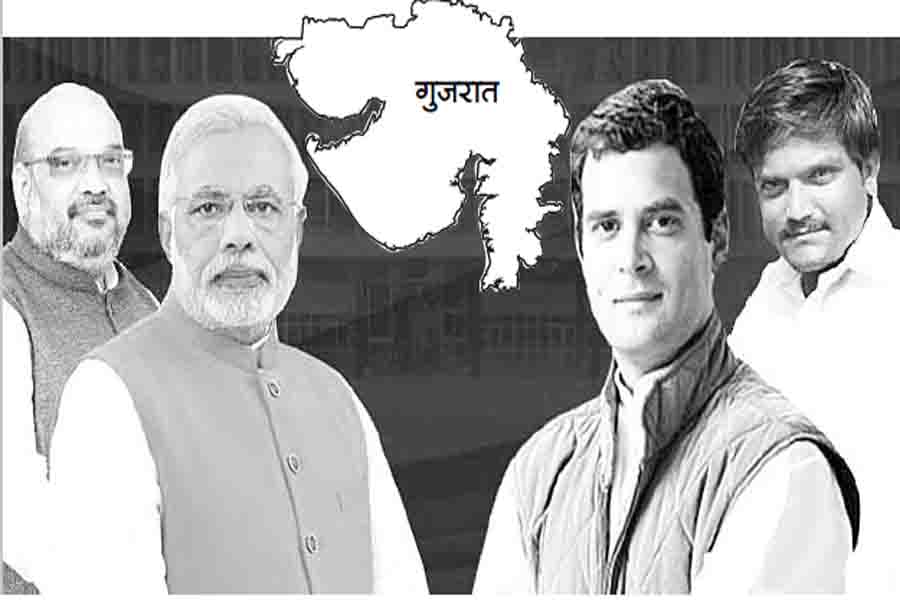गिरिजा देवी को भले ही ठुमरी साम्राज्ञी और ठुमरी की रानी मात्र कहा गया, लेकिन वे छंद-प्रबंध, ध्रुवपद धमार, ख्याल, तराना, ठुमरी, दादरा टप्पा, कजरी, चैती, होली, झूला और भजन आदि जैसी दर्जनों गान विधाओं की कंठसिद्ध गायिका थीं| डॉक्टरों के मना करने पर भी वे गाती रहीं… लोगों को हंसाती रहीं… रूलाती लुभाती और मनाती रहीं… और फिर गहरी नींद में सो गईं…फिर कभी न खुलने वाली नींद में…
विदुषी गिरिजादेवी २४ अक्टूबर की रात जिस समय अपने जीवन की अंतिम सांसें ले रहीं थीं, लगभग उसी समय दिल्ली के एक सभागार में मंच से मैं उनका जिक्र कर रहा था| वे मेरी मुंहबोली बुआ थीं…. मेरे चाचाजी पं. श्रीचंद्र मिश्र की वे प्रिय और प्रमुख शिष्या थीं और उन्हें तथा मेरे बाबूजी तबला शिरेामणि पंडित गामा महाराज को ‘भैया’ कहकर बुलाती थीं| इसलिए, हम सब बचपन से ही उन्हें बुआ कहते थे|
पद्मश्री, पद्मभूषण और पद्मविभूषण जैसे अलंकरणों, केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी सम्मान, अकादमी की रत्न सदस्यता और डी.लिट् की मानद उपाधियों सहित देश-विदेश के सैंकड़ों सम्मानों से विभूषित और ठुमरी साम्राज्ञी, ठुमरी की रानी तथा क्वीन ऑफ ठुमरी के सम्बोधन से निर्विवाद रूप से संबोधित की जानेवाली गिरिजा देवी का सांगीतिक सफर बहुत आसान नहीं था| उनका विवाह मात्र १७ वर्ष की उम्र में हो गया था और विवाह के बाद ही ससुराल वालों की ओर से उनके संगीत को प्रतिबंधित करने का प्रंयास आरंभ हो गया था| उन दिनों वे बहुत दुखी रहा करती थीं| लेकिन, गाना उन्होंने नहीं छोड़ा| वे अपने घर-परिवार रिश्ते और रिश्तेदारों का पूरा ध्यान रखते हुए भी संगीत के अभ्यास के लिए समय निकाल ही लेती थीं| सब्जी काटते समय, खाना बनाते समय या घर के अन्य कार्यों को करते समय भी उनका गला चलता रहा था वे गाती-गुनगुनाती रहतीं थीं|
उनके पति श्री मधुसूदन दास ने, जो वाराणसी के उच्चवर्गीय व्यवसायी थे, जब संगीत के प्रति उनकी दीवानगी को महसूस किया तो उन्हें बहुत दुख हुआ और उन्होंने गिरिजा देवी को गाने की अनुमति दे दी, लेकिन, साथ ही यह अनुरोध भी किया कि वे सिर्फ प्रतिष्ठित मंचों पर ही अपने गायन का कार्यक्रम देने की यथासंभव कोशिश करें| गिरिजा देवी ने भी अपने पति को वचन दिया कि पारिश्रमिक चाहे कितना भी अधिक, कितना भी आकर्षक क्यों न हो वे किसी की भी निजी महफिल में नहीं गाएंगी… किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं गाएंगी… किसी राजा, नवाब, सेठ या रईस के लिए नहीं गाएंगी… वे जब भी गाएंगी खास नहीं आम लोगों के लिए गाएंगी… जनता जनार्दन के लिए गाएंगी|
यह घटना १९४६ के अंत और १९४७ के आरंभिक दिनों की है| देश और गिरिजा देवी दोनों आजाद होने के लिए छटपटा रहे थे… दोनों की आजादी लगभग तय हो चुकी थी और अंततः १९४७ में दोनों को आजादी मिल भी गई लेकिन कुछ शर्तों के साथ| पति की आज्ञा मिलते ही गिरिजा देवी संगीत साधना में प्राण पण से जुट गईं लेकिन, इसके बावजूद पति और परिवार की सुख-सुविधा की अवहेलना नहीं की| उन्होंने दोनों मोर्चों पर मुस्तैदी और ईमानदारी से काम किया और पूरी तरफ सफल रहीं| १९४९ में उन्होंने आकाशवाणी से गाना शुरू कर दिया था| जो उस समय बहुत बड़ी बात थी| १९५१ में उन्होंने आरा (बिहार) में पहला सार्वजनिक कार्यक्रम दिया था जो उनके जीवन में मील का पत्थर साबित हुआ|
प्रख्यात पखावज वादक और जमीरा के राजा श्री शत्रुंजय प्रसाद सिंह उर्फ ललन बाबू उन दिनों तबला के महान कलाकार खलीफा पं. बिक्कू महाराजजी और उनके सुपुत्र तबला शिरोमणि पं. गामा महाराज से तबला सीखने प्रायः बनारस आते रहते थे| पं. गामा महाराज और पं. श्रीचंद्र मिश्र कहने को तो आपस में चचेरे भाई थे लेकिन, उनका आपसी प्रेम सहोदर से भी ज्यादा था| रहना और खाना दोनों एकसाथ होता था| दूसरी ओर बाबू ललनजी पखावज वादक के साथ-साथ संगीत उन्नायक की भूमिका में भी स्वयं को रेखांकित कर रहे थे| पं. अनोखे लाल मिश्र, पं. सामता प्रसाद गुदई महाराज, उ. हबीबुद्दीन खां पं. सियाराम तिवारी, विदुषी दमयंती जोशी और आशा ओझा जैसे उस जमाने के अनेक प्रतिभावान और गुमनाम संगीतकारों को उनका संरक्षण प्राप्त था| वे अपने निजी प्रयासों से बड़े-बड़े संगीत समारोह भी आयोजित करते थे जिसमें पं. कंठे महाराज, पं. ओंकारनाथ ठाकुर, उ. अमीर खां और उ. बड़े गुलाम अली खां जैसे कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देते थे| ऐसे ही एक संगीत समारोह में १९५१ में पं. गामा महाराज और पं. श्रीचंद्र मिश्र के कहने पर उन्होंने २२ वर्षीय गिरिजा देवी को गाने का अवसर दिया, और गिरिजा देवी ने वह महफिल जीत ली| उस रात गिरिजा देवी के संगीत का जादू लोगों के सिर चढ़कर बोला और फिर गिरिजा देवी को कभी पीछे मुड़कर देखने का अवसर नहीं मिला| गिरिजा देवी जमीन से जुड़ी गायिका थीं| वे बहुत ही सहज और सरल थीं| इतनी बड़ी और गुणी गायिका होने बावजूद उनका सभी के साथ आत्मीय और स्नेहिल हो जाना उनकी बहुत बड़ी विशेषता थी| उन्होंने अपने से वरिष्ठ कलाकार पं. कंठे महाराज की संगति में भी गायन पेश किया था और अपने समकालीन तबला वादकों पं. किशन महाराज, पं. गुदई महाराज, पं. रंगनाथ मिश्र और पं. शीतल प्रसाद मिश्र के साथ भी| इसके अलावा युवा पीढ़ी के सुधीर पांडेय, अकरम खान और विनोद लेले से लेकर सरित दास, शुभ महाराज, जयशंकर मिश्र और अभिषेक मिश्र आदि जैसे नयी पीढ़ी के अनेक होनहार तबला वादकों को अपने साथ संगति का अवसर देकर उन्होंने उनके आगे बढ़ने के लिए एक नया द्वार खोल दिया था|
इस महान गायिका को भले ही ठुमरी साम्राज्ञी और ठुमरी की रानी मात्र कहा गया, लेकिन मैं इस बात का गवाह हूं कि वे छंद-प्रबंध, ध्रुवपद धमार, ख्याल, तराना, ठुमरी, दादरा टप्पा, कजरी, चैती, होली, झूला और भजन आदि जैसी दर्जनों गान विधाओं की कंठसिद्ध गायिका थीं| वे नियम से अपने हर कार्यक्रम का शुभारंभ विलंबित ख्याल से करती थीं| इसके बाद द्रुत ख्याल और फिर ठुमरी आदि गान विधाओं की ओर मुड़ती थीं| उनके कहन ओर पुकार का अंदाज सबसे निराला था| बोल बनाव के समय जिन स्वप्निल परिकल्पनाओं का परिचय वे अपने कंठ से देती थीं वह उन्हीं के वश की बात थी| काकु भेद अथवा स्वरों के उतार-चढ़ाव मात्र से एक ही शब्द के अनेक अर्थ रच देने में उन्हें महारत हासिल थीं|
मैंने उन्हें बचपन से ही अपने घर में आते जाते गाते हुए देखा सुना था| वे चाहें जितनी भी बड़ी गायिका थीं मेरे लिए तो घर के आम सदस्य की ही तरह थीं| मेरे बनारस छोड़ देने के बाद भी आरा, पटना, समस्तीपुर, बनारस और लखनऊ आदि के कार्यक्रमों में छोटी-मोटी मुलाकातें होती रहती थीं| लेकिन फिर मेरे जीवन में संघर्ष का एक ऐसा दौर आया कि १९७७ में मुझे अचानक ७ वर्षों के लिए असम जाना पड़ गया, उसके बाद ६ वर्षों तक राजस्थान में रहा, फिर अन्य स्थानों पर और इस तरह ३५ वर्ष निकल गए गिरिजा देवी से मिले बिना| वे भी एक तरह से कोलकाता में बस गई थीं| लेकिन हम दोनों तक एक दूसरे की सूचनाएं, हाल-चाल पहुंचती रहती थीं| इस बीच मैं दिल्ली आ गया था| दिल्ली आने के बाद मेरा कार्य क्षेत्र बदल गया| उन दिनों प्रख्यात संतूर वादक, पद्मश्री पं. भजन सोपोरी ने सामापा- सोपोरी एकेडमी ऑफ म्यूजिक एंड परफार्मिग आर्ट्स की स्थापना की थी-जिसमें बहुत छोटी ही सही लेकिन मेरी भी भूमिका थी| सामापा के त्रिदिवसीय भव्य संगीत समारोहों की गूंज देश-विदेश तक सुनाई देने लगी थी| इसी समारोह में एक वर्ष गिरिजा देवी और हेमा मालिनी को सम्मानित करने का निर्णय लिया गया| उस दिन करीब ३५ वर्षों के बाद हम दोनों- मैं और गिरिजा देवी आमने-सामने थे| उन्होंने अंतिम बार मुझे १६ वर्ष की उम्र में देखा था और अब ५१ वर्ष की उम्र में देख रहीं थीं| स्वाभाविक ही था कि उन्होंने मुझे नहीं पहचाना| मैंने उनके नजदीक जाकर नमस्ते करते हुए जब अपना नाम बताया तो उन्होंने उसी ३५ वर्ष पूर्व की आत्मीयता से प्यार से मेरा गाल थपथपाते हुए मुझे गले लगा लिया| उस शाम पूरे समारोह के दौरान वे मेरा हाथ थामे बैठीं रहीं| जब भी किसी चीज की जरूरत पड़ी मुझसे बोलीं| और अगले दिन तो उन्होंने हद ही कर दी|
कमानी सभागार के मंच पर गाने के लिए जब वे जाने लगीं तो उनका हाथ पकड़े उनके साथ मैं था| उन्हें मंच पर बैठाने के बाद मैंने पूछा- क्या सामने बैठकर आपका गाना सुनूं? उन्होंने गर्दन हिलाकर सहमति दी, फिर तानपूरा आदि मिलाने लगीं| गाना शुरू करने के पूर्व उन्होंने पं. भजन सोपोरी और उनकी संस्था सामापा को धन्यवाद और शुभकामनाएं देते हुए स्वीकारा कि एक कलाकर द्वारा जब किसी दूसरे कलाकार को सम्मानित किया जाता है तो एक प्रकार की आंतरिक खुशी मिलती है| लगता है कि मेरी विधा का जानकार व्यक्ति मेरे गुणों की प्रशंसा कर रहा है| इसके बाद वे बोलीं, यह मेरा सौभाग्य है कि मेरे सामने, मेरा गायन सुनने के लिए मेरे घराने के खलीफा पं. विजय शंकर मिश्र बैठे हुए हैं| मैं इनके घर की शिष्या हूं… इनके घर की जूठन हूं और आज जो कुछ भी इनके घर की बदौलत हूं| उनकी वाणी, उनके शब्द मेरे रोम-रोम को झंकृत कर गए| मैं अविचल बैठा रह गया| उनका गायन संपन्न होने के बाद मैं स्वयं को रेाक नहीं पाया| मुझे यह आवश्यक जान पड़ा कि कुछ स्पष्टीकरण जरूरी हैं| अतः मैंने माइक पर कहा कि- ‘‘अभी आप जिन गिरिजा देवी को सुन रहे थे-यह सच है कि ये मेरे घर की शिष्या हैं, लेकिन ये मेरे घर की जूठन नहीं हैं… ये मेरे घर की आन-बान- शान हैं| इस शानदार परम्परा की शानदार धरोहर हैं, विभूति हैं| इन पर हम सबको गर्व है और व्यक्तिगत तौर पर मेरा यह सौभाग्य है कि मैं इन्हें बुआ कहता हूं|’’ फिर मैंने उनके पैर छुए|
इसके बाद ही दिल्ली दूरदर्शन के नेशनल चैनल के लिए मुझे उनका साक्षात्कार लेने का सुयोग मिला| साक्षात्कार के दौरान भी और उसके बाद भी उनसे ढेर सारी बातें करने का अवसर मिला| वे संगीत साधना के प्रति युवाओं की निष्ठा में आई कमी से चिंतित थीं… वे इस बात से परेशान थीं कि युवा संगीतकारों में धैर्य नहीं है… वे रातोंरात सब कुछ पा लेना चाहते है| और, इसके लिए वे हर प्रकार के लटके-झटके-हथकंडे अपना लेते हैं| जबकि वे इसे साधना और आराधना मानती थीं|
गिरिजा देवी बहुमुखी प्रतिभा की धनी कलाकर थीं| उन्होंने कई प्रकार के गीत, ठुमरी आदि का लेखन भी किया था| उ. बिस्मिल्लाह खां, उ. विलायत खां, उ. अमजद अली खां, पं. बिरजू महाराज, पं. राजन-साजन मिश्र और पं. हरिहरन जैसे अलग-अलग पीढ़ियों के कलाकारों के साथ मिलकर कार्यक्रम दिया था| काशी हिन्दू विश्वविद्यालय और आई.टी. सी. संगीत रिसर्च अकादमी (कोलकाता) में संगीत की नई पीढ़ी को प्रशिक्षित किया तो मालिनी अवस्थी, शालिनी वेद त्रिपाठी, पद्मजा चक्रवर्ती, रीता देव, मधुरानी शुक्ला और इन जैसे दर्जनों सुशिक्षित कलाकारों को तैयार किया और ठुमरी की ठुमक को एक नई पहचान दी|
विदुषी गिरिजा देवी की बात हो, ठुमरी की बात हो और दिल्ली के श्री विनोद कपूर की बात न हो तो बात शायद अधूरी रह जाएगी| सेवा निवृति के बाद शिथिल पड़ती जा रही गिरिजा देवी और ठुमरी गायकी को विनोद कपूर ने एक नई जान दी थी| उन्होंने गिरिजा देवी के नाम पर ठुमरी गायन के क्षेत्र में एक पुरस्कार की स्थापना की और देश के भिन्न-भिन्न भागों में विभिन्न स्तरीय ठुमरी प्रतियोगिताओं का आयोजन आरंभ किया था, जिससे कई बड़े-बड़े कलाकार और संगीत समीक्षक गहराई से जुड़े हुए थे| इन पंक्तियों का लेखक यद्दपि इस आयोजन से नहीं जुड़ा था, तथापि एक तटस्थ और सामान्य श्रोता के रूप में इसने अनुभव किया कि इससे ठुमरी गायकी एक बार फिर लोकप्रियता की ओर मुड़ी थी| आशा करनी चाहिए कि यह यात्रा चलती रहेगी|
विगत कुछ समय से गिरिजा देवी पर उम्र का असर दिखने लगा था| वे हृदय रोग से भी पीड़ित थीं| इसलिए वे संगीत से संन्यास लेने को सोचने लगीं थीं| यद्दपि उनके चिकित्सकों ने उन्हें २००६ में ही गायन और भ्रमण दोनों पर रोक लगाने की सलाह दी थी, लेकिन वे नहीं मानीं| उन्होंने अपने चिकित्सकों से कह दिया था कि गाना नहीं गा तो ऐसे ही मर जा- इसलिए मैं गाते हुए मरना चाहती हूं, और वे गाती रहीं| निधन के दो महीने पहले साहित्य कला परिषद द्वारा दिल्ली के कमानी सभागार में आयोजित ठुमरी महोत्सव में गाकर उन्होंने सबको भावविभोर कर दिया था| उसके बाद भी वे गाती रहीं… लोगों को हंसाती रहीं… रूलाती लुभाती और मनाती रहीं… और फिर गहरी नींद में सो गईं…फिर कभी न खुलने वाली नींद में…