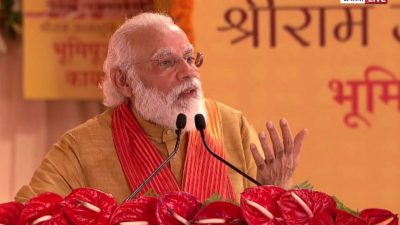हमें पश्चिमी प्रतिमानों या उदाहरणों का गहराई से अध्ययन विश्लेषण करना चाहिए और यदि संभव हो तो उनसे लाभ भी उठाना चाहिए। लेकिन उन्हें अपने भावी विकास का आदर्श प्रतिमान मानने की गलती नहीं करनी चाहिए। आत्मनिर्भरता का वैचारिक अधिष्ठान यही है।
चीनी वायरस के कारण पांच महीने में ही दुनिया भर की लगभग सभी अर्थव्यवस्थाओं ने घुटने टेक दिए हैं। पिछले लगभग 200 वर्षों से दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं का आधार, भले वह समाजवादी हो या पूंजीवादी, अर्थशास्त्री रिकार्डो का ’तुलनात्मक लाभ का सिद्धांत’ रहा है। अंग्रेजी में यह ’थ्योरी ऑफ कम्पेरेटिव एडवांटेज’ के नाम से प्रचलित है। इसका सिद्धांत का आधार है कि प्रत्येक देश कुछ चुनिंदा चीजों का उत्पादन करें जिसमें उसे अन्य देशों की तुलना में कम लागत आती है। प्रत्येक देश अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादित हुई इन चीजों का विनिमय कर लें। इस प्रकार संसाधनों का सर्वश्रेष्ठ इस्तेमाल होगा और सभी फायदे में रहेंगे। इस प्रकार ’आत्मनिर्भरता’ और ’स्वदेशी’ की अवधारणा को रिकार्डो के सिद्धांत पर चलने वाले दुनिया के ज्यादातर अर्थशास्त्रियों ने नकार ही नहीं दिया बल्कि उन्हें अर्थशास्त्र में किसी भी सार्थक स्तर पर स्वीकार तक नहीं किया।
पिछले कुछ दिनों से पुन: भारत को आत्मनिर्भर बनाने का विषय चर्चा में है। चीनी वायरस के कारण दुनिया भर में जो आर्थिक स्थितियां बन गई हैं, उससे यह स्पष्ट हो गया है कि ’स्वदेशी’ का समय आ गया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक श्री मोहन भागवत ने 26 अप्रैल को देश भर में स्वयंसंवकों सहित संपूर्ण समाज को संबोधित करते हुए भारत को आत्मनिर्भर बनाने के यज्ञ में जुटने का आवाहन किया। इसके उपरांत 12 मई की शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी कोविड-19 के उपरांत उभर रही भारत की संभावित तस्वीर को स्वदेशी व आत्मनिर्भरता के संकल्प से जोड़ा। 13 मई को केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने 20 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज की पहली कड़ी के बारे में जानकारी देते हुए पुन: अपनी सरकार द्वारा लिए गए इस संकल्प को दोहराया कि भारत की आर्थिक नीतियां अब उसे आत्मनिर्भर बनाने पर केंद्रित होंगी।
’स्वदेशी’ व ’भारत की आत्मनिर्भरता’ एक ही सिक्के दो पहलू हैं। इस विषय में चर्चा हो रही है तो उसे चुनौती मिलना भी स्वाभाविक है क्योंकि जहां पश्चिमी अर्थशास्त्र की अवधारणाएं स्पष्ट रूप से परिभाषित हैं वहीं अब तक स्वदेशी अर्थशास्त्र के सिद्धांतों के बारे में बहुत ज्यादा चर्चा अपने यहां नहीं हुई।
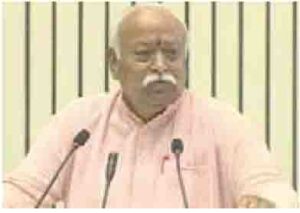 ऐसा नहीं है कि इस विषय पर काम नहीं हुआ या इन सिद्धांतों का निरूपण नहीं हुआ। पर जैसा अन्य क्षेत्रों में हाल है वैसा ही अर्थशास्त्र में भी है। पश्चिमी अर्थशास्त्र के सिद्धांतों में पले बढ़े अर्थशास्त्रियों ने ’स्वदेशी’ मॉडल का अध्ययन करने वाले अर्थशास्त्रियों को कभी भी मुख्यधारा में शामिल ही नहीं होने दिया। इसका सबसे दिलचस्प उदाहरण हैं नागपुर विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉ. एम. जी. बोकरे।
ऐसा नहीं है कि इस विषय पर काम नहीं हुआ या इन सिद्धांतों का निरूपण नहीं हुआ। पर जैसा अन्य क्षेत्रों में हाल है वैसा ही अर्थशास्त्र में भी है। पश्चिमी अर्थशास्त्र के सिद्धांतों में पले बढ़े अर्थशास्त्रियों ने ’स्वदेशी’ मॉडल का अध्ययन करने वाले अर्थशास्त्रियों को कभी भी मुख्यधारा में शामिल ही नहीं होने दिया। इसका सबसे दिलचस्प उदाहरण हैं नागपुर विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉ. एम. जी. बोकरे।
बोकरे घनघोर मार्क्सवादी चिंतक थे। अर्थशास्त्र की उनकी कक्षाएं कम्युनिस्टों के लिए भर्ती शिविर की तर्ज पर चलती थीं। पश्चिमी अर्थशास्त्र का उनका गहन अध्ययन था तथा गांधीवादी अर्थशास्त्र पर उनकी पुस्तक को इस विषय पर संदर्भ पुस्तक का दर्जा प्राप्त था। बोकरे की मित्रता प्रखर चिंतक व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक दत्तोपंत ठेंगड़ी से भी थी। ठेंगड़ी का भी इस विषय पर गहन अध्ययन था और वह 1960 के दशक से ही कह चुके थे कि दुनिया को न पूंजीवाद बचा सकता है न साम्यवाद। वह पंरपरागत ’मुक्त व्यापार’ के उस सिद्धांत को भी लगातार चुनौती दे रहे थे जिसके कारण दुनिया भर में शोषण में लगातार वृद्धि हुई तथा आर्थिक सुधारों के नाम पर गरीब और गरीब होता चला गया तथा अमीर और अमीर।
ठेंगड़ी ने बोकरे को प्रेरित किया कि वह हिंदू धर्मशास्त्रों का अध्ययन कर यह जानने का प्रयास करें कि वहां अर्थशास्त्र अथवा आर्थिक सिद्धांतों के बारे में कितनी जानकारी है तथा वर्तमान में ये जानकारी अथवा शास्त्रीय सिद्धांत कितने प्रासंगिक हैं। बतौर वामपंथी बोकरे ने हिंदू शास्त्रों का गहन अध्ययन आरंभ किया और कुछ ही समय में उनकी सोच ही बदल गई। अंतत: अथक परिश्रम के बाद उन्होंने 1990 के दशक के आरंभिक वर्षों में एक पुस्तक प्रकाशित की जिसका शीर्षक था ’हिंदू अर्थशास्त्र: एक अनवरत आर्थिक व्यवस्था’। इस पुस्तक में स्वदेशी मॉडल की बड़ी स्पष्ट रूपरेखा दी गई है। बोकरे ने कहा है कि यूरोप व अमेरिका के अर्थशास्त्री यह साबित करने का प्रयास करते रहे हैं कि भारत के पास अर्थशास्त्र की कोई प्राचीन परंपरा नहीं है और अर्थशास्त्र का जो भी ज्ञान उपजा वह पश्चिम में ही उपजा। लेकिन सच यह है कि एडम स्मिथ की ’वेल्थ ऑफ नेशन्स’ तथा डेविड रिकार्डो की ’प्रिन्सिपल्स ऑफ पोलिटिकल इकॉनॉमी’ प्रकाशित होने से हज़ारों वर्ष पहले ही भारत की प्राचीन स्मृतियों व वेदों में हर उस आर्थिक सिद्धांत के बारे में विस्तार से जानकारी है जिसकी किसी भी व्यक्ति, समाज या प्रशासन को आवश्यकता हो सकती है। ये सिद्धांत पश्चिम के अस्थायी सिद्धांतों की तुलना में कहीं ज्यादा स्थायी हैं और आज पहले से भी ज्यादा प्रासंगिक हैं। इसका एक उदाहरण बोकरे ने इस पुस्तक में एक अध्याय में दिया है जहां उन्होंने हिंदू अर्थशास्त्र के आधार पर पूरी तरह से करमुक्त बजट की अवधारणा का सैद्धांतिक ही नहीं व्यवहारिक निरूपण भी किया है।
बोकरे के अतिरिक्त स्वयं ठेंगड़ी द्वारा स्वदेशी मॉडल का विस्तार से निरूपण किया गया है। जिन्हें भी स्वदेशी मॉडल को लेकर किसी भी प्रकार की आशंका है उन्हें बोकरे व ठेंगड़ी की पुस्तकों व टिप्पणियों को पढ़ना व सुनना चाहिए। ठेंगड़ी ने ’थर्ड वे’ में स्पष्ट कहा है कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने का अर्थ यह नहीं है कि हम दुनिया भर से अपने को काट कर अलग-थलग कर लेंगे। ’स्वदेशी अर्थशास्त्र’ में कहा गया है कि हम सभी देशों से आर्थिक सहयोग करेंगे पर अपने हितों को सुरक्षित रखते हुए। उन्होंने इस संदर्भ में बिल्कुल स्पष्ट कहा, ”औद्योगिक क्रांति के समय संयोगवश कुछ ऐसी घटनाएं हुईं जिससे पश्चिमी जगत के राष्ट्रों को बहुत अधिक लाभ हुआ। इन घटनाओं में हवाई यातायात का युग आने से पहले समुद्री-मार्गों के भू-राजनीतिक महत्व में वृद्धि, कच्चे माल की बहुलता और प्रभावी विपणन क्षमता वाले देशों का अपने आंतरिक व्यापार और वाणिज्य के विकास में तल्लीन, नौ सैनिक शक्ति वाले राज्यों के लिए विशाल साम्राज्य निर्माण हेतु अनुकूल परिस्थितियों, उपनिवेशों के शोषण के आधार पर अपनी आंतरिक अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने की व्यावहारिकता आदि शामिल थे । लेकिन तीसरी दुनिया के देशों के लिए ऊपर गिनाई गई ये परिस्थितियां लौटकर आने वाली नहीं हैं। गोरे राष्ट्रों की सम्पन्नता और समृद्धि जिन तत्वों पर आधारित थी, वे अब अश्वेत राष्ट्रों को उपलब्ध नहीं होंगे। अत: पश्चिमी देशों की नकल करने और उन्हें अपना आदर्श, प्रतिमान मानने का कोई औचित्य शैष नहीं रह जाता।
पश्चिमी देशों के उदाहरणों की विफलता और ऐतिहासिक घटनाक्रम में स्पष्ट दिखाई देने वाली भिन्नता को ध्यान में रखकर विकास और प्रगति हेतु प्रयत्नशील सभी राष्ट्रों को अपने लिए नए लक्ष्यों का निर्धारण करना बहुत आवश्यक हो गया है। इसलिए अब हमें अपनी राष्ट्रीय संस्कृति, अपनी पुरानी परम्परा, वर्तमान आवश्यकताओं और भविष्य की आकांक्षाओं को ध्यान में रखकर अपनी प्रगति और विकास का प्रतिमान सुनिश्चित करना चाहिए। हमें पश्चिमी प्रतिमानों या उदाहरणों का गहराई से अध्ययन विश्लेषण करना चाहिए और यदि संभव हो तो उनसे लाभ भी उठाना चाहिए। लेकिन उन्हें अपने भावी विकास का आदर्श प्रतिमान मानने की गलती नहीं करनी चाहिए।
————