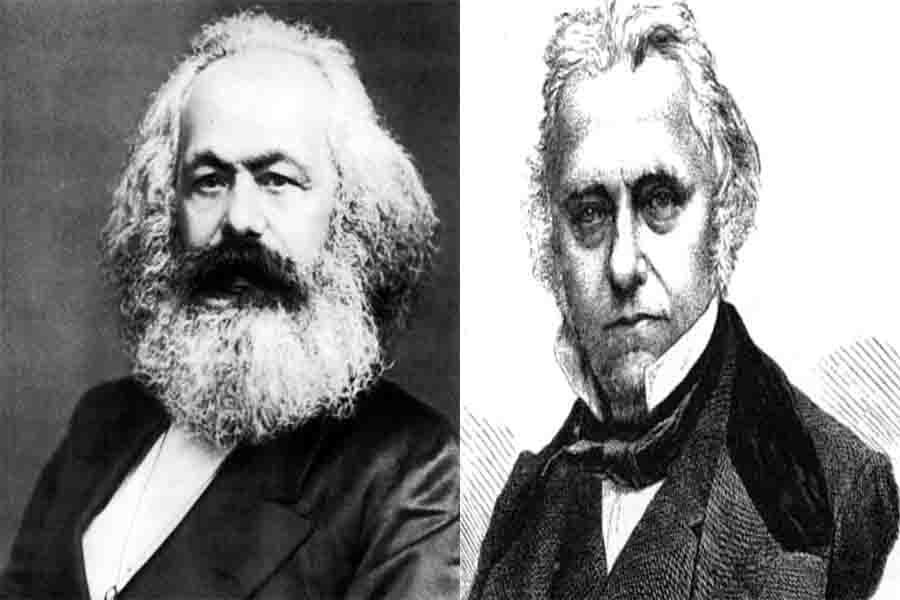कि सी देश में वैचारिक यथास्थितिवाद उसे प्रगतिगामी नहीं होने देता है| यह चिंतन और समझ को एक दायरे में बंधक बनाकर रखता है| आज़ादी के बाद भारत में कुछ ऐसा ही हुआ| औपनिवेशिक शासन का तो अंत हुआ परन्तु औपनिवेशिक संस्कृति सोच और समझ यथावत बनी रही| इसने लगभग तीन पीढ़ियों को स्वतंत्र चिंतन और अपनी मिट्टी की सुगंध को अभिव्यक्त करने नहीं दिया| यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है| स्वयं जवाहरलाल नेहरू ने जाने-अनजाने इस सच को स्वीकार किया था कि उन्होंने भारत को पश्चिम के प्रिज्म से समझा है| वे अकेले नहीं थे| आज़ादी के बाद कांग्रेस के भीतर जो राजनीतिक संस्कृति भारतीयता को प्राथमिकता देकर देश की शिक्षा एवं राजनीतिक संरचना को ढालना चाहती थी उसे नेहरू के जबर्दश्त विरोध का सामना करना पड़ा| उन्होंने सत्ता का उपयोग वैकल्पिक सांस्कृतिक और वैचारिक धारा को समाप्त करने के लिए किया| १९५० के दशक में कांग्रेस के भीतर जो सत्ता संघर्ष था वह सिर्फ कुर्सी की ही लड़ाई नहीं थी बल्कि दो सांस्कृतिक धाराओं की भी लड़ाई थी| इसी मुकाम पर नेहरू ने बौद्धिकता के क्षेत्र में मैकालेवादी औपनिवेशिक अवशेष एवं मार्क्सवादियों के साथ वैचारिक त्रिवेणी बना ली| दूसरी तरफ उन्होंने कांग्रेस के भीतर डॉ. राजेन्द्र प्रसाद, एन.वी. गाडगील, पुरूषोत्तम दास टंडन, शंकरराव देव एवं कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी जैसे चिंतक-नेताओं को हाशिए पर डालने का काम किया| इसका सबसे अच्छा उदाहरण सोमनाथ मंदिर के निर्माण के प्रश्न पर नेहरू, राजेन्द्र प्रसाद और मुंशी के बीच का पत्राचार है| जहां मुंशी सोमनाथ मंदिर के निर्माण को भारत की सामूहिक चेतना की अभिव्यक्ति मानते थे, वहीं नेहरू गज़नी और गौरी के द्वारा ध्वस्त मंदिर के पुनर्निर्माण को सांप्रदायिक मानते थे| नेहरू अपने व्यवहार में कितने अधिनायकवादी थे वह एक दूसरे उदाहरण से पता चलता है| उन्होंने कांग्रेस के निर्वाचित अध्यक्ष पुरूषोत्तमदास टंडन को पद त्यागने के लिए बाध्य कर दिया था| वे कैसे लोकतांत्रिक थे यह इस बात से पता चलता है कि वे संघ के किसी भी व्यक्ति की योग्यता के बावजूद किसी भी पद पर नियुक्ति को रोकने के लिए अपने पद की गरिमा का ख्याल किए बिना कूद पड़ते थे| इस बात की पुष्टि इस उदाहरण से होती है| नेहरू द्वारा यह सवाल उठाए जाने पर कि पंजाब के एक विश्वविद्यालय में संघ से जुड़े एक शिक्षाविद् की नियुक्ति उपकुलपति के रूप में हुई है| पंजाब के तत्कालिन प्रधान मंत्री (तब मुख्यमंत्री को प्रधान मंत्री कहा जाता था) गोपीचंद भार्गव (१९४७-५१) ने १४ फरवरी, १९४८ को उन्हें जवाब में लिखा, आपने यह कैसे समझ लिया कि आरएसएस से जुड़े किसी वयक्ति को मैं उपकुलपति नियुक्त कर दूंगा? इस प्रकार देश में एक ऐसी बौद्धिक जमात को राज्य के संरक्षण में जन्म दिया गया जो राष्ट्रवाद, भारतीय संस्कृति, देश की सांस्कृतिक और बौद्धिक विरासत की बात करने वालों को ‘प्रतिक्रियावादी’, ‘फासीवादी’ और ‘साम्प्रदायिक’ घोषित करते रहे| इसका प्रमाण नेहरू खानदान के संरक्षण में सत्ता के द्वारा सक्रिय सहयोग से सुभद्रा जोशी के द्वारा स्थापित साम्प्रदायिकता विरोधी कमेटी था, जिसका एकमात्र उद्देश्य राष्ट्रवादी संगठनों के विरूद्ध दुष्प्रचार करना था| इस प्रकार वैचारिक कट्टरता के आधार पर विश्वविद्यालय परिसरों, मीडिया और सार्वजनिक विमर्शों को इसी जमात के लोगों ने बंधक बना लिया| अकादमिक स्वतंत्रता और वैकल्पिक सोच को हर तरह से दबाया जाता रहा| तभी तो आज़ादी के सात दशकों के बाद भी शिक्षा एवं संस्कृति, राजनीतिक संरचनाएं यूरोप केन्द्रित हैं| भारत के समाज विज्ञान में भारत ही लुप्त है| भारत की ज्ञान परंपरा को अछूत बना दिया गया| तभी तो असम के शंकर देव, महाराष्ट्र के समर्थ रामदास, कश्मीर के अभिनव गुप्त उनके प्रांतों से बाहर के छात्रों के लिए अजनवी नाम हैं|
लेकिन भारत की बौद्धिक उर्वरा भूमि न तो उपनिवेशवाद के दमन से, न ही उससे पहले मुगलों की बर्बरता से और न ही मैकाले और मार्क्स पुत्रों की वैचारिक कट्टरता से बंजर भूमि बनी| उपनिवेशवाद के दौरान लाल, बाल, पाल, महर्षि अरविन्द, राज नारायण बसु सिर्फ भौगोलिक एवं राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए नहीं लड़ रहे थे बल्कि भारत की अस्मिता, इसकी अपनी संस्कृति, इसकी बौद्धिक परम्परा को लेकर आगे बढ़ रहे थे| आज़ादी के बाद तमाम दमनकारी उपक्रमों के बावजूद भारत के धरोहर को वर्तमान और भविष्य से जोड़ने के लिए बौद्धिक एवं राजनीतिक प्रयास जारी रहा| उपेक्षा, उलाहना और दमन को बर्दाश्त करते हुए वैकल्पिक विचार अस्सी के दशक के बाद विभिन्न रूपों में प्रकट होने लगे| २०१४ में सत्ता परिवर्तन वैचारिक अधिष्ठान का भी परिवर्तन था| भारत में सत्ता के संरक्षण में पले-बढ़े बौद्धिकों को भले ही इसका आभास देर से हुआ परन्तु ब्रिटेन के बौद्धिकों ने इस परिवर्तन के सार तत्व को समझ लिया था| तभी तो ब्रिटेन के अखबार गार्जियन ने १८ मई, २०१४ को अपने सम्पादकीय में लिखा था, आज १८ मई, २०१४ इतिहास में इस बात के लिए जाना जाएगा कि ब्रिटेन ने अंतत: भारत छोड़ दिया| इसको स्पष्ट करते हुए सम्पादकीय में कहा गया, नरेन्द्र मोदी की चुनाव में जीत उस युग का अन्त है जिसमें भारत में राजनीतिक संरचना ब्रिटेन के शासन के दौरान की संरचना से बहुत अधिक भिन्न नहीं थी| कांग्रेस शासन के दौरान भारत बहुत अर्थों में अंग्रेजी शासन की ही निरंतरता थी|
यह टिप्पणी कई अर्थों में असाधारण है| ब्रिटिश अखबार ने स्वीकार किया कि भारत की पुरानी राजनीति ने वैचारिक परतंत्रता को अपने भीतर आत्मसात कर लिया था| यह इस हद तक था कि उसमें ब्रिटेन की औपनिवेशिक शैली की निरंतरता साफ झलकती थी| वैचारिक परजीवियों ने राजनीतिक संरचना और दर्शन को यूरोप की कार्बन कॉपी बना दिया| अपनी विरासत के प्रति अलगाव व यूरोपीय मन-मस्तिष्क-मानसिकता से लगाव की जो संस्कृति पीढ़ी-दर-पीढ़ी पैदा की गई थी, उसने भारत के अभिप्राय को देशज से विदेशज बना दिया|
मौलिक विचारों में स्थापित विचार को तहस-नहस कर देने की क्षमता होती है| ऐसा करते समय मौलिकता को अनेक प्रकार के आरोप-प्रत्यारोप एवं आघात से गुजरना पड़ता है| परन्तु उसमें वैचारिक यथास्थितिवाद को समाप्त करने की क्षमता बढ़ती ही जाती है| ऐसा ही २०१४ के बाद हुआ| जब भारत के इतिहास की पुस्तकों, समाज विज्ञान एवं सार्वजनिक विमर्शों में भारतीयता का भाव उभरने लगा तब वैचारिक कट्टरपंथियों ने अपनी पूरी ताकत इस मौलिक विचार के उभार को रोकने में लगा दी| उन्होंने कुछ घटनाओं को सामने रख कर जिनमें साहित्यकार कलबुर्गी, कम्युनिस्ट नेता पानसारे और अखलाक की हत्या को लेकर पूरे देश में मुहिम छेड़ दी| इन हत्याओं का मोदी सरकार या विचारधारा से कोई सम्बंध नहीं था| परन्तु उनकी मुहिम इन घटनाओं के प्रति न होकर राष्ट्रवादी विचार और सांस्कृतिक उभार के प्रति थी| ये वही लोग थे जिन्होंने लोकसभा चुनाव से पहले ८ अप्रैल, २०१४ को जनसत्ता में अपील जारी की थी कि ‘फासीवादी’, ‘नस्लवादी’ और ‘साम्प्रदायिक’ नरेन्द्र मोदी को मतदान न करें| इस उपक्रम में उन्हें भारत विरोधी श्वेत बुद्धिजीवियों का भी सहारा मिला| न्यूयॉर्क टाइम्स के १९ सदस्यीय सम्पादकीय मंडल ने भारत के मतदाताओं से इसी प्रकार की अपील जारी की थी| उधर ब्रिटेन के द गार्जियन ने भी ऐसी ही अपील अपने अखबार में प्रकाशित की थी| पर ये सभी निष्प्रभावी हुए|
ये वे लोग हैं जो अपने मन और प्रशिक्षण से स्टालिनवादी और माओवादी हैं| इनका एक इतिहास रहा है| इनके जमात में भी जिन लोगों ने इनके प्रति असहमति जाहिर की उन्हें अपमानित करने और मिटा देने में इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी|
हिंदी साहित्य में त्रिलोचन जी एक बड़ा नाम हैं| वे सोच से वामपंथी थे| उनका घोर अपमान और दमन अपने ही विचारधारा के साहित्यकारों द्वारा इस हद तक किया गया कि उन्हें दिल्ली शहर छोड़ना पड़ा| रामविलास शर्मा दूसरा बड़ा नाम है| वे भी मार्क्सवादी थे| परन्तु भारतीय संस्कृति के प्रति जब उनका रूझान बढ़ने लगा तब उनके साथ क्या व्यवहार किया गया, यह किसी से छिपा नहीं है| संवेदना के प्रति ये कितने जागरूक हैं इसका उदाहरण अवार्ड लौटाने वाले अशोक वाजपेयी का वह कथन है, जो उन्होंने भोपाल में यूनियन कार्बाइड के गैस त्रासदी के बाद कहा था| तब हजारों लोग मारे गए थे| उस वक्त वाजपेयी अंतरराष्ट्रीय काव्य सम्मेलन करा रहे थे| संवेदनशील लोगों ने उसे स्थगित करने की अपील की तो वाजपेयी ने कहा, ‘मुर्दों के साथ रचनाकार नहीं मरते|’ जिस सफदर हाशमी की हत्या कांग्रेस शासन में खुलेआम हुई वही ‘सहमत’ कांग्रेस सरकार से लाखों का अनुदान लेता रहा|
जो समाज लम्बे समय तक विदेशी विचार, भाषा और संस्कृति के अधीन रहने के लिए बाध्य होता है उसका बौद्धिक नेतृत्व आलसी, परजीवी और सुविधाभोगी बन जाता है| उसमें नए सिरे से ज्ञान परम्परा को पुनर्स्थापित करने की इच्छाशक्ति और ऊर्जा दोनों ही नहीं होती है| ऐसा ही भारत के अधिकांश बौद्धिकों के सम्बंध में कहा जा सकता है| वे पश्चिम के संदर्भ, सोच, समझ से बाहर नहीं निकल पाते हैं| उनके लिए धर्मपाल जैसे चिंतकों का प्रयास अर्थहीन और देश को पीछे धकेलने वाला होता है| धर्मपाल जी ने भारत की ज्ञान परम्परा की श्रेष्ठता को स्थापित करने का काम किया| अपने शोध के द्वारा उन्होंने ब्रिटिश रिकॉर्ड के आधार पर बताया कि १ जुलाई, १८३६ में कलेक्टर के द्वारा दिए गए सर्वे रिपोर्ट में कहा गया कि मद्रास के २१ जिलों में ११,५७५ स्कॉलर्स, १,५७,१९५ छात्र और उच्च शिक्षा के १०९४ संस्थाएं थीं| क्या यह जानकारी भारत के बच्चों के मन में स्वाभिमान पैदा करेगी या हीन भावना?
बौद्धिक आतंकवादी इन सब श्रेष्ठताओं को मिटा देना चाहते थे| तभी तो वे सिख गुरू तेगबहादुर को इतिहास की पुस्तक में ‘लुटेरा’, शिवाजी महाराज को ‘शोषक’ एवं शहीद भगत सिंह को ‘आतंकवादी’ बता कर छात्रों को पढ़ाते रहे| आज मौलिकता का स्वर उन्हें परेशान कर रहा है और वे आत्मालोचन एवं प्रायश्चित करने की जगह इस राजनीतिक वैचारिक परिवर्तन के खिलाफ जिहादी बन कर बौद्धिक उत्पात मचा रहे हैं|
इन बौद्धिकों के पास इस प्रश्न का उत्तर नहीं है कि बंकिम का ‘आनंदमठ’, स्वामी दयानंद का ‘सत्यार्थ प्रकाश’, वीर सावरकर का ‘हिन्दुत्व’, तिलक का ‘गीता रहस्य’, बिपिनचन्द्र पाल का ‘न्यू इंडिया’ और महर्षि अरविंद का दर्शन भारतीय विश्वविद्यालयों व शोध संस्थाओं में अध्ययन के विषय क्यों नहीं बन पाए? पचास वर्षों से यह साहित्य अघोषित रूप से ‘प्रतिबंधित’ रहा है| क्या यह एक दु:खद आश्चर्य नहीं है कि स्वामी विवेकानंद को विश्व धर्म संसद (शिकागो, १८९३) में अपने जिस भाषण के लिए श्रेष्ठ, कुशाग्र एवं उच्च दर्जे का संन्यासी-विद्वान घोषित किया गया था और जिसके कारण औपनिवेशिक युग में भारत को प्रतिष्ठा प्राप्त हुई थी, आज तक वह भाषण भारतीय पाठ्यक्रम का अंग नहीं बन पाया? लेकिन शायद उन्हें पता नहीं है कि राष्ट्र का भी भाग्योदय होता है और आज भारत वर्ष अपने वर्तमान को विरासत से जोड़ कर एक नए स्वर्णिम भविष्य को दस्तक दे रहा है| वैचारिक जंग का जारी रहना अस्वाभाविक नहीं है| परन्तु हिंदी के महान कवि सूर्यकांत त्रिपाठी ‘निराला’ ने जो भगवान श्री राम के लिए कहा था वह पंक्ति भारत के राष्ट्रवादी चिंतन धारा के लिए उपयुक्त है- होगी जय, होगी जय, हे पुरूषोत्तम नवीन|