धर्म-अर्थ-काम व मोक्ष पुरुषार्थ की भारतीय संस्कृति के हरेक अंग एक दूसरे के पूरक हैं, सहायक हैं। उस संस्कृति के अंतर्गत जगवत्सल हमारे ऋषि-मुनियों द्वारा निर्मित व्यवस्थायें प्रकृति के साथ सुसंगत हैं, साधन-शुद्ध हैं, साध्य शुद्ध है, सचराचर जगत के लिए अभय-प्रदाता है, अहिंसक हैं।
भारतीय संस्कृति का एक अनन्य तत्व है- गाय व संपूर्ण गौवंश। गाय को मानव दृष्टि की माता का स्थान दिया गया है। गाय की कल्पना जन मानस में किसी पशु के रुप में नहीं है। ऐसा कहा जा सकता है कि ‘इट इज ए क्रिएचर ऑफ इट्स ओव्न अनपॅरालालेड क्लास।’ पौराणिक कथा के अनुसार सुर-असुर संग्राम के बाद समुद्र मंथन में जो अनेक अमूल्य नीधियाँ निकली उनमें से गाय एक वरदान स्वरुप भेंट जगत को मिली। यह कामधेनु मानव की सभी जरुरतें पूरी करने की क्षमता रखती है और इतिहास साक्षी है कि जब तक प्रजा ने गाय और गौवंश का जतन किया है, तब तक गौमाता ने भी प्रजा के लिये समृद्धी की लहरें सर्जित की हैं।
इस देश का दुर्भाग्य रहा कि उसे पश्चिम की अनात्मवादी अपसंस्कृतिका आक्रमण झेलना पड़ा और यह आक्रमण प्रत्यक्ष गुलामी का काल पूरा होने के बाद भी आज भी चालू है। इस आक्रमण का भोग गाय और गौवंश बना है। विशाल पैमाने पर गौवंश की कतल हो रही है, जो कि वास्तव में इस देश के सौभाग्य की कतल है।
वर्तमान में पर्यावरण सुरक्षा एक विकट समस्या बन गयी है। ग्लोबल वॉर्मिंग की गंभीर असर से विश्व चिंतित है। किंतु कोई यह स्वीकार करने को तैयार नहीं कि जो फसल हमने बोई उसी को काटने को हम विवश हैं। समस्या से निपटने के लिये तरह-तरह के सुझाव दिये जाते हैं, आंतरराष्ट्रीय गोष्टियाँ, सेमिनार होते हैं, अबजों रुपये की पर्यावरण सुधार योजनाएं बनती हैं, ‘कार्बन क्रेडिट’ नामक स्वांग बनाया जाता है, फिल्में बनती हैं, तृतीय विश्व के कमजोर राष्ट्रों को धमकाया जाता है, इत्यादि इत्यादि। किंतु जब तक आधुनिक स्वरुप के विकास का भूत कब्जा जमाये बैठेगा तब तक पर्यावरण समस्या का कोई कारगर उपाय नहीं होगा।
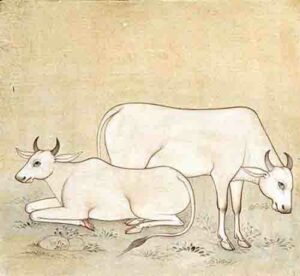 संस्कृति के सर्वश्रेष्ठ विश्वगुरु भारत के पास इसका उपाय है, नया नहीं पर युगों युगों से आजमाया हुआ उपाय है और वह है- गौसंरक्षण।
संस्कृति के सर्वश्रेष्ठ विश्वगुरु भारत के पास इसका उपाय है, नया नहीं पर युगों युगों से आजमाया हुआ उपाय है और वह है- गौसंरक्षण।
भारत के पास विश्व प्रसिद्ध 26 गौवंश प्रजातियाँ थीं। ‘थीं’ इसलिये कि उसमें से कई लुप्त हो गई हैं, कई लुप्त प्राय हैं और जो बची हैं वह अपने मूल स्वरुप से बहुत कमजोर हालत में हैं। उन 26 प्रजातियों को तीन मुख्य भागों में विभाजित किया जा सकता है- एक प्रचुर दूध देने वाली प्रजातियाँ, दो-खेतो और वाहन व्यवहार में खूब मेहनत कर सकनेवाली प्रजातियाँ और तीन- इन दोनों का संगम अर्थात ठीक-ठीक दूध देने वाली व ठीक-ठीक श्रम करनेवाली प्रजातियाँ।
गौवंश संरक्षण पर्यावरण की रक्षा कैसे कर सकता है उसका विचार करें। गाय का दूध इस धरती का अमृत है। प्रजा के स्वास्थ्य की वह बीमा-पॉलिसी है। आयुर्वेद तो गाय के दूध, पंचामृत और घी को स्वास्थ्य की चाबी युगों से मानता ही है। आधुनिक वैज्ञानिक संशोधन भी भारतीय गाय के दूध के गुणों को स्वीकारने लगा है। परंतु भारतीय अर्थ व्यवस्था में तो गौवंश का सबसे महत्वपूर्ण प्रदान उसके गोबर को माना गया है और इसी गोबर में पर्यावरण की रक्षा की चाबी छुपी है।
गाय एक चलती फिरती डेयरी है, चलती फिरती खाद की फेक्टरी है, चलती फिरती सिमेंट की फेक्टरी है और इसके अलावा अन्य कई आनुषंगिक उद्योगों की भी फेक्टरी है।
आधुनिक उद्योग-निरपवाद रुप से- प्रदूषण के सर्जक हैं। फिर चाहे वह वायु का प्रदूषण हो, जल का प्रदूषण हो, भूमि का प्रदूषण हो या प्रजा के मानस को दूषित करने वाला वैचारिक या चारित्रिक प्रदूषण हो। इसके विरुद्ध गौवंश मानव सृष्टि की सभी आवश्यकताएं किसी भी प्रदूषण के बिना पूरी कर सकता है।
भारतीय कृषि परंपरा में गौवंश का गोबर युगों से खाद के रुप में प्रयुक्त होता आया है। गौवंश से ‘बाय प्रोडक्ट’ के रुप में, बोनस के रुप में, किसान के अपने द्वार पर, किसी खर्च के बिना, हर चौबीस घंटों में मिलने वाला गोबर कृषि भूमि को सर्वश्रेष्ठ पोषण प्रदान कर प्रचुर मात्रा में अन्न उगाने में कारणभूत बनता आया है। किसी भी तरह के प्रदूषण के बिना, पर्यावरण को कोई हानि पहुँचारे बिना पौष्टिक व शुद्ध अनाज पैदा करने में यह प्राकृतिक खाद मूल्य सेवा देता था। आज गौवंश की अंधाधूंध कत्ल के कारण गोबर की खाद की बेहद कमी हो गई है। विकल्प के रुप में किसानों के सर रासायनिक खाद थोप दिया गया है। रासायनिक खाद बनाने वाले कारखाने प्रदूषण के बहुत बड़े सर्जक हैं। रासायनिक खाद का उत्पादन ही नहीं, खेतों में उसका उपयोग भी महा प्रदूषक है। यह खाद कृषि की भूमि को प्रदूषित करती है, जमीन में गहराई तक जा कर उसके रसायन भूगर्भ जल को प्रदूषित करते हैं, खेत में बिखेरने पर वायु प्रदूषित होती है और उसके उपयोग से उत्पन्न अनाज भी प्रदूषित होता है। इस तरह रासायनिक खाद प्रदूषण की लंबी परंपरा का निर्माण करती है। रासायनिक खाद के आर्थिक बोझ की, या अनाज में पौष्टिकता की कमी से होने वाले रोगों के उपचार के आर्थिक बोझ की तो हम चर्चा ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि लेख का विषय पर्यावरण तक सीमित है।
कृषि के क्षेत्र में ही आगे चलें। एक महत्व की क्रिया है कीट नियंत्रण। गौवंश के मूत्र और गोबर का घोल बनाकर उसमें नीम के पत्ते, नीम के फल व अन्य वनस्पतियाँ मिलाकर बनाया जाने वाला कीट नियंत्रक भारतीय किसान की अपनी अप्रतिम सूझबूझ से पैदा किया गया उपाय है। आधुनिक कृषि ने कारखानों में बनने वाले अत्यंत जहरीले कीट नाशक अपनाये। कातिल जहरीले रसायनों से बनाये जाने वाले ये कीट नाशक उनकी उत्पादन प्रक्रिया के दौरान ही भयंकर प्रदूषण फैलाते हैं। उनके उत्पादन से जुड़े मजदूरों को धीमी मौत देते हैं और जब ये कीट नाशक खेतों में अनाज सब्जियों और फलों पर छीटे जाते हैं तब ये उनको प्रदूषित ही नहीं, जहरीले भी बनाते हैं। छिटकाव की क्रिया के दौरान वायू को प्रदूषित करते हैं। यह जहर जमीन पर गिरकर जमीन को और भीतर जाकर भूगर्भ जल को प्रदूषित करता है। कीट नाशक छीटने वाला व्यक्ति भी अपनी सांस द्वारा यह जहर अपने शरीर में पहुंचाता है और अनेक भयानक रोगों का भोग बनता है। माताओं के स्तन के दूध में और गाय तथा अन्य पशुओं के दूध में भी कीट नाशक जहर के अंश पाये गये हैं। इन जहरीले कीट नाशकों के आर्थिक बोझ की तो हम बात ही नहीं कर रहे। ये कीट नाशक ढाई से तीन हजार रुपये लीटर के दाम से बिकते हैं।
 गोबर के उपयोग की एक महत्वपूर्ण बात करनी रह गई और वह है गोबर गैस का उत्पादन। गोबर गैस के बारे में हम सभी जानते ही हैं। यह गैस एक वैकल्पिक उर्जा तो है ही, गोबर गैस प्लांट से निकलने वाली ‘स्लरी’ एक उत्कृष्ट खाद है, और पूर्णतया प्रदूषण मुक्त।
गोबर के उपयोग की एक महत्वपूर्ण बात करनी रह गई और वह है गोबर गैस का उत्पादन। गोबर गैस के बारे में हम सभी जानते ही हैं। यह गैस एक वैकल्पिक उर्जा तो है ही, गोबर गैस प्लांट से निकलने वाली ‘स्लरी’ एक उत्कृष्ट खाद है, और पूर्णतया प्रदूषण मुक्त।
गोबर का तीसरा महत्वपूर्ण उपयोग देखें। भारत के ग्रामीण विस्तारों में गारे-मिट्टी के मकान ही ‘सस्टेनेबल/अफोर्डेबल हाउसिंग’ दे सकते हैं और युगों युगों से एसे ही मकान जो ‘इको फ्रेंडली’ भी हैं, बनाये जाते रहे हैं। गारे मिट्टी के मकान बनाने में मुख्य घटक गाँव के तालाब की मिट्टी और गौवंश का गोबर है। गोबर ‘‘बोन्डिंग’’ का काम करता है जो आधुनिक गृह निर्माण के विज्ञान में सिमेन्ट का काम है। गोबर का उपयोग सर्वथा बिन प्रदूषक है जबकि सिमेन्ट के कारखाने कितने प्रदूषक होते हैं वह हम सभी जानते हैं। अनमोल प्राकृतिक संपदाओं का अंधाधुंध उपयोग करके बनायी जाने वाली सिमेन्ट, सिमेन्ट कारखानों में काम करने वाले मजदूरों को धीमी मृत्यु के मुँह में ढकेलती है और कारखाने के आसपास के 10-20 मील के विस्तार को अतिशय प्रदूषण से भर देती हैं। सिमेन्ट उद्योग शोषण व मुनाफाखोरी का कैसा गढ है, उस बात को अभी जाने दें। सिर्फ घर बनाने में ही नहीं, घर के रख-रखाव में, घर की मरम्मत में भी-मामूली मजदूरी या घर के मालिक के स्वयं के श्रम के अलावा बिल्कुल मुक्त में गोबर उपयोगी बनता है और वह भी एकदम प्रदूषण मुक्त तरीके से।
गौवंश के तो अनन्त उपकार हैं और गोबर के अगणित उपयोग हैं। इसी क्रम में और भी आगे बढें।
गोबर का एक महत्वपूर्ण उपयोग ईंधन के रुप में है। गौवंश का कोई भी वयस्क पशु रोज 12 से 15 किलो गोबर देता है। ग्रामीण घरों की स्त्रीयाँ इस गोबर से घर के बाडे में कंडे बनाती हैं जो सूर्य की गरमी में 2-3 दिन में सूख जाते हैं। वर्षा ऋतु के लिए ऐसे कंडों का संग्रह कर लिया जाता है। इन कंडो का उपयोग रसोई पकाने के लिए ईंधन के रुप में किया जाता है। मुक्त मिलने वाले इस ईंधन का उत्पादन सर्वथा प्रदूषण मुक्त है, जबकि पेट्रोलियम उत्पादों आधारित ईंधन-मिट्टी का तेल या रसोई-गैस के उत्पादन के साथ जुड़े प्रदूषण के बारे में तो हम जानते ही हैं। इस लेख में आर्थिक पक्ष की चर्चा नहीं कर रहे। किन्तु पुख्ता गणित के आधार पर गोबर के ईंधन की तुलना अन्य ईंधनों की कीमत से करें तो वह वार्षिक एक लाख करोड़ रुपये जितनी होती है। इस एक लाख करोड़ रुपये की बचत तो होती ही है, साथ ही प्रदूषण से मुक्ति मिलती है और पर्यावरण की भी सुरक्षा होती है।
गोबर का ईंधन के रुप में उपयोग करने से ईंधन के लिए काटे जाने वाले जंगल की रक्षा होती है। पर्यावरण चक्र में जंगलों का महत्व समझाने की आवश्यकता नहीं है। एक पशु के गोबर से बनने वाले कंडे, ईंधन के लिये काटे जाने वाले 6 वृक्षों को बचाते हैं। एक पूर्ण विकसित वृक्ष एक वर्ष में 15 लाख रुपये की कीमत का तो मात्र ऑक्सीजन देता है। जरुरी हिसाब लगाकर पशु का गोबर कितनी कीमत के पर्यावरण की रक्षा करता है वह गिनती हम पाठकों पर छोड़ते हैं।
पर्यावरण रक्षक गौवंश के साथ और आगे बढें। गोबर के ईंधन का उपयोग कर रसोई बना ली। चूल्हा ठंडा हुआ। चूल्हे में राख बची। यह राख भी निरुपयोगी नहीं है। इस राख से हमारी दादी-नानी ने युगों से घर के बरतन साफ किये हैं। पानी की कमी ही क्यों न हो! पहले थोड़ी गीली राख से और फिर सूखी राख से ताँबे-पितल के बरतन ऐसे चमचमाते साफ होते थे जैसे दर्पण हों। आज राख के स्थान पर क्लिनिंग पावडर या ‘लिक्विड सोप’ का उपयोग होता है जिसमें बहुत पानी की जरूरत पडती है और ये चीजें गृहिणी के हाथ की त्वचा और पर्यावरण दोनों को हानि पहुँचाती है। इनकी बिक्री के लिये करोड़ों रुपये विज्ञापन पर खर्च होते हैं। गंदे पानी के साथ बहकर यह क्लिनिंग पावडर कही जमता है और वहाँ की मिट्टी को बिगाड़ता है, जबकि राख तो मिट्टी के साथ मिलकर एक जीव हो विलय हो जाती है।
पर्यावरण की दृष्टि से राख का एक और उपयोग देखें। गाँवों में खेती की दृष्टि से संभाव्य कमजोर वर्षों के लिये की जाने वाली व्यवस्था के अन्तर्गत स्थायी रुप से हर घर में 2-3 वर्ष चले इतने अनाज का संग्रह मिट्टी की बनी बड़ी बड़ी कोठियों में किया जाता था। यह कोई जमाखोरी नहीं थी, अपितु समझदारी भरी सावधानी थी। मिट्टी की कोठी अपने आप में एक ‘इको फ्रेंडली कन्टेनर’ है। इनमें अनाज भरते समय कोई कीड़े या अन्य जीव न हों इसके लिये अनाज में कंडे की राख मिलाई जाती। राख अनाज से नमी को सोख लेती और अनाज सूखा रहने से उसमें कीड़े पैदा नहीं होते। कोठी का मुँह गोबर से बंद कर दिया जाता और कोठी ‘एयर-टाईट’ हो जाती। इतनी सुंदर पेकिंग व भंडारण व्यवस्था के सामने आधुनिक टेट्रा पेकिंग अथवा वातानुकूलित भंडार घर भी ओछे पड़ेगें।
राख के बदले अब प्रिझर्वेटिव का उपयोग होता है जिनमें केमिकल्स का प्रयोग होता है। अनाज में रखने के लिये गोलियाँ बनती हैं, जो अगर गलती से अनाज के साथ पिस जायें तो स्वास्थ्य के लिये खतरनाक हो सकता है। और फिर केमिकल्स आधारित किसी भी वस्तु का उत्पादन पर्यावरण को दूषित करता ही है। आर्थिक पहलू की हम फिर चर्चा नहीं करेंगें। हमारी कोठियाँ मुफ्त में बनती थीं ओर हमारी राख भी हमें मुफ्त में मिलती थी।
राख के अन्य भी उपयोग हैं। आयुर्वेद में कई चर्म रोगों के लिये त्वचा पर राख मलने का प्रयोग बताया है। राख एक उत्तम ‘डीजीन्फेक्टटन्ट’ है। आज की पीढी राख को हीन दृष्टि से देखती है। एलोपेथी राख के औषधीय गुणों को नहीं मानती और उसके बदले चर्म रोगों के लिये महंगी क्रीम व गोलियाँ देती हैं। ये क्रीम पर्यावरण के साथ कितनी सुसंगत हैं यह संशोधन का विषय है। भगवान शिव ने अपने शरीर पर भस्म धारण कर राख के महत्व को जगत के समक्ष उजागर किा है।
 राख का पर्यावरणलक्षी एक और उपयोग देखें। ग्रामीण रहन-सहन में घर के पीछे बाड़े के एक कोने में छाती जितनी ऊंचाई के, गारे-मिट्टी की दीवाल के, किन्तु बिना छत के खुले पाखाने बनाये जाते थे। वैसे तो दिन के प्रथम मल त्याग के लिये लोग सूर्योदय से पहले लोटे में पानी लेकर खेतों में जाते थे। दिन व रात में उपयोग के लिये तथा बीमार व्यक्ति के लिए घरों के पाखाने होते थे। इनमें मल त्याग के बाद हर बार दो-चार मुठ्ठी राख डाली जाती थी। एसा करने से दुर्गंध रुक जाती। राख मल की नमी को सोख लेती और मल काफी हद तक सूखा हो जाता। मल ढक जाने से मक्खी-मच्छर भी नहीं होते। पाखाने की छत नहीं होने से सूर्य के प्रखर ताप से मल पूरा सूख जाता और दूसरे दिन उसे टोकरे सें इकट्ठा करके खेतों में बिखेर दिया जाता व अत्यंत ऊँचे दर्जे की खाद का काम करता। चीन में तो आज भी पूरे देश का मल खाद में रुपांतरित करके खेतों में उपयोग किया जाता है। इस पूरी व्यवस्था में कंही भी पानी का जिक्र आया? आज राष्ट्रीय स्तर पर रोज का अबजों लीटर पानी पाखानों के फ्लश में बहाया जाता है। पानी की कमी दिन-ब-दिन बढती जा रही है और वह एक गंभीर पर्यावरणीय समस्या बन गई है। इस स्थिति में यह पुरानी व्यवस्था, जिसके मूल में गाय है, कितनी सुसंगत है!
राख का पर्यावरणलक्षी एक और उपयोग देखें। ग्रामीण रहन-सहन में घर के पीछे बाड़े के एक कोने में छाती जितनी ऊंचाई के, गारे-मिट्टी की दीवाल के, किन्तु बिना छत के खुले पाखाने बनाये जाते थे। वैसे तो दिन के प्रथम मल त्याग के लिये लोग सूर्योदय से पहले लोटे में पानी लेकर खेतों में जाते थे। दिन व रात में उपयोग के लिये तथा बीमार व्यक्ति के लिए घरों के पाखाने होते थे। इनमें मल त्याग के बाद हर बार दो-चार मुठ्ठी राख डाली जाती थी। एसा करने से दुर्गंध रुक जाती। राख मल की नमी को सोख लेती और मल काफी हद तक सूखा हो जाता। मल ढक जाने से मक्खी-मच्छर भी नहीं होते। पाखाने की छत नहीं होने से सूर्य के प्रखर ताप से मल पूरा सूख जाता और दूसरे दिन उसे टोकरे सें इकट्ठा करके खेतों में बिखेर दिया जाता व अत्यंत ऊँचे दर्जे की खाद का काम करता। चीन में तो आज भी पूरे देश का मल खाद में रुपांतरित करके खेतों में उपयोग किया जाता है। इस पूरी व्यवस्था में कंही भी पानी का जिक्र आया? आज राष्ट्रीय स्तर पर रोज का अबजों लीटर पानी पाखानों के फ्लश में बहाया जाता है। पानी की कमी दिन-ब-दिन बढती जा रही है और वह एक गंभीर पर्यावरणीय समस्या बन गई है। इस स्थिति में यह पुरानी व्यवस्था, जिसके मूल में गाय है, कितनी सुसंगत है!
यह तो गौवंश द्वारा प्रदत्त गोबर व मूत्र की बात हुई। गौवंश के प्रत्यक्ष प्रदान की तरफ नजर करें और बैलों द्वारा खेती और वाहन व्यवहार क्षेत्र में दी जानेवाली सेवाओं और उसके पर्यावरणीय लाभ देखें। भारतीय संस्कृति की ऋषि कृषि में उसके उद्भव समय से ही बैलों का श्रम सहायक रहा है। हल से खेल जोतना, खेतों में बीज डालना, गोबर की खाद को खेत में समतल पाटना, सिंचाई के लिये कुओं से पानी खींचना, अनाज काटने के बाद पौधों के खूंटो को फिर से जमीन में पाट देना, खलिहान में अनाज के दाने पौधे से अलग करना, बैलगाड़ी से अनाज घर/बाजार तक पहुँचाना, अनाज के अन्य शहरों में व्यापार के लिये बैलगाड़ियों के कारवां में जुड़ना, तेल के कोल्हू चलाना, गन्ने के रस निकालने के कोल्हू चलाना, घर के सदस्यों के लिये आसपास के 10-15 मील के गांवों में जाने के लिये आरामदेह बैलगाड़ियों में जुड़ना- एसे कई कई कामों में बैलों का उपयोग होता था। आज भयंकर कत्ल के कारण बैल उपलब्ध नहीं हैं और पेट्रोल-डीजल व बिजली से चलने वाले साधन उपयोग किये जाते हैं, जैसे कि ट्रेक्टर, पम्प, थ्रेशर, टेम्पो, ट्रक इत्यादि। इन सभी साधनों के उत्पादन का खर्च अलग रखें तो भी पेट्रोल-डीजल के उपयोग से कितना प्रदूषण होता है!
गौवंश का संरक्षण इन सभी प्रदूषणों से हमें बचा कर प्रजा की अनन्य सेवा करने को समर्थ है। जरुरत है तो सिर्फ इतनी कि इन सेवाओं का मूल्य-महत्व हम समझें। प्रजा तो यह महत्व समझती है, परंतु हमारे शासक, योजना आयोग में बैठे नीति-निर्माता, कृषि और पशुपालन की नीति के निर्माताओं को यह मूल्य समझ में आये तो प्रजा की अमूल्य पूँजी के नाश के बजाय उसके संरक्षण की नीतियाँ बने। आशा है यह संदेश योग्य स्थानों तक पहुँचेगा।



