नाट्य संगीत में प्रयुक्त पद शास्त्रीय संगीत पर एवं शास्त्रों को ध्यान में रखकर ही प्रयुक्त किए जाते हैं। इसी कारण संगीत और नाट्य संगीत का परस्पर संबंध वैसे ही है जैसे सोने में सुहागा।
नाट्य संगीत अर्थात नाटकों में संगीत का समावेश। नाटक में अभिनय के साथ-साथ यदि संगीत का समावेश हो तो यह सोने में सुहागा वाली कहावत को चरितार्थ होती है। नाटकों में शब्दों के माध्यम से भावनाविष्कार होते समय यदि संगीत का समावेश हो तो भावनाओं को व्यक्त करने में अधिक गति मिलती है।
काव्य संपूर्ण साहित्य में श्रेष्ठ माना जाता है। शब्दों के माध्यम से ध्वनि का माध्यम अधिक व्यापक व गंभीर होता है, क्योंकि मन की उत्कृष्ट भावनाओं को ध्वनि के माध्यम से जिस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है उस प्रकार शब्दों के द्वारा उसे अभिव्यक्त नहीं कर सकते। लय और नाद के साथ ही कोई भी रचना श्रोता जब सुनता है तो झूम उठता है। संगीत कला का मुख्य कार्य लय और नाद के द्वारा रसोत्कर्ष निर्माण करना है।
अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम भला संगीत के अलावा क्या हो सकता है! भारत जैसे अध्यात्मिक, धर्मप्राण देश में जहां प्राचीन समय से ही ऋषि-मुनियों ने ईश्वर उपासना का माध्यम संगीत में ही ढूं़ढा था, स्वाभाविक था कि मराठी नाटकों में संगीत का समावेश करने पर भारतीय मानव के एक अंतर पहलू भक्ति को प्रधानता, अहम रूप दिया गया।
इस रंगमंच के लिए तत्कालीन नाटककार स्व. गोविंद बल्लाल देवल, राम गणेश गडकरी, कृष्णजी प्रभाकर खाडिलकर, अण्णा साहेब किर्लोस्कर ने तत्कालीन उपलब्ध अभिनेताओं के लिए योग्य संगीत नाटक लिखे। उपरोक्त नाटककारों ने नाटकों में सूत्रधार अथवा गायकों के लिए बड़ी संख्या में गीत रखे हैं। ये गीत रसिक श्रोताओं के लिए किसी शाही दावत से कम नहीं होते थे। ये गीत मधुर, रस युक्त तथा आध्यात्मिकता से परिपूर्ण होते थे जैसे मराठी का यह पद देखें, “नरवर कृष्णा समान, वद जाऊ कुणाला शरण, पतित तू पावना म्हणवीसी नारायना” आदि। इन नाटकों में सौभद्र, शाकुंतल, राम राज्य वियोग आदि नाटक लोकप्रियता के शिखर पर थे।
शास्त्रीय संगीत को अमुमन आम श्रोता उबाऊ संगीत के नाम से पहचानता है, उसे नाट्य संगीत के माध्यम से लोकप्रिय बनाने का कार्य तत्कालीन मराठी नाटककार, गायक अभिनेताओं के द्वारा किया गया। नाट्य संगीत मिश्र संगीत है, शुद्ध शास्त्रीय संगीत नहीं। इसमें शास्त्रीय संगीत के नियमों का बंधन नहीं होता। स्वर वैचित्र ही इस संगीत का वैशिष्ट होता है। सांगीतिक आविष्कार की दृष्टि से देखा जाए तो प्राचीन भाव गीत, ठुमरी, गजल, लावणी और भी कई मिश्र संगीत के प्रकार नाट्य संगीत के उपयोग में लाए जाते हैं। स्वर सौंदर्य के कारण सभी श्रोता इस नाट्य संगीत से आनंद प्राप्त करते हैं।
विद्वानों का तर्क है कि मराठी नाट्य संगीत की परंपरा संत ज्ञानेश्वर के समय से चली आ रही है। स्व.वी.का.राजवाड़े को तंजावर में एक रामदासी मठ से ईस्वी सन 1690 के लगभग श्री लक्ष्मी नारायण नाटक की हस्तलिपि की प्रति मिली है। इतिहासकार राजवा़डे का मत है कि इस हस्तलिपि से पता चलता है कि मराठी नाटकों की परंपरा संत ज्ञानेश्वर काल जितनी पुरानी है। इस नाटक की नांदी (आरंभ गीत) इस प्रकार है :-
जय जलाधिगंभीर,जय सुखचराचर ।
जय शामित अभिराम, जय भक्तानुकूल ॥
“श्री लक्ष्मीनारायण कल्याण”, “ललित दशावतारी” आदि नाटक 150 साल तक लोगों का मनोरंजन करते रहे, परंतु सांगली में नाटक का प्रथम प्रयोग स्व.विष्णुदास भावे ने 1843 में करके मराठी रंगमंच की प्राण प्रतिष्ठा की। भावे ने रामायण, महाभारत तथा भागवत में से करीब पचास लोकप्रिय आख्यान पर पद रचे।
ललित नाटक, गोंधल, स्वांग, बहुरूपिए, कठपुतली आदि छोटे-छोटे नाट्य प्रकारों में मराठी संगीत नाटकों की नींव सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ललित शब्द काफी प्राचीन है। संत तुकारामजी ने एक अभंग में कहा है कि “गलित झाली काय हेची तलित पंढरिराया” अर्थात अंत मंगलमय हो।
19वीं शताब्दी के प्रारंभ में मुंबई के दादोषदंत नामक एक मराठा व्यक्ति ने ललित दिखाने की शुरुआत की। यह नाट्य विधा 17वीं शताब्दी से महाराष्ट्र में चलन में थी। कीर्तन का ही एक ललित सामान्यतः 19वीं शताब्दी की नाट्य विधा थी जिसमें कीर्तनकार का मध्यांतर हुआ कि ललित में उनके रूप वासुदेव, छड़ीदार, भालदार आगे आते थे। संभाषण अभिनय करते एवं भगवान की आरती के उपरांत प्रसाद मांगते एवं फिर कीर्तनकार का शेष भाग होता था। इस प्रकार ललित मिश्रित कीर्तन समाप्त होता था।
मराठी नाट्य संगीत रंगमंच की ऐसी विशिष्ट गायन विधा है जो भारतीय शास्त्रीय संगीत की देन है। यद्यपि कालीदास, भवभूति आदि प्राचीन नाट्याचार्यों के गद्य एवं पद्यात्मक नाटकों से ही इसका आविष्कार हुआ है, फिर भी मराठी रंगमंच पर इस संगीत का विकास व स्वरूप कुछ नवीनता लिए हुए मोहक रूप में सामने आया। मराठी रंगमंच की यह विशेषता दो अर्थों में असाधारण है। पहला, शास्त्रीय संगीत की प्रकृति को हानि न पहुंचाते हुए नाटक के अनुकूल संगीत नियोजन करना तथा प्राचीन नाट्याचार्यों द्वारा रचित पद्य प्रकारों का रूपांतर करके उस पर संगीत रूपी साज चढ़ाया जाना, जो हर प्रकार से नाट्य के लिए लाभदायक एवं रसपोषक हो। ऐसा कार्य नि:संदेह सरल नहीं है। प्राचीन नाट्याचार्यों की परंपरा के आधार पर ऐसे स्वरूप में नाट्य संगीत का आविष्कार दूसरे किसी प्रांत में दिखाई नहींदेना इसका दूसरा असाधारण पहलू है।
सन 1911 से 1934 का समय मराठी रंगमंच का स्वर्ण काल माना जाता है। संगीत की दृष्टि से यह समय अत्यंत सफल एवं श्रोताओं पर प्रभावशाली माना जाता है। पूरब की ठुमरी से लेकर भाव गीत एवं ख्याल से भजन तक ऐसे सभी गायन के प्रकार रंगमंच पर आए। श्रेष्ठ संगीत निर्देशक भी इसी समय हुए, जिन्होंने शास्त्रीय संगीत पर आधारित नवीन धुनों को बनाया एवं कई बार पुरानी धुनों को संशोधित करके दिया। इतना ही नहीं, वे धुनें किस प्रकार गाई जाएं इसका भी मार्गदर्शन किया तथा इस संगीत को सामान्य श्रोताओं, दर्शकों के सम्मुख लाने के लिए गायक अभिनेताओं की एक स्वतंत्र परंपरा का निर्माण कर शास्त्रीय संगीत को लोकप्रिय बनाने का बीड़ा उठाया। मराठी नाट्य संगीत विशिष्ट गायन प्रकार है एवं मराठी भाषियों के लिए यह विद्या अपरिचित नहीं है। महाराष्ट्र के घर-घर में यह संगीत लोकप्रिय है। परंतु अन्य प्रांतों के लिए यह विद्या अपरिचित ही है। जो सामान्य वर्ग शास्त्रीय संगीत को सुनने, समझने वाला नहीं है ऐसा जन सामान्य श्रोता वर्ग भी नाट्य संगीत को बड़ी तन्मयता के साथ सुनता है। इसलिए यह जानना जरूरी हो जाता है कि मराठी नाट्य संगीत क्या है एवं शास्त्रीय संगीत के समानांतर कैसे है? इस तथ्य को जान लेने के उपरांत ही जन सामान्य पर इसके प्रभाव को जान पाने में सुविधा होगी।
वैसे तो मराठी नाट्य संगीत एक व्यापक विषय है जिसमें नाट्य संगीत के कुछ विशिष्ट नियम जैसे- उसकी स्वर रचना तथा विस्तार कैसे हो, लय-ताल का प्रयोग, शब्दोच्चारण, गायक, अभिनेता, पार्श्व संगीत एवं नृत्य का स्थान, पद कैसा व कितना गाया जाए, संगत साजो का उपयोग कितना व कैसा हो आदि कई बातों का ध्यान रखना पड़ता है। परंतु यह एक व्यापक एवं विस्तृत अध्ययन का विषय है। मराठी नाट्य संगीत में शास्त्रीय संगीत के अनेक रागों का परिचय सरल एवं सहजता से करवाया, जिसमें कई राग जैसे- भूपाली, मांड, खमाज, पहाड़ी, पीलू, बिहाग, जोगिया, भीमपलासी आदि हैं एवं इन रागों मे निबद्ध नाट्य पदों में धूमाली, कहरवा, त्रिताल, एकताल आदि तालों का प्रयोग किया गया है। मराठी नाट्य संगीत में विभिन्न रागों का प्रयोग देखने को मिलता है, जो निम्नानुसार है :-
मृग नयना रसिक मोहिनी (संशय कल्लोल- दरबारी कान्हड़ा), नभ मेघानी आक्रमिले (सौभद्र- गौड़ मल्हार), दिन गेले भजनाविण सारे (कट्यार काळजात घुसली- अलैया बिलावल), जगी हम भागा सुखी चीर असुख (एकच प्याला- बिहागड़ा), प्रिये पहा रात्रिचा समय (सौभद्र- देसकार), वद जाऊ कुणाला शरण (सौभद्र- जोगिया), घेई छंद मकरंद (कट्यार काळजात घुसली- धानी) आदि। इसके अलावा लगभग सभी नाट्य गीत रागों पर ही आधारित व शास्त्र सम्मत रहते हैं। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि नाट्य संगीत में प्रयुक्त पद शास्त्रीय संगीत पर एवं शास्त्रों को ध्यान में रखकर ही प्रयुक्त किए जाते हैं। इसी कारण संगीत और नाट्य संगीत का परस्पर संबंध वैसे ही है जैसे सोने में सुहागा।


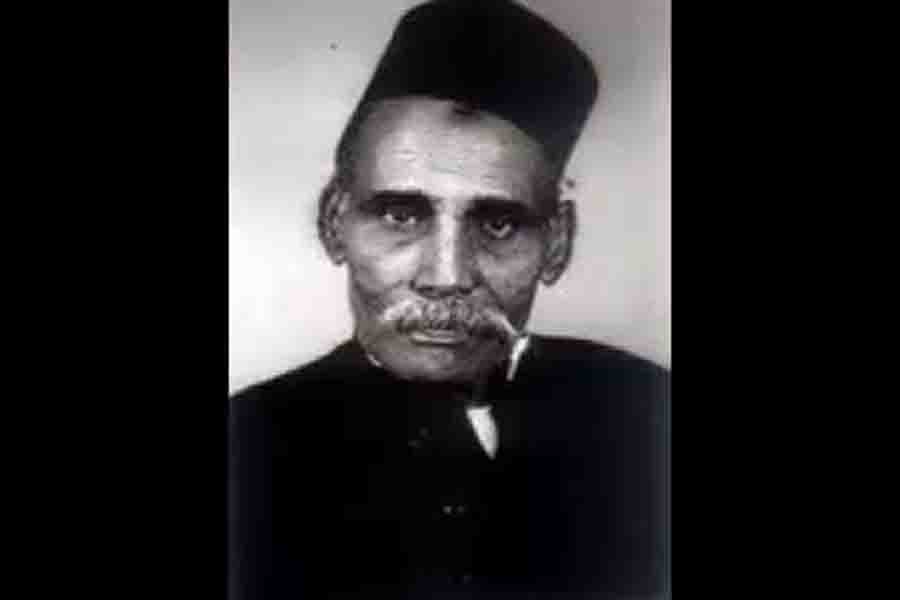

Hi