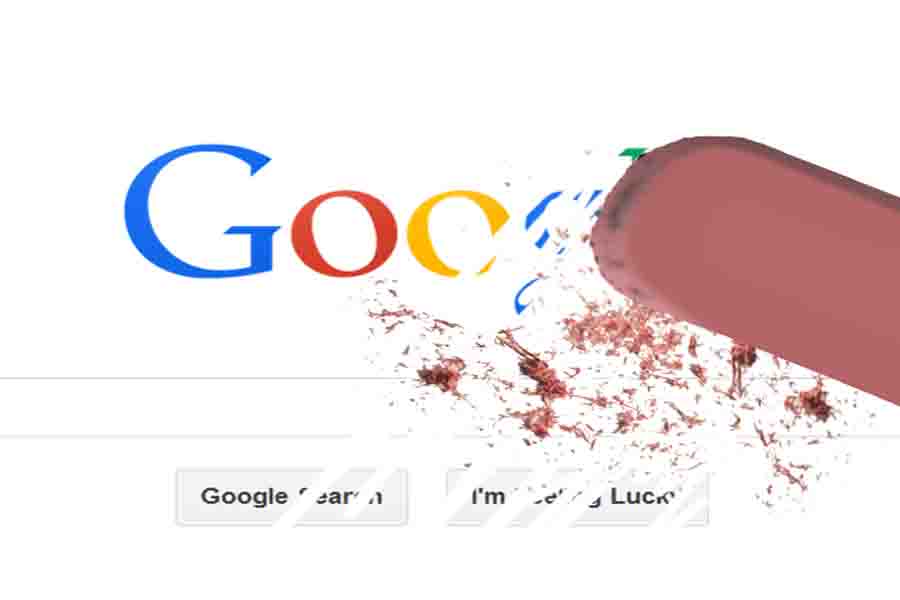सूचना अधिकार बीसवीं सदी की देन है, तो सूचना निरसन अधिकार इक्कीसवीं सदी की देन मानने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। स्पेन व यूरोप से चली यह आंधी भारत तक पहुंच चुकी है और पिछली मई में दिल्ली उच्च न्यायालय में ऐसा एक मामला दायर हो चुका है। इस मामले में गुगल, ‘इंडियन कानून’ वेबसाइट व केंद्र सरकार को समन जारी किया गया हे। अगली सुनवाई 21 सितम्बर को है।
इस आलेख का शीर्षक ही कुछ अबूझी पहेली जैसा लगता है। सूचना याने जानकारी। अंग्रेजी में यही इंफारमेशन शब्द में व्यक्त होता है। अब तक हमने सूचना याने जानकारी पाने के अधिकार की बात सुनी है। कई देशों में इसके लिए कानून भी बने हैं। लेकिन सूचना या जानकारी को निरस्त कर देने याने निरसन के अधिकार की बात नहीं सुनी है। सूचना के अधिकार में जिस तरह सार्वजनिक उपयोग की जानकारी पाने का आपको अधिकार प्राप्त होता है, वैसे ही सार्वजनिक संजाल (इंटरनेट) पर प्रस्तुत ‘अधूरी, असम्बद्ध, तारतम्यविहीन, या बेमतलब’ की जानकारी निरस्त कर देने, हटा देने का आपको बुनियादी अधिकार है। इसे अंग्रेजी में ‘राइट टु बी फॉरगॉटन’ अर्थात सूचना निरसन का अधिकार कहते हैं। फॉरगॉटन का अर्थ है भूल जाना, छोड़ देना, हटा देना आदि। मतलब सूचना को खत्म कर देना या निरस्त कर देना। इसलिए सरल शब्द-प्रयोग की दृष्टि से मैंने इसे ‘सूचना निरसन अधिकार’ कहा है। भारत में इस पर अभी बहस आरंभ हुई है। यह अंग्रेजी मीडिया में है, भाषाई मीडिया में अभी पहुंची नहीं है। इसलिए भाषाई शब्द-प्रयोग विकसित नहीं हुआ है। भाषाई मीडिया को मेरा यह शब्द-प्रयोग स्वीकार करना चाहिए, फिर भी इससे बढ़िया या सरल सटीक शब्द-प्रयोग मिले तो उसका स्वागत ही है। अब इस अधिकार को पाने का किसे हक है, यह देखते हैं। यह अधिकार उसे ही प्राप्त हो सकता है, जिसने वह जानकारी सूचना संजाल (इंटरनेट, यूट्यूब, बिंग, याहू, फेसबुक, वेबपेज, वेबपत्रिका, व्हाट्सएप, ट्विटर, निजी नेट-ग्रुप आदि) को दी है या वह व्यक्ति जिसके बारे में यह जानकारी है। सूचना अधिकार बीसवीं सदी की देन है, तो सूचना निरसन अधिकार इक्कीसवीं सदी की देन मानने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। स्पेन व यूरोप से चली यह आंधी भारत तक पहुंच चुकी है और पिछले मई माह में दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक मामले में गुगल व ‘इंडियन कानून’ वेबसाइट, केंद्र सरकार को समन जारी किया हे। इस मामले का विस्तृत जिक्र आगे करूंगा ही। पहले अधिकारों के लिए चल रहे अभियान के बारे में थोड़ा सा।
मानव अधिकारों की मांग ने लम्बा सफर तय किया है। स्त्री-पुरुष समानता, स्त्री को शिक्षा, मतदान, स्वयं-निर्णय आदि के अधिकार से आरंभ यह आंदोलन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शिक्षा और रोजगार के अधिकारों, बाल अधिकारों तक पहुंचा है और भविष्य में कई नए अधिकार इसमें शामिल होंगे, जबकि पुराने निरर्थक अधिकार अपने-आप ही समाप्त हो जाएंगे। कानून के बारे में यह तो बिल्कुल सटीक बैठता है। भारत में अंग्रेजों के जमाने में बने 300 से अधिक कानून अब निरर्थक हो गए हैं और उनका अब कोई उपयोग भी नहीं करता। ऐसे कानूनों को खत्म करने की अब तैयारी चल रही है। किसी जमाने में सरकार से कोई जानकारी मांगना, गोपनीयता का भंग माना जाता था, लेकिन अब तो यह कानूनी अधिकार बन गया है। यही स्थिति सूचना निरसन अधिकार के बारे में है। इसकी अवधारणा अभी शैशवावस्था में हैं, लेकिन यह अवश्य है कि यह अधिकार देससबेर प्रदान करना ही पड़ेगा।
वर्तमान युग जानकारी के विस्फोट का युग है। चारों ओर से बेहिसाब जानकारी प्राप्त हो रही है। वेदों ने भी चारों ओर से ज्ञान को स्वीकार करने को कहा है, लेकिन यह सतर्कता भी व्यक्त की है कि व्यक्ति नीरक्षीर विवेक से ही जानकारी को स्वीकार करें। इस सूचना युग में वेदों का पहला परामर्श तो अमल में आ रहा है, लेकिन नीरक्षीर की बात मुश्किल हो रही है। गॉसिप, फरेबी फोटो, अश्लील या नितांत निजी अंतरंग फोटो, झूठी कहानियां और न जाने क्या-क्या नेट पर भेजा जाता है। अनजान व्यक्ति भी आप के आईपी पर पहुंच कर यह सब डाल देता है। उसे रोकने का आपके पास कोई जरिया नहीं है। ऐसी किसी जानकारी का सच, झूठ पता करना तक मुश्किल हो रहा है। इस कारण कई प्रतिष्ठित व चर्चित व्यक्ति, विशेष रूप से राजनीतिक व फिल्मी हस्तियां बेवजह बदनाम हो जाती हैं। कोई उद्यमी या आम आदमी भी इसकी चपेट में आ जाए तो आसपास के परिसर में उसका जीना दुश्वार हो जाता है। इसलिए यह मुद्दा सामने आया कि जिसने जानकारी दी है वह या जिनके बारे में जानकारी है वे यदि ऐसी जानकारी हटा देना या निरस्त करने की मांग करें तो यह उनका अधिकार बनता है और गुगल, बिंग, यू ट्यूब जैसे सर्च इंजनों को उसे हटा देना चाहिए। और यदि वे नहीं हटाते तो वे व्यक्ति की मानहानि के कानूनी रूप से दोषी माने जाए।
सूचना निरसन अधिकार की चर्चा जिस घटना से आरंभ हुई उसके संक्षिप्त विवरण को देखें तो बहुत सी बातें अपने-आप स्पष्ट हो जाएंगी। कहानी 1998 से आरंभ होती है, जब मारियो कोस्तेजा गोंजालेज नामक स्पैनिश व्यक्ति ने ‘ला वेंगुआर्दिया’ नामक वेब-अखबार में उसके बारे में जारी लेख को हटाने और लेख को प्राप्त करने वाली लिंक को निरस्त कर देने का आग्रह किया। इस आलेख में कहा गया था कि ॠण न चुकाने के कारण उसका घर जब्त कर लिया गया है। यह वास्तविकता थी, लेकिन यह भी तथ्य था कि उसने अब ॠण चुका दिया है और उसका घर जब्ती से हट गया है। वेब-अखबार ने कहा कि उसने जो बात लिखी वह सच है, वह उसे नहीं हटाएगा। कोस्तेजा ने इसकी शिकायत स्पैनिश डेटा सुरक्षा एजेंसी से की। एजेंसी ने भी यह कह कर दावा ठुकरा दिया कि लेख नेट पर उपलब्ध तथ्यों पर आधारित है। लेकिन, गुगल के खिलाफ शिकायत दर्ज की और कहा कि वह यह जानकारी हटा दें। गुगल ने इसे नहीं माना और यूरोपीयन कोट ऑफ जस्टिस में चुनौती दी। यूरोपीय अदालत ने गुगल की अर्जी ठुकरा दी और कहा कि संजाल पर उपलब्ध जानकारी के लिए सर्व इंजन (गुगल, याहू, बिंग, फेसबुक, ट्विटर, विकीपीड़िया आदि) जिम्मेदार हैं और सम्बंधित व्यक्ति यदि उसे हटाने की मांग करता है तो वह उसका अधिकार बनता है। यह बात ही सूचना निरसन अधिकार की जननी है। 13 मई 2014 को यह फैसला आया। गुगल ने इस फैसले के बाद उस पर अमल शुरू कर दिया और पहले ही दिन अर्थात 30 मई 2014 को 12 हजार आवेदनकर्ताओं ने अपनी निजी जानकारी हटाने का गुगल से आग्रह किया। गुगल ने कोई 14 लाख लिंक, फेसबुक ने 12 हजार, यूट्यूब ने 6 हजार, गुगल ग्रुप ने सवा सात हजार एवं ट्विटर ने साढ़े चार हजार यूआरएल (लिंक) हटा दिए। अभी 2016 के मध्य तक इसकी संख्या में और इजाफा होगा, लेकिन उसके आंकड़ें अभी उपलब्ध नहीं हैं। लिंक हटा देने की मांग करने वालों में आम लोग ज्यादा हैं अर्थात 95 फीसदी। अपराधियों, राजनेताओं एवं चर्चित हस्तियों की संख्या महज 5 फीसदी है।
जर्मनी का किस्सा और मजेदार है। 27 अक्टूबर 2009 को वोफगैंग वेरी नामक एक हत्यारे ने विकीपीड़िया के एक आलेख से अपना नाम हटा देने की मांग की। वेरी ने मैनफ्रेड लौबर नामक व्यक्ति के साथ मिल कर वाल्टर सेडलमायर नामक व्यक्ति की हत्या की थी और इसके लिए उसे दोषी करार देकर सजा भी हुई थी। दोनों ने सजा भी भोग ली, अतः अब उनका नाम उछालने की जरूरत नहीं है, यह हत्यारों का तर्क था। जर्मनी के हम्बुर्ग की अदालत ने दोनों की बात मान ली। लेख के जर्मन संस्करण से उनके नाम हटा दिए गए, लेकिन अंग्रेजी संस्करण में अभी भी उनके नाम छप रहे हैं और मामला अब अमेरिकी अदालत में है।
अर्जेंटीना में कलाकार वर्जिनिया दा-कुन्हा की शिकायत पर उनके फोटो गुगल एवं याहू ने हटा दिए। ये फोटो वर्जिनिया की सहमति से लिए गए थे और नेट पर डाले गए थे। वर्जिनिया ने इस पर आपत्ति की और कहा कि ये फोटो सर्व इंजन में पोर्नोग्राफी (लैंगिक) शीर्षक में मिलते हैं, जिससे उनकी बदनामी होती है। उनकी बात मान ली गई।
अमेरिका में मेलविन विरुद्ध रीड एवं सिदीज विरुद्ध एफआर पब्लिसिंग कार्पोरेशन ये दो कानूनी मामले सूचना निरसन अधिकार के बारे में बहुचर्चित हैं। मेलविन वेश्या थी, लेकिन बाद में उसने पेशा छोड़ दिया और सामान्य जिंदगी बिताने लगी। लेकिन, ‘द रेड किमोनो’ फिल्म में उसकी कथा उजागर की गई और उसने निर्माता पर मुकदमा ठोक दिया और वह जीत गईं। दूसरा किस्सा भी रोचक है। विलियम जेम्स सिदीज बचपन में जादुई खेल दिखाता था, लेकिन वयस्क बनने पर वह शांति से जीवन बिताना चाहता था। ‘द न्यूयार्कर’ में छपे एक लेख के कारण उसका जीवन ही बर्बाद हो गया। मामला अदालत में गया। अदालत ने कहा कि किसी का जीवन नियंत्रित कर देने का किसी को अधिकार नहीं है। वे लोकप्रिय व्यक्ति इसलिए हैं कि वे वैसा रहना चाहते हैं। जून 2014 में ‘फोर्ब्ज’ में प्रकाशित अपने स्तंभ में जोसेफ स्टेनबर्ग ने कहा कि ‘प्रौद्योगिकी विकास ने लोगों के निजी जीवन को सीमित कर दिया है। अभिव्यक्ति सीमित हो गई है। इसलिए सूचना निरसन जैसा अधिकार व्यक्ति को प्राप्त होना चाहिए।’
अब भारत में दायर मामले की ओर चलते हैं। नई दिल्ली के एक बैंक अधिकारी ने दिल्ली उच्च न्यायालय में मुकदमा दायर कर यह सवाल उठाया है कि क्या संविधान में उल्लेखित बुनियादी ‘जीने के अधिकार’ के अंतर्गत ‘सूचना निरसन का अधिकार’ भी शामिल है? न्यायमूर्ति मनमोहन ने इस पर केंद्र सरकार, गुगल और ऑनलाइन वेबसाइट ‘इंडियन कानून’ को नोटिस जारी किया है। अधिकारी चाहता है कि वेबसाइट को उसकी निजी जानकारी की लिंक हटा देनी चाहिए। यह जानकारी उसके पत्नी से झगड़े के बारे में है, जिस पर कुछ वर्षों पूर्व ही समझौता हो चुका है। फिर भी सर्च करने पर यह मामला ‘इंडियन कानून’ की साइट पर दिखाई देता है। मामले की विस्तृत जानकारी भी गुगल और अन्य सर्व इंजनों पर उपलब्ध है। वकीलद्वय रोहित मदान एवं आकाश वाजपेयी ने उनकी पैरवी कर रहे हैं। मामले में विदेशों व यूरोप के कई उदाहरण देकर ‘सूचना निरसन के अधिकार’ का अनुरोध किया गया है। भारत में इस तरह का कोई कानून नहीं है। इसलिए अदालत क्या रुख लेती है, यह रोचक होगा। अगली सुनवाई अब 21 सितम्बर को होनी है।
सूचना निरसन अधिकार की परिभाषा अभी शैशव में है। यह शब्द-प्रयोग पहले यूरोपीय कानून में किया गया। यह इंटरनेट का युग है। उसके बिना हम अपना अस्तित्व ही खो देंगे। सर्च इंजनों से जानकारी प्राप्त करने पर नियंत्रण लगा देने से सूचनाएं प्राप्त करने पर भी अपने आप नियंत्रण लग जाएगा। इस तरह का नियंत्रण ही ‘सूचना निरसन अधिकार’ का स्रोत है। इसका उद्देश्य व्यक्ति की निजी जानकारी को नेट से हटाने के लिए सर्च इंजनों को कह कर व्यक्ति के जीवन को सुरक्षा प्रदान करना है। अधिक सरल भाषा में कहना हो तो ऐसी जानकारी को लिंक खत्म कर देना है याने लिंक कट-ऑफ!
इस अधिकार के सकारात्मक पक्ष के अलावा नकारात्मक पक्ष भी हैं। इस पर सारी दुनिया में इस समय बहस छिड़ी हुई है। गुगल का कहना है कि भले ही वह लिंक हटा दें, फिर भी वह सामग्री कहीं न कहीं पड़ी रहती ही है। किसी ने पहले ही किसी ड्राइव में सेव कर रखी होगी तो उसे हटाना गुगल के बस की बात नहीं है। अभी तो यूरोप में वहां की अदालत की आज्ञा के कारण इस अधिकार को गुगल ने स्वीकार किया है, लेकिन यूरोप के बाहर वही सामग्री आसानी से उपलब्ध है। वह एशिया, अफ्रीका या अमेरिका में कोई प्राप्त कर यूरोप भेज दें तो गुगल कुछ नहीं कर पाएगा।
इस अधिकार को विश्व स्वीकार कर लें तो पूरी दुनिया में अघोषित सेंसरशिप लागू हो जाएगी और इंटरनेट का मूल उद्देश्य ही ध्वस्त हो जाएगा। आस्ट्रेलिया ऐसे किसी अधिकार के पक्ष में नहीं है। चीन, जापान, अरब देशों के रुख का अभी पता नहीं है। विकासशील देशों में भारत के रुझान पर बहुत कुछ निर्भर है। अन्य विकासशील एवं अविकसित देश यहां के परिवर्तन से अछूते नहीं रहते। अदालत क्या रुख लेती है, इसका सितम्बर में ही पता चलेगा, जब अगली सुनवाई होगी।