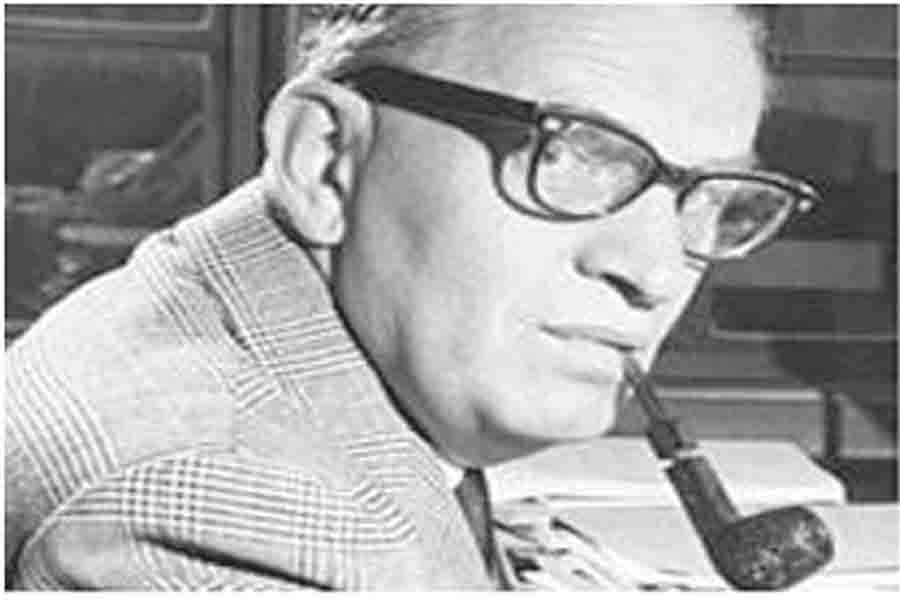कश्मीर संकट पर राष्ट्रसंघ का प्रस्ताव क्रमांक 47 और उससे जुड़े अन्य प्रस्ताव निष्फल और कालबाह्य हो चुके हैं। ये प्रस्ताव कागजी शेर बन कर रह गए हैं। प्रस्तावों के इस हश्र के लिए पाकिस्तान जिम्मेदार है; क्योंकि प्रस्तावों की पूर्वशर्त के अनुसार उसने अपने कब्जे वाले इलाके से अपनी फौज नहीं हटाई। शंखगाम घाटी तो उसने चीन को ही दे दी। अब तो पाकिस्तान-चीन एक तरफ और भारत दूसरी तरफ यह स्थिति बन गई है।
जम्मू-कश्मीर संघर्ष को लेकर राष्ट्रसंघ के प्रस्ताव पर हमेशा बहस होती है। इस प्रस्ताव पर पिछले 70 वर्षों से युद्धविराम के अलावा और कोई अमल नहीं हो पाया। ऐसा क्या है कि प्रस्ताव महज कागजी दस्तावेज बन कर रह गया? वर्तमान परिस्थितियों में इसका क्या कोई औचित्य भी रह गया है? ये ऐसे प्रश्न हैं जिनकी गहराई में जाने के पूर्व यह जानना जरूरी है कि यह प्रस्ताव आखिर क्या है? और किस पृष्ठभूमि में यह पारित किया गया? क्या यह पृष्ठभूमि आज मौजूद है या उसमें आमूल परिवर्तन हो चुका है?
कश्मीर समस्या की पृष्ठभूमि में भारत का विभाजन है। 1947 में ब्रिटिशों ने धर्म के आधार पर भारत और पाकिस्तान नामक दो देश बना दिए। लेकिन इससे समस्या और उलझ गई। ब्रिटिश भारत में कोई 562 रियासतें थीं। ब्रिटिशों ने उन्हें यह स्वतंत्रता दे दी कि वे इन दो देशों में से या तो किसी एक देश में शामिल हो सकते हैं अथवा अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रख सकते हैं। जम्मू-कश्मीर के साथ यह समस्या थी कि उसके तीन प्रमुख संभागों में तीन अलग-अलग धर्म थे। जम्मू हिंदूबहुल था, कश्मीर घाटी मुस्लिमबहुल और लद्दाख बौद्धबहुल। तीनों संभागों में तीनों धर्म मानने वालों की संख्या लगभग समान थी। इसी कारण तत्कालीन राजा हरिसिंह किस तरफ जाए यह निर्णय नहीं कर पाए और स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखने की कोशिशों में लगे रहे। राजा हरिसिंह की भूमिका को लेकर बहुत कुछ उल्टा-सीधा लिखा जा चुका है। इन मुद्दों या तर्कों का परीक्षण इस लेख का उद्देश्य नहीं है। लेकिन इतना सच है कि राजासाहब की ढुलमुल नीतियों के कारण ही पाकिस्तान को राज्य पर आक्रमण करने का मौका मिल गया।
अगस्त 1947 में विभाजन के बाद से ही बड़े पैमाने पर दंगे-फसाद आरंभ हो गए। पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधान मंत्री लियाकत अली ने महाराजा पर पाकिस्तान में शामिल होने के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया। उनकी ही शह पर जम्मू-कश्मीर के मुस्लिमबहुल पश्चिमी इलाके में बड़े पैमाने पर उपद्रव शुरू हो गए। उपद्रवियों ने राज्य में जीवनावश्यक वस्तुओं की आपूर्ति रोक दी। महाराजा ने भारत से सहायता मांगी, लेकिन भारत ने इनकार कर दिया।
इस बिंदु पर लार्ड माउंटबैटन की भूमिका पर गौर करना होगा। कहा जाता है कि महाराजा के अनुरोध पर केंद्रीय मंत्रिमंडल की सुरक्षा समिति की बैठक हुई। भारत भले ही आजाद हुआ था, लेकिन सत्तांतरण की प्रक्रिया चल रही थी। अंतिम वायसराय माउंटबैटन ही कार्यवाहक राष्ट्रप्रमुख थे। इसलिए उनकी अध्यक्षता में ही यह बैठक हुई। बैठक में प्रधान मंत्री पं. नेहरू, उप प्रधान मंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल भी उपस्थित थे। कहते हैं कि स्वयं माउंटबैटन ने ही बैठक में सुझाव रखा कि जब तक महाराजा भारत में विलय के दस्तावेज पर हस्ताक्षर नहीं करते तब तक वहां हस्तक्षेप करना संभव नहीं है। बैठक में इस सुझाव का किसी ने विरोध नहीं किया। ब्रिटिशों की यह कूटनीतिक चाल लगती है, इस पर स्वतंत्र ग्रंथ हो सकता है। लेकिन इससे किसी भी स्थिति में ब्रिटिशों को लाभ ही होने वाला था और पाकिस्तान को घुसपैठ का मौका मिलने वाला था।
इस सुझाव का पाकिस्तान ने लाभ उठाया और 22 अक्टूबर 1947 को आक्रमण कर दिया। पाकिस्तान पहले-पहल तो यह कहता रहा कि आजादी चाहने वाले कबीलियाई पठानों का यह हमला है, पाकिस्तानी फौज इसमें शामिल नहीं है; लेकिन बाद में उसने इसे स्वीकार कर लिया। कबीलियाई फौज जब श्रीनगर के आसपास पहुंची तब महाराजा ने अपने दूत जस्टिस मेहरचंद को दिल्ली भेज कर विलय की इच्छा जाहिर की। विलय दस्तावेजों पर महाराजा के हस्ताक्षर का भी रोमांचक किस्सा है। महाराजा सुरक्षा की दृष्टि से अपने महल से निकल कर हवाईअड्डे पर पहुंचे थे। वहीं भारतीय अधिकारी दस्तावेजों के साथ पहुंचे और हवाईअड्डे के एक कमरे में इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए गए। 26 अक्टूबर को दस्तावेजों पर हस्ताक्षर हुए और 27 अक्टूबर से भारत ने अपनी फौज को विमानों से श्रीनगर उतारना शुरू किया। अब यह लड़ाई पाकिस्तान और भारत के बीच की लड़ाई बन गई।
इस पृष्ठभूमि को जाने बिना इस सम्बंध में राष्ट्रसंघ द्वारा पारित प्रस्ताव को समझना मुश्किल होगा। अब जम्मू-कश्मीर भारत का अविभाज्य अंग बन चुका था। भारत को अपनी भूमि की रक्षा करनी थी और पाकिस्तान वहां से हटना नहीं चाहता था। इसलिए दोनों में युद्ध बढ़ता गया। तीन माह से लड़ाई चल रही थी। इस बिंदु पर भारत से एक चूक हो गई, जिसका खामियाजा आज तक भुगतना पड़ रहा है। प्रधान मंत्री पं.नेहरू 1 जनवरी 1948 को इस मामले को राष्ट्रसंघ में ले गए। राष्ट्रसंघ संविधान के अनुच्छेद 35 के अंतर्गत सुरक्षा परिषद में यह मामला उठाया गया। इस अनुच्छेद के अनुसार दो राष्ट्रों की लड़ाई से अंतरराष्ट्रीय शांति को खतरा उत्पन्न हो तो राष्ट्रसंघ हस्तक्षेप कर सकता है।
भारत के दो मुद्दे थेः एक- जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा बन गया है; अतः उस पर हमले से पाकिस्तान को रोका जाए। दो- जनइच्छा जानने के लिए वहां जनमत संग्रह कराने और उसके परिणाम स्वीकार करने के लिए भारत तैयार है। पाकिस्तान ने भी जवाब में दो मुद्दे पेश किएः एक- भारत ने धोखाधड़ी एवं हिंसा के जरिए जम्मू-कश्मीर का विलय करवाया है। दो- पाकिस्तान ने वहां हमला नहीं किया है और भारत मुस्लिमों का नरसंहार करवा रहा है। यह जनमत संग्रह ही आगे कूटनीति और टकराव का बिंदु बन गया।
राष्ट्रसंघ का इस विवाद पर पहला प्रस्ताव 20 जनवरी 1948 को पारित हुआ। इसे प्रस्ताव क्रमांक 39 कहा जाता है। इस प्रस्ताव के तहत सुरक्षा परिषद ने शिकायतों की जांच के लिए तीन सदस्यीय आयोग के गठन का निर्णय किया। लेकिन यह आयोग मई 1948 तक अस्तित्व में ही नहीं आया।
इसी बीच चीन ने 18 मार्च को नया प्रस्ताव पेश किया। इस प्रस्ताव में तीन प्रमुख बातें थीं- एकः पहले चरण में पाकिस्तान कबीलों एवं अपनी फौज को जम्मू-कश्मीर से हटाए, दोः दूसरे चरण के रूप में भारत अपनी सेना को धीरे-धीरे कम करें और उतनी ही फौज रखें जितनी कानून व व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी हो, और तीनः भारत सभी पक्षों को लेकर राज्य में सरकार गठित करें, राष्ट्रसंघ द्वारा मनोनीत जनमत संग्रह प्रशासक नियुक्त करें, जो दोनों देशों के सहयोग से मुक्त व निष्पक्ष जनमत संग्रह करवाए। इस प्रस्ताव को नौ विरुद्ध शून्य मत से मंजूरी मिली। सोवियत संघ एवं यूक्रेन ने मतदान नहीं किया। यही प्रस्ताव क्रमांक 47 कहा जाता है, जो हमेशा चर्चा का विषय है।
इस प्रस्ताव के भी ‘तीन तेरह’ हो गए। पहली बात तो यह थी कि सुरक्षा परिषद ने हमलावर के रूप में पाकिस्तान को नहीं लताड़ा, न ही जम्मू-कश्मीर के भारत में विलय को लेकर कोई सवाल उठाए। सुरक्षा परिषद चाहती तो इसके वैधानिक पक्ष पर अंतरराष्ट्रीय अदालत से सलाह मांग सकती थी। इससे सुरक्षा परिषद दोषी पक्ष की शिनाख्त कर उस पर कार्रवाई कर सकती थी। सुरक्षा परिषद की इस ढुलमुल नीति से विवाद सुलझना ही नहीं था। यह प्रस्ताव किसी भी पक्ष पर बंधनकारी न होने और सद्भावनात्मक होने से अव्यावहारिक साबित हो गया।
इसके पश्चात मूल प्रस्ताव क्रमांक 39 के तहत भारत और पाकिस्तान दोनों पांच सदस्यीय जांच आयोग के गठन पर सहमत हुए। इस आयोग में अर्जेंटीना, बेल्जियम, कोलम्बिया, चेकोस्लोवाकिया एवं अमेरिका सदस्य थे। आयोग के अध्यक्ष के रूप में चेकोस्लोवाकिया के प्रतिनिधि जोसेफ कोर्बेल चुने गए। आयोग ने दोनों देशों की सरकारों से चर्चा करने और प्रत्यक्ष स्थिति का मुआयना करने के बाद प्रस्ताव क्रमांक 47 में संशोधन पेश किए। ये संशोधन निम्न थेः
एक- युद्धविराम अर्थात पूरी तरह लड़ाई रोक देना।
दो- शांति समझौता। इसके तहत कब्जेवाली भूमि से पाकिस्तानी सेना, कबीलों एवं पाकिस्तानी नागरिकों की पूरी तरह वापसी, इस तरह रिक्त क्षेत्र का राष्ट्रसंघ आयोग की निगरानी में प्रशासन। पाकिस्तान की वापसी के बाद भारत से सेना में कमी और कानून व व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक न्यूनतम फौज की ही तैनाती।
तीन- शांति समझौते के बाद दोनों देश जम्मू-कश्मीर का भविष्य तय करने के लिए जनमत जानने के लिए व्यवस्था के बारे में आयोग से सलाह-मशविरा करेंगे।
इस संशोधित प्रस्ताव की भाषा गौर करने लायक है। इसमें पाकिस्तान को स्पष्ट रूप से ‘हमलावर’ करार दिया गया है। जनमत संग्रह (प्लेबिस्किट) शब्द का इस्तेमाल न करते हुए जनता की राय जानने के अन्य विकल्पों का भी मार्ग खुला रखा गया है। भारत ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है; क्योंकि उसके पक्ष को आयोग ने ज्यादातर स्वीकार किया है। पाकिस्तान ने इस प्रस्ताव को अलग-अलग बहाने देकर लगभग नामंजूर ही किया। लेकिन अंत में 1 जनवरी 1949 को दोनों पक्षों ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। अगले माह फरवरी में आयोग फिर दोनों देशों के दौरे पर आया, ताकि प्रस्ताव को अमली जामा पहनाया जा सके।
दोनों पक्षों ने प्रस्ताव के पहले हिज्जे अर्थात युद्धविराम को लागू कर दिया, लेकिन शांति समझौते और जनइच्छा जानने के मुद्दों पर कोई समझौता नहीं हो सका। अंत में 9 दिसम्बर 1949 को आयोग ने विफल होने की रिपोर्ट दे दी। झगड़े का मुख्य मुद्दा यह था कि पाकिस्तान अपने कब्जे वाले क्षेत्र से फौज हटाए, जो उसने अलग-अलग बहाने बनाकर स्वीकार नहीं की। अंत में सुरक्षा परिषद ने कनाडा के प्रतिनिधि ए.जी.एल.मैकनौघटन से दोनों देशों से फौज हटाने को लेकर बातचीत करने के लिए कहा। भारत के विरोध के बावजूद मैकनौघटन ने दोनों देशों के बीच मध्यस्थ नियुक्त करने का प्रस्ताव पेश किया, जिसे प्रस्ताव क्रमांक 80 कहा जाता है। इसका हश्र भी पहले के प्रस्तावों की तरह हुआ और वह निष्फल साबित हुआ। मार्के की बात यह है कि सन 2001 में राष्ट्रसंघ महासचिव कोफी अन्नान ने अपने भारत दौरे के समय कहा कि कश्मीर के बारे में राष्ट्रसंघ द्वारा अब तक पारित प्रस्ताव महज सलाह है और उनकी तुलना पूर्वी तिमूर या इराक के बारे में पारित प्रस्तावों से नहीं की जा सकती।
राष्ट्रसंघ के ये प्रस्ताव निरर्थक और कालबाह्य साबित हो चुके हैं। इसके कारण ये बताए जा सकते हैं-
1. पाकिस्तान ने समझौते की कब्जे वाले इलाके से फौज हटाने की शर्त का कभी स्वीकार नहीं किया। भारत ने अपने संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत कश्मीरी कौम के संरक्षण की गारंटी दी गई है, जबकि पाकिस्तान वाले कश्मीर में ऐसी कोई गारंटी नहीं है और गैर-कश्मीरियों को वहां लाकर स्थापित किया जा रहा है। 1948 के मुकाबले वर्तमान में जनसंख्या का स्वरूप पूरी तरह बदल गया है। कश्मीर घाटी से हिंदू पंडितों को भगाया गया है और वहां मुस्लिमों को स्थापित किया जा रहा है। अतः पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से गैर-कश्मीरियों को हटाना और भारत के कब्जे वाले कश्मीर में हिंदू पंडितों को पुनः वापस लाना संभव नहीं हो पा रहा है।
2. जनमत संग्रह का मूल सुझाव भारत का था, जो पाकिस्तान को तब मंजूर नहीं था। अब वह इसका आग्रह कर रहा है और ऐसा करते समय फौज हटाने की पूर्वशर्त को नजरअंदाज कर देता है।
3. पाकिस्तान ने 1963 में शंखगाम घाटी चीन को दे दी, जबकि उसे वैसा कोई अधिकार ही नहीं था। चीन के पाकिस्तान को समर्थन का कारण इससे पता चल जाता है।
4. यदि वर्तमान में जनता से राय मांगी जाए तो वह कभी निर्णायक रूप से सिद्ध नहीं होगी। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के गिलगिट, बाल्टीस्तान जैसे इलाके पाकिस्तान के पक्ष में राय दे सकते हैं, जबकि जम्मू और लद्दाख भारत के पक्ष में। शंखगाम घाटी तो चीन को ही दान दे दी गई है, जो चीन के पक्ष में जाएगी। कश्मीर घाटी की राय स्वतंत्र राज्य की हो सकती है। इस तरह कोई भी रायशुमारी कोई वास्तविक परिणाम नहीं दे पाएगी।
5. चीन ने गिलगिट-बाल्टीस्तान में अरबों डॉलर का निवेश किया है। चीनी फौज भी वहां तैनात की गई है। शंखगाम घाट तो चीन को मिली ही है। इस स्थिति में क्या पाकिस्तान या चीन चाहेगा कि यह इलाका अस्थायी ही क्यों न हो भारत के हाथ चले जाए? ऐसी स्थिति में पाकिस्तान और चीन की सीमाएं भी एक-दूसरे से जुड़ी नहीं होंगी।
इस चर्चा से स्वयं स्पष्ट हो जाएगा कि राष्ट्रसंघ का प्रस्ताव क्रमांक 47 और उससे जुड़े अन्य प्रस्ताव निष्फल और कालबाह्य हो चुके हैं। इसका और कोई विकल्प खोजना होगा। क्या भारतीय महासंघ जैसा कोई विकल्प हो सकता है? या क्या कुछ बातें समय पर ही छोड़ देनी चाहिए?
–