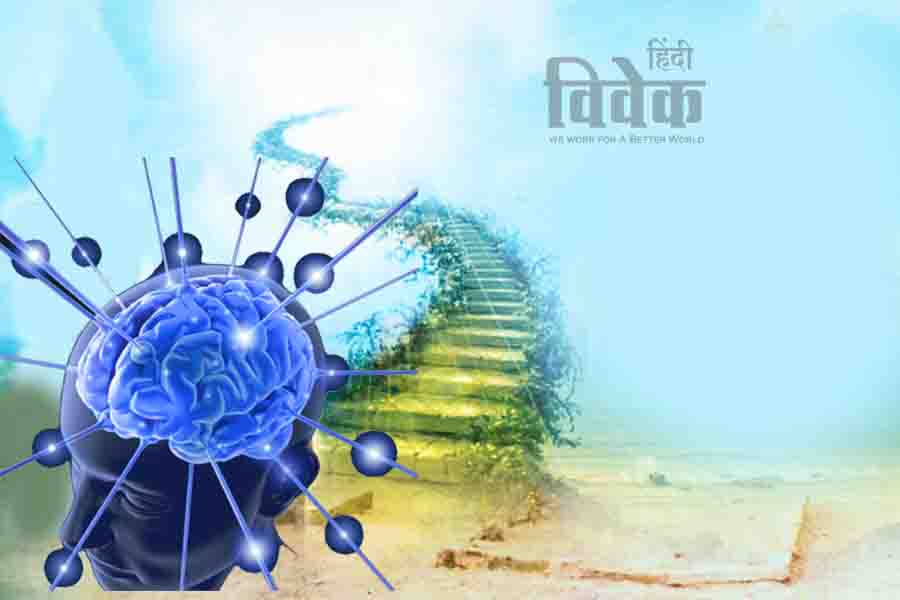स्पिनोज़ा का मानवमुक्ति का सिद्धांत ऋग्वेद की ‘ऋत’ संकल्पना सरीखा ही है। यह संकल्पना कहती है कि आत्मा, जीव, सृष्टि व परमेष्टि को जोड़ने वाला तत्व एक ही है और वह एक विशिष्ट नियम से कार्यरत रहता है। इस तरह स्पिनोज़ा के तत्वज्ञान एवं वेदांत में बहुत समानता है। इस अर्थ में स्पिनोज़ा हिंदू ही थे। ऐसा अनेक पाश्चात्य विचारकों का मानना है।
भारत में पश्चिमी तत्वज्ञान के जानकारों में से अनेक लोगों को बरूच डी स्पिनोज़ा का नाम शायद नहीं मालूम होगा। उनका जन्म 24 नवंबर 1632 में एमस्टरडम में हुआ एवं मृत्यु 21 फरवरी 1677 को हुई। उनका जन्म जिस यहूदी (जू) धर्म मानने वाले घराने में हुआ, उस घराने ने पुर्तगाल में हुए इनक्विजिशन से बचने लिए नीदरलैंड में शरण ली थी। उनका घराना धनी एवं व्यापारी था परंतु स्पिनोज़ा ने तत्वज्ञान के अध्ययन को ही अपना जीवन-कार्य माना। उनके विचारों के कारण यहूदी धर्म गुरूओं ने उन्हें यहूदी धर्म से बहिष्कृत कर दिया था। धर्म गुरूओं के दबाव के कारण स्पिनोज़ा को कुछ समय के लिए एमस्टरडम से देश-निकाला भी दिया गया था। दूरबीन के उत्तल तथा अवतल लेन्स बनाने का उनका व्यवसाय था।
स्पिनोज़ा की जीवनी में हिन्दू तत्वज्ञान के संबध में उनकी जानकारी का कोई उल्लेख नहीं है। परंतु उनका तत्वज्ञान व जीवन तथा हिन्दू तत्वज्ञान का इतना निकट संबध है कि उन्नीसवीं सदी के बाद जब पश्चिमी बुद्धिजीवियों को हिन्दू तत्वज्ञान का परिचय होने लगा तब उनके ध्यान में आया कि स्पिनोज़ा के तत्वज्ञान एवं वेदांत में बहुत समानता है। 19वीं सदी के जर्मन संस्कृतज्ञ थिओडोर गोल्डस्टर के अनुसार, “सभी देशों में एवं हमेशा जिस पश्चिमी तत्वज्ञान ने स्पिनोज़ा के प्रथम श्रेणी का महत्व प्राप्त किया है उसकी वेदांत के तत्वज्ञान से इतनी समानता है कि उसका स्पिनोज़ा की जीवनी में कहीं भी उल्लेख न होने के बावजूद स्पिनोज़ा ने अपने मूलभूत तत्व हिंदुओं से लिए हैं एवं उसकी उसे अच्छी जानकारी है। अपने तत्वज्ञान के अनुसार स्पिनोझा का जीवन किसी सच्चे वेदांती तत्वज्ञ जैसा नैतिक शुद्धता एवं उपभोग-मुक्त जीवन का उत्तम उदाहरण है। इन दोनों के मूलभूत तत्वों की तुलना कर यह स्पष्ट रूप से दर्शाया जा सकता है कि स्पिनोज़ा हिंदू था व उसका तत्वज्ञान वेदांत तत्वज्ञान का अगला अध्याय है।”
मैक्समूलर ने स्पिनोज़ा के विषय में कहा है, “स्पिनोज़ा ने अपने तत्वज्ञान में ‘सबस्टेन्शिया’ की संकल्पना प्रस्तुत की है, जो उपनिषदों द्वारा कल्पित तथा बम्हन की शंकराचार्य द्वारा की गई व्याख्या अनुरूप है।”
ऐसे कुछ और भी उदाहरण दिए जा सकते हैं। भारत में स्पिनोज़ा के तत्वज्ञान के बारे में गहराई एवं गंभीरता से अध्ययन होना आवश्यक था; परंतु स्वतंत्रता के बाद के काल में मार्क्सवाद के प्रभाव के कारण मार्क्स के आगे जाकर बहुत कम लोगों का गंभीरता से विचार किया गया।
स्पिनोज़ा का तत्वज्ञान
स्पिनोज़ा के तत्वज्ञान को दो भागों में बांटा जा सकता है। व्यक्ति का उद्देश्य क्या है एवं उसके विकास की कारण मीमांसा करने वाला पहला भाग एवं राज्यव्यवस्था तथा व्यक्ति के संबध कैसे होने चाहिए इसका विवेचन करने वाला दूसरा भाग। इन दोनों विवेचनाओं का आपस मे संबध है।
सभी महत्वपूर्ण तत्वज्ञान जीवन का मूलभूत उद्देश्य क्या है, इस प्रश्न पर पहुंच जाते हैं। लोकायत तत्वज्ञान का यदि अपवाद छोड दें तो आत्मस्वरूप का दर्शन ही सभी हिंदू चिंतनों की नींव है। उसका स्वरूप एवं उसके दर्शन की पद्धति से अलग-अलग तत्वज्ञानों की उत्पत्ति हुई। क्या आत्मा का स्वरूप बुद्धिग्राह्य है? यह इसमें कूट प्रश्न है। बुद्धि विवेचना करने वाली है तो श्रद्धा के लिए विश्वास आवश्यक है। विश्वास की सीढ़ी चढ़े बिना श्रद्धा के शिखर तक नहीं पहुंचा जा सकता। परंतु जब तक हमारी सभी शंकाओ का समाधान नहीं हो जाता तक बुद्धि विश्वास की सीढ़ी नहीं चढ़ने देती। इसके कारण बुद्धि और अहंकार एक दूसरे से जुड़े हैं। आत्मज्ञान के लिए आत्मविलोप आवश्यक है परंतु बुद्धि अपना अस्तित्व सिद्ध करते रहती है। इस पृष्ठभूमि में स्पिनोज़ा ने यह मेल तर्कशुद्ध पद्धति से किया है।
स्पिनोज़ा के अनुसार परमेश्वर याने प्रकृति यह स्वयंसिद्ध है। उसके अस्तित्व के आगे उसे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। प्रकृति याने ही परमेश्वर। वह परिपूर्ण है एवं विशिष्ट नियमों से बंधा है। मनुष्य भी प्रकृति की निर्मिति होने के कारण प्रकृति एवं मनुष्य का जैविक संबध है। यह संबध व्यक्ति के मन में प्रस्थापित रहता है। व्यक्ति के चारों ओर का वातावरण प्रकृति का भाग होने के कारण उनका सतत एक दूसरे के साथ संपर्क होता रहता है, संवाद होता रहता है। प्रत्येक व्यक्ति में स्वत: के अस्तित्व की रक्षा का महत्वपूर्ण गुण होता है। उस गुण का रक्षण करते हुए हमारी बुद्धि मार्गक्रमण करती है। उसका प्रकृति से जो संवाद होता है उसमें से उसके अस्तित्व रक्षण की दृष्टि से जो प्रतिसाद पैदा होता है उसमें से उसका गुण वैशिष्ट्य प्रकट होता है। व्यक्ति संसार को उपयुक्तता की दृष्टि से देखता है। उसे लगता है कि यह संसार मेरे उपभोग के लिए ही है। वह समझता है कि उसे जो आवश्यक है वह प्राप्त करने की उसे स्वतंत्रता है। यह वैसा ही अज्ञान है जैसे किसी बच्चे को लगता है कि रोने से उसे उसकी इच्छित वस्तु मिल जाएगी या किसी शराबी को लगता है कि शराब पीने के बाद कुछ भी बोलने की उसे आजादी है।
स्पिनोज़ा के समय में तत्वज्ञान पर रेने देकार्त के तत्वज्ञान का प्रभाव था। इसमें मन एवं बुद्धि का अर्थात भावना तथा विचारों का दो स्वतंत्र चिजे हैं ऐसा माना जाता है। मन भावनाओं से जुड़ा है तथा बुद्धि कार्य-कारण भाव से जुड़ी है। यह अंतर करते करते हुए देकार्त ने धर्म तथा विज्ञान का क्षेत्र अलग किया। इसके कारण मानवी व्यक्तित्व की एकरूपता समाप्त हो गई एवं उसमें व्दैत निर्माण हो गया। स्पिनोज़ा ने यह व्दैत अमान्य किया एवं विचार तथा भावना की वैचारिक दृष्टि से एकरूपता स्थापित की। वह स्थापित करते हुए प्रकृति, मन, बुद्धि तथा मानवी व्यवहार की तार्किक रूप से संबध स्थापना की। वह करते हुए उन्होने तीन मूल घटकों को रखा। पहला याने अस्तित्व रूप, दूसरा याने उसके गुण एवं तीसरा याने पद्धति।
एक बार दृष्टिकोण निर्माण होने के बाद भावनाएं नियंत्रण में रहती हैं। इसके लिए मानव मन का विकास होेना आवश्यक है। यह विकास होने के लिए व्यक्ति को होने वाले ज्ञान को स्पिनोज़ा ने अपने विवेचन में तीन भागों में बांटा है। पहला प्रकार याने घटित हो रही घटनाओं को दिया जाने वाला स्वाभाविक प्रतिसाद। इस प्रतिसाद में कोई भी सुसूत्रता नहीं होती केवल अविश्वास होता है। दूसरे प्रकार में मनुष्य अपनी सम्यक् बुद्धि का उपयोग करता है परंतु यह सम्यक् बुद्धि आत्मपरीक्षण तक सीमित रहती है। इस प्रकार को अपूर्ण सद्गुण कहा जाता है। तीसरे प्रकार में जब व्यक्ति के मन में एकात्म भाव जागृत होता है तब प्रकृति की चैतन्यता से वह जुड़ता है एवं तब सच्चे अर्थों में मन के स्वतंत्रता की यात्रा प्रारंभ होती है।
मानवी अस्तित्व प्रकृति के अस्तित्व का ही एक भाग है। अगर ऐसा नहीं होता, तो उसके चारों ओर घटित होने वाली घटनाओं का उस पर असर नहीं होता। भावनाओं के रूप में यह प्रतिसाद मन पर छाप छोड़ता है। यह भावना में दो प्रकार की होती है। पहला प्रकार कार्यशील करने वाली भावनाओं का होता है। जब भावनाएं परिपूर्ण रूप से समझ में आ जाती हैं तब उसमें से कृतिशीलता निर्माण होती है। जब उससे होने वाला बोध परिपूर्ण बोध होने के बाद भी कृतिशील न होने की स्थिति से अलग है। परिपूर्ण बोध होने से भी न की हुई कृति भी कृति ही होती है। परिस्थिति एक होने के बावजूद मनुष्यों द्वारा दिए गए प्रतिसाद अलग-अलग होते हैं। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की आकलन शक्ति का स्वरूप अलग होता है। इस बोधात्मक आकलन के बाद व्यक्ति अपनी कृति के माध्यम से जो प्रतिसाद देता है उसके कारण या तो उसका उन्नयन होता है या अपनयन होता है। इसीसे आनंद या दु:ख की स्थिति निर्मित होती है। इसके साथ ही प्रत्यक्ष कृति न करते हुए भी जिस बात से हमें आनंद मिलता है ऐसी कोई भी बात अन्य कहीं भी घटित हो तो उसके प्रति हमें प्रेम उत्पन्न होता है। जिन बातों से हमें दु:ख होता है ऐसी घटनाएं यदि कहीं घटित होती हैं तो उसके बारे में दु:ख, तिरस्कार या द्वेष होता है। इतिहास में घटित हो चुकीं अथवा भविष्य में घटित होने वाली बातों के बारे में भी हमारे मन में ऐसी ही भावनाएं निर्माण होती हैं। (यही मूल्य भाव निर्माण होने की मानसिक प्रक्रिया है) इन मूल्य भावनाओं के आधार पर ही घटित हुईं या होने वाली घटनाओं के प्रति हमारे मन में प्रेम या दु:ख निर्माण होता है। (इसी में से प्रत्येक व्यक्ति के मन में नायक या खलनायक आकार लेते हैं।) यह महसूस होने की प्रक्रिया की तीव्रता अवलंबित होती है घटनाओं के परिणाम की तीव्रता पर। इसी से आनंददायक प्रतीत होने वाली बातों के निर्माण एवं तिरस्कारयुक्त बातों के विरोध की इच्छा निर्माण होती है। परंतु इसीके साथ ही जिन पर हम प्रेम करते हैं उनके पास यदि आनंद देने वाली बातें है तो वे हमें हासिल करनी चाहिए यह भावना निर्माण होती है और यदि ऐसा नहीं होता तो उस व्यक्ति के बारे में तिरस्कार निर्माण होता है। ऐसे समय जिस पर उस व्यक्ति ने प्रेम किया है वह प्रेम नष्ट करने के लिए हम हमारे मन में और अधिक तिरस्कार की भावना पैदा करते हैं। एक बार जब मन में तिरस्कार की भावना निर्माण हो जाती है तब उस बात को नष्ट करने हेतु व्यक्ति उद्युक्त हो जाता हैं। जैसे धर्मांतरित व्यक्ति और अधिक उत्साह से अपने पुराने धर्म का द्वेष करने लगता है। यदि ऐसा करते समय उसे यह समझ में आता है कि इसमें मेरा नुकसान है तो ही वह उससे परावृत्त होता है। यदि प्रेम करने लायक कोई बात न भी हो तब भी यदि कोई व्यक्ति प्रेम करने लगता है तो उसे प्रेम से ही उत्तर दिया जाता है।
भावना व्यक्ति को बंधनकारक भी होती है और उसमें शक्ति भी होती है। भावनाओं का उपयोग किस प्रकार किया जाए यह केवल व्यक्ति पर ही निर्भर है। प्रकृति इस मामले में तटस्थ है। व्यक्ति जैसा विचार करते हैं, वैसी भावनाएं निर्माण होती हैं, उससे इच्छा निर्माण होती है एवं इच्छाओं का रूपांतरण कृति में होता है। कर्मों के अच्छे बुरे परिणाम व्यक्ति को भोगने पड़ते हैं। स्पिनोज़ा के अनुसार मन में निर्मित इच्छा तभी बदल सकती है जब उससे अधिक प्रबल इच्छा निर्माण हो। प्रत्येक भावना का आधार इस बात पर निर्भर होता है कि उससे आनंद प्राप्त होगा कि दु:ख। इससे व्यक्ति की सुख, दु:ख के विषय में क्या कल्पना है, इस पर भावनाओं की गुणवत्ता परखी जाती है। यदि कोई बात घटित होने की मन को पूर्ण संभावना हो तो भावनाओं की तीव्रता बढ़ती है। यदि इस प्रकार की भावनाओं को इतिहास का आधार हो तो भावना अधिक विश्वासयुक्त होती है। यदि किसी व्यक्ति को अच्छे-बुरे की समझ है तो पैदा होने वाली भावनाओं पर नियंत्रण रख सकता है। इसके कारण अच्छी एवं बुरी भावनाओं का विवेकपूर्ण विश्लेषण कैसे हो यह प्रश्न निर्माण होता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने अस्तित्व की रक्षा हेतु एवं वह और सुरक्षित हो, विकसित हो इसके लिए निर्णय करता है, इसके कारण मेरे अस्तित्व का क्या प्रयोजन है इसका विचार करता है एवं निर्णय लेता है। यहीं पर बुद्धि का अर्थात कार्यकारणभाव का प्रश्न निर्माण होता है। इसके कारण मन की दृष्टि से अच्छे बुरे का निर्णय उसके अस्तित्व के प्रयोजन से जुड़ा रहता है। इस प्रयोजन के संदर्भ में जिन लोगों की वृत्ति एक जैसी हैं वे लोग स्वाभाविकत: एकसाथ आते हैं। एकसाथ रहने के लिए वे अपनी बुद्धि का उपयोग करते हैं एवं समान हितसंबंधों के मुद्दे निश्चित करते हैं।
इस सब प्रक्रिया से मानव मुक्ति का मार्ग कैसे ढूंढ़ा जाए यह प्रश्न निर्माण होता है। इसके लिए स्पिनोज़ा ने तीन तत्व निश्चित किए हैं। विश्व में एकात्म भाव यह पहला तत्व, जो घटित हो रहा है वह नियमानुसार है यह दूसरा तथा व्यक्ति प्रकृति में एक ही चैतन्य भाव भरा है, यह तीसरा तत्व। इसके कारण जो भावनाएं इस एकात्म भाव की ओर ले जाती हैं, उसकी नियमबद्धता का आकलन कर लेती हैं वे भावनाएं अच्छी भावनाओं की निर्मिति करती हैं। यह एकात्म भाव निर्माण होने के बाद वह केवल भावना नहीं होती तो उससे एक दृष्टिकोण तैयार होता है। एक बार दृष्टिकोण निर्माण होने के बाद भावनाएं नियंत्रण में रहती हैं। इसके लिए मानव मन का विकास होेना आवश्यक है। यह विकास होने के लिए व्यक्ति को होने वाले ज्ञान को स्पिनोज़ा ने अपने विवेचन में तीन भागों में बांटा है। पहला प्रकार याने घटित हो रही घटनाओं को दिया जाने वाला स्वाभाविक प्रतिसाद। इस प्रतिसाद में कोई भी सुसूत्रता नहीं होती केवल अविश्वास होता है। दूसरे प्रकार में मनुष्य अपनी सम्यक् बुद्धि का उपयोग करता है परंतु यह सम्यक् बुद्धि आत्मपरीक्षण तक सीमित रहती है। इस प्रकार को अपूर्ण सद्गुण कहा जाता है। तीसरे प्रकार में जब व्यक्ति के मन में एकात्म भाव जागृत होता है तब प्रकृति की चैतन्यता से वह जुड़ता है एवं तब सच्चे अर्थों में मन के स्वतंत्रता की यात्रा प्रारंभ होती है। एक बार जब यह एकात्म भाव निर्माण हो गया तब उसमें से विशुद् प्रेम की निर्मिति होती है। शरीर का नाश होता है परंतु मन अविनाशी है। इसके कारण मृत्यु के बाद शरीर का विनाश होने के बाद भी मन शेष रहता है। जिस मन को प्रकृति की चेतना का साक्षात्कार होता है उसकी बुद्धि शुद्ध होती है। अपना मन अविनाशी है इसका साक्षात्कार होने के बाद हमारी इच्छाओं को इस विनाशी संसार से मर्यादित रखने की अपेक्षा प्राकृतिक चैतन्य की अनुभूति लाने की इच्छा बलवत्तर होती है एवं उसमें से वास्तविक स्वतंत्रता के मार्ग पर मार्गक्रमण प्रारंभ होता है।
स्पिनोज़ा का मानवमुक्ति का सिद्धांत ऋग्वेद की ‘ऋत’ संकल्पना सरीखा ही है। यह संकल्पना कहती है कि आत्मा, जीव, सृष्टि व परमेष्टि को जोड़ने वाला तत्व एक ही है और वह एक विशिष्ट नियम से कार्यरत रहता है। मनुष्य के मन पर अज्ञानता का आवरण होता है इसलिए वह इस तत्व के विषय में अज्ञानी होता है।
स्पिनोज़ा का तत्वज्ञान निश्चिततावाद में शुमार है।