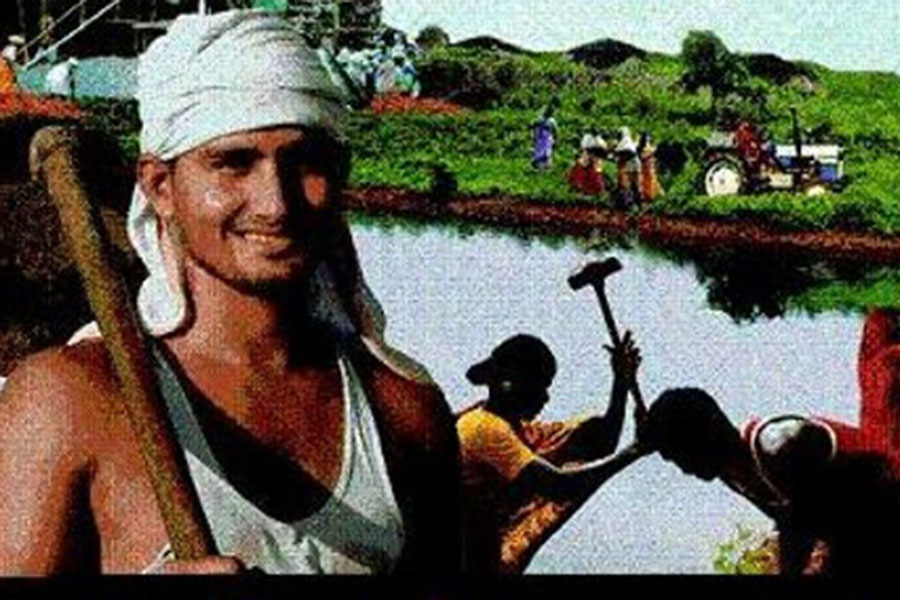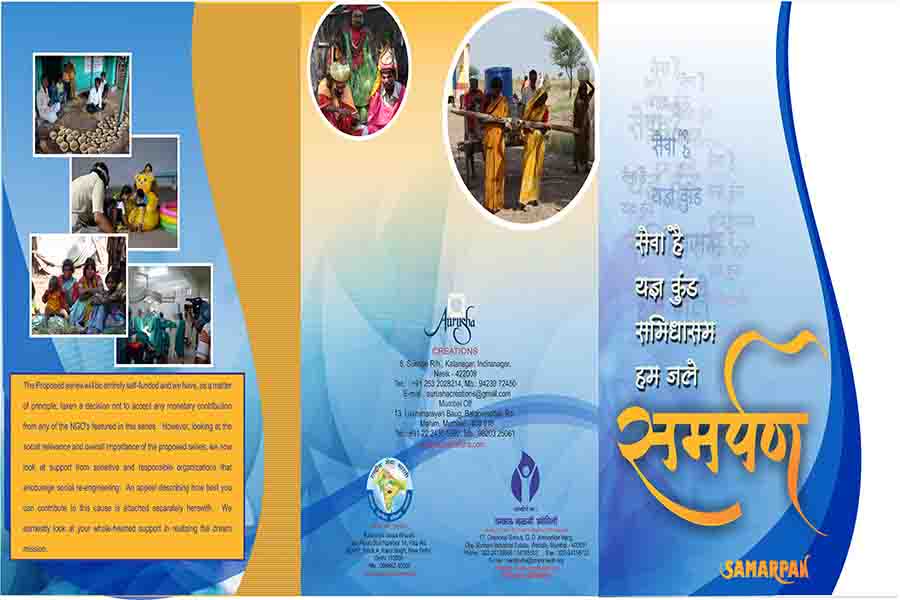यदि आप डूल्टन के मिट्टी के बरतनों के कारखानों को देखने जाएं तो सौजन्यता के साथ आपको टाल दिया जाएगा। फिर भी हिंदुस्थानी कारीगरों को मजबूर किया गया कि वे अपने कपड़ों के थानों को धोकर सफेद करने के तरीके और अपने दूसरे औद्योगिक रहस्य मैनचेस्टर वालों को प्रकट कर दें। अंतत: उन्हें रहस्य खोलने पड़े।
ॠग्वेद की एक ॠचा है, ‘विश्व पुष्टं ग्रामीण आसमिन अनातुरम‘ अर्थात मेरे गांव से ही मुझे विश्व के होने की पुष्टि होती है। मसलन खुशहाली और समृद्धि से परिपूर्ण ऐसे गांव हों,जहां से विश्व के उत्थान और संपन्नता का रास्ता खुलता हो। एक समय हमारे गांव वास्तव में समृद्धि के ऐसे ही स्रोत थे, इसीलिए देश सोने की चिड़िया कहलाता था। ॠग्वेद के इसी मंत्र से प्रेरणा लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ‘ग्राम उदय से भारत उदय‘ की रचनात्मक पहल की है। यह निश्चय ही स्वागत योग्य है। इस लिहाज से जरूरी है कि 15 लाख गांवों को कृषि और कृषि आधारित उन लघु-कुटीर उद्योगों की श्रृंखला से जोड़ा जाए, जिनके चलते देश अतीत में सोने की चिड़िया कहलाता था।
भारत के गांव कितने समृद्धिशाली थे, इस तथ्य की पड़ताल यदि अतीत से करें तो पता चलता है कि ब्रिटेन का औद्योगिक साम्राज्य हमारे गांवों से लूटी गई धन-संपदा की ही नींव पर खड़ा हुआ था। अंग्रेजों की इस लूट का हैरतअंगेज खुलासा यहां अंग्रेज लेखकों की पुस्तकों से करते हैं। ब्रुक्स एडम्स ने अपनी पुस्तक ‘द लॉ ऑफ सिविलाइजेशन एंड डीके‘ में लिखा है,‘शायद दुनिया के शुरू होने से अब तक कभी भी,किसी भी पूंजी से इतना लाभ किसी भी व्यवसाय में नहीं हुआ है, जितना भारतवर्ष की लूट से अंग्रेजों को हुआ। क्योंकि यहां करीब 50 साल तक इंगलिस्तान से कोई मुकाबला करने वाला नहीं था। इस लूटे गए धन का उपयोग 1760 से 1815 के बीच अंग्रेजों ने अपने देश के औद्योगिक विकास में लगाया।‘ वाकई ब्रिटेन का यही वह समय था,जब वहां आश्चर्यजनक उन्नति हुई। अकेली मुर्शिदाबाद की लूट का हवाला देते हुए अंग्रेज इतिहासकार ऑर्म ने अपनी किताब ‘हिस्ट्री ऑफ हिंदुस्तान‘ में लिखा है, 6 जुलाई 1757 तक कलकत्ते की अंग्रेज कमेटी के पास चांदी के सिक्कों के रूप में 72 लाख 71 हजार 666 रुपए पहुंच गए थे। यह खजाना 100 संदूकों में भरकर 100 किश्तियों के जरिए नदियों तक पहुंचाया गया। वहां से अंग्रेजी जंगी जहाजों के मार्फत झंडे फहराते व विजय का डंका पीटते हुए इस धन को ब्रिटेन रवाना किया गया। इससे पहले अंग्रेज कौम को एक साथ इतना अधिक नगद धन कहीं से नहीं मिला था।‘ विलियम डिग्बे ने लिखा है, ‘प्लासी से वाटर लू तक यानी 1757 से 1815 के बीच करीब एक हजार मिलियन पौंड यानी 15 अरब रूपए भारत से लूटकर इंगलिस्तान भेजे गए। मसलन इन 58 वर्षों में 25 करोड़ रुपए सालाना कंपनी के अधिकारी भारतीयों को लूटकर ब्रिटेन भेजते रहे। इस लूट की तुलना में महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी की लूटों की तुलना के बरक्स पहाड़ की तुलना राई से करने जैसी है।
इन बानगियों से स्पष्ट होता है कि भारत के गांवों में न केवल खेती-किसानी उन्नत थी,बल्कि लघु व कुटीर उद्योग भी गुणवत्तापूर्ण उत्पादकता के चरम पर थे। उस समय तक न तो हमारे यहां उद्योगों का यांत्रिकीकरण हुआ था और न ही हम वस्तुओं का आयात दूसरे देशों से करते थे। बावजूद ज्ञान परंपरा के बूते आत्मनिर्भर थे। स्वाधीनता के बाद जगह-जगह कृषि विश्वविद्यालय, कृषि विज्ञान व अनुसंधान केंद्र और प्रशिक्षण केंद्र खोले गए। इन संस्थागत ढांचों ने हमारी पारंपरिक खेती का अध्ययन किए बिना ही विदेशी तकनीकों को अपनाकर खुद अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम किया। इस तकनीक से 50 साल के भीतर ही शत-प्रतिशत खेती का यांत्रिकीकरण हो गया। किसान को कर्ज देकर ट्रेक्टर व अन्य कृषि उपकरण खरीदवाए गए। तब यह वातावरण बन गया था कि ट्रेक्टर प्रगतिशील कृषक की निशानी है। किंतु कालांतर में यही लाभदायी दर्शन, महंगी खेती का कारण तो बना ही,किसान की अर्थव्यवस्था को चौपट करने का सबब भी बना। इस आग में घी डालने का काम रासायनिक खाद और कीटनाशक दवाओं ने किया। इन उपायों ने एक ओर जहां भूमि की सेहत खराब की,वहीं दूसरी तरफ कर्ज का मारा किसान आत्महत्या को विवश हुआ। बावजूद हमारी नीतियां खेती में मशीनीकरण को बढ़ावा देने में लगी हैं। कृषि विश्वविद्यालय वही पाठ्यक्रम पढ़ा रहे हैं, जो अमेरिका और ब्रिटेन की कृषि एवं अर्थव्यवस्था के अनुरूप बने हैं। हमारी पारंपरिक खेती में रासायनिक खाद एवं कीटनाशकों का उपयोग वर्जित है। क्योंकि हमारे यहां केचुएं जैसे कीट खेत की मिट्टी को जैविक तरीके से उपजाऊ बनाने का काम करते हैं। लेकिन आयातित शिक्षा के अनुरूप जब हमने कीटनाशकों का उपयोग बड़े पैमाने पर शुरू कर दिया तो हमारे खेतों से केंचुआ लुप्त हो गया। अमेरिकी जमीन में कीटनाशक इसलिए लाभदायी हो सकते हैं,क्योंकि वहां बर्फीली भूमि और तापमान कम होने के कारण केंचुआ पाया ही नहीं जाता है। गोया कृषि पाठ्यक्रमों को भी भारतीय भूमि और भूगोल के अनुसार बदलने की जरूरत है ?
हालांकि अब बदलाव आ रहा है। वर्मी कॉम्पोस्ट प्रक्रिया के जरिए केंचुए पैदा करके खेतों में डाले जा रहे हैं। रासायनिक खाद के बदले गोबर, गौमूत्र और नीम के घोल के उपयोग किए जाने लगे हैं। किंतु यह परिवर्तन तब आया,जब हमने पंजाब की बरबादी से सबक लिया। पंजाब भारत में रासायनिक खादों और कीटनाशकों का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करने वाला राज्य है। पंजाब में भी इसका सबसे अधिक उपयोग मालवा क्षेत्र में हुआ। इनकी अधिकता ने मानव स्वास्थ्य और स्थानीय पर्यावरण को इतना नुकसान पहुंचाया कि आज पूरा मालवा क्षेत्र कैंसर के भयावह संकट से जूझ रहा है। यहां की मिट्टी की उर्वरा क्षमता का नाश हो चुका है। बावजूद अभी कृषि नीतियों में व्यापक बदलाव के संकेत नहीं मिल रहे हैं।
भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के बाद अंग्रेजों ने बड़ी चतुराई से पहले भारत में देशी उपकरणों व तरीकों से की जाने वाली खेती को समझा और फिर उसे मशीनीकरण में बदलने के षड्यंत्रकारी उपाय किए। भारत की खेती को उन्नत और वैज्ञानिक बताते हुए 1795 में कैप्टन थॉस हालकॉट ने कंपनी को लिखे एक पत्र में लिखा, ‘अब तक मैं मानता था कि कतारबद्ध जुताई एवं बुवाई आधुनिक यूरोप का आविष्कार है,लेकिन अभी मैं दक्षिण भारत के एक खेत से गुजरा तो खेती की तकनीक देखकर हैरान रह गया। मैंने पंक्तिबद्ध हल-बैलों से जुताई देखी। वह अद्वितीय हल भी देखा,जो बेहद कलात्मक तरीके से बनाया गया था। किसानों से पूछने पर पता चला कि इसी तरीके से पूरे देश में जुताई व बुवाई होती है। कई प्रकार के अनाज, दालों, कपास, सन और तिलहन फसलें उगाई जाती हैं। बीज बोने की यहां जो तकनीक हाथ से अमल में लाई जाती है,वह ब्रिटेन में अपनाई जाने वाली यांत्रिकीकरण से कहीं ज्यादा कारगर है। यहां प्रयोग में लाया जाने वाला हल भी हमारे यांत्रिक हल से कहीं ज्यादा बेहतर, सस्ता और सरल है। इसे खराब होने पर स्थानीय बढ़ई ही दुरूस्त कर देते हैं।‘
इस जानकारी के बाद फिरंगियों ने ब्रिटेन में निर्मित खेती के काम आने वाले यांत्रिक उपकारणों को भारत लाना और उनसे खेती करने का रास्ता प्रशस्त करने की विधि अपनाई। इसके बाद उत्तरोत्तर ऐसा मशीनीकरण होता चला आ रहा है कि हम आजादी के 70 साल बाद भी उससे छुटकारा नहीं पा पाए हैं। आज कृषि और किसान की दुर्दशा का यही यांत्रिकीकरण प्रमुख कारण है।
ग्रामोदय से भारतोदय करना है तो कृषि को देशज उपायों से उन्नत करने के साथ लघु एवं कुटीर उद्योगों को भी ग्राम व कस्बाई स्तर पर सक्षम करना होगा। क्योंकि अकेली फसल उगाकर किसानों के समृृद्धि की बात तो छोड़िए, उन्हें पेट पालना भी मुश्किल है। अंग्रेजों के हुक्मरान बनने से पहले तक हम वस्त्र, लौह, जहाजरानी, चीनी और कागज निर्माण के उद्योगों में अग्राणी देश थे। वस्त्र रंगाई की कला में हमारे शिल्पकार अत्यंत निपुण थे। यही वजह है कि आज भी वाराणसी, चंदेरी और महेश्वर में उच्च गुणवत्ता की साड़ियां हथकरघों से बनाई जा रही हैं। ज्ञान परंपरा से दक्ष इन कारीगरों से सीखने की बजाए हम कौशल प्रशिक्षण में करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। संस्थागत प्रशिक्षक सैद्धांतिक ज्ञान तो साझा कर सकते हैं, लेकिन प्रायोगिक ज्ञान में वे सर्वथा अनभिज्ञ होते हैं। नतीजतन हमारे जिला उद्योग केंद्र अर्जियों को कर्ज हेतु बैंकों तक पहुंचाने का जरिया भर बनकर रह गए हैं। तकनीक के व्यावहरिक ज्ञान में यह पूरा संस्थागत ढ़ांचा लगभग शून्य है। वैसे भी कोई एक दिमाग हजारों प्रकार के वस्तु निर्माण की जानकारी देने में निपुण नहीं हो सकता है। अंग्रेजी शिक्षा और आयातित तकनीक के मोह ने हमें इतना दिग्भ्रिमित कर दिया है कि आज हम यह मानने को शायद ही तैयार हों कि लघु उद्योगों की तकनीकें फिरंगियों ने हमसे चुराई थीं। भारत वस्तुओं के निर्माण में अपनाई जाने वाली तकनीक की द़ृष्टि से कितना बहुआयामी देश था, इसे पहले अंग्रेजों की भाषा में ही जानते हैं।
उद्योगों से जुड़ी तकनीकों के रहस्य-सूत्र पहले फिरंगियों ने शिल्पकारों से रजामंदी से जानना चाहे, किंतु जब इसमें उन्हें सफलता नहीं मिली तो उन पर अमानुषिक जुल्म ढाए गए। जे.बी. कीथ ने 7 सितंबर 1891 के ‘पायनियर‘ में लिखा है, ‘हर कोई जानता है कि शिल्पकार एवं कारीगर अपने पेशागत रहस्यों को सावधानीपूर्वक छिपाकर रखते हैं। यदि आप डूल्टन के मिट्टी के बरतनों के कारखानों को देखने जाएं तो सौजन्यता के साथ आपको टाल दिया जाएगा। फिर भी हिंदुस्तानी कारीगरों को मजबूर किया गया कि वे अपने कपड़ों के थानों को धोकर सफेद करने के तरीके और अपने दूसरे औद्योगिक रहस्य मैनचेस्टर वालों को प्रकट कर दें। अंतत: उन्हें रहस्य खोलने पड़े। इंडिया हाउस के महकमे ने एक कीमती संग्रह तैयार किया, ताकि उसकी मदद से मैनचेस्टर दो करोड़ पौंड अर्थात 30 करोड़ रुपए सालाना भारत के शिल्पकारों से वसूल सकें। इस तकनीकी अध्ययन संग्रह की प्रक्रिया ब्रिटेन के व्यापारियों के संगठन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स को मुक्त भेंट की गई और देश की प्रजा को उसकी कीमत चुकानी पड़ी। संभवत: राजनीति के अर्थशास्त्र की द़ृष्टि से यह सब जायज हों, किंतु वास्तव में इस तरह के काम में प्रच्छन्न रूप से लूट की हैरतअंगेज भावना अंतनिर्हित है।‘
इस संग्रह में 700 प्रकार की वस्तुओं के नमूने और तरीके 18 बड़ी जिल्दों में इकट्ठे किए गए। संग्रह की 20 प्रतियां तैयार की गईं। इनमें से 18 जिल्दें ब्रिटेन के औद्योगिक प्रतिष्ठानों में रखी गईं। इस संग्रह को तैयार करके अंग्रेजों ने एक तीर से दो निशाने साधे। एक तो ब्रिटेन के कारीगरों को इस तकनीक में दक्ष किया और फिर वैसी ही वस्तुओं का निर्माण कराया। इसी प्रकारांतर में फिरंगियों ने भारतीय शिल्पकारों पर इतने जुल्म ढाए कि आजीविका से तो उन्हें हाथ धोने ही पड़े,उनके अंग-भंग भी किए गए। यहां तक कि जिन्होंने विद्रोही तेवर दिखाए, उन्हें प्राण भी गंवाने पड़े। कालांतर में 11 सितंबर 1813 को मार्क्विस हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल की हैसियत से भारत आया तो उसने अपने पूर्ववर्तियों की बर्बरतापूर्ण कार्यवाहियों को एक ऐसी नीति का रूप दे दिया, जिससे भारत के उद्योग-धंधे चौपट होते चले गए और ब्रिटेन के उद्योगों व उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं की उन्नति होने लग गई। इस बाबत यूरोपियन लेखक रॉबर्टसन ने लिखा है, ‘1760 तक ब्रिटेन में सूत कातने के यंत्र आविष्कार की अत्यंत आरंभिक अवस्था में तो थे ही, बेडौल भी थे, जबकि भारत में यही यंत्र बेहद उन्नत किस्म के थे।‘
गोया, जब ब्रिटेन हमारे कपड़ा उद्योग पर अतिक्रमण कर रहा था, तब हमारे यहां 2400 और 2500 काउंट के महीन धागे बनाने में जुलाहे निपुण थे। केवल एक ग्रेन में 29 गज लंबे धागे हमारे कारीगर बना लिया करते थे। जबकि आज हम जिस कंप्यूटराइन्ड उन्नत व आधुनिकतम तकनीक की बात करते हैं, उसके जरिए भी 400 से 600 काउंट तक के धागे बनाए जाना संभव हो पा रहा है। ढाका और मुर्शिदाबाद में 2400 से लेकर 2500 काउंट तक के महीन धागे बनाए जाते थे। कारीगरों की इस दक्षता को नष्ट करने के लिए अंग्रजों द्वारा निर्ममतापूवर्र्क उनके अंगूठे काट दिए थे। इस दुष्टता के बाद भारत में ब्रिटेन के कपड़ा उद्योग को स्थापित करने का मार्ग खुल पाया था।
चार्ल्स ट्रेविलियन ने 1884 में एक रोजनामचे में लिखा है, ‘1816 में जितना सूती कपड़ा बंगाल से विदेशों को भेजा गया, उसका मूल्य 1,65,94,380 रुपए था। इसके बाद यह घटकर 1832 में 8,32,891 रुपए रह गया। इसके विपरीत ब्रिटेन का बना हुआ जो कपड़ा बंगाल में आया, उसका मूल्य 1814 में महज 45000 रुपए था, जिसकी खपत 1816 में बढ़कर 3,17,603 रुपए हो गई।‘ 1828 में यही खपत बढ़कर 79,96,383 रुपए हो गई। भारत वस्त्र निर्माण में इतना सक्षम देश था कि उसे 1832 तक एक गज सूत भी विदेश से आयात करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, किंतु 1828 में करीब 80,00000 रुपए के कपड़ों के अतिरिक्त 35,22,640 रुपए का सूत भी ब्रिटेन से बंगाल आया। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि जो देशी वस्त्र बुनकर तथा कपास व सूत उत्पादक किसान इस व्यवसाय से करीब 1,80,00000 रुपए की पूंजी का वार्षिक उत्पादन किया करते थे, उनके आर्थिक स्रोत छिनने के बाद वे किस बदहाली में रहे होंगे? गोया, हमें घरेलू स्तर पर आयात के नीतिगत उपायों को ग्रामीण अर्थव्यवस्था की लाभ-हानि के स्तर पर समझना होगा ? इस द़ृष्टि से नरेंद्र मोदी नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार ने अहम् निर्णय बीते सालों में लिए हैं। किसान की आय बढ़ाने से लेकर फसल पर न्यूनतम मूल्य भी बढ़ाए हैं। ग्रामीण स्त्रियों को गेस सिलेंडर और शोचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं देकर उनके जीवन को सुरक्षित बनाने के सार्थक उपाय किए हैं। आयुषमान योजना भी गरीब, किसान और मजदूरों को गंभीर बीमारियों से निजात दिलाने का काम कर रही है। युवाओं को डिजीटल मध्ययमों में आर्थिक छूट देकर ग्रामीण उद्यमिता के लिए प्रोत्साहित किया है। इन संदर्भों में यदि चीन से लघु व कुटीर उद्योगों से जुड़ी सामग्री आयात करना बंद कर दिया जाए तो इन योजनाओं की उपलब्धियां सार्थक दिखने लग जाएंगी।