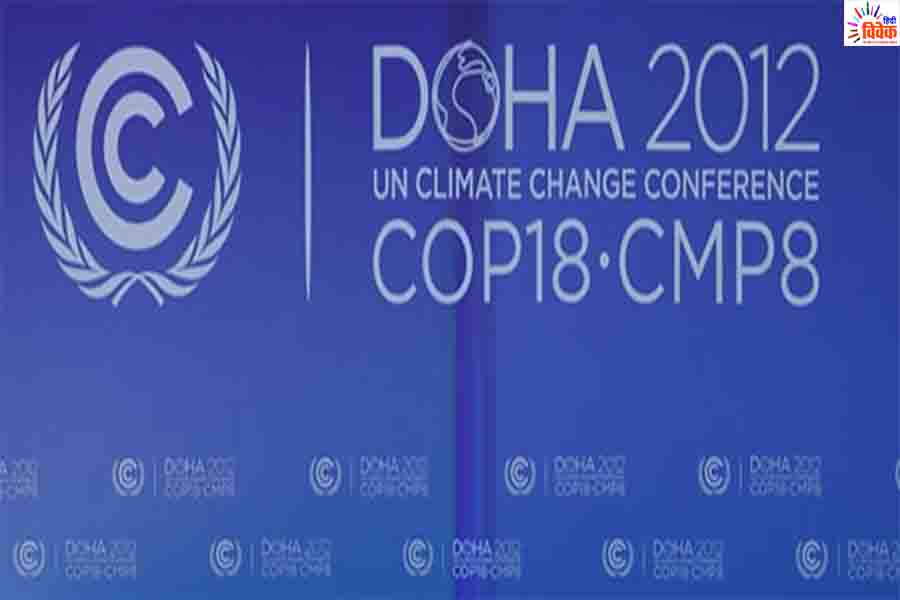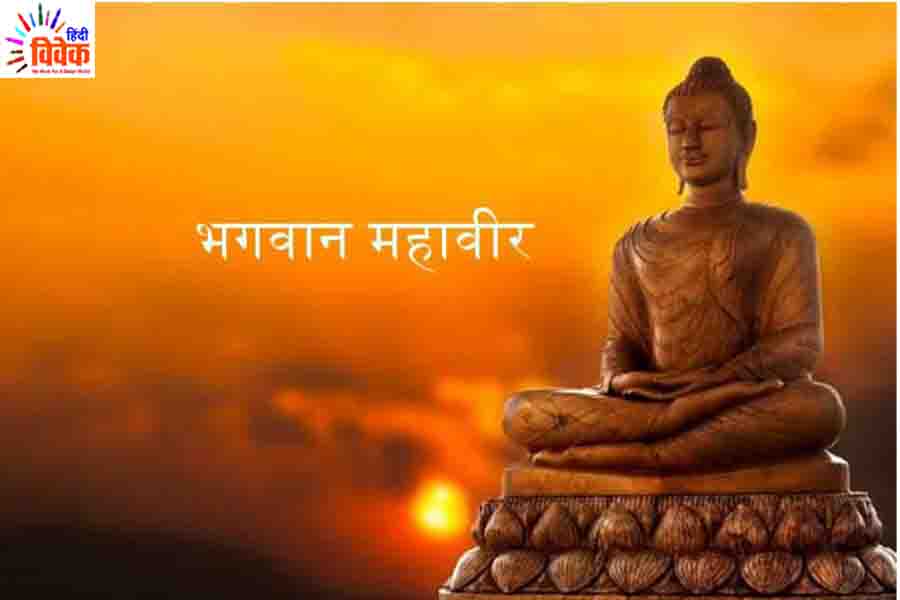भौतिक उन्नति और भोगवादी प्रवृत्ति के कारण इस समय समूचा भूमण्डल पर्यावरण के संकट में घिर गया है। दुनिया भर के पर्यावरण शास्त्री, विशेषज्ञ, वैज्ञानिक और जनप्रतिनिधि जलवायु में हो रहे परिवर्तन से चिन्तित हैं। वैश्विक सम्मेलनों में विविध स्तरों पर इस संकट से निकलने की चर्चाएं हो रही हैं। किन्तु सबसे बड़ी विडम्बना यह है कि बड़े पैमाने पर पूरे विश्व को पर्यावरण संकट में डालने वाले धनी और सुविधाभोगी देश अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं।
जलवायु परिवर्तन के खतरों से निपटने के मुद्दे पर कतार की राजधानी दोहा में पिछले वर्ष-2012 के दिसम्बर माह में आयोजित वार्ता सम्मेलन बिना किसी ठोस नतीजे पर पहुंचे ही समाप्त हो गया। यह 18 वां मौका था जब दुनिया भर के देश कार्बन उत्सर्जन, उससे उत्पन्न खतरों और संकट से बाहर निकलने का मार्ग तलाशने के लिए इकट्ठा हुए थे। मुद्दा हर बार की तरह ही इस बार भी वही था कि दुनिया को जलवायु परिवर्तन के खतरों से कैसे बचाया जाए।
आज से बीस वर्ष पूर्व सन् 1992 में ‘यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन आन क्लाइमेट चेन्ज’ बना था। तभी से विश्व भर के देशों के बीच जलवायु परिवर्तनों से निपटने के उपायों पर चर्चा शुरू हुई। किन्तु इनसे निपटने के लिए कोई ठोस रणनीति हम नहीं बना पाये हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो इस सम्मेलन में अब तक काम नहीं हुआ, सिर्फ जलवायु परिवर्तन पर राजनीति होती आयी है। विश्वस्तरीय पर्यावरण वार्ताओं में दो शब्दों का प्रमुखता से इस्तेमाल होता रहा है- मिटिगेशन और एडैप्टेशन। मिटिगेशन का तात्पर्य उन गैसों के उत्सर्जन में कटौती से है, जिनकी वजह से धरती गर्म हो रही है। एडैप्टेशन का मतलब ऐसे उपायों से है, जिनसे जलवायु संकट कम किया जा सके।
क्योटो प्रोटोकाल-
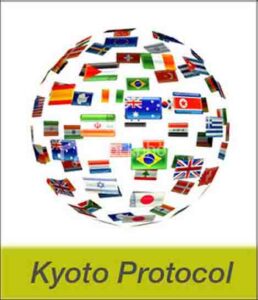 पर्यावरण को क्षति पहुँचाने वाली गैसों के उत्सर्जन के विषय पर जापान के शहर क्योटो में दिसम्बर, 1997 में कांफ्रेन्स आफ पार्टीज की तीसरी बैठक हुई थी। जलवायु परिवर्तन के विषय पर अब तक की सभी बैठकों में इसका सर्वाधिक महत्व है। इस बैठक में दुनिया भर के डेढ़ सौ देशों ने भाग लिया था। गम्भीर चर्चा के उपरान्त एक संयुक्त प्रस्ताव पारित किया गया जिसे ‘क्योटो प्रोटोकाल’ के नाम से जाना जाता है। इस क्योटो प्रोटोकाल में कुछ यूरोपीय और औद्योगिक देशों के लिए वर्ष 2008 से 2012 तक वर्ष 1990 के स्तर से 6 से 8 प्रतिशत ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन घटाने की कानूनी बाध्यता तय की गयी। किन्तु खेद उस बात का है कि इस कानून की सीमा में आने वाले पश्चिमी और अमेरिकी देश इससे बाहर निकलने का मार्ग ही तलाशते रहे। इसे लागू करने में उन्होंने कभी रूचि नहीं ली।
पर्यावरण को क्षति पहुँचाने वाली गैसों के उत्सर्जन के विषय पर जापान के शहर क्योटो में दिसम्बर, 1997 में कांफ्रेन्स आफ पार्टीज की तीसरी बैठक हुई थी। जलवायु परिवर्तन के विषय पर अब तक की सभी बैठकों में इसका सर्वाधिक महत्व है। इस बैठक में दुनिया भर के डेढ़ सौ देशों ने भाग लिया था। गम्भीर चर्चा के उपरान्त एक संयुक्त प्रस्ताव पारित किया गया जिसे ‘क्योटो प्रोटोकाल’ के नाम से जाना जाता है। इस क्योटो प्रोटोकाल में कुछ यूरोपीय और औद्योगिक देशों के लिए वर्ष 2008 से 2012 तक वर्ष 1990 के स्तर से 6 से 8 प्रतिशत ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन घटाने की कानूनी बाध्यता तय की गयी। किन्तु खेद उस बात का है कि इस कानून की सीमा में आने वाले पश्चिमी और अमेरिकी देश इससे बाहर निकलने का मार्ग ही तलाशते रहे। इसे लागू करने में उन्होंने कभी रूचि नहीं ली।
दरअसल क्योटो प्रोटोकाल में बचाव के कुछ रास्ते भी हैं। एक व्यवस्था के अनुसार यदि औद्योगिक देश ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन अधिक करते हैं, तो वे गरीब देशों से उत्सर्जन का व्यापार कर सकते हैं। अर्थात उत्सर्जन क्रेडिट अथवा उधार ले सकते हैं। इसके बदले उन्हें उसका मूल्य चुकाना होगा। इसी की आड़ में धनी देश। इसी की आड़ में धनी देश अब तक बचते आ रहे हैं। यही कारण है कि दिसम्बर, 2012 में आयोजित सम्मेलन भी बिना किसी निष्कर्ष पर पहुंचे समाप्त हो गयी। यही नहीं क्योटो प्रोटोकाल को एक प्रकार से ताक पर रख दिए जाने से मिटिगेशन की बात ही ठंढ़े बस्ते में चली गयी है।
अमीर बनाम गरीब देश-
जलवायु परिवर्तन को लेकर अब तक हुई वैश्विक बैठकों का केन्द्र बिन्दु असली समस्या से ज्यादा अमीर देशों के हितों पर आधारित रहा। एक तरह से यह मोर्चा अमीर और गरीब देशों के बीच लड़ाई का मोर्चा बन गया है। न तो अमीर देश अपनी जिम्मेदारी को समझ रहे हैं, और न ही गरीब देश किसी मध्यमार्ग पर चलने को तैयार हैं। इस बार दोहा सम्मेलन में यह खुलकर दिखाई दिया। धनी और निर्धन देशों के बीच कार्बन उत्सर्जन को लेकर काफी गहरा मतभेद बना रहा। धनी और निर्धन देशों के बीच कार्बन उत्सर्जन को लेकर काफी गहरा मतभेद बना रहा। धनी और औद्योगिक देश ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए जलवायु सम्बन्धी वित्तपोषण और प्रौद्योगिकी अन्तरण को लेकर अभी भी कोई वचन देने को राजी नहीं हैं। वे बराबरी का हक चाहते हैं, जो निर्धन और विकासशील देशों को मन्जूर नहीं है। हालांकि तमाम गतिरोधों के बीच दोहा के इस सम्मेलन में क्योटो प्रोटोकाल की अवधि बढ़ाने पर सहमति बन गयी है, जिसके माध्यम से वर्ष 2020 तक कुछ धनी देशों में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को नियंत्रित किया जाएगा।
क्लाइमेट गेटवे
दोहा सम्मेलन में करीब दो सौ देशों ने क्योटो प्रोटोकाल को अगले आठ वर्षों तक कायम रखने पर सहमति जताई। किन्तु यह समझौता कुछ ही देशों पर लागू होगा। ये वे देश हैं, जो दुनिया की कुल ग्रीन हाउस गैसों का 15 प्रतिशत उत्सर्जन करते हैं। भारत सहित चीन और अमेरिका जैसे बड़े प्रदूषक देश इसके दायरे से बाहर होंगे। यूरोपीय संघ, आस्ट्रेलिया, स्वीटजरलैण्ड और आठ अन्य औद्योगिक राष्ट्रों ने वर्ष 2020 तक उत्सर्जन कटौती के बाध्यकारी समझौते पर हस्ताक्षर किए। सम्मेलन के अध्यक्ष अब्दुल्ला बिन हमद अल अतिया ने इस समझौते को ‘दोहा क्लाइमेट गेटवे’ बताया। वर्ष 2012 में समाप्त हुआ यह ऐतिहासिक समझौता वह एकमात्र उपाय है, जो औद्योगिक देशों को कार्बन उत्सर्जन में कटौती के लिए बाध्य करता है। इस बार भी दोहा सम्मेलन में धनी और निर्धन देश लांग टर्म को आपरेटिव एक्शन (एलसीए) को लेकर सहमत नहीं हुए हैं और न ही धनी देशों द्वारा पर्यावरण संकट का सामना करने के लिए गरीब देशों को वित्तीय सहायता का कोई आश्वासन ही दिया गया है। यहाँ तक कि अमेरिका ने इस सम्मेलन के तहत खुद को किसी नए समझौते से जोड़ने की बात से ही इन्कार किया है। रूस ने प्रस्ताव को खारिज कर दिया जबकि जी-77, चीन और बेसिक समूह के देशों ने दोहा के नतीजों का स्वागत किया है। सम्मेलन में यह निर्णय भी हुआ कि वर्ष 2015 में क्योटो प्रोटोकाल की जगह एक अन्य समझौते पर सहमति बने, जो दुनिया के सभी देशों पर लागू हो।
 भयावह स्थिति
भयावह स्थिति
इस समय पूरी दुनिया पर्यावरण के भयंकर दुष्परिणामों से जूझ रही है। जलवायु में हो रहे परिवर्तन से वैश्विक ऊष्माकरण बढ़ रहा है। विश्व के सभी बड़े हिमनद पिघल रहे हैं, जिससे समुद्र का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। परिणामत: समुद्रतटीय भू-भाग डूब रहे हैं। प्रदूषण के बढ़ने से अनेक प्रकार की बीमारियां बढ़ रही हैं। मौसम में परिवर्तन से फसलचक्र गड़बड़ा है, जिसके कारण कृषि उत्पादन भी प्रभावित हुआ है।
दुनिया को भीषण पर्यावरण संकट से बचाने के लिए ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन घटाना नितान्त आवश्यक है। आज चीन और भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है। इस समय चीन विश्व में ग्रीन हाउस गैसों का सर्वाधिक उत्सर्जन करने वाला देश बन गया है। भारत में भी इसकी मात्रा बढ़ रही है। विकसित देशों की मांग मुखर होने लगी है। किये दोनों देश पहले उत्सर्जन में कटौती करें। जबकि चीन और भारत का कहना है कि उनका प्रतिव्यक्ति उत्सर्जन विकसित देशों खासकर अमेरिका की तुलना में काफी कम है। भारत का यह भी कहना है कि विकसित देशों द्वारा पर्यावरण को अब तक जो क्षति पहुंचायी गयी है, उसकी वे भरपाई करें। लगभग दो दशक पूरे हो गये, किन्तु आज भी दुनिया जबाबी दलीलों से ही जूझ रही है। वैश्विक तापमान में वृद्धि का सिलसिला जारी है, लेकिन हमने अंधा धुंध विकास की जगह किसी वैकल्पिक समाधान को नहीं अपनाया है। टिकाऊ विकास की चुनौती आज भी हमारे सामने बनी हुयी है।
जनता की भागीदारी महत्वपूर्ण
विगत बीस वर्षों में वैश्वीकरण की नव उदारवादी नीतियों और निजीकरण ने हमारे सामने अनेक चनौतियों को जन्म दिया है। इससे आर्थिक विकास के माडल भी लड़खड़ाने लगे हैं। भूख, खाद्य असुरक्षा और गरीबी ने न केवल निर्धन देशों पर अपना प्रभाव डाला है, अपितु धनी और विकसित देशों को भी परेशानी में डाल दिया है। जलवायु, र्ईंधन और जैव-विविधता से जुड़े संकटों ने आर्थिक विकास पर भी प्रभाव डाला है। आज हमारे सामने पर्यावरण बनाम विकास का मुद्दा है। और दोनों में किसी की अनदेखी करना सम्भव नहीं है।
भारतीय जीवनशैली त्यागपूर्ण उपभोग की रही है। भौतिकवाद के बजाय हम प्रकृतिवादी हैं। मनुष्य के जीवन की ही तरह पशु-पक्षियों, कीट-पतंगों और वृक्षों के जीवन को भी महत्वपूर्ण मानते हैं। उपभोग को जीवन की रक्षा तक ही सीमित मानते हैं। इसलिए हमेशा प्रकृति के साथ तादात्म्य स्थापित करके चलते रहे हैं। यज्ञ और पशुरक्षा को जीवन का अभिन्न मानते हैं। जबसे इस सोच और जीवन शैली पर पश्चिमी भोगवादी प्रवृत्ति का प्रभाव पड़ने लगा है, तभी से पर्यावरण की समस्या भारत में भी उठ खड़ी हुई है। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण इत्यादि उपभोग में अनियंत्रित वृद्धि के ही परिणाम है। इसलिए यदि इस सुफलाम्, सुजलाम् धारा की रक्षा करती है, तो हमें अपनी भारतीय जीवन शैली को ही प्रमुखता देनी होगी। प्रकृति की रक्षा के लिए सन्नल्द होना होगा। नदियों, सरोवरों को प्रदूषण मुक्त रखना होगा। इस समस्या का समाधान जनसमूह की साझेदारी के बिना सम्भव नहीं है। सामूहिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सामूहिक प्रयास की आवश्यकता होती है। इसलिए जलवायु परिवर्तन के विषय में भी सबसे बड़ी जरूरत जनता की जागरूकता और उसके सहयोग की है।