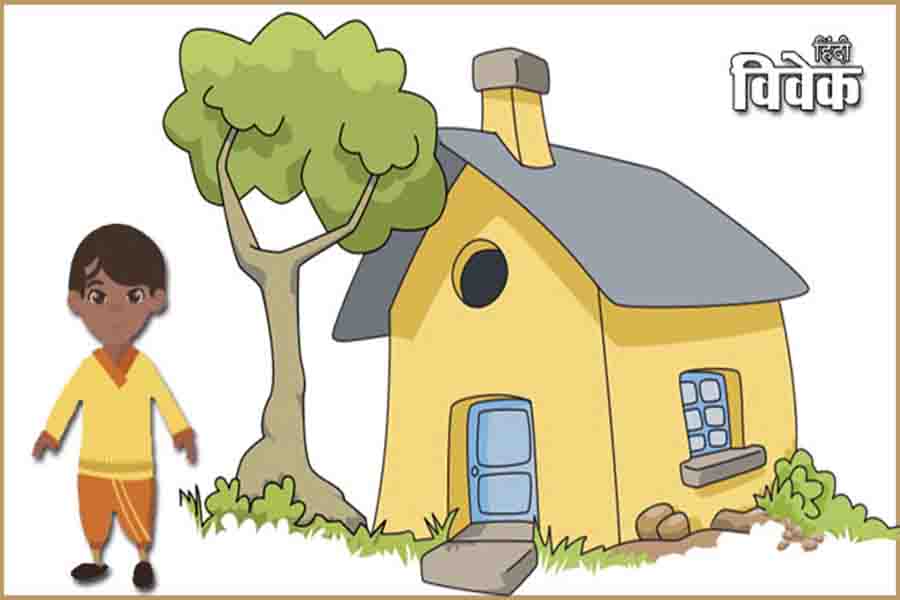जैसी असम की चाय की सब तरफ प्रसिद्ध है, वैसी ही मेघालय की हल्दी, त्रिपुरा की बांस निर्मित कलात्मक वस्तुएं, अरुणाचल के नाना प्रकार के फल-फूल, नगालैंड की तीखी मिर्ची, मणिपुर की लकड़ी की कलात्मक वस्तुएं, मिजोरम के विविध मसालें, सभी राज्यों की भिन्न-भिन्न जनजातियों की शालें जैसी वस्तुओं को शेष भारत में उस प्रदेश के नाम पर प्रसिद्ध एवं उपलब्ध करने के लिए कुछ कार्यक्रम बनाना पूर्वोत्तर के ग्राम विकास में सहायक होंगे|
दुनिया के किसी भी देश के विकास का आधार उसके ग्रामों के विकास पर निर्भर होता है| वर्षों से चले आ रहे परंपरागत ग्रामीण रोजगार बहुत हद तक अपने अस्तित्व के संकट से गुजर रहे हैं| यांत्रिक क्रान्ति ने तो इसे मरनासन्न अवस्था में पहुंचा दिया है| अनेक नई-नई रचनाओं के पीछे का आधार परंपरागत ग्रामीण कौशल रहा है| कंप्यूटर आधारित यांत्रिकीकरण के कारण उत्पादन की गति बढ़ जाने से हस्तकला से निर्मित उत्पाद की गति पीछे रह गई है| कारखानों की संख्या बढ़ती जा रही है| परिणामस्वरूप शहरों की संख्या भी बढ़ती जा रही है| ऊर्जा के नए-नए स्रोत खोजे जा रहे हैं| कोयला खदान या तेल जैसी चीजें सामने आईं| मनुष्य का स्थान मशीनों ने ले लिया है| प्रतिस्पर्धा बढती जा रही है| प्रदूषण के स्रोत भी बढ़ते जा रहे हैं| प्रकृति का संतुलन बिगड़ रहा है| केवल आर्थिक उन्नति की ओर दौड़ लगी हुई है| मशीनी प्रशिक्षण के नए-नए केंद्र खुल रहे हैं|
समाज की उन्नति में यांत्रिक क्रान्ति का बड़ा योगदान होते हुए भी यांत्रिक शक्ति अभी तक पूरी तरह ग्रामीण भागों में पहुंच नहीं पाई है| यदि यह शक्ति पूरी तरह गांवों तक पहुंची तो किसी भयानक परिणाम की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता| इस यांत्रिक शक्ति को एक विशेष प्रकार के संतुलन को ध्यान में रख कर ही गांवो तक पहुंचाना होगा|
किसी भी बात पर गहराई से विचार किया जाए तो बहुत-सी बातें सामने आती हैं| उदाहरण के लिए कृषि का विचार करें, जो हमारे देश का प्रमुख व्यवसाय रहा है| मनुष्य को जिन्दा रहने के लिए अनाज की जरूरत है| आदिम काल में कंद, मूल, फल या कुछ प्राणियों को खाकर मनुष्य जिन्दा रहता था| परन्तु जैसे-जैसे उसका शारीरिक तथा मानसिक विकास होता गया, उसने नए-नए प्रयोग कर कृषि का मार्ग अपनाया| खेती के साथ जुड़े अनेक उद्योग भी प्रारंभ हो गए| खेत में हल चलाने के लिए जानवरों की आवश्यकता हुई| गाय और बैल का समीकरण सामने आया, गाय का उपयोग दूध के लिए तो बैल का उपयोग खेती के अलावा आवागमन के साधन के रूप में भी होने लगा| बैलगाड़ी की रचना हुई| हल आदि औजार बनाने के लिए तथा खेती से सम्बंधित अन्य कामों के लिए लुहारी, ब़ढ़ईगीरी, चर्मकारी जैसे विविध कार्यों में लोग कुशलता प्राप्त करने लगे| नए व्यवसाय सामने आए| इस प्रकार ग्राम आधारित अनेक व्यवसाय अस्तित्व में आए, इन सबके बीच संतुलन बनाने के लिए संस्कारक्षम शिक्षा व्यवस्था, न्याय, नीति, धर्म की व्यवस्था थी ही, जिसमें समय-समय पर संशोधन भी हुआ| इसी व्यवस्था से सुदृढ़ और सम्पन्न समाज की रचना हुई| प्रत्येक जाति (क्वालिटी) के लोगों के निर्माण की यह संगठित सामाजिक संरचना थी|
परन्तु दुर्भाग्य से इस समाज व्यवस्था को तोड़ो, फोड़ो और राज करो वाली नीति की नजर लग गई| इसका सारा इतिहास हमारे सामने है| यवनों, पुर्तगालियों, अंग्रेजों आदि के आक्रमणों से यह देश परतंत्र रहा| स्वतंत्रता के बाद प्रजातांत्रिक आधार पर प्रगति के मार्ग पर बढ़ने हेतु संविधान की रचना हुई|
अनेक देशों के आक्रमणों के साथ-साथ उन देशों की विचारशैली भी समाज को प्रभावित करने लगी| इन नए विचारों के कोलाहल में भी गांधी, विनोबा भावे, संत तुकड़ोजी जैसे तथा बाद में नानाजी देशमुख, दीनदयाल उपाध्याय जैसे विचारकों ने ग्राम व्यवस्था को केंद्र में रख कर अर्थव्यवस्था का विचार रखा| स्वतंत्रता के बाद ग्राम विकास के लिए सरकारी योजना/अनुदान भी प्राप्त हुए| फिर भी गांव बिरले होते गए तथा शहरों की संख्या बढ़ती गई| कहीं न कहीं हम ग्राम व्यवस्था के साथ पटरी बैठाने में असमर्थ रहे| इसका मुख्य कारण रोजगार है| कर्ज और गरीबी के कारण किसानों की आत्महत्या में बढ़ोतरी होती गई| गांव का युवा वर्ग शहर की ओर आकर्षित होता गया| वैश्वीकरण की दौड़ में देश की आर्थिक ऊंचाई बनाए रखने के लिए हमारी योजनाएं बड़े-बड़े उद्योगों के लिए केन्द्रित होने लगी| इसमें कालानुसार धातु, रासायनिक पदार्थ, कंप्यूटर जैसे उद्योगों का समावेश हुआ| धरती मां के गर्भ से अकूत खनिज निकलने के उद्योग में बढ़ोतरी हुई| इसमें भी खनिज तेलों को प्राथमिकता प्राप्त हुई| स्वाभाविक रूप से खाड़ी के देश और पश्चिमी राष्ट्र इस मोर्चे पर आगे थे| दुनिया पर राज करने के लिए महायुद्ध शुरू हुए, परिणाम स्वरूप वैश्विक आर्थिक मंदी का दौर शुरू हुआ, जिसकी आंच से हम भी बच नहीं सके|
वैकल्पिक रूप से हमने पुनः ग्राम विकास की ओर ध्यान देना शुरू कर दिया है| कम से कम रासायनिक खाद का उपयोग कर फल, औषधीय पौधे या उस तरह की अन्य प्राकृतिक सम्पदा के उत्पादों पर अधिक ध्यान देना होगा| अपने देश में विशेष रूप से पूर्वोंत्तर को आर्गेनिक हब घोषित किया गया है| इसी बहाने हम पूर्वोत्तर के ग्रामीण विकास का अवलोकन करेंगे| बेहिसाब प्राकृतिक सम्पदा का धनी पूर्वोत्तर तुलनात्मक रूप से अविकसित और पिछड़ा हुआ है| राज्य और केंद्र सरकार ने विकास की जो योजनाएं बनाई हैं उसे गति देने की जरूरत है|
असम के लिए ब्रह्मपुत्र वरदान है तो अभिशाप भी है| एक ओर बरसात में इसकी भयंकर बाढ़ से अस्तव्यस्त जीवन, तो दूसरी ओर इसी नदी के तलछट से बनी उपजाऊ जमीन, जहां तीन-तीन बार फसल ली जा सकती है| उत्तर की ओर का समतल और अपर ब्रह्मपुत्र का क्षेत्र में (धेमाजी, लखीमपुर, शोणितपुर, दरंग, उसी प्रकार तिनसुकिया, डिब्रूगढ़, जोरहाट, शिवसागर और गोलाघाट) चावल, गन्ना, सरसों; मध्य ब्रह्मपुत्र के क्षेत्र के नागाव, मोरिगाव में चावल, तांत, दलहन, सरसों; ब्रह्मपुत्र के निचले भाग में (कामरूप, ग्वालपाड़ा, धुबरी, कोकराझार, बारपेटा और नलबारी) चावल, तांत, सरसों, आलू, गेहूं, दलहन; बराक क्षेत्र में (कछार, हायालाकंदी, करीमगंज) चावल, गन्ना, आलू और पर्वतीय प्रदेश में (कर्बिअलंग, उत्तर कछार) मका और गन्ने जैसी फसलें ली जाती हैं| बांस की उपलब्धता पूर्वोत्तर में सभी जगह है| असम और त्रिपुरा में तो बड़ी मात्रा में है| उत्पादन की क्षमता को देखते हुए छोटे प्रोसेसिंग सेंटर खोले जाए तो कच्चे माल की ढुलाई की दृष्टि से बहुत से फायदे हो सकते हैं और स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा| बांस से प्लाईवूड बनाने के कारखाने कुछ स्थानों पर हैं|
पूर्वोत्तर के बहुत से युवा व्यवसाय की तरक्की में लगे हुए हैं| गुवाहाटी से ५५ किलोमीटर दूर सोई गांव में ग्रामीण सहारा नामक संस्था सहकारिता के आधार पर काम कर रही है| हाथ करघे पर बुनाई जैसे काम वहां हो रहे हैं| गुवाहाटी के व्यवसायी पन्नालाल बंसाली के सहयोग के कारण इस उपक्रम को हम देख पाए| यहां के आसपास के १०० गांवों के परिवार की महिलाएं हाथ करघे पर वस्त्रों का उत्पादन करती हैं, उनका संकलन कर उसकी वाजिब कीमत मिले इसका भी सफल प्रयास किया जाता है| इस संस्था को कई पुरस्कारों से अब तक गौरवान्वित किया जा चुका है| संस्था के मुखिया से बात करते ज्ञात हुआ कि एक बड़ी व्यवसायिक कंपनी ने हल्दी के उत्पाद के लिए उपक्रम शुरू करने के लिए ७ करोड़ रुपये की सहायता का आश्वासन दिया है|
असम में कुछ स्थानीय युवाओं से पहले से ही दोस्ती थी, कुछ और नए मित्र भी बने| बातचीत के दौरान धीरज नाम के युवक ने बताया की कालिया भौर इस क्षेत्र में पटसन से कपड़ा बनाने वाली एक फैक्ट्री है, जो अब बंद होने के कगार पर है| पूर्व दीपंकर बोरा, पारस मजुमदार, राजेश सील, जुगांत दास और धीरज हम सब ने फैक्ट्री में जाने का तय किया| यहां आने के बाद देखा कि बहुत बड़े क्षेत्र में, आधुनिक यंत्रों से सुसज्ज, सहकारी आधार पर चलने वाली इस फैक्ट्री में जुट से बड़ी दरियां बनाने का काम होता है| यहां का अधिकतर माल बिहार, उत्तर प्रदेश इन राज्यों में जाता है| सन १९७० में इस कंपनी की शुरुआत हुई आज यह कंपनी १००० लोगों को रोजगार देती है| परन्तु अब किन्हीं कारणों से उसमें शिथिलता आने लगी है| वहां के अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार पटसन (जूट) का संग्रहण न किए जाने की सरकारी नीति के कारण जूट का उत्पादन कम होना तथा प्लास्टिक के बढ़ते उपयोग के कारण यह स्थिति बनी है| मैंने उन्हें सलाह दी कि यदि १००० कर्मचारियों को ध्यान में रख कर कोई योजना बने तो फिर से यह कंपनी खड़ी हो सकती है| १००० मजदूर परिवार को जूट उत्पादन का प्रशिक्षण दिया जाए, उस उत्पादित जूट को यही संस्था खरीदेगी| बड़ी दरियों के उत्पादन के साथ-साथ आसपास के लोगों को सिलाई का प्रशिक्षण देकर कंपनी में निर्मित कपड़े से स्कूलों के थैले, कलात्मक वस्तुएं, प्लास्टिक की थैलियों के अन्य वैकल्पिक उत्पाद बनाए जा सकते हैं, नया रोजगार भी पैदा होगा| आज प्रकृति के लिए घातक कचरे का समापन हम सबके सामने बड़ी चुनौती है| मुख्य रूप से पैकिंग के लिए प्लास्टिक जैसी चीजों का प्रयोग उत्पाद खरीदने के दूसरे क्षण ही बेकार हो जाता है, प्राकृतिक रूप से इस कचरे के समापन में लम्बा समय लगता है| जिसका दुष्परिणाम प्रकृति को भुगतना पड़ रहा है| ग्रामों में भी अब इस कचरे की मात्रा बढ़ती जा रही है| शहर में भी इस कचरे से पुनरुत्पाद की मशीनरी कम पड़ रही है| स्वाभाविक रूप से इस कचरे का डम्पिंग करने के लिए शहर का खुला भाग कम पड़ रहा है, जिससे यही कचरा ग्रामों के खुले क्षेत्र की ओर बढ़ रहा है| प्रकृति पर आक्रमण हो तो प्रकृति अपना कैसा रूप दिखाती है इसका हमें अनुभव है ही| इसीलिए जिसका कचरा शीघ्र ही प्रकृति से एकरूप हो जाए, ऐसे उत्पादों के उपयोग को ही प्राथमिकता दी जाए तो उपरोक्त समस्या का सहज समाधान हो सकता है|
पूर्वोत्तर के अधिकांश भागों में वर्ष में आठ नौ महीने कड़ाके की ठण्ड होती है| स्वेटर, मफलर, शाल, कनटोप जैसे वस्त्रों का प्रयोग ठण्ड से सुरक्षा के लिए किया जाता है| आज अधिकांश उत्पाद लुधियाना, त्रिचुर, भूटान, चीन जैसे स्थानों से आते हैं| अलग-अलग प्रकार के नक्कासीदार झालर वाले, पारंपरिक निशान वाले गर्म कपड़े बुनने की यहां की परंपरा है, सुंदर-सुंदर वस्त्र परिधान यहां भी लोगों को भाते हैं| गुवाहाटी में राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय तथा स्थानीय उत्पादनों का बड़ा बाजार उपलब्ध है| पर उसकी पहुंच मध्यम तथा उच्च वर्ग के सीमित लोगों तक है| पूर्वोत्तर के छोटे शहरों में इसके बाजार की बहुत संभावनाएं हैं| मध्यम वर्ग को ध्यान में रख कर गर्म कपड़ों का निर्माण तथा विपणन का बड़ा काम शुरू हो सकता है| मेघालय के लंदेम नामक स्थान पर सुरेन्द्र वेलंकर ने सन २००० में शाल निर्माण का काम शुरू किया था, स्थानीय महिलाओं को प्रशिक्षण देकर दस मशीनों की व्यवस्था भी की थी| कुछ तकनिकी कारणों से यह उपक्रम चल नहीं पाया| इस प्रकल्प को पुनर्जीवित करने के मैंने प्रयास भी किए, उसकी रिपोर्ट भी बनाई| वहां की प्रशिक्षित महिलाओं से संपर्क कर उनको उत्साहित करने का काम भी किया, परन्तु कुछ कठिनाइयों के कारण उसे मूर्त रूप नहीं आ पाया, क्योंकि किसी भी नए व्यवसाय को स्थिर होने के लिए कुछ समय देना पड़ता है, इस दौरान पूंजी का विनियोग, साथ-साथ तकनिकी ज्ञान और सरकारी नीति का समन्वय होना जरूरी होता है| यदि ऐसा हुआ तो बड़ी संख्या में स्वरोजगार पैदा हो सकता है|
मेघालय के क्षेत्र में आलू, मसाले के पदार्थों, केले, किवि या कटहल जैसे फल बड़ी मात्रा में होते हैं| यहां छोटे स्तर पर फलों पर प्रक्रिया करने का काम स्थानीय उत्पादन क्षेत्र में होना जरूरी है| झाड़ू बनाने की घास पूरे भारत में मेघालय से प्राप्त होती है, परन्तु मेघालय में झाड़ू बनाने के कारखाने नहीं के बराबर हैं| पर्यटन की दृष्टि से यहीं के एक गांव मवालेनीयांग का एशिया के स्वच्छ गांव के नाम पर चयन हुआ है| मेघालय की राजधानी शिलांग से ७८ किलोमीटर दूर बांग्लादेश की सीमा के पास बसा है यह गांव| गांव में सुंदर रास्ते हैं, घर के बाहर बांस की बनी टोकनी में कचरा डालने की व्यवस्था, घर के आसपास खूबसूरत फूलों के पेड़, उसकी नियमित देखभाल, सुपारी, आलू की फसल, संतरा और केले के फल, विविध सब्जियों की खेती, साथ-साथ १००% साक्षरता यहां की विशेषता है| २००२ में एशिया के स्वच्छ गांव के रूप में इसका चुनाव हुआ| तब से इसे पर्यटक स्थल का दर्जा प्राप्त होता गया| देशी-विदेशी पर्यटक यहां आने लगे| स्वच्छता के माध्यम से यहां एक अद्भुत और सफल उपक्रम शुरू हो गया, साथ में उत्पादों के नए स्रोत भी बनते गए| सरकार को इस गांव को ध्यान में रख कर अन्य गांवों में भी इस प्रकार के उपक्रम चालू करने की योजना बनानी चाहिए|
मणिपुर में भी चावल और गन्ने की फसल ली जाती है| पूरे पूर्वोत्तर में घर-घर में लोग हाथ करघे की कला से परिचित हैं| साथ में बांस से कलात्मक वस्तुएं बनाने की कला भी बहुत से लोगों को आती है| मणिपुर में काठ लकड़ी से देवी-देवताओं की मूर्ति बनाने की कला परंपरागत रूप से विद्यमान है| मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल सहित सभी राज्यों में विविध प्रकार के फल-फूल होते हैं| अधिकांश भागों में सुपारी के सघन वृक्ष हैं| सुपारी के वृक्ष के ऊपर के भाग की छाल से दोने पत्तल भी बनाए जाते हैं| यदि इन्हें बनाने की प्रक्रिया के लिए छोटी मशीनों को इन सुपारी उत्पादक गांवों में लगाकर दिया जाए तो स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा|
इस पूरे पूर्वोत्तर को प्रकृति ने दोनों हाथों से लुटाया है| प्राकृतिक दृष्टि से पूर्वोत्तर का सौंदर्य कैलिफोर्निया से कम नहीं है| प्रत्येक गांव में अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य दिखाई देता है| दो-तीन कमरों का छोटा सा मकान, घर के बाजू में छोटा सा तालाब, जहां मछली पालन किया जाता है, सामान्यतः पूर्वोत्तर के घरों की ऐसी औसत रचना है| यदि अपने घर में या घर से लगे हुए भाग में पर्यटकों के निवास की व्यवस्था हो, उन्हें पारंपरिक संस्कृति और नृत्यादी दिखाया जाए, खेती के उत्पाद की वहीं बिक्री हो, छोटी गाड़ी की व्यवस्था कर आसपास के दर्शनीय स्थल दिखाए जा सके, तो इस प्रकार की व्यवस्था से पर्यटकों में यहां के ग्रामीण जीवन शैली को निकट से देखने का उत्साह बढ़ेगा| सरकार को इस प्रकार की योजना पर भी अध्ययनपूर्वक ध्यान देना चाहिए|
मेरे पूर्वोत्तर के प्रवास के निमित्त अपर ब्रह्मपुत्र क्षेत्र के विश्वनाथ चारी आली स्थान के पोभोय गांव में जाना हुआ| असम के तत्कालीन गवर्नर श्री पद्मनाभ आचार्य ने उस गांव के एक युवक नीलम दत्ता से मेरा परिचय करा दिया था| श्री दत्त के आमंत्रण पर मैं दो दिन के लिए उनके निवास पर गया| मैंने एक शिक्षित युवक द्वारा २५ एकड़ में की गई लाभदायक कृषि का अद्भुत उदहारण वहां देखा| श्री दत्ता ने लगभग चार तालाबों का निर्माण किया था| उसी के आधार पर चावल की खेती हो रही थी| भिन्न-भिन्न प्रकार के फूल भी लगाए गए थे| परिसर के बेकार हरे पत्तों को जमा कर सेंद्रिय खाद का प्रकल्प भी उन्होंने खड़ा किया था| विभिन्न प्रकार की साग-सब्जियों की भी बुआई की थी| वहां के उत्पाद को निकट के बाजार में भेजने की भी व्यवस्था उनके पास थी| खेत परिसर में ही उन्होंने चार सुविधायुक्त कमरों का निर्माण किया हुआ था| उन्होंने बताया कि इन कमरों का निर्माण गांव की खेती देखने आने वाले पर्यटकों के लिए किया गया है| श्री दत्त ने बताया कि आधुनिक खेती के लिए, फल प्रक्रिया केंद्र, बांस, हाथकरघा आधारित हस्तकला प्रशिक्षण जैसे काम प्रारंभ किए जा सकते हैं| अरुणाचल प्रदेश की सीमा से लगा यह प्रदेश, वहां विशेष रूप से पक्षियों पर चल रहा अध्ययन, वहां के चाय बागान, उसी प्रकार तेजपुर के पास का रमणीय स्थल आदि स्थानों पर पर्यटन की भी व्यवस्था की जा सकती है| शिक्षा पूरी होने के बाद सामान्य रूप से युवा शहर की ओर जाते हैं, परन्तु इस युवक ने अपनी महाविद्यालयीन शिक्षा पूरी करने के बाद गांव में रह कर खेती का विकल्प चुन कर ग्रामीण क्षेत्र में भी उत्पादों के स्रोत सफलतापूर्वक ढूंढ़ निकाले, यह मैं स्वयं अनुभव कर रहा था| सरकार को ऐसे तरुणों को प्रोत्साहित कर ग्राम विकास के मार्ग को आगे बढ़ाना चाहिए और सर्वांगीण विकास के लिए सरकार को ऊपर दी गई कुछ बातों पर स्वयंमेव विचार करना चाहिए|
मेरे विचार से यदि ग्रामीण विकास पर ध्यान देना है तो जो स्थानीय लोग प्रशिक्षण लेकर विभिन्न व्यवसायों में कार्यरत हैं, उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ प्राथमिकता पूर्वक प्राप्त होना चाहिए, जिसमें सड़क तथा अन्य निर्माण कार्य हो सकते हैं| स्थानीय उत्पादों के लिए ७,८ किलोमीटर की परिधि में प्रक्रिया केंद्र वहां के उत्पाद को ध्यान में रख कर खोलना चाहिए| मुगा, ईरी जैसे कीड़ों का संवर्धन कर रेशम के उत्पादन पर जोर देना चाहिए| हाथ करघों पर बने कपड़ों का शालाओं के गणवेश के लिए उपयोग का आग्रह होना चाहिए| ऐसा ही आग्रह स्थानीय सरकारी कर्मचारियों के ड्रेस के लिए भी होना चाहिए| पर्यटन को सुनिश्चित प्राथमिकता देते हुए अधिक से अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए योजना बनाने के साथ-साथ विज्ञापनों पर भी जोर देना चाहिए| आवागमन के नए विकल्प खोजने की जरुरत है| पर्वतीय भाग में दूर-दूर बसे गांवों की दूरी को कैसे कम किया जा सकता है, इस दृष्टि से भी विचार होना चाहिए| रोप-वे एक क्रांतिकारी विकल्प हो सकता है| ब्रह्मपुत्र के चौड़े पात्र पर जल परिवहन कैसे शीघ्र चालू किया जा सकता है इस पर काम होना जरुरी है| उचित दर पर हेलिकॉप्टर से आवागमन पर भी विचार किया जा सकता है, जो पर्यटकों के लिए पूर्वोंत्तर का अतिरिक्त आकर्षण हो सकता है| शेष भारत के बाजार में पूर्वोत्तर वासियों को योग्य स्थान प्राप्त हो इसकी योजना भी सरकार को प्राथमिकता के साथ बनानी चाहिए| जैसी असम की चाय की सब तरफ प्रसिद्धि है, वैसी ही जानकारी मेघालय की हल्दी, त्रिपुरा की बांस निर्मित कलात्मक वस्तुएं, अरुणाचल के नाना प्रकार के फल-फूल, नगालैंड की तीखी मिर्ची, मणिपुर की लकड़ी की कलात्मक वस्तुएं, मिजोरम के विविध मसाले, सभी राज्यों की भिन्न-भिन्न जनजातियों की शालें जैसी वस्तुओं का बाजार में परिचय उस प्रदेश के नाम पर प्राप्त कराने के लिए कुछ कार्यक्रम बनाने चाहिए| रेल द्वारा वहां के सामानों को शेष भारत में लाने के लिए भी विशेष योजना की जरूरत है|
यदि हमने प्राकृतिक रीति की खेती को केंद्र में रख कर, मानव और जानवर की शक्ति के साथ पारंपरिक और प्राकृतिक ऊर्जा स्रोत का प्रयोग कर, खेती और तत्सम उत्पादों के लिए संस्करण केंद्र बढ़ा कर ऐसे उद्योगों को आगे बढ़ाने की नीति अपनाई तो मानव जाति का और पूरे विश्व का भी कल्याण होगा|