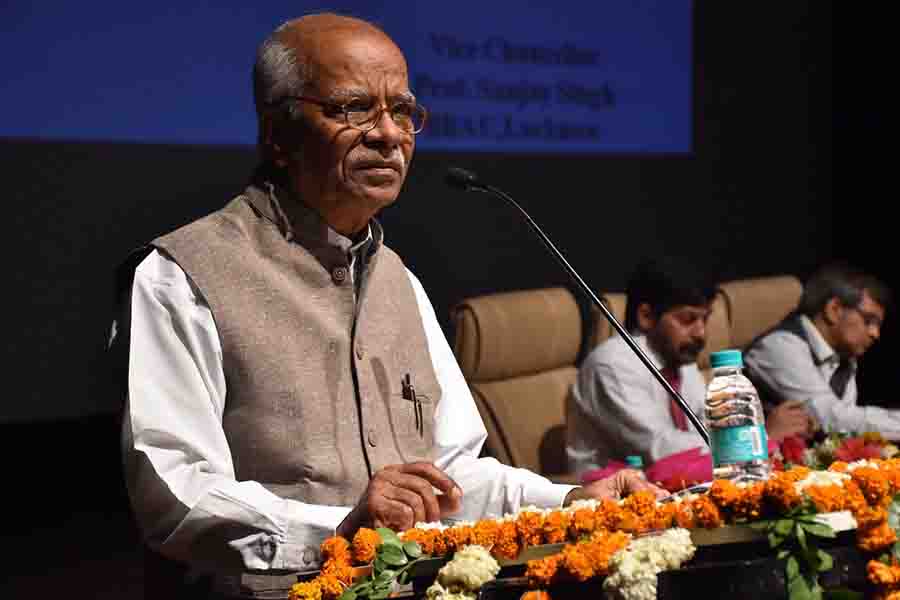संघ विचारक और विवेक समूह की मातृ-संस्था हिंदुस्थान प्रकाशन संस्था के अध्यक्ष श्री रमेश पतंगे का सम्पूर्ण जीवन ही संघमय और देशमय है। देशहित में किसी भी तरह का शिवधनुष उठाने में सदा तत्पर रहते हैं। वे अपने जीवन के 75 साल पूरे कर रहे हैं। उनके संघ-कार्य के प्रदीर्घ अनुभवों एवं देश के समक्ष विभिन्न मुद्दों पर उनसे हुई विस्तृत बातचीत के महत्वपूर्ण अंश यहां प्रस्तुत हैं-
एक समय ऐसा था जब सामाजिक, राजनैतिक, पत्रकारिता सहित अन्य क्षेत्रों में अपना भविष्य संवारने के लिए हिंदुत्व को नकारना पड़ता था, ऐसे समय में आपने हिंदुत्व का कार्य आरंभ किया। आपके जीवन के इस अहम पड़ाव पर प्रकाश डालिए?
न तो मुझे राजनीति करनी थी, न ही पत्रकारिता करनी थी। ये दोनों ही मेरे जीवन के लक्ष्य नहीं थे। हालांकि मेरे पिताजी उस जमाने में अंधेरी (मुंबई के उपनगर) में जनसंघ का कार्य करते थे। लेकिन मुझे राजनीति में पहले से ही रुचि नहीं थी। मैं तो पत्रकार भी संयोग से बना। मुझ पर संघ कार्यों का दायित्व था। साथ ही परिस्थितिवश मुझे रोजी-रोटी के लिए भी कुछ करना था। उस समय मुझे ‘साप्ताहिक विवेक’ का कार्य करने का प्रस्ताव मिला। जिसे मैंने स्वीकार कर लिया। पहले ही दिन से मुझे संपादकीय कार्यों की जिम्मेदारी दी गई। धीरे-धीरे मैं इस कार्य को सीखता गया और इसमें मैं रम गया।
जहां तक हिंदुत्व की बात है वह तो मेरी नस-नस में है। मेरी हर सांस में है। मैंने पत्रकारिता को कभी करियर की दृष्टि से नहीं देखा। हिंदुत्व और देश के लिए जो हितकर है, उसे सही समय आने पर प्रकाशित करना ही चाहिए, इसी विचार से मैंने हमेशा निडर होकर लिखा। इसे पाठकों ने भी बहुत पसंद किया। यही मेरे जीवन का अहम पड़ाव था। इसके बाद हिंदुत्व का भगवा ध्वज लेकर स्वामी विवेकानंद के मार्ग पर ‘विवेक’ चल पड़ा और पत्रकारिता क्षेत्र में कई उपलब्धियां प्राप्त कीं।
यह सही बात है कि मैं चिंतन करता हूं, लिखता हूं, पढ़ता हूं लेकिन मैं इसी अवस्था में 24 घंटे नहीं रह सकता। कोई भी व्यक्ति हो, वह थक जाता है, उसे विश्राम की आवश्यकता होती है। वह मनोरंजन के लिए मूवी, संगीत, नाटक आदि का उपयोग करता है। मैं सबसे अधिक शास्त्रीय संगीत सुनता हूं। उससे मेरी सारी शारीरिक व मानसिक थकान दूर हो जाती है।
आपके इस रवैये का क्या असर हुआ?
इसका व्यापक असर समाज पर हुआ। मुझे उस समय का एक लेख स्मरण आ रहा है, जब बोफोर्स घोटाले में राजीव गांधी का नाम आया था। तब मैंने ’राजीव गांधी चालते व्हा’ (राजीव गांधी चलते बनो) शीर्षक से एक लेख लिखा था। इसे विवेक की कवर स्टोरी के रूप में प्रकाशित किया गया था। उस समय कई पाठकों ने मेरे इस साहसपूर्ण लेख की खूब सराहना की थी और मेरी हिम्मत की दाद दी थी। परंतु साथ ही यह भी कहा था कि ‘इस तरह के लेख लिखने से आपको नुकसान भी पहुंच सकता है।’ ये भयपूर्ण विचार लोगों के मन में थे, परंतु मेरे मन में कभी नहीं आए। मेरे मन में यह दृढ़ निश्चिय था कि जो हिंदुत्व एवं देशहित में होगा वह मैं जरूर लिखूंगा और मैंने वही लिखा भी। इसके अलावा जब एक वोट से अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार गिर गई थी, उसमें तत्कालीन राष्ट्रपति के.आर.नारायणन (जो कि भाजपा के धुर विरोधी थे) ने अहम भूमिका अदा की थी। तब मैंने उनके खिलाफ एक संपादकीय में लिखा था कि अटल सरकार गिराने में इस खलनायक की भूमिका को नहीं भूलना चाहिए। साथ ही उन्होंने कैसे खलनायक की भूमिका निभाई इसका भी मैंने उल्लेख किया था। इसके बाद सोलापुर के एक दैनिक समाचार पत्र के कार्यालय से किसी ने मुझे फोन किया और कहा कि ‘आपने राष्ट्रपति को खलनायक कहा है, आप पर केस हो सकता है और आपको जेल भी जाना पड़ सकता है।’ तब मैंने उनसे कहा, ‘भाई साहब! मुझे जेल जाने की धमकी न देना। मैं संविधान की रक्षा के लिए 14 महीने जेल जाकर आया हूं। मैं अपना एक भी शब्द वापस नहीं लूंगा। जो करना है, कर लो।’ मेरा यह मानना है कि यदि आप अपनी सत्यनिष्ठा के प्रति अडिग रहते हैं और उससे पूरी तरह से सहमत हैं तो प्रतिकूल बातें भी आपके लिए अनुकूल बन जाती हैं। मेरे इसी रवैये से समाज में सकारात्मक परिवर्तन का आभास हुआ और देशहित में संघर्ष की भावना लोगों में निर्माण हुई।
आपका बचपन झुग्गी-झोपड़ी में गुजरा है। वहां सामाजिक चिंतन इत्यादि से दूर-दूर तक कोई नाता नहीं होता। फिर आप में समता, सामाजिक समरसता, राष्ट्र चिंतन, सामाजिक न्याय, वैभवशाली राष्ट्र जैसे विचार कहां से आए?
मैं बचपन से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक रहा हूं। बचपन मेेंजो संस्कार होते हैं, वे बहुत गहरे होते हैं। बाल्यावस्था में मुझ पर जो संघ के संस्कार हुए, वे बेहद प्रभावी थे। हम सब हिंदू हैं, हम सब भाई हैं, भारत हमारी माता है। किसी भी प्रकार का ऊंच नीच, भेदभाव हमें नहीं करना चाहिए। सबके साथ आत्मीय व्यवहार करना चाहिए। हर जाति-धर्म के लोगों के घर जाना चाहिए। ऐसे मानवीय विचार हम शाखा में सीखते थे। बौद्धिक वर्ग एवं बैठक में हमसे प्रश्न पूछे जाते थे कि आपकी गट व्यवस्था क्या है? क्या सभी स्वयंसेवकों के घर आपको पता हैं? क्या उनके माता-पिता से आपका परिचय है? कितनी बार उसके घर भोजन करने गए हैं? ऐसे प्रश्नों का मतलब होता था कि ये सब काम हमें करने हैं। इससे समाज में आत्मीय एवं भावनात्मक संबंध सहजता से होता है।
आपने झुग्गी-झोपड़ी की बात की। झोप़डियों में रहने वाले लोग आपस में अधिक प्रेम-पूर्वक रहते हैं। एक दूसरे के सुख-दुख में साथ रहते हैं। समय आने पर एक-दूसरे की सहायता करते हैं। जाति-पाति का कोई भेद नहीं होता। सभी लोग एक दूसरे के घर भोजन भिजवाते हैं और स्नेहपूर्वक खाते हैं। आज भी झुग्गी-झोप़डियों में मानवता एवं आत्मीयता बसती है। इन क्षेत्रों में अपराध, नशा, अशिक्षा, मूलभूत सुविधाओं से वंचित जैसी अनेक समस्याएं हैं लेकिन झोपड़ियों में ही लोगों एवं बच्चों के चेहरे पर सच्ची मुस्कान देखने को मिलती है। संघ कार्य के अंतर्गत सामाजिक समरसता का दायित्व निभाते समय मैंने खूब अध्ययन भी किया। डॉ. बाबासाहब आंबेडकर की पुस्तकें पढ़ीं। हम हर किसी के घर आते-जाते हैं, उनके घर भोजन करते हैं, सामाजिक समरसता पूरे देश में निर्माण हो, इसके लिए सबसे अधिक काम भी करते हैं। बावजूद इसके कुछ लोग संघ को बदनाम करते हुए कहते हैं कि संघ दलित विरोधी है, मनुवादी है, जातिवादी है। मैं सोचता हूं कि इन्हें यह सब कहां से मिला? वास्तविकता तो ऐसी है नहीं। मनगढ़ंत बातें कुछ लोग फैलाते हैं, जिसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। इस सत्य का दर्शन कराने के लिए मैंने ‘मैं, मनु और संघ’ पुस्तक लिखी। इसमें झुग्गी झोप़डियों के अनुभवों को मैंने साझा किया है और यथार्थ से अवगत कराया है।
आपातकाल के समय आपको 14 माह के लिए मीसाबंदी के रूप में कारावास में रखा गया था। इस दौरान ऐसा क्या हुआ कि जेल से छूटने के बाद आपके विचारों में प्रखरता आ गई और आप देश में एक चिंतक, विचारक के नाते प्रसिद्ध हो गए?
मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जन्म हिंदुत्व का सामाजिक आशय प्रकट करने के लिए ही हुआ है इसलिए मैंने स्वयं को ईश्वरीय कार्य हेतु झोंक दिया। राजनैतिक बंदी होने के कारण जेल में हमसे कुछ काम नहीं कराया जाता था। पूरा समय हमारे हाथ में ही था, पढ़ने-लिखने आदि की हमें स्वतंत्रता थी। उस समय मैंने पहली बार डॉ. बाबासाहब आंबेडकर का जीवन चरित्र पढ़ा। इसके बाद मेरे अंदर का चिंतक जाग गया। मुझे संज्ञान हुआ कि मैं अपना पूरा जीवन हिंदू संगठन के लिए लगा तो रहा हूं, संघ जी तो रहा हूं, लेकिन हिंदू समाज की वास्तविकता मुझे पूरी तरह से पता नहीं थी। मैं संघ के सात्विक वातावरण में पला बढ़ा हूं; लेकिन संघ को छोड़ कर जो बाकी समाज है वह जाति-पाति, भेद-भाव, छूआ-छूत और ऊंच-नीच को मानने वाला है। यह सब जानकारी मेरे लिए नई थी। क्योंकि मुंबई जैसे शहर एवं झुग्गी-झोप़डियों में जाति-पाति का भेदभाव दिखाई नहीं देता है। संघ में सामाजिक समरसता के माहौल के कारण इस सबसे मैं अनभिज्ञ था। संघ के बाहर की दुनिया को समझने की मेरी जिज्ञासा बढ़ने लगी। इसी जिज्ञासा के चलते मैंने अध्ययन किया और अस्पृश्यता, छुआ-छूत, जाति-पाति के बंधन से समाज को मुक्त करने के लिए सामाजिक समरसता निर्माण हेतु कार्य प्रारंभ किया। डॉ. केशव बलिराम हेडगेवार ने एक ऐसा तंत्र शाखा के माध्यम से स्थापित किया है कि ऑपरेशन भी हो जाता है, जख्म भी भर जाता, जख्म के निशान तक दिखाई नहीं देते और मरीज को पता भी नहीं चलता है। उक्त सामाजिक बुराइयों को को दूर करने के लिए अनेक महापुरूषों ने बड़ा संघर्ष व प्रयत्न किया। बावजूद इसमें वे शतप्रतिशत सफल नहीं हुए। लेकिन दूरद्रष्टा प.पू.डॉ. हेडगेवार ने सहजता से परिवर्तन कर दिया और समाज व देश के लिए वे आदर्श बने। इसलिए संघ में कहीं भी जाति-पाति, छूआछूत और अस्पृश्यता नहीं है। जेल में किए गए गहरे अध्ययन व चिंतन के कारण मेरे जीवन को एक नई दिशा मिली। श्रद्धेय दत्तोपंत ठेंगडीजी ने सामाजिक समरसता मंच की स्थापना की उस काम का दायित्व मेरे उपर आया। मै लिखता गया और पाठकों ने मुझे विचारक बना दिया परंतु मैं आज भी सामान्य स्वयंसेवक ही हूं।
डॉ.आंबेडकर और डॉ.हेडगेवार इन दोनों द्वारा सामाजिक समरसता को लेकर किए गए कार्यों को आप किस तरह देखते हैं?
डॉ. आंबेडकर का लक्ष्य था हिंदू समाज में व्याप्त अस्पृश्यता, छुआछूत, जाति-पाति आदि बुराइयों को खत्म करना। इन बुराइयों को खत्म किए बिना देश बड़ा नहीं हो सकता और समाज शक्तिशाली भी नहीं हो सकता। उन्होंने धार्मिक सुधार एवं सामाजिक सुधार के जरिए समता प्राप्त करने के लिए आजीवन संघर्ष किया। नागरिकों की स्वतंत्रता एवं समता पर उन्होंने अधिक बल दिया। हमारा संविधान हमें यह अधिकार देता है। लेकिन केवल कानून बनाने से ऐसा होना संभव नहीं है। यह समाज में स्वाभाविक रूप से आनी चाहिए। स्वाभाविक रूप से आनी चाहिए। इसके लिए सभी में बंधुत्व की भावना आनी चाहिए। यह सब डॉ. आंबेडकर ने कहा, लेकिन कैसे आनी चाहिए इसका चिंतन, विचार, क्रिया उन्होंने नहीं बताई। मेरे अध्ययन व आकलन के अनुसार सामाजिक समरसता का सिद्धांत डॉ.आंबेडकर ने दिया और डॉ. हेडगेवार ने उसे यथार्थ में कर दिखाया। इसमें दोनों की एक दूसरे से तुलना नहीं करनी चाहिए और न ही उनमें समानता की बात करनी चाहिए। दोनों का कार्यक्षेत्र अलग था। अपने – अपने कार्यों के आधार पर दोनों ही महापुरूष हैं। संविधान ने हमें मानव अधिकार, स्वतंत्रता व समता तो दी है लेकिन उसमें बंधुता के विषय में कुछ भी नहीं कहा गया है। क्योंकि कानून बनाने से बंधुता का पालन होना संभव नहीं है।
समाज में बंधुत्व की भावना निर्माण किए बिना सामाजिक समरसता होना संभव नहीं है, इन विचारों को यथार्थ में लाने के लिए आपने अपना पूरा जीवन लगा दिया। समाज में अब आपको क्या परिवर्तन महसूस हो रहा हैं?
जब हमने समरसता मंच का कार्य प्रारंभ किया तब हमारे पास कोई ब्लूप्रिंट नहीं था, कैसे करना है इसकी कुछ विशेष जानकारी भी नहीं थी। बस पूजनीय डॉ. हेडगेवार जी की प्रेरणा एवं सिद्धांत ही थे कि समाज हित एवं देश हित में किया गया कार्य सफल होना ही है। शुरुआत में हमारे कार्यों में कुछ कमियां दिखाई देंगी लेकिन समय के साथ सीख भी जाएंगे और कमियां भी खत्म हो जाएंगी। इसी तरह शुभ संकल्प के साथ कार्य करते-करते सामाजिक समरसता परिषद, सामाजिक समरसता मंच, भटके विमुक्त परिषद आदि अनेक नए संगठनों का निर्माण कर हम समाज के बीच निरंतर जाकर कार्य करने लगे, जन जागरण करने लगे। सबसे पहले हमने सामाजिक व धार्मिक सुधार के क्षेत्र में कार्य कर चुके महापुरूषों की जयंतियां, पुण्यतिथियां मनाना प्रारंभ किया और उसके माध्यम से समाज सुधार का एक आंदोलन चल पड़ा। डॉ. बाबासाहब आंबेडकर, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, अण्णाभाऊ साठे, राजर्षि शाहू महाराज, स्वा. सावरकर आदि समाज सुधारकों की जयंतियों पर हमने सबसे अधिक कार्यक्रम किए। इसी के माध्यम से समाज में बंधुत्व का निर्माण हुआ और सामाजिक समरसता एवं एकता को बल मिला और इसके साथ ही समाज में सकारात्मक परिवर्तन दिखाई देने लगे।
हिंदू धर्म पर आघात करने के लिए समाज में भेदभाव, नफरत फैलाकर सामाजिक तानाबाना तोड़ने के लिए अनेक साहित्यिक सम्मेलन होते हैं। ऐसे साहित्यिक सम्मेलन करानेवाले नकारात्मक विचारों के संगठन महाराष्ट्र में सक्रिय हैं। क्या सरकार को इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए?
हां, इनके खिलाफ कार्रवाई करना बेहद जरूरी है। इनकी झूठी जहरीली विचारधारा समाज में कटुता निर्माण करती है। सामाजिक समरसता विषय पर काम करते हुए मुझे इनके बारे में जानकारी मिली। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि महाराष्ट्र में 30 से 32 प्रकार के साहित्य सम्मेलन होते हैं। जिनमें कथित रूप से आंबेडकरी, आदिवासी, मूल निवासी, कामगार, दलित आदि विषयों की आड़ में हिंदुत्व को गालियां दी जाती हैं। इसमें आदिवासी कहेगा कि हम हिंदू नहीं हैं। दलित कहेगा कि ये सब मनुवादी हैं, हम पर हमला हो रहा है। कामगार कहेगा कि हिंदुत्व कामगार विरोधी है। ब्राह्मणों ने हम पर बहुत अत्याचार किए हैं। इस तरह की मनग़ढ़ंत व भड़काऊ बातें साहित्य सम्मेलनों में की जाती हैं। जब मैंने इसका अध्ययन किया तो पता चला कि 25-30 वक्ता ही हैं जो हर मंच पर जाकर जहरीली समाज विरोधी बातें करते हैं। समाज विघातक शक्तियों का नाश करना सरकार व देशहित में है इसलिए इस विषय का संज्ञान लेकर देश की सुरक्षा एजेंसियों एवं पुलिस प्रशासन को जांच कर कार्रवाई करनी चाहिए।
क्या ऐसे साहित्य सम्मेलनों में सभी विचारकों को अभिव्यक्ति की आजादी होती है?
जी, बिल्कुल नहीं। पहली बात तो यह है कि इनके साहित्य सम्मेलनों में किसी बाहरी विद्वान, विचारक, विशेषज्ञ को बुलाया ही नहीं जाता। इसलिए अभिव्यक्ति की आजादी का तो सवाल ही नहीं उठता। वे केवल अपने ही लोगों को बुलाते हैं और येन – केन प्रकारेण अपना एजेंडा फैलाकर चले जाते हैं। एक बार मुझे उनके ‘विचार सम्मेलन’ में अपने विचार रखने का मौका मिला था। उस समय मैंने साफ शब्दों में कहा था कि समाज में नफरत और जाति-पाति की भावना को बढ़ावा देने के लिए आप लोग जिम्मेदार हैं और कैसे जिम्मेदार हैं इसकी पूरी व्याख्या भी की थी। उस समय सभी बड़े – बड़े दिग्गज वहां मौजूद थे। मैंने सभी के सामने बिना डरे यह बात कही थी। उस दिन विचाररूपी शस्त्र से मैंने उनकी धज्जियां उड़ा दी थीं। उनके ही हथियार से मैंने उनको घायल कर दिया था। उसके बाद उनकी हिम्मत नहीं हुई मुझे बुलाने की। इसके अलावा टीवी शो पर इन्हीं सम्मेलनों के दो लोगों के साथ मेरी बहस का कार्यक्रम तय हुआ था। जिसे इन्होंने डर के मारे रद्द करवा दिया था। मेरी इस पर राय है कि इन साहित्य मंच वालों को उनकी ही भाषा में जवाब देना चाहिए। यदि आपको लड़ाई करनी है तो उस क्षेत्र के शस्त्र से ही लड़ना चाहिए। वैचारिक लड़ाई लड़नी है तो आपको विचार रखने वाले लोग चाहिए, विचार चाहिए और विषय ज्ञान के लिए पुस्तकें चाहिए। इसके बाद हमने निर्णय किया कि हम भी समरसता साहित्य सम्मेलनों का आयोजन किया करेंगे और पहले ही साहित्यिक सम्मेलन में हमें अभूतपूर्व प्रतिसाद मिला। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के चलते हमारे साथ एक बड़ा बुद्धिजीवी वर्ग जुड़ गया और उन्होंने आग्रह किया कि हमें आपके हर साहित्य सम्मेलन में बुलाओ। बुद्धिजीवियों का कहना था कि आपका आयोजन साहित्य को बढ़ावा देने वाला है और बाकी जो अधिकतर साहित्य सम्मेलन होते हैं वे खाने, पीने, गाली देने, आलोचना करने, शराब पीने आदि में ही बीत जाते हैं। आपके यहां ऐसा कुछ भी नहीं है इसलिए बेहद आनंद आता है। हमारी संघर्ष यात्रा को आप यह कह सकते हैं कि हम चलते गए और पीछे कारवां बनता गया। इस बार हमारा 20वां भव्य समरसता साहित्य सम्मेलन होने वाला है।
भटके विमुक्त परिषद की स्थापना कैसे हुई और उसके द्वारा कौन से विशेष कार्य किए गए?
सामाजिक समरसता मंच की बैठक के दौरान श्री गिरीश प्रभुणे ने ‘भटके विमुक्त समाज’ की दयनीय अवस्था के संदर्भ में एक घंटे तक विस्तार से वर्णन किया। इसके बाद हमने निर्णय किया कि हमें इस विषय पर भी काम करना चाहिए। उस समय सुखदेव नवले जी, जो समरसता मंच से प्रारंभ से ही जुड़े हुए थे उनका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता था। विचारों को अमल में कैसे लाना है, प्रैक्टिकल कैसे करना है, इस मामले में वे मास्टर थे, विशेषज्ञ थे। सर्वप्रथम उन्होंने ही यह सुझाव दिया था कि हमें ‘भटके-विमुक्त परिषद’ नाम से एक संगठन बना कर कार्य आरंभ करना चाहिए। इसके बाद काम शुरू किया गया। उनका संपर्क भी व्यापक था। टिटवाला के एक दानवीर ने हमें 18 एकड़ जमीन छात्रावास के लिए दान दी। तब हमारे पास पैसे भी नहीं थे और अधिक कार्यकर्ता भी नहीं थे। डॉ. हेडगेवार जी ने कहा था कि हमारा कार्य ईश्वरीय कार्य है इसलिए काम की चिंता स्वयं ईश्वर को है। इसी सत्यनिष्ठा के आधार पर हमने कार्य शुरू किया। साप्ताहिक विवेक में लोगों से अपील कर और अन्य माध्यमों से हमने प्रयास किए। जिसके बाद चारों ओर से इतने साधन आने लगे और कार्यकर्ता भी आगे आकर कार्य करने लगे कि आज घुमंतू जाति के लोगों के आश्रय स्थान के नाम से यह छात्रावास बीज से वट वृक्ष का रूप धारण कर चुका है।
हिंदू धर्म में ही सामाजिक न्याय का स्रोत है, यह विचार आपने अपने साहित्य के माध्यम से समय – समय पर रखा है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे?
सामाजिक न्याय केवल जाति-पाति तक सीमित नहीं है। उसका बहुत ही व्यापक व गहन अर्थ निकलता है। बेहद कम ही लोग इसकी सटीक व्याख्या कर सकते हैं। समाज की व्यवस्था में राज व्यवस्था है, धर्म व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था है, कानून व्यवस्था है, अर्थ व्यवस्था है आदि व्यवस्थाओं के आधार पर समाज चलता है और इन सारी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए नियम बनाए जाते हैं, जिसे हम कानून कहते हैं। कभी-कभी कानून जनविरोधी हो जाते हैं; क्योंकि वे कानून समाज के बड़े वर्ग पर अन्याय करते हैं। राज्य कानून, अर्थ आदि व्यवस्था के कानून अन्याय करने वाले होते हैं। कानूनी अत्याचार से मुक्ति को ही सामाजिक न्याय कहा जाता है। यदि सामाजिक न्याय स्थापित करना है तो हमारे वाङ्मय और संतों के साहित्य में इस संदर्भ में काफी कुछ लिखा गया है। यह कोई नई बात नहीं है। यह बेहद पुरानी बात है। जैसे वरिष्ठ लेखक वीरेंद्र याज्ञिक जी ने अपने एक लेख में उल्लेख किया है कि श्रेष्ठ विकसित राज्य व्यवस्था का एक ही मानदंड है कि जिसका जिक्र राम चरित मानस में तुलसीदास जी ने किया है…
नहीं दरिद्र कोई, दुखी न दीन।
नहीं कोई अबुध, न लच्छन हीन॥
अर्थात वह राज्य व्यवस्था श्रेष्ठ है जहां न कोई दुखी है, न दीन है, न कोई अशिक्षित है और न ही कोई चरित्रहीन है। ऐसा जो समाज होगा, वह श्रेष्ठ समाज होगा। यह बहुत ही प्राचीन काल से हमारे यहां की संकल्पना है, संघकार्य की भी यही आत्मा है। हम कहते हैं कि इस राष्ट्र को परम वैभवशाली बनाना है। वैभवशाली का क्या अर्थ है, इसका मतलब है कि जहां कोई दीन, दुखी, गरीब, अनाथ कोई नहींं होगा। सभी के लिए जीवनावश्यक वस्तुएं आसानी से प्राप्त हो जाएंगी। इस प्रकार का एक समाज जीवन यहां स्थापित करना है। सामाजिक न्याय की संकल्पना भी संघ कार्य का अंतर्निहित अंग है। संघ की यह नई सोच है ऐसा बिल्कुल नहीं है। यह हमारी धार्मिक मान्यता, पुरानी परंपरा में निहित है। समय के अनुसार जिस भाषा और व्याख्या से लोग समझेंगे उस तरह से इस विचार को प्रस्तुत किया जाएगा।
हिंदू समाज और मुस्लिम समाज में अंतरद्वंद्व का भाव क्यो है, क्या वह आज का ज्वलंत विषय है?
मेरे दृष्टि से यह प्रश्न अपनी – जगह बेहद महत्वपूर्ण है लेकिन यह ज्वलंत नहीं है। मुस्लिम समाज की बात करें तो भारत में रहने वाला मुसलमान भारतीय वंश का है। वह अरब वंश का नहीं है। बावजूद इसके वे अरब संस्कृति, सभ्यता भाषा को अपना कर भारत में अलगाव के बीज बो रहे हैं। ऐसा लगता है कि वे अरब संस्कृति के गुलाम बन गए हैं। वर्तमान समय में मुसलमान पुरुषों व महिलाओं का जो पेहराव है वह अरबों की देन है। अरबों की संस्कृतिक गुलामी में क्यों रहें? यह मुस्लिम समाज को ही सोचना चाहिए। यदि मैं भारत में जन्मा हूं , मेरी नस्ल यहां की है, मैं संस्कृति से भी भारतीय हूं तो मैं अरब संस्कृति का गुलाम क्यों बनूं? इसका इस्लाम से क्या संबंध है? दाढ़ी, बुर्का का इस्लाम से क्या संबंध है? आधे पैजामे से इस्लाम का क्या संबंध है? इस्लाम का संबंध तो सीधे ईश्वर यानि अल्लाह से है। उससे मैं अधिक गहरा ज्ञान कैसे प्राप्त कर सकता हूं, यह सोच हो। ईश्वर और मानव में जो अंतर है उसे कम करने का जो मार्ग बताते हैं उसे धर्म कहते हैं। धर्म का खानपान, पेहराव आदि से कोई संबंध नहीं होता है। अरब में बहुत अधिक गर्मी, धूप होती है इसलिए पूरे शरीर को ढंकना पड़ता है। भारत में ऐसी कोई बात नहीं है। यहां सभी ऋतुएं समायानुसार आती हैं और जाती हैं। यह चक्र पहले से ही चलता आया है। उसे धर्म या मजहब के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। यह होगा, यह प्रक्रिया बड़ी ही तेजी के साथ आगे बढ़ेगी। मुस्लिम समाज समय के साथ भारतीय संस्कृति में ढलेगा, उनमें भी अन्य मुस्लिम देशों की तरह जागरूकता आ रही है। अरबी मानसिक गुलामी से वे बाहर जरूर आएंगे लेकिन उसके लिए उन पर दबाव बनाना और यह कहना कि ‘यदि इस देश में रहना होगा तो वंदेमातरम् कहना होगा’ यह बात उचित नहीं है। किसी पर कुछ लादने से कुछ नहीं होता है। जैसे बच्चे को ‘मां’ कहना है तो उसके लिए पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती है। वह सहजता से उसके मुख से निकलता है। इसी तरह भारत मेरी मां है यह उनके मुख से भी सहजता से आना चाहिए। किसी पर थोपने से मातृत्व भाव नहीं आता है। मुसलमानों को भी यह समझना व आकलन करना चाहिए कि विश्व के अन्य देशों में मुसलमानों की स्थिति क्या है? और भारत में रहने वाला मुसलमान कितना आजाद है। सामाजिक विषमता का एक कारण राजनीतिक विषमता भी है। वोट बैंक के लिए जाति-पाति को बढ़ावा देना, तुष्टिकरण करना, जातियों में भाषा, प्रांत, राज्य आदि के नाम पर भेद निर्माण करना और ‘फूट डालो और राज करो‘ की नीति भी राजनैतिक बनाम सामाजिक विषमता का मुख्य कारण है। सामाजिक विषमताएं समय के साथ ही धीरे – धीरे समाप्त होने के कगार पर हैं। ‘जन जागरण, साथ में पढ़ना, खाना, खेलना, काम करना, तथा आर्थिक व्यवहार के चलते सामान्य रूप से समाज चल पड़ा है। जन जागरण, समाज प्रबोधन और समय के साथ ही सामाजिक विषमताएं समाप्त हो जाएंगी। राजनीति द्वारा जो समाज को बांटने और विभाजन करने का षड्यंत्र किया जा रहा है, यह चिंता की बात है। समाज को जोड़ने वाली राजनीति को हम कैसे ला सकते है, इस पर हमें चिंतन करना होगा।
आप संघ, हिंदुत्व और सामाजिक समरसता से जुड़े हुए हैं, गांधीजी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में आपने गांधी विचारों को भी समाज के सामने प्रस्तुत करना प्रारंभ किया है, यह आपका विचार परिवर्तन है या संस्कार है?
मुझ पर संघ संस्कारों का बहुत ही गहरा प्रभाव है और संघ का मानना है कि जिसने भी राष्ट्रहित में निस्वार्थ भाव से कार्य किया है, वे सब हमारे हैं। उस व्यक्ति की विचारधारा क्या है, यदि वह संघ को कुछ भला-बुरा भी कहता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उसकी राष्ट्र सेवा का सम्मान संघ करता है और देश हित में किया हुआ कार्य – समर्पण यह चिरंतन रहने वाला है, यह संघ का मानना है। निस्वार्थ भाव से राष्ट्र सेवा करने वालों से स्वत: ही संघ का नाता जुड़ जाता है। गांधीजी की बात करें तो उनका पूरा जीवन समाज समर्पित था और देश के अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को जोड़ने का जो उनका प्रयास रहा वह उनकी सबसे बड़ी महानता है। भारतीय मूल्यों, संस्कारों का पालन करते हुए उन्होंने समाज के सामने जो आदर्श स्थापित किए वे अनुकरणीय हैं। इसलिए उन्हें ‘महात्मा’ कहा जाने लगा। राम भक्ति, गो भक्ति और धमार्र्ंतरण का प्रखर विरोध करने वाले सत्यनिष्ठ गांधीजी का आध्यात्मिक जीवन सभी के लिए प्रेरणादायी है। एक स्वयंसेवक और इस राष्ट्र का एक घटक होने के नाते मेरा यह कर्तव्य है कि महात्मा गांधी के सकारात्मक प्रासंगिक विचारों को मैं सबके सामने लाऊं।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी से मिलने पतंगे जी के साथ जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। राष्ट्रपति भवन में जाने से पहले मन पर एक प्रकार का दबाव था कि देश के प्रथम नागरिक से मिलने जा रहे हैं, वह किस प्रकार से बात करेंगे। लेकिन जब वहां मिलने का अवसर आया तब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी अत्यंत सरलता से हम सभी से वार्ता कर रहे थे। राष्ट्रपति कोविंद जी बिहार से हैं। रमेश पतंगे जी ने मा. कोविंद जी के साथ में समरसता का कार्य बिहार में किया है। मुलाकात के समय रमेश जी ने राष्ट्रपति जी से कहा- हमें गर्व है कि समरसता का कार्य करने वाले कोविंद जी आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति के रूप में हमसे मिल रहे हैं। रमेश पतंगे जी की ये बातें सुन कर कोविंद जी अत्यंत नम्रतापूर्वक कहने लगे- रमेश जी इस संपूर्ण प्रवास में आपके विचारों का बहुत बड़ा योगदान हमें मिला है।
गांधीजी के जीवन मूल्यों और संघ के मूल्यों को जोड़ने का आप प्रयास करते हैं, इन दोनों में किस प्रकार की समानता है?
गांधी और संघ में समानता के अनेक मुद्दे हैं। डॉ. हेडगेवार ने संघ शाखा शुरू करते समय एक गहरा चिंतन यह किया कि देश के नागरिकों के सामने मुझे ऐसा एक कार्यक्रम रखना चाहिए जो करते समय उनमें यही भावना रहनी चाहिए कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूं वह देश के लिए कर रहा हूं। एक घंटे की संघ शाखा में क्या होता है, ध्वज प्रणाम, महापुरूषों का स्मरण, संघ प्रार्थना, खेल, योग, व्यायाम, देशभक्ति गीत। इसमें किसी का व्यक्तिगत विचार, धार्मिक विचार, जातिगत विचार नहीं होता है। केवल देशहित के विचारों पर ही मंथन, चिंतन होता है। इसमें किसी को व्यक्तिगत लाभ नहीं होता। यह सब मुझे देश के लिए करना है, रा. स्व. संघ की प्रार्थना में ‘त्वदियाय कार्याय बद्धा कटियम’ का ही हम संकल्प करते हैं। गांधीजी ने भी कुछ ऐसा ही किया। देश के साधारण नागरिकों को भी लगे कि मैं देश के लिए कुछ करता हूं। इस संदर्भ में गहरा चिंतन करने के बाद उन्होंने चरखा चलाने और सूत कातने की बात देश के नागरिकों के सामने रखी। और ये कार्य करते समय मन में यह भाव होना चाहिए कि ये जो मैं चरखा चला रहा हूं वह देश के लिए चला रहा हूं। इससे धागा बनेगा, फिर वस्त्र बनेगा। देश का नागरिक स्वदेशी वस्त्र पहनेगा, यह विचार पूरे देश की भावना बन गई। एक घंटे की संघ शाखा और एक घंटा चरखा चलाना इन दोनों के तत्व, दृष्टिकोण में कोई अंतर मुझे दिखाई नहीं देता। दूसरी प्रमुख समानता की बात बताता हूं। गांधीजी ने कहा था कि जिसे समाज सेवा एवं देशसेवा करनी है उसे एकादश व्रत का पालन करना चाहिए। इसमें सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, शुद्धता, सदाचार आदि 11 व्रत नियम उन्होंने बताए। दूसरी ओर संघ में कोई लिखित रूप से नियम नहीं हैं लेकिन संघ का कार्य करना है तो स्वयंसेवक का निस्वार्थ होना आवश्यक है। यदि आप निस्वार्थ कार्य करेंगे तो ही टिक पाएंगे। समय का पालन करना चाहिए। शाखा 6.30 बजे लगनी है तो उसी समय लगनी चाहिए, जिस समय कार्यक्रम तय हुआ है उसी समय वह शुरू होना चाहिए, अनुशासन का कड़ाई से पालन होना चाहिए। ऐसे ही अलिखित लेकिन प्रभावी नियमों का संघ स्वयंसेवक पालन करता है। गांधीजी के व्रत नियमों और संघ के आचरण रूपी नियमों के शब्दों में हेरफेर हो सकता है लेकिन उसके तत्वज्ञान में अंतर नहीं हो सकता। इसमें समानता साफ दिखाई देती है। इसके अलावा गांधीजी ने कहा कि यदि देश का काम करना है तो हमें फल की आशा नहीं करनी चाहिए। उसी तरह संघ का भी यही कहना है कि निस्वार्थ भाव से देश के लिए कार्य करो लेकिन कुछ पाने की इच्छा मत करो। जैसे हमारी सरकार बनेगी तो हमें यह पद मिलेगा, वह पद मिलेगा। ऐसी तुच्छ भावना से काम नहींं करना चाहिए बल्कि कर्तव्य भाव से राष्ट्रहित में कर्म करना चाहिए। जब देश को आजादी मिली तब गांधीजी चाहते तो राष्ट्रपति बन सकते थे। गर्वनर जनरल बन सकते थे। जो चाहे वह बन सकते थे लेकिन उन्होंने किसी पद की लालसा नहीं की और कलकत्ता के नोआखाली में भीषण दंगे को शांत करने के लिए वहां चले गए। सत्ता से वे सदा ही दूर रहे। गांधीजी ने इसका चिंतन भी किया कि हजारों सालों से हमारा राष्ट्र जीवित कैसे रहा, इसलिए कि हमारा समाज कभी भी सत्ता के आश्रित नहीं रहा, सत्ता पर निर्भर नहीं रहा। हमारा समाज आत्मनिर्भर होना चाहिए। संघ इसकी मिसाल है। संघ कभी भी सत्ता पर निर्भर नहीं रहा। संघ अपने कार्य के लिए राज्य सत्ता से एक पाई भी नहीं लेता। केंद्र में हमारी सरकार है तो गुरु दक्षिणा बढ़ी है ऐसा बिल्कुल नहीं होता। संघ का कार्यालय बनाना है तो इसके लिए भी सरकार से कभी भी आर्थिक सहयोग नहीं लिया गया। एक स्वयंसेवक के नाते समाज द्वारा मिले सहयोग के आधार पर ही संघकार्य आगे बढ़ता रहा है। समाज के आधार पर ही हमें खड़ा रहना है। समाज सर्वशक्तिमान है। वहीं समय आने पर सब कुछ देगा। यह गांधीजी और संघ विचारों की बहुत बड़ी समानता है।
वर्तमान मे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में जो कार्य चल रहा है इसे आप किस दृष्टी से देखते है?
स्वयंसेवकों के सत्ता में आने के कारण दूरगामी परिवर्तन होने लगे हैं। पहले राजनीति का केंद्रबिंदु व्यक्ति विशेष, फिर पार्टी और जाति हुआ करती थी; लेकिन अब राजनीति का केंद्रबिंदु ‘देश’ होने लगा है। धारा 370, 35 – ए हटाना, पुलवामा के बाद पाकिस्तान के अंदर घुस कर बदला लेना, चंद्रयान-2का प्रयास आदि महत्वपूर्ण कदम देशहित में काम करने के प्रमुख उदाहरण हैं। हमने हजारों वर्षों की गुलामी झेली तो उसका मूल कारण यह था कि हमें देश के लिए जीना है, त्याग, बलिदान, समर्पण करना है, देश की सुरक्षा के लिए हमें सर्वस्व न्योछावर करना है, यह हम भूल गए थे। देशहित की भावना जगाने का काम मोदी सरकार के आने के बाद तेज गति से हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदीजी ने अपील की कि गैस सब्सिडी छोड़ दो तो लाखों लोगों ने अपनी सब्सिडी छोड़ दी। आजादी के बाद ऐसा पहली बार हुआ है। गांधीजी के काल में ऐसा होता था। जब गांधीजी कोई बात कहते थे तो उनके पीछे देश चल पड़ता था। आज फिर उसी तरह मोदी जी के पीछे देश सहित दुनिया चल रही है।
देश मे हो रहे परिवर्तन मे रा. स्व. संघ के योगदान को आप किस परिदृश्य में देख रहे है?
परिवर्तन का जो मंजर दिखाई दे रहा है उसके पीछे संघ के 92 वर्षों के अथक परिश्रम, तपस्या व साधना का ही सुफल है। संघ का विचार कोई नया नहीं है। यह बहुत ही पुरातन-सनातन, संतों का विचार है। स्वामी विवेकानंद, महात्मा गौतम बुद्ध, डॉ. बाबासाहब आंबेडकर, छत्रपति शिवाजी महाराज आदि महापुरूषों के विचारों को लेकर ही संघ चला है। जैसे ढाई हजार वर्ष पहले गौतम बुद्ध ने जो महान कार्य किए थे, उनकी प्रेरणा से वैसे ही कार्य संघ भी कर रहा है। हजारों वर्षों के कालचक्र में महापुरूषों के विचार क्षीण हो जाते हैं या विलुप्त हो जाते हैं। उन्हें फिर से जगाना पड़ता है। आज की परिस्थिति में प्रश्न क्या है, आज की परिभाषा क्या है, भाषा क्या है, कौन सी भाषा में बात कहने से लोगों को सुलभ तरीके से समझ में आएगा वही पुरातन विचार प्रासंगिक होने पर नए ढंग से रखना पड़ता है। संघ वही करता है। विषय, विचार, तत्व के लिए जीने वाले लक्ष्य के लिए मरने मिटने वाले कार्यकर्ताओं की विशाल फौज संघ ने पूरे देश और दुनिया में खड़ी की है। लोग अध्यात्म तो जानते हैं लेकिन उसे अपने जीवन में उतार नहीं पाते। जब लोग सत्यनिष्ठा आध्यात्मिक जीवन जीने वाले आदर्श पुरूष को साक्षात देखते हैं तो उन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। संघ ऐसे ही चरित्रवान आदर्श पुरूष खड़ा करने का महान कार्य करता है। यह संघ की सबसे बड़ी विशेषता, सफलता और उपलब्धि है। मेरा मानना है कि परिवर्तन के दौर में समय के साथ संघ ने भी स्वयं में परिवर्तन किया है और यह प्रक्रिया निरंतर जारी रहेंगी। बावजूद इसके सफलता का श्रेय संघ स्वयं लेगा ऐसा बिल्कुल नहीं है। संघ का मानना है कि श्रेय का अधिकार केवल समाज को है। संघ तो केवल निमित्त मात्र है।
ट्रेन, चाय, सर्दी और शाल
पुणे में विवेक का कार्य बड़े विस्तार से चलता है। इस कारण अक्सर पुणे में आना जाना चलता रहता था। एक बार एक समारोह के निमित्त रमेश पंतगे जी के साथ मेरा पुणे जाना हुआ। पुणे से आते वक्त हम दानों ट्रेन से प्रवास कर रहे थे। दिसंबर का महीना होने के कारण ठंड अपनी चरम सीमा पर थी और ठंड के कारण चाय पीने की इच्छा बार-बार हो रही थी। ऐसे में चायवाला -चायवाला कह के गुजर रहे एक चायवाले को हमने दो चाय देने के लिए कहा। चाय कप में डालते समय ठंड के कारण उसके हाथ कांप रहे थे। उसकी इस स्थिति को देख कर हमने उस पर एक नजर घुमाई। तब हमें महसूस हुआ कि वह चायवाला सिर्फ एक बनियान पर घूम रहा है। हमने उसके पास से दो चाय ली मैंने दो चाय के पैसे उसको दे दिए। जैसे ही वह जाने लगा तब पंतगे जी ने उसे रोका एवं उससे कहा- थोडा रुकिए। पंतगे जी ने इस थोड़े से अवधि में अपनी हैन्ड बैग से शाल निकाली और उस चाय वाले के कंधे पर रख दी और कहा- इस शाल को अपने बदन पर रख कर चाय बेेचो, अंत्यत कड़ाके की ठंड पड़ रही है।
आपके दृष्टी से हिंदुत्व की परिभाषा क्या है?
मेरा व्यक्तिगत मानना है कि हिंदुत्व शब्दप्रयोग उचित नहीं हैं क्योंकि हिंदुत्व शब्द कहने के बाद एक क्लोज फिलॉसफी बनती है, जैसे कम्यूनिज्म है, सोशलिज्म है, कैपिटालिज्म है, लेकिन‘हिंदू’ में इज्म नहीं है। परंतु हिंदुत्व कहने के बाद लोग इसे इज्म की दृष्टि से देखते हैं। इसलिए हम हिंदुत्व शब्द से सीमित हो जाते हैं। हिंदू शब्द तो वैश्विक है इसलिए इसका सही शब्दप्रयोग करना है तो हिंदूपन (अंग्रेजी में कहना हो तो हिंदूनेस) कहना उचित होगा। या केवल हिंदू कहना ही पर्याप्त होगा, ‘त्व’ लगाने की आवश्यकता नहीं है। हिंदू की परिभाषा यह है कि वह न केवल संपूर्ण विश्व के कल्याण की बात सोचना है बल्कि चराचर सृष्टि के साथ ही पूरे ब्रह्मांड के कल्याण की भी कामना करता है। जहां तक किसी ने सोचा तक नहीं है।
क्या हिंदुत्व के सहारे भाजपा ने सत्ता प्राप्त की है?
कांग्रेसी विचारधारा के अंतर्गत नेहरूवाद, सेक्यूलरिज्म आदि के मायाजाल को तोड़ने के लिए और देश की आत्मा, भावना को जगाने हेतु भाजपा ने हिंदुत्व शब्द का प्रयोग किया। ‘हिंदुत्व ही राष्ट्रीयत्व है’ के आधार पर प्रखर राष्ट्रवाद का भाजपा ने जोरशोर से मुद्दा उठाया, जिसका उसे लाभ मिला और उसे सत्ता के सिंहासन तक पहुंचने में मदद मिली। राष्ट्रीय अस्मिता से जुड़े राम जन्मभूमि आंदोलन, राम जानकी रथ यात्रा, देश की एकता व अखंडता के लिए धारा 370 खत्म करना, जम्मू – कश्मीर और लद्दाख को अलग कर दोनों को ही केंद्रशासित प्रदेश बनाना, पाकिस्तान और चीन को उसकी ही भाषा में जवाब देना आदि अनेक कार्य भाजपा के सत्ता में पहुंचने में सहायक रहे हैं।
आप 25 वर्षों तक सा. विवेक के सम्पादक रहे और अब हिंदुस्थान प्रकाशन संस्था के अध्यक्ष के रूप में अपना योगदान दे रहे हैं। विवेक परिवार और संस्था की प्रगति में आपने कैसे अहम भूमिका निभाई?
विवेक जैसी संस्था किसी एक व्यक्ति के कर्तृत्व पर खडी नहीं होती। उसमे सबका सामुहिक योगदान होता हैं। समरसता मंच, भटके विमुक्त विकास परिषद, साहित्य परिषद आदि संस्थाओं का काम सामूहिक रूप से ही चलता हैं। विवेक का काम करते समय किसी भी विषय पर सबकी सहमति बनानी होती हैं। सहमति होने के कारण हाथ में लिया हुआ काम अपना लगने लगता हैं। मैने और दिलीप करंबेलकर जी ने यही किया। एक टीम खडी की और सामूहिक भाव से काम किया। सफलता के कुछ मुख्य कारण होते हैं जैसे कि हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। स्वयं का स्वार्थ नहीं होना चाहिए कि यह कार्य सफल होने पर मुझे क्या मिलेगा। मुझे कोई बड़ा पद, प्रतिष्ठा या पुरस्कार मिलेगा क्या? यदि ऐसी कोई भावना हमारे मन में रही तो उसका असर हमारे काम पर और हमारी टीम पर होता है। जब टीम यह देखती-महसूस करती है कि हमारा मुखिया कार्य के प्रति निस्वार्थ रूप से समर्पित है तो वह भी उसी भाव से कार्यों में जुट जाती है। ऐसा कार्य शुरू हो गया तो उसमें सफलता तो मिलनी ही है। इस सकारात्मक मार्ग से गए और असफल हो गए ऐसा होना तो असंभव है। हमारा कार्य ईश्वरीय कार्य है, इसी भावना से हम कार्य करते गए और हमें एक के बाद एक सफलता मिलती गई। इसी मार्ग से आगे भी विवेक चलना चाहिए।
मैं, मनु और संघ, हमारा मौलिक संविधान आदि दर्जनों प्रसिद्ध पुस्तकें आपने लिखी हैं। क्या आप अपने लेखन से संतुष्ट हैं या इससे भी आगे जाकर कुछ करना चाहते हैं?
पत्रकारिता व साहित्यिक क्षेत्र में लंबा सफर तय करने के बाद मन में ऐसा ख्याल आता है कि बस अब रुकना चाहिए, विश्राम करना चाहिए, जितना करना था उतना कर दिया। ऐसा विचार मन में आते ही जो हम से काम कराने वाला ऊपर बैठा है वह फिर कोई बड़ी जिम्मेदारी व विचार मन में डाल देता है। फिर ध्यान में आता है अरे यह विशेष कार्य तो रह गया है। हिंदुत्व का सामाजिक आशय विषय होने के बाद मेरे सामने संविधान का विषय आया। उस समय तक तो मैं संविधान के बारे में कुछ जानता भी नहीं था और उसे पढ़ा भी नहीं था। फिर मन में यह भाव आया कि आगे जाकर तो हमें ही देश चलाना है। स्वयंसेवक ही देश का नेतृत्व करेंगे और देश संविधान से चलता है, इसके लिए संविधान को जानना- समझना भी बेहद जरूरी है। इसके बाद मेरा गहन अध्ययन शुरू हुआ और फिर मैंने संविधान पर पुस्तक लिखी। इसके उपरांत गांधीजी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में उनके जीवन पर प्रकाश डालने का विचार मन में आया और मैंने गांधीजी के आदर्श जीवन के अनेक पहलुओं तथा उनके विचारों की वर्तमान समय में प्रासंगिकता को समाज के सामने रखा। गांधीजी की महापुरुषों से तुलना करना मैं ठीक नहीं समझता। लेकिन वाकई उनका कद भी महापुरुषों के समतुल्य था। यह कार्य संपन्न होने पर लगता है कि बस अब हो गया लेकिन आने वाले समय में ईश्वर मुझे कोई अन्य कार्य सौंप दे तो मैं बता नहीं सकता।
बाल स्वयंसेवक से लेकर अब तक संघ कार्यों से आप जुड़े रहे हैं। इस दौरान लगभग सात दशकों का सफर आपने तय किया है। क्या आपके मन में ऐसा सवाल नहीं उठा कि समग्र संघकार्य पर भी आपको एक मौलिक पुस्तक लिखनी चाहिए?
बहुत पहले मैंने ‘डॉ. साहब मेरी दृष्टि में’ पुस्तक लिखी थी, डॉ. हेडगेवार जी के बारे में। उम्र के इस पड़ाव में मुझे ऐसा लगता है कि संघ को जितना मैंने जाना है, समझा है, अनुभव किया है उस पर मुझे लिखना चाहिए। वैसे संघ पर बहुत किताबें लिखी गई हैं, उनमें से कई किताबें मैंने पढ़ी हैं लेकिन उससे मुझे संतुष्टि नहीं मिली है। मेरी अंतरात्मा को उतना आनंद नहींं आता है जितना मुझे चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि इससे भी गहरा कुछ लिखना चाहिए। क्योंकि संघ जैसा चिंतन और संघकार्य जो है वह युग परिवर्तन कार्य है। इस युग परिवर्तन कार्य को विस्तारपूर्वक और सही परिप्रेक्ष्य में शब्दबद्ध करना चाहिए, ऐसी मेरी इच्छा है। यदि समय मिला और स्वास्थ्य उत्तम रहा तो यह कार्य मैं जरूर पूरा करूंगा।
खरीदूं तो चूल्हा जलें
पंतगे जी के साथ अमरावती प्रवास में मैं भी गया था। अमरावती में जाने से पहले देहाती गांवों से होकर गुजरना पड़ता है। यह बात 1997-98 की है। रास्ते में बहुत सारे आदिवासियों की बस्ती लगती थी। रास्ते में एक मोड पर एक आदिवासी महिला जंगल से संबधित खाद्य पदार्थों की बिक्री कर रही थी। पंतगे जी ने वहां से कुछ दूरी पर गाडी को रुकवाया और गाडी से उतर कर उस महिला के पास वन संपदा से जुड़े जोे-जो खाद्य पदार्थ थे, उन सभी को एक-एक करके खरीदा। अंदाजन 200 रुपयों तक पंतगे जी ने उस महिला के पास से खरीदारी की। जब हम दोनों गाड़ी की तरफ जाने लगे तब मैंने पतगे जी से पूछा- पंतगे जी ये जो खाद्य पदार्थ आपने लिए हैं वे खाएगा कौन? तब उन्होंने सहजता से कहा कि जहां हम कार्यक्रम के लिए जाने वाले हैं वहां किसी को दे देंगे। नहीं तो अमरावती के संघ कार्यालय में रखेंगे। उनकी इस बात को सुनकर मैं ने उनसे पूछा- पंतगे जी यह खाद्य खाना नहीं है, किसके लिए ले रहे हैं यह नहीं जानते, फिर आपने उस महिला से यह चीजें क्यो खरीदीं? तब पंतगे जी ने कहा- अमोल, उस महिला की स्थिति को तुमने ठीक से देखा, अत्यंत गरीब घर की आदिवासी महिला है। निश्चित रूप से उसका पति नशे के अधीन होगा। उसकी स्थिति को देखते हुए उसे आज के खाने की चिंता जरूर होगी। ऐसे अदिवासी महिला से मैं कुछ खरीदता हूं तो उसका उपयोग वह महिला आज शाम अपने घर चूल्हा जलाने के लिए कर सकती है।
संघकार्य करते समय राजनीति में अपना सिक्का जमाने का विचार क्या कभी आपके मन में आया है?
जागते समय या सोते समय भी मेरे मन में ऐसा विचार कभी नहीं आया कि मुझे राजनीति में जाना चाहिए। क्योंकि उसमें मुझे कोई रूचि नहीं है। जब मैं बोरिवली भाग का कार्यवाह था तब रामभाऊ नाईक हमारे विधायक थे। कार्यवाह के नाते उनसे मिलना जुलना और घर आना जाना होता था। तब मैं देखता था कि लोग उनके घर के बाहर सुबह 6 बजे से आकर बैठे रहते थे। उस समय मेरे मन में सवाल आता था कि यदि मैं उनकी जगह होता तो 10 दिन में ही भाग खड़ा होता। क्योंकि किसी का नल टूटा है, सड़क पर गड्ढे हैं जैसे विषय यह मेरा कार्य नहीं है। मैं इसमें टिकने वाला व्यक्ति नहीं हूं। जब हमारी सरकार बनी तब मैंने महाराष्ट्र और केंद्र सरकार से भी कहा कि मुझे किसी भी पद पर मत भेजना, मैं नहीं जाना चाहता हूं। उन्होंने मुझसे सवाल किया कि हमारे यहां तो लोग लाइन लगाकर बैठे हैं ऐसे में आप मना क्यों कर रहे हैं? तब मैंने उनसे कहा कि ये सारे काम तो कोई भी कर सकता है लेकिन मैं जो लेखन का काम कर रहा हूं, वह मेरे सिवा दूसरा कोई नहीं कर सकता। फिर मैं इसमें अपना समय क्यों बर्बाद करूं। बावजूद इसके मुझे सेंसर बोर्ड में भेजा गया। एक बार नाम आने के बाद और कार्य सौंपने के बाद उसे नकारना भी ठीक नहीं था और संघ की पद्धति क्या है यह मुझे पता है इसलिए उसे मैंने स्वीकार कर लिया और मैं सहर्ष काम कर रहा हूं। संघ स्वयंसेवक का स्वभाव ऐसा होना चाहिए कि उसे जो काम सौंपा जाए उसे वह सहर्ष स्वीकार करें। इस संदर्भ में बालासाहब देवरस जी कहा करते थे कि आपको बहुत ज्ञान है इसलिए वहां भेजा जा रहा है ऐसा नहीं है। वह काम करो, धीरे – धीरे सीख जाओगे करते-करते।
सफलता प्राप्त करने के लिए अपनी ताकत, हुनर और अपनी कमियों को पहचानना बेहद जरूरी होती है। इस पर आपकी क्या राय है?
हमारा सामर्थ्य क्या है? हर किसी को अपनी पहचान होनी चाहिए। वह दो प्रकार की होनी चाहिए। मैं क्या कर सकता हूं और क्या नहीं कर सकता हूं यह पता होना चाहिए। यह भी पता होना चाहिए कि यह मेरा फील्ड नहीं है। यदि ये बातें पता हो तो हमें कभी कठिनाई नहीं आएगी।
आप अच्छे खाने के बहुत शौकिन हैं और अच्छे रसोइये भी हैं। क्या आपकी सजग पत्रकारिता एवं सेहत का राज आपका खानपान है?
बचपन से ही मुझे गरमागरम खाना पसंद है। मैं कभी भी ठंडी रोटी नहीं खा सकता। स्वयंसेवक के नाते मुझे सैंकड़ों घरों में भोजन के लिए जाना पड़ता था। कहीं मुझे स्वादिष्ट खाना मिला तो मैं पूछता था कि आपने यह व्यंजन कैसे बनाया। मुझे स्वाद से ही पता चल जाता है कि इसमें क्या डाला गया है। एक रसोइया होने के कारण मैं घर पर वहीं व्यंजन बनाता था, जिसे खाकर सभी लोग मेरी खूब तारीफ करते थे। आज भी जब कभी समय मिलता है, मैं स्वयं अपने हाथों से भोजन बनाता हूं और सबको खिलाता हूं। काम के सिलसिले में जब मैं कहीं बाहर जाता हूं तो भोजन के लिए बड़े – बड़े होटलों में नहीं जाता क्योंकि वहां उतना स्वादिष्ट पौष्टिक खाना नहीं मिलता। स्थानीय दुकानदार या वाहन चालक से पूछता हूं कि भाई यहां पर अच्छा खाना कहां मिलेगा तब वे 2-4 होटलों के नाम गिनाते हैं और वहां पर 99 फीसदी बहुत ही अच्छा खाना मिलता है। फर्स्ट क्लास होटलों में उतना अच्छा खाना नहीं मिलता जितना ढाबे में मिलता है। यह बात सत्य है कि अच्छे खानपान से ही स्वास्थ्य उत्तम रहता है। मेरी भी सेहत में सात्विक भोजन का अहम योगदान है।
आपकी सफलता के पीछे आपकी धर्मपत्नी का सबसे बड़ा योगदान माना जाता है। कृपया इस बारे में कुछ बताएं?
यह बात बिल्कुल सही है, मेरी पत्नी ने मेरा भरपूर साथ दिया और अब भी पूरी निष्ठा से दे रही है। जैसे विवेक में आना ‘नियति‘ की इच्छा थी उसी तरह मेरी उनके साथ शादी होना भी ईश्वर की कृपा थी। उनके चाचा मेरे साथ जेल में थे। जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने मेरे सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। मुझे बड़ा ही आश्चर्य हुआ क्योंकि वे आर्थिक रूप से 20वीं पायदान पर होंगे तो मैं पहली पायदान पर था। ऐसी आर्थिक स्थिति में हमारा विवाह कैसे हो सकता है यह बात मैंने उन्हें बताई और कहा कि आपने रमेश पतंगे का भाषण सुना, जेल में देखा, एक कार्यकर्ता के रूप में आप मुझे पसंद करते होंगे, यहां तक तो ठीक है; लेकिन घर – परिवार चलाने के लिए इतना काफी नहीं होता, उसके लिए तो आर्थिक स्थिति ही सबसे अधिक मायने रखती है। मैं तो बेहद सामान्य व्यक्ति हूं। इसके बाद उन्होंने कहा कि सब चलेगा, फिर मैंने कहा कि लड़की से भी पूछें। उस समय पुराने संस्कारों के अनुरूप मां-बाप, भाई जैसा कहेंगे, वैसे शादी करने के रिवाज के तहत हमारी शादी हो गई। एक आलिशान घर में पली-बढ़ी वह, चाल के मेरे एक छोटे से घर में आकर रहने लगी। लेकिन इससे उसे प्रारंभ से ही अप्रसन्नता नहीं हुई। जो है जैसे है वैसे आनंद से रहना यह उसका स्वभाव था। ये चाहिए वो चाहिए, इतने छोटे घर में मैं कैसे रहूंगी, इस तरह के शिकवे-शिकायतें उसने कभी नहीं कीं। यह उसकी सबसे बड़ी विशेषता थी। एक संपन्न घर से आना और छोटे से घर में रहना बड़ा ही मुश्किल होता है। मैं बड़ा ही सौभाग्यशाली हूं कि मुझे इतनी अच्छी धर्मपत्नी जीवन संगिनी के रूप में मिली।
आपने सफलताओं की कई ऊंचाइयों को छुआ है, बावजूद इसके आपकी संवेदनशीलता एवं मानवीयता में कोई कमी नहीं आई। आपने अपने मन की संवेदनशीलता को कैसे बरकरार रखा है?
मेरा पूरा बचपन गरीबी रेखा से नीचे जीने वाले स्तर पर गुजरा है। भूख क्या होती है, दुख क्या होता है इसका मैंने अनुभव किया है। पूरा दिन भूखा रहने की पीड़ा क्या होती है, उस समय बच्चा कितना असहाय होता है, यह मैं जानता हूं। वह खुद तो कुछ कर नहीं सकता है, कमा नहीं सकता है, तब वह रोता-बिलखता हुआ मां के पास ही जाएगा। मां भी कितनी असहाय अवस्था में होती है। ऐसी स्थिति बहुत ही हृदय विदारक होती है। इन सब दृश्यों को मैंने अपनी आखों से देखा है इसलिए मेरी संवेदनशीलता आज भी वैसे ही बरकरार है जैसे तब थी। यदि कोई दुख तकलीफ में है तो यथासंभव मैं उसकी सहायता करने का प्रयास करता हूं।
आप एक चिंतक, विश्लेषक, विचारक हैं और एक अच्छे श्रोता भी हैं साथ में संगीत में भी रूचि रखते हैं। यह सब कैसे कर पाते हैं आप?
मानव जीवन बहुआयामी होता है, और जो उसका सार्वजनिक जीवन होता है, जिसे देख कर उसे ही सही मान लेना यह ठीक नहीं है। यह सही बात है कि मैं चिंतन करता हूं, लिखता हूं, पढ़ता हूं लेकिन मैं इसी अवस्था में 24 घंटे नहीं रह सकता। कोई भी व्यक्ति हो, वह थक जाता है, उसे विश्राम की आवश्यकता होती है। वह मनोरंजन के लिए मूवी, संगीत, नाटक आदि का उपयोग करता है। मैं सबसे अधिक शास्त्रीय संगीत सुनता हूं। उससे मेरी सारी शारीरिक व मानसिक थकान दूर हो जाती है और मुझ में फिर से एक नई ऊर्जा संचारित हो जाती है। शास्त्रीय संगीत की एक खासियत यह है कि जो उसे सुनेगा वह उसमें ही खो जाएगा, रम जाएगा। शास्त्रीय संगीत को सुनने, समझने और अनुभव करने के बाद फिर किसी अन्य संगीत सुनने की आवश्यकता ही महसूस नहीं होती। कभी-कभी खाली समय में अथवा आते-जाते कानों में शास्त्रीय संगीत के स्वर स्वयं ही सुनाई देते हैं, जो असीम शांति का आनंद प्रदान करते हैं। फिर घर जाने पर मैं वही शास्त्रीय संगीत सुनता हूं; जो मुझे अद्भुत शांति के साथ ही प्रसन्नचित्त कर देता है।
चर्मकार भी बाराती – विवेक साप्ताहिक का कार्यालय प्रभादेवी में सिद्धि विनायक मंदिर के सामने है। इस कारण कोई हमारा पता पूछे तो हम बताते हैं कि सिद्धि विनायक के प्रभाव क्षेत्र में हमारा कार्य चलता है। कार्यालय के रास्ते पर और सिद्धि विनायक मंदिर के सामने एक जूते सिलने वाला चर्मकार (जाटव) गत 30 सालों से वहां अपनी छोटीसी दुकान लगाकर बैठता है। चर्मकार के उस दुकान को और उस चर्मकार के पेहराव को देख कर उसकी गरीबी का अहसास हमें होता है। रोज कार्यालय में आते समय उस चर्मकार के दर्शन हमें होते हैं। रमेश पतंगे जी की सबसे छोटी लड़की की शादी मुलुंड में संपन्न हुई। उस शादी में रा. स्व. संघ के सरसंघचालक डॉ. मोहनजी भागवत, रा. स्व. संघ के सरकार्यवाह भैयाजी जोशी, भारतीय जनता पार्टी के गोपीनाथ मुंडे जी आदि नेता उपस्थित थे। इनके अलावा साप्ताहिक विवेक के रास्ते पर रोज दिखने वाला चर्मकार भी उपस्थित था। वह सफारी पहने हुए आया था। रोज के उसके दर्शन और आज के दर्शन में बहुत अंतर था। वह कह रहा था, पंतगे जी जैसे एक विचारक द्वारा मुझ जैसे चर्मकार को अपनी लड़की की शादी में बुलाना यह मेरे जीवन का सबसे सुखद क्षण है।
75 वर्ष के आयु में भी आप अपने आप को वर्तमान समय के साथ अपडेट रखते हो। इस बढती आयु में भी आप यह सब कैसे आत्मसात कर पाते हैं?
व्यक्ति यदि अपनी बढ़ती उम्र के बारे में ही सोचता रहेगा तो वह मन से भी बूढा हो जाएगा। मैं कभी अपनी आयु के बारे में सोचता भी नहीं हूं। मेरी इस बारे में ऐसी धारणा है कि कालचक्र के अनुसार समय चलता जाएगा, क्या उसी प्रकार मैं भी अपने कार्यों को गति दे सकता हूं, समाज और देशहित में कोई आवश्यक कार्य कर सकता हूं, कुछ नया सीख सकता हूं जिससे देश का भला हो। जन्मदिन मनाना मुझे अच्छा नहीं लगता; क्योंकि वह मुझे बढ़ती उम्र की याद दिलाता है। जब भी कोई मुझे जन्मदिन पर शुभकामना संदेश भेजता है तब ध्यान में आता है कि मेरे जीवन का बड़ा हिस्सा गुजर गया है। मेरी इच्छा है कि जब तक मैं जीऊं तब तक मेरे इस शरीर द्वारा देशहित में कार्य होता रहे। जापान और अन्य विकसित देशों के बुजुर्गों की एक विशेषता होती है कि वे अपनी जिंदगी के अंतिम पड़ाव में भी कुछ न कुछ नया सीखते रहते हैं और उस पर काम करते रहते हैं। उसी तरह मैं भी अपना जीवन सार्थक बनाना चाहता हूं। इसलिए मैंने भी समय के साथ बदलाव किया है और आध्ाुनिक विचार और अत्याधुनिक यंत्रों का उपयोग करता हूं। कैंडल नामक यंत्र से घर बैठे ही जो चाहे पुस्तके सस्ती किमतों पर मंगा कर उसे पढ़ता रहता हूं। इसमें अधिक संख्या में पुस्तकों का भंडारण किया जा सकता है। हालांकि मेरे बच्चों ने ही मुझे इसे कैसे चलाना है, यह सिखाया है। हमारे देश का यह दुर्भाग्य है कि अधिकतर लोग 60-70 वर्ष की उम्र पार करने के बाद यह सोचते लगते हैं कि अब तो मैं मरने वाला हूं, अब मैं क्या करूं, अब मुझ से कुछ नहीं होगा। मेरा मानना है कि यह विचार देशहित में नहीं है। मैं तो युवाओं से अधिक युवा उस बुर्जुग को मानता हूं जो उम्र ढलने के बाद भी युवाओं से भी तेज गति और उत्साह से कार्य करते हैं।
आप दूरदृष्टि के धनी हैं, भविष्य में घटित होने वाली स्थिति का अनुमान आप हर समय लगाते है जो की कई बार सही होता है, आनेवाले समय का सही अनुमान आप कैसे लगा लेते हैं?
समाज जीवन जीने वाले और राष्ट्र के लिए समर्पित जिसका दृष्टिकोण बहुत ही व्यापक है वह सहजता से यह अनुमान लगा सकता है कि भविष्य में क्या होने वाला है, देश की क्या स्थिति आने वाली है। वीर सावरकर, डॉ.हेडगेवार, गुरूजी, गौतम बुद्ध आदि महापुरूषों द्वारा की गई भविष्यवाणियां शतप्रतिशत सही हुई हैं। जैसे वीर सावरकर ने कहा था कि जिस दिन हिंदू समाज संगठित हो जाएगा उसी दिन नेता अपने कपड़ों के उपर जनेऊ पहनने लगेंगे, यह बात सत्य भी हुई। जो कांग्रेसी नेता कभी मंदिर नहीं जाते थे, तिलक नहीं लगाते थे, वह भी चुनाव के समय माथे पर बड़ा तिलक लगाकर मंदिर-मंदिर घूमते फिरते हैं। कांग्रेस के एक बड़े नेता ने तो स्वयं को जनेऊधारी हिंदू कह कर अपने कप़ड़ों के ऊपर जनेऊ पहन कर दिखाया भी था।
गांधीजी की बात करें तो उनका पूरा जीवन समाज समर्पित था और देश के अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को जोड़ने का जो उनका प्रयास रहा वह उनकी सबसे बड़ी महानता है। एक स्वयंसेवक और इस राष्ट्र का एक घटक होने के नाते मेरा यह कर्तव्य है कि महात्मा गांधी के सकारात्मक प्रासंगिक विचारों को मैं सबके सामने लाऊं।
आनेवाले समय की सबसे जटिल समस्या कौन सी होगी?
मेरे हिसाब से जनसंख्या का विस्फोट बहुत बडी समस्या के रूप मे हमारे सामने होगा। आनेवाले प्रत्येक जीव के लिए रोटी, कपडा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात के साधन इत्यादि सभी निर्माण करना होगा। हमारा देश बहुत बड़ा है परंतु प्राकृतिक संसाधन सीमित हैं। सीमित संसाधनों पर मांग का असीमित दबाव पड रहा हैं। हम यह मांगे कैसे पूर्ण करेंगे?
पर्यावरण की भीषण समस्याये सामने आ रही हैं। यह केवल हिंदूओं तक सीमित नहीं हैं, वरन सम्पूर्ण मानव जाती को प्रभावित करनेवाली है। अतः हमारा दायित्व है की सर्वप्रथम हम हिंदू जीवन दृष्टी के अनुसार जीना शुरू करें। प्रकृती से उतना ही ले जितना आवश्यक हैं और जिसकी आपूर्ति प्राकृतिक रूप से ही की जा सकेगी। इस जीवन दृष्टी की दिक्षा सम्पूर्ण विश्व को देना और उसके लिए अपने आप को सबल बनाना यही हमारे सामने सबसे बडी चुनौती है।
उस जैकेट का कमाल!
दिल्ली के खादी भवन में रमेश पतंगे जी खादी से जुड़ी कुछ चीजें खरीदने गए थे। दिल्ली का खादी भवन तीन मंजिली होने कारण वहां अपनी रुचि की विभिन्न बातें उपलब्ध होती हैं। पंतगे जी खादी का जैकेट लेने के लिए उस काऊंटर पर गए। खादी के विविध प्रकार के जैकेट देखने के बाद दो जैकेट उन्होंने खरीदी किए। उस समय उनका ध्यान एक युवा की तरफ गया। वह युवा बहुत अस्वस्थ दिखाई दे रहा था। काऊंटर पर खड़े सेल्समैन से बार-बार निवेदन कर रहा था कि आप मुझे उस रंग का जैकेट देने की कृपा करें। पतंगे जी ने उस अस्वस्थ युवक को देखा और उस युवक के पास जाकर उसको उसकी अस्वस्थता का कारण पूछने लगे। जब रमेश पतंगे जी उस युवक को उसकी अस्वस्थता का कारण पूछ रहे थे तब वह युवक एकदम से शांत होकर रमेश पतंगे जी के पहने हुए जैकेट की ओर देख रहा था। उस युवक ने कहा- आज मेरे नाटक का पहला शो होने वाला है। कुछ समय के बाद वह शो शुरू होने वाला है और मुझे विशिष्ट प्रकार के जैकेट की अत्यंत आवश्यकता है। जो यहां पर मुझे उपलब्ध नहीं हो रहा है। पतंगे जी ने उसे पूछा- वह विशिष्ट जैकेट किस प्रकार का है? उसकी विशेषत: क्या है?
तब उसने पंतगे जी के पहने जैकेट की ओर देखा और कहा इसी प्रकार का जैकेट मुझे अपेक्षित है। तब पंतगे जी ने अपना जैकेट उतार कर उस युवक के हाथ में दिया और कहा- जल्दी जाकर आपकी भूमिका को साकार करो। जब उस युवा ने अपने जेब मे हाथ डाल कर जैकेट की कीमत देने की इच्छा जताई तब पंतगे जी ने कहा- अपनी भूमिका अच्छी तरह से निभाओ यही इस जैकेट की कीमत होगी। उस युवा ने रमेश जी का दूरभाष लेकर वहां से चला गया। दूसरे दिन पंतगे जी के दूरभाष पर उस युवक का फोन आया। अब मैं नया जैकेट नहीं खरीदूंगा। इस भूमिका को साकर करते वक्त आपके दिए हुए जैकेट का ही हरदम उपयोग करूंगा। क्योंकि, इस जैकेट को पहन कर जब मैं भूमिका साकार करने के लिए रंगमंच पर आ गया तब मुझ में एक ऊर्जा का वरदान निर्माण हुआ था।