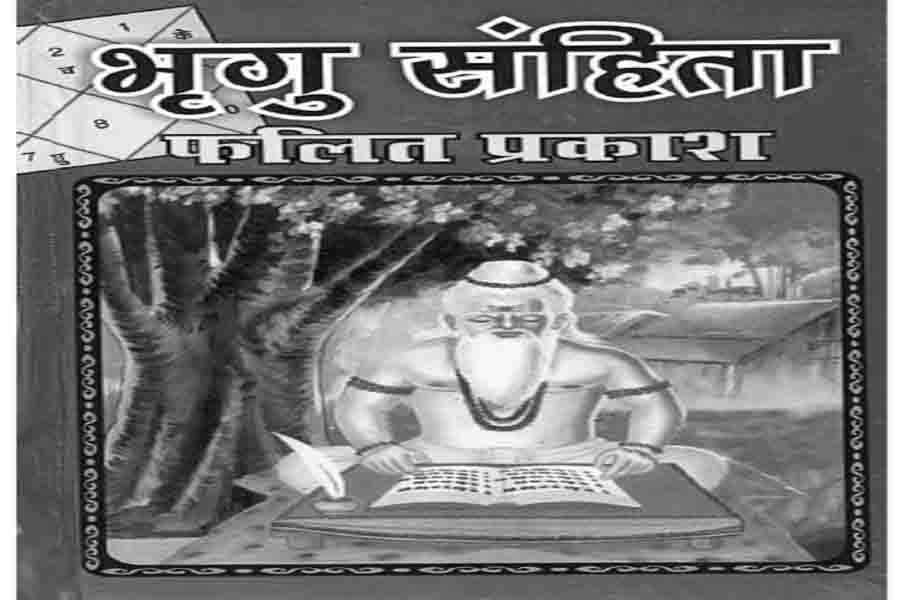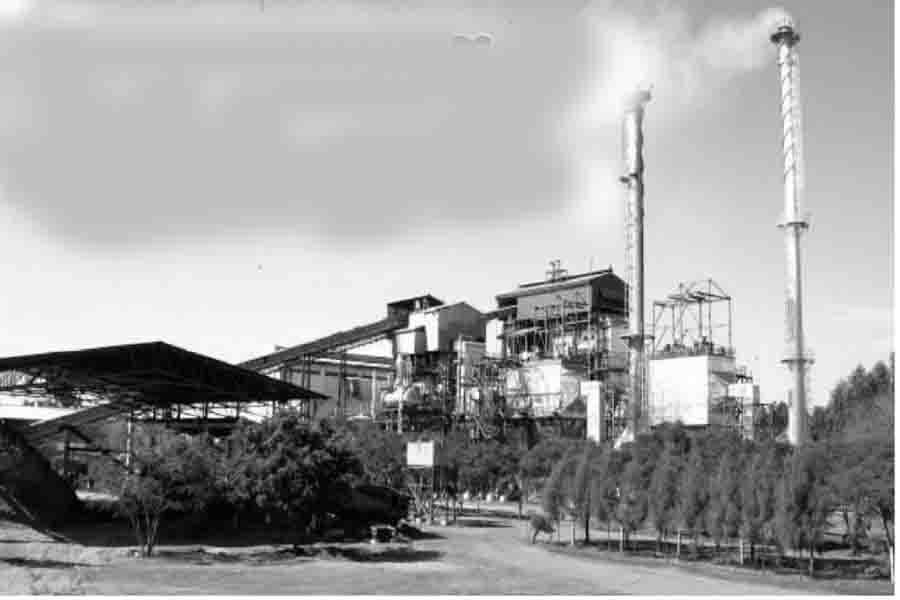ऊर्जा संरक्षण के विभिन्न उपायों के क्रम में वास्तुशास्त्र में बताए गए उपाय करने से न केवल ऊर्जा का संरक्षण करने में ही मदद मिलती है; अपितु हमारा जीवन भी अधिक स्वस्थ, सुखी और समृद्ध होता चला जाता है।
र्जा संरक्षण आधुनिक विश्व की महती आवश्यकता है; क्योंकि इसका सम्बंध न केवल पर्यावरण से है, बल्कि हम कह सकते हैं कि ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा का संरक्षण है। हजारों वर्ष पूर्व भारतीय ऋषि-मनीषियों के व्यापक अनुसंधान से सृजित वास्तुशास्त्र प्राचीनतम उपलब्ध विज्ञानों में से एक है तथा पूरे विश्व को भारत की एक अनुपम देन है जो जाति, धर्म और देश की सीमाओं से उठकर मानवमात्र का कल्याण करने को कटिबद्ध है। आधुनिक आर्किटेक्चरल विज्ञान किसी भी भवन को सुंदर और सुविधाजनक बनाने में तो सक्षम है, किन्तु उस भवन में निवास या व्यवसाय करने वाले लोगों के सुखपूर्वक जीवनयापन की गारंटी केवल भारतीय वास्तुशास्त्र ही देता है। यह गारंटी देने में वास्तुशास्त्र के सक्षम होने के कई कारणों में से एक कारण यह है कि वास्तुशास्त्र के मूल सिद्धांत प्रकृति के समानांतर अनुकूलन बनाकर चलने का निर्देश देते हैं तथा ऊर्जा संरक्षण भी उनमें से एक है।
भारतीय वास्तुशास्त्र की मिट्टी परीक्षण सम्बंधी अवधारणा का सम्बंध भी सीधे-सीधे ऊर्जा संरक्षण से ही है तथा इसकी वैज्ञानिकता के आगे आधुनिक विज्ञान भी नतमस्तक है। भृगु संहिता के अनुसार भूमि खरीदने से पूर्व भूखंड की मिट्टी की पांच प्रकार से अर्थात रूप, रंग, गंध, रस और स्पर्श से परीक्षा करनी चाहिए। ’विश्वकर्म प्रकाश’ में लिखा है कि ’पूर्व भूमि परीक्षयेत पश्चात् वास्तु प्रकल्पयेत’ यानि कि सर्वप्रथम भूमि परीक्षण करके फिर वंहा निर्माण कार्य करना चाहिए। इस ज्ञान के आधार पर हुए निर्माण कार्य सहस्राब्दियों बाद भी अपनी कहानी खुद बयां करने को आतुर आज भी गर्व से खड़े हैं। मोहनजोदड़ो, लोथल, द्वारिका इत्यादि इसके जीवंत उदाहरण हैं। दूसरी ओर वास्तुशास्त्र के आलोचक यह कहते नहीं थकते थे कि मिट्टी भी भला क्या सूंघने और चखने की वस्तु है? भला यह मिट्टी परीक्षण का कौनसा तरीका हुआ? आइये देखें कि इस सम्बंध में वास्तुशास्त्र के सिद्धांतों पर आधुनिक विज्ञान का दृष्टिकोण क्या है। वास्तुविज्ञान के अनुसार सफ़ेद, पीली या कामचलाऊ रूप में लाल रंग की मिट्टी जिसका स्वाद मीठा या मामूली नमकीन हो, वह भूमि खरीदने योग्य होती है। इन रंगों की मिट्टियों में कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और मेंग्नीज जैसे तत्वों की उपस्थिति के कारण इनमें प्राकृतिक रूप से ही कीट नियंत्रण की क्षमता होती है। इस प्रकार की मिट्टी की जल संग्रहण क्षमता यानि कि वाटर लॉगिंग कैपेसिटी कम होने के कारण नींव को मजबूती व सुरक्षा मिलने के साथ ही मौसमी उतार-चढ़ावों के दुष्प्रभाव और भूमि धंसने यानि कि डिफरेंशियल सेटलमेंट की आशंकाओं से भी बचाव हो जाता है। सफ़ेद और पीले रंग के कारण मिट्टी की तापरोधी क्षमता उच्च होती है जिसके फलस्वरूप सौर उर्जा के सीधे दुष्प्रभाव में कमी हो जाने से घर के आसपास का वातावरण भी सुखदायी रहता हैं रात्रि में तापमान कम हो जाने के बाद ऐसे स्थानों पर भवन और मानव शरीर का तुरंत तादात्म्य स्थापित हो जाता है तथा पंखे, कूलर और एसी इत्यादि साधनों पर तुलनात्मक रूप से कम ऊर्जा खर्च करने से काम चल जाता है। नीव का भार सहने की अतिरिक्त क्षमता के कारण ऐसी मिट्टी भूमि पर निर्माण कार्य भी तुलनात्मक रूप से सस्ता पड़ता है। इसके विपरीत काली और मटमैली मिट्टी इंजीनियर और भवन मालिक के लिए सरदर्द सरीखी होती है क्योंकि काली मिट्टी में मोंटमेरिलोनाईट नामक तत्व की बहुतायत होती है। मोंटमेरिलोनाईट के क्रिस्टल्स की फूलने की उच्च प्रवृति के कारण भूमि के धंसकने और नींव तथा दीवारों में दरारें आने की आशंका बढ़ जाती है। साथ ही काले रंग के कारण मिट्टी की तापरोधी क्षमता कम होने से दिन के समय यह अधिक ताप को ग्रहण और संग्रहित करती है तथा दिन ढलते ही इस ऊर्जा को वातावरण में छोड़ने लगती है जिससे पूरी रात घर का वातावरण स्वास्थ्य की दृष्टि से प्रतिकूल बना रहता है तथा रात्रि में पंखे, कूलर और एसी परिचालन पर तुलनात्मक रूप से अधिक ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है। सौर ऊर्जा के अत्यधिक अवशोषण के कारण क्षेत्र की चुम्बकीय रेखाओं अर्थात मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन्स में बिखराव से चारों तरफ कॉस्मिक डिसऑर्डर की स्थिति बन जाती है। यही कारण है कि भारतीय वास्तुशास्त्र काली, मटमैले इत्यादि रंगों की मिट्टियां जो स्वाद में खट्टी यानि कि एसिडिक हो उस भूमि को खरीदने का निषेध करता है।
वास्तुशास्त्र एक परिणाम आधारित (रिज़ल्ट ओरिएंटेड) विज्ञान है। वास्तुशास्त्र को नहीं मानने वाले लोग प्रायः वास्तु के बारे में कुछ भी नहीं जानते अन्यथा यह इतना विज्ञान सम्मत है कि कोई इसको माने बिना नहीं रह सकता। सुनीसुनाई भ्रांतियों या पूर्वग्रहों के आधार पर वास्तुशास्त्र को नकारने के बजाय यह जानने का प्रयास करना चाहिए कि आधुनिक विज्ञान वास्तुशास्त्र के सिद्धांतों पर अनुसंधान करके किस निष्कर्ष पर पहुँचा है। हजारों वर्षों से भारतीय वास्तुशास्त्र यह कहता आया है कि भवन के वास्तुनुरुप होने से ही जीव के साथ उसका तादात्म्य स्थापित हो पाता है जिससे उसको सुकून मिलता है परन्तु दुनिया ने इस बात को १९७० में जाकर तभी माना जब डॉ. अर्नेस्ट हर्टमन ने अनुसंधान करके पुष्टि की कि पृथ्वी की सतह से उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम की ओर ऊर्जा रेखाएं उभरती हैं जिन्हें उन्होंने बीईएम (बायो इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फील्ड) का नाम दिया और प्रमाणित किया कि किसी भी जीव के शरीर की कोशिका अपनी स्वयं की वायब्रेटरी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के कारण एक रेडियो रिसीवर की भांति कार्य करती है और वह बीईएम से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकती। वास्तुनुरुप निर्माण की स्थिति में भवन का बीईएम पूर्णरूप से संतुलित रहता है तथा निवास करने वाले की कोशिकाओं का बीईएम से सामंजस्य रहने के कारण वह सुकून और शांति का अनुभव करता है।
ऊर्जा संरक्षण की दृष्टि से वास्तुशास्त्र यह भी निर्देश देता है कि बहुमंजिला भवनों में या तो सभी मंजिलों की आंतरिक ऊंचाई सामान रहे अथवा ऊपर के मंजिलों की आतंरिक ऊंचाई को क्रमशः कम रखा जाए। जैसे-जैसे ऊंचाई बढती है, तापमान भी क्रमशः बढ़ता जाता है तथा सबसे ऊंची अंतिम मंजिल की छत तो सीधे ही गर्मी को उस मंजिल में प्रेषित करना शुरू कर देती है। आतंरिक ऊंचाई कम रखने से ऊपर की सभी मंजिलों में एसी ज्यादा प्रभावी तरीके से काम कर पाता है तथा ऊर्जा भी कम खर्च होती है।
वास्तु शास्त्र के अनुसार किसी परिसर में भवन बनाते समय सेट बेक छोड़ने में विशेष सावधानी अपेक्षित होती है। इसका सम्बंध ऊर्जा संरक्षण से भी है। आधुनिक विज्ञान ने भी इस बात की पुष्टि की है कि वास्तुनुरूप सेटबैक विज्ञान सम्मत है तथा ऊर्जा संरक्षण में भी सहायक है तथापि आधुनिक विज्ञान के पास इस बात का कोई जवाब नहीं है कि पूर्वी सेट बेक को यदि पश्चिमी सेट बेक से चौड़ा रखा जाता है तो उस घर में रहने वाले पुरुषों की प्रतिष्ठा और गौरव में वृद्धि क्यों होती है और किसी भी परिवार के अभावों से जूझने की स्थिति में दक्षिणी सेट बेक की चौड़ाई का क्या सम्बंध है; क्योंकि वास्तुशास्त्र के अनुसार अभावों के कई कारणों में से एक प्रमुख कारण दक्षिणी सेट बेक की चौड़ाई का उत्तरी सेट बेक की चौड़ाई से अधिक होना होता है। ऐसे घरों में स्त्रियों को भी स्वास्थ्य सम्बंधी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार भवन के उत्तरी दिशा के सेट बेक की चौड़ाई दक्षिणी सेट बेक से अधिक होनी चाहिए तथा पूर्वी सेट बेक की चौड़ाई भी पश्चिमी सेट बेक से अधिक होनी चाहिए। विदिशा भूखंडों में आग्नेय और वायव्य सेट बेक्स की चौड़ाई बराबर होनी चाहिए, परन्तु भवन के नैॠत्य की तरफ खुला भाग ईशान क्षेत्र की तुलना में कम होना चाहिए। दरअसल प्रातःकालीन सूर्य की धूप में अल्ट्रा वोइलेट किरणों की मात्रा अत्यधिक होती है। वास्तुशास्त्र के नियमानुसार जब पूर्व दिशा में अधिक और बड़े खिड़की दरवाजे रखे जाते हैं तथा कम ऊँची दीवारों, केवल छोटे पौधों और पानी के स्रोत का प्रावधान किया जाता है तो वास्तव में हम यह सुनिश्चित कर रहे होते हैं कि हमको स्वास्थ्यवर्धक, विटामिन डी से युक्त, बेक्टीरिया को मारने में सक्षम और त्वचा के केंसर का उपचार करने में सक्षम अल्ट्रा वायलेट युक्त सूर्य की रौशनी अधिकाधिक मात्रा में मिले। ऐसा करने से हमें भवन के अंदर जो पर्याप्त रौशनी मिलती है उसके कारण बिजली के बल्ब और ट्यूबलाइट्स को कम जलाना पड़ता है। शाम के समय जब अंधेरा होने लगता है तो वैसे भी बल्ब और ट्यूबलाइट्स को जलाना पड़ता ही है तथा वास्तुशास्त्र भी कहता है कि पश्चिम दिशा में कम चौड़ा सेटबैक, बड़े पेड़ तथा कम खिड़की दरवाजे होने चाहिए। आधुनिक विज्ञान भी इसकी पुष्टि करते हुए कहता है कि सूर्यास्त के समय सूर्य की किरणों में अल्ट्रा वायलेट न होकर इन्फ्रारेड्स किरनें होती हैं तथा उसके अधिक सेवन से केंसर तक हो सकता है।
भवन के किसी दिशा विशेष वाले भाग में और पारिवारिक पृष्ठभूमि व परिस्थिति विशेष के अनुरूप रंगों का चयन व उपयोग की विधि वास्तुशास्त्र के मूल सिद्धांतों में शामिल है। पूर्व और उत्तर दिशाओं का आधारभूत गुणधर्म उनका स्रोत दिशाएं होना है; क्योंकि पूर्वदिशा प्राणिक ऊर्जा और उत्तर दिशा जैविक उर्जा की स्रोतदिशाएं हैं, जबकि इसके विपरीत दक्षिण और पश्चिम दिशाएं क्रमश: जैविक और प्राणिक ऊर्जा की ’सिंक डायरेक्शंस’ हैं। यही कारण है कि पूर्व और उत्तर दिशाओं की दीवारों पर चटकीले और हलके (फ्लैशी) रंग उनकी दिशाओं की प्रकृति के अनुरूप और उन दिशाओं के गुणधर्मों को बढ़ावा देने वाले होते हैं और साथ ही इस कारण से ये दीवारें तापरोधी होकर कम ऊर्जा ग्रहण करती हैं जिससे पूरे दिन घर का तापमान सामान्य बना रहता है तथा दिन में बाहर का तापमान बढ़ जाने पर भी अंदर का तापमान धीरे-धीरे बढ़ता है जिससे तापमान नियंत्रित रखने के लिए तुलनात्मक रूप से कम उर्जा खर्च करने से काम चल जाता है। इसके विपरीत वास्तुशास्त्र पश्चिम और दक्षिण दिशाओं के लिए गहरे और मटमैले (डल एंड मेट फिनिश) रंग उपयुक्त मानता है। गहरे रंग दोपहर बाद सूरज ढलने के साथ ही अधिक ऊर्जा ग्रहण करने लगते हैं जिससे रात्रि में जब बाहर का तापमान कम होने लगता है तब भी भीतर का तापमान तुलनात्मक रूप से सामान्य बना रहता है। ऊर्जा संरक्षण के अलावा भी आधुनिक विज्ञान ने भी मन-मस्तिष्क पर पड़ने वाले रंगों के प्रभाव को स्वीकार कर लिया है और रंगों के माध्यम से चिकित्सा भी होने लगी है। देश-विदेश में कई मनोचिकित्सक रोगियों को चित्रकला के माध्यम से सहज बनाने का प्रयास कर रहे हैं। वैसे सहस्राब्दियों से वास्तुशास्त्र में ’रंग-चक्र’ के माध्यम से मानव मात्र के हित में रंगों के सुनियोजित प्रयोग का विधान रहा है तथापि प्राचीन काल से ही हमारे देश में रंग चिकित्सा का प्रचलन भी रहा है। प्राचीन मिश्र में भी स्वास्थ्य पर रंगों के प्रभाव का व्यापक अध्ययन किया गया था। प्राचीन चीन में भी रंगों से इलाज के संकेत मिलते हैं। माना जाता है कि प्रख्यात गणितज्ञ पैथोगोरस और वैज्ञानिक गैलेन रंग चिकित्सा में पारंगत थे। अपने समय के प्रसिद्ध अरबी चिकित्सक इब्रे-सीन भी उपचार प्रक्रिया में रंगों का उपयोग करते थे। दरअसल चाहे वास्तुशास्त्र हो, चिकित्सा विज्ञान हो, समाज शास्त्र हो या फिर अन्य कोई भी क्षेत्र, अपने विषय के विशेषज्ञ रंगों की प्रकृति और प्रभाव के ज्ञान के आधार पर रंगों का बहुत ही खूबसूरती और कलात्मक तरीके से उपयोग करते आए हैं। उनमें से कई रंग हमें उत्साह और उल्लास से भर देते हैं, वहीं कई रंग हमें निराशा और उदासी के आगोश में पहुँचा देते हैं। ऊर्जा संरक्षण के विभिन्न उपायों के क्रम में वास्तुशास्त्र में बताए गए उपाय करने से न केवल ऊर्जा का संरक्षण करने में ही मदद मिलती है; अपितु हमारा जीवन भी अधिक स्वस्थ, सुखी और समृद्ध होता चला जाता है।