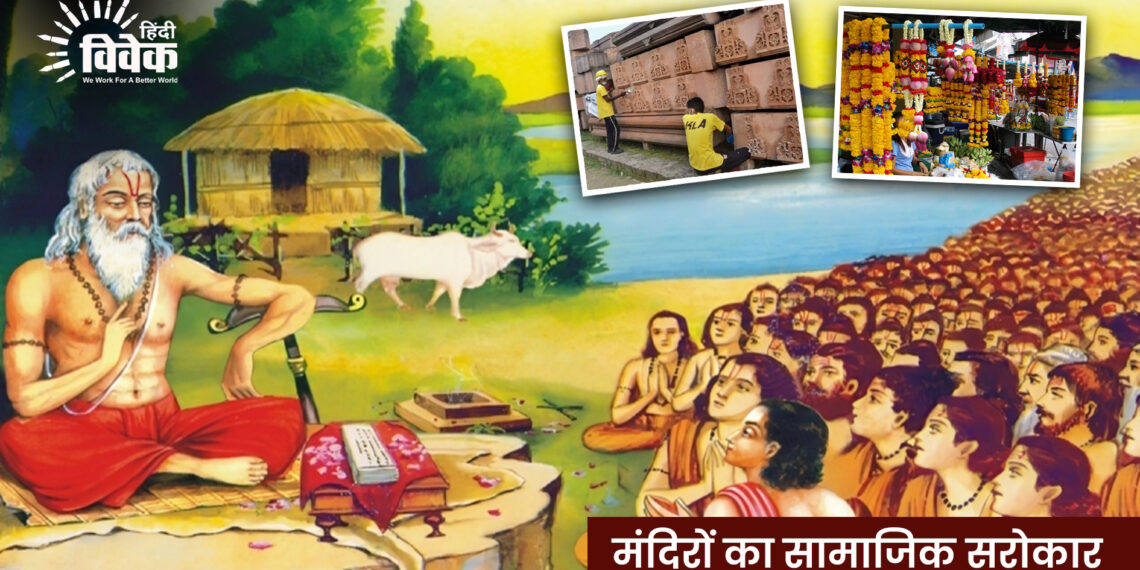“भारत में मंदिरों की संकल्पना समाज के केंद्र के रूप में रही है। शिक्षा तथा अन्य सामाजिक कार्यों के लिए लोग मंदिरों पर निर्भर रहते थे तथा उससे जुड़ाव महसूस करते थे। वर्तमान समाज को भी इससे सीखने की आवश्यकता है।”
हिंदू युगचक्र को चार भागों में विभाजित किया गया है। सतयुग, त्रेतायुग, द्वापरयुग और कलियुग। यदि प्रत्येक युग की समयावधि ढाई से 3 हज़ार वर्ष की मानी जाए तो हिंदू संस्कृति साढ़े सात से 10 हज़ार वर्ष पुरानी संस्कृति हो सकती है। यह बात अब प्रमाणों से सिद्ध हो चुकी है।
इस संस्कृति के प्रमुख ऋषि-मुनि ब्रह्मज्ञानी थे। ये ऋषि-मुनि शास्त्रज्ञों के समान अपने काल के वैज्ञानिक थे। जिन्होंने गुरु परम्परा के माध्यम से अपना ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सौंपा और वेदों की रचना की। इस सारे मंथन से यह तय हुआ कि समाज व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। यहीं से आश्रम व्यवस्था का निर्माण हुआ। ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम, संन्यासश्रम। इन चारों आश्रमों से व्यक्ति क्रमानुसार आगे बढ़ता है। यहीं से कर्म मार्ग का उदय हुआ। कर्म का मार्ग अर्थात उत्थान की दृष्टि से किए गए अच्छे कर्म या स्वयंके, कुटुंब और समाज कल्याण के लिए किए गए अच्छे कार्य हैं। इसी विचार से गुरुकुल शिक्षा प्रणाली प्रारंभ हुई। छात्रों की चयन प्रक्रिया उनके अच्छे गुण और व्यवहार को देखकर की जाती थी। इस तरह बने हुए राजा अपनी प्रजा के प्रति पितृवत प्रेम रखते थे। उनसे निर्माण हुए ऋषियों ने निराकार ईश्वर को यथाशीघ्र प्रसन्न करने के लिए उसे सगुण साकार रूप में लाया तथा वास्तुशास्त्र, दिशाशास्त्र, पंचमहाभूत इन सबको मिलाकर मंदिर संस्था को जन्म दिया।
ऋषि-मुनि दूरदर्शी थे। उन्होंने भविष्य में मनुष्य, प्राणी और पर्यावरण में होने वाले परिवर्तन ध्यान में रखकर, मनुष्य की सुख, संतुष्टि, आनंद और आध्यात्मिक प्रगति के लिए किस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए इसका सम्पूर्ण रूप से विचार किया और योग, साधना, वृक्ष, आयुर्वेद और सर्वोच्च स्थान पर मंदिर को महत्व दिया गया।
मंदिर की वास्तुकला में पंचमहाभूतों का विशेष संबंध है। मंदिरों का निर्माण प्राकृतिक स्थान पर किया जाता है। मंदिर के किनारे नदी, तालाब, समुद्र, जंगल आदि की आवश्यकता होती है। जलतत्व शांति का प्रतीक है। नदी, तालाब, झरना, कुआं आदि में जल तत्व होता है। सूर्य और जंगल में अदृश्य रूप में अग्नि तत्व होता है। वायुतत्व तथा आकाशतत्व सर्वव्यापी है। इनकी कोई सीमा नहीं है। इन पंचमहाभूतों के सहयोग से सृष्टि का निर्माण हुआ है।
इसके अलावा अक्षांश और देशांश के माध्यम से भूमिगत जल प्रवाह के गुरुत्वाकर्षण घनत्व का सटीक अनुमान लगाया जा सका अर्थात पांच महाभूतों का विचार करके ही मंदिरों की रचना की गई इसीलिए बड़े-बड़े मंदिर भूकंप, तूफ़ान और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं से हमेशा सुरक्षित रहे हैं। इसी वजह से हजारों साल पुराने मंदिर आज भी देखने को मिलते हैं।
इस बात का भी अध्ययन किया गया कि मनुष्य और प्राणी मात्राओं के बीच परस्पर पूरक जीवन कैसे होगा। पंचमहाभूत के साथ-साथ पंचांग (ज्योतिषशास्त्र) का भी प्रयोग किया गया। 1 पल (क्षण) = 24 सेकंड, 60 सेकंड या दो पल = 1 मिनट , 24 मिनट = एक घड़ी, 2 घड़ी = एक घंटा, तीन घंटा या 7 घड़ी का एक प्रहर, 8 प्रहर अथवा 24 घंटे एक दिन (पूरा रात दिन)। इस काल गणना के कारण प्रकृति में क्या परिवर्तन हो रहा है और इन परिवर्तनों के कारण कौन सा दैवीय तत्व काम करने वाला है, उदाहरण के लिए नक्षत्र से सम्बंधित वहां के अनुसार वर्षा होती है मृग नक्षत्र में भरपूर वर्षा होती है इसकी जानकारी ऋषियों को पहले से ही तपस्या के माध्यम से मिलने लगी।
उदाहरण के लिए नक्षत्र से सम्बंधित वाहन के अनुसार ही वर्षा होती है। मृग नक्षत्र में जोरदार वर्षा होती है। मार्गशीर्ष या अगहन वर्षा के नौ नक्षत्रों में से पहला नक्षत्र है। इस नक्षत्र में किसान जोर -शोर से बुवाई शुरू करता है। भारत के जून महीने में मृग नक्षत्र की शुरुआत होती है। कुंभ मेला भी सिहस्थ पंचांग के आधार पर आयोजित किया जाता है। उत्तर से दक्षिण तक सभी पर्वत श्रृंखलाओं के कारण भारत की भौगोलिक संरचना अद्वितीय है। हिमालय पर्वत से नीलगिरी पर्वत तक जलवायु, आकार और ऊंचाई में भिन्नता है इसीलिए भारत में पूरे वर्ष वातावरण उत्साही, ऊर्जावान और सुखद रहता है।
इसका एक सुंदर उदाहरण है। कोकण की राजापुर तहसील में हर 3 वर्ष बाद दत्त जयंती के समय गंगा प्रकट होती है। वर्षा ऋतु ना होते हुए भी गंगा का प्रकट होना प्रकृति का चमत्कार ही है। उस समय चलनेवाली सुखद सुहावनी हवा, वातावरण में प्रसन्नता, सकारात्मक ऊर्जा का उत्पन्न होना जैसे प्राकृतिक परिवर्तन तीव्रता से महसूस होते हैं। जिन स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन होता है, वहां भी एक जीवंत वातावरण बन जाता है। यहां के पानी में, हवा में, निर्माण होने वाली जीवनशक्ति का लाभ उठाने के लिए हजारों भाविक यहां स्नान के लिए आते हैं। अतः हमारे स्वभाव में रज और तम गुण कम हो जाते हैं और सत्व गुण बढ़ते हैं और सात्विकता भी बढ़ जाती है।
यहीं हमारी आध्यात्मिक प्रगति होती है। इस आध्यात्मिक अनुभूति को प्राप्त करने में मंदिर की संरचना मदद करती है और इसीलिए तीर्थ स्थान तथा मंदिर उन्हीं स्थानों पर बनाए जाते हैं, जहां सकारात्मक ऊर्जा सक्रिय होती है।
मंदिर की वास्तुकला इस तरह से बनाई गई थी कि उस स्थान पर शांति और दिव्यता उत्पन्न हुई। मंदिर का गर्भगृह ध्वनि सिद्धांत के अनुसार बनाया जाता है। इसके ऊपर गुंबद होता है। मंदिर के गुंबद के नीचे ईश्वर की मूर्ति की स्थापना की जाती है। मंदिर में मंत्रों के उच्चार तथा नामजप गुंबद के अंदर से दिव्य देवताओं के तत्वों को आकर्षित करते हैं। आध्यात्मिक विज्ञान के अनुसार जो भक्त मूर्ति की परिक्रमा करते हैं, उन्हें इसका लाभ मिलता है। इस मंत्र उच्चारण की ध्वनि मंदिर में उपस्थित व्यक्तियों को प्रभावित करती है। जब आप मूर्ति को स्पर्श करते हैं या नतमस्तक होते हैं, तब मंदिर की ऊर्जा आप में प्रवेश करती है और आत्म शक्ति की अनुभूति होती है। आपका मन और मस्तिष्क प्रसन्न होता है। मंत्रों के स्वर, घंटी, तथा शंख की आवाज से मन प्रसन्न होता है। मंदिर की पवित्रता भी व्यक्ति को प्रभावित करती है। इससे अंतर्मन को शुद्ध रखने की प्रेरणा मिलती है। इससे शरीर में उत्साह और नई चेतना का निर्माण होता है। इन सब बातों की लोगों को अनुभूति होने लगी और लोग धार्मिक स्थलों को भेंट देकर आध्यात्मिक निवास करने लगे। इससे लोगों को आध्यात्मिक वातावरण की अनुभूति होने लगी। यदि सामान्य परिस्थितियों में 10% सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती हो तो मंदिर की संरचना तथा इसके प्राकृतिक लाभों के कारण 70% सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होने लगी। साथ ही दैनिक आध्यात्मिक अभ्यास के महत्व के कारण मंदिरों को अद्वितीय महत्व प्राप्त हुआ।
हमारा देश अनेकता में एकता की संस्कृति से सजा हुआ है। हमारे देश में प्रत्येक त्यौहार का अद्वितीय महत्व है। हर तरह के त्यौहार एक के बाद एक मनाए जाते हैं। जिसमें रिश्तों को बनाए रखना, सकारात्मक ऊर्जा, भक्ति, आध्यात्मिक ऊर्जा का स्त्रोत, मन की शांति सकारात्मक दृष्टिकोण सब त्यौंहारों के माध्यम से निर्माण होता है। यह त्यौहार सृष्टि की घटनाओं के क्रम और ऋतुओं में परिवर्तन से जोड़े गए। भारतीय त्योहारों की शुरुआत चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि गुड़ीपाड़वा से होती है। इसे सृष्टि का निर्माण दिवस माना जाता है। इसके बाद गुढी पड़वा, रामनवमी, हनुमान जयंती, माघी गणपति, वट पूर्णिमा, रक्षा बंधन, श्रीकृष्ण जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी, नवरात्रि, दशहरा (विजयादशमी), दीवाली, मकर संक्रांति, महाशिवरात्रि, होली जैसे त्यौहार सालभर में आते हैं। इसी तरह हर चार वर्ष के बाद कुंभ मेला होता है। चारधाम, ज्योतिर्लिंग, 51 शक्ति पीठ जैसी यात्राएं सांस्कृतिक और आध्यात्मिक रूप से संतुष्टिदायक और परिपूर्ण होती हैं।
भारत में अनेक विविधतापूर्ण संस्कृति और धर्म है। यहां 33 कोटि देवी-देवताओं का निवास माना जाता है। देश के विभिन्न राज्यों में उन देवताओं के बड़े-बड़े मंदिर हैं। शैव, वैष्णव, गणपति, दुर्गादेवी, राम के दशावतार, कृष्णअवतार तथा विभिन्न देवी देवताओं को समर्पित विभिन्न शैलियों और वास्तुकला वाले हजारों मंदिर मिलते हैं। जिसमें प्रमुखता से अयोध्या का श्री राम मंदिर, श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा, महाराष्ट्र के अष्टविनायक गणपति मंदिर, आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी मंदिर, गुजरात का द्वारका मंदिर, उत्तराखंड में केदारनाथ- बद्रीनाथ मंदिर (चारधाम), उड़ीसा का जगन्नाथ पुरी मंदिर, वाराणसी का काशी विश्वनाथ मंदिर आदि का समावेश होता है। और इन सभी स्थानों पर भगवान प्रकट हुए ऐसी पुराणों में कथा है। कभी भक्तों के रक्षण के लिए, तो कभी अपने महान संतों की तपश्चर्या का फल देने के लिए। इसी लिए इन सभी धार्मिक स्थलों पर चैतन्य अबाधित रहा है।
इन सभी मंदिरों की रचना अर्थात धर्म, संस्कृति, आनंद, शांति आदि के लिए की गई उपाय योजना है। इन सभी मंदिरों में त्यौहार, उत्सव, व्रत वर्ष भर मनाए जाते हैं। साथ ही, मंदिर की वास्तु तथास्तु बोलती रहती है। अपनी मन की इच्छाएँ पूर्ण होने के कारण लाखों भक्त उत्सव के लिए मंदिरों में आते हैं।
इसीलिए हिंदू मंदिर भारतीय संस्कृति का अविभाज्य अंग है। भारतीय इतिहास और संस्कृति दोनों के विकास के साथ-साथ सनातन धर्म के अर्थशास्त्र में भी मंदिरों का बहुत बड़ा योगदान है। मंदिरों में होने वाले त्यौंहारों और उत्सवों के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर बनी है। कैसे? आइये देखते हैं।
मनुष्य की आवश्यकता, इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए होने वाली वस्तुओं का निर्माण, लेनदेन, वस्तुओं की बिक्री, इन सारी दैनंदिन क्रियायों से अर्थशास्त्र का निर्माण हुआ। मंदिर व्यवस्था के कारण भगवान की सारी पूजा विधि, वस्त्र, अलंकार, फूल – पत्ती, यज्ञ सामग्री, पंचमहाभूत देवी- देवताओं के अभिषेक करने के लिए लगने वाला दूध, दही, घी, शहद, चीनी यह सारा हवीर द्रव्य, मंदिर के सामने किए जाने वाले बड़े-बड़े यज्ञ, आहुति देने के लिए लगने वाली समिधा तथा अग्नि आदि वस्तुओं की वास्तुदेवता के लिए पूर्तता की जाने लगी।
ऋषि मुनियों का स्थान गुरु का था। उनके द्वारा रचित मंत्र उनके निरंतर प्रयोग और व्याकरण द्वारा सिद्ध किए गए थे। जैसे-जैसे शास्त्र परिपक्व हुए, मनुष्य को उच्च आनंद की प्राप्ति हुई और मनुष्य संतुष्ट हो गया। ईश्वर का नाम स्मरण, जप, मंत्रों का पाठ, सत्संग, मंदिर के कार्य में दिया गया सहयोग, निरपेक्ष भावना से किया गया कार्य, शरीर को कष्ट होकर भी मिलने वाला आनंद, त्याग अर्थात तन, मन, धन का त्याग कर सभी लोग साधना करने लगे और इस तरह गुरुकुल व्यवस्था से सुसंस्कृत राजाओं का निर्माण होता गया। इनके माध्यम से मंदिर, यज्ञ, कुंभ मेला, व्यवस्था और वित्त की देखभाल की जाने लगी। इस तरह अनजाने में ही मंदिर आधारित अर्थव्यवस्था को गति मिलती गई। मंदिर व्यवस्था का उदय ग्राम व्यवस्था और गुरुकुल व्यवस्था द्वारा हुआ।
मंदिर दान के प्रतीक बन गए। दान देने से बढ़ोतरी होती है, यह महसूस करने के बाद ज्यादा से ज्यादा लोग दान करने लगे। आम जनता से लेकर राजा तक यदि किसी को धन की आवश्यकता होती, तो मंदिर के व्यवस्थापक बिना ब्याज के धन उपलब्ध करा देते थे। मंदिरों द्वारा धर्मशालाएं, भंडारा और लंगर चलाए जाते थे। ज्ञान का कार्य भी किया जाता था। इन सबका आर्थिक बोझ मंदिर प्रबंधन उठाता था। किसी को नौकरी की आवश्यकता नहीं थी, सभी लोग स्वतंत्र आचार-विचार से जीवन व्यतीत करते थे। यह सब बहुत ही ईमानदारी से चलता था। क्योंकि दैवीय अनुष्ठान ही सम्पूर्ण व्यवस्था का मूल था।
जनता में कोई भी भूखा प्यासा नहीं था। दु:खी नहीं था। भिखारी नहीं था। सभी लोग खुश, सुखी और संतुष्ट थे। गीत, संगीत, नृत्य देवताओं के लिए प्रस्तुत होने लगे। सर्वप्रथम ईश्वर को वस्त्र और आभूषण अर्पित कर फिर स्वयं उपयोग करने की प्रथा बन गई। स्त्री देवता, पुरुष देवता, स्थान देवता, ग्राम देवता तथा कुल देवता, सभी को श्रद्धा पूर्वक अर्पित करने की भावनात्मक प्रथा के कारण, आगे चलकर मंदिर की अर्थव्यवस्था का विस्तार हुआ। त्योहार, परम्परा, विशेष मुहूर्त, विवाह आदि विशेष अवसरों के लिए अलग-अलग हिस्सों में बढ़ती जरूरतों और उसके अनुरूप वस्तुओं के निर्माण के साथ व्यापार शुरू हुआ। इस प्रकार सम्पूर्ण भारत में स्वर्ण युग का उदय हुआ।
भारतीयों की तुलना में ईसाइयों और मुसलमानों में त्यौहारों की संख्या बहुत कम है। भारतीय संस्कृति में सम्पूर्ण वर्ष त्यौहार और उत्सव मनाए जाते हैं। ईसाइयों में क्रिसमस और मुसलमानों में ईद, मुहर्रम और रमजान त्यौहार मनाए जाते हैं। इसलिए उनमें भारतीयों की तुलना में वस्तुओं का निर्माण बहुत ही कम मात्रा में होता है।
पूर्व समय में भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक महिमा के बारे में सुनकर विदेशी शासक आश्चर्यचकित रह जाते थे। भारत सोने की चिड़िया है। वहां से सोने का धुंआ निकलता है और हमारे यहां हम संपत्ति का निर्माण नहीं कर सकते, इस बात की उन्हें बहुत ईर्ष्या थी। इसी इर्ष्या के कारण भारत पर लगातार आक्रमण होते थे। शक, हूंण, सिकंदर, अरब, अलाउद्दीन खिलजी, मुस्लिम आक्रांता भारत पर लगातार आक्रमण कर यहां की संपत्ति लूट कर ले जाते थे। खास बात यह थी कि, भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक परम्परा का चक्र लगातार चलता रहता था। इसलिए आक्रमण के बाद 3 से 4 वर्ष में अर्थव्यवस्था पुन: पूर्व रूप में आ जाती थी और यही अर्थव्यवस्था बाद में फिर से चरम पर पहुंच जाती थी।
परिणामस्वरुप यदि विदेश की अर्थव्यवस्था 2 प्रतिशत बढ़ती थी तो भारतीय अर्थव्यवस्था 10% की चरम सीमा पर पहुंच जाती थी। इसके कारण मंदिर के आसपास के गांव परिपूर्ण होते गए। देश के आंतरिक हमले कम होते गए। हर कोई ईश्वर से डरता था। समाज पाप से डरता था। सभी लोग सुखी और समृद्ध जीवन जी रहे थे। जिन लोगों में विशेष गुण होते थे, उन्हें राजा के दरबार में काम मिलता था। कृषि भी फलती फूलती गई।
देश को आजादी मिलने के बाद हम मंदिर के माध्यम से उच्च स्तर पर त्योहार और उत्सव मनाते गए। आज भी भारतीय शहर और उन शहरों के मंदिर आर्थिक दृष्टि से सक्षम है। बहुत बड़ी मात्रा में रोजगार उपलब्ध हुए हैं। गाय से मिलने वाला पंचगव्य अर्थात दूध, दही, घी, गोमूत्र तथा गोबर आदि धार्मिक साहित्य की मांग बढ़ गई है। मंदिर निर्माण के लिए लगने वाली आवश्यक सामग्री, पर्यटन व्यवस्था में बढ़ा यातायात, मंदिर में पुजारी जैसी चीजों की मांग दिन-दिन बढ़ती जा रही है। मांग के अनुरूप आपूर्ति के सिद्धांत पर मंदिर व्यवस्था अधिक समृद्ध हो रही है। आज धार्मिक पर्यटकों की संख्या बहुत अधिक है। इसलिए इन सभी कारकों के कारण मंदिरों से हर साल करोड़ों का राजस्व प्राप्त होता है। इस पृष्ठभूमि में भारत की जीडीपी आसानी से 8 से 9 प्रतिशत तक बढ़ सकती है। अगर अर्थशास्त्री इसका गहराई से अध्ययन करें, तो कई महत्वपूर्ण बातें सामने आ सकती हैं।
अस्वस्थता, नैराश्य, भय, क्रोध, और असंतोष से आज पूरा विश्व ग्रसित है। मंदिर से भक्ति के साथ ही शांति और समृद्धि मिलती है। इसलिए बाकी लोगों के साथ ही विदेशों से भी लोग यहां शांति के लिए एवम संस्कृति का अभ्यास करने के लिए आते हुए दिखाई पड़ते हैं। इसी कारण सभी की निगाहें भारत की ओर लगी हुई हैं। भविष्य में यह दायरा आम आदमी की कल्पना से कई गुना ज्यादा होने वाला है। यदि दुनिया को पर्यावरणपूरक आर्थिक रूप से टिकाऊ समाधान देना है, तो मंदिर संस्कृति आधारित संरचना को पूरी दुनिया के सामने रखने की शुरुआत करनी चाहिए।
वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ है पूरा विश्व एक कुटुंब है। यह पूरी दुनिया को भारत द्वारा दिया गया उपहार है। इस प्रकार, एक मंदिर की संरचना सम्पूर्ण धरती की खुशहाली के लिए एक टिकाऊ संरचना हो सकती है।
भारत की मंदिर संस्कृति आज स्वयंपूर्ण, आत्मनिर्भर, स्वावलंबी, किसी को भी गुलाम न बनाने वाली और सभी को प्रेरणा देने वाली है। मंदिर व्यवस्था से देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है। मंदिर हमारी अर्थव्यवस्था की नीव है और यह हमारी सनातन हिंदू संस्कृति और समस्त भारत वासियों के लिए गौरव की बात है।
-रविंद्र प्रभुदेसाई