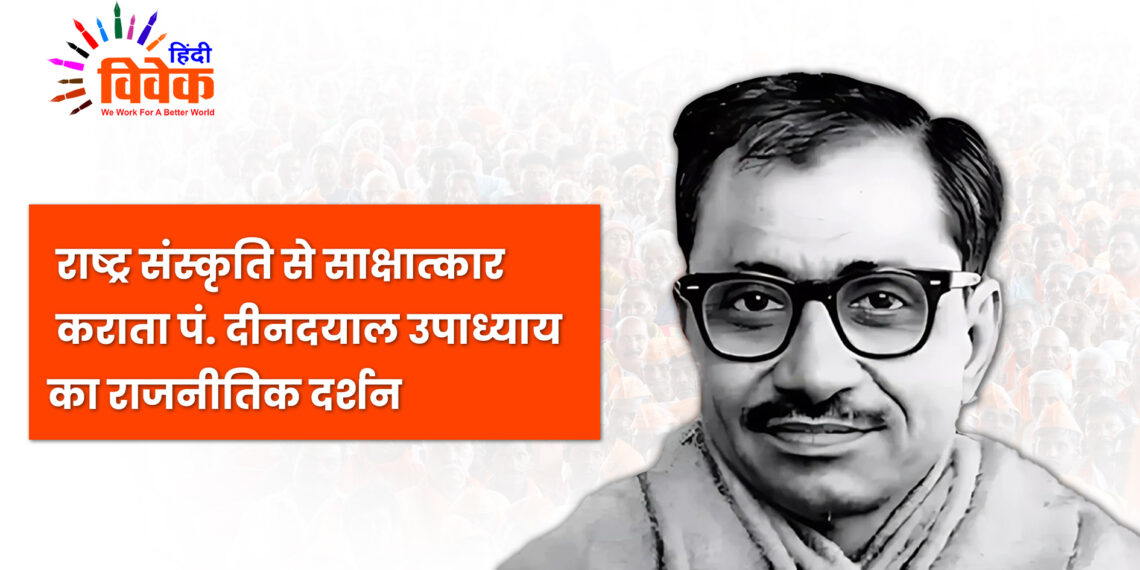भारतीय राजनीति के वृहदाकाश में दैदीप्यमान पं. दीनदयाल उपाध्याय अपने राष्ट्रीय विचारों और प्रखर चिंतक, विचारक के तौर पर प्रतिष्ठित हैं। सनातन हिन्दू संस्कृति के मुखर पक्षधर और तदानुरुप रीति-नीति के आधुनिक राजनीतिक प्रवर्तकों की अग्रगण्य पंक्ति में उनकी गिनती होती है। पंडित जी ने केवल विचार ही नहीं दिए..अपितु राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और जनसंघ के माध्यम से विचारों को धरातलीय रूप भी दिया। एकात्म मानव दर्शन और अन्त्योदय जैसे मूल्य जनसंघ से होते हुए वर्तमान भाजपा की नीतियों में स्पष्ट परिलक्षित होते हैं। पण्डित जी विचारकों में प्रतिष्ठित व सुशोभित होने के साथ-साथ ही चिन्तन और दर्शन के बहुआयामी लोकल्याणकारक मान-बिन्दुओं के द्वारा नूतन प्रस्थापनाएँ करते हैं। साथ ही वैचारिक और कार्य स्तर पर कई सारी भ्रामक, अहितकारी रूढ़ियों को तोड़ते हुए भारतीयता के अनुरूप मार्ग प्रशस्त करते हैं। उनके विचार एवं दर्शन के विविध रुप हैं जिनमें उनका राजनीतिक दर्शन भी अपने आप में अनूठा है। उनके राजनीतिक दर्शन के मूल में भी राष्ट्र, संस्कृति, धर्म, उच्च आदर्श और समाज है। वे स्पष्ट उद्घोषणा करते हैं कि राजनीति राष्ट्र के लिए ही होनी चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार की संकीर्णता या स्वार्थ प्रेरित हित लाभ के दृष्टिकोण अराष्ट्रीय प्रवृत्ति एवं भारत की राष्ट्रीयता के लिए एक प्रकार का खतरा ही हैं। वे राजनीतिक शुचिता व राजनीति, दल, विचारधारा के मूल में राष्ट्रोन्नति और जनकल्याण को ही रखते हैं। येनकेन प्रकारेण सत्ता प्राप्ति , अवसरवादिता और मूल्यों से पृथक राजनीति को तिलांजलि देते हैं।
पं. दीनदयाल उपाध्याय एक श्रेष्ठ चिंतक-विचारक होने के साथ सजग थे। उन्होंने भारत ही नहीं बल्कि विश्व परिदृश्य में गहरा हस्तक्षेप करने वाली विचारधाराओं का गहन अध्ययन किया था। भारतीय दृष्टि के आधार पर उनका विश्लेषण और मीमांसा की थी। वे भारतीय राजनीति और वैश्विक राजनीति में अपना प्रभाव रखने वाली विचारधाराओं की तात्विक समीक्षा करते हुए उनका नीर-क्षीर विवेचन करते हैं। साथ ही स्वातन्त्र्योत्तर काल के उपरान्त पश्चिमी प्रभाव से ग्रस्त राजनीतिज्ञों की स्वदेशी की ओर न देखकर पश्चिम के अन्धानुकरण की प्रवृत्ति का विरोध करते हैं। पश्चिमी अन्धानुकरण की प्रवृत्तियों को पंडित जी भारत और भारतीयता के लिए आत्मध्वन्सात्मक बतलाते हैं। उनके मतानुसार आधुनिक पाश्चात्य देशों का उदय केवल पाँच सौ से सात सौ वर्षों की अवधि के पूर्व ही हुआ है, किन्तु भारत हजारों वर्षों से आसेतु हिमालय की भाँति एक उत्कृष्ट राष्ट्र के रूप में अवस्थित है। अतएव वे पाश्चात्य देशों की कसौटी और उनके निष्कर्षों पर भारत के आँकलन और अनुकरण करने को न्यायसंगत नहीं मानते हैं। दीनदयाल जी का मानना था कि जो हमारा है उसे समयानुकूल बनाया जाए तथा जो विदेशी है, उसे राष्ट्रानुकूल बनाया जाए। वे भारतीय समाज में केवल विदेशी होने के कारण श्रेष्ठताबोध और भारतीय होने के कारण उसे उपेक्षित और नकारने की दुष्प्रवृत्ति का विरोध करते हैं। चूँकि राजनीतिक अन्धानुकरण के चलते स्वातंत्र्योत्तर भारत में पराजयबोध, हीनभावना की व्याप्ति अकादमिक स्तर पर क्रमशः स्थापित की गई। इसलिए वे इस पर तीक्ष्ण प्रहार करते हुए कहते हैं स्वत्व एवं स्वाभिमान का मेरुदण्ड सीधा तना न हो तो विश्व में भौतिक दृष्टि से बलशाली, प्रभावशाली,विजयशाली तथा वैभवशाली माने जाने वाले राष्ट्रों का अनुसरण करने की प्रवृत्ति बल पकड़ती है। अपने पिछड़े और दरिद्र समाज से लज्जा आने लगती है। यह अनुसरण बड़ी बातों से लेकर छोटी-छोटी दैनिक बातों तक छनता चला आता है।
पंडित दीनदयाल उपाध्याय का विभिन्न विचारधाराओं और पश्चिमी व्यवस्थाओं को लेकर उनका गहन अध्ययन रहा है। वे व्यापक शोध एवं विश्लेषण के उपरान्त निष्कर्षत: यह कहते हैं कि -पश्चिम की नकल मॉडर्न होने का प्रमाण बन गया है। यह चहुँमुखी अनुकरण ठीक नहीं, क्योंकि पश्चिमी चिन्तन और व्यवस्था मानव कल्याण में असफल रही है। आगे वे मैकॉले शिक्षा प्रणाली और उसके दुष्प्रभाव पर कहते हैं किसी ने स्वदेशी पर जोर दिया तो उसे असभ्य बता दिया जाता है। हम ब्रिटिशों से हार गए। चालाक मिशनरियों तथा शासकों ने मैकॉले शिक्षा प्रणाली के माध्यम से हमारे मन में अनेक बीज बो दिए। तब से हमारे शिक्षितों में और उनकी देखादेखी समाज के अन्य लोगों में भी पाश्चात्यों के अनुकरण की प्रवृत्ति बढ़ती गई है। स्वतन्त्रता के बाद तो वह निरंकुश हो गई है।
वे मार्क्स के दर्शन के पूर्णतः ङ्गभौतिकवादीफ होने के सिद्धांत को अनुपयुक्त मानते हैं जिसके उदाहरण के तौर पर वो रूस, चीन के क्रूर प्रकरणों का विश्लेषण करते हैं। वहीं पंडित जी समाजवाद और लोकतान्त्रिक समाजवाद के द्वारा मनुष्य की स्वतन्त्रता की समाप्ति और समाजवाद के द्वारा मानवीय जीवन में राज्य के वर्चस्व को भी अस्वीकार करते हैं। वे कहते हैं कि लोकतान्त्रिक समाजवाद जैसी कोई चीज नहीं है, शब्द भर है। क्योंकि समाजवाद लाने में लोकतन्त्र की हत्या करनी पड़ती है। साथ ही उन्होंने पूँजीवादी व्यवस्था को भी मानव कल्याण के लिए असफल माना है। इन सबका हल सुझाते हुए वे कहते हैं विश्व की समस्याओं का हल समाजवाद पूँजीवादी लोकतन्त्र नहीं, वरन् हिन्दूवाद है। यही एक ऐसा जीवनदर्शन है जो जीवन का विचार करते समय उसे टुकड़ों में नहीं बाँटता, अपितु सम्पूर्ण जीवन को इकाई मानकर उसका विचार करता है।
वे इसे हिन्दुत्व और मानवता के तौर पर स्वीकार किए जाने की बात करते हुए स्पष्ट कहते हैं कि यही भारत की आत्मा के अनुरूप व जनमानस में उत्साह को सञ्चारित करेगा। साथ ही विभ्रान्ति के चौराहे में खड़े विश्व के लिए मार्गदर्शक के रूप में भी काम करेगा। पंडित जी राष्ट्र को जीवमान इकाई मानते हुए कहते हैं कि एक भूमि विशेष में रहने वाले लोगों का, जिनके हृदय में मातृभूमि के प्रति असंदिग्ध श्रद्धा का भाव हो, जिनके जीवनादर्शों में साम्य हो, जीवन के प्रति स्पष्ट दृष्टि हो, शत्रु-मित्र समान हों। ऐतिहासिक महापुरुष एक हों; इन सबसे राष्ट्र का निर्माण होता है। इसके विपरीत आक्रान्ता से इसलिए सहानुभूति रखना कि वे हम-मजहब हैं, अराष्ट्रीय प्रवृत्ति है। इसी तरह वैश्विक राजनीति और भारतीय परिदृश्य में राष्ट्रवाद सर्वदा चर्चित रहता है, भारत की वामपंथी विचारसरणी, सिद्धांत विहीन दल- भारतीय राष्ट्रवाद – राष्ट्रीय विचारों को प्रायः हिटलर, मुसोलिनी से जोड़कर लाँछित करने लगते हैं। जबकि यह सर्वज्ञात तथ्य है कि भारत की राष्ट्रीय एकीकरण की भावना के कारण ही स्वातन्त्र्य यज्ञ सफल हुआ था, अन्यथा स्वतन्त्रता असंभव सी थी। जोकि समस्त क्षेत्रों की चैतन्यता के फलस्वरूप मिली।
पण्डित जी राष्ट्रवाद के सन्दर्भ में विस्तृत व्याख्या करते हुए कहते हैं -यूरोपीय राष्ट्रवाद और भारतीय राष्ट्रवाद में अन्तर है। यूरोपीय चिन्तन पारस्परिक संघर्ष की अवधारणा पर आधारित है। जबकि भारतीय राष्ट्रीयता का जन्म संघर्ष में नहीं हुआ है,अपितु सभ्यता के आरम्भ से ही भारत सांस्कृतिक राष्ट्र रहा है जिसमें कई राजनैतिक सत्ताएँ थी किन्तु राष्ट्र एक था। भारत का राष्ट्रीय विचार न तो विस्तारवादी है, न ही साम्राज्यवादी और आक्रमणशील बल्कि भारतीय विचार वसुधैव कुटुम्बकम् पर आधारित है जो प्राणिमात्र के प्रति कल्याण का भाव रखता है। भारतीय विचार की तुलना पर वे कहते हैं पश्चिम के राष्ट्रवाद से भारत के विचार की तुलना करना ही गलत है। पश्चिम ने द्वैत के आधार पर संघर्ष का नगाड़ा बजाया और भारत ने अद्वैत के आधार पर एकात्म की बाँसुरी बजायी। दोनों वाद्य होते हुए भी दोनों की स्वरलहरियों में भारी अन्तर है। इस भेद को समझकर हमें राष्ट्रवाद का विचार करना चाहिए। स्पष्ट है जब पंडित दीनदयाल उपाध्याय भारतीय राष्ट्रवाद शब्द का प्रयोग करते हैं तो यहां वे राष्ट्रीयता को ही संबोधित करते हैं। आगे पंडित जी वे भूमि, जन, संस्कृति के संघात से राष्ट्र के निर्माण की बात कहते हैं। उनकी दृष्टि में भारतीय संस्कृति का अभिप्राय ही हिन्दू संस्कृति है। साथ ही उनके मतानुसार भारतीय राष्ट्रवाद का आधार यह संस्कृति है।
भारत की एकात्मता तभी सम्भव है, जब संस्कृति के प्रति निष्ठा रहे। वे हिन्दू संस्कृति, शक्ति और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के सम्बन्ध में यथार्थबोध प्रस्तुत करते हैं – भारतीय राष्ट्रवाद सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है, क्योंकि भारतवर्ष को राजनीति और हमलावरों ने कई बार विखण्डित किया, किन्तु संस्कृति ने उसे कश्मीर से कन्याकुमारी तक अखण्ड रखा। जहाँ हिन्दू संस्कृति और हिन्दू धर्म कमजोर हुआ वह हिस्सा भी देश से कट गया। इन्हीं सब कारणों के चलते भारत और भारतीयता की मूल पहचान के रूप में हिन्दू संस्कृति को केन्द्र व मानबिन्दु के रूप में रखते हैं। साथ ही वे भारत में व्याप्त विविधताओं में पृथकता के स्थान पर एकत्व को प्रतिष्ठित करते हुए भाषा,प्रान्त, वेशभूषा,खान-पान,रहन-सहन उपासना पद्धति के आधार पर किसी भी प्रकार के विभाजन की विकृति को अस्वीकार करते हैं। सभी के मध्य सांस्कृतिक एकता के सूत्र में पिरोई हुई माला के रुप में राष्ट्रीय चेतना और भारतमाता की भव्य झाँकी को देखते हैं।वे विवेकानन्द की परम्परा का पथानुसरण करते हुए कहते हैं – हमारा धर्म (नॉट रिलिजन) हमारे राष्ट्र की आत्मा है। बिना धर्म के राष्ट्र जीवन का कोई अर्थ नहीं रहता है। भारत धर्म प्राण देश है, और राष्ट्र का जातीय उद्देश्य धर्म है, क्योंकि भारत में धर्म पर अभी आघात नहीं हुआ। अतः यह जाति जीवित है। वे अल्पसंख्यक अवधारणा को प्रच्छन्न द्विराष्ट्रवाद या बहुराष्ट्रवाद मानते हैं।
इसी प्रकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय अल्पसंख्यक और मुस्लिम हठधर्मिता को लेकर एकदम सुस्पष्ट हैं। उनका मत था कि- मुसलमानों या ईसाइयों का प्रश्न कहलाने वाली समस्या वस्तुतः धार्मिक है ही नहीं। यदि धार्मिक होती तो नानक, कबीर, गांधी आदि के सर्वधर्म समभाव के प्रयत्नों से सुलझ गई होती, किन्तु सैकड़ों सालों के प्रयास के बाद भी सुलझी नहीं क्योंकि समस्या राजनीतिक है। मुस्लिम बहुसंख्या सदैव अन्य मतावलम्बियों के प्रति असहिष्णु होती है और उनकी अल्पसंख्या सदा उपद्रवकारी। स्वयं को इस्लामी घोषित करने वाले किसी भी देश में यह अनुभव किया जा सकता है। जहां वे लोग परिणामकारक अल्पसंख्या में होते हैं वहाँ वे उपद्रव खड़ा करते हैं क्यों ? इसलिए कि उनके मन में अपने समाज का राजनीतिक वर्चस्व प्रस्थापित करने की आकांक्षा होती है। मुसलमानों का यह सामूहिक स्वभाव बन गया है। धर्म और राजनीति में वे कोई अन्तर नहीं मानते। धर्म के आवरण में अपनी राजनीतिक आकांक्षाओं की पूर्ति करा लेने का मुसलमानों और ईसाइयों द्वारा अखण्ड प्रयास किए जाने के कारण उत्पन्न समस्या ही हिन्दुस्तान के अल्पसंख्यकों की समस्या का वास्तविक रूप है।
आगे वे भारतीय मुसलमानों के परावलम्बन, राजनीतिक हठधर्मिता, राष्ट्र-संस्कृति के प्रति अलगाव के कारण भारत में व्याप्त मुस्लिम समस्या का समाधान सुझाते हैं। वे
मुस्लिमों के राजनीतिक पराभव और उनके समावेशन का मार्ग बतलाते हैं। वे कहते हैं -मुसलमानों की हठधर्मिता का पराभव करने का श्रेष्ठ उपाय है कि उनका राजनीतिक पराभव किया जाए। जब तक उनकी यहाँ राजनीतिक पराजय नहीं होती उनकी समस्या उलझती ही रहेगी, किन्तु उनकी राजनीतिक हार हो जाए तो वे निश्चय ही अपनी पूर्व स्थिति पर विचार करेंगे और जिस समय वे इस प्रकार विचार करने की मानसिकता में आएँगे तभी दोनों (हिन्दू और मुसलमान) समाजों में सच्चा सांस्कृतिक सहयोग प्रारम्भ होगा। पराजय आत्मनिरीक्षण करवाती है हिन्दुओं की तो परम्परा ही ऐसी रही है कि किसी पंथ को नष्ट करने की झंझट में न पड़ते हुए उसे अपने में समा लेना। हमारी नीति राष्ट्रीय स्तर पर आक्रामक, धर्म के स्तर पर सहिष्णु तथा सामाजिक धरातल पर समावेशक रहनी चाहिए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का स्पष्ट मानना था कि मुस्लिम और ईसाई बाहर से आए हुए लोग नहीं हैं।
उनके पूर्वज हिन्दू ही थे। धर्म बदल जाने से राष्ट्रीयता नहीं बदलती, संस्कृति नहीं बदलती। इसीलिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय कहते हैं कि मुसलमान व ईसाई चाहे जैसे अपने धर्म को मानें, रोजे रखें, चर्च जाएँ किन्तु इस देश की संस्कृति को अपनी संस्कृति मानें। मक्का-मदीना या वेटीकन सिटी से ज्यादा काशी और अयोध्या से लगाव रखें क्योंकि संस्कृति का सम्बन्ध राष्ट्र के अस्तित्व के साथ होता है। भारतीय संस्कृति के मूल्यों, आदर्शों, राष्ट्र पुरुषों, परम्पराओं तथा श्रद्धा केन्द्रों के प्रति विरोध एवं विध्वंस की भावना तथा राजनीतिक प्रभुता की आकांक्षा संघर्ष का कारण बनेगी। पन्थनिरपेक्षता के सम्बन्ध में भी दीनदयाल जी स्पष्ट हैं। वे इस पाश्चात्य अवधारणा के सम्बन्ध में कहते हैं सेक्युलरिज्म भारतीय धरती पर बलात् रोपा गया विदेशी पौधा है। इसके सही स्वरूप को न समझ पाने के कारण ही भारतीय राजनीतिज्ञों ने इसका अर्थ ही बदल डाला। भारत में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ सर्वधर्म समभाव के स्थान पर हिन्दू धर्म, सभ्यता, संस्कृति से जुड़ी हर बात का विरोध तथा मुसलमानों व ईसाइयों की हर उचित-अनुचित माँग का चाहे वह राष्ट्र विघातक व संविधान विरोधी क्यों न हो।
इसका समर्थन करना तुष्टिकरण ही रह गया है।
लोकतन्त्र में उनकी दृढ़ आस्था थी वे व्यक्ति से अधिक दल को, दल से अधिक सिद्धांत को, सिद्धांत से ज्यादा लोकतन्त्र को और लोकतन्त्र और राष्ट्र में विरोध होने पर राष्ट्र को महत्व देते हैं। वे राष्ट्र को केवल भूमि का टुकड़ा नहीं मानते हैं। अपितु वे जीवंत मानते हैं। राजनीति के लिए उनका ध्येय वाक्य था -फराजनीति राष्ट्र के लिएफ .. इसे और सुपरिभाषित करते हुए पंडित दीनदयाल उपाध्याय कहते हैं कि-कोई भी संगठन या दल तभी ठीक प्रकार से काम कर पाता है, जबकि उसकी प्रेरणा राष्ट्र हो। राजनीति को लेकर उनकी दृष्टि एकदम सुस्पष्ट थी। वे राष्ट्र के ऊपर किसी मवादफ को मानने वाले दलों को आड़े हाथों लेते हुए कहते हैं जो लोग राष्ट्रीयता का मखौल उड़ाकर, राष्ट्र के विचारों को तिलांजलि देकर विभिन्न प्रकार के वादों में उलझते हैं वे भूल करते हैं। उनके हाथ से कोई अच्छा कार्य नहीं हो सकता। समाजवाद, पूँजीवाद, प्रजातंत्र अथवा कोई भी वाद अधिक से अधिक एक रास्ता है, प्रगति का आधार नहीं । व्यक्तिगत, दलगत या वादगत कोई विचार लेकर चलने से प्रगति नहीं हो सकती। राजनीति आखिर राष्ट्र के लिए ही है। यदि राष्ट्र का विचार छोड़ दिया, यानी राष्ट्र की अस्मिता, उसके इतिहास, संस्कृति, सभ्यता को छोड़ दिया तो राजनीति का क्या उपयोग? राष्ट्र का स्मरण कर कार्य होगा तो सबका मूल्य बढ़ेगा। राष्ट्र को छोड़ा तो सब शून्य जैसा ही है।
इस प्रकार जब हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय के राजनीतिक दर्शन के सूत्रों को देखते हैं तो उनमें राष्ट्र सर्वोपरि की भावना और चिंतन दिखाई देता है। वे बारंबार इस बात पर बल देते हैं कि राजनीति को राष्ट्रीयता का पोषण करने वाली होना चाहिए। साथ ही वे राष्ट्र को क्षीण करने वाली राजनीति को त्याज्य मानते हैं। अनुशासन और शुचिता को महत्व देते हैं। इसीलिए वे किसी भी दल के लिए – दर्शन, नेता, नीति, कार्यकर्ता और कार्यक्रम जैसे पांच प्रमुख सूत्र देते हैं। राजनीति का उद्देश्य सत्ता प्राप्ति की होड़ नहीं अपितु जनहित राष्ट्रहित की ओर प्रेरित और पथप्रदर्शित करते हैं। स्पष्टतः पं दीनदयाल उपाध्याय के राजनीतिक दर्शन में भारतीयता और संस्कृति स्पष्ट रूप से प्रतिबिम्बित होती है। उनकी राष्ट्रोन्नति से आप्लावित वैचारिक चेतना में राष्ट्र के सर्वाङ्गीण विकास का दिशाबोध और स्पष्ट दृष्टिकोण प्राप्त होता है। जो सतत् नूतन भारत को गढ़ने का मार्ग दिखाता है। पंडित जी का पूरा दर्शन राष्ट्रीय एकता, अखंडता, एकात्मता और समस्याओं का नीर-क्षीर विवेचन कर- राष्ट्र संस्कृति से सबको संस्कारित करता है। मूल्यों की विरासत के साथ राष्ट्रनिष्ठ- शुचितापूर्ण राजनीति का युगबोध प्रदान करता है।
कृष्णमुरारी त्रिपाठी अटल