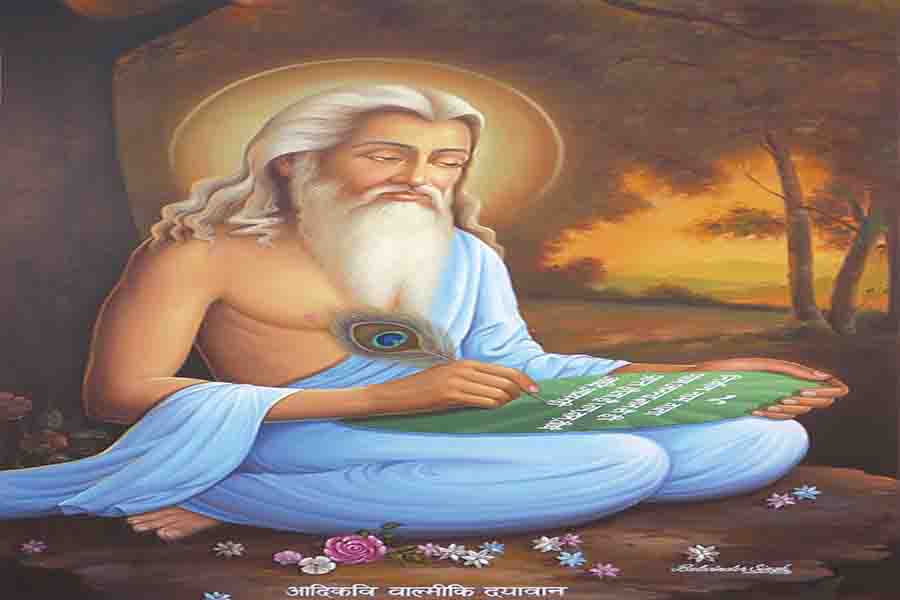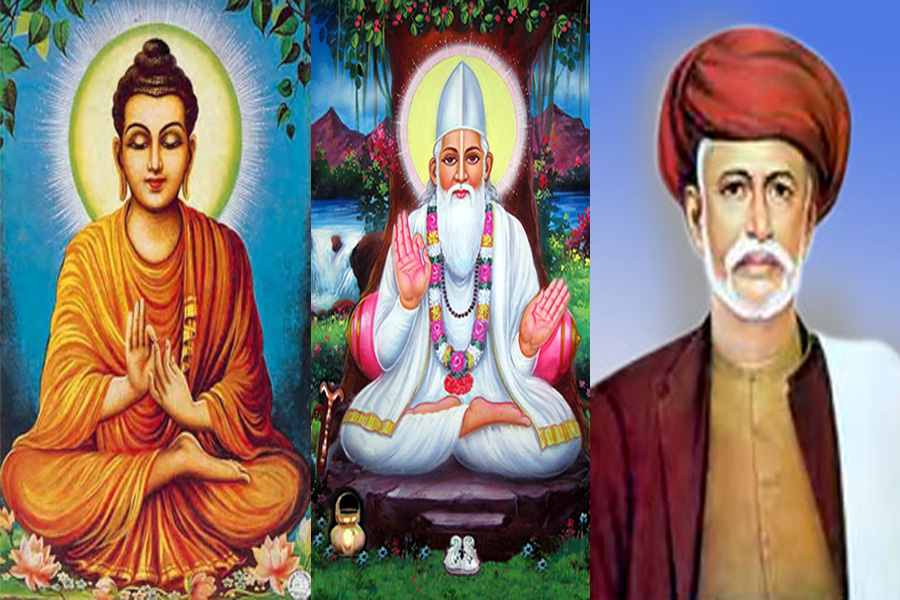भा रत की सनातन परम्पराऔर चिंतनधारा की एक विशेषता रही है कि समाज की निरंतरता और जीवन प्रवाह में जब भी किसी प्रकार का अवरोध अथवा अवमूल्यन का अवसर आया, तब तब किसी न किसी महापुरुष ने इस पवित्र भारत भूमि पर जन्म लेकर अपने प्रेरक व्यक्तित्व एवं कृतित्व से तत्कालीन समाज में व्याप्त कुरीतियों और दोषों का उन्मूलन करके उसे फिर से नवजीवन प्रदान किया है। यही कारण है कि हजारों वर्षों से भारत अभी तक अपने सनातन और चिन्मय स्वरूप में अवस्थित है और उसकी प्राचीन सभ्यता और संस्कृति आज भी विश्व मानवता को सार्थक संदेश दे रही है। भारत के वाङमय ने स्पष्ट रूप से घोषणा की।
एतदृेश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मन्।
स्वं स्वंचरित्र शिक्षरेन पृथिव्या: सकल मानवा॥
अर्थात् इसी भारत की पवित्र भूमि ने समय-समय पर ऐसे महापुरुषों को जन्म दिया है, जिनके विमल व्यक्तित्व के प्रकाश में समस्त मानवता को एक नई सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि प्राप्त हुई, जिसके फलस्वरुप समाज में परस्पर सद्भाव और सहिष्णुता के वातावरण का निर्माण हुआ और केवल भारत ही नहीं संपूर्ण विश्व का कायाकल्प हो गया। इस दृष्टि से यदि भारत की सनातन परम्परा का विहंगालोकन करें तो पाएंगे कि प्राचीन काल से ही ऐसे ऋषतुल्य, दूरद्रष्टा महापुरुषों की यह मालिका निरंतर चली आ रही है और समाज उनके पावन कर्तृत्व से स्वयं को उपकृत अनुभव करता रहा है।
यह हम सब जानते ही हैं कि भारत की जीवन पद्धति और परंपरा का आधार ऋषि और कृषि संस्कृति रहा है। प्राचीन काल में ऋषि समाज का वैचारिक प्रबोधन करते थे और कृषि समाज को समृद्धि, संपन्नता और आर्थिक सामर्थ्य प्रदान करके उसे वैभवपूर्ण बनाती थी। यह ऋषि परम्परा ही थी जिसने आदिकाल से भारत को तत्व चिंतन दिया, जो सनातन और सर्वस्पर्शी था और प्राणी मात्र को सुख और आनंद प्रदान करने वाला था। फलस्वरुप भारत की ऋषि परंपरा का उद्घोष था कि यह समस्त पृथ्वी एक कुटुंब के समान है, इसमें कोई पराया नहीं और कुछ भी निजी नहीं, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं। सभी समान हैं, सभी उदार हैं।
अयं निज: परोवेति, गणेना लघुचेतसाम्।
उदार चरितानन्तु वसुधैव कुटुंबकम्॥
भारत की संस्कृति और व्यवहार प्रणाली उपर्युक्त सूत्र और तत्व चिंतन पर आधारित होकर पल्लवित हुई अत: प्राणीमात्र में एक ही ईश्वर के दर्शन करके सबके सुख, आरोग्य और समृद्धि की कामना करती है
सर्वेभवन्तु सुखिन: सर्वेसन्तु निरामया।
सर्वेभद्राणि पश्यंतु, मा कश्चिद दुख भाग भवेत॥
तथापि मध्यकाल तथा उससे भी पहले देश पर मुगलों और बाद में ब्रिटिशों के आक्रमण के फलस्वरूप भारत के संस्कार और जीवन-व्यवहार में विकृतियां आईं, उसका परिणाम हुआ कि हिन्दू समाज में जाति के आधार पर अस्पृश्यता अथवा छुआछूत की कुरीति ने जन्म लिया। जिसने उन्नीसवीं शताब्दी तक आते-आते पूरे हिन्दू समाज को विभिन्न जातियों-उपजातियों में बांट दिया और हिन्दू समाज में इस भेदभाव के कारण आर्थिक तथा सामाजिक स्तर पर अनेक प्रकार की विकृतियों ने जन्म लिया और हिन्दुस्थान सैंकडों वर्षों तक विदेशी शक्तियों के आधीन रहा। समाज को अस्पृश्यता तथा छुआछूत के इस कलंक से मुक्त कराने के लिए बीसवीं शताब्दी में डॉ. भीमराव आंबेडकर जैसी महान विभूति ने जन्म लेकर समाज को नई दिशा दी और अपने ओजस्वी व्यक्तित्व से हिन्दू समाज के दलित वर्ग को नया आत्मविश्वास दिया जो स्तुत्य है। यद्यपि इससे पहले भी समाज में समरसता के भाव को पैदा करने के लिए अनेक संतों तथा महापुरुषों ने भरपूर प्रयत्न किए थे किन्तु डॉ. भीमराव आंबेडकर ने जिस प्रकार से दलितों और समाज के उपेक्षित समाज का नेतृत्व किया था उससे हिन्दू समाज को एक ओर तो अपनी गलती स्वीकार करनी पड़ी और दूसरा अस्पृश्यता उन्मूलन का यह आंदोलन समग्र रूप से अधिक शक्तिशाली और परिपक्व होकर उभरा। तथापि, यह ध्यान देने योग्य है कि डॉ. भीमराव आंबेडकर ने अस्पृश्यता को समाप्त करने का यह काम भारत की चिंतन पद्धति तथा परम्परा के आधार पर ही आगे बढ़ाया था। यह बात हमें उनके विचारों में स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है। ६ फरवरी, १९५४ को उन्होंने आचार्य अत्रे द्वारा निर्मित फिल्म ‘महात्मा फुले’ का उद्घाटन किया था, उस अवसर पर उन्होंने कहा था ‘आज देश में चरित्र नहीं बचा है…। जिस देश में नैतिकता नहीं होती उसका भविष्य कुंठित होता है। फिर देश के प्रधान मंत्री जवाहरलाल नेहरू हो या मुख्यमंत्री मोरारजी देसाई, तुम्हारा भविष्य अंधकारमय ही रहेगा। मंत्री देश का उद्धार नहीं कर सकते, जिसने धर्म को भलीभांति समझा है, वहीं देश को तार सकता है। महात्मा फुले ऐसे ही धर्म सुधारक थे। विद्या, प्रज्ञा, करुणा, शील और मैत्री भाव इन धर्मतत्वों से प्रत्येक को अपना चरित्र बनाना चाहिए। करुणा रहित विद्यावान को मैं कसाई समझता हूं, करुणा के अर्थ में मानव-मानव के आपसी प्रेम से ही मनुष्य को आगे आना चाहिए।
डॉ. आंबेडकर की उक्त अभिव्यक्ति, वास्तव में भारत की आर्ष परम्परा का ही तो दर्शाती है। भारत की आर्ष परम्परा में ऐसे महापुरुषों-ऋषियों की एक लंबी सूची है, जो जन्म से निम्न जाति के थे, किन्तु उन्होंने अपने तप:पूत जीवन और साधना से भारत की सनातन परम्परा को सदैव समृद्ध किया। ऋषि विश्वामित्र क्षत्रिय कुल में पैदा हुए थे, किन्तु अपने तपबल से वे महर्षि बने और उन्होंने श्रीराम एवं लक्ष्मण का समुचित मार्गदर्शन किया था। इसी प्रकार से रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मिकि, यद्यपि शिकारी थे किन्तु अपनी साधना से वे भी महर्षि के रूप में प्रतिष्ठित हुए। संपूर्ण हिन्दू समाज को भगवान राम के जीवनचरित से अवगत कराने वाले महर्षि वाल्मिकि की गोस्वामी तुलसीदास ने राम चरित मानस के प्रारंभ के मंगलाचरण में हनुमानजी के साथ वंदना की है।
सीता राम गुण ग्रामो पुण्यारण्य विहारिणौ
वन्दे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो।
श्री सीताराम के गुण समूह रूपी पवित्र वन मेंे विहार करने वाले, विशुद्ध विज्ञान संपन्न कविश्वर श्री वाल्मिकी जी और कपीश्वर श्री हनुमानजी की मैं वंदना करता हूं। यहां यह दृश्य है कि उक्त श्लोक में महाकवि तुलसी ने श्री हनुमानजी से भी पहले महर्षि वाल्मिकि का उल्लेख करके उनकी वंदना की है जो यह सिद्ध करती है कि सनातन समाज व्यवस्था में जातिगत आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव का विचार नहीं किया जाता था। महर्षि वाल्मिकि, यद्यपि वे निम्न जाति के थे, उनको विश्व साहित्य में आदि कवि के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त है। जब उन्होंने काम-क्रीडा में रत क्रौंच पक्षी के जोड़ में से नर पक्षी को व्याध द्वारा तीर से मार दिए जाने पर, मादा पक्षी के करुणा विलाप को देखा तो हृदय विदारक दृश्य से वाल्मिकि का कवि हृदय भी करुणा से भर गया और उससे उत्पन्न भाव कवित्व के रूप मे स्वत: फूट पड़े और काव्य की रचना हुई। और निम्न पंक्तियां विश्व साहित्य की पहली कविता मानी गई-
मा निषाद प्रतिष्ठां त्व गम: शाश्वती समा
यत्क्रौंच मिथुनादेकं अवधी काम मोहिता।
इन्हीं विश्ववंद्य वाल्मिकि ने उसके बाद रामायण की रचना की जिससे आज सारा संसार लाभान्वित और संपूर्ण हिन्दू समाज गौरवान्वित अनुभव करता है। ‘यद्यपि, यहां यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि महर्षि वाल्मिकि को रामायण ग्रंथ लिखने की प्रेरणा देने वाले देवर्षि नारद भी जाति के आधार पर कोई उच्च कुल का जन्मा नहीं थे, बल्कि एक दासी के पुत्र थे। इसका उल्लेख श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंध के पांचवें अध्याय में आता है, जिसमें स्वयं नारद स्वयं कहते हैं-
अहं पुरातीत भवे भवे मुने
दास्यास्तु कस्याचन वेदवादिनाम।
निरुपितो बालक एवं योगिना
शुश्रुषणों प्रावृषि निर्विविसताम (श्रीमद् भागवत १/५/२३)
मुने, पिछले कल्प में अपने पूर्व जीवन में मैं वेदवादी ब्राह्मणों की एक दासी का पुत्र था। वे योगी वर्षाऋतु में एक स्थान पर चातुर्मास कर रहे थे। बचपन में मैं उनकी सेवा में नियुक्त कर दिया गया। यद्यपि मैं उस समय बालक ही था, फिर भी मैं निष्ठापूर्वक उनकी सेवा करता था। बाद में यही बालक देवर्षि नारद के रूप में संपूर्ण सनातन हिन्दू धर्म और वाङमय के प्रणेता बने। ऐसे दासी पुत्र देवर्षि नारद से, व्याध से महर्षि बने वाल्मिकि ने पूछा कि मेरा मन बहुत अशांत है और इस अशांत मन को शांत और स्वस्थ करने के लिए मैं क्या करूं। इस पृथ्वी पर इस समय कौन ऐसा महापुरुष हैं जिसके जीवन चरित्र का वर्णन करके मैं स्वयं धन्यता का अनुभव करूं और शांति प्राप्त करूं-
कोन्वस्मिन साम्प्रंत लोके गुणवान कश्च वीर्यवान्
धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्य दृढ़व्रत:
इस समय पृथ्वी पर कौन ऐसा गुणवान, धर्मज्ञ, सत्यवादी और दृढ़ प्रतिज्ञ व्यक्ति है, जिसका गुणगान किया जा सकता है। तब दासी पुत्र देवर्षि नारद ने इक्ष्वाकु वंशोत्पन्न ‘राम’ के गुणों का उल्लेख करते हैं और वाल्मिकि को राम चरित पर काव्य की रचना करने का निवेदन करते हैं-
नियतात्मा महावीर्योघुतिमान धृतीमान वशी
बुद्धिमान नीतिमान वाग्मी श्रीमाच्छत्रुनिवर्हण:
तमेव गुण सम्पन्न राम सत्य पराक्रमम्
ज्येष्ठं ज्येष्ठ गुणौर्युक्त प्रियं दशरथ: सुतम॥
तब महर्षि वाल्मिकि लोकवंद्य मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के चरित्र को ‘रामायण’ में निरूपित करके समस्त हिन्दू समाज को एक आदर्श चरित्र प्रदान करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने उन्हीं के ग्रंथ को अपनी प्रेरणा का स्रोत मान कर अवधी हिन्दी में श्री रामचरित मानस की रचना की है।
इसी प्रकार से छांदग्योपनिषद के ऋषि के रूप में प्रतिष्ठित हुए ऋषि मतंग निम्न जाति के थे, लेकिन वे हिन्दू धर्म की परंपरा में ब्रहर्षि के पद पर प्रतिष्ठित हुए। भारत के इतिहास के पूर्ववर्ती काल में चन्द्रगुप्त मौर्य यद्यपि निम्न जाति के थे, कौटिल्य चाणक्य के निर्देशन में उन्होंने नंद वंश का नाश करके संपूर्ण भारत में हिन्दू साम्राज्य को स्थापित किया।
आधुनिक काल में अर्थात उन्नीसवीं तथा बीसवीं शताब्दी में जिन महापुरुषों ने हिन्दू धर्म और हिन्दुत्व को नव चैतन्य प्रदान किया, वे भी ब्राह्मण नहीं थे। महर्षि अरविन्द, स्वामी विवेकानन्द तथा महात्मा गांधी आदि सभी ऐसे व्यक्तित्व थे जो अब्राह्मण थे, किंतु उन्होंने अपनी तेजस्विता और तप से भारतीय समाज के आलोक स्तंभ के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त की है। डॉ. भीमराव आंबेडकर उसी मालिका के ज्योतिपुंज नक्षत्र हैं, जिन्होंने भारत को विश्व का सबसे बड़ा और सर्वस्पर्शी संविधान दिया जो आज भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था का आधार है, जिसमें भारत के प्रत्येक नागरिक को न्याय-आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्वतंत्रता: विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, समानता: पद और अवसर की तथा उनमें व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करते हुए बंधुता की गारंटी देने का संकल्प व्यक्त किया गया है। भारत का संविधान भारत की शासन व्यवस्था और विधि की गंगोत्री है, जिससे विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका निदेशित और निगमित होती हैं।
डॉ. आंबेडकर के संपूर्ण चिंतन में समाज में समरसता, परस्पर सद्भाव, सहिष्णुता को स्थापित करने का आह्वान मिलता है। अस्पृश्य समाज-महार जाति में जन्म होने तथा तत्कालीन तथाकथित उच्च वर्ण और वर्ग के लोगों द्वारा अस्पृश्य होने के बावजूद उन्होंने २५ नवम्बर, १९४७ को दिए गए एक वक्तव्य में कहा था, ‘हम सब भारतीय परस्पर सगे भाई हैं- ऐसी भावना अपेक्षित है, इसे ही बंधुभाव कहा जाता है और आज उसी का अभाव है। जातियां आपसी ईर्ष्या और द्वेष बढ़ाती हैं अत: यदि राष्ट्र के उच्चासन तक हम पहुंचना चाहते हैं तो इस अवरोध को दूर करना होगा। क्योंकि जहां राष्ट्र का अस्तित्व होगा, नहीं बंधुभाव पनपेगा। बंधुभाव ही नहीं रहेगा तो समता, स्वाधीनता का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा।’
अपने चिंतन की दिशा और आधार भूमि को स्पष्ट करते हुए डॉ. आंबेडकर साहब ने कहा था, ‘मेरा तत्वज्ञान राजनीति से नहीं धर्म से उपजा है। भगवान बुद्ध के उपदेशों से मैंने वह ग्रहण किया है। उसमें स्वाधीनता और समता को स्थान प्राप्त है। किन्तु अपरिमित स्वाधीनता से समता का नाश होता है। मेरे तत्वज्ञान में स्वाधीनता और समता का उल्लंघन न हो, केवल इसलिए सुरक्षा के नाते कानून के लिए जगह है किन्तु केवल कानून ही स्वाधीनता और समता की गारंटी है ऐसा मैं नहीं मानता। इसलिए मेरे विचार में बंधुभाव ही सुरक्षा की गारंटी हो सकता है। इसी बंधुता का दूसरा नाम मानवता है और मानवता ही धर्म है।
डॉ. आंबेडकर के इस मानव धर्म की झलक हम अपने प्राचीन वाङमय-उपनिषद में भी पाते हैं
सहनाववतु, सहनौभुनक्तु, सह वीर्य करवाव है
तेजस्विनांवधीत मस्तु। मा विद्विषावहै, ॐ शांन्ति, शान्ति, शान्ति
आओ हम सब की रक्षा करें, सभी मिल कर सुख प्राप्त करें (भोग करें)। हम सह एक साथ मिलकर पुरुषार्थ करें। हमारी विद्या तेजस्वी हो। हम एक दूसरे से द्वेष न करें।
इसी बंधुभाव को स्थापित करके एक समरसता और ममतापूर्ण समाज की कल्पना डॉ. आंबेडकर ने की थी, जिसमें किसी भी प्रकार से भेदभाव न हो, सभी को समान अवसर प्राप्त हो और सामाजिक दृष्टि से सभी ही सहिष्णु बनें इस प्रकार डॉ. आंबेडकर ने भारत की सनातन चिंतन धारा को युगानुकूल स्वरुप देकर समाज में समता और समरसता को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। यही कारण है कि स्वातंत्र्यवीर सावरकर जैसे प्रखर हिन्दुत्वनिष्ठ और क्रांतिकारी महापुरुष ने डॉ. आंबेडकर के व्यक्तित्व और कृतित्व की भूरि भूरि प्रशंसा की थी। १४ अप्रैल, १९४२ को बाबासाहब के ५० वें जन्मदिवस पर शुभकामनाएं देते हुए उन्होंने कहा था, ‘‘आंबेडकर अपने व्यक्तित्व, विद्वता, संगठन कुशलता और नेतृत्व कुशलता के कारण ही देश के एक आधारभूत महापुरुष गिने जा सकते थे। किन्तु अस्पृश्यता के उन्मूलन और लाखों अस्पृश्य बंधुओं में साहसपूर्ण आत्मविश्वास और चेतना जगाने में उन्हें जो यश मिला है, उससे उनके द्वारा भारत की अमूल्य सेवा हुई है।
आंबेडकर जैसे महान व्यक्ति का जन्म, तथाकथित अस्पृश्य जाति में हुआ, यह बात अस्पृश्य वर्ग की निराशा मिटाकर कथित स्पृश्यजनों के थोथे बड़पन्न को चुनौती देने की प्रेरणा दिए बगैर नहीं रहेगी। आंबेडकर के व्यक्तित्व के प्रति आदर रखते हुए मैं उनके स्वस्थ दीर्घ जीवन की कामना करता हूं, जिससे वे अपने समाज में प्रभावी परिवर्तनकारी अभियान चला सकें।’’ ऐसे ऋषि परंपरा के प्रतिनिधि भारत रत्न डॉ. भीमराव आंबेडकर की चेतना का कोटि कोटि अभिवंदन!
मो.: ९८२०२१९१८१