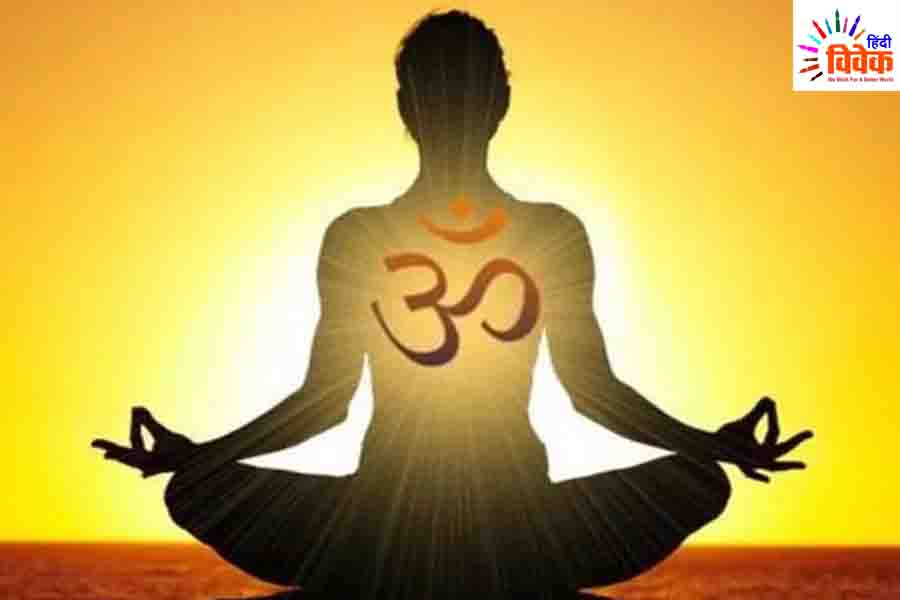भारत में 1993 को नयी औद्योगिक नीति की घोषणा हुई। विदेशी ऋण चुकाने के लिए भारत का जून 1991 में 43 टन सोना गिरवी रखना पड़ा। बाद में अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आई.एम.एफ.) ने भारत को 6.25 बिलियन डॉलर का ऋण दिया, किन्तु साथ-साथ अपनी शर्तें रखीं। यह क्रम भी तैयार किया गया कि इन शर्तों को समाहित करने वाली उद्योग-वित्त नीति पहले घोषित हो, बाद में सहायता मिलेगी। इन्हीं शर्तोंं के आधार पर यह नयी नीति बनी।
आई.एम.एफ. की शर्तें
सभी समस्याग्रस्त, बीमार एवं आर्थिक संकट से जूझते देशों को वित्त सहायता देते समय विश्व बैंक या आई.एम.एफ. उन दिनों प्राय: 4 शर्तें रखते थे- 1) डी-लाइसेंसिंग 2) डी-वैल्यूएशन 3) डी-फ्लेशन और 4) डी-इन्वेस्टमेंट। इनको उन दिनों ‘डी-4 कोर्स’ के नाम से भी जाना जाता था।
1. डी-लाइसेंसिंग- लाइसेंस या परमिट राज के चलते उत्पादन प्रक्रिया में तेजी से विकास सम्भव नहीं होगा इसलिए सरकार हस्तक्षेपी स्थान से हट जाये और उत्पादन ढांचे को मुक्त करे। इसका अर्थ यह कि कोई भी, जो चाहे वह उत्पाद या सेवा बना सकेगा और उसमें सरकार का हस्तक्षेप नहीं होगा, यह एक शर्त बनी थी।
2. डी-वैल्यूएशन- दूसरी शर्त थी भारत की मुद्रा का अवमूल्यन करने की। उन दिनों 19 रुपया एक डॉलर के लिए विनिमय की दर भारत ने तय करायी थी। वैश्विक मुद्रा बाजार में भारत की मुद्रा बहुत ही गिरी है, इसलिए अब मुक्त अर्थ व्यवस्था के अन्दर इस ऊंचे दर पर आयात-निर्यात सम्भव नहीं है। इसको भारत ने स्वीकार करते हुए अनुबन्धित विनिमय दर को हटाकर मुद्रा के विनिमय की दर वैश्विक वित्तीय व्यवस्था को तय करने के लिए सौंपी जाये और जो वाजिब स्तर लगता है, वह विनिमय की दर होगी, इसे शर्त के रूप में भारत ने स्वीकार किया। परिणाम स्वरूप जो डॉलर 19 रुपये में मिलता था, उसके लिए तब 40 रुपया देना पड़ा और इस तरह अवमूल्यन की शर्त को भी भारत ने माना। आज नीचे खिसकते खिसकते यह विनिमय दर अब रु.60 पर पहुंची है।
3. डी-फ्लेशन– तीसरी शर्त थी, मुद्रा स्फीति को रोकना। घाटे के बजट आजादी के बाद भारत में प्रस्तुत होते आये हैं। जानकारों की यह अवधारणा रही है कि ऐसा करने से बेरोजगारी निम्न स्तर पर रहती है और लोगों की आय के अवसर बढ़ते हैं। किन्तु यह वित्तीय घाटा पूरा करने के लिए सरकारें देशी-विदेशी ऋण लेती आयी हैं उसी तरह ज्यादा नोट छापना और उन्हें वितरित करने का काम भी बराबर होते आया है। ऐसी अतिरिक्त मुद्राएं भयंकर महंगाई फैलाती हैं और जीवन-यापन मुश्किल होता है, इसलिए शर्त के रूप में सलाह यह आयी कि वित्तीय घाटा कम करें और मुद्रा स्फीति को रोकें।
4. डी-इन्वेस्टमेंट- अन्त में चौथी और महत्वपूर्ण शर्त थी, सरकारी उपक्रमों के विनिवेश करने की। तर्क यह था कि इससे पूंजी बढ़ेगी, निवेश बढ़ेगा एवं उत्पादनों में स्पर्धा होगी। सरकारी उद्योगों में हो रहे अंधाधुंध व्यय पर रोक लगेगी, उत्पादन के तरीके बदलेंगे, उद्योगों की बीमारी का बोझ सीधा सरकार पर नहीं आएगा। यह संकट से उबारने का एक रास्ता था और यह शर्त भी औद्योगिक नीति के तहत भारत ने मानी।
साथ-साथ विश्व स्तर पर व्यापार को लेकर 1986 से चल रही वार्ताएं भी वैश्विक व्यवस्था के आमूल-चूल परिवर्तन के प्रस्तावों को लेकर अन्तिम चरण में पहुंच चुकी थीं। गैट एवं यू.एन.सी.टी.ए.डी. (यूनाइटेड नेशन्स कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एण्ड डेवलपमेंट) तब तक व्यापार के वैश्विक संचालन में जुटे थे। अब उनके स्थान पर डब्ल्यू.टी.ओ. गठित करते हुए वैश्विक व्यापार चलाने का मन बड़ी ताकतों ने बनाया था। इस तरह विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू.टी.ओ.) का 1/4/94 को निर्माण हुआ।
विश्व व्यापार मुक्त हो, निवेश सर्वसंचारी रहे, बौद्धिक सम्पदा सुरक्षित रहे और व्यापार में वस्तुओं के साथ सेवाएं शामिल हों आदि बुनियादी चिन्तन के बिन्दुओं पर डब्लू.टी.ओ. का निम्न कार्यक्रम बन गया-
1) सदस्य देश व्यापार या निवेश के लिए अपने दरवाजे खोलें 2) आयात शुल्क या सीमा शुल्क न्यूनतम बनाएं 3) व्यापार केवल वस्तुओं तक सीमित न रहकर उसमें सेवाएं भी सम्मिलित रहें और 4) आदान-प्रदान मुक्त रूप से चले और कोई भेदभाव न हो आदि।
विदेशी मुद्रा संकट से भारत पहले से ही झुका हुआ था और विवश था, इसलिए बिना ज्यादा विरोध किये भारत को इस नयी व्यवस्था में शामिल होना पड़ा। इस कारण से हुए सम्प्रभुता के संकोच को भी स्वीकार करना पड़ा। एक तरफ अब नयी व्यवस्था में सरकारी उद्योगों का विनिवेश करना था तो दूसरी तरफ डब्लू.टी.ओ. की नीति के तहत विश्व व्यापार के नये दौर में विदेशी निवेश के लिए दरवाजे खोलने थे। अब इन आयामों पर काम कैसा हो? कितना हो? तथा कौन से क्षेत्र में विदेशी निवेश को आहुत किया जाये? आदि अनेक प्रश्न थे। विषय भी नये थे तथा किसी को इसका प्रत्यक्ष अनुभव नहीं था।
विदेशी निवेश की नीति के तहत काम करके भी देश हित को आगे बढ़ाया जा सकता है, इसका कुछ नमूना तब तक चीन ने विश्व के सामने प्रस्तुत किया था। किन्तु भारत में इन सारे विषयों पर न बहस हुई; न किसी ने जनता की राय पूछना जरूरी समझा।
विदेशी निवेश आवश्यक है, पूंजी की ताकत बढ़ाने के लिए। अब यह पूंजी विदेशी क्यों चाहिए? इस बुनियादी सवाल का जवाब आज तक किसी भी सरकार ने दो टूक नहीं दिया है। फिर दूसरा एक महत्वपूर्ण सवाल यह भी रहा है कि विदेशी मुद्राएं आएंगी उसका सरकार क्या करेगी? इसका भी सीधा जवाब सरकारों ने नहीं दिया। समय-समय पर उत्तर बदलते रहे हैं।
पहले कहा था कि विदेशी मुद्राएं आएंगी तो विदेशी ऋण पूरा लौटाकर उससे निजात पा लेंगे।
फिर एक बार यह बताया गया कि ऐसी जमा-पूंजी से बुनियादी विकास के काम करेंगे तथा उत्पादक इकाईयों का निर्माण करके रोजगार बढ़ाएंगे।
अब सरकार कहती है कि ऐसी जमा-पूंजी सरकार गरीबों पर खर्च करेगी। सच तो यह है कि विनिवेश कार्यक्रमहै, कोई नीति नहीं।
विदेशी ऋण के बदले विदेशी निवेश
एक बहस उन दिनों ऐसी भी चली थी कि विदेशी ऋण लेकर ब्याज समेत ऋण की किश्तेें चुकाने से अच्छा है कि विदेशी पूंजी को निवेश के लिए आहुत किया जाये। इससे ऋण का बोझ सरकार पर नहीं पड़ेगा और निवेश के लाभ या हानि दोनों की जिम्मेदारी निवेशक की होगी। इसलिए भारत को सीधा विदेशी ऋण नहीं लेना चाहिए उसके विकल्प के रूप में:-
1. सरकार उद्योगों की विनिवेश प्रक्रिया में विदेशी निवेशक अपनी पूंजी लगाएं, अथवा
2. निजी क्षेत्र के उद्योगों में पूंजी निवेश करते हुए साझेदारी निभाएं, अथवा
3. अपनी पूंजी लेकर सीधे ही अपना कारोबार शुरू करें, अथवा
4. सरकार, निजी क्षेत्र और विदेशी क्षेत्र तीनों मिलकर संयुक्त उद्यम चलाएं।
आदि तरीकों को आजमाना चाहिए, किन्तु सरकार ऋण भी ले रही है और विनिवेश भी कर रही है। स्पष्टता के अभाव में यह हो रहा है।
भारत एक विशाल मार्केट सरकार जरूरत के आधार पर यह तय करती है कि सरकारी उद्यम की कितनी इक्विटी अपने पास रखे और कितनी बेचे। विदेशी भारत को एक विशाल मार्केट मानते हैं। भारत के 25 प्रतिशत लोग ऐसे हैं जिनके पास पर्याप्त स्रोत हैं। उनके जीवनमान का स्तर प्रतिदिन ऊंचा हो रहा है, इसलिए विदेशी महंगी आरामदायी चीजें, सौन्दर्य प्रसाधन, खान-पान की महंगी चीजें बेचने वाले मार्केट तथा टूरिजम, होटल, एंटरटेनमेंट आदि कारोबार भारत में तेजी से बढ़ रहा है। खाद्यान्न बाजार में निरन्तर मांग है। बीमा क्षेत्र के लिए अभी विस्तार के काफी अवसर हैं, इसलिए सारे विदेशी उद्यमी, व्यापारी, निवेशक लालचभरी आंखों से भारत को देख रहे हैं। विदेशी निवेश बिना शर्त हो, मुद्राएं विनिवेश करके निकाल लेना भी सहज बने और मुनाफा विदेश में ले जाने की पूरी छूट हो, ऐसी स्थिति भारत के सभी उपलब्ध क्षेत्रों में 100 प्रतिशत एफ.डी.आई. की छूट जब तक नहीं बनती तब तक विदेशी ताकत भारत के राजनेताओं, नीति बनाने वालों और नौकरशाहों पर अपने जाल फेंकते रहेंगे।
स्थायी सरकार कौन सी?
भारत में हर पांच वर्ष के बाद जनता अपनी सरकार चुनती है। विपक्षी सरकार में आ जाये तो नीतियां बदलती हैं एवं वही गठबंधन दुबारा चुनकर आये तो भी नीतियां बदल सकती हैं यह यूपीए. सरकार नं 2 देखने के बाद प्रतीत हुआ है। ज्यादातर चुनाव जीतने की तरफ ध्यान केन्द्रित करती हुई नीतियां एवं कार्यक्रम रखने के कारण राजनैतिक दल एवं राजनेता दीर्घ सूत्री नीतियों की तरफ नहीं देखते हैं; न ही उनकी समझ के दायरे में वे रहती हैं। ऐसे में राजनेताओं की सरकार अस्थायी और नौकरशाहों की सरकार स्थायी मानी जाती है। इसलिए विदेशी निवेश की नीति पर चर्चा का महत्वपूर्ण बिन्दु यह है कि भारत के नीति सूत्र क्या हैं? यह समझने के लिए पूछना पड़ेगा की नौकरशाही समझ क्या है?
विदेशी निवेश पर चिन्तन
15% की इक्विटी होल्डिंग पर भारत की किसी भी कम्पनी के प्रबंधन पर कब्जा किया जा सकता है। ऐसे में विदेशी निवेश के लिए 26%, 49%, 74%, 100% ऐसे विभिन्न स्तरों के निवेश खोलने का क्या मायने बनता है? इसका स्पष्ट चिन्तन क्या भारत के नौकरशाहों ने किया है? एक दो उदाहरण देखें।
टेलिकॉम कम्पनियां कितने ही देशों में जासूसी करती रही हैं। ऐसे में कोई टेलिकॉम कम्पनी 74% निवेश लेकर भारत में काम करेगी तो बचे हुए 26% को लेकर पार्टनर बनने वाला क्या इस जासूसी के खतरे को रोकने की स्थिति में होगा? इसका जवाब न किसी राजनेता के पास है न ही किसी नौकरशाह के पास।
कोई भारत की कम्पनी गढ्ढे बनाने का ठेका चीन की कम्पनी को देती है और भारत की सड़कों पर चीनी मजदूर मेहनतकश कामों में लगे हैं यह नजारा क्या भारत के हितों के पक्ष में है अथवा नहीं? ऐसे कितने ही आयामों पर भारत की स्थायी सरकार को चलाने वाले नौकरशाह क्या सोचते हैं एवं उनकी सोच का सूत्र क्या है, यह परखना पड़ेगा।
एन. के सिंह कमेटी रिपोर्ट-
ऐसे एक नौकरशाह थे भारत सरकार के महत्वपूर्ण विभाग में सेक्रेटरी पद पर काम कर चुके श्रीमान एन. के. सिंह। उनकी अध्यक्षता में वर्ष 2000 में विदेशी निवेश को लेकर एक कार्यदल गठित हुआ था। भा. म. संघ एवं अन्य संगठनों ने बड़ा हंगामा किया और तब इस कार्यदल की रिपोर्ट ठण्डे बस्ते में चली गयी। वह रिपोर्ट आज भी उपलब्ध है । इससे भारत की नौकरशाही का अन्तर्मन उजागर होता है।
फसल को छोड़कर अन्य खेती व्यवसाय में, उत्पादन क्षेत्र में, सड़क निर्माण में, होटल, टूरिज्म, रिअल इस्टेट एवं बैंकिंग इन सभी क्षेत्रों में 100% विदेशी निवेश को इजाजत देने की सिफारिश समिति ने की थी। अब उन दिनों जो सिफारिशें खारिज हुई थीं। वे लगभग सारी पिछले आठ वर्षों की पिछले दरवाजे से आकर स्थापित हुई हैं। यह भारत के नीति निर्माताओं का अन्तर्मन है।
टेलिकॉम, ईंधन तेल की खोज एवं बिक्री, कोयला, एटमी धातु, हीरा-पन्ना आदि खदान, हवाई अड्डे आदि क्षेत्रों में 74% की सिफारिश लागू हुई है। आयुध निर्माण में 26% की अनुमति को छोड़ दिया जाये तो बाकी सभी उत्पादन प्रक्रिया में, उद्योगों में 49% की सिफारिशें थीं। अब यूपीए सरकार आयुध निर्माण में भी इसे लागू करना चाहती है। एन. के. सिंह के बाद के 10 वर्षों मेंवित्तीय विदेश निवेश का चिन्तन इतना आगे बढ़ गया है कि अब पेंशन संचालन में 26% की पहल यह सरकार कर रही है। अर्थात वह रिपोर्ट जो जनता के दबाव में एक बार खारिज हुई थी, वह ज्यों की त्यों सरकार ने लागू की है। यह विदेशी निवेश की सच्चाई है और यही भारतीय नौकरशाही का अन्तर्मन है।
रोजगार निर्माण पर मोंटेक सिंह कमेटी
ऐसी ही एक रिपोर्ट 2002 में मोंटेक सिंह अहलुवालिया की अध्यक्षता वाली समिति ने दी थी। इस कार्यदल का काम था रोजगार के अवसर खोजना। आगामी विनिवेश एवं विकास की दिशा को जानने के लिए इस समिति की रिपोर्ट को देखना महत्वपूर्ण है। वह इसलिए भी कि मोंटेंक सिंह आज योजना आयोग के अध्यक्ष हैं और प्रधानमंत्री के विश्वासपात्र हैं। दोनों विश्व बैंक के पूर्व कर्मी हैं, तथा दोनों बैंक के पेंशनधारी भी हैं।
रोजगार निर्माण की मोंटेक सिंह कार्यदल की सोच ने पूरे देश को उन दिनों चकित किया था। यह रिपोर्ट भी प्रदर्शनों एवं विरोध के चलते उन दिनों सरकार द्वारा खारिज की गयी। किन्तु यूपीए सरकार में मोंटेक भी स्थापित हुए एवं उनकी सोच भी। बताया गया था कि 8% की विकास दर अर्जित हो जाये तो बेरोजगारी समाप्त होगी। किन्तु यह प्रतिपादन भी कुछ शर्तों के साथ ही आया था। दो महत्वपूर्ण क्षेत्रों के बारे में सुधार के जो सुझाव आये थे, वे महत्वपूर्ण थे।
खुदरा व्यापार क्षेत्र
पहला क्षेत्र था खुदरा व्यापार का। यह बताया गया कि खुदरा व्यापार करने वालों में कौशल की कमी है और ग्रहक की लूट होती है, इसलिए बड़े पैमाने पर खुदरा व्यापार में काम करने वाली विदेशी कंपनियों के हाथों यह कारोबार देना होगा क्योंकि देशी उद्यमियों के पास पर्याप्त अनुभव नहीं है। अब यह करते समय व्यापारी अगर रोजगार विहीन हो जाते हैं तो उने बड़े विदेशी उद्योगों की दुकानों पर काम करने का मौका मिल सकता है; लेकिन कुल मिलाकर रोजगार बढ़ेंगे। अब यह प्रस्ताव उन दिनों सिरे से खारिज हुआ था। लेकिन नवम्बर 2012 में संसद में फिर इन्हीं प्रस्तावों पर बहस हुई।
खेती का क्षेत्र
दूसरा क्षेत्र था किसानों का। यह बताया गया कि छोटे-छोटे टुकड़ों में बंटा हुआ खेती व्यवसाय बड़े उद्योग के रूप में चलाया जाये तो उत्पादन भी बढ़ेगा और विस्थापित किसानों को खेतीहर मजदूर बनकर जीविका का मौका भी मिलेगा। कुल मिलाकर रोजगार बढ़ेंगे। यह बताने में मोंटेंक सिंह नहीं भूले कि ऐसे बड़े पैमाने पर खेती को उद्योग मानकर चलाना इसका अनुभव भारतीय उद्यमियों को न होने के कारण यह कार्पोरेट खेती भी विदेशियों द्वारा चलायी जाये। रिपोर्ट की यह सिफारिश भी उन दिनों खारिज हुई थी। अब सभी अनुभव कर रहे हैं कि खुदरा व्यापार क्षेत्र यूपीए सरकार ने विदेशियों के लिए खोला है। यदि इसी तरह की नीतियां चलती रहीं तो आने वाले कुछ वर्षों में भारत के किसानोंको भी कार्पोरेट का बंधुआ खेतीहर मजदूर बनता हुआ हम देखेंगे।
जैसे पहले भी कहा गया कि एफ.डी.आई. प्रक्रिया में मुख्य कसौटी होती है देश हित की एवं समाज हित की। इसी के साथ यह भी आकलन करना होता है कि क्या विदेशी पूंजी ऐसे क्षेत्रों में आहुत करना अनिवार्य है? सारे घरेलू स्रोत क्या प्रयोग में लाये गए हैं? आने वाली विदेशी पूंजी क्या देश के उत्पादक विकास में लगायी गई है। इन सवालों का जवाब अगर ‘ना’ है तब ऐसे में विदेशी निवेश को पूरी तरह से रोकना चाहिए। यही देश हित का तकाजा है?
स्वदेशी निवेश का दायरा बढ़ाओ
खुदरा व्यापार में विदेशी पूंजी बुलाने के लिए अमेरिका लगातार भारत पर दबाव बना रहा है। भारत इस दबाव के सामने झुका है ऐसी एक चर्चा है। देश की संप्रभुता कायम रखना है तो यह निश्चित करना होगा कि कोई विदेशी ताकत भारत की बांह को मरोड़कर क्षेत्र खोलने पर मजबूर न करती हो।
सकल घरेलू बचत की दर क्या है? इस पर विकास की दर तय है ऐसी मान्यता है। किन्तु विदेश में जो उत्पादक ‘निवेश’ होता है, उसे ही ‘बचत’ माना जाता है। भारत में बड़े पैमाने पर गृह निर्माण और सोना-चांदी आदि की खरीद जैसे अनुत्पादक कामों में बचत चली जाती है। इसलिए पूंजी की उपलब्धता बढ़ाना हो तो जनजागरण के सही तरीके अपनाते हुए उत्पादक निवेश जनता को उपलब्ध कराने होंगे एवं निवेश के लिए जनमत भी बनाना होगा। भारत में पिछले कुछ वर्षों में बड़ी कम्पनियों सरकारी बैंकों इक्विटी निर्गम कुछ ही घण्टों में ओवर सब्स्क्राइब हुए थे। यह अच्छा संकेत है। इसे जानकर ऐसे अवसर जनता को और प्रदान करने होंगे। यह ताकत है, इसे पहचानना होगा। अच्छे विकल्प देकर इस ताकत को देश के कारोबार में लगाना होगा। यह न करते हुए विदेशी निवेश के नाम पर एक संस्थान, कारोबार और उद्योग विदेशियों के कब्जे में देना यह कौन सी अक्लमंदी है? भारत के उत्पादन क्षेत्र का अनमोल हीरा-मारुति हमने सुजुकी को बेचकर कौन सी अक्लमंदी का परिचय दिया है? यह मूर्खतापूर्ण नीतियां तुरन्त रद्द करनी चाहिए।
सावधान भारत! गुलामी की आहट सुनो।