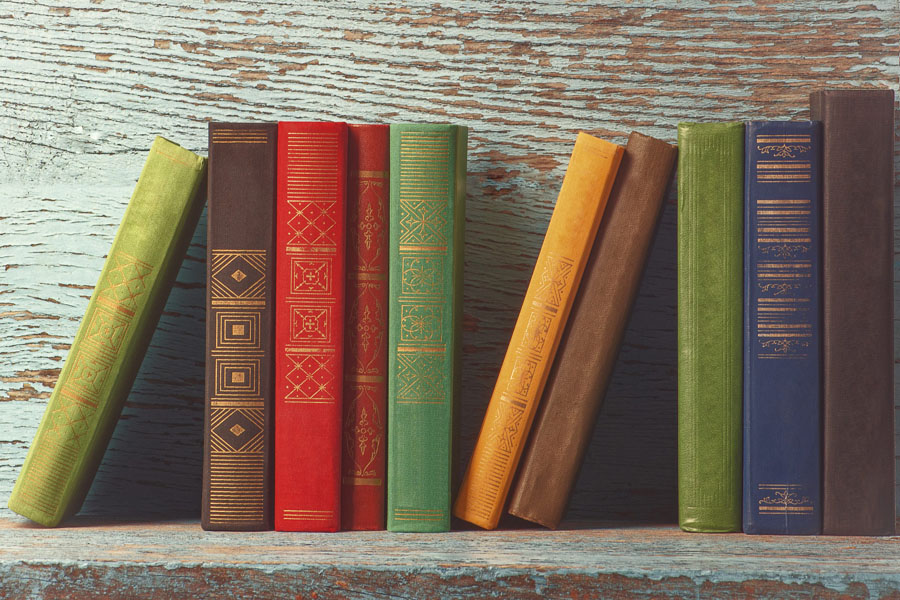हिंदी के प्रकाशकों पर छल का आरोप लगाते हुए विनोद कुमार शुक्ल का जो वीडियो आया है, उस पर चुप्पी साध लेना ठीक नहीं है। प्रकाशकों से यह न्यूनतम मांग की जा सकती है कि वे विनोद कुमार शुक्ल के आरोपों पर अपना पक्ष रखें या कम से कम उनके संशय दूर करें। हालांकि राजकमल प्रकाशन ने इसको लेकर सफ़ाई दी है, लेकिन उस सफ़ाई से भी एक सवाल पैदा होता है। राजकमल के मुताबिक विनोद कुमार शुक्ल के सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास ‘नौकर की कमीज़’ की बीते दस साल में महज 5,500 प्रतियां बिकी हैं। अगर देश में साहित्यिक प्रकाशनों से सबसे बड़े केंद्र से हिंदी के सबसे महत्वूर्ण समकालीन लेखकों में एक विनोद कुमार शुक्ल के सर्वाधिक चर्चित उपन्यास की बिक्री का यह हाल है तो बाक़ी किताबें क्या बिकती होंगी?
यह लेखक की विफलता है, प्रकाशक की या हिंदी के पाठक संसार की? यह विचारणीय प्रश्न है कि जिस भाषा में हर रोज़ डेढ करोड़ से ज़्यादा अखबार बिकते हों, वहां दस साल में एक किताब की पांच हज़ार प्रतियां क्यों बिकती हैं? जिस समाज की फिल्में पांच दिन में सौ करोड़ का कारोबार कर लेती हैं उस समाज के लेखक जीवन भर में अपनी किताबों से दो लाख क्यों नहीं कमा पाते? यह शर्मनाक है। इस शर्मिंदगी को कुछ और बढ़ाना हो तो याद कर सकते हैं कि इन दिनों प्रकाशक सार्वजनिक तौर पर मानने लगे हैं कि वे किताबों के 300 प्रतियों के संस्करण ला रहे हैं। उनकी दलील है कि अब तकनीक ने संस्करण लाना आसान कर दिया है। लेकिन सूचना और संचार के रोज़ व्यापकतर होते इस दौर में किसी किताब की 300 प्रतियां हास्यास्पद से भी कुछ ज़्यादा हैं।
बेशक, सारी किताबों की यह नियति नहीं होती। पिछले कुछ वर्षों में हिंदी में कई किताबों के कई-कई संस्करण बड़ी तेज़ी से सामने आए हैं। खासकर कविता-कहानी, उपन्यास की दुनिया से बाहर इतिहास, राजनीति और समाजशास्त्र की जो किताबें लिखी जा रही हैं, वे ख़ूब बिक रही हैं। लेकिन यह बिक्री फिर भी कितनी है? दस-पंद्रह हज़ार से ज्यादा कौन सी किताबें बिक रही हैं? बस वही किताबें, जिनके लेखकों को किसी और माध्यम से मिली प्रतिष्ठा या लोकप्रियता का सहारा है। लेखक अगर टीवी ऐंकर हैं, मशहूर नेता हैं, फिल्मी सितारे हैं तो उनके नाम पर किताबें बिक जाती हैं- चाहे वे जितनी कूड़ा हों। लेकिन इनसे अलग क्या कोई किताब अपने दम पर पचास हज़ार या एक लाख प्रतियों तक बिक पाती है? इस सवाल का जवाब मायूस करता है। हिंदी के बेस्ट सेलर अभी इस सीमारेखा से काफ़ी पीछे हैं। लेकिन कम से कम 40 करोड़ हिंदीभाषियों के प्रदेश में कोई किताब 50,000 भी क्यों नहीं बिक पाती? क्या इसलिए कि वह ख़राब किताब होती है? या इसलिए कि प्रकाशक उसका ठीक से प्रचार नहीं करते? या फिर वे वास्तविक बिक्री संख्या छुपाते हैं? या फिर इसलिए कि हिंदी समाज किताब नहीं पढ़ना चाहता?
इन सब सवालों पर अलग-अलग विचार किए जाने की ज़रूरत है। शुरुआत लेखन की गुणवत्ता से करें। इसमें संदेह नहीं कि हिंदी में कथा और कविता लेखन लगभग विश्वस्तरीय है। यह बात कम से कम हिंदी के सर्वश्रेष्ठ लेखन के बारे में कही जा सकती है। लेकिन शिक्षा और ज्ञान के दूसरे अनुशासनों में जब हम हिंदी की स्थिति देखते हैं तो अचानक वह कमजोर और नाकाफ़ी क़िस्म के लेखन का ही प्रमाण सुलभ कराती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि शिक्षा और ज्ञान की सारी शाखाओं पर, शोध और अनुसंधान से जुड़े सारे संसाधनों पर अंग्रेज़ी का क़ब्ज़ा है। अचानक अंग्रेज़ी हमारे लिए स्रोत भाषा हो जाती है और हम उसमें हो रहे शोध और चिंतन के दोयम दर्जे के व्याख्याकार और अनुवादक होकर रह जाते हैं। फिर इसमें जो किताबें आती हैं, वे हिंदी की वैचारिक दरिद्रता का आईना बन जाती हैं।
जिन लेखकों के भीतर यह महत्वाकांक्षा होती है कि वे भी अपनी किताब शोध और अनुसंधान के सहारे लिखें, वे या तो इसमें अपने संसाधन झोंकते हैं या फिर किसी सरकारी फेलोशिप का इंतज़ार करते हैं जो लगातार कम होती जा रही है और अक्सर ख़राब लेखकों को मिलती है। इस दुष्चक्र के बीच जो कुछ अच्छी किताबें लिख ली जाती हैं वह भी हिंदी की पुस्तक संस्कृति का शिकार हो जाती हैं। लेकिन क्या किताबें इस वजह से नहीं बिक रहीं कि वे अच्छी नहीं लिखी जा रहीं? अंग्रेजी के औसत पत्रकारों की औसत वैचारिक किताबें भी खूब बिक जा रही हैं। हिंदी में भी बेचने वाले बहुत सारी घटिया सामग्री बेच ले रहे हैं। जाहिर है यहां प्रकाशकों की भूमिका प्रश्नों से घिरती है। वे किताब को बाज़ार तक लाने का कोई प्रयास करते दिखाई नहीं पड़ते। वे अपने लेखक और किताब को वह प्रचार नहीं देते जिससे पाठक उस तक पहुंचे। जिस बाज़ार में लोग टूथपेस्ट तक विज्ञापन देखकर खरीदते हैं, वहां कोई किताब विज्ञापित होती नज़र नहीं आती। जबकि यह अनुभव है कि जिन किताबों को किसी भी वजह से चर्चा मिली, वे लाखों में बिकीं। तसलीमा नसरीन की ‘लज्जा’ या भीष्म साहनी का ‘तमस’ इसके सटीक उदाहरण हैं। हिंदी के प्रकाशक लेकिन अपनी किताबों की बिक्री के लिए या तो पुस्तक मेलों का इंतज़ार करते हैं या पुस्तकालयों की सरकारी ख़रीद का इंतज़ाम करते हैं।
जाहिर है, प्रकाशक यह भोला भाला दावा नहीं कर सकते कि किताबें नहीं बिकती हैं तो वे लेखकों को रॉयल्टी कहां से दें। बहुधा यह शक होता है कि वह किताबें बेचना नहीं चाहते, बस अपनी दुकान चलाए रखना चाहते हैं। इसके लिए सरकार ने उन्हें एक मुफ़ीद तरीक़ा सुझा दिया है। इसी से प्रकाशन व्यवसाय में कमीशनखोरी का खेल शुरू होता है जो सरकारी अफसरों, हिंदी अफसरों और प्राध्यापकों को भी रास आता है। इस खेल में प्रकाशक किताबों के नाम और कवर बदल बदल कर किताब बेचते पाए गए हैं। प्रकाशकों के मुंह पर दूसरा खून उन महत्वाकांक्षी अफ़सर लेखकों ने लगाया है जो लिखते चाहे जैसा हों, लेकिन पहले पैसे देकर किताब छपवाते हैं, और फिर भव्य लोकार्पण करवाते हैं और फिर पुरस्कार जुटाते हैं और फिर अपने ऊपर भी किताब लिखवा लेते हैं।
राजकमल प्रकाशन विनोद कुमार शुक्ल का कविता संग्रह भले न बेच पाया हो, लेकिन तीन साल पहले उसने एक अफसर लेखक के तीन कविता संग्रह एक साथ छापे और दो महीनों के भीतर उनके नए संस्करण प्रकाशित कर दिए। दिलचस्प ये था कि इन तीन संग्रहों में आधी कविताएं लगभग समान थीं। उनकी भूमिकाएं भी एक थीं। यह भी स्पष्ट नहीं था कि कौन सी पहली, दूसरी या तीसरी किताबें हैं। वे बस जुड़वां बहनें थीं जिन्हें जबरन प्रसव से बाहर लाया गया था। जब मैंने इस बारे में लेखक से पूछा तो उन्होंने बताया कि उन्होंने तो बस अपनी एक पांडुलिपि दी थी, उससे यह तीन किताबें तैयार कर ली गईं। जाहिर है, प्रकाशक को दो के मुकाबले तीन किताबें छापना और बेचना ज़्यादा मुनाफे का सौदा लगा होगा। कुछ दिन बाद दिल्ली के एक कॉलेज की प्रिंसिपल ने उन अफ़सर पर भी एक किताब संपादित कर दी।
लेखकों और प्रकाशकों की इस बेईमानी का खमियाजा ज़्यादातर उन नए और दूरदराज़ के लेखकों को भुगतना पड़ता है जो अच्छा लिखते हैं, लेकिन कम चर्चित हैं और चाहते हैं कि रचना के दम पर उनकी कोई किताब प्रकाशित हो। इनमें से कई लोग हताश होकर अंततः पैसे देकर अपनी किताब छपवाते हैं। कुछ साल पहले मेरी एक मित्र ने- जो मेरी नज़र में ठीक-ठाक कवयित्री हैं- मुझे बताया कि वह पैसे देकर किताब छपवाने की तैयारी में हैं। मैंने उनको मना किया- कहा कि एक लेखक को अपनी किताब इस तरह नहीं प्रकाशित करवानी चाहिए। लेकिन उनका तर्क दिलचस्प और मानवीय था। उन्होंने कहा कि जो मौजूदा प्रवृत्ति है, उसके हिसाब से उनकी रचनाओं के आधार पर उनका संग्रह कोई छापेगा, इसकी उम्मीद उन्हें नहीं है। फिर या तो वे अप्रकाशित रह जाएं या फिर पैसे देकर किताब छपवाएं। उन्होंने कहा कि उनके लिए किताब गहने की तरह है- अगर वे गहने खरीदने पर पैसे खर्च कर सकती हैं तो किताब प्रकाशित करवाने पर क्यों नहीं।
दरअसल हिंदी के तमाम प्रकाशक पैसे लेकर किताब छपते हैं, यह लगभग ‘ओपन सीक्रेट’ है। जिन प्रकाशकों को अपनी किताबें खूब बेचने के लिए जाना जाता है वह भी कई लेखकों से पैसे लेकर उनकी किताब छाप देते हैं। जब पुस्तक प्रकाशन इस दुष्चक्र का शिकार हो तो रॉयल्टी का सवाल कहां छूट जाता है, इस बारे में कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। यह सच है कि प्रकाशन व्यवसाय आसान काम नहीं है। जिन लेखकों ने प्रकाशकों के रवैये से हताश होकर अपना प्रकाशन शुरू किया, या अपनी किताबें खुद छापीं, उनका अनुभव कोई बहुत अच्छा नहीं रहा। हिंदी के मशहूर लेखक उपेंद्रनाथ ‘अश्क’ ने एक ज़माने में अपनी मायूसी में परचून की दुकान खोलने का फैसला किया था, जबकि उनके पास ‘नीलाभ’ प्रकाशन था। राजेंद्र यादव ने एक बार निजी गपशप में बताया था कि प्रकाशन का उनका अनुभव बहुत अच्छा नहीं रहा।
लेकिन इस पूरी चर्चा का एक पक्ष और है- हिंदीं भाषी समाज का पक्ष। हिंदी भाषी समाज, बांग्ला या मराठी या मलयालम बोलने वाले समाजों की तरह कभी पुस्तक प्रेम के लिए जाना नहीं गया। लेकिन आज की स्थिति ज़्यादा विकट है। पठन-पाठन की दुनिया में हिंदी एक मरती हुई भाषा है। पूरा का पूरा मध्यवर्गीय समाज अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा दिला रहा है और उनके लिए अंग्रेज़ी में किताबें खरीद रहा है। हिंदी उसके लिए बोली भर रह गई है। हिंदी के चालू अख़बारों ने इस बात को समझा है और वे बस बोलचाल की ऐसी हिंदी को अखबार की भाषा बनाकर काम कर रहे हैं जिसे अंग्रेज़ी के मुताबिक चलना है। उनके लिए अंग्रेजी के लेखक, पत्रकार और टिप्पणीकार बड़े हैं। इस स्थिति की गाज सबसे ज़्यादा हिंदी की पढ़ाई-लिखाई और हिंदी किताबों पर गिरी है। विश्वविद्यालयों में हिंदी कोई पढ़ना नहीं चाहता। दिल्ली विश्वविद्यालय में जहां किसी भी अन्य विषय के लिए 95 फ़ीसदी अंक चाहिए होते हैं, वहीं 65 फ़ीसदी अंक लाकर हिंदी में किसी भी बेहतरीन कॉलेज में दाखिला मिल सकता है।
इस स्थिति ने हिंदी साहित्य का सामाजिक दर्जा भी घटाया है। लोग शान से अंग्रेजी किताबें ख़रीदते हैं, लेकिन हिंदी किताबें ख़रीदने में हिचक जाते हैं। तमाम जगहों पर जो किताब दुकानें हैं, उनमें सिर्फ अंग्रेजी का बोलबाला है और एक आध शेल्फ हिंदी किताबों के दिखती है। तो हिंदी साहित्य मूलतः लेखकों का साहित्य रह गया है। बेशक इन लेखकों की संख्या भी पांच हज़ार से दस हज़ार या इससे भी ज़्यादा है, लेकिन वे अपनी भी किताब बांटते हैं और उम्मीद करते हैं कि दूसरे भी उन्हें अपनी किताब भेजेंगे। हिंदी का बागीचा सबको अपना लगता है और सब सोचते हैं कि अपने अमरूद कौन ख़रीद कर खाए। लेकिन दिलचस्प यह भी है कि विनोद कुमार शुक्ल का वीडियो सामने आने के बाद हिंदी के लेखकों को रॉयल्टी और अनुबंध का सवाल सता रहा है। जैसे यह प्रश्न उनके जीवन में कभी रहा ही नहीं। अब कई लोग दावा कर रहे हैं कि वह तो अग्रिम रॉयल्टी के बिना लिखते ही नहीं और ऐसी पत्रिकाओं में रचनाएं भेजते ही नहीं जो पारिश्रमिक न देती हों। निश्चय ही इन सब लेखकों को हमने तमाम जगहों पर लहालोट होते देखा है- प्रकाशकों के दरबारों में भी और पुरस्कारदाताओं के दरवाजों पर भी। दरअसल हिंदी की दीनता के ज़िम्मेदार उसके ये कामयाब लेखक भी हैं जो चापलूसी से बगावत तक को एक मुद्रा की तरह ओढ़ते हैं और हवा देखकर अपना रुख़ तय करते हैं।
बहरहाल, अनुबंध और रायल्टी के सवाल पर लौटें। हिंदी के पारिवारिक संबंधों वाली दुनिया में अनुबंध को अक्सर स्थगित की जा सकने वाली चीज़ माना जाता है। मेरी जो बारह किताबें प्रकाशित हैं, उनमें चार बिना किसी अनुबंध के हैं। बेशक, मुझे इनके लिए मामूली सी एकमुश्त राशि मिली, लेकिन इसे पेशेवर तरीक़ नहीं कहा जा सकता। जिन अनुबंधों पर अब तक मैंने दस्तख़त किए, उन्हें पूरी तरह या बहुत ठीक से नहीं पढ़ा। हालांकि इसका खमियाजा भी भुगतना पड़ा। प्रकाशकों ने बस किताब छापी, उसके प्रचार के लिए एक धेला खर्च नहीं किया, लेकिन किताब के नाट्य रूपांतरण, फिल्मांकन, ऑडियो विजुअल सारे अधिकार अपने पास रख लिए।
जब मुझे अपने उपन्यास पर वेब सीरीज के लिए एक प्रस्ताव आया तो प्रकाशक ने पहले अड़ंगा डाला और फिर अनुबंध के बाद प्रोडक्शन कंपनी से पैसे लेकर रख लिए कि छह महीने बाद हिसाब होगा। मुझे बाकायदा इसके लिए सख़्त मेल लिखना पड़ा और तब जाकर पैसे मिले। इसके बाद मैंने निश्चय किया है कि प्रकाशकों को सिर्फ किताब के प्रकाशन का अधिकार दूंगा, बाकी नहीं। बिल्कुल हाल की बात है। एक परिचित लेखिका की किताब के ऑडियो राइट्स प्रकाशक ने बिना बताए एक कंपनी को दे दिए और कई महीनों बाद लेखिका को पता चला। जब उन्होंने शिकायत की तो उनसे ऐसा जताया गया जैसे उनकी किताब छाप कर प्रकाशक ने कोई एहसान किया हो। अंततः जब उन्होंने कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी तब प्रकाशक में पैसे भी लौटाए और अनुबंध से भी हाथ खींचे।
मैंने फ्रीलांसिंग के दिनों में जम कर अनुवाद किए और उसके पैसे भी पूरे लिए। मैं खूब लिखता हूं। लेकिन मेरा यह मलाल बना हुआ है कि लिखने के लिए कितना समय देना चाहिए, वह दे नहीं पाता। क्योंकि घर चलाने के लिए मुझे नौकरी करनी पड़ती है। सिर्फ़ फ्रीलांसिंग से घर चलाना चाहूं तो वह भी कर सकता हूं। लेकिन हिंदी में पारिश्रमिक घटे हैं, लिखने की जगहें भी। इसके अलावा जो गैर पेशेवर माहौल है, उसमें किन-किन नाकाबिल लोगों को झेलना पड़े, यह ख़याल डराता है।
लेकिन क्या वाकई हिंदी की दुनिया को हिंदी लेखक या लेखन की फ़िक्र है? विनोद कुमार शुक्ल जैसे बड़े लेखक का वीडियो आता है तो उनकी बेचारगी- उचित ही- सहानुभूति और आक्रोश पैदा करती है। लेकिन क्या यह बात छुपी हुई है कि हिंदी का लेखक और अनुवादक अंततः एक गरीब प्राणी है जिसे न्यूनतम मज़दूरी तक नहीं मिलती? निश्चय ही प्रकाशक इसके अकेले ज़िम्मेदार नहीं हैं। लेकिन इसमें संदेह नहीं कि इस दुष्चक्र का सबसे ज़्यादा फ़ायदा उन्हीं को मिला है। यही नहीं, उनसे जिस पेशेवर रवैये की उम्मीद की जाती है, वह दूर-दूर तक नहीं दिखता। ज़्यादातर प्रकाशकों के यहां संपादक नहीं हैं। जो हैं उनमें काबिल लोग बहुत कम हैं।
किताबों के चयन का उनका कोई पैमाना नहीं है और किताबों के प्रकाशन की कोई डेडलाइन नहीं है। किताबें बरसों तक प्रकाशकों के पास पड़ी रहती हैं। 25 बरस से ऊपर हुए, यह शायद मनोहर श्याम जोशी या उपेंद्रनाथ ‘अश्क’ ने एक परिचर्चा में मुझसे कहा था कि हिंदी का प्रकाशक छोटा दुकानदार है जो किताबों को एक गोदाम से उठाकर दूसरे गोदाम में डाल देता है। आज की तारीख में वह आर्थिक हैसियत के लिहाज से काफी बड़ा हो चुका है, लेकिन उसे कामकाजी और पेशेवर ढंग से बदलना अभी बाक़ी है। निश्चय ही इस बदलाव में लेखकों की भी अहम भूमिका होगी।
लेकिन वह एक वरिष्ठ लेखक के वीडियो के साथ रहस्योद्घाटन वाले अंदाज़ में सोशल मीडिया पर चीख-पुकार के साथ नहीं होगी, लेखक को मासूम और प्रकाशक को खलनायक करार देने के हुंकार के साथ भी नहीं होगी, उसके लिए अपने अनुबंध और अपनी रॉयल्टी को गंभीरता से लेना होगा- सबसे ज़्यादा अपने लेखन को। जिस डिजिटल और मल्टीमीडिया युग में हम रह रहे हैं उसमें लेखक के सामने अवसर और चुनौतियां दोनों भरपूर हैं। इन्हें समझना और इनकी कसौटियों पर खरा उतरना होगा। जहां तक विनोद कुमार शुक्ल का सवाल है, फिर दोहराने की जरूरत है कि उनसे उनके प्रकाशकों को बात करनी चाहिए- उनकी शिकायत दूर की जानी चाहिए। वे ऐसे लेखक हैं जिनकी दीवार में खिड़की रहती है।
– प्रियदर्शन