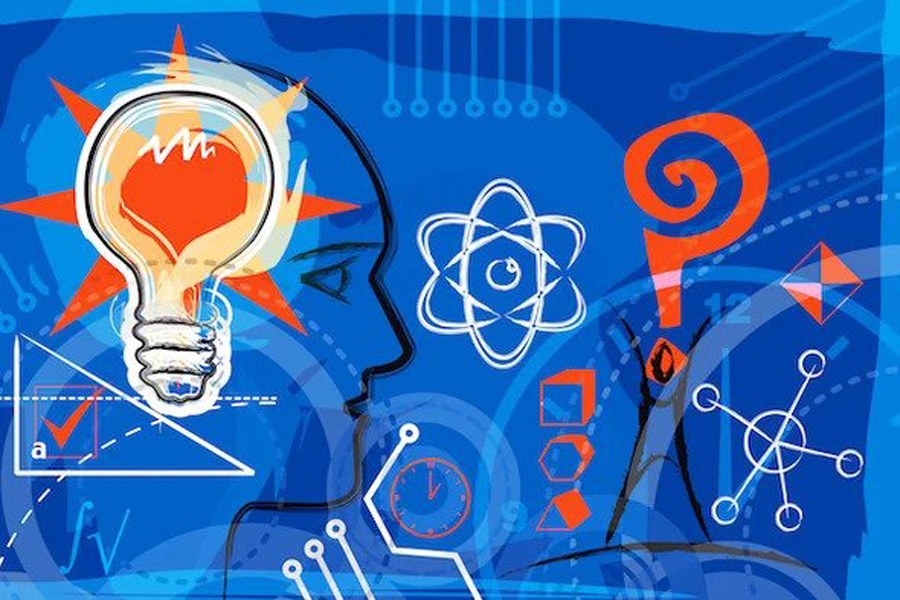उनका प्रिय सवाल आपने न सुना हो, ऐसा तो नहीं हो सकता! चाहे आप किसी भी क्षेत्र में प्रगति की बातें कर लें, ये नारेबाज गिरोह का प्रिय सवाल आएगा ही। आप मंगलयान कहेंगे तो वो पूछेंगे, इससे ग़रीब को रोटी मिलेगी क्या? आप शिक्षा के क्षेत्र में नए विषयों को जोड़े जाने की बात करें तो वो पूछेंगे, इससे ग़रीब को रोटी मिलेगी क्या? आप बुलेट ट्रेन कहें, सड़कों का निर्माण कहें, उत्तर-पूर्व में कोई पुल बनने की बात करें, कुछ भी कह लें वो हर बार पूछेंगे, इससे ग़रीब को रोटी मिलेगी क्या? उनके आपसी झगड़े भी देखेंगे तो वो सरकार के किसी फ़ैसले के समर्थन में एक भी शब्द कह बैठे अपने ही साथी को फ़ौरन ‘टुकड़ाखोर’ बुलाना शुरू कर देते हैं।
ऐसे में जब नारेबाज गिरोहों की ‘वैज्ञानिक सोच’ की बात होगी तो ज़ाहिर है कि रोटी जहाँ से आती है, उस कृषि पर ही चर्चा होगी। भारत तो वैसे भी कृषि प्रधान देश माना जाता है, इसलिए भी कृषि पर हुए ‘वैज्ञानिक शोध’ की चर्चा होनी चाहिए। हमारा ये किस्सा हमें पिछली शताब्दी के शुरुआत के दौर में आज से करीब सौ साल पहले ले जाता है। ये दौर रूस में कम्युनिस्ट शासन का ‘लाल काल’ कहा जा सकता है। इस काल में, स्टालिन के नेतृत्व में, कम्युनिस्ट शासन (शोषण) के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने वाले हज़ारों लोग गुलाग (नाज़ी कंसंट्रेशन कैंप जैसी जेलों) में फिंकवा दिए गए। मारे गए लोगों की गिनती भी लाखों में की जाती है।
इसी दौर में एक अज्ञात से तथाकथित कृषि वैज्ञानिक हुए जिनका नाम था ट्रोफिम ल्यिसेंको (Trofim Lysenko)। इन्होंने 1928 में गेहूँ उपजाने की एक नई विधि ढूँढने का दावा किया। उनका कहना था कि इस विधि से खेती करने पर उपज तीन से चार गुना तक बढ़ाई जा सकती है। इस विधि में कम तापमान और अधिक आर्द्रता वाले माहौल में गेहूँ उपजाना था। खेती से थोड़ा बहुत भी वास्ता रखने वाले जानते हैं कि नवम्बर में जब गेहूँ बोया जाता है, तब जाड़ा आना शुरू ही होता है। मार्च के अंत में इसकी फसल काटने तक, ठण्ड और आर्द्रता वाला मौसम ही होता है। ल्यिसेंको का दावा था कि ठण्ड और आर्द्रता के एक ख़ास अनुपात से पैदावार कई गुना बढ़ेगी।
ऐसे दावे करते वक्त उन्होंने विज्ञान और अनुवांशिकता सम्बन्धी जो नियम बीजों और खेती पर लागू होते, उन्हें ताक पर रख दिया। इस अनूठी सोच के विरोधियों को उन्होंने कम्युनिस्ट विचारधारा (अगर इस नाम की कोई चीज़ होती हो तो) का शत्रु घोषित करना शुरू कर दिया। अपने विरोधियों की तुलना वो साझा खेती का विरोध कर रहे किसानों से भी करने लगे। सन् 1930 के दौर में रूस खेती के नियमों को जबरन बदलने की कोशिशों के कारण खाद्य संकट के दौर से गुजर रहा था। सन् 1935 में जब ल्यिसेंको ने अपने तरीके के विरोधियों को मार्क्सवाद का विरोधी बताया तो स्टालिन भी वो भाषण सुन रहे थे। भाषण ख़त्म होते ही स्टालिन उठ खड़े हुए तो ‘वाह कॉमरेड वाह’ कहते ताली बजाने लगे।
इसके बाद तो ल्यिसेंको के तरीकों पर सवाल उठाना जैसे कुफ्र हो गया! वैसे तो ‘वैज्ञानिक सोच’ का मतलब सवालों को सुनना और विरोधी तर्कों को परखना होता है, लेकिन वैसा कुछ गिरोहों की “वैज्ञानिक सोच” में नहीं होता। लेनिन अकैडमी ऑफ़ एग्रीकल्चरल साइंसेज ने 7 अगस्त 1948 को घोषणा कर दी कि ‘ल्यिसेंकोइज्म’ को ही ‘इकलौते सही तरीके’ के तौर पर पढ़ाया जाएगा। बाकी सभी सिद्धांतों को बुर्जुआ वर्ग का और फासीवादी विचारों का कहते हुए हटा दिया गया। 1934 से 1940 के बीच कई वैज्ञानिकों को स्टालिन की सहमति से, ल्यिसेंकोइज्म का विरोधी होने के कारण मरवा दिया गया, या जेलों में फेंक दिया गया।
निकोलाई वाविलोव को 1940 में गिरफ़्तार किया गया था और कम्युनिस्ट कंसंट्रेशन कैंप में ही उनकी 1943 में मौत हो गई। गिरफ़्तार किए गए या कंसंट्रेशन कैंप में डालकर मरवा दिए गए वैज्ञानिकों में आइजेक अगोल, सोलोमन लेविट भी थे। हरमन जोसफ मुलर को अनुवांशिकता (जेनेटिक्स) पर बातचीत जारी रखने के कारण भागना पड़ा और वो स्पेन के रास्ते अमेरिका चले गए। 1948 में ही अनुवांशिकता (जेनेटिक्स) को रूस ने सरकारी तौर पर बुर्जुआ वर्ग की (फासीवादी) सोच घोषित करते हुए, ‘फ़र्ज़ी विज्ञान’ (सूडो-साइंस) घोषित कर दिया। जो भी अनुवांशिकता पर शोध कर रहे वैज्ञानिक थे, उन्हें नौकरियों से निकाल दिया गया।
इस पूरे प्रकरण में 3000 से ज्यादा वैज्ञानिकों को गिरफ़्तार किया या मार डाला गया था। उनकी नौकरियाँ छीन ली गईं और कइयों को देश से भागने पर मजबूर होना पड़ा। कहने की ज़रूरत नहीं है कि कृषि की दुर्दशा ऐसे फ़र्ज़ी विज्ञान से पूरे ल्यिनकोइज्म के दौर में जारी रही। ये सब 1953 में स्टालिन की मौत होने तक जारी रहा था। बाकी और दूसरी चीज़ों की तरह ही ‘वैज्ञानिक सोच’ के मामले में भी होता है। ‘कॉमरेड की वैज्ञानिक सोच’ का हाल काफी कुछ भस्मासुर से छू देने जैसा है। जिस चीज़ को वो छू दें, उसका समूल नाश होना तय ही है।
“You must be the change you wish to see in the world.” – Mahatma Gandhi
ये सबसे प्रसिद्ध जुमलों में से एक है | आपने भी इसे सुना ही होगा | ये अपनी तरह का इकलौता हो ऐसा भी नहीं है | ऐसी ही एक कविता कि पंक्तियाँ थी, “समता समता चिल्लाये जग, समता क्या यूँ ही आएगी, समता आती पहले भीतर, फिर बाहर भी वो आएगी” | किसने लिखी थी ये याद नहीं, बस चार लाइन ही याद रही | किसी एक ने नहीं ये कई बार कई लोगों ने कहा है |
बार बार इतने लोगों को यही बाद क्यों कहनी पड़ी ? क्योंकि भारत का बहुसंख्यक समाज इसे सुनकर अनसुना करने का अच्छा उदाहरण होता है | जैसे ही कोई दुर्घटना होती है, वैसे ही एक भीड़ इकठ्ठा हो जाती है, जिसे बस उचक कर क्या हुआ ये देखकर आगे किसी और को सुनाने के लिए आगे बढ़ जाना होता है | बिलकुल वैसे ही जब कोई सौ-पचास लोगों के धर्म-परिवर्तन करने का, पलायन कर जाने का किस्स सुनाई देता है तो ये बहुसंख्यकों की भीड़ उचक उचक कर देखना शुरू करती है क्या हुआ ? फिर जैसे भीड़ को सरकार, पुलिस, नेताओं को दोष देते हुए आगे बढ़ जाना होता है वैसे ही ये बहुसंख्यक समाज की भीड़, किसी संघ को, किन्हीं मंदिरों को, किन्हीं साधू संतों को कुछ ना करने का दोषी ठहराते हुए आगे निकलती है |
क्यों भाई ? क्यों चाहिए ये लोग तुम्हें, तुम्हारा अपना खुद का काम करने के लिए ? नौकर रखा है तुमने उन्हें कि ठेका दे रखा है कि कोई और ही करेगा ? आप तो राजा साहब हैं, खुद से जूता भी पहनने के लिए झुक जाएँ तो बेइज्जती हो जाएगी | युवराज के खुद झुककर डाटा केबल उठाने जैसा न्यूज़ बन जायेगा ? फोटो छप जाएगी अखबार में ? ऐसे इंतज़ार करते लोगों का एक बड़ा सा सवाल ये भी होता है कि मैं अकेला क्या कर सकता हूँ ? भाई आपके जैसे एक एक व्यक्ति से ही समाज बनता है | आप इन्टरनेट चला रहे हैं तो बड़ी आसानी से मुफ्त में संस्कृत के कुछ श्लोक, गीता जैसे ग्रंथों के MP3 डाउनलोड कर सकते हैं | उन्हें अपने घर में बजा सकते हैं | महीने दो महीने में ये किताबें जो कभी आपने देखी ही नहीं वो आपको याद हो जाएँगी |
एक और जो बड़ी वाली ग़लतफ़हमी है वो ये है कि संस्कृत में जो भी लिखा गया वो धर्म की किताबें हैं | ऐसा कुछ भी नहीं है | कला, नृत्य, नाटक, विज्ञान, गणित, जैसे विषयों पर लिखे ग्रन्थ 70% होते हैं और सिर्फ करीब 30% धर्म ग्रन्थ हैं | आपको ये ग़लतफ़हमी इसलिए हो जाती है क्योंकि व्याकरण, न्याय जैसे विषयों को भी कई बार वेद अध्ययन का ही एक हिस्सा माना जाता है | इसी के जरिये ये ग़लतफ़हमी फैलाई गई है कि संस्कृत में सिर्फ ब्राह्मणों द्वारा ग्रन्थ लिखे गए | आप आसानी से हर महीने ऐसे ग्रन्थ खरीदने के लिए सौ-दो सौ रुपये निकाल कर अलग कर लीजिये और किसी रविवार किसी छुट्टी के दिन उन पैसों से किताबें खरीद लाइए | किताबें आपके पास होंगी तो अपने आप ही आपके घर में दो चार लोग वापिस अपनी जड़ों से जुड़ने लगेंगे | आपके प्रयास से कम से कम आपकी अगली पीढ़ी तो बदल ही जाएगी |
पूरे परिवार में एक भी किताबें पढ़ने वाला नहीं ? कोई बात नहीं एक छोटा सा काम कर सकते हैं | पास के सरकारी स्कूल का पता वहां के प्रिंसिपल से मांग लीजिये हो सके तो बालिका विद्यालय का पता ले लीजिये | सुधर्मा नाम का संस्कृत अखबार आता है | उसका साल भर का सब्सक्रिप्शन 400 रुपये में हो जाएगा | आराम से सब्सक्रिप्शन लीजिये और भेजने के पते में स्कूल की लाइब्रेरी का पता दे दीजिये | अगर स्कूल में संस्कृत अखबार पहुँच रहा हो तो कोई ना कोई बच्चा तो पढ़ेगा ही ना ? एक पीढ़ी आगे आपने भेज दिया भाषा को | आसान तरीके इस्तेमाल कीजिये | क्या नहीं हो रहा या किसने क्या नहीं किया का रोना रोने से कहीं बेहतर है कि जो किया जा सकता है, जो आपके बस में है वो कीजिये | अब पांच सौ रुपये बचा कर स्कूल के लिए अखबार का सब्सक्रिप्शन लेने में तो दिक्कत नहीं है ना ? चंदा कैश में किसी को नहीं दे रहे इसलिए किसी किस्म के दुरुपयोग का भी खतरा नहीं !
इतना भी ये मुश्किल नहीं है जितना आप सोचते हैं | कोशिश कर के देखिये, करने से होता है | बाकी रोने से कुछ नहीं होता ये आप पहले ही जानते हैं |
“द अलकेमिस्ट” एक मशहूर किताब है और जो लोग किताबें पढ़ने का कोई विशेष शौक नहीं रखते, उनमें से भी कई लोगों ने इसका नाम सुन रखा होगा। मोटे तौर पर इसकी कहानी एक ऐसे नौजवान की है जो किसी “खजाने” की खोज में निकलता है। पूरी दुनिया का चक्कर लगाकर आने के बाद उसे पता चलता है कि असल में उसके पास खजाने को देखकर पहचान पाने का दृष्टिकोण ही नहीं था! दुनिया का चक्कर लगाने में उसने कई चीजें देखीं, काफी कुछ सीखा-समझा, फिर जब वो लौटा तो देख पाया कि जिसकी तलाश में वो भटकता फिर रहा था, वो तो असल में उसके घर में, उसके ही आँगन में पड़ा है! पक्का-पक्का कहानी में ऐसा ही नहीं होता। हाँ, कहानी का मूल, उसकी शिक्षा या सार की बात करें, तो आप इसे कहानी का सार कह सकते हैं।
वैसे भी “द अलकेमिस्ट” की कहानी बता देना मेरा उद्देश्य नहीं रहा होगा, इस बात का अंदाजा तो मेरी पोस्ट पढ़ने वाले कई लोग ऐसे ही लगा चुके होंगे। असल में हमें “अलकेमिस्ट” शब्द याद दिलाना था। पुराने ज़माने में माना जाता था कि एक धातु को दूसरे किसी पदार्थ में किन्हीं प्रक्रियाओं से बदला जा सकता है। ऐसा मानने और प्रयास करने वालों को कीमियागर भी बुलाया जाता था। इसे एक किस्म का जादू-टोना ही मानते थे। ऐसा सोचा जाता था कि “अलकेमिस्ट” पारस पत्थर जैसी कोई चीज बनाने में जुटे होते हैं। कोई ऐसी चीज जिससे छूते ही कोई भी धातु स्वर्ण में बदल जाये। ये जो जादू-टोने जैसी विद्या थी, उसी का परिशोधित रूप आज की “केमिस्ट्री” या रसायनशास्त्र है। थोड़े ही समय पहले तक #ओहसोप्रगतिशील समुदाय के लोग ऐसे “जादू-टोने” के प्रयास करने वालों को पकड़-पकड़ कर जीवित जलाया करते थे। कुछ वर्ष पहले तो चर्च ने जोन ऑफ आर्क को जीवित जलाने की माफ़ी भी माँगी थी।
पुस्तकों से निकलकर टीवी शृंखलाओं पर आयें तो एक विदेशी शृंखला है “द मेंटलिस्ट”। इसका नायक बिना पूछे ही लोगों के इतिहास, उनके जीवन की विचित्र घटनाओं के बारे में बताता रहता है। “द मेंटलिस्ट” शृंखला में वो पुलिस विभाग के साथ काम कर रहा सलाहकार होता है। उसकी वजह से कई मामले आसानी से सुलझने लगते हैं। वो जो कर रहा होता है, उसे अगर शृंखला में देख लेंगे तो आपको “कर्ण पिशाचनी” कहलाने वाली सिद्धि याद आ जाएगी। जैसे कर्ण पिशाचिनी के बारे में माना जाता है कि इसे जिसने सिद्ध कर रखा हो उसके कान में आकर ये लोगों का नाम, पारिवारिक सम्बन्ध, इतिहास आदि के बारे में बता जाती है, कुछ वैसा ही “द मेंटलिस्ट” का नायक करता हुआ दिखेगा। पूरी शृंखला देखने पर ये भी समझ आने लगता है कि इस नायक के पिता उसे इस काम के लिए कैसे बड़ी मेहनत से प्रशिक्षित करते हैं।
यू-ट्यूब पर आपको शायद “मेंटलिस्ट” ढूँढ़ने से कई ऐसा करने वाले लोगों के वीडियो भी दिख जायेंगे। जैसे कहा जाता है कि सिद्धि पाने के लिए तपस्या करनी होती है, वैसे ही “मेंटलिस्ट” बनने के लिए कितनी मेहनत लगेगी, उसका अनुमान होने लगेगा। जहाँ कई चीजें दिख रही हों, उन सबसे ध्यान हटाकर केवल एक ही व्यक्ति, जिसके विषय में जानना है, उसकी हरकतों पर, उसके पहनावे पर, बोलने के तरीके इत्यादि पर एकाग्र रहना भर भी कोई आसान काम नहीं है। फिर ये भी है कि सभी तो डॉक्टर या इंजिनियर या सीए हो नहीं सकते न? किसी को जबरन पकड़ कर क्रिकेट खेलने का खूब अभ्यास करवाया जाए, अच्छे कोच दिला दिए जाएँ, तो भी वो चौदह वर्ष की आयु में तेंदुलकर हो जाये, ऐसा आवश्यक नहीं होता। कुछ वैसे ही कर्ण पिशाचिनी की सिद्धि, क्षमा कीजियेगा, “मेंटलिस्ट” होने की योग्यता मिल भी जाये, तो कितने अच्छे “मेंटलिस्ट” होंगे, ये कहा नहीं जा सकता।
इससे पहले कि कोई ये सोचने लगे कि थोड़ी सी वैज्ञानिक सोच होने से “अलकेमिस्ट” कैसे “केमिस्ट” यानि वैज्ञानिक हो जाता है, या “कर्ण पिशाचिनी” की #ओहसोरिग्रेस्सिव “सिद्धि” बदलकर #ओहसोकूल “मेंटलिस्ट” होना हो सकता है, थोड़ा और आगे चलते हैं।
एक फिल्म आई थी “कांस्टेंटीन” जो कि ईसाइयों के तंत्र-मन्त्र, जादू-टोने पर आधारित थी। काफी सफल फिल्म थी, जो लोग “रैशनल” सोच रखते हैं, “रेशनलिस्ट” होते हैं, उन्होंने संभवतः ये फिल्म देखी होगी। बिना किसी वैज्ञानिक शोध के ही अपने पूर्वाग्रहों के आधार पर पैगन या काफिरों के सारे ज्ञान को सिरे से खारिज कर देने वाले लोगों को ये फिल्म समझ में नहीं आएगी। इस हिट फिल्म में नरक के शैतानों का धरती पर आना दिखाया गया है और फिल्म की जो नायिका होती है, वो कई तथाकथित प्रगतिशीलों की ही तरह बिलकुल “इर्रैशनल” है।
मुझसे पूछेंगे कि इस तरह की बातों में विश्वास है क्या? तो मेरा जवाब हाँ होता है। जी हाँ, बिलकुल है। आप पूछेंगे लव जिहाद में कोई जादू-टोना होता है? हम कहेंगे हाँ होता है। आप पूछेंगे बागेश्वर धाम वाले बाबा क्या बिना बताये कई बातें जान सकते हैं? हमारा जवाब है कि सिर्फ वही नहीं, कई ऐसे लोग होते हैं जो ये कर सकते हैं। आपके हिसाब से ये जादू-टोना होता है, मेरे हिसाब से बस इतना है कि इनपर ढंग से वैज्ञानिक शोध नहीं हुआ। इनपर शोध करने की बात किसी ने की भी तो उसे पोंगापंथी और रिग्रेस्सिव बताकर खदेड़ दिया गया। लव-जिहाद के मामलों में तो तो कई इर्रैशनल लोग होते हैं जो ये भी मानने को तैयार नहीं होते थे कि कोई लव जिहाद होता है। जो हमारे जैसे रैशनल लोग होते हैं, वैज्ञानिक सोच वाले लोग होते हैं, वो बिना शोध के ऐसे ही पूर्वाग्रह नहीं पालते।
बाकी बागेश्वर धाम वाले बाबा को भी जब ईसाई संतों जैसा चमत्कार दिखाने वाला बताया जाये तो पहले जरा सैंट पॉल, सैंट ज़ेवियर, सैंट फलाना इत्यादि पर शोध करके उनके चमत्कारों की जाँच कर आइये। आपके शहर के स्कूल-कॉलेज का नाम ही अगर किसी अंधविश्वास के नाम पर है, तो वहीँ से पढ़कर निकले लोगों पर “अंधविश्वासों” को न मानने की जिम्मेदारी कैसे थोप सकते हैं?
– आनन्द कुमार