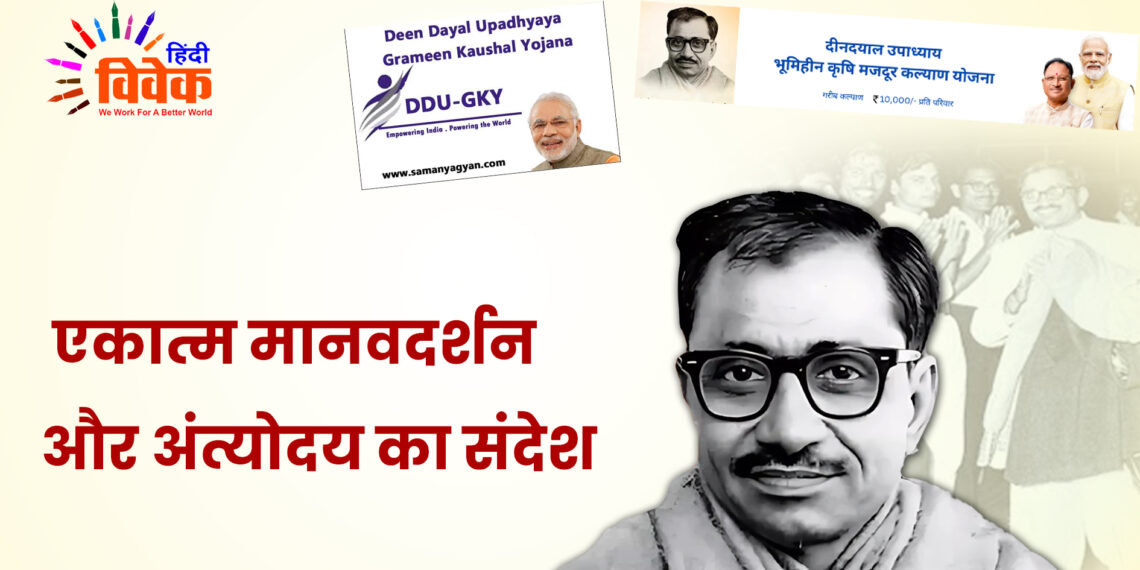‘हर पेट को रोटी’—‘हर खेत को पानी’—‘हर हाथ को काम’ ये केवल राजनीतिक नारे नहीं बल्कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जीवन-दर्शन की संक्षिप्त व्याख्या थे। उनके लिए अखंड भारत मात्र भौगोलिक एकता का प्रतीक नहीं था बल्कि भारतीय जीवन-दर्शन का आधार स्तंभ था— जहाँ विविधता में भी एकात्मता का भाव निहित है। यही दृष्टि उनके एकात्म मानवदर्शन और अन्त्योदय की आत्मा है।
जीवन: सादगी, संघर्ष और समर्पण
25 सितंबर 1916 को मथुरा जिले के नगला गाँव में जन्मे दीनदयाल उपाध्याय बचपन से ही विषमताओं से जूझते रहे। माता-पिता का साया ढाई वर्ष की आयु में और नाना-नानी का स्नेह भी शीघ्र ही छिन गया। नौवीं कक्षा में छोटे भाई शिवदयाल की मृत्यु ने मानो उनके जीवन को शोक की निरंतर छाया में ढाल दिया। फिर भी शिक्षा में उन्होंने निरंतर उत्कृष्टता प्राप्त की। कानपुर से स्नातक और आगरा के सेंट जॉन कॉलेज से अंग्रेजी साहित्य में स्नातकोत्तर किया। प्रशासनिक परीक्षा उत्तीर्ण की, किंतु धोती-कुर्ता और टोपी पहनकर दिए गए इंटरव्यू के बाद जब उन्हें “पंडित जी” कहकर संबोधित किया गया, तब भी उन्होंने सरकारी सेवा स्वीकार नहीं की। प्रधानाध्यापक का पद भी उन्होंने यह कहकर ठुकरा दिया —
“मेरी आवश्यकता केवल धोती-कुर्ते और दो समय के भोजन भर की है। इसके लिए महीने के तीस रुपये से अधिक की ज़रूरत नहीं। शेष धन का मैं क्या करूंगा?”
यही सादगी और निस्वार्थता उनके व्यक्तित्व की पहचान रही। लखनऊ में देश की परिस्थितियाँ देखकर उन्होंने संघ के कार्य में अपने को पूरी तरह समर्पित कर दिया। उनका स्पष्ट कथन था— “आज समाज हमारे सामने भीख का कटोरा लिए खड़ा है। यदि हम उसकी मांगों के प्रति उदासीन रहे, तो एक दिन हमें अपने जीवन और कार्यों का बहुत बड़ा मूल्य चुकाना होगा।”
1939 व 1942 के संघ प्रशिक्षणों के बाद वे संगठन में सक्रिय हुए। 1955 में प्रांतीय आयोजक बने। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जब जनसंघ का गठन किया तो दीनदयाल की क्षमता से प्रभावित होकर कहा —“अगर मुझे दो दीनदयाल मिल जाएँ, तो मैं भारतीय राजनीति का नक्शा ही बदल दूँ।”
1953 में मुखर्जी जी के निधन के बाद दीनदयाल जी ने जनसंघ की बागडोर संभाली। 1965 का ‘दिल्ली चलो’ अभियान और 1967 में अध्यक्ष पद पर आसीन होना उनके राजनीतिक जीवन की बड़ी उपलब्धियाँ रहीं। 11 फरवरी 1968 को मुगलसराय स्टेशन पर उनका रहस्यमय निधन हुआ। वे राष्ट्रधर्म, पाञ्चजन्य, स्वदेश जैसी पत्रिकाओं के संपादक और सम्राट चंद्रगुप्त, जगद्गुरु शंकराचार्य जैसी कृतियों के लेखक भी रहे।
एकात्म मानवदर्शन: भारतीय दृष्टि का प्रतिपादन
दीनदयाल उपाध्याय ने पूंजीवाद और समाजवाद दोनों को भारतीय समाज के लिए अनुपयुक्त माना। उनका मत था कि पश्चिमी व्यक्तिवाद ने परिवारों को खंडित कर दिया है, जबकि भारत में व्यक्ति, परिवार, समाज और राष्ट्र एक-दूसरे के पूरक हैं। उनका उद्घोष था— “व्यक्ति परिवार के बिना अधूरा है; परिवार समाज के बिना, समाज राष्ट्र के बिना और राष्ट्र विश्व के बिना अधूरा है। सम्पूर्णता ही जीवन का लक्ष्य है।”
उनका दर्शन मानव को केवल जैविक प्रवृत्तियों— आहार, निद्रा, भय और मैथुन — तक सीमित नहीं करता बल्कि उसे शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा के एकात्म संयोजन के रूप में देखता है। जीवन के चार पुरुषार्थ — ‘धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष’ का संतुलन ही भारतीय जीवन-दर्शन है।
वे डार्विन के Survival of the Fittest का खंडन करते हुए कहते थे- “भारत में संघर्ष नहीं, सहयोग; प्रतिस्पर्धा नहीं, समन्वय है।” उनका सूत्र — “यत् पिण्डे तत् ब्रह्मांडे”— स्पष्ट करता है कि मनुष्य और ब्रह्मांड का संबंध एकात्मक है। यही विचार उनके अन्त्योदय के सिद्धांत की नींव बना।
शिक्षा का दृष्टिकोण: ‘सा विद्या या विमुक्तये’
उनका मत था कि शिक्षा का उद्देश्य केवल रोजगार या ज्ञानार्जन नहीं बल्कि मुक्ति और संस्कार है। विद्यालय ऐसे हों जो राष्ट्रप्रेम, मातृभाषा और संस्कृति के प्रति गौरव का भाव उत्पन्न करें। विद्यार्थियों को पंच लक्षणों— काक चेष्टा, वको ध्यानम, स्वान निद्रा, अल्पहारी और गृहत्यागी— से युक्त होना चाहिए। शिक्षक चरित्रवान और त्यागमयी हों, जो सीमित संसाधनों में भी उत्कृष्ट शिक्षा दे सकें। वे मानते थे कि शिक्षा केवल ग्रंथ-आश्रित नहीं बल्कि अनुभव आधारित भी होनी चाहिए। स्वाध्याय और जीवनपर्यंत शिक्षा को उन्होंने अत्यंत आवश्यक बताया।
राष्ट्र, संस्कृति और चिति
दीनदयाल जी ने स्पष्ट किया कि राष्ट्र केवल भूखंड नहीं, बल्कि संस्कृति का जीवंत स्वरूप है। भूमि, जन और संस्कृति के संगम से राष्ट्र बनता है। संस्कृति उसका शरीर है, चिति उसकी आत्मा और विराट उसका प्राण। उन्होंने कहा—“हमारी राष्ट्रीयता का आधार भारत माता है। केवल भारत नहीं। यदि ‘माता’ शब्द हटा दें, तो यह मात्र जमीन का टुकड़ा रह जाएगा।”
एकात्म मानवदर्शन और प्रकृति
उनके अनुसार मानव, पशु और पादप सब एक जैविक समुदाय के अंग हैं। उन्होंने कहा- “प्रकृति आप हमारी माँ हैं; आप हमारा पोषण करती हो।” इसलिए पर्यावरण-संरक्षण और संतुलित उपभोग उनके दर्शन के अभिन्न तत्व थे। ऋग्वेद के मन्त्र “आ नो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतः” (सभी ओर से कल्याणकारी विचार आएं) से सहमत थे, किंतु चेताते थे कि अपनी जड़ों से कटकर विचारों को अपनाना आत्मविनाश का कारण बनेगा।
अन्त्योदय: अंतिम व्यक्ति तक विकास
उनका सबसे बड़ा योगदान था अन्त्योदय— विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँचना चाहिए। उनका उद्घोष था- “सब में बाँटो, कोई भूखा न रहे।” वे कहते थे कि ‘अनपढ़ और मले-कुचले लोग ही हमारे नारायण हैं’। भारतीय संस्कृति में यह भाव निहित है— “सो हाथों से कमाओ और हज़ार हाथों से बाँटो।”
क्यों उनके जन्मदिवस को अन्त्योदय दिवस कहा जाता है,
अन्त्योदय उनके जीवन-दर्शन का मूल था।
उनका व्यक्तित्व और कर्म सादगी, सेवा और संगठन का जीवंत उदाहरण रहे।
यह दिवस समाज को स्मरण कराता है कि नीति और योजनाओं का केन्द्र अंतिम व्यक्ति होना चाहिए।
अन्त्योदय दिवस केवल स्मरण नहीं बल्कि सेवा-संकल्प का अवसर है।
हमें क्या करना चाहिए — व्यवहारिक सुझाव
शिक्षा को राष्ट्रचेतना और संस्कारों से जोड़ना।
योजनाओं में ‘अंतिम व्यक्ति’ की पहुँच को प्राथमिकता देना।
परिवार और समाज के मूल्यों को सुदृढ़ करना।
स्थानीय संगठनों और स्वयंसेवा को सक्रिय करना।
राजनीति में सेवा-निष्ठ नैतिकता और पर्यावरण-अनुकूल विकास पर बल देना।
जन्मदिवस पर प्रत्यक्ष सेवा-कार्य करना।
दीनदयाल जी के विचारो की प्रासंगिकता
आज़ादी तभी सार्थक है जब यह हमारी संस्कृति की अभिव्यक्ति का साधन बने।
एकात्म मानवदर्शन सामाजिक मतभेदों को मिटाने में सहायक है।
यह भारतीय मूल्यों को पुनर्जीवित करने और उपभोक्तावाद से मुक्ति का मार्ग है।
अधिकार और स्वतंत्रता के संतुलन से संघर्षों को कम किया जा सकता है।
अन्त्योदय आज भी कल्याणकारी योजनाओं का नैतिक मार्गदर्शक है।
एकता, अखंडता, सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण उनके विचारों में अंतर्निहित हैं।
दीनदयाल जी का व्यवहारिक संदेश — अर्थव्यवस्था और समाज
व्यक्ति प्रारंभिक इकाई है, किंतु व्यापक हित के लिए त्याग उसका धर्म है।
अर्थव्यवस्था सदैव राष्ट्रीय जीवन और प्रकृति के अनुकूल होनी चाहिए।
बच्चों, बुजुर्गों और रोगियों की देखभाल समाज की जिम्मेदारी है; प्रत्येक व्यक्ति को जन्म से भोजन का अधिकार है।
आश्रित मानसिकता के स्थान पर आत्मनिर्भरता और जिम्मेदारी को बढ़ावा देना चाहिए।
कालीकट अधिवेशन में दीनदयाल जी का उद्घोष
“हम किसी विशेष समुदाय या वर्ग की नहीं बल्कि पूरे देश की सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हर देशवासी हमारे खून का खून है और हमारे मांस का मांस। हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक हम उनमें से हर एक को यह गर्व की भावना न भर दें कि वे भारतमाता की संतान हैं। हम भारत माता को सुजला-सुफला शब्दों के वास्तविक अर्थ में बनाएंगे; दुर्गा के रूप में वह बुराई का नाश करेगी, लक्ष्मी के रूप में सर्वत्र समृद्धि देगी और सरस्वती के रूप में वह अज्ञानता का अंधकार दूर करेगी। परम विजय के विश्वास के साथ आइए, हम अपने को इस कार्य के लिए समर्पित करें।”
— पंडित दीनदयाल उपाध्याय, कालीकट अधिवेशन
पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जीवन और दर्शन केवल बीते युग की स्मृति नहीं है बल्कि आज और आने वाले कल का मार्गदर्शक है। उनका एकात्म मानवदर्शन हमें यह सिखाता है कि विकास केवल आँकड़ों या सकल घरेलू उत्पाद से नहीं मापा जा सकता; वह तब सार्थक है जब व्यक्ति की आत्मा, परिवार की गरिमा, समाज का कल्याण और राष्ट्र की संस्कृति सब मिलकर प्रगति करें।
उनका अन्त्योदय हमें स्मरण कराता है कि जब तक समाज का अंतिम व्यक्ति प्रसन्न और सुरक्षित नहीं होगा, तब तक राष्ट्र की प्रगति अधूरी रहेगी। यही वह संदेश है जो उन्हें आज भी प्रासंगिक और कालजयी बनाता है।
– दीपक द्विवेदी