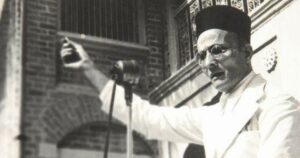
आदि काल से ही भारतीय संस्कृति, इसके मूल्य एवं इसकी व्यावहारिकता दुनिया को दिशा प्रदान करते रहे हैं। यद्यपि, यह सत्य है कि एक सामूहिक चेतना ने इतिहास की धारा को परिवर्तित किया एवं समाज की बेहतरी का मार्ग प्रशस्त किया, किंतु कुछ व्यक्तित्व इतने प्रभावशाली रहे एवं उनकी दृष्टि इतनी सारगर्भित रही कि उससे आज भी समाज को एक नई दिशा मिलती है। मुझे यह स्वीकारने में कोई संकोच नहीं है कि ऐसे व्यक्तित्वों को में से कुछ को हमारे इतिहासविदों ने समुचित महत्व नहीं दिया। वीर विनायक दामोदर सावरकर एक ऐसे ही व्यक्तित्व थे जिनमें अभूतपूर्व वैचारिक मतांतर के बावजूद अपनी मौलिक विशिष्टता का लोहा मनवाने की क्षमता थी। अब जब राष्ट्र सावरकर की 137वीं जयंती मना रहा है, इस यशवंचित नायक के आदर्शों को अधिक गहराई और व्यापकता से समझना उपयुक्त होगा।
ऐतिहासिक दृष्टि से, यह तथ्य उल्लेखनीय है कि वीर सावरकर एक चितपावनी ब्राह्मण थे जबकि डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर समाज के निम्न वर्ग का प्रतिनिधित्व करते थेे, फिर भी हमें उनके विचारों में समानता देखने को मिलती है जिसपर इतिहास बहुधा मौन रहा। ऐसे कई अवसर आए जब दोनों ने भारत के बारे में अपनी अवधारणा एक साथ सामने रखी। वस्तुतः सावरकर डॉ. बी.आर. आम्बेडकर की अंतर्दृष्टि और मौलिक विचारधारा से काफी प्रभावित थे। सावरकर सामाजिक सुधारों, भाईचारे और दलितों के उत्थान के लिए अपने विचार रखते समय डॉ. आम्बेडकर की राय का हवाला अक्सर दिया करते थे। उनका मत था कि हर सच्चे भारतीय को सात बेड़ियों से मुक्त होना होगा। ये बेड़ियां थीं- वेदोक्तबंदी अर्थात् वैदिक साहित्य को चंद लोगों के लिए सीमित रखना, व्यवसायबंदी अर्थात किसी समुदाय विशेष में जन्म के कारण उस समुदाय के पारम्परिक व्यवसाय को जारी रखने की बाध्यता, स्पर्शबंदी अर्थात् अछूत प्रथा, समुद्रबंदी यानी समुद्री मार्ग से विदेश जाने पर प्रतिबंध, शुद्धिबंदी अर्थात् हिंदू धर्म में फिर से लौटने पर रोक, रोटीबंदी अर्थात दूसरी जाति के लोगों के साथ खानपान पर प्रतिबंध और बेटीबंदी अर्थात् अंतर्जातीय विवाह समाप्त करने संबंधी अड़चनें। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इन सुधारवादी विचारों को हमारे संविधान में भी सम्मिलित किया गया।

हिंदू समाज की इन्हीं बेड़ियों के परिप्रेक्ष्य में, सावरकर कहते हैं-“जिस महार जाति को निम्न जाति समझा जाता है, उसी ने हमें चोखा मेला जैसे दिव्य संत और डॉक्टर आम्बेडकर जैसे असाधारण चिंतक दिए जिनकी धर्मपरायणता और बौद्धिकता कई ब्राह्मणों से कहीं अधिक है।”
व्यवसायबंदी के बारे में डाॅ. अम्बेडकर को इंगित करते हुए उन्होंने अपने विचार रखते कि यह व्यक्ति की अपनी इच्छा, क्षमता और रुचि पर निर्भर करता है कि वह कौन सा व्यवसाय करे- चाहे उसका जन्म किसी भी जाति में हुआ हो।
वस्तुतः, सावरकर जाति-प्रथा के प्रबल विरोधी थे। सावरकर उन थोड़े व्यक्तियों में से थे जो जातिविहीन भारत की सोच रखते थे। उन्होंने अपने समर्थकों को सनातन धर्म की जाति व्यवस्था से प्रति आगाह किया था। उनका विचार था कि सनातन का अर्थ ऐसे विचारों और विश्वासों से है जो अनंत काल से चले आ रहे हैं जिन्हें स्वयंसिद्ध और अटूट मान लिया गया है। उन्होंने लिखा- “सनातन की इस अमूर्त धारणा को देखते हुए इसे धर्म से मनमाने तरीके से जोड़ना और फिर उसे मनुष्य के द्वारा बनाए रीति-रिवाजों और प्रथाओं का हिस्सा बताना सनातन सत्य से मुंह मोड़ना है। हम जाति प्रथा जैसी सामाजिक परम्पराओं अथवा विधवा विवाह के विरोध को अटूट अथवा सनातन सत्य कैसे बता सकते हैं जबकि ये धीरे-धीरे हमारे समाज का हिस्सा बने हैं? इन्हें तुरन्त समाप्त किया जा सकता है और इसलिए इन्हें “सनातन” का अभिन्न अंग नहीं माना जा सकता।”
सावरकर ने साफ शब्दों में कहा कि सामाजिक खाई को पाटने के लिए इन बेड़ियों को तोड़ना जरुरी है। उनकी स्पष्ट राय थी कि “अपने ही देश के लाखों लोगों को पशुओं से भी बदतर दर्जे में रखकर हमने नितान्त अमानवीय कार्य किया है। यह कैसी व्यवस्था है जिसमें किसी कुत्ते या पालतू पशु की पीठ थपथपाना तो आपको ठीक लगता है लेकिन आम्बेडकर जैसे विद्वान से हाथ मिलाना आपको अपनी जाति गंवाने जैसा मालूम पड़ता है? क्या यह आपको अतर्कसंगत नहीं लगता? यही कारण है कि जिन लोगों ने चतुर्वर्ण व्यवस्था को नष्ट कर अछूतों के रुप में पांचवे वर्ण को जन्म दिया, आज वही कह रहे हैं कि इस प्रथा के समाप्त होने से सनातन धर्म खतरे में पड़ जाएगा। इससे बड़ी विडम्बना भला क्या हो सकती है?”
सावरकर ने सामाजिक चेतना के विकास के लिए तर्कों पर लगातार जोर दिया। उनके विचारों के कारण कई लोग मनुष्यता संबंधी विरोधाभासी विचारों का परित्याग करने को बाध्य हुए। 1920 में अपने भाई नारायण राव को लिखे एक पत्र में वे जाति आधारित असामनता एवं भेदभाव के विषय में स्पष्टता से अपने विचार रखे हैं ‘‘मैं महसूस करता हॅंू कि जितना आवश्यक भारत पर विदेशी आधिपत्य के खिलाफ लड़ना है उतना ही आवश्यक जातिगत भेदभाव एवं अस्पृश्यता से लड़ना है।‘‘ सेल्युलर जेल से छुटने के बाद उन्होंने रत्नागिरि को अपना कार्यक्षेत्र बनाया और भारत में एक शक्तिशाली समाज सुधार का कार्यक्रम शुरू किया। 1931 में उन्होंने पतित-पावन मंदिर का निर्माण किया एवं दलितों सहित सभी हिन्दुओं के प्रवेश को अनुमति दी और सामुदायिक सहभोज का भी आयोजन किया। 1931 में ही उन्होंने पेठकिला, रत्नागिरि में एक मंदिर के उद्घाटन के लिए डाॅ0 अम्बेडकर को आमंत्रित किया था। 14 अप्रैल 1942 को डा0 अम्बेडकर के 50वें जन्मदिवस पर सावरकर अपना विशेष संदेश उन्हें प्रेषित करते हैं – ‘‘अपने व्यक्तित्व, विद्वता, संगठन कौशल और नेतृत्व क्षमता से डाॅ0 अम्बेडकर आज देश के मुख्य आधार स्तंभ बन गए हैं, लेकिन अस्पृश्यता उन्मूलन में उनकी सफलता और उस समाज में आत्मविश्वास की भावना रहना भारत के लिए उनकी महान सेवा है। उनका कार्य शाश्वत और मानवतावादी है जो प्रत्येक देशवासी में गौरव की भावना भरता है।”
वीर सावरकर ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1857 के विद्रोह को भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम की संज्ञा दी थी। उन्होंने अपनी पुस्तक ‘‘1857 का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम‘‘ में इसे स्वतंत्रता के लिए प्रथम युद्ध की संज्ञा दी। वे ऐसे पहले राजनेता थे जिन्होंने 1900 के दशक में ही भारत को स्वतंत्र करने का लक्ष्य निर्धारित किया था। कॉलेज में प्रवेश के लगभग तुरन्त बाद से ही उन्होंने अपनी वाक्पटुता और लेखन-कला की बदौलत अंग्रेजों के विरोध में लोगों को संगठित करना और अपने क्रांतिकारी विचारों के प्रसार का काम शुरु कर दिया था। जबकि कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता के लक्ष्य को बहुत बाद में, 1929 के लाहौर अधिवेशन में स्वीकार किया। 1910 में उनका फ्रांस तट के निकट ब्रिटिश जहाज से कूदकर भागने का प्रयास उनके साहस एवं प्रतिबद्धता को प्रमाणित करता है। यहां यह जानना भी रोचक है कि लगभग एक सदी पहले, वो सावरकर ही थे, जिनके कारण उस समय की दो उपनिवेशवादी शक्तियों ब्रिटेन एवं फ्रांस को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के साथ हेग में स्थित मध्यस्थता के स्थाई कोर्ट में जाने को विवश होना पड़ा।
अपने असाधारण कार्यों के जरिए उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए लंदन एवं यूरोप के अन्य भागों में भी बहुत से बहादुर युवाओं को प्रेरित किया एवं नेतृत्व प्रदान किया।
सावरकर के सपनों का भारत विविधताओं से भरा एक ऐसा एकीकृत भारत था जिसमें सभी संस्कृतियों के लिए स्थान था। वे महसूस करते थे कि समावेशिता की भावना से ही भारतीय जन-मन को आंदोलित किया जा सकता है। दुर्भाग्यवश, कुछेक विरोधियों ने 1937 में अहमदाबाद के कर्णावती में हिंदू महासभा के 19वें सत्र में सावरकर के अध्यक्षीय संबोधन के कुछेक हिस्सों का हवाला देकर उन्हें द्विराष्ट्र सिद्धांत का समर्थक बता दिया, जो कि सत्य से परे है। 1939 में कलकत्ता में हिंदू महासभा के 21वें सत्र में सावरकर ने अपने अध्यक्षीय संबोधन में स्पष्ट रूप से कहा कि हिंदू और मुसलमान अपने ऐतिहासिक मतभेदों को भुलाकर ही हिंदुस्तानी की साझा भावना से संवैधानिक देश बना सकते हैं।
तथापि, 15 अगस्त, 1943 को उन्होंने नागपुर से प्रकाशित मराठी साप्ताहिक ‘आदेश‘ के कार्यालय में पत्रकारों से अपने वक्तव्य को स्पष्ट करते हुए कहाः
“राष्ट्र और राज्य की अवधारणा को लेकर कोई भ्रम की स्थिति नहीं रहनी चाहिए। राज्य न रहे,तो भी राष्ट्र का अस्तित्व बना रहता है। जब हम पर मुसलमान शासक राज कर रहे थे, तब सरकार यानी राज्य उनके मातहत होते थे। किंतु, हिंदुओं का अस्तित्व तब भी अक्षुण्ण रहा। इसके बावजूद, हिंदुओं ओर मुसलमानों के साझा राज्य में भी कोई समस्या नहीं है। पहले भी कई राष्ट्र रहे हैं, जैसे- महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, देवराष्ट्र (बिरार के पास)। अब ये राष्ट्र कहां हैं? वे सब एक-दूसरे में मिल गए……इसलिए, अगर मुसलमान चाहें तो वे वे अल्पसंख्यक समुदाय के रुप में हिंदुओं के साथ सहजता से रह सकते हैं………..हिंदुस्तान में मुसलमानों के संबंध में यह कहा जा सकता है कि आप हिंदू लोग तो उन्हें अपने साथ रखना चाहते हैं लेकिन क्या मुसलमान भी ऐसा चाहते हैं? अंततः, किसी भी राष्ट्र की अहमियत उसकी आकांक्षा की बदौलत ही होती है।”
वस्तुतः यह सावरकर नहीं बल्कि सर सैयद अहमद खाॅं थे जिन्होंने द्वि-राष्ट्र सिद्धांत को प्रतिपादित किया और बाद में जिसे जिन्ना ने अपना हथियार बनाया। यहां 14 मार्च,1988 को मेरठ में सर सैयद अहमद खाॅं के संबोधन का जिक्र करना आवश्यक है क्योंकि यहीं उन्होंने द्विराष्ट्र के सिद्धांत की बात थी जिसके परिणाम आगे चलकर भारत के लिए विनाशकारी सिद्ध हुए। सर सैयद अहमद खाॅं ने अपने सार्वजनिक संबोधन में कहा था- “भारतीय साम्राज्य का प्रशासन किनके हाथों में होगा? मान लीजिए, सभी अंग्रेज और उनकी सेना अपने सभी कायदे-कानून, हथियार और अपनी बाकी सारी चीजें लेकर भारत से लेकर विदा हो जाए, तो भारत का शासन किनके हाथों में आ जाएगा? क्या ऐसे में, यह संभव है कि मुसलमान और हिंदू दोनों सत्ता में साथ-साथ रहें और उनके हाथों में शक्तियां भी एक जैसी हों? निश्चय ही, ऐसा संभव नहीं होगा। दोनों में से एक यह जरुर चाहेगा कि वह दूसरे को अपने मातहत रखे। यह सोचना कि दोनों एक समान रह सकते हैं, एक असंभव और अकल्पनीय आकांक्षा है।”
मई 1952 में, सावरकर यह घोषणा करने के लिए पुणे गए कि 1904 में गठित गुप्त क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत को बंद किया जा रहा है जिसकी स्थापना उन्होंने स्वतंत्रता संघर्ष के लिए अपने छात्र जीवन में की थी। इस संगठन के विघटन की सार्वजनिक रुप से घोषणा करते समय उन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर के इस विचार पर जोर दिया कि संवैधानिक व्यवस्था में क्रांतिकारी संगठनों के लिए कोई जगह नहीं होती।
भारतीय समाज को विभाजित करने की मंशा से कांग्रेस और वाम दलों ने राजनीतिक लाभ के लिए ऐसे अनमोल रत्न पर विरोधाभासी आरोप लगाए, लेकिन ऐसा करते हुए वे यह भूल गए कि सावरकर से जुड़े शताब्दी आयोजनों के दौरान इंदिरा गांधी ने क्या कहा था। स्वातंत्र्य वीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारक के सचिव पंडित बाखले को 20 मई, 1980 को लिखे पत्र में उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भारत के इस सपूत के अमिट योगदान की चर्चा करते हुए कहा था कि स्वाधीनता संघर्ष में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध वीर सावरकर के साहसिक प्रयासों के प्रति उनके मन में बड़ा सम्मान है।
सावरकर मशीन-आधारित अर्थव्यवस्था के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने कहा था कि भारतीय नेताओं को यूरोपीय गलतियों से सबक लेने की जरुरत है। भारतीय सिनेमा के प्रति उनकी भविष्य की दृष्टि प्रशंसनीय थी। वे मानव मन की नवोन्मेषी प्रवृत्ति में विश्वास रखते थे। वे एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्तित्व थे यथा – स्वतंत्रता सैनानी, समाज-सुधारक, लेखक, कवि, इतिहासकार, राजनैतिक नेता और दार्शनिक। उथली समझ पर आधारित दुर्भावनापूर्ण इतिहास लेखन से सावरकर की छवि विवादास्पद बना दी गई है।
आधुनिकता, सामाजिक और धार्मिक सुधारों, वैज्ञानिक चेतना के विकास और तकनीक को अपनाने के संबंध में सावरकर के विचार कोरोना संकट के बाद नए भारत के निर्माण की दृष्टि से आज भी प्रासंगिक बने हुए हैं। नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार भारत के ऐसे महान सपूतों के संगत विचारों से प्रेरणा लेकर ही एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण के लिए कदम उठा रही है। आज वीर सावरकर की जयंती पर देशभक्ति के उनके जज्बे और उनके उल्लेखनीय योगदान का स्मरण ही भारतीय इतिहास की इस महान क्रांतिकारी चेतना के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि होगी।
लेखक – श्री अर्जुन राम मेघवाल- केंद्रीय राज्यमंत्री-ं संसदीय कार्य मंत्रालय और भारी उद्योग तथा लोक उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार तथा लोकसभा में बीकानेर से सांसद




भाईसाहब को सादर प्रणाम.
एक नये आलोक में आपका यह मनोगत, बहुत से अनछुए पृष्ठों को खोलनेवाला तथा समाज को नयी दिशा देने वाला सिद्ध होगा,ऐसी आशा है, और यदि ऐसा होता है,तो यह,उस नरश्रेष्ठ को सर्वश्रेष्ठ श्रद्धांजली होगी.
हमें गर्व है,कि केन्द्र सरकार में आप हमारे प्रतिनिधी हो.सादर.