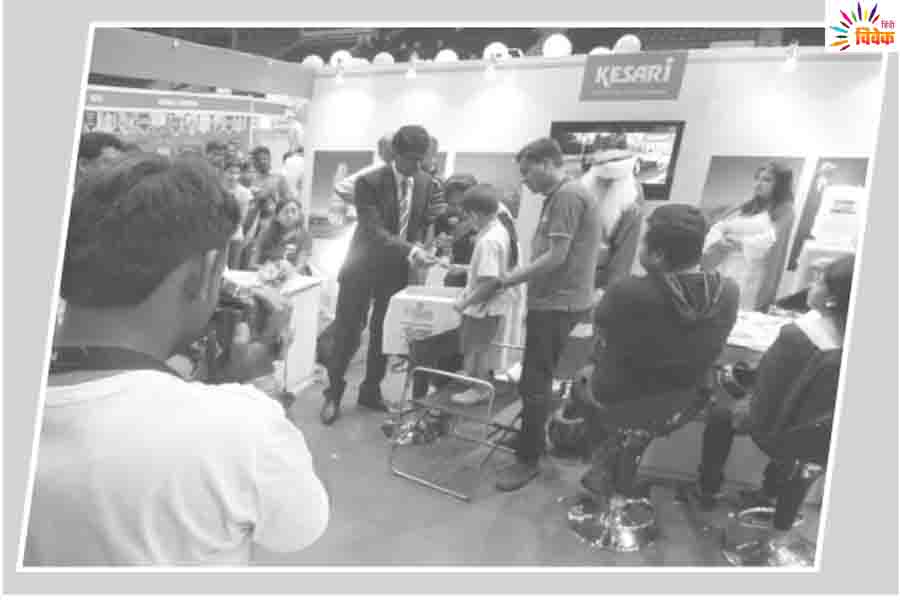किया जाता है, वे शक्तियां वास्तव में शब्दों की शक्तियां ही हैं। लेकिन मंत्रों में निहित शब्दों की शक्ति का अनुभव पाने के लिये मंत्रों को, अर्थात शब्दों को स्वयंसिद्ध अनंत शक्ति के प्रत्यक्ष प्रभाव का अनुभव हमें यदि किन्हीं शब्दों ने दिया है, तो वे शब्द हैं- ‘वंदे मातरम् !’ मात्र दो शब्द, छह अक्षर। लेकिन अनंत शक्ति के वाहक। हजारों परमाणु बमों के मालिक चीन या अमेरिका के किसी भी व्यक्ति के हृदय में उन बमों की उपस्थिति उतनी ऊर्जा के अणुमात्र अंश की अनुभूति नहीं भर सकती, जितनी किसी भी भारतीय के हृदय में मात्र इन दो शब्दों की बिजली सी कौंध-‘वंदे मातरम्!’
भारतीय स्वाधीनता संग्राम में जिन क्रांतिकारी महिलाओं के नाम उनके अदम्य साहस और अदभुत बलिदान की वजह से स्वर्णाक्षरों में लिखे रहेंगे, उनमें एक प्रमुख नाम है मांतगिनी हाजरा। बंगला की इस वीरांगना को जब अंग्रेजों की गोली लगी, तो मातृभूमि के लिए प्राणों की आहूति देते हुए मातंगिनी के होठों से जो अंतिम शब्द मंत्र की तरह उच्चारित हुए, वे थे ‘वंदे मातरम !’ स्वाधीनता संग्राम में ‘वंदे मातरम’ का यह पहला उद्घोष था। इसके बाद तो कितने ही क्रांतिकारियों ने ‘वंदे मातरम!’ का उद्घोष करते हुए गोलियां खायीं, फांसी के फंदों को गले लगा लिया। आज़ादी चाहने वाले भारत के बच्चे-बच्चे के होठों पर एक ही मंत्र था ‘वंदे मातरम!’ कांग्रेस के नरम दल, गरम दल, तमाम सशस्त्र क्रांति के वीर, बंगाली, पंजाबी, मराठी, उत्तर भारतीय, दक्षिण भारतीय सबके हृदयों से एक ही आवाज निकलती थी-‘वंदे मातरम्!’
अंग्रेजों के लिए आतंक बन गये थे ये दो शब्द! अघोषित पाबंदी लगा दी गयी थी। ये शब्द नहीं थे, शोले थे, जिनकी तेज आंच से अंग्रेजों का मनोबल बुरी तरह झुलस जाता था, लेकिन फिर यही दो शब्द थे जो आज़ादी के लिए प्राणों की आहुति देने वाले क्रांतिवीरों की मृत्य-पीड़ा को शीतलता प्रदान करते थे। सुभाषचंद्र बसु की ‘आजाद हिंद फौज’ के सिपाही ‘वंदे मातरम’ गा-गाकर ही शहीद होते थे।
‘वंदे मातरम’ की रचना के 136 साल गुजर गये। आजादी के 64 साल गुजर गये। ‘वंदे मातरम्’ की शक्ति है कि निरंतर बढ़ती ही जाती है। आज भी जनसाधारण किसी भी अवसर पर जब राष्ट्रीय भावनाओं से उद्वेलित होता है, भावुक होकर, उत्तेजित होकर प्राणपण उद्घोष करता है-‘वंदे मातरम्!’
आइये, ‘वंदे मातरम्’ के संक्षिप्त इतिहास से गुजरते हुए एक बार फिर अपनी शिराओं में हम राष्ट्रभक्ति की प्रचंड ऊर्जा का संचार कर लें।
भारतीय साहित्य के अमर उपन्यासकार, बांग्ला साहित्यकार श्री बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय (जन्म 27, जून सन् 1838, मृत्यु: 8 अप्रैल 1894) बड़े परेशान थे। कोलकाता विश्वविद्यालय के प्रथम दो स्नातकों में से एक बंकिमचंद्र डिप्टी मजिस्ट्रेट थे, यानी उन दिनों के पराधीन भारत की गोरी सरकार के वेतनभोगी कर्मचारी। गोरी सरकार उस वक्त अपने राष्ट्रगीत ‘गॉड सेव द क्वीन’ को भारतीयों पर भारत के राष्ट्रगीत के रूप में थोपने की तैयारी कर रही थी। बंकिम इसी बात को लेकर परेशान थे। परेशानी के ही आलम में उन्होंने एक बंगाली कीर्तनकार को कीर्तन गाते हुए सुना-‘एशो एशो बंधु, मायेर आंचले बोशो’ (आओ आओ बंधु, मां के आंचल तले बैठो।)
कीर्तन में देवी दुर्गा को ‘मां’ कहा जा रहा था। दुखी बंकिम के मन में कीर्तन सुनते हुए दुर्गा की जगह बार-बार भारत माता का चित्र उभर कर आता था। मन ही मन उन्होंने भारत को मां दुर्गा का रूप दे दिया। डिप्टी मजिस्ट्रेट के पद पर रहते हुए तो वह अंग्रेजों की साजिश का जवाब दे नहीं सकते थे, इसलिए ‘गॉड सेव द क्वीन’ के जवाब में उन्होंने भारत माता को मां दुर्गा के रूप में कल्पना करते हुए राष्ट्रगीत के तौर पर मातृवंदना लिख डाली-‘वंदे मातरम्।’
बंकिम की शिक्षा अंग्रेजी में हुई थी, लेकिन वे संस्कृत के विद्वान थे, बांग्ला के तो प्रकांड विद्वान थे ही। लेकिन वे गद्यकार थे, कवि-गीतकार नहीं, जबकि दुखी और भावुक मन में मातृवंदना के रूप में कोई गीत ही मचल रहा था। गीत ‘वंदे मातरम्’ की रचना के तौर पर कागज पर उतारा। बंकिम का दुख कुछ हल्का तो हुआ, लेकिन एक महान लेखक-साहित्यकार के तौर पर इस गीत से उन्हें साहित्यिक संतुष्टि नहीं मिल सकी। सच भी है। उन्हें स्वयं लगा कि गीत की रचना किसी एक भाषा में नहीं हो पायी है, बांग्ला के साथ संस्कृत की अधखिचड़ी युति है। न पूरी तरह बांग्ला है, न संस्कृत। फिर गीत के अलग-अलग चरण, अलग-अलग मात्राओं में रचे गये हैं।
विभिन्न चरणों में पंक्तियों की संख्या भी एक सी नहीं। पूरी की पूरी रचना ही संस्कृत या बांग्ला गीत-विधा के गणितीय ढांचे के अनुकूल नहीं थी। कोई पंक्ति छह-सात शब्दों की, तो कोई पंक्ति दस-बारह शब्दों की। कहीं अत्यंत सरल बांग्ला, तो कहीं अत्यंत कठिन संस्कृत। साहित्यिक स्तर पर इस गीत को मान्यता मिलना कठिन ही था। फलत: बंकिम ने इस गीत को अपनी दराज के एक कोने में रख दिया। यह बात सन् 1875 की है।
साल भार बाद की बात है। बंकिम ‘बंगदर्शन’ नाम की एक मासिक पत्रिका का प्रकाशन करते थे। एक दिन ‘बंग दर्शन’ के सहायक संपादक रामचंद्र बंधोपाध्याय बंकिम के पास आये। बताने लगे कि पत्रिका को उसी दिन छापने के लिए प्रेस भेजना था, लेकिन सामग्री कम पड़ जाने से थोड़ी जगह बच रही थी। रामचंद्र बंधोपाध्याय की निगाह दराज में पड़े गीत पर पड़ी। उन्होंने सहज भाव से उसे ही ले लिया और जगह भरने की खातिर ‘फिलर’ के तौर पर उसे छाप भी दिया। छपने के बाद भी गीत पर किसी की नजर नहीं पड़ी। उसे कोई महत्व नहीं मिल सका।
इसके चार वर्ष बाद बंकिमचंद्र ने जब सन् 1857 ई. के संन्यासी विद्रोह की घटनाओं के आधार पर अपने अमर उपन्यास ‘आनंदमठ’ की रचना की, तो मातृवंदना और देशवंदना को एकाकार करते हुए उन्होंने विद्रोही संन्यासियों के समवेत कंठों से अपने उसी उपेक्षित गीत को गाते हुए दिखा दिया। ‘आनंदमठ’ का प्रकाशन सन् 1880ई. में हुआ और आजादी के संघर्ष के उन उत्तप्त दिनों में ‘आनंदमठ’ को बंगाल समेत सारे देश ने हाथों-हाथ लेकर माथे से लगा लिया और उसमें शामिल विद्रोही संन्यासियों के गीत ‘वंदे मातरम्’ को उन्होंने भारतवंदना के रूप में देश की आज़ादी के लिए मातृचरणों में प्राण न्यौछावर करने की अजस्त्र प्रेरणा देने वाले गीत के तौर पर सीने से लगा लिया।
साहित्यिक मूल्यों पर कसते हुए रामचंद्र बंद्योपाध्याय ने जब इसे असाहित्यिक रचना बताया था, तब बंकिम ने कहा था-‘देखना, एक दिन यही साधारण गीत देश में असाधारण महत्व पायेगा। बच्चे-बच्चे के कंठ में गूंजेगा। कालजयी होगा।’
वही हुआ भी, इतिहास इसका गवाह है। वर्ष 1886 के कोलकाता कांग्रेस अधिवेशन की शुरुआत इसी गीत के गायन से हुई। गीत की धुन संगीतकार यदुनाथ भट्टाचार्य ने बनायी थी। वर्ष 1896 में तो कमाल ही हुआ। कोलकाता के बिडन स्क्वायर में हुए कांग्रेस अधिवेशन की शुरुआत फिर ‘वंदे मातरम्’ से ही हुई और इसे वहां गाया स्वयं विश्वकवि रवींद्रनाथ ठाकुर ने। रवींद्रनाथ ने ही उसकी धुन भी बनायी। वह धुन रवींद्रनाथ के ‘गीतवितान’ की स्वरलिपि में शामिल है। लेकिन उस अपूर्व-अद्भुत गायन को सुनने के लिए तब गीत के रचयिता बंकिम बाबू रह नहीं गए थे। उनका देहावसन सन् 1894 ई. में ही हो गया था। फिर तो कांग्रेस में मानो परंपरा ही पड़ गयी थी कि इसी गीत से उसके अधिवेशनों की शुरूआत होती। सन् 1901 ई. के कोलकाता अधिवेशन में दक्षिणाचरण सेन ने, सन् 190ई. के वाराणसी अधिवेशन में सरला देवी चौधुरानी ने इसे गाया। सन् 1905 ई. में बंगभंग के खिलाफ हुए उग्र आंदोलन में यह गीत भारतीय आंदोलनकारियों के लिए हथियार की तरह सशक्त बनकर उभरा। अंग्रेजों ने देखा कि एक गीत में कितनी ताकत होती है। वे घबराये। आज़ादी की लड़ाई में इस गीत ने ऐतिहासिक ऊर्जा का निर्माण किया। सारा भारत एक स्वर में गा उठा-‘वंदे मातरम्!’ अंग्रेज जितना खून बहाते, जितना अत्याचार करते, ‘वंदे मातरम्’ का उदघोष उतना गगनभेदी होता जाता। ‘वंदे मातरम्’ की अजेय शक्ति की प्रशंसा में स्वयं रवींद्रनाथ ठाकुर ने एक गीत की रचना की-‘वंदे मातरम्, वंदे मातरम्, एक सूत्रे बांधियाछि सहस्त्रही मन/एक कार्ये सौंपियाछि सहस्त्र जीवन’ (वंदे मातरम् के एक सूत्र में सहस्त्र हृदयों को बाधा है, एक कार्य में सहस्त्र जीवन सौंपे हैं)
सन् 1907 में जब भिकाजी कामा ने भारत के राष्ट्रध्वज के रूप में पहली बार तिरंगा का निर्माण किया और जर्मनी के स्टुटगार्ड में उसे फहराया, तब राष्ट्रगीत के तौर पर वहां ‘वंदे मातरम्’ का ही गायन हुआ। लेकिन जब आज़ादी का समय आया, तब देश के राष्ट्रध्वज के साथ ही जब राष्ट्रगीत के चयन की बात आयी, तब रवींद्रनाथ ठाकुर के ‘जन गण मन’ के मुकाबले ऐतिहासिक ‘वंदे मातरम्’ पिछड़ गया।
सन् 1907 में जब भिकाजी कामा ने भारत के राष्ट्रध्वज के रूप में पहली बार तिरंगा का निर्माण किया और जर्मनी के स्टुटगार्ड में उसे फहराया, तब राष्ट्रगीत के तौर पर वहां ‘वंदे मातरम्’ का ही गायन हुआ। लेकिन जब आज़ादी का समय आया, तब देश के राष्ट्रध्वज के साथ ही जब राष्ट्रगीत के चयन की बात आयी, तब रवींद्रनाथ ठाकुर के ‘जन गण मन’ के मुकाबले ऐतिहासिक ‘वंदे मातरम्’ पिछड़ गया। हालांकि ‘वंदे मातरम्’ की रचना ‘जन गण मन’ से 36 वर्ष पहले हुई थी। ‘वंदे मातरम्’ का राष्ट्रीय महत्व ज्यादा था, लोकप्रिय भी अपार था, फिर भी इसके राष्ट्रगीत न बन पाने के कई कारण थे।
कांग्रेस के अधिवशनों में जब इसे गाया जाने लगा, तो कांग्रेस की सर्वभारतीय, सर्वधर्मीय, सर्वजातीय छवि को देखते हुए, ‘वंदे मातरम्’ के प्रति गैर हिंदु धर्मियों की भावना का ध्यान रखा गया।
राष्ट्रगीत न बन पाने के बावजूद ‘वंदे मातरम्’ को जो सम्मान देश भर में मिला, वह अनन्य है। 14 अगस्त सन् 1947 ई. की मध्य रात्रि को स्वतंत्र भारत की पहली संसद की जो पहली सभा हुई, उसकी शुरुआत ‘वंदे मातरम्’ से हुई, समापन ‘जन गण मन’ से। 24 जनवरी, 1950 ई. को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डा. राजेंद्र प्रसाद ने संसद में बयान दिया कि ‘वंदे मातरम्’ की लोकप्रियता और आज़ादी की लड़ाई में उसकी महान भूमिका का सम्मान करते हुए देश उसे राष्ट्रगीत ‘जन गण मन’ के समान सम्मान का अधिकारी मानता है और उसे ‘राष्ट्रगान’ का दर्जा देता है।
वर्ष 2002 ई. में बीबीसी वर्ल्ड सर्विस ने दुनिया भर के लोकप्रिय गीतों का जो सर्वेक्षण करवाया, उसमें कुल 7000 गीतों में ‘वंदे मातरम्’ को दूसरा स्थान मिला।
‘वंदे मातरम्’ का अंग्रेजी अनुवाद सन् 1909 ई. में ऋषि अरविंद घोष (आरोबिंदो) ने किया-घ् ंदै ूद ूप, स्दूप! राजीव गांधी की केंद्रीय सरकार में मंत्री रहे आरिफ मोहम्मद खान ने उर्दू में अनुवाद किया ‘तस्लीमात, मां, तस्लीमात!’
‘वंदे मातरम्’ दुनिया भर का एक मात्र ऐसा गीत है, जिसकी सौ से ज्यादा धुनें विभिन्न संगीतकारों ने बनायीं। आकाशवाणी में जो धुन बजती है, वह पं. रविशंकर ने बनाई। पं विष्णु दिगम्बर पलुस्कर, पं. उओंकारनाथ ठाकुर, हीराबाई बड़ोदेकर, हेमंत कुमार, एम.एस. सुब्बलक्ष्मी, मास्टर कृष्णाराव पंडित, दिलीप कुमार राय, तिमिरबरन और स्वयं विश्वकवि रवींद्रनाथ ठाकुर आदि ने ‘वंदे मातरम’ की अपनी-अपनी धुनें बनायीं।
हां, एक बात बताकर लेख का समापन करुंगा। ऊपर मुंबई के ‘फ्रीप्रेस जर्नल’ के जिस सर्वेक्षण की बात बतायी गयी है, उसमें ‘वंदे मातरम्’ के लिए सर्वाधिक अंक देने वाला प्रांत अपना महाराष्ट्र ही था। वंदे मातरम्।