भारतीय निर्मित वस्त्र और हस्तशिल्प कई देशों को निर्यात किए जाते हैं। निर्यात के लिए अमेरिका प्राथमिक बाजार है, लेकिन देशों की कुल संख्या 100 तक है। निर्यात में 41% हिस्सेदारी के साथ रेडीमेड वस्त्र सबसे बड़ा खंड है। कपड़ा मंत्रालय के रिकॉर्ड के अनुसार, भारत ने पिछले साल की तुलना में 7% की वृद्धि के साथ 17 बिलियन अमेरिकी डॉलर का कपड़ा निर्यात किया। कच्चे माल, कुशल श्रम, और अच्छी डिजाइनिंग क्षमताओं की आसान उपलब्धता के कारण भारत को एक कपड़ा केंद्र माना जा रहा है। ह्यूगो, बॉस और डीजल जैसे विश्व प्रसिद्ध लेबल भी भारत से कपड़े आयात कर रहे हैं। इस प्रकार, इस उद्योग से निर्यात लाभ काफी हैं।
भारतीय वस्त्र उद्योग देश का सबसे पुराना उद्योग है और इसकी बहुत लंबी और समृद्ध परंपरा है। वस्त्र उद्योग ने असल विदेशी मुद्रा आय और सकल घरेलू उत्पाद में योगदान के मामले में राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में एक बड़ा योगदान दिया है। वित्त वर्ष 2019 में भारत के वस्त्र उद्योग ने उद्योग उत्पादन का सात प्रतिशत (मूल्य के संदर्भ में) योगदान दिया। इसने भारत के सकल घरेलू उत्पाद में दो प्रतिशत का योगदान दिया और वित्त वर्ष 2019 में 4.5 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार दिया। वित्त वर्ष 2019 में भारत की निर्यात आय के लिए इस क्षेत्र ने 15 प्रतिशत का योगदान दिया। वस्त्र उद्योग में देश भर में 35.22 लाख हथकरघा श्रमिकों सहित लगभग 4.5 करोड़ कार्यरत श्रमिक हैं। वित्त वर्ष 2019 में घरेलू वस्त्र एवं परिधान का बाजार अनुमानित अमेरीकी डॉलर 100 बिलियन (7.00 लाख करोड़ रूपये) था। वित्त वर्ष 2020 में भारत में कच्चे कपास का उत्पादन 3.604 करोड़ गट्ठे तक पहुंच गया है। वित्त वर्ष 2019 के दौरान, भारत में रेशे का उत्पादन 10.44 लाख टन (मीट्रीक टन) रहा और वित्त वर्ष 2020 में (जनवरी 2020 तक) 10.60 मीट्रीक टन तक पहुंच गया, जबकि सूत के लिए उत्पादन इसी अवधि के दौरान 476.2 करोड़ किलोग्राम रहा।
भारत की लगभग 27% विदेशी मुद्रा वस्त्रों के माध्यम से है। यह उम्मीद की जाती है कि वर्ष 2024-25 तक भारत से वस्त्र निर्यात 185 बिलियन अमेरिकी डॉलर को छू जाएगा। भारत का वैश्विक वस्त्र और परिधान व्यापार में लगभग 5% हिस्सा है।
भारतीय वस्त्र उद्योग का सामर्थ्य:
-
कम लागत और कुशल जनशक्ति की उपलब्धता
-
कपास रेशों की विस्तृत किस्मों की उपलब्धता और तेजी से बढ़ते संश्लिष्ट रेशे के उद्योग होना।
-
अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सूत के सबसे बड़े निर्यातकों में से एक
-
बढ़ती अर्थव्यवस्था, संभावित घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजार।
-
उद्योग में बड़े और विविधतापूर्ण खंड हैं जो विभिन्न प्रकार के उत्पाद प्रदान करते हैं।
भारतीय वस्त्र उद्योग की संरचना:
वस्त्र उद्योग की उत्पादन श्रृंखला में रेशों से लेकर पोशाक/परिधान/गढ़ंत तक निम्नलिखित खंड हैं:
-
रूई ओटना/ रेशों का विनिर्माण
-
कताई / सूत विनिर्माण / बुनावट
-
रेशे बनाना – बिनाई, बुनाई, गैर-बुने कपड़े
-
सूत और रेशे का रासायनिक प्रसंस्करण – विरंजन, रंगाई। मुद्रण और परिष्करण
-
पोशाक बनाना और गढ़ंत।
-
तकनीकी वस्त्र।
भारत सरकार की नवीनतम परिभाषाओं के अनुसार, विभिन्न क्षेत्रों के लिए कार्यशाला एवं यंत्र में निवेश निम्न प्रकार है।
-
सूक्ष्म उद्योग क्षेत्र: 25 लाख रुपये तक का निवेश।
-
लघु उद्योग क्षेत्र: 25 लाख से 5 करोड़ तक का निवेश।
-
मध्यम स्तर का क्षेत्र: 5 करोड़ से 50 करोड़ तक का निवेश।
-
बड़े पैमाने पर क्षेत्र: 50 करोड़ रुपये से ऊपर का निवेश।
-
बहुत बड़ी परियोजना: 350 से 2000 तक प्रत्यक्ष रोजगार और स्थान के आधार पर 200 से 1500 करोड़ का निवेश केंद्र और राज्य, दोनों सरकारों ने इन सभी क्षेत्रों में नए और साथ ही मौजूदा निवेशकों के लिए कई प्रोत्साहन दिए हैं।
वस्त्रों के क्षेत्र में निवेश के अवसर:
अब हम भारतीय वस्त्र उद्योग में क्षेत्रवार निवेश संभावनाओं पर विचार करेंगे:
- रूई ओटना और रेशों का विनिर्माण:
 रूई ओटना: रूई ओटना एक उद्योग है जहां कपास के पौधे से प्राप्त कच्चे कपास से बीज निकाल दिए जाते हैं। रूई ओटने में बीज निकालने के बाद प्राप्त कपास के रोएं को लगभग प्रत्येक 165 किलोग्राम वजन वाले कपास के गट्ठे में पैक किया जाता है। इन गट्ठों को फिर आगे की प्रक्रिया के लिए कताई मिलों में पहुंचाया जाता है।
रूई ओटना: रूई ओटना एक उद्योग है जहां कपास के पौधे से प्राप्त कच्चे कपास से बीज निकाल दिए जाते हैं। रूई ओटने में बीज निकालने के बाद प्राप्त कपास के रोएं को लगभग प्रत्येक 165 किलोग्राम वजन वाले कपास के गट्ठे में पैक किया जाता है। इन गट्ठों को फिर आगे की प्रक्रिया के लिए कताई मिलों में पहुंचाया जाता है।
रूई ओटने का उद्योग आम तौर पर लघु या मध्यम स्तर की औद्योगिक श्रेणी में आता है। एक रूई ओटने वाली मिल को न्यूनतम 12 डबल रोलर ओटनी के साथ शुरू किया जा सकता है और बड़ी मिलों में 24 या 36 डबल रोलर ओटनी हो सकती हैं। एक 12 डबल रोलर रूई ओटने के कारखाना को लगभग 10 करोड़ के निवेश की आवश्यकता होगी। रूई ओटने का उद्योग, एक वर्ष में केवल 200 दिनों के लिए काम करता है क्योंकि यह कपास की कटाई के मौसम पर निर्भर करता है। ऐसी ओटनी का वार्षिक उत्पादन लगभग 25000 गट्ठा प्रति वर्ष है। कपास उगाने वाले क्षेत्रों के पास रूई ओटने के उद्योग की स्थापना की जानी चाहिए।
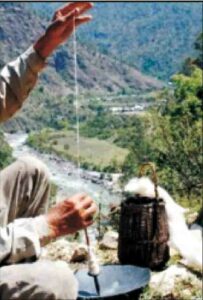 रेशों का विनिर्माण: रेशों के विनिर्माण कारखानों में मानव निर्मित रेशें जैसे विस्कोस, नायलॉन, पॉलिएस्टर और पॉलीप्रोपाइलीन का निर्माण किया जाता है। ऐसे उद्योग बड़े स्तर के औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं क्योंकि ऐसे उद्योगों में निवेश बहुत बड़ा है – 300 करोड़ से कुछ हजार करोड़ रुपये तक। रेशों के विनिर्माण उद्योग में इतने बड़े निवेश में सक्षम बड़े कॉर्पोरेट समूह ही केवल निवेश करते हैं।
रेशों का विनिर्माण: रेशों के विनिर्माण कारखानों में मानव निर्मित रेशें जैसे विस्कोस, नायलॉन, पॉलिएस्टर और पॉलीप्रोपाइलीन का निर्माण किया जाता है। ऐसे उद्योग बड़े स्तर के औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं क्योंकि ऐसे उद्योगों में निवेश बहुत बड़ा है – 300 करोड़ से कुछ हजार करोड़ रुपये तक। रेशों के विनिर्माण उद्योग में इतने बड़े निवेश में सक्षम बड़े कॉर्पोरेट समूह ही केवल निवेश करते हैं।
- कताईसूत विनिर्माणटेक्सचरिंग उद्योग:
कताई उद्योग: प्रचलन में दो प्रकार की कताई तकनीक होती हैं। ए. रिंग कताई और बी. रोटर कताई। भारत में ज्यादातर कताई मिलें रिंग कताई मिलें हैं। केवल एक बहुत छोटा अनुपात रोटर कताई मिलों का है।
कताई उद्योगों में निवेश को मध्यम स्तर या बड़े स्तर के उद्योग क्षेत्र में वर्गीकृत किया जाता है। लगभग 25000 तकली की न्यूनतम क्षमता के साथ एक कपास रिंग कताई मिल शुरू की जा सकती है। 25000 तकली की कताई मिल के लिए निवेश आज लगभग 85 से 90 करोड़ रुपये है। ऐसी मिल द्वारा कुल बिक्री 100 करोड़ रुपये के आसपास है। एक नई कताई मिल में ‘सघन कताई’, ‘सूत कताई संयोजन’ और सूत दोहरीकरण यंत्र जैसे संयोजन शामिल करना अनिवार्य है, जो मूल्य वर्धित सूत का उत्पादन कर सकते हैं जो समय की मांग है।
सूत विनिर्माण: सूत दोहरीकरण कारखानों में निवेश भी बहुत आकर्षक है। रेशे बनाने में बड़े पैमाने पर दोहरे सूत का उपयोग किया जा रहा है और इसलिए इन सूतों की बढ़ती मांग है। एक सूत दोहरीकरण कारखाना 5.00 करोड़ रुपये के निवेश से शुरू हो सकता है और ऐसी इकाई की कुल बिक्री 30.00 करोड़ रूपये के आसपास है। ऐसी संभावना है कि दोहरीकरण इकाई को ठेके पर काम के आधार पर भी चलाया जा सकता है। सूत विनिर्माण के तहत अन्य संभावनाएं हैं, ए) सिलाई धागा निर्माण बी) फीता और रस्सी निर्माण, सी) फैंसी सूत निर्माण आदि। सी. सूत टेक्सचरिंग: टेक्सचरिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका इस्तेमाल पॉलिएस्टर और नायलॉन जैसे मानव रचित सूत को आकार प्रदान करने के लिए किया जाता है, ताकि उन्हें परिधान में अधिक आरामदायक बनाया जा सके।
- रेशे बनाना – बिनाई, बुनाई, गैर-बुने कपड़े और अन्य:
बुनाई: बुनाई भारतीय रेशा निर्माण क्षेत्र में सबसे बड़ा खंड है। भारत में चार प्रकार की बुनाई मशीनें मौजूद हैं: 1. हथकरघा, 2. सपाट विद्युत करघे, 3. स्वचालित करघे और 4. बिना बिनाई की नली के करघे (प्रोजेक्टाइल प्रकार, रैपियर प्रकार, एयर जेट प्रकार और वाटर जेट प्रकार) भारत का लगभग 95% बिनाई क्षेत्र छोटे असंगठित स्वरूप का है। विकेंद्रीकृत क्षेत्र में लगभग 23.8 लाख हथकरघे, 25.20 लाख विद्युत करघे हैं। भारत के रेशा उत्पादन में विकेंद्रीकृत विद्युत करघा क्षेत्र का योगदान लगभग 78% है, जबकि हथकरघा क्षेत्र का योगदान लगभग 16% है। 25.2 लाख विद्युत करघों में से केवल 50000 के आसपास आधुनिक बिना बिनाई की नली के करघे हैं। वस्त्र सामग्री में अपेक्षित वृद्धि के लिए विद्युत करघा क्षेत्र को भविष्य में अहम भूमिका निभानी होगी। सादे और स्वचालित बिनाई की नली करघे में कई कमियां हैं और इसलिए उनके विस्तार की सीमाएं होंगी। इसलिए, यदि भारत के वस्त्र उद्योग को विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करना है, तो बिना बिनाई की नली के करघों को मुख्य भूमिका निभानी होगी। इसलिए भविष्य का विस्तार, बिना बिनाई की नली के करघा क्षेत्र में होने की उम्मीद है। इसलिए, इस क्षेत्र में निवेश के बेहतरीन अवसर होंगे। बिनाई: बिनाई क्षेत्र मुख्य रूप से तमिलनाडु के थिरूपुर के पास मौजूद है। कर्नाटक में बेंगलुरु और पंजाब में लुधियाना। अंतर्वस्त्रों और ऊपरी वस्त्रों की बढ़ती मांग के कारण बिनाई उद्योग के लिए काफी गुंजाइश है और यह मांग तेजी से बढ़ रही है। बिनाई इकाई को चार से छह बिनाई मशीनों के साथ शुरू किया जा सकता है और ऐसी इकाई में लगभग 4 से 5 करोड़ रु. निवेश करना होगा। हालांकि, अकेले करघा उद्योग की तरह बिनाई इकाइयां बहुत सफल नहीं हुई हैं। ये इकाइयां सफल होती हैं यदि इन्हें बिने हुए कपड़े और परिधान सुविधाओं के रासायनिक प्रसंस्करण के साथ संघटित किया जाता है।
 बगैर बिनाई: बगैर बिनाई तकनीक वह है जहां वस्त्रों को रेशों से सीधे, धागे में परिवर्तित किए बिना बनाया जाता है। ये वस्त्र इसलिए, बिने या बुने हुए वस्त्रों की तुलना में तुलनात्मक रूप से कम महंगे हैं। हालांकि बगैर बिनाई वाले कपड़ों में परिधान वस्त्रों के उपयुक्त गुणवत्ता नहीं होती और इसलिए उनका प्रयोग मुख्य रूप से औद्योगिक वस्त्रों और तकनीकी वस्त्रों तक सीमित हैं। बगैर बिनाई कपड़ों के निर्माण में, पहले आवश्यक मोटाई के अच्छी तरह से खुले हुए रेशों की एक चादर बनाई जाती है और चादर में रेशे एक साथ गुंथे होते हैं। इस श्लेषण को चादर की परतों को एक साथ सिलाई करके या चादर में आसानी से विगलित होने वाले रेशों को समाविष्ट करके और पानी के एक जेट द्वारा चादर में रेशों को गर्म करने या उलझाकर विगलित करने वाली रासायनिक विधियों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। बगैर बिनाई वाले वस्त्रों का नाम प्रयुक्त विधि के आधार पर पड़ता है, जैसे रसायन संश्लेषित, सुई संश्लेषित, उष्ण संश्लेषित या जल धार संश्लेषित आदि। निवेश के लिए बगैर बिनाई के क्षेत्र में कई अवसर हैं।
बगैर बिनाई: बगैर बिनाई तकनीक वह है जहां वस्त्रों को रेशों से सीधे, धागे में परिवर्तित किए बिना बनाया जाता है। ये वस्त्र इसलिए, बिने या बुने हुए वस्त्रों की तुलना में तुलनात्मक रूप से कम महंगे हैं। हालांकि बगैर बिनाई वाले कपड़ों में परिधान वस्त्रों के उपयुक्त गुणवत्ता नहीं होती और इसलिए उनका प्रयोग मुख्य रूप से औद्योगिक वस्त्रों और तकनीकी वस्त्रों तक सीमित हैं। बगैर बिनाई कपड़ों के निर्माण में, पहले आवश्यक मोटाई के अच्छी तरह से खुले हुए रेशों की एक चादर बनाई जाती है और चादर में रेशे एक साथ गुंथे होते हैं। इस श्लेषण को चादर की परतों को एक साथ सिलाई करके या चादर में आसानी से विगलित होने वाले रेशों को समाविष्ट करके और पानी के एक जेट द्वारा चादर में रेशों को गर्म करने या उलझाकर विगलित करने वाली रासायनिक विधियों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। बगैर बिनाई वाले वस्त्रों का नाम प्रयुक्त विधि के आधार पर पड़ता है, जैसे रसायन संश्लेषित, सुई संश्लेषित, उष्ण संश्लेषित या जल धार संश्लेषित आदि। निवेश के लिए बगैर बिनाई के क्षेत्र में कई अवसर हैं।
- रासायनिक प्रसंस्करण:
 धागे का रासायनिक प्रसंस्करण: कुछ समय के लिए धूसर धागे को वस्त्र में बदलने से पहले प्रक्षालित, रंगे या मर्सराइज किए जाने की आवश्यकता होती है। धारियों या चेकों के साथ शर्टिंग,सूटिंग या ड्रेस सामग्री जैसे वस्त्र, टेरी तौलिए, डिज़ाइन किए गए फर्निशिंग वस्त्रों को ऐसे रासायनिक रूप से संसाधित धागों की आवश्यकता होती है। जैसे-जैसे फैशन उन्मुख वस्त्रों की मांग बढ़ती जाएगी, ऐसे धागों की आवश्यकता भी बढ़ेगी। धागा प्रसंस्करण कारखानों को आमतौर पर धागा रंगाई इकाइयों के रूप में कहा जाता है। इस प्रकार धागों की रंगाई निवेश के लिए एक बहुत ही आकर्षक क्षेत्र है। परंपरागत रूप से धागे की रंगाई हस्तचालित मशीनों द्वारा की जाती थी। ये हाथ रंगाई इकाइयां पुरानी होती जा रही हैं क्योंकि इनमें बहुत अधिक मानव शक्ति की आवश्यकता होती है और गुणवत्ता की निरंतरता की समस्या होती है। इसलिए मशीन रंगाई इकाइयां आज अधिक लोकप्रिय हो गई हैं। एक धागा रंगाई कारखाना को प्रति दिन लगभग दो टन की न्यूनतम क्षमता के साथ शुरू किया जा सकता है। 20 टन प्रति दिन की क्षमता वाले बड़े कारखाने भी मौजूद हैं। दो टन प्रतिदिन की क्षमता वाली धागा रंगाई इकाई के लिए लगभग 5 से 7 करोड़ रुपये के निवेश की आवश्यकता होगी।
धागे का रासायनिक प्रसंस्करण: कुछ समय के लिए धूसर धागे को वस्त्र में बदलने से पहले प्रक्षालित, रंगे या मर्सराइज किए जाने की आवश्यकता होती है। धारियों या चेकों के साथ शर्टिंग,सूटिंग या ड्रेस सामग्री जैसे वस्त्र, टेरी तौलिए, डिज़ाइन किए गए फर्निशिंग वस्त्रों को ऐसे रासायनिक रूप से संसाधित धागों की आवश्यकता होती है। जैसे-जैसे फैशन उन्मुख वस्त्रों की मांग बढ़ती जाएगी, ऐसे धागों की आवश्यकता भी बढ़ेगी। धागा प्रसंस्करण कारखानों को आमतौर पर धागा रंगाई इकाइयों के रूप में कहा जाता है। इस प्रकार धागों की रंगाई निवेश के लिए एक बहुत ही आकर्षक क्षेत्र है। परंपरागत रूप से धागे की रंगाई हस्तचालित मशीनों द्वारा की जाती थी। ये हाथ रंगाई इकाइयां पुरानी होती जा रही हैं क्योंकि इनमें बहुत अधिक मानव शक्ति की आवश्यकता होती है और गुणवत्ता की निरंतरता की समस्या होती है। इसलिए मशीन रंगाई इकाइयां आज अधिक लोकप्रिय हो गई हैं। एक धागा रंगाई कारखाना को प्रति दिन लगभग दो टन की न्यूनतम क्षमता के साथ शुरू किया जा सकता है। 20 टन प्रति दिन की क्षमता वाले बड़े कारखाने भी मौजूद हैं। दो टन प्रतिदिन की क्षमता वाली धागा रंगाई इकाई के लिए लगभग 5 से 7 करोड़ रुपये के निवेश की आवश्यकता होगी।
वस्त्र का रासायनिक प्रसंस्करण: इससे पहले कि धूसर वस्त्रों को बाजारों में या वस्त्र बनाने के लिए भेजा जाए, उन्हें विरंजन, मर्सराईजिंग, रंगाई, छपाई और प्रसंस्करण के लिए आवश्यकता के अनुसार संसाधित किया जाना आवश्यक है। ये सभी प्रक्रियाएं रासायनिक प्रसंस्करण इकाइयों में की जाती हैं। परंपरागत रूप से ये प्रक्रियाएं हाथ से चलने वाली प्रक्रियाओं के रूप में हस्तचालित इकाइयों में की जाती थीं। हालांकि समय के साथ ऐसी प्रक्रियाएं समाप्त हो गई हैं और अधिकांश प्रक्रियाएं प्रसंस्करण मशीनों के साथ काम कर रही हैं। इन प्रसंस्करण इकाइयों की तीन श्रेणियां हैं:
- निम्न और घरेलू गुणवत्ता वाले वस्त्रों के लिए प्रक्रियाएं। इस प्रकार की इकाइयां आमतौर पर अनिश्चित गैर-स्वचालित और कम लागत वाली मशीनों का उपयोग करती हैं,
- परिधान बनाने और मध्यम गुणवत्ता के निर्यात वस्त्रों के लिए आवश्यक बेहतर गुणवत्ता वाले वस्त्रों के लिए आवश्यक मध्यम गुणवत्ता के लिए प्रक्रियाएं। ये प्रक्रियाएं स्वचालित नियंत्रण के साथ घरेलू या आयातित मशीनों का उपयोग करती हैं। हालांकि, ये मशीनें गैर-सतत बैच प्रसंस्करण पर संचालित होती हैं। इस तरह की मशीनों पर बेहद अधिक लंबाई में स्थिरता से गुणवत्ता प्राप्त करना मुश्किल है।
- सतत मशीनों के साथ उच्च गुणवत्ता वाले वस्त्रों की प्रक्रियाएं: ये प्रक्रियाएं सतत विरंजन और सतत रंगाई मशीनों जैसी मशीनों का उपयोग करती हैं। ऐसी मशीनों पर 50000 मीटर से लेकर 10000 मीटर तक की गुणवत्ता वाली स्थिरता आसानी से संभव है। बहुत उच्च गुणवत्ता वाले निर्यात और परिधान कारखानों के लिए जहां बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता है, ऐसी इकाइयों की आवश्यकता होती है। पहले प्रकार की निम्न गुणवत्ता वाली प्रसंस्करण इकाई 10 से 15 करोड़ रुपये के निवेश के साथ शुरू की जा सकती है। हालांकि ग्राहकों में बढ़ती गुणवत्ता की आवश्यकताओं के साथ इस प्रकार की प्रसंस्करण इकाइयों की मांग कम हो रही है। भारत में मध्यम और उच्च सतत गुणवत्ता प्रसंस्करण इकाइयों की भारी कमी है। रासायनिक प्रसंस्करण क्षेत्र में आधुनिकीकरण उसी गति से नहीं हुआ है जैसे कताई या बिनाई क्षेत्र में आधुनिकीकरण हुआ है। केंद्र और राज्य सरकारें, इसलिए मध्यम गुणवत्ता और उच्च गुणवत्ता वाली सतत प्रसंस्करण इकाइयों के क्षेत्र में निवेश के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन प्रदान करती हैं। एक मध्यम गुणवत्ता वाले प्रसंस्करण के लिए 30 से 50 करोड़ रुपये तक निवेश की आवश्यकता होगी। जबकि सतत प्रसंस्करण मशीनों के साथ एक उच्च गुणवत्ता वाली प्रसंस्करण इकाई के लिए 80 से 120 करोड़ रुपये के बीच निवेश की आवश्यकता होगी। प्रसंस्करण इकाइयों की मुख्य आवश्यकता पानी है। लगभग 50000 मीटर प्रति दिन की क्षमता (जो कि न्यूनतम आर्थिक रूप से व्यवहार्य क्षमता है) के साथ प्रक्रिया के लिए प्रसंस्करण इकाई को लगभग 5.00 लाख लीटर पानी प्रति दिन आवश्यकता होगी। इसलिए, रासायनिक प्रसंस्करण इकाइयां वहीं शुरू की जा सकती हैं, जहां पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध हो। रासायनिक प्रसंस्करण इकाइयों से जुड़ी दूसरी समस्या, चाहे धागा प्रसंस्करण की हो या वस्त्र प्रसंस्करण की हो, अपशिष्ट और उत्सर्जित पानी के उपचार की है। शून्य उत्सर्जन के साथ भविष्य की सभी रासायनिक प्रसंस्करण इकाइयों की योजना बनाना आवश्यक होगा। इस उद्देश्य के लिए आवश्यक प्रकार के अपशिष्ट उपचार संयंत्र को शामिल किया जाना चाहिए।
- परिधान और गढ़ंत: पारंपरिक वस्त्र सामग्री के उत्पादन में अंतिम कड़ी परिधान बनाना या गढ़ंत वस्त्र हैं।
 परिधान बनाना: यह एक ऐसा चरण है जहां परिधानों को तैयार वस्त्रों से सिला जाता है। परिधान बनाने वाली इकाइयों की संख्या बहुत कम है। छोटा, साथ ही मध्यम स्तर का क्षेत्र। लगभग 50 सिलाई मशीनों के साथ और लगभग 1.00 करोड़ रू. के निवेश के साथ परिधान बनाने की सबसे छोटी इकाई शुरू की जा सकती है। इस प्रकार की इकाइयां कहीं भी शुरू की जा सकती हैं और कोई स्थानिकता की सीमाएं नहीं हैं। आवश्यकता केवल यह है कि पर्याप्त महिला श्रम उपलब्ध होना चाहिए क्योंकि सिलाई मशीनें आमतौर पर महिलाओं द्वारा संचालित की जाती हैं। आम तौर पर प्रति मशीन 1-5 श्रमिकों की आवश्यकता होती है। केंद्र और प्रदेश सरकारों, दोनों द्वारा परिधान इकाइयों के लिए प्रोत्साहन की अनेक पेशकश की जाती है, क्योंकि ये इकाइयां महिलाओं और विशेषकर
परिधान बनाना: यह एक ऐसा चरण है जहां परिधानों को तैयार वस्त्रों से सिला जाता है। परिधान बनाने वाली इकाइयों की संख्या बहुत कम है। छोटा, साथ ही मध्यम स्तर का क्षेत्र। लगभग 50 सिलाई मशीनों के साथ और लगभग 1.00 करोड़ रू. के निवेश के साथ परिधान बनाने की सबसे छोटी इकाई शुरू की जा सकती है। इस प्रकार की इकाइयां कहीं भी शुरू की जा सकती हैं और कोई स्थानिकता की सीमाएं नहीं हैं। आवश्यकता केवल यह है कि पर्याप्त महिला श्रम उपलब्ध होना चाहिए क्योंकि सिलाई मशीनें आमतौर पर महिलाओं द्वारा संचालित की जाती हैं। आम तौर पर प्रति मशीन 1-5 श्रमिकों की आवश्यकता होती है। केंद्र और प्रदेश सरकारों, दोनों द्वारा परिधान इकाइयों के लिए प्रोत्साहन की अनेक पेशकश की जाती है, क्योंकि ये इकाइयां महिलाओं और विशेषकर  ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार प्रदान करती हैं। कपड़ा इकाई स्थापित करते समय पहले उत्पाद मिश्रण को तय करना पड़ता है, क्योंकि कमीज, नीचे पहनने के लिए और बिने वस्त्र के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सिलाई मशीनें अलग होती हैं। इसलिए उत्पाद मिश्रण का तय किया जाना आवश्यक है। परिधान इकाइयों को काम के आधार पर या खुद के उत्पादन के आधार पर क्रियान्वित किया जा सकता है। वहां कई बड़े ब्रांड हैं जो छोटी परिधान इकाइयों के लिए काम करते हैं।
ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार प्रदान करती हैं। कपड़ा इकाई स्थापित करते समय पहले उत्पाद मिश्रण को तय करना पड़ता है, क्योंकि कमीज, नीचे पहनने के लिए और बिने वस्त्र के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सिलाई मशीनें अलग होती हैं। इसलिए उत्पाद मिश्रण का तय किया जाना आवश्यक है। परिधान इकाइयों को काम के आधार पर या खुद के उत्पादन के आधार पर क्रियान्वित किया जा सकता है। वहां कई बड़े ब्रांड हैं जो छोटी परिधान इकाइयों के लिए काम करते हैं।
गढ़ंत: गढ़ंत वस्त्रों की इकाइयां परिधान इकाइयों के समान होती हैं, ये इकाइयां केवल आम उपभोक्ता सामान जैसे कि चादरें, तकिया कवर, पर्दे, सोफा कवर इत्यादि सिलती हैं। जैसे-जैसे आम उपभोक्ता अधिक से अधिक प्रभावशाली होते जा रहे हैं, ऐसे आम उपभोक्ता सामानों की मांग बढ़ रही है और इसलिए ऐसी मेकिंग अप इकाइयों में निवेश की अच्छी गुंजाइश है।
- तकनीकी वस्त्र: तकनीकी वस्त्र भारत में एक नई आगामी शाखा है। आज वस्त्र सामग्री का उपयोग कृषि, ऑटोमोबाइल, उद्योग, खेल, पैकेजिंग, चिकित्सा, सुरक्षा और संरक्षण, आदि जैसे कई क्षेत्रों में किया जा रहा है। ऐसी सामग्रियां तकनीकी वस्त्रों की श्रेणी में आती हैं। यह क्षेत्र बहुत तेजी से पूरी दुनिया में बढ़ रहा है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम स्तर के उद्योगों में इस क्षेत्र में निवेश के कई अवसर हैं। ऐसे उद्योग की मुख्य आवश्यकताएं डिजाइन अभियांत्रिकी और अनुसंधान क्षमताएं हैं।
भारतीय खुदरा उद्योग:
वस्त्र उद्योग का प्रसार करने वाला एक प्रमुख क्षेत्र भारतीय खुदरा बाजार है। भारतीय खुदरा उद्योग स्वर्णिम दौर से गुजर रहा है। खुदरा उद्योग के लिए परिधान और वस्त्र दूसरे सबसे बड़े कमाई वाले उत्पाद हैं। भारत में संगठित खुदरा व्यवसाय बढ़ने और भारतीयों की क्रय शक्ति में वृद्धि के साथ, वस्त्र उद्योग का विस्तार होना तय है। यह भारतीय वस्त्र उद्योग के लिए सुखद है। यह उद्योग घरेलू रूप से 13% की दर से बढ़ा और इससे 5 से 7% की दर से आगे बढ़ने की अपेक्षा है।
निर्यात:
भारतीय निर्मित वस्त्र और हस्तशिल्प कई देशों को निर्यात किए जाते हैं। निर्यात के लिए अमेरिका प्राथमिक बाजार है, लेकिन देशों की कुल संख्या 100 तक है। निर्यात में 41% हिस्सेदारी के साथ रेडीमेड वस्त्र सबसे बड़ा खंड है। कपड़ा मंत्रालय के रिकॉर्ड के अनुसार, भारत ने पिछले साल की तुलना में 7% की वृद्धि के साथ 17 बिलियन अमेरिकी डॉलर का कपड़ा निर्यात किया। कच्चे माल, कुशल श्रम, और अच्छी डिजाइनिंग क्षमताओं की आसान उपलब्धता के कारण भारत को एक कपड़ा केंद्र माना जा रहा है। ह्यूगो, बॉस और डीजल जैसे विश्व प्रसिद्ध लेबल भी भारत से कपड़े आयात कर रहे हैं। इस प्रकार, इस उद्योग से निर्यात लाभ काफी हैं।



