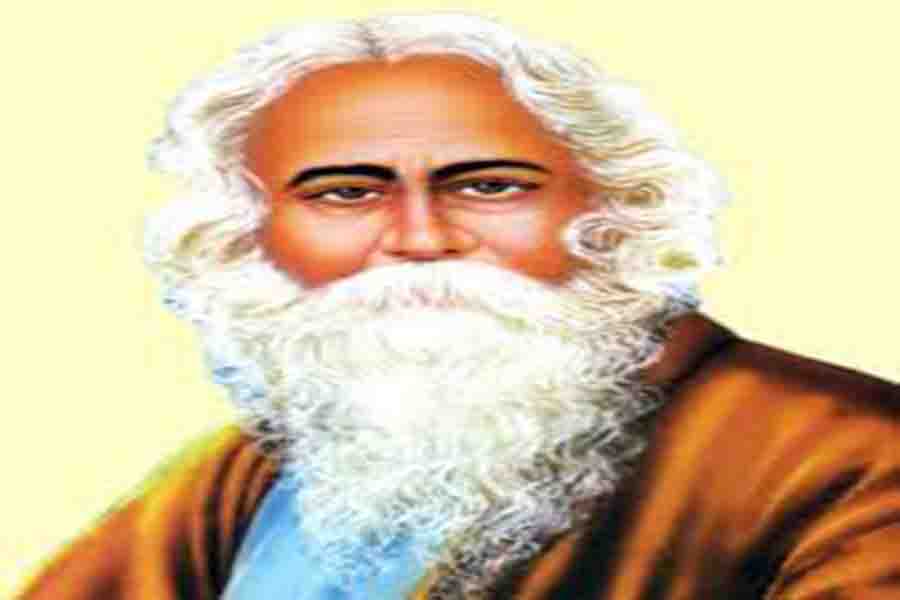स्वयं उत्कृष्ट गायक। समस्त राग – रागिनियों के गहरे जानकार। नई धुनों के सर्जक। चार हज्जार (जी हां, मैं जान -बूझ कर ‘हजार ’ शब्द को ‘हज्जार ’ लिख रहा हूं इस संख्या की विपुलता को रेखांकित करते हुए पाठकों का विशेष ध्यान आकर्षित करने के लिए ) गीतों के शब्द -शिल्पी गीतकार, उनमें से २२३० गीतों के संगीतकार -गायक ; भारतीय शास्त्रीय संगीत, बंगाल का लोक संगीत (बाउल -भाटियाली -कीर्तन आदि ) और विदेशी पाश् चात्य संगीत के समुचित सम्मिश्रण से अपनी एक स्वतंत्र निजी संगीतशैली के सर्जक, जो शैली ‘रवींद्र संगीत ’ के नाम से संसार भर में मान्य -सम्मान्य …
… माफ करें, अगर मैं उन्हें ‘संगीत -सम्राट ’ कहूं, तो क्या कुछ गलत कहूंगा !
लोग या तो सिर्फ गायक होते हैं, या वादक, या फिर सिर्फ धुनों के सर्जक संगीतकार -और यह सब काम भी सिर्फ दर्जनों या सैकड़ों के आंकड़े तक सीमित।
और यहां ? यहां हजारों के पार का आंकड़ा। गायन भी, वादन भी, धुनों की सर्जना भी, गीतों की शब्द -रचना भी, अपनी अलग शैली का निर्माण भी।
और वह भी तब, जब संगीत उनकी कुल प्रतिभा का मात्र एक अंश भर है। वास्तविक प्रतिभा तो काव्य और साहित्य की है। काव्य के ही बल पर तो विश् वकवि माने गए। जबकि मात्र कविता ही नहीं, साहित्य की लगभग सभी विधाओं में पारंगत -कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध -प्रबंध, समीक्षा, संस्मरण, यात्रा -विवरण। इतने तमाम में से सिर्फ कविता -वह भी सिर्फ १०३ गीतों वाला मात्र एक ही संकलन ‘गीतांजली ’ के बल पर विश् व में साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार ‘नोबल ’ ले आए।
कुशल अभिनेता, प्रभावशाली वक्ता, कुशल चित्रकार। मृत्यु के ७५ वर्षों बाद उनकी काव्यकला और संगीतकला की ही तरह उनकी चित्रकला को लेकर भी पूरे विश् व में आश् चर्य मिश्रित मुग्ध प्रशंसाभाव है।
आज लेकिन, उनकी सांगीतिक प्रतिभा के ही बारे में थोड़ी -बहुत चर्चा यहां प्रस्तुत है।
रवींद्र नाथ ठाकुर में कविता की ही तरह संगीत की प्रतिभा भी जन्मगत थी, और थी विपुल -विराट। बचपन से ही गाते थे। सुमधुर स्वर, अत्यंत ही सुरीला, आकर्षक। प्रत्येक बात को बहुत ही गंभीरता से लेने वाले रवींद्र नाथ संगीत की अपनी इस स्वाभाविक -प्राकृतिक प्रतिभा से ही संतुष्ट होकर नहीं रह गए। काव्य -प्रतिभा की ही तरह उन्होंने अपनी संगीत -प्रतिभा को अपने गहन अध्यवसाय से खूब मांजा -चमकाया। सिर्फ गाकर ही संतुष्ट नहीं रहे, संगीत की खूब पढ़ाई भी की। शिक्षण -प्रशिक्षण के साथ ही संगीत पर स्वतंत्र चिंतन -मनन -मंथन भी किया। बाद में इस अध्यवसाय का सुपरिणाम तब देखने में आया, जब अल्प आयु में ही संगीत के विषय में उनके मौलिक विचारों को वह अत्यंत ही आत्मविश् वास के साथ प्रगट करने लगे मात्र २० वर्ष की आयु में रवींद्र नाथ ने एक सार्वजनिक सभा में ‘संगीत और भाव ’ शीर्षक से अपने एक निबंध का पाठ किया। सभा में यदु भट्ट, सुरेंद्र नाथ बंद्योपाध्याय, राम प्रसाद मिश्र, जगत चंद्र गोस्वामी, राधिका प्रसाद गोस्वामी और श्याम सुंदर मिश्र के समान उस जमाने के सिद्ध -प्रसिद्ध गायक -संगीतज्ञ उपस्थित थे। युवा रवींद्र नाथ ने अपने निबंध में जो कुछ कहां, स्वयं गाकर उदाहरण प्रस्तुत करते हुए अपने बातों को प्रमाणित भी किया। सभा में उपस्थित विद्वत्मं : रवींद्र नाथ की काव्य -प्रतिभा से पहले से ही परिचित थी, अब जब उनकी गायन -प्रतिभा को देखा, तो सभा में उपस्थित प्रसिद्ध गायक पंडित यदु भट्ट ने रवींद्र नाथ को इन शब्दों में अभिनंदित किया – ‘वंदे वाल्मीकिकोकिलम् !
वाल्मीकि का काव्य और कोयल की तान एक साथ एक व्यक्तित्व में !
उस छोटी उम्र के पहले ही निबंध में रवींद्र नाथ ने संगीत -प्रस्तुति के बारे में अपने क्रांतिकारी विचार बड़े ही साहस के साथ पेश किए थे। उन्होंने कहा था कि शास्त्रीय गायक अपने स्वर और प्रस्तुति को आकर्षक बनाने का कोई प्रयास ही नहीं करते। तान लगाते समय भाव -भंगिमा हिंसक हो, या ऊपर के स्वर टूटें, खरज के स्वर बिला जाएं, तो भी लज्जित नहीं होते।
रवींद्र नाथ ठाकुर ने समय -समय पर संगीत के बारे में कई लेख लिखे। ‘संगीत और भाव ’, ‘संगीत की उत्पत्ति और उपयोगिता, ’‘संगीत और कविता ’, ‘संगीत की मुक्ति ’ और ‘गान के विषय मेें प्रबंध ’ जैसे अनेक लेख उनके संगीत -ज्ञान की गहराई का पता देते हैं और संगीत के बारे में उनके मौलिक विचारों का प्रतिपादन करते हैं। उनके मे लेख ‘छंद ’, ‘संगीत -चिंता ’ और ‘हमारा संगीत ’ नामक उनके ग्रंथों में संकलित हैं। ये ग्रंथ १९१७ से १९२१ के बीच प्रकाशित हुए, तब रवींद्र नाथ की उम्र ५६ और ६० के बीच थी। वह ८० साल जिए। मैं कहना यह चाह रहा हूं कि अपने विपुल साहित्यिक लेखन (१० विधाओं में १४१ पुस्तकें, जो २७ खंडों में छपीं – १५ कविता संग्रह (१२ हजार कविताएं ), ११ गीत संग्रह (४ हजार गीत ), ४७ नाटक, १३ उपन्यास, १२ कहानी संग्रह, ६ यात्रा -विवरण। लेख -निबंध -आलोचना आदि के ३४ संग्रह। ३ खंडों से आत्मकथा।) के बीच भी वह ६० साल की उम्र तक सिर्फ संगीत पर उतना लिख चुके थे।
उन्होंने बड़े ही साहस के साथ कहा कि शास्त्रीय गायक लोग सिर्फ राग -रागिनियों और सुरों की शुद्धता पर ही ध्यान देते हैं। वे स्वर की मिठास पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। शब्दों के उच्चारणों को भीषण तरीके से बिगाड़ देते हैं। कथ्य और भावार्थ पर ध्यान तो देते ही नहीं, बल्कि उनकी तो हत्या ही कर देते हैं। रवींद्र नाथ को राग -रागिनियों से, सुरों से, उनकी शुद्धता से कोई असहमति नहीं थी। वह तो गायकों के प्रस्तुतिकरण के अद्भुत तौर -तरीकों से असहमत थे। उनका मानना था कि राग भाव चाहे सुख के पेश करते हों या दुख के, मीठे तरीके से ही पेश करने चाहिए, क्योंकि यह संगीत है। यहां मिठास का, शालीनता का, कोमलता का पूरा ध्यान तो रखना ही होगा। टेढ़ी -मेढ़ी मुख भंगिमाएं, गर्दन के झटके, हवा में लहराते -कांपते -मुट्ठियां बांधते हाथ, मटकती आंखें, लंबे -लंबे तानों -आलापों के बीच गीत के शब्दों को गोल -गोल कर खा जाना, गलत -सलत उच्चारण, आधे -अधूरे बोल … क्या हैं ये सब ? सिर्फ राग -रागिनियों को शुद्ध रखने के लिए भाषा की हत्या, शब्दों की हत्या, बोलों की हत्या, भावों की हत्या, गीत की हत्या, अपने रूप की, अपने हावों -भावों की हत्या – क्या है यह ? जो प्रस्तुति बहुत सुंदर, बहुत कोमल, बहुत शालीन हो सकती थी, उसे इतना घनघोर बना देना, संगीत के साथ यह कैसा व्यवहार है ? सरल को जटिल बना देना ! क्यों ऐसा होना चाहिए ? उनका स्पष्ट मानना था कि इन्हीं रूढ़ जटिलताओं के कारण भारतीय शास्त्रीय संगीत लोकप्रिय नहीं हो पाया। उनका कहना था कि संगीत मनोरंजक हो, यह आवश्यक है, किंतु इससे भी ज्यादा जरूरी है कि संगीत श्रोता की आत्मा को सुख, शांति और आनंद प्रदान करे।
यही कारण है कि ‘रवींद्र -संगीत ’ में राग -रागिनियों की मारामारी नहीं। उन्होंने अपने ज्यादातर गीतों को भैरवी, अहीर भैरव, भूपाली, आसावरी, मल्हार और केदार रागों में बांधा। उनके संगीत में ये सभी राग अपनी पूरी शुद्धता के साथ प्रस्तुत होते हैं, लेकिन अत्यंत ही शांतभाव से, शालीनता के साथ, विश् व प्रसिद्ध बंगाली ‘भद्रलोक ’ की भद्रता के साथ। ये सभी राग आराम से उठते हैं, धीमे से उतरते हैं, अहिस्ता से गिरते हैं और धीमी सांसों के साथ दम लेते हुए थमते हैं। अधिकता गीत विलंबित लय में ही बांधे गए हैं। द्रुत लय के गीत भी काफी हैं, पर उनमें उठा -पटक नहीं, तमीजदारी है।
उन्होंने कहा – ‘सुख -दुख के आवेग से हमारे कंठ में जो स्वाभाविक परिवर्तन होते हैं, उन्हीं की चरम अभिव्यक्ति अनुकूल भावों की सांगीतिक प्रस्तुति में होनी चाहिए। सुर -स्वर -राग की शुद्धता तो गौण है। दर असल राग -रागिनी की शुद्धता की जिद संगीत -प्रतिभा के संवर्द्धन में बाधा ही है। ’
उन्होंने कहा – ‘सांगीतिक व्याकरण को यांत्रिकता से मुक्त कराना होगा। ’
और उन्होंने अपने ‘रवींद्र -संगीत ’ में यह करके दिखाया। उन्होंने कहा और अपने सिरजे संगीत में ‘नंदन -तत्व ’ और ‘रंजन -तत्व ’ को अहमीयत दी। उन्होंने अपने रचे गीतों और उन्हें दीं धुनों से यह प्रमाणित किया कि राग के लिए शब्द नहीं, शब्द के लिए राग हैं, और यह भी कि रागों की सार्थकता भावों को प्रगट करने में ही है। बिना भावों को सिद्ध किए रस -निष्पत्ति नहीं हो सकती और यदि रस -निष्पत्ति ही नहीं हुई, तो फिर संगीत की क्या सार्थकता ? क्या आवश्यकता ?
उनकी पुस्तक ‘छिन्न पत्रावली ’ से पता चलता है कि उनके मन में भैरवी, पूरबी, टोड़ी, मुलतानी, भूपाली, रामकेलि और यमन कल्याण राग -रागिनियों के प्रति गहरी रुचि और सम्मान -भाव था।
अपने गीतों को उठापटक, मारामारी और कसरत से बचाने के लिए उन्होंने कुछ नए तालों का आविष्कार किया। आज भारतीय संगीत में रवींद्र नाथ के रचे इन तालों की विशिष्ट जगह है। ये ताल नवपंच, षष्ठी, रुपकड़ा, एकादशी और झंपक ताल के नाम से जाने जाते हैं, अपने संगीत को शोरगुल से बचाने के लिए रवींद्र नाथ ने यह निश् चित कर दिया था कि उनके गीतों के साथ सिर्फ तार -वाद्य (तंबूरा, सारंगी ) और पखावज, मृदंग या खोल ही बजेंगे। उनके अधिकतर गीत ध्रुपद पद्धति में निबद्ध हैं। शांत रस में निमग्न।
रवींद्र नाथ ठाकुर संगीत में पं . विष्णु चक्रवर्ती के शिष्य थे। पं . विष्णु चक्रवर्ती बंगाल के प्रसिद्ध विष्णुपुर संगीत घराने की परंपरा के सार्थक वाहक थे। विष्णुपुर घराने की स्थापना संगीत -सम्राट तानसेन के वंशज उस्ताद बहादुर खान ने की थी।
यह सच है कि ‘रवींद्र -संगीत ’ में भावों और अर्थों की प्रधानता है। गीत की एक -एक पंक्ति और पंक्ति के एक -एक शब्द के अर्थ को अत्यंत ही महत्व दिया गया है। गीत के जो भाव हैं, उन्हीं भावों को महत्व देकर उन्हें उभार कर रस -निष्पत्ति तक ले जाने के ही लिए धुनों का इस्तेमाल किया गया है। भावों की प्रमुखता के ही कारण लोगों को रवींद्र -संगीत में अपने सुखी -दुखी का प्रतिबिंब दिखता और लोगों को उन गीतों से लगाव हो जाता है। भावों तथा अर्थों की प्रमुखता होने के ही कारण लोगों को उन गीतों में अपनी समस्याएं, अपनी हताशाएं या फिर अपनी खुशियां, आकांक्षांए, अपने सपने साफ -साफ दिखाई देते हैं और लोग तुरंत उन गीतों से जुड़ जाते हैं। यही कारण है कि रवींद्र नाथ के गए ७५ साल हो गए (८० वर्ष की उम्र में ७ अगस्त १९४१ में निधन ), लेकिन ‘रवींद्र -संगीत ’ की लोकप्रियता दिनोंदिन बढ़ती ही जाती है। बंगाल के दर्जनों बड़े गायक सिर्फ रवींद्र -संगीत गाकर ही बड़े बने हैं पंकज मल्लिक, के . एल . सहगल, हेमंत कुमार, मन्ना डे, सचिन देवबर्मन, किशोर कुमार, कणिका बंद्योपाध्याय, सुचित्रा मित्र ऐसे ही गायक हैं। कुछ बहुत बड़े गायक तो ऐसे हैं, जिन्होंने जीवन भर सिर्फ और सिर्फ रवींद्र संगीत ही गाया और अमर हो गए। सिर्फ रवींद्र -संगीत गाकर ही जीविका चलाने वाले बंगाल में सैकड़ों गायक हैं। ‘विश् व भारती ’ विश् वविद्यालय से रवींद्र संगीत एम . ए . करने वाले छात्रों की संख्या दिनोंदिन बढ़ती ही जाती है। पूरे बंगाल में ‘रवींद्र संगीत ’ सिखाने के सैकड़ों स्कूल हैं, जो लाखों रुपए कमाते हैं। पूरे भारत के लगभग सभी प्रांतों में रवींद्र संगीत सिखाने वाले स्कूल हैं। मुंबई में तो कई हैं। पुणे में, नागपुर में कई हैं। रवींद्र संगीत के रेकॉडर्स और सीडीज से ग्रामोफोन कंपनी से लेकर तमाम म्यूजिक कंपनियां करोड़ों रुपयों का व्यापार हर साल करती हैं। यह आंकड़ा हर साल बढ़ता जाता है।
इस अपार लोकप्रियता का प्रभाव फिल्मों पर भी पड़ना ही था। तथ्य यह है कि सत्यजित राय से लेकर मृणाल सेन, तरुण मजुमदार, अग्रदूत, वंदना मुखोपाध्याय, अपर्णा सेन, गौतम घोष आदि -आदि कम से कम १३ फिल्म निर्माता -निर्देशक बंगाल में ऐसे हैं, जिन्होंने गुरुदेव की कहानियों -उपन्यासों पर फिल्में बनाईं, तो उन फिल्मों के सारे गीत ‘रवींद्र संगीत ’ से ही लिए। जो बांग्ला फिल्में रवींद्र नाथ की कथानों पर नहीं बनीं – आज के लेखकों की कहानियां पर बनीं वहां भी कई जगह रवींद्र -संगीत का ही कोई गीत काम आया, और वह बहुत सफल रहा।
बांग्ला फिल्मों के बहुत सफल और लोकप्रिय गीतकार थे पुलक बंद्योपाध्याय और गौरीप्रसन्न मजुमदार। दोनों ने पैंतीस -चालीस वर्षोतक कितनी ही सुपर -डुपर हिट बांग्ला फिल्मों के गीत लिखे। काल के नियमानुसार अपनी -अपनी पारी सफलतापूर्वक पूर्ण करके अपने -अपने समय पर जब एक -एक कर दोनों का प्रयाण हुआ, तो उसके कुछ दिनों बाद मुंबई के एक कार्यक्रम में मेरी भेंट हिंदी फिल्मों के सफल गीतकार आनंद बख्शी से हुई। उन्होंने पूछा – ‘पुलक दा और गौरी दा तो चले गए। आजकल बांग्ला फिल्मों में गाने कौन लिख रहा है ? ’ मेरा जवाब था – ‘जब दोनों थे, तब भी, और आज जब दोनों नहीं हैं, तो अब भी, बांग्ला फिल्मों के एवरग्रीन सफलतम और लोकप्रियतम गीतकार तो रवींद्र नाथ ठाकुर ही हैं।
और हिंदी फिल्में ? लंबी सूची है। सिर्फ कुछ ही का जिक्र कर रहा हूं। इसी से पता चल जाएगा कि गुरुदेव संगीत के कितने बड़े गुरु हैं। डेढ़ सौ साल (जन्म १८६१ ) पुराना यह संगीतकार कितना आधुनिक है।
सचिन देवबर्मन, हेमंत कुमार, अनिल विश् वास, कल्याणजी -आनंदजी, बप्पी लाहिड़ी, राजेश रोशन, राहुल देवबर्मन जैसे अनेक गुणी -ज्ञानी संगीतकारों ने हिंदी फिल्मों के अपने संगीत में जरूरत पड़ने पर गुरुदेव की धुनों का खूबसूरत इस्तेमाल किया। सूची देखकर आप जान जाएंगे कि गुरुदेव की धुनों पर बने हिंदी फिल्मों के ये गीत कितने लोकप्रिय हुए। इन गीतों का शुमार हिंदी फिल्मों के स्वर्ण युग के सदाबहार गीतों में होता है।
१ . मेरा सुंदर सपना बीत गया … (गायिका – गीता दत्त, संगीतकार -सचिन देवबर्मन, फिल्म – दो भाई, गुरुदेव का गीत – ओ जे माने ना माना )
२ . जाएं तो जाएं कहां …. (गायक – गायिका – तलत महमूद -लता मंगेशकर, संगीतकार – सचिन देवबर्मन, फिल्म – टैक्सी ड्राइवर, गुरुदेव का गीत – हे क्षणिकेर अतिथि )
३ . राही मतवाले … (गायक – तलत महमूद, संगीतकार – सचिन देवबर्मन, फिल्म – टैक्सी ड्राइवर, गुरुदेव का गीत – ओ रे गृहवासी )
४ . जलते हैं जिसके लिए … (गायक – तलत महमूद, संगीतकार – सचिन देवबर्मन, फिल्म – सुजाता, गुरुदेव का गीत – एकदा तुमि प्रिय )
५ . नैना दीवाने बतियां न माने … (गायिका – सुरैया, संगीतकार – सचिन देवबर्मन, फिल्म -, गुरुदेव का गीत – शे दिन दुजोने )
६ . तेरे मेरे मिलन की ये रैना … (गायक -गायिका – किशोर कुमार -लता मंगेशकर, संगीतकार – सचिन देवबर्मन, फिल्म – अभिमान, गुरुदेव का गीत – जोदी तारे नाइ चिनी गो शे दिन )
७ . मन मेरा उड़ता जाए बादल के संग दूर गगन में … (गायक -गायिका – हेमंत कुमार -लता मंगेशकर, संगीतकार – हेमंत कुमार, फिल्म – मां -बेटा, गुरुदेव का गीत – मन मोर मेधेर संगी, टिप्पणी : इस हिंदी गीत के बोल भी गुरुदेव के बांग्ला गीत का अनुवाद है।)
८ . नन्हा सा पंछी रे तू … (बप्पी लाहिड़ी, फिल्म – टूटे खिलौने, गुरुदेव का गीत – मेंगे मोर घरेर चाभी )
९ . छूकर मेरे मन को किया तूने जो इशारा … (गायक – किशोर कुमार, संगीतकार – बप्पी लाहिड़ी, फिल्म – याराना, गुरुदेव का गीत – आमार होलो शुरु )
१० . प्यार हुआ चुपके से … (गायक -गायिका – कुमार सानू -कविता कृष्णमूर्ति, संगीतकार – राहुल देवबर्मन, फिल्म – लव स्टोरी १९४७, गुरुदेव का गीत – एशो श्यामल सुंदर )
११ . नाना पाटेकर अभिनीत फिल्म ‘युगपुरुष ’ के सभी ८ गीतों की धुनें गुरुदेव की सिरजी धुनें हैं। कोई फेर -बदल नहीं है। संगीतकार हैं राजेश रोशन। इस फिल्म के २ गीत याद आ रहे हैं :
१ . कोई जैसे मेरे दिल का तार … (गुरुदेव का गीत – ‘तुमी कैमोन कोरे गान ’) २ . बंधन खुला पंछी उड़ा … (पांगला हावा बादल दिने ) के साथ शायद शत्रुघ्न सिन्हा थे। फिल्म के संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। पूरी फिल्म में बार -बार एक प्रसंग आता है कि धर्मेंद्र अपने पुराने दिनों की याद में खोकर माउथ ऑर्गन पर एक बहुत ही मार्मिक धुन बजाते हैं। वह धुन गुरुदेव की धुन है। गीत है – ‘पुरानो शेई दिनेर कथा ’, गुरुदेव के इस गीत के बोल के अर्थ हैं – उन पुराने दिनों की बातों को क्या कभी भूला जा सकता है ?
मैं फिल्मों का बिलकुल भी जानकार नहीं। सूची अधूरी ही दे पाया हूं। फिल्मों में रुचि रखने वाला कोई शोधार्थी हिंदी फिल्मों में गुरुदेव के अवदानों पर यदि शोधकार्य करे, तो वह एक पूरी पुस्तक हो सकती है। हिंदी फिल्म संगीत के साथ ही गुरुदेव की कितनी ही कहानियां -उपन्यासों पर भी तो हिंदी फिल्में बनी हैं। भारत के दो साहित्यकार, जिनकी कथाओं पर बांग्ला -हिंदी सहित विभिन्न भारतीय भाषाओं की सबसे ज़्यादा फिल्में बनी हैं, वे हैं गुरुदेव रवींद्र नाथ ठाकुर और अमर कथाशिल्पी शरतचंद्र चटोपाध्याय। यह अद्भुत सुंदर संयोग ही है कि शरतचंद्र भी उत्कृष्ट गायक थे।