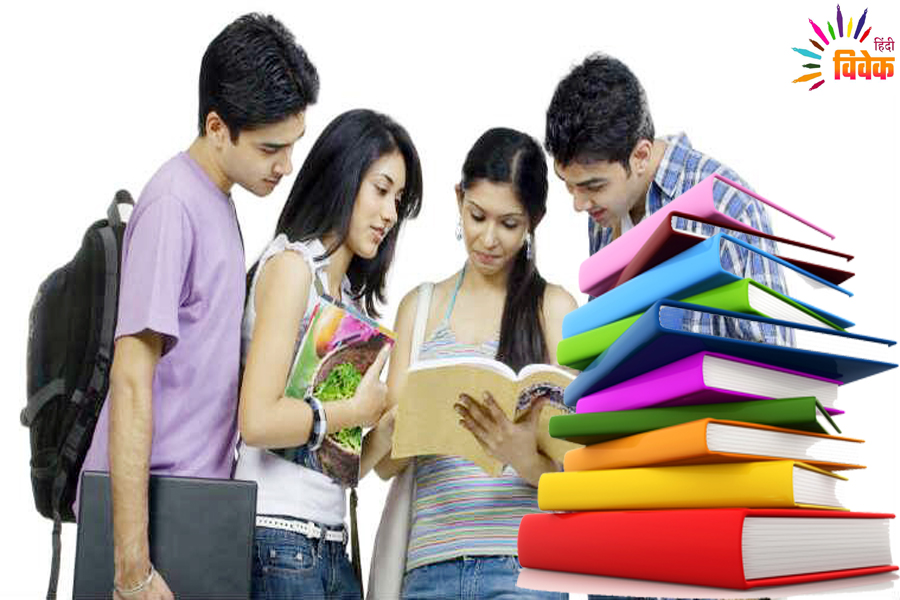दरअसल अब नई शिक्षा नीति के अंतर्गत वास्तव में राष्ट्र की लुप्त कर दी गई सांस्कृतिक संपदा के महत्व को अंगीकार करते हुए ज्ञान, कर्म, संस्कार, भाषा, संस्कृति और कौशल दक्षता को विद्यार्थी में विकसित करने का काम मातृभाषाएं करेंगी। मानव को मानवीय बनाने के यही मानविकी विषय हैं। व्यक्तित्व निर्माण की यही परिकल्पना व्यक्ति में राष्ट्रबोध का प्रादुर्भाव करती है। मूल्य-बोध के इन संस्कारों से संपूर्ण राष्ट्र में सांस्कृतिक चेतना का लोकव्यापीकरण होगा और सनातन मानवीय मूल्यों की सुरक्षा होगी। यही मूल्य न केवल व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाएंगे, बल्कि देश को भी आत्मनिर्भता के शिखर पर पहुंचाएंगे।
नई शिक्षा नीति के चलन में आने के बाद मातृभाषाओं में शिक्षा की जो सर्वश्रेष्ठ देन होगी, वह नागरिक में राष्ट्रबोध जगाने के साथ उसका व्यक्ति के स्तर पर भारतीयकरण करना। कल का विद्यार्थी ही कालांतर में देश का नागरिक होता है। दरअसल अब नई शिक्षा नीति के अंतर्गत वास्तव में राष्ट्र की लुप्त कर दी गई सांस्कृतिक संपदा के महत्व को अंगीकार करते हुए ज्ञान, कर्म, संस्कार, भाषा, संस्कृति और कौशल दक्षता को विद्यार्थी में विकसित करने का काम मातृभाषाएं करेंगी। मानव को मानवीय बनाने के यही मानविकी विषय हैं। व्यक्तित्व निर्माण की यही परिकल्पना व्यक्ति में राष्ट्रबोध का प्रादुर्भाव करती है। मूल्य-बोध के इन संस्कारों से संपुर्ण राष्ट्र में सांस्कृतिक चेतना का लोकव्यापीकरण होगा और सनातन मानवीय मूल्यों की सुरक्षा होगी। यही मूल्य न केवल व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाएंगे, बल्कि देश को भी आत्मनिर्भरता के शिखर पर पहुंचाएंगे। देश की सांस्कृतिक संप्रभुता की पहचान को भी अक्षुण्ण बनाए रखने का काम करेंगे। कोरोना महामारी के दंश ने भी पुरातन मूल्यों को अपनाने का संदेश दिया है। योग, आयुर्वेद्र और भारतीय ज्ञान-परंपरा में अंतनिर्हित मूल्यों को भी समझने का रास्ता इस संकट ने खोला है। एकल परिवारों की अवधारणा कौटुम्बिक महत्ता को जानने को उत्सुक हुई है। यही सब वे मूल्य थे, जिन्हें औपनिवेशिक अंग्रेजी शिक्षा ने सुनियोजित ढंग से पृथक किया और भारतीय नागरिक भारतीय सनातन मूल्यों को भूलता चला गया।
भारत में अंगे्रजों का शासन स्थापित होने के बाद एक समय तक अंग्रेजों की भाषा-नीति में बदलाव होता रहता था। सन् 1833 में मैकाले मिनिट्स के होते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी ने अदालती तथा अन्य शासकीय कार्यों में अरबी-फरसी का मिश्रित रूप अपनाया था। हिंदू राजाओं के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी अपने पत्र-व्यवहार में स्थानीय बोलियों के शब्दों का भी प्रयोग करती थी। सन् 1880 में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई। उस समय अंग्रेजी शासन की राजधानी कलकत्ता थी। जॉन ग्रिलक्राइस्ट उस कॉलेज के भाषा विभाग के अध्यक्ष बनाए गए। उन्होंने खड़ी बोली के प्रयोग को प्रोत्साहित किया और कंपनी सरकार की भाषा नीति तय करने में आवश्यक सुझाव दिए। वह हिंदी को हिंदुई तथा हिंदुस्तान कहते थे और उसके लिए रोमन लिपि को आवश्यक मानते थे, किंतु न तो हिंदी का नाम बदल सके और न ही लिपि। देवनागरी लिपि से संबंधित हिंदी का संघर्ष सफल रहा। गिलक्राइस्ट के बाद मैकाले की भाषा-नीति मानी गई और उच्च शिक्षा से संस्कृत एवं हिंदी का माध्यम समाप्त कर दिया गया। उन्नीसवीं शताब्दी के चौथे दशक में सरकारी कामकाज में उर्दू को वरीयता दी गई और हिंदी को उपेक्षित कर दिया गया। उस युग में बनारस हिंदी का केंद्र था और बनारस की दो बड़ी हस्तियां हिंदी में लिख रहीं थीं। एक थे राजा शिवप्रसाद ’सितारे हिंद’ और दूसरे भरतेंदु हरिशचंद्र। राजा शिवप्रसाद अंग्रेजी सरकार की सेवा में थे और अंग्रेजों की भाषा नीति का समर्थन करते हुए उन्होंने उर्दू का पक्ष लेते हुए हिंदी की निंदा की। उनकी वफादारी देखकर सरकार ने उन्हें ’सितारे हिंद’ की उपाधि दी। हरिशचंद्र ने सरकार की भाषा-नीति का विरोध किया और जगह-जगह जाकर हिंदी के समर्थन में सभाएं कीं। जनता ने हरिशचंद्र को ’भारतेंदु’ की उपाधि से विभूषित किया। भारतेंदु की लोकप्रियता के सामने सितारे हिंद अस्त-पस्त हो गए। जॉन गिलक्राइस्ट जैसे अनेक अंग्रेज हिंदी के समर्थक थे। ऐसे अंग्रेजों में हेनरी पिनकोट ने भारतेंदु के समर्थन में हिंदी के पक्ष में बहुत काम किया। राजा शिवप्रसाद की तरह राजा लक्ष्मण सिंह (1826-96) भी सरकारी नौकर थे, किंतु उन्होंने हिंदी का समर्थन किया और उसी में लिखा भी।
इस दौरान देश में जो विवि और राज्यस्तरीय शिक्षा मंडल अस्तित्व में आए, उन्होंने अंग्रेजी विषयक पाठ्यक्रमों में आंग्ल साहित्य का अध्ययन, अध्यापन बीसवीं सदी की शुरूआत में ही कर दिया था। इस समय भारतीय लेखक जो भी कुछ अंग्रेजी में लिख रहे थे, उसे पाठ्यक्रम में शामिल कर दिया गया। इनमें ज्यादातर लेखक बंगाली थे और इन पाठ्यक्रमों की शुरूआत भी बंगाल में हुई। इन लेखकों की लिखने की पद्धति लगभग अंग्रेजियत में सराबोर थी। चारण-भाटों की शैली में इन्होंने अंग्रेजी का स्तुतिगान तो किया ही, तात्कालिक लाभ के लिए इनमें से कई क्रिश्चियन भी हो गए। भारत की धरती पर अंग्रेजी का बीज बोने और इसे उर्वरा बनाने के पैरोकार मैकाले ने ऐसे लोगों को वजीफे दिलाए और लंदन की मुफ्त में सैर भी कराई। सही मायनों में ये तथाकथित अंग्रेजी के लेखक इंग्लैंड के बंधुआ साहित्यकार थे। इन्होंने अंग्रेजी के प्रभुत्व को स्थापित करने के उपायों के साथ विस्तार के मार्ग भी प्रशस्त किए। इनमें तोरूदत्त, माइकल, मधुसूदन दत्त और मनमोहन घोष प्रमुख थे। गोया, ब्रिटिश हुक्मरानों के भय के चलते इन बंधुआओं से लेखन में भारतीयता का प्रभाव डालने की उम्म्ीद कतई नहीं की जा सकती थी। जिस राष्ट्रीय चेतना को हम स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में लेते हैं, उस तरह के लेखन का भारतीय अंग्रेजी लेखकों में सर्वथा अभाव था। हालांकि ‘वंदे मातरम’ गीत के रूप में भारत को उसकी व्यापक राष्ट्रीयता की पहचान देने वाले महान बंगला उपन्यासकार बंकिमचंद्र चटर्जी न केवल बंगाल के चुनिंदा लेखकों में से एक थे, बल्कि उन्हें भारतीय अंग्रेजी साहित्य के शुरूआती लेखन का श्रेय भी जाता है। उन्होंने ‘राजमोहन वाइफ’ उपन्यास अंग्रेजी में लिखा था। किंतु राष्ट्रीय स्वाभिमान के चलते कालांतर में उन्होंने केवल बंगला और संस्कृत में लिखने का संकल्प लिया और फिर अंग्रेजी में रचना-सृजन पर विराम लगा दिया। भाषाई अस्मिता और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के प्रकल्प का ऐसा अनूठा संकल्प था, जिसने वंदे मातरम के माध्यम से फिरंगी सत्ता को चुनौती देते हुए जनमानस में सर्वाधिक राष्ट्रबोध जगाने का काम किया।
 साहित्य, मानविकी और मानवाधिकार विषयों का अध्ययन-अध्यापन व्यक्ति में वैचारिक उर्जा पैदा करने का काम करते हैं। इनके पढ़ने से इच्छाशक्ति प्रबल होती है। लेकिन 1991 में लाए गए भूमण्डलीय आर्थिक उदारवाद के बाद जिस बेतुके ढंग से शिक्षा संस्थानों का व्यवसायीकरण हुआ और साहित्य व मानविकी विषयों को भी जिस बेढंगेपन से रोजगारोन्मुखी बनाने की कोशिशें हुईं, इससे शिक्षा के मूल पर आघात हुआ। विश्वविद्यालय अप्रजातांत्रिक हो गए। शिक्षा परिसरों में व्यावसायिक स्थापना के लिए थाने तक खोलने पड़े। जाहिर है, ये उपाय शिक्षा के लोकव्यापीकरण, शिक्षा में गुणवत्ता लाने अथवा छात्र के चरित्र निर्माण की दृष्टिगत नहीं किए गए, बल्कि शिक्षा को औद्योगिक उत्पाद बना देने के लिए हुए।
साहित्य, मानविकी और मानवाधिकार विषयों का अध्ययन-अध्यापन व्यक्ति में वैचारिक उर्जा पैदा करने का काम करते हैं। इनके पढ़ने से इच्छाशक्ति प्रबल होती है। लेकिन 1991 में लाए गए भूमण्डलीय आर्थिक उदारवाद के बाद जिस बेतुके ढंग से शिक्षा संस्थानों का व्यवसायीकरण हुआ और साहित्य व मानविकी विषयों को भी जिस बेढंगेपन से रोजगारोन्मुखी बनाने की कोशिशें हुईं, इससे शिक्षा के मूल पर आघात हुआ। विश्वविद्यालय अप्रजातांत्रिक हो गए। शिक्षा परिसरों में व्यावसायिक स्थापना के लिए थाने तक खोलने पड़े। जाहिर है, ये उपाय शिक्षा के लोकव्यापीकरण, शिक्षा में गुणवत्ता लाने अथवा छात्र के चरित्र निर्माण की दृष्टिगत नहीं किए गए, बल्कि शिक्षा को औद्योगिक उत्पाद बना देने के लिए हुए।
मनुष्य का सशक्तिकरण, जीवनस्तर में सुधार और निर्णय लेने की प्रक्रिया में शिक्षा की सबसे अहं भूमिका है। मानविकी और मानवाधिकार शिक्षा के वास्तविक अर्थ अपने इतिहास, भूगोल, भाषा और लोक व्यवहार के परिप्रेक्ष्य में समाज और सामाजिक समस्याओं को जानना है। तत्पश्चात उन्हें लोक व्यवहार में अपनाना और उनके वैधानिक निदान तलाशना है। जिससे समाज में समरसता बढ़े और उसका लोकतांत्रिक नजरिया मुखर हो। महात्मा गांधी ने कहा था कि ‘कोई समुदाय तभी लोकतांत्रिक हो सकता है, जब समुदाय के सबसे कमजोर व्यक्ति को सर्वोच्च नागरिक जैसे सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक अधिकार मिलें।’ लेकिन आर्थिक उदारवादी नीतियां लागू होने के बाद देश में आवारा पूंजी का दबाव इस हद तक बढ़ा कि हम पूंजी आधारित लिप्सा और औपनिवेशिक शक्तियों की व्यवस्था को विकास व प्रगति का आदर्श मानक मानने लगे। नतीजतन आर्थिक विसंगति बढ़ी और असंतोष उपजा। माओवाद बनाम नक्सलवाद की जड़ें गहरी करने में इस असंतोष ने उर्जा का काम किया। वामपंथी चरमपंथ ने इस असंतोष को अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए भुनाने का काम किया।
समरसता व समावेशन संबंधी जो मूल अवधारणाएं हैं, वे सभी हमारे आधुनिक और प्रगतिशील माने जाने वाले संविधान में परिभाषित हैं। उनका उल्लंघन होने पर एक कानूनी प्रक्रिया से गुजरने के बाद दंड का समुचित विधान है। बावजूद 73 सालों में हम एक समान समाज की संरचना करने की बजाय विषमता और वैमनस्यतापूर्ण समाज की रचना करने में लगे रहे। जबकि नागरिक समाज में हमें संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार हासिल करने की सैद्धांतिकी लगातार पढ़ाई जा रही है। आज यदि हम इस कथित नागरिक संहिता द्वारा निर्मित पीढ़ी का तटस्थ मूल्यांकन करें तो हमें यह पूरी की पूरी पीढ़ी संकीर्ण, जातीय और सांप्रदायिक संस्कारों में जकड़ी नजर आती है। त्याग, संवेदनशीलता, अपरिग्रह और परोपकार की बजाय यह पीढ़ी संवेदनशून्यता, स्वार्थ और धनलिप्सा में ज्यादा जकड़ी है। दरअसल कल्याणकारी संस्कार पाठ्यक्रमों में निहित सूचनात्मक संदेशों या उपदेशों की बजाय समाज में मौजूद उदात्त वातावरण से ग्रहण किए जाते हैं। ऐसे में मातृभाषा, साहित्य और मानविकी विषयों के अध्ययन हमारे भीतर वैचारिक उर्जा का संचयन करते हैं और इससे उपजी आंतरिक शक्ति हमें समरस समाज बनाने की अंतःप्रेरणा देती है। राजनीतिक चेतना के विकास में भी यह उर्जा संवाहक का काम करती है। लेकिन विचार स्वातंत्र्य को यदि खूंटी से बांध दिया जाएगा तो बौद्धिक-एकरूपता के खतरे बढ़ जाएंगे। अंततः भूमण्डलीय आर्थिकी ने इसी एकरुपता को आगे बढ़ाने का काम किया है, जो अब नई शिक्षा नीति में उल्लेखित मातृभाषाओं के प्रावधानों से खंडित होना तय है।
दरअसल विचार-निर्माण के लिए शैक्षिक परिसरों में लोकतांत्रिक खुलेपन की जरुरत है, जिससे शिष्य, शिक्षक से प्रश्न करने में कोई संकोच न करे। दुर्भाग्यवश हमने आज्ञाकारी शिष्य को आदर्श माना हुआ है। यह आज्ञाकारिता नव-सृजनशीलता के लिए बाधक है। यही कारण है कि हम नवोन्वेष, वैज्ञानिक अनुसंधान और देशज उत्पादकता में पिछड़ते जा रहे हैं। हमारी पूरा शिक्षाजन्य ढांचा, आज्ञापालन को प्रोत्साहित व पुरस्कृत करता है। स्वंतत्र्य-चेता विद्यार्थी की नूतन पहल, जिज्ञासा और प्रश्नाकूलता को फटकारा जाता है। विचार नियंत्रण की यह क्रूरता नव-सर्जक की भ्रूण-हत्या कर देती है। यही कारण है कि हम आजादी के इन 73 सालों में न तो नचिकेता, अष्टावक्र और विवेकानंद पैदा कर पाए और न ही सीवी रमन, जगदीशचंद्र बासु और रामानुजन ?
दरअसल औपनिवैशिक शिक्षा पद्धति और अंग्रेजी की अनिवार्यता के चलते हमारे शिक्षा संस्थान महज डिग्रीधारी नकलचियों की फौज खड़ी करने में लगे हैं। वे रोबोट और क्लोन बनाने की दक्षता को ही श्रेष्ठता का पर्याय मानकर चल रहे हैं, क्योंकि रोबोट विरोध नहीं करते और क्लोन से विकसित प्राणी प्रकृति प्रदत्त विलक्षणता खो देते हैं, अतएव उनकी मौलिक सृजनशीलता बचपने में ही कुंठित हो जाती है। आज्ञापालकों के ये उत्पाद अंततः सृजन से जुड़ी वैचारिकता के लिए आघातकारी सिद्ध होते हैं, केवल कैरियर बनाना और पैसा कमाना इनका मुख्य ध्येय रह जाता है। शिक्षा में भारतीयकरण के नए उपायों से वे सब मिथक टूटेंगे, जो अंग्रेजी की अनिवार्यता के लिए गढ़े गए थे।