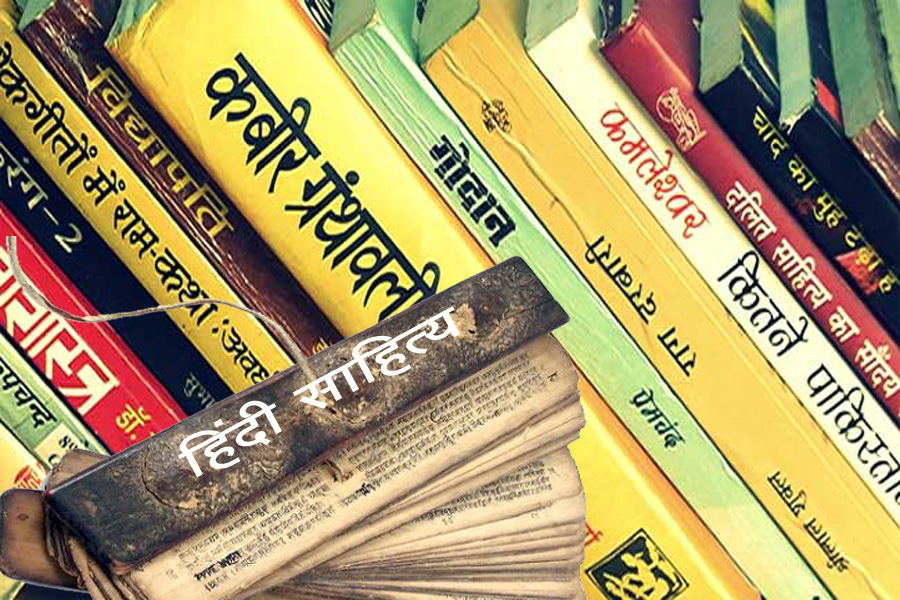साहित्य का काम होता है समाज को योग्य दिशा देना तथा उसकी बुराइयों को शीशे की ही भांति उसे दिखाना परंतु साहित्यिक अखाड़ों की गोलबंदी ने उसका काफी नुकसान किया है। वैसे तो हर युग में बड़े साहित्यकारों को इनकी क्षुद्र मानसिकता का सामना करना पड़ा है लेकिन वर्तमान समय में यह प्रवृत्ति काफी बढ़ गई है।
र्तमान हिंदी साहित्य का विषय वैविध्यपूर्ण है किंतु दिशा स्पष्ट नहीं है। सुकवि, अकवि और महाकवि का मानक बदलता-सा प्रतीत होता है। गुटबंदियों एवं वैचारिक हदबंदियों की चारदीवारी में ऐसा साहित्य प्रकाश में नहीं आ सकता जिसमें जीवन टिमटिमाता हो। मानव-पीड़ा के साथ-साथ ब्रह्मांड की वेदना भी शामिल की गई हो। सामर्थ्य और प्रभाव के बल पर घटिया साहित्य दीप्त है। अधिकृत विद्वान भी उसी को स्वीकार किया जाता है जो किसी खास विचारधारा का पोषक एवं प्रचारक हो। उसके जय जयकार में पूरी व्यवस्था लग जाती है। यहां तक कि साहित्यिक धर्मांतरण भी धड़ल्ले से किया जाता है। यदि कोई रचनाकार अपने सिद्धांतों पर कायम रहता है तो उसे एकांतवासी बना दिया जाता है। सम्बंधित विचारधारा वाले मंच, माइक, पद, प्रतिष्ठा और पुरस्कार से अलंकृत होते हैं।
हिंदी साहित्य का वर्तमान परिदृश्य संतोषप्रद नहीं कहा जा सकता। बाजारवाद की श्यामलता लेखकों-प्रकाशकों के चरित्र को प्रभावित कर रही है। एक तरफ तथाकथित बुद्धिजीवी लेखक बड़े प्रकाशकों के लिए एजेंट बने हैं तो दूसरी ओर अपने जीवन की उत्तर अवस्था में कतिपय साहित्यकार बड़े प्रकाशकों के चंगुल में पड़े छटपटा रहे हैं। पिछले दिनों हिंदी के वरिष्ठ लेखक विनोद कुमार शुक्ल (जिनकी उम्र लगभग 85 वर्ष है) ने लेखक/अभिनेता मानव कौल को यह बताया कि छह वर्षों से लगातार लिखित और मौखिक रूप से मना करने के बावजूद प्रकाशक उनकी किताबें छापता जा रहा है। एक प्रकाशक ने पिछले 25 वर्षों में 5000 प्रति वर्ष के हिसाब से 3 किताबों की रॉयल्टी दी है जबकि दूसरे प्रकाशक ने 6 किताबों के एवज में विगत 4 वर्षों में 17000 वार्षिक राशि भेजी है। यह झूठा हिसाब है, क्योंकि उनकी किताबें हिंदी पाठकों,अध्येताओं और छात्रों में काफी लोकप्रिय हैं।
हिंदी के साहित्य जगत में सरकारी पुरस्कारों के लिए प्रायोजित रणनीतियां इन दिनों बड़ी कारगर हैं। पुस्तक लेखन से लेकर लोकार्पण एवं राष्ट्रीय स्तर की पत्र-पत्रिकाओं में समीक्षाओं के प्रकाशन तक सभी पूर्व निर्धारित। बस, जित देखा तित तू ही तू है। ये सभी हथकंडे व्यक्ति विशेष, संगठन अथवा विचारधारा का तो भला कर सकते हैं किंतु साहित्य का कतई नहीं। संजय कुंदन ने ठीक ही लिखा है, जो दिलाए पुरस्कार/ जो बिकवाए किताब/ वह सुकवि/ जो दिलवाए नौकरी/ वह महाकवि। राजनीति की तरह साहित्य में भी बयानबाजी (मौखिक/लिखित दोनों) चलती रहती है। गुटबंदी से अलग मात्र रचनाशीलता को रेखांकित करने वाली साहित्यिक पत्रिका ‘दस्तावेज’ पर ‘ठंडी’ होने का आरोप लगाया गया। परिणामस्वरूप दस्तावेज के यशस्वी संपादक डॉ. विश्वनाथ प्रसाद तिवारी ने लिखा, गरम और आक्रामक होना तथा हिंसा और दूसरों का मांस भक्षण करना ऐसे लोगों की नजर में संभवतः सद्गुण हो। ‘दस्तावेज’, इन सबसे दूर चुपचाप अपना काम करती रही।
दूसरी ओर साहित्यिक मठाधीश, जो नीति और नियति-नियंता हैं, नवांकुरों को पनपने नहीं देते। उनके दरबार में हमेशा काटने-उखाड़ने की बात होती है। जीवन की सूक्ष्म धड़कनों को पकड़ने वाला आज का कवि भली भांति जानता है :
खेसाड़ी दाल की तरह निंदित
उखाड़ कर फेंक दिया जाऊंगा
भारतीय कविता के क्षेत्र से क्योंकि अब
इतिहास के गति के भरोसे न बैठ
इतिहास की मति बदलने की तकनीक है
उनकी मुट्ठी में खो जाऊंगा
जिस तरह खो गई है
बटलोई में दाल चुरने की सुगंध
अधिकतर घरों में
– ज्ञानेन्द्रपति
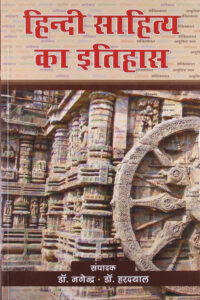 वर्तमान परिदृश्य में गम्भीर लेखन कम हो रहा है। उतराई मछलियों की तरह सोशल मीडिया पर अनगिनत रचनाकार सक्रिय हैं। पसंद एवं सकारात्मक प्रतिक्रिया के लिए इंस्टा, फेसबुक आदि मंचों पर धड़ल्ले से अधकचरी रचनाओं को साझा किया जा रहा है। ऐसी स्तरहीन रचनाओं को सोशल मीडिया पर बड़ी संख्या में लोग सराह भी रहे हैं। वायरल सेलिब्रेटी बनने की हड़बड़ी है। ऐसे में पुस्तक-संस्कृति खतरे में है। कुछ पाश्चात्य विचारकों ने भविष्यवाणी भी की है कि आने वाले 50 वर्षों में पुस्तक-संस्कृति समाप्त हो जाएगी। विगत कई दशकों से इन पर हमले हो रहे हैं। इनका सबसे बड़ा अहित बाजार ने किया अब रही – सही कसर सोशल मीडिया पूरा कर रही है। वर्तमान की क्षणिक-जीवी दौड़ में बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक शामिल होना चाहते हैं। पुस्तकों से दूरी बढ़ रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि पुस्तक-युग समाप्त होने के कगार पर है। इस आहट को कई समर्थ रचनाकारों ने महसूस किया है। किसी कवि ने ’पुस्तक’ शीर्षक कविता में ठीक ही लिखा है, जहां भी रख दें वे/पड़ी रहना इंतजार में/आएगा कोई न कोई/दिग्भ्रमित बालक जरूर/किसी शताब्दी में/अंधेरे में टटोलता अपनी राह/स्पर्श से पहचान लेना उसे/आहिस्ते – आहिस्ते खोलना अपना हृदय/जिसमें सोया है अनंत समय/और थका हुआ सत्य/और गूंगा प्यार /दुश्मनों के जासूस/पकड़ नहीं सके जिसे। दूसरी ओर कुछ भारतीय विद्वानों का मानना है कि पुस्तकें बची रहेंगी। इसमें से गुजरते हुए हम मनचाहा ठहराव ले सकते हैं। इनसे सुख-दुःख साझा कर सकते हैं। भागने या भगा देने की असंवेदनशीलता नहीं है यहां। रस्किन बॉन्ड ने तो लिखा है कि पुस्तकें मेरी दुनिया हैं। मैं इनके बीच ही रहना चाहता हूं। हमारी संस्कृति में अक्षर को ब्रह्म माना गया है क्योंकि यह क्षरित नहीं होता। इसकी सत्ता अनंतकाल से चली आई है और भविष्य में भी बनी रहेगी।
वर्तमान परिदृश्य में गम्भीर लेखन कम हो रहा है। उतराई मछलियों की तरह सोशल मीडिया पर अनगिनत रचनाकार सक्रिय हैं। पसंद एवं सकारात्मक प्रतिक्रिया के लिए इंस्टा, फेसबुक आदि मंचों पर धड़ल्ले से अधकचरी रचनाओं को साझा किया जा रहा है। ऐसी स्तरहीन रचनाओं को सोशल मीडिया पर बड़ी संख्या में लोग सराह भी रहे हैं। वायरल सेलिब्रेटी बनने की हड़बड़ी है। ऐसे में पुस्तक-संस्कृति खतरे में है। कुछ पाश्चात्य विचारकों ने भविष्यवाणी भी की है कि आने वाले 50 वर्षों में पुस्तक-संस्कृति समाप्त हो जाएगी। विगत कई दशकों से इन पर हमले हो रहे हैं। इनका सबसे बड़ा अहित बाजार ने किया अब रही – सही कसर सोशल मीडिया पूरा कर रही है। वर्तमान की क्षणिक-जीवी दौड़ में बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक शामिल होना चाहते हैं। पुस्तकों से दूरी बढ़ रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि पुस्तक-युग समाप्त होने के कगार पर है। इस आहट को कई समर्थ रचनाकारों ने महसूस किया है। किसी कवि ने ’पुस्तक’ शीर्षक कविता में ठीक ही लिखा है, जहां भी रख दें वे/पड़ी रहना इंतजार में/आएगा कोई न कोई/दिग्भ्रमित बालक जरूर/किसी शताब्दी में/अंधेरे में टटोलता अपनी राह/स्पर्श से पहचान लेना उसे/आहिस्ते – आहिस्ते खोलना अपना हृदय/जिसमें सोया है अनंत समय/और थका हुआ सत्य/और गूंगा प्यार /दुश्मनों के जासूस/पकड़ नहीं सके जिसे। दूसरी ओर कुछ भारतीय विद्वानों का मानना है कि पुस्तकें बची रहेंगी। इसमें से गुजरते हुए हम मनचाहा ठहराव ले सकते हैं। इनसे सुख-दुःख साझा कर सकते हैं। भागने या भगा देने की असंवेदनशीलता नहीं है यहां। रस्किन बॉन्ड ने तो लिखा है कि पुस्तकें मेरी दुनिया हैं। मैं इनके बीच ही रहना चाहता हूं। हमारी संस्कृति में अक्षर को ब्रह्म माना गया है क्योंकि यह क्षरित नहीं होता। इसकी सत्ता अनंतकाल से चली आई है और भविष्य में भी बनी रहेगी।
वर्तमान हिंदी साहित्य में एक ऊहापोह की स्थिति बनी है। पीतल और सोने के बीच अंतर स्पष्ट करने वाले विवेक की नितांत आवश्यकता है। ऐसा विवेक जो रचनाकार के शब्द और चरित्र दोनों का सम्यक मूल्यांकन करे। उसकी दृष्टि शब्द-कर्म के साथ-साथ चरित्र (जिसे कुछ रचनाकारों ने व्यक्तिगत मान लिया है, जिसमें किसी को झांकने की अनुमति नहीं है) का भी भेदन करे। उसे किसी रचनाकार के जीवन का उज्ज्वल पक्ष ही नहीं बल्कि श्यामल पक्ष भी देखना चाहिए। किसी भी रचना की परख मात्र कथ्य और शिल्प के आधार पर नहीं होनी चाहिए। यदि ऐसा होता है तो यह एकांगी एवं पक्षपातपूर्ण कहा जाएगा। शास्त्रों में तो मनुष्य के चरित्र को सर्वाधिक महत्व दिया गया है। कहा गया है, वृत्तेन हतो हत: अर्थात् चरित्र जाने पर मनुष्य मृतक के समान होता है। हमारी संस्कृति में उसे आदर्श माना जाता है जिसने ’त्याग’ और ’आत्म’ को महत्व दिया है। मनुष्य का ’चरित्र’ भी ’आत्म’ का हिस्सा है। इसीलिए ऋषियों-मुनियों से लेकर महान साधु-संतों ने अपने चरित्र की यत्नपूर्वक रक्षा की है तथा दूसरों को इसके लिए प्रेरित भी किया। अपनी सुविधानुसार हम ’चरित्र-निर्माण’ को आउटडेटेड नहीं कह सकते क्योंकि यह हमारे जीवन-मूल्यों से जुड़ी अनमोल निधि है। मूल्यों के क्षरण के नाम पर आज के साहित्यकार हमारी संवेदना को झिंझोड़कर बड़ी चिंता के कवि बन जाते हैं, उनके साथ अनेकों साहित्यिक विशेषण स्वतः जुड़ने लगते हैं। ऐसे में उनके व्यक्तित्व विशेष में दस्तक देना उनकी निजता को भंग करना होता है। यह स्थिति साहित्य और समाज के सामने प्रश्नचिह्न खड़ा करती है।
हिंदी साहित्य में गुटबंदी अथवा दलबंदी की बात नई नहीं है। महाकवि गोस्वामी तुलसीदास से लेकर महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी ’निराला’ तक सबने अपने जीवन में इसका सामना किया। कल्पना कीजिए कि तुलसीदास की बहुचर्चित पंक्ति किस मनोस्थिति में लिखी गई होगी : ‘मांगि के खैबो, मसीत को सोइबो, लैबो एकु न दैबो को दोऊ। इसके बावजूद उनकी जनपक्षधरता रत्ती मात्र भी कम नहीं है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल तुलसी के लोकोन्मुख विचारों में जनपक्षधरता का उल्लेख करते हुए लिखते हैं- ‘वे (तुलसीदास) व्यक्ति की स्वतंत्रता का हरण नहीं चाहते जिसमें व्यक्ति इच्छानुसार हाथ-पैर भी न हिला सके। वे व्यक्ति के आचरण का इतना ही प्रतिबंध चाहते हैं जितने से दूसरों के जीवन-मार्ग में बाधा न पड़े और हृदय की उदात्त वृत्तियों के साथ लौकिक सम्बंधों का समांजस्य बना रहे।’ तुलसी का लोक ऐसे राजा द्वारा शासित है जो स्वयं अनुशासित और मर्यादित है। गोस्वामी जी ने एक तरफ कुव्यवस्था के कारण अराजकता का चित्रण किया है तो दूसरी ओर रामराज्य की परिकल्पना को भी प्रस्तुत किया है। यह तुलसी की भेदक दृष्टि है जो समकालीन आलोचना को सदैव नयी दृष्टि प्रदान करती रहेगी। ‘कविरेव प्रजापतिः’ को पुनर्स्थापित करने वाले संत शिरोमणि तुलसीदास स्वयं के लिए ‘कवित्त विवेक एक नहिं मोरे’ का उद्घोष करते हैं। उनकी इसी विनम्रता के कारण ‘रामचरितमानस’ में भारतीय मनीषा साकार एवं सावाक् हो उठी है। वहीं दूसरी ओर ‘सरोज स्मृति’ में व्यक्त आर्त क्रंदन से महाप्राण निराला की व्याकुलता का पता चलता है। ऐसा भान होता है कि वह विचलित है। कहीं पर वह ‘अशब्द अक्षरों का सुना भाष/ मैं कवि हूं, पाया है प्रकाश’ कहकर आत्मशांति महसूस करता है तो कहीं पर कवि जीवन की सार्थकता पर प्रश्नचिह्न लगाता है- ‘तब भी मैं इसी तरह समस्त/कवि जीवन में रहा व्यर्थ व्यस्त।’ साहित्यिक मठाधीशों की बहुलता तथा उनकी प्रधानता से निराला आहत थे। वे जानते थे कि इनकी बहुलता तथा सीमित विचारधारा भविष्य के लिए घातक है। यह साहित्य में कई खेमों को जन्म दे सकती है। निराला ने इनका वैचारिक विरोध भी किया किंतु ऐसा करना कवि को भारी पड़ा। आलोचना की दूरदर्शी, तीक्ष्ण और भेदक नजर से निराला का साहित्य वंचित रहा। तमाम आक्षेपों के तुले तूर्ण उन्हें विदीर्ण करने के लिए सतत चलायमान थे। इसी बात को महाप्राण निराला लिखते हैं –
देखे वे हंसते हुए प्रवर
जो रहे देखते सदा समर
एक साथ जब शतघात घूर्ण
आते थे मुझ पर तुले तूर्ण
देखता रहा मैं खड़ा अपल
वह शरक्षेप, वह रण कौशल।
इसी प्रकार आज भी कई रचनाकार जिनमें असीम सम्भावनाएं हैं, दुर्भावना का शिकार होंगे।
साहित्य के क्षेत्र में छल, क्षद्म, अहंकार, यश और महत्त्वाकांक्षा जैसे विकारों की जरूरत नहीं है। इसमें तो स्वाधीन चेतना की सर्वाधिक जरूरत है। चेतना ऊर्ध्वगामी होती है। इसका प्रवाह अनंत की ओर होता है। जब यह साहित्य में उतरती है तो वैचारिक हदबंदी ध्वस्त हो जाती है। ’सहित’ का भाव प्लावित होने लगता है। विमर्शों की दुकान बंद होने लगती है। तब सृष्टि के सभी भूतों की धड़कन सुनाई देती है। ’विश्वैक नीड़म् के समक्ष कोई विराट विचारधारा ही ठहर सकती है। इसमें सबके मंगल की कामना निहित होती है। साहित्य को बांट कर कोई अपना सर्वोत्तम नहीं दे सकता। साहित्य में परपीड़ा को स्थान मिला है। ’परपीड़ा’ से तात्पर्य केवल ’मानवपीड़ा’ नहीं बल्कि ’ब्रह्मांड की पीड़ा’ से है। ऐसी दृष्टि रखने वाले रचनाकार प्रत्येक काल एवं प्रत्येक युग में हुए। ऐसे दूरदृष्टि संपन्न ऋषितुल्य शब्द शिल्पियों एवं कलाकारों ने अपने बारे मौन रहना उचित समझा। इन्हीं के बारे में डॉ. विश्वनाथ प्रसाद तिवारी ने लिखा है, भारतीय ऋषियों, संतो, भक्तों और मनीषियों ने अहंकार को ही व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु कहा है। संत कबीर अपने ’मैं’ को ’नान्हा’ करि- करि पीसने का उपदेश देते हैं। भारत में न जाने कितने महान कवि-कलाकार हुए जिन्होंने अद्भुत कलाकृतियों के सृजन किए पर अपने बारे में उन्होंने मौन रहना ही उचित समझा। अजंता, एलोरा, महाबलीपुरम, कोणार्क, खजुराहो के कलाकारों के बारे में हम कितना जानते हैं? वाल्मीकि, व्यास, कालिदास, तुलसीदास के बारे में सिवा कुछ थोड़ी-सी किवदंतियों के, क्या है हमारी जानकारी में? ऐसे ही महानतम महापुरुषों के कारण हम अपने ज्ञान और संस्कृति को स्वयं में जीवित रखे हैं। इनके लिए किसी प्रमोटर की जरूरत नहीं।
माना कि वर्तमान में हिंदी-साहित्य-क्षितिज पर काले-गहरे बादल छाएं हैं। इससे कुछ समय के लिए दिशाहीनता की स्थिति प्रतीत अवश्य है किंतु बादलों के पार समूचा गगनमंडल आलोकित है, ’स्व’ की आभा से दीप्त प्रत्येक नक्षत्र अपनी-अपनी कक्षा में चल रहा है। तमभेदी दृष्टि इस उजास को साफ-साफ देख रही है। ’चरैवेति’ की शाश्वत यात्रा में वांछित-अवांछित पड़ावों से गुजरना ही होता है। ’तमसो मा ज्योतिर्गमय’ नैरंतर्य बना रहना चाहिए। अस्तु।
डॉ. जीतेन्द्र पाण्डेय