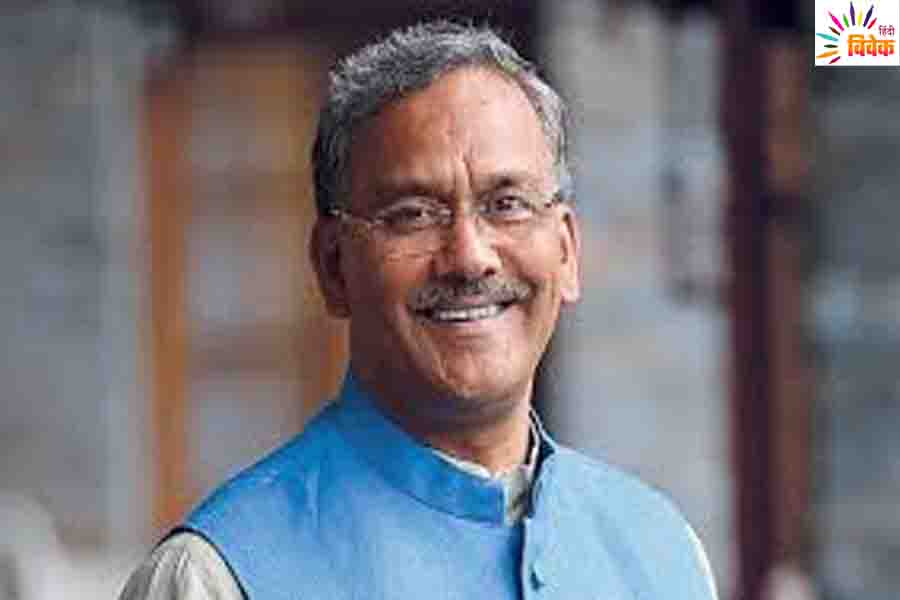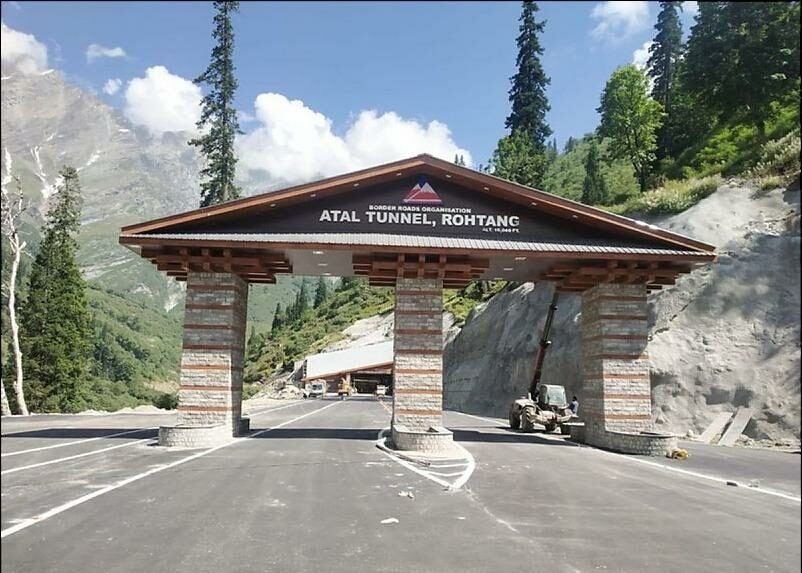देवभूमि उत्तराखंड को रोजगारोन्मुख बनाकर आत्मनिर्भर बनाने के लिए त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार ने कई योजनाओं की घोषणा की है। इस तरह राज्य अपनी आत्मनिर्भरता के साथ देश की आत्मनिर्भरता में योगदान कर रहा है।
————
उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर उत्तराखंड के लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रदेश की त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार ने कई रोजगारोन्मुख योजनाएं बनाई हैं। इन योजनाओं के बलबूते सरकार का प्रयास है कि उत्तराखंड को आत्मनिर्भर बनाते हुए भारत को आत्मनिर्भर बनाने में यथासंभव योगदान दिया जा सके।
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना
उत्तराखंड के उद्यमशील युवाओं और उत्तराखंड के ऐसे प्रवासियों को, जो कोविड-19 के कारण उत्तराखंड राज्य में वापस आए हैं, कुशल एवं अकुशल दस्तकारों एवं हस्तशिल्पियों तथा शिक्षित शहरी व ग्रामीण बेरोजगारों आदि को अभिप्रेरित कर स्वयं के उद्योग या व्यवसाय की स्थापना हेतु प्रोत्साहित करने के लिए उद्यम, सेवा अथवा व्यवसाय की स्थापना हेतु
राष्ट्रीयकृत या अनुसूचित
वाणिज्यिक बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के माध्यम से ॠण सुविधा उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से निम्नांकित मार्गदर्शक सिद्धांतों के अधीन ‘मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना’ संचालित की जा रही है।
फल संरक्षण उद्योग योजना
फलों एवं सब्जियों के मौसमी उत्पादन के कारण इनके अल्पकालिक बाजार को दीर्घकालिक बनाने के लिए इनके उत्पादों के संरक्षण की आवश्यकता है। प्रत्येक फलों-फूलों व सब्जियों के संरक्षण की अलग-अलग विधियां होती हैं। सेब मुख्यतः उत्तर भारत के पहाड़ी प्रदेशों में जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में ज्यादा होता है; वहीं चटनी, मुरब्बा की उपयोगिता राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय बाजार में सर्वत्र व्याप्त है। फलों के अपने मूल रूप में सड़ गलकर बरबाद होने की ज्यादा संभावनाओं को देखते हुए उन्हें परिरक्षित कर उन्हें जैम, जैली, स्क्वैस, जूस, मार्मलेड, मुरब्बा, चटनी, आचार के रूप में दीर्घकालिक बाजार में व्यापक स्तर पर बेचा जा सकता है। पहाड़ी फलों व मसालों की खुशबू का अपना एक विशिष्ट स्थान होने से मिक्सिंग का उचित अनुपात फलों व मसालों की स्वच्छता आदि को ध्यान में रखकर गुणवत्ता कायम रखी जाए तथा अपनी विशिष्टता व गुणवत्ता को मजबूत रखते हुए सही भरोसेमंद अपना ब्रांडनेम दिया जाए।
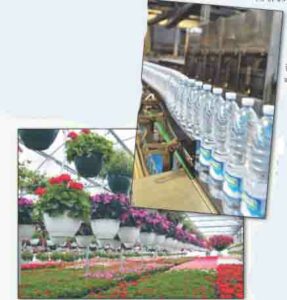 आटा चक्की व धान कुटाई योजना
आटा चक्की व धान कुटाई योजना
आटा चक्की पर्वतीय क्षेत्रों में पहले नंबर का व्यवसाय है। अनाज पिसाई के लिए एक रु. या इससे अधिक प्रति किग्रा की दर से पिसाई चार्जेज लेकर प्रायः ग्रामीण क्षेत्रों में चक्कियां चलाई जा रही हैं। शहरी क्षेत्रों में गेहूं ख़रीदकर सफाई करके आटा बेचने के लिए भी उपलब्ध हो रहा है। इसकी उपयोगिता स्थानीय मांग व आवश्यकता पर निर्भर करती है। जिन क्षेत्रों में धान अधिक होता है वहां पर धान कुटाई का कार्य भी अच्छा चल सकता है।
जड़ी बूटी उद्योग योजना
उत्तराखंड में जड़ी बूटियों का अपार भंडार है। यदि भेषजसंघ द्वारा स्थानीय जड़ी बूटियों का एकत्रण कर आयुर्वेदिक दवाइयां बनाई जाए तो इसकी एक अलग ही गुणवत्ता रहेगी। यहां पर प्रायः हरड, आंवला, बहेडा, सनाय, अश्वगंधा, सर्पगंधा ब्राह्मी, सतावर, कालमेघ, जटामांसी, सफेद मूसली, चिरायता, रीठा, बच, पुनर्नवा, बजदंती, रूद्रवंती, दारूहल्दी या किल्मोड़ा, धतूरा, बनतुलसी, कंटकारी, घृतकुमारी या एलूवेरा, गोखरी, तेजपत्ता, जम्बू, डोलू, पाषाणमेद आादि अनेकों जड़ी बूटियां पाई जाती हैं।
फ्लोरीकल्चर योजना
उत्तराखंड के थ्रस्टसैक्टर उद्योगों में पुष्प कृषि को प्रथम स्थान दिया गया है। उत्तराखंड के प्रत्येक फूल व वनस्पति औषधीय गुणों से युक्त है। प्रस्तुत योजना में जिरेनियम को उदाहरण स्वरूप लिया गया है। इसकी कटिंग लगाने हेतु लगभग 50 नाले भूमि की आवश्यकता हो सकती है। लगभग 300 कटिंग प्रतिनाली की दर से रोपण किया जाता है। इसके लिए जैविक खाद एवं उचित सिंचाई की व्यवस्था हेतु जल स्रोत एवं टैंक पाईप आदि की जरूरत होती है।
होटल और रिसोर्ट योजना
उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल में नैनिताल अपने सौंदर्य के लिए देश-विदेश मे प्रसिद्ध है। यह जनपद पर्यटन की दृष्टि से उत्तराखंड में प्रमुख रूप से जाना जाता है, यहां पर पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। इको टयूरिज्म की दृष्टि से नैनीताल, भीमताल, नौकुचियाताल, रामनगर कोर्बेट पार्क, रामगढ़, खुर्पाताल व सातताल प्रमुख केन्द्र है। पर्यटन की मुख्य जरूरतों में होटल हैं। वर्तमान में इसकी मांग को देखते हुए यह कार्य आर्थिक रूप से फायदेमंद हो सकता है।
बुटीक व रेडीमेड गारमेन्टस योजना
रेडीमेड गार्मेन्टस के बढ़ते युग में कटिंग टेलरिंग उद्योग काफी लाभकारी उद्यम है। यह जॉबवर्क के रूप में सेवा उद्यम तथा रेडीमेड गार्मेन्टस निर्माण की दृष्टि से निर्माणकारी की श्रेणी में भी आता है। पर्वतीय क्षेत्रों में प्रायः दर्जीगिरी एक जॉबवर्क सेवा उद्यम ही हैं। शहरों में बुटीक रेडीमेड कपड़ों का निर्माण कार्य काफी लाभदायक है।
मौंन, मधुमक्खी पालन योजना
भारतीय मौंन अथवा मधुमक्खी एक सामाजिक कीट है। इसके परिवार में एक रानी मौंन होती है और एक वंश में 30 से 40 हजार तक कमेरी मौंन होती हैं। इन्हें वर्कस कहा जाता है। प्रजनन काल में प्रत्येक मौंन वंश में 100 से 2000 तक नर मौन पैदा होते हैं। इनका कार्य केवल रानी को गर्भित करना होता है। रानी तथा कमेरी दोनों ही मादा होती हैं परन्तु रानी अंडे देेने का कार्य करती है और कमेरी शिशू पोषण तथा मधु एकत्रण छत्ता निर्माण आदि समस्त कार्य करती है। रानी का पोषण छोटी अंगुली के पोरवे के समान विशेष आकृति के लटके हुए कोष्ठक में होता हैं। रानी को वयस्क बनने में 15 या 16 दिन लगते हैं तथा कमेरी व नर मौंन के परिवर्धनल में 3 से 4, या 15 से 16 दिन लगते हैं तथा कमेरी व नर मौंन के परिवर्धन में 3 से 4 सप्ताह तक का समय लगता है।
 मसाला उद्योग योजना
मसाला उद्योग योजना
पहाड़ी मसाले जैसे हल्दी, धनिया, मेथी, अदरक, लहसुन तथा बड़ी इलायची व मिर्च काफी ज्यादा खुशबूदार होते हैं। इन्हें जैविक खाद, गोबर खाद में उत्पादित करने पर इनकी विशिष्टता और बढ़ जाती है। ताजे पहाड़ी मसालों का विपणन क्षेत्र पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। यदि इन्हें साफ करके सही ढंग की पैकेजिंग करके बड़े-बड़े होटलों एवं रेस्टारेन्टों में सप्लाई किया जाए तो यह नवरंग, एम.डी.एच. या गोल्डी मसालों से प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता रखते हैं।
मिनी बेकरी योजना
प्रायः डबलरोटी, केक और बंद ऐसे बेकरी उत्पाद हैं जो ग्रामीण एवं शहरी सभी क्षेत्रों में सर्वाधिक पसंद किए जाते हैं। यद्यपि बाजार में, ब्रिटानिया, पारले, प्रियागोल्ड या सनफिस्ट आदि अनेक बिस्कुट हैं, परन्तु घरेलू चाय नाश्ते में बेकरी उत्पादों का अपना एक अलग ही महत्व है। बेकरी उत्पादों की गुणवत्ता सही हो तथा उपभोक्ता की पसंद एवं मांग के अनुरूप इसे तैयार किया जाए तो इसकी बिक्री भी बड़े स्तर पर की जा सकती है। इसकी स्थानीय एवं बाह्य क्षेत्रों में बराबर मांग बनी रहती है लेकिन उपभोक्ता मांग की सही परख होने पर ही यह उद्योग लाभप्रद है।
आलू चिप्स व नमकीन उद्योग योजना
आलू चिप्स व नमकीन दालमोठ का उपयोग दैनिक नाश्ता, मीटिंग या शादी व्याह के अवसरों पर अथवा फिर यात्रा के दौरान बहुतायत से सभी उम्र एवं वर्ग के लोगों द्वारा किया जाता है। यद्यपि प्रतिस्पर्धा युक्त बाजार में अनेक कम्पनियां इस कार्य में संलग्न भी हैं लेकिन अगर कुशल कारीगर द्वारा लघु स्तर पर घरेलू उद्यम के तौर पर इस कार्य को समर्पित भाव से शुरू किया जाय तो इसकी मांग सर्वत्र व्याप्त होगी। स्वादिष्टता व गुणवत्ता का ध्यान रखे जाने पर इसकी बाजार मांग स्वतः ही उत्पन्न हो जाती है।
मशरूम उत्पादन योजना
शाकाहारी भोज्य पदार्थों में खनिज लवण, कैल्सियम, विटामिन्स एवं प्रोटीन की दृष्टि से मशरूम का आधुनिक खान-पान में विशिष्ट स्थान है। आजकल बड़े-बड़े होटलों रेस्टोरेंट शादी विवाह के व्यंजनों एवं दावत पार्टियों में शाकाहारी लोगों के लिए यह एक उत्तम खाद्य पदार्थों के रूप में परोसा जाता है। आजकल सब्जी मंडियों में मशरूम के पैकेट बिक्री हेतु लगभग सर्वत्र सुलभ दिखाई पड़ते हैं। इसका प्रचलन विशेषतः विदेशी पर्यटकों की बढ़ती हुई आवाजाही के कारण ज्यादा बढ़ा है। पर्यटक स्थलों के होटल, रेस्टोरेंटों में तो इसकी विशेष मांग रहती है। इसे शाकाहार की पोष्टिक खाद्य पदार्थों की श्रेणी में रखा जाता है। मशरूम या खुम्बी के उत्पादन/ विपणन हेतु व्यावसायिक तकनीकी ज्ञान टैक्निकल नॉलेज की विशेष आवश्यकता है। क्योंकि गेहूं या चावल की भूसी एवं कम्पोस्ट को वेवस्टीन व फार्मेलीन के साथ मिश्रित कर
लकड़ी के ट्रे में भूसी मिश्रण को भरकर उसमें स्पॉन को बोया जाता है तथा एक निश्चित तापमान पर उत्पादन कक्ष में बंद करके रखा जाता हैं। नमी व तापमान के उचित तालमेल न होने से इसका अंकुरण प्रस्फुटन एवं विकास प्रभावित हो जाता है। अतः इसकी तकनीकी व्यावहारिक जानकारी नेशनल सेंटर फॉर मशरूम रिसर्च एण्ड ट्रैनिंग सेंटर-सोलन, हिमाचल प्रदेश अथवा फिर हॉर्टिकल्चर विभाग में प्राप्त की जा सकती है। केवल किताबी ज्ञान से मशरूम की इकाई स्थापित नहीं की जा सकती है।
हर्बल अगरबत्ती योजना
उत्तराखंड की देवभूमि में गांव-गांव घर-घर देवालय तो हैं ही साथ ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान रखने वाले धार्मिक पर्यटन से जुड़े हुए अनेक तीर्थ भी यहां हैं। जैसे हरिद्वार, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, ॠषिकेश, बागेश्वर, जागेश्वर आदि-आदि। अतः अगरबत्ती की काफी मांग बनी रहती है। यहां पर अगरबत्ती आपूर्ति की जा रही है। यदि यहां पर भी कुटीर उद्योग के रूप में इसे अपनाया जाय तो इसकी पार्याप्त बाजार संभावनाएं हैं।
हर्बल कॉस्मेटिक उद्योग योजना
विज्ञान/दूरदर्शन के प्रभाव के आज कॉस्मेटिक का व्यापक प्रचलन हो चुका है। कैमिकल्स के दुष्प्रभावों को देखते हुए आज ज्यादातर लोग हर्बल उत्पादों की ओर ज्यादा आकृष्ट हो चुके हैं। ब्यूटीपार्लरों में भी आज हर्बल उत्पादों का प्रचलन बढ़ गया हैं। श्रृंगार की बढ़ती चाहत एक अभिन्न अंग के रूप में हर्बल कॉस्मेटिक की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इसके निर्माण में प्रयुक्त कच्चा माल, हरड़ आंवला, बेहड़ा, सिफला, शिकाकाई फोमिंग एजेंट, मुल्तानी मिट्टी, रीठा, नीम की छाल व पत्ती एवं सुगंधित द्रव्य आदि स्थानीय बाजारों में आसानी से सुलभ हो जाते हैं।
रिंगाल व बांस हस्तशिल्प योजना
रिंगाल और बांस दोनों करीब एक ही प्रजाति के पौधे होते हैं और करीब दो शताब्दी पूर्व तक गांव के घरेलू उपयोगी वस्तुओं में इसका काफी अधिक महत्व था। पर्वतीय अंचलों में सूप, डलिया, कंडी, टोकरी, डोका, पिटारा, मोस्टा, चटाई आदि हस्तशिल्प उत्पादों का बहुत ज्यादा महत्व था। आज भी जो ग्रामीण लोग खेती से जुड़े हैं वे सूप, डलिया, टोकरी, चटाई आदि का प्रयोग करते हैं, लेकिन अब यह ग्रामीण दस्ताकरों द्वारा पार्ट टाईम जॉब के रूप में ही किया जाता है।
मिनरल वाटर व बोटलिंग प्लांट योजना
पेयजल की उपलब्धता आज के प्रदूषण भरे वातावरण में एक प्रमुख आवश्यकता बन चुकी है। प्रदूषित जल अनेक बीमारियों का कारक है। अतः शुद्ध पेय जल का प्रतीक मिनरल वाटर एक ऐसा उभरता उद्योग है जिसकी बाजार मांग काफी व्यापक पैमाने पर है। आजकल शादी विवाह, पार्टी समारोह, बड़ी-बड़ी बैठकों, रेलवे प्लेटफार्म, बस स्टैण्ड एवं पर्यटक स्थलों में लोगों द्वारा मिनरल वाटर की मांग तेजी से होती है।
काष्ठ कला व कार्पेन्ट्र उद्योग योजना
यह जनपद पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है लकड़ी की कलात्मक वस्तुएं बनाकर विक्रय करना काफी लाभकारी रहेगा। बढ़ईगिरी या काष्ठ कला उद्योग मूलतः वास्तुशिल्प की अप्रतिम विद्या है। आज वनोपजों पर प्रतिबंध के फलस्वरूप काष्ठकला का पुरातन स्वरूप बदल चुका है। प्लास्टिक व आयरन इंजीनियरिंग के विकल्प मिल जाने से काष्ठकला काफी हद तक कम हुई है, पुरानी नक्काशीदार दरवाजे चौखटों की जगह सीधे सपाट विंडो डोर फ्रेम बनने लगे हैं।
पोल्ट्री फार्म योजना
मांसाहार एवं मद्यपान के बढ़ते प्रचलन के कारण कुक्कुट पालन आज एक लाभकारी उद्यम हो गया है। ग्रामीण व शहरी सभी क्षेत्रों में इसकी व्यापक मांग बढ़ी है। चूंकि वह व्यवसाय अत्यधिक संवेदनशील है, अतः इसको चलाने वाले उद्यमी को प्रशिक्षित होने के साथ ही मुर्गियों के भोजन, उनकी दवा, दिनचर्या, परिवर्धन विधियों एवं मुख्य रोग तथा उसके निदान आदि से भली-भांति भिज्ञ एवं व्यावहारिक ज्ञान वाला होना चाहिए। थोड़ी सी भी चूक होने पर सारा उद्यम समाप्त होते देर नहीं लगती इसलिए इसमें सक्रियता एवं व्यवहार कुशलता जरूरी है।
ताम्र उद्योग योजना
ताम्र उद्योग उत्तराखंड का एक परम्परागत हस्तशिल्प उद्योग रहा है। जनपद रामनगर में टम्टा शिल्पियों द्वारा तांबे के परम्परागत उत्पाद घड़े, कलश, गगरी, तौले, परात, लोहे, दीपक, मूर्तियां, वाद्ययंत्र, अर्ध्य आदि बनाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त बदलते फैशन, डिजाइन के अनुरूप नक्काशीयुक्त जग, फिल्टर, लोटे, कलश, देवप्रतिमाएं एवं बाल हेंगिग्स आदि उत्पाद भी तैयार किए जाते हैं। शादी ब्याह धार्मिक उत्सवों में ताम्र उत्पादों का प्रयोग अधिक होता है।
ऊनी हथकरघा एवं हस्तकला कार्पेट उद्योग योजना
ऊनी हथकरघा उद्योग के अंतर्गत शॉल, पंखी, थुल्मा, चुटका, पंखी टवीड, मफलर, टोपी, बनियान आदि बुने जाते हैं तथा हस्तकला उद्योग के अंतर्गत ऊनी कालीन व कार्पेट आसन, सोफा, बाल हेगिग्स आदि बनाए जाते हैं। जनपदीय, राष्ट्रीय, प्रांतीय में मेले-प्रदर्शनी के माध्यम से इनके उत्पाद विपणन की अच्छी व्यवस्था संभावनाएं हैं।
मिनी डेरी योजना
दुग्ध एवं दुग्धजन्य पदार्थां की मांग निरंतर बढ़ती जा रही है, यह श्वेत क्रांति का आधारभूत उपक्रम है। मिल्क रूटों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों का दूध शहरी क्षेत्रों में आसानी से पहुंच जाता है। अतः डेरी उत्पादों तथा घी, दूध, दही, मक्खन, पनीर, खोया आदि की मांग काफी व्यापक है। घरेलू उपयोग के अलावा बड़े होटलों व रेस्टोरेंटों में भी इसकी व्यापक मांग है।
रामबांस उद्योग योजना
अगेव या अगेवे सी कुल के रामबांस की लगभग 300 प्रजातियां पाई जाती हैं। इनके पत्तों से रेशा निकालकर सीसल फाइबर, चटाइयां, पर्स, वॉल हेंगिग्स, गदियां, बैग्स आदि अनेक उपयोगी वस्तुएं बनाई जाती हैं। औद्योगिक प्रयोजन से रेशा उत्पादन हेतु अगेव सिसलाना हाईब्रीड व लीला हाईब्रीड नामक प्रजाति अधिक उपयुक्त होती है। इसके उत्पाद विपणन एवं बाजार मांग की पर्याप्त संभावनाएं हैं। शहरी क्षेत्र के बाजारों तथा प्रसिध्द प्रांतीय व अंतरराष्ट्रीय मेले प्रदर्शनियों में इसके फेंन्सी आइटम पर्याप्त मात्रा में बेचे जा सकते हैं।
फास्टफूड सेंटर योजना
उत्तराखंड पर्यटन की दृष्टि से प्रसिद्ध है। यहां फास्ट फूड सेंटर स्थापना की अच्छी संभावनाएं हैं। आधुनिक भागदौड़ के युग में खान-पान की संस्कृति बदल चुकी है और लोग होटल के आदी हो चुके हैं। बाहर जाने पर सोने जागने के समय में गड़बड़ी से हर एक का मन सीधे-साधे दाल-चावल, रोटी की अपेक्षा तीव्र एवं तीक्ष्ण भोजन करने का होता है। इसलिए पर्यटन स्थलों या आवागमन के स्टेशनों में यत्र-तत्र, फास्ट फूड रेस्टोरेंटों की महक रहती है। नई पीढ़ी के बच्चे परम्परागत भोजन की अपेक्षा फास्टफूड में ज्यादा रूचि रखते हैं।
शहद निर्माण की योजना
शहद का उपयोग लगभग हर घर में किया जाता है। शहद में ग्लूकोज खनिज लवण, विटामिनों की मात्रा के कारण इसका औषधीय महत्व भी है। आयुर्वेद में बहुत सी दवाएं शहद में देने के कारण इसका औषधीय महत्व और अधिक बढ़ जाता है। शहद निर्माण प्राकृतिक रूप से होता है। मधुमक्खियों के छत्तों को जलाकर मक्खियों के उड़ने के बाद छत्तों को निचोड़कर शहद निकाली जाती है।
फ्रूट एवं वेजिटेबिल प्रिजर्व कैण्डीज निर्माण योजना
फल तथा सब्जियां के प्रिजर्व व कैण्डीज का मुख्यतः उपयोग स्वीट, बेकरी व कन्फेक्शनरी, आईसक्रीम और फ्रूट स्वाद के रूप में होता है। फल तथा सब्जियों के प्रिजर्व व कैण्डीज के लिए केन्द्रीय तकनीकी खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान मैसूर में विकसित की है जिसमें फल सब्जियां जैसे सेब, आंवला, पपीता, आम, स्ट्रावेरी, रसबेरी, पेठा, गाजर, अन्नानास, संतरा, अंगूर, चेरी, अदरक आदि से टूटी, फ्रूटी, पेन, गाजर आदि उत्पादित किए जा सकते हैं। अदरक प्रिजर्व, आंवला, कैण्डी, अदरक कैण्डी, जैसे अनेक उत्पाद कच्चे माल की उपलब्धता के आधार पर तैयार किए जा सकते हैं। उत्तरांचल का फल उत्पादन में अपना विशिष्ट स्थान है।
लेमीनेटेड दोना पत्तल योजना
शादी विवाह सहित तमाम सामूहिक कार्यों में दोना व पत्तल का उपयोग किया जाता है। दोना पत्तल से साफ सफाई व रखरखाव का खर्च बच जाता है। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में मालू पात के रूप मे कच्चा माल उपलब्ध है जिससे इस विर्निमाण उद्यम की स्थानीय क्षेत्र में चलने की अच्छी संभावनाएं हैं। विभिन्न उत्सवों, शासकीय कार्यालयों में पेपर प्लेट एवं दोना पत्तल की अत्यधिक मांग होती है। वर्तमान समय में केटरर्स द्वारा भी इनका उपयोग किया जाता है। अतः उत्तराखंड में दोना पत्तल इकाई का बाजार अत्यधिक संभावित नजर आता है।
स्वर्णकारी योजना
महिला सौन्दर्य हेतु स्वर्ण एवं रजत आभूषणों की मांग का इतना ज्यादा प्रभाव आज देखने को मिलता है कि यह एक स्टेटस सिम्बल तथा पूंजीगत निवेश का अभिन्न अंग बन गया है। ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में इनकी बाजार संभावनाएं व्याप्त हैं। ज्यों-ज्यों स्वर्ण-रजत की कीमतो में वृद्धि हो रही है त्यों-त्यों लोगों का उसकी तरफ और आकर्षण बढ़ रहा है और इसलिए ही स्वर्णकारी का बाजार भी निरंतर बढ़ता जा रहा है।
————