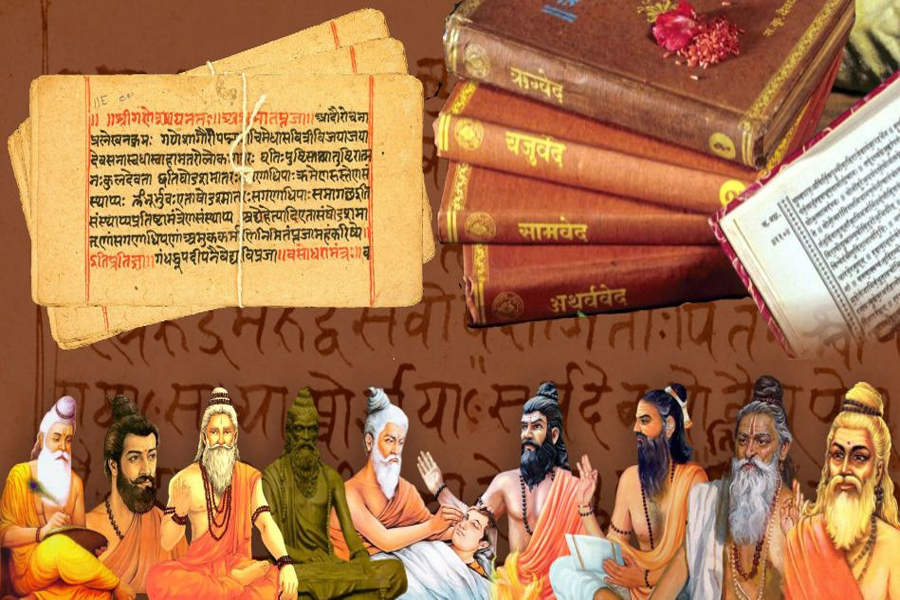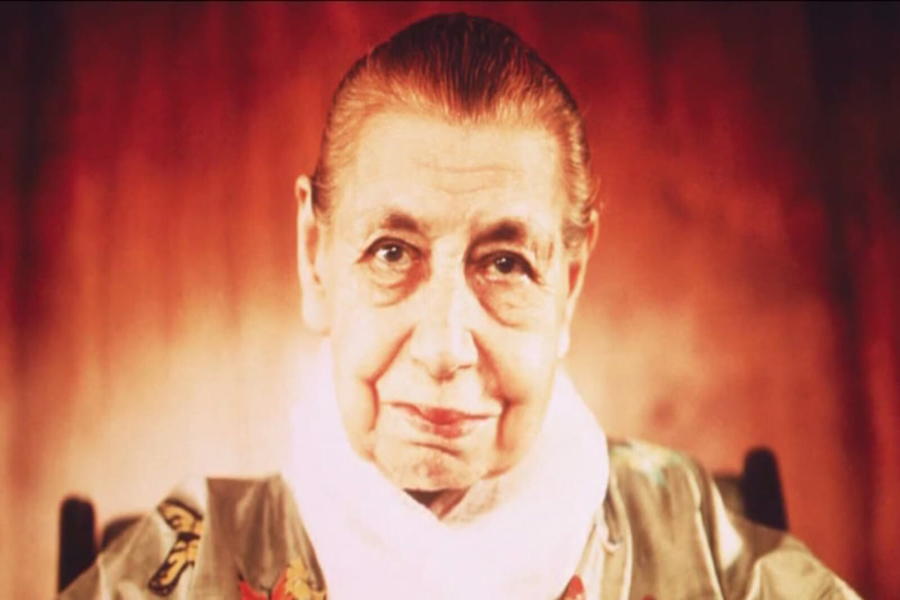भारतीय साहित्य का जहाँ से उद्गम हुआ, वह स्रोत निर्विवाद रूप से वेद है। वेद आर्ष काव्य की श्रेणी में आते हैं। हमारे प्राचीन ऋषि मनुष्य थे, समाज के साथ थे। वे आपसी प्रेम और सद्भाव को सबसे अधिक मूल्यवान समझते थे। इसीलिए मनुष्य की जिजीविषा, उसके सामाजिक सरोकार और समाजिक जीवन की योजनाओं के सुंदर चित्र वेदों में से बार-बार झाँकते हुए दिखाई पड़ते हैं। सर्वप्रथम वैदिक ऋषियों ने ही उस सामाजिक समरसता की परिकल्पना की, जो परवर्तीकाल में हमें भारतीय साहित्य की आत्मा के रूप में पहचान में आती है। ऋग्वेद के सबसे अंत में जो समापन-गीत है, उस पर हमारा ध्यान जाता है। यह सामाजिक समरसता का पहला गीत है, जो सदियों से समवेत स्वर में गाया जाता है।
गीत इस प्रकार है-
सं गच्छध्वं सं वदध्वं सं वो मनांसि जानताम्।
देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते।।
समानो मन्त्र: समिति: समानी
समानं मनः सह चित्तमेषाम्।
समानं मन्त्रमभि मन्त्रये वः
समानेन वो हविषा जुहोमि।।
समानी व आकूति: समाना हृदयानि वः।
समानमस्तु वो मनो यथा वः सुसहासति।।
ऋषि चाहता है कि हम साथ-साथ आगे बढ़ें,आपस में संवाद बनाये रखें, मन में अच्छे विचारों को आने दें।आपसी समझ के साथ अपने-अपने कर्तव्य का पालन करते रहें। वह यहाँ पर यह भी चाहता है कि सबके लिये एक नियम हो, सबके लिये एक ही नीति हो। सबके मन, सबके चित्त एक हों, और हम संगठित हो कर रहें। सबसे अंत में ऋषि एक ही बात बहुत जोर देकर कहता है कि हम सबका संकल्प एक हो, हम सबके हृदय समान हों, हम सबका मन एक हो। आपस में कोई विरोध कभी न उपजने पाये।
मनुष्य आदिकाल से ही सामाजिक समरसता की भावनाओं को सींचते हुए यहाँ तक आया है। वह अंधकार और मृत्यु से घिरा होने के बाद भी सदैव मनुष्यता में जीने के संकल्प से भरा हुआ दिखाई देता है। ऋग्वेद में ऐसे सूक्तों की संख्या बहुत बड़ी है, जो हम सब में यह विश्वास जगाते हैं कि मनुष्य अपने समाज के साथ ही ऊपर उठना चाहता है। वह मनुष्यता के पक्ष में जब भी आवाज उठाता है, तब वह सामाजिक समरसता की ही बात कर रहा होता है। एक जगह ऋषि के उद्गार हैं-“मनुष्वत्वा नि धीमहि मनुष्वत् समिधीमहि।अग्ने मनुष्वदङ्गिरो देवान् देवयते यज।।(ऋग्वेद 5:21:1)” अर्थात् हम मनुष्य की तरह होना चाहते हैं, मनुष्य की तरह जीना चाहते हैं, मनुष्यता के विचार में बहते हुए ही हम जीवन का लक्ष्य पा लेना चाहते हैं। वैदिक ऋषि बार-बार मनुष्यता से ही प्रीति रखने की बात कहते हुए, मनुष्यता के लिये जीवित रहने का आह्वान करता है। वह चाहता है कि मनुष्य मनुष्यता से ही आगे बढ़े, मनुष्यता में ही रस ग्रहण करे।
वैदिक साहित्य के मूल में यह विचार काम करता है कि मनुष्यों में न तो कोई बड़ा है, न कोई छोटा। सब आपस में भाई-भाई हैं, और अपने कल्याण के लिये सब मिलकर प्रयत्न करते हैं। इस सम्बन्ध में ऋग्वेद में ऋषि का स्पष्ट कथन है-‘अज्येष्ठासो अकनिष्ठास एते सं भ्रातरा वावृधु: सौभगाय।'(ऋग्वेद:5:6:5) अथर्ववेद के पृथ्वीसूक्त का गायक ऋषि जब घोषणा करता है कि ‘माता भूमि: पुत्रोऽहं पृथिव्या:’, तब वहाँ सब मनुष्य समभाव से धरती के पुत्र है। इसी संकल्पना ने वैदिक समाजवाद की नींव रखी। यही भाव तब भी मुखर हुआ, जब यजुर्वेद के सुप्रसिद्ध राष्ट्रगान ‘आ ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायतामाराष्ट्रे राजन्यः शूर इषव्योऽति व्याधी महारथी जायताम्।……..’ में सामाजिक समरसता के लिये प्रार्थना की।
वैदिक ऋषियों का जीवन उच्चतर लक्ष्यों की ओर उठा हुआ है, लेकिन वह सामंजस्य और साहचर्य की नींव को बहुत मजबूती से पकड़कर रखना जानता है। वे समाज के दायित्वों से विमुख होकर जंगल की विरक्ति के पीछे नहीं भागते। वे जीवन से प्रेम करते हैं, और यह जानते हैं कि जीवन का सुखभाग समाज में घुल-मिल कर रहने में है। वैदिक वाङ्मय में जातिवाद के लिये कोई जगह नहीं। वर्णव्यवस्था का कोई आश्रम नहीं है वहाँ। वहाँ महत्व है मनुष्य के संघर्षों से उपजे उस विचार का, जो सामाजिक अभ्युदय का पथ प्रशस्त करता है। इसीलिए वेदों में जो महत्व वसिष्ठ, विश्वामित्र, वामदेव और अत्रि का है, वही महत्व जनकवि कहलाने वाले उस कवष ऐलूष का भी है, जिसने ऋग्वेद को वह अक्षसूक्त दिया, जो एक जुआरी का एकालाप है। करुणा से भरे हुए इस सूक्त की अंतिम ऋचा जुआरी को जुआ खेलने से छुड़ाकर समाज से जोड़ती है, कृषि से जोड़ती है, पशुपालन से जोड़ती है, समाज के अर्थतंत्र से जोड़ती है, और सुखी परिवार की सम्भावना से जोड़ती है। कितनी समृद्ध है यह ऋचा, देखिए-
अक्षैर्मा दीव्यः कृषिमित्कृषस्व।
वित्ते रमस्व बहुमन्यमानः।
तत्र गावः कितव तत्र जाया
तन्मे विचष्टे सवितायमर्यः।।
वैदिक साहित्य को देखने की दृष्टि बदलना होगी। वह भारतीय समाज की आँखों से देखे गये भारतीय समाज का उज्ज्वल चित्र सामने लेकर आता है। वहाँ समाज का विद्रूप भी है, लेकिन वहाँ मनुष्य के वे प्रयास भी हैं, जो सामाजिक शान्ति से चलकर विश्व शान्ति की ओर जाते परिलक्षित होते हैं। परस्पर प्रेम और सौहार्द, परस्पर रक्षा का सद्भाव, परस्पर सहयोग और साहचर्य से जीवन का भोग, एक-दूसरे को अपनी शक्ति से सींच कर मजबूत सामाजिक संगठन खड़ा करने के ही विचार से वैदिक साहित्य का वह नवनीत निकल कर आया, जिसकी ध्वनि वेदोत्तरकाल में और उसके बाद भी गूंजती रही है। वह नवनीत है-‘सह नाववतु सह नौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै। तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै।।’ इस मंत्र में सम्पूर्ण सामाजिक समरसता का गहरा संदेश छिपा हुआ है। इसे अनदेखा कर भारतीय समाज आगे नहीं बढ़ सकता।
ऋग्वेद में ही वह सूक्त भी है, जिसमें ‘केवलाघो भवति केवलादी’ जैसी पंक्ति भी आती है। जो अकेला खाता है, वह केवल पाप खाता है। इतना उत्तेजक वाक्य देने वाला दान सूक्त ऋग्वेद के महासागर में अलग से पहचान में आता है। इस सूक्त में भिक्षु ऋषि ने उन धनी मित्रों की जम कर भर्त्सना की, जो कभी अपनी सुख सुविधाओं से बाहर निकलने का कष्ट भी नहीं उठाते। ऋषि प्रशंसा करता है उनकी, जो अपना यत्किञ्चित् धन भी लुटा देते हैं उन पर, जो भूखे हैं, याचक हैं, असहाय हैं। भारतीय साहित्य में, सामाजिक समरसता का इससे बड़ा उदाहरण कहाँ मिलेगा? इस सूक्त की पहली ऋचा देखिए-
न वा देवा: क्षुधमिद्वधं ददुरु-
ताशितमुप गच्छन्ति मृत्यव:।
उतो रयि: पृणतो नोप दस्यत्यु-
तापृणन्मर्डितारं न विन्दते।।
(ऋग्वेद.10:117:1)
ऋषि कहता है कि ‘भूखे ही नहीं मरते संसार में। मरते तो वे भी हैं, मित्र! जो पेट भर जीमते हैं अकेले। बाँट कर खाते-पीते , तो ठीक था। अकेले पेट भरते रहे अपना तो हुआ क्या? मर तो वे भी रहे हैं। द्वार पर खड़ा हुआ भूखा मांग रहा दो रोटियाँ। तुम अनदेखा कर बैठे घर में अपनी थाली सजा कर। मुँह में निवाला लेते हुए मन में हुआ नहीं कुछ। व्यर्थ हैं अन्न के भंडार। सच कहता हूँ,जमाखोरी ही तुम्हारी मृत्यु है। अकेले खाने वाले तुम पाप ही खाते रहे जीवन भर।’ यह है वेद की भाषा। इसकी सम्प्रेषणीयता ने आर्यों का चरित्र बदला, उसे नयी ऊँचाई दी। सदियों ने सामाजिक समरसता का पाठ हमें घुट्टी में पिलाया गया, जिसके आश्चर्यजनक परिणामों के रूप भारतीयता का उज्ज्वल चरित्र सामने आया।
यह सच है, कि वेद प्रार्थनाओं का विशाल संग्रह है। इतना बड़ा प्राचीन संग्रह भारतीय साहित्य को छोड़ किसी दूसरे साहित्य के पास नहीं है। ये जो वैदिक प्रार्थनाएँ हैं, किसी एक व्यक्ति के कुशल-क्षेम के लिये नहीं है, समाज की कुशलता के लिये है, समाजिक उत्कर्ष की लम्बी आयु के लिये है। केवल ऋग्वेद ही नहीं, यजुर्वेद भी सामाजिक अभ्युदय के मनोरथों से भरा हुआ है। वहाँ भले ही कर्मकाण्ड को एक यज्ञीय विधिशास्त्र के रूप में मान्यता मिली हुई है, लेकिन विनियोग के मंत्रों की बृहत् शृंखला हमें सीधे-सीधे हमारे समाज के सुख-दुःख से जोड़ती है। इस ओर से हम आँखें बंद किये बैठे हैं। वेद की भाषा और उसके अर्थ पर जायेंगे, तो हम भारतीयों मस्तक ऊँचा हो जायेगा। क्या सोचते थे हमारे ऋषि। उदाहरण के लिये प्रसिद्ध रुद्र सूक्त के केवल इस एक मंत्र पर दृष्टि डालिए-
मा नो महान्तमुत मा नो अर्भकं
मा न उक्षन्तमुत मा न उक्षितम्।
मा नो वधी: पितरं मोत मातरं
मा नः प्रियास्तन्वो रुद्र रीरिषः।।
हे रुद्र! मनुष्य समाज के वृद्धजनों को मत मारो। हमारे बच्चों को मत मारो।तरुणों को मत मारो।गर्भस्थ शिशु को मत मारो। पिता को मत मारो। माता को मत मारो। हमारे प्रिय जनों को मत मारो।
यह है भारतीय साहित्य में सामाजिक समरसता का निकष। कितनी अपार संवेदना? परदु:खकातरता की कैसी मार्मिक अभिव्यक्ति? कितनी उदात्त दृष्टि? इसी ने वेदों को सर्वोच्च गरिमा दी। मानवता की इस उच्चतम अभिलाषा ने ही वैदिक ऋषियों को चरितार्थता दी।
सहयोग और सामञ्जस्य, परस्पर प्रेम और भ्रातृत्व, एक मन और एक हृदय, एक चित्त और एक ध्यान, ये ही तो वे मधुर अभीप्साएँ हैं, जो वैदिक मंत्रों में सर्वत्र ही किसी न किसी रूप में परिलक्षित होती हैं अथर्ववेद में एक सांमनस्य सूक्त मिलता है, जिसमें आपके और हमारे परिवारों की वह प्रार्थना है, जो हमें आपस में जोड़ती है, सामाजिक समरसता का आश्वासन देती है। इस सूक्त के जो भाव हैं, वे द्रष्टव्य हैं-
ओ मेरे प्यारे भाई-बहन!
आओ, हम द्वेष का जंगल जला डालें।
आपस में मिल बैठ हँसें-बोलें,
साथ-साथ चल पड़ें ,
साथ-साथ काम करें।
हम सब साथ-साथ होंगे
तो सब देवता भी हमारे साथ होंगे।
हम सबमें समन्वय होगा
तो सब देवता भी हमारे निमित्त
आपस में सुसमञ्जस होंगे।।4।।
आओ सब,
कंधे से कंधा मिला कर आओ।
साथ-साथ आपस में हँसते-गाते आओ।
एकचित्त हो कर ऊपर उठो,
हम सबके मन की भी एक दिशा हो।
अथर्ववेद के इस सूक्त की सामाजिक उपादेयता सहस्रों सदियाँ बीत जाने के बाद भी ज्यों की त्यों बनी हुई है, तो इसकी एक यही वजह है कि भारतीय मन सामाजिक समरसता के आग्रह से अब भी भरा हुआ है। वह जानता है कि वेदोत्तरकाल और उसके बाद रामायणकाल और महाभारतकाल में भी भारतीय साहित्य का मूल स्वर सामाजिक समरसता ही है। इस सूक्त के अंतिम दो मंत्रों का मूल पाठ यहाँ भावार्थ के साथ देकर अपने कथ्य का समापन कर रहा हूँ।
समानी प्रपा सह वोन्नभागः
समाने योक्त्रे सह वो युनज्मि।
सम्ञ्चोऽग्निं सपर्यतारा
नाभिमिवाभितः।।
एक जगह बैठ कर जलपान करें हम,
एक जगह बैठ कर भोजन करें हम,
एक जगह मिलें, जुड़ें आपस में ऐसे,
रथचक्र की धुरी में तीलियाँ हों जैसे।
सध्रीचीनान् वः संमनसस्कृणो-
म्येकश्नुष्टीन्त्संवननेन सर्वान्।
देवा इवामृतं रक्षमाणा:सायं-
प्रातः सौमनसो वो अस्तु।।
बहुत कठिन है जीना यहाँ अकेले में,
मिल जाना श्रेयस्कर अपने मेले में।
अमृत की रक्षा सहज नहीं हो जाती,
यदि देवों की मति एक नहीं हो पाती।
– मुरलीधर चांदनीवाला