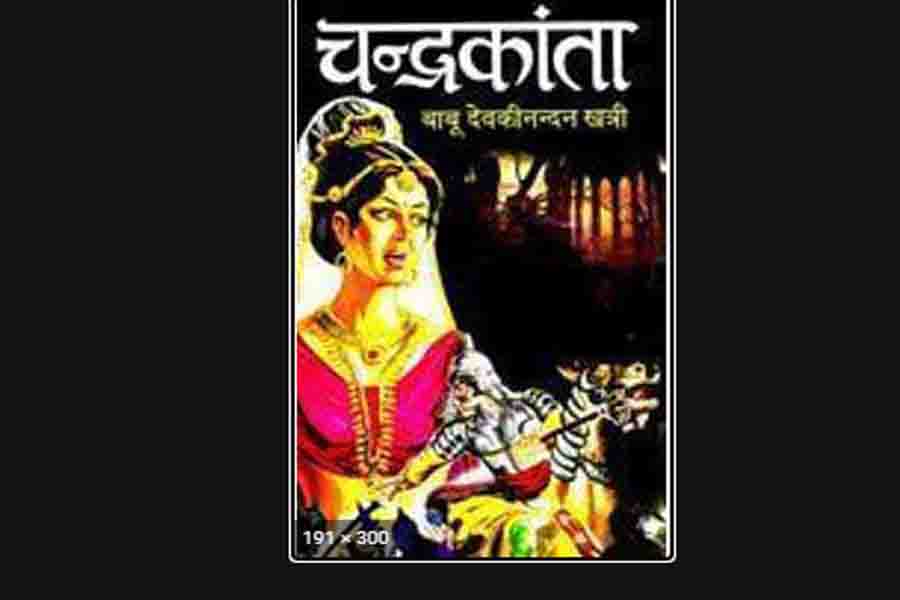सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश आध्यात्मिक दृष्टि से समृद्ध क्षेत्र है, जहां राम और कृष्ण ने जन्म लिया, बुद्ध और महावीर की तपोभूमि रही और बाबा विश्वनाथ, मां अन्नपूर्णा एवं मां विध्यवासिनी के आराध्य स्थल हैं। देवभूमि उत्तरांचल कभी उत्तर प्रदेश का ही अंग रहा, जहां केदारनाथ, बद्रीनाथ जैसे पवित्र धामों के अतिरिक्त गंगोत्री, जमुनोत्री जैसी पवित्र नदियों के रमणीक स्रोत हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल का अध्यात्म और धर्म के क्षेत्र में विशेष स्थान है। सर्वविद्या, धर्म और संस्कृति की राजधानी काशी (वाराणसी) की महिमा अद्भुत है। विश्व के प्राचीनतम नगरों में काशी ऐसी नगरी है, जो बाबा विश्वनाथ की नगरी के रूप में पूरे विश्व में प्रतिष्ठित है। प्राचीनकाल में वाराणसी का विशेष महत्व इसकी भौगोलिक स्थिति के कारण रहा। गंगा नदी के बायें (उत्तरी) तट पर अर्धचन्द्राकार में यह नगर आबाद है। काशी उद्भुत नगरी है। धार्मिक ग्रंथों में वाराणसी को काशी अर्थात ‘प्रकाश स्तम्भ’ कहा गया है, जिसे कैलाश पर्वत से उतरकर भगवान शिव ने अपना आवास बनाया। ऐसी मान्यता है कि काशी भगवान शिव के त्रिशूल पर स्थाप्ति है, इसलिए यह तीन लोकों से न्यारी है। विश्व में काशी ही एकमात्र ऐसा दिव्य तीर्थ है, जहां तीन नदियां, आठ कूप, ११ कुण्ड, ८४ घाट, एक ज्योतिर्लिंग, २९ छन्द, अष्ट रूद्र, अष्ट भैरव, २१८ देवियां, हनुमान पीठ, अष्ट यात्राएं, शक्तिपीठ, देवताओं और ऋषियों द्वारा स्थाप्ति ३२४ शिवलिंग और शिवमूर्तियां हैं। काशी में पांच हजार से अधिक मन्दिर हैं। हर गली में कोई न कोई मन्दिर है। सभी के ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व हैं। अमेरिका के प्रख्यात लेखक मार्क ट्वेन १८९६ में भारत यात्रा के दौरान वाराणसी आए थे। उनका मानना है कि वाराणसी में मन्दिरों की संख्या इतनी अधिक है कि उनकी गणना नहीं की जा सकती। गंगा स्वयं में एक मन्दिर है। काशी अद्भुत धार्मिक नगरी, जहां बौद्ध, जैन, सिख, मुस्लिम, ईसाई सभी के कोई न कोई तीर्थ है। वाराणसी ‘लघु भारत’ भी है, जहां देश के सभी राज्यों की धर्म और संस्कृति के दर्शन होते हैं।
काशी लोक और परलोक दोनों के लिए कल्याणकारी है। पूजन-अर्चन से लोक बनता है तो काशी में मरने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए काशी को ‘मुक्ति धाम’ भी कहते हैं। ‘मुक्ति’ के देवता यमराज हैं लेकिन बनारस में मुक्ति के देवता ‘शिव’ हैं। काशी को ‘महाश्मशान’ के रूप में भी जाना जाता है। यहां हजारों वर्षों से पवित्र गंगा नदी अपने तट से विचलित नहीं हुई। काशी में तीन श्मशान हैं, मणिकर्णिका, हरिश्चन्द्र घाट और मुर्दहवा घाट, जहां अन्तिम संस्कार किया जाता है। लोगों को ऐसा विश्वास है कि काशी लोगों को संसार से मुक्ति प्रदान करती है-‘काष्यां मरणान् मुक्ति:’ काशी की महिमा अपरम्पार है। विश्व में काशी ही अकेला ऐसा नगर है जिसके अनेक नाम हैं। काशी, बनारस, अविमुक्त क्षेत्र, आनन्द वन, रूद्र क्षेत्र, शिवपुरी, महाश्मशान जैसे अनेक नामों से विख्यात वाराणसी इसका आधुनिक नाम है। काशी की महिमा पर हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत सहित अनेक भाषाओं में जितनी पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं उतनी पुस्तकें विश्व के किसी एक नगर के बारे में प्रकाशित नहीं हुई हैं। मन्दिर, मठ, आश्रम, संत-महात्मा आदि से इस नगरी को काफी ख्याति मिली है। कुछ प्रमुख मंदिरों का संक्षिप्त विवरण यहां प्रस्तुत है-
काशी विश्वनाथ मन्दिर
बाबा विश्वनाथ का मन्दिर हिन्दू समाज के लिए असीम आस्था का केन्द्र है। हिन्दू धर्मानुयायी विश्व के किसी भी क्षेत्र में रहता हो, उसकी उत्कट अभिलाषा बाबा विश्वनाथ के दर्शन की रहती है। यह ज्योतिर्लिंगों में एक है। शिवपुराण काशी खण्ड के ३८वें अध्याय में उल्लेख है कि काशी विश्वनाथ के समान विश्व में दूसरा लिंग नहीं है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान विष्णु ने विधिवत पूजा-अर्चन करके विश्वनाथ लिंग की काशी में स्थापना की। भगवान शिव स्वयं पार्वती सहित काशी में स्थापित हुए। सतयुग में राजा कुबेर, राजा इन्द्र ने काशी में आकर शिव को प्राप्त करने हेतु तपस्या की और कुबेरेश्वर शिवलिंग की स्थापना की। सतयुग में चन्द्र, शुक्र, शनि, बृहस्पति, बुध आदि ग्रहों ने काशी में आकर विश्वनाथ की पूजा-अर्चना की और अपने नाम से शिवलिंग की स्थापना की। सतयुग के सभी ऋषियों, सन्तों, राजाओं ने काशी आकर बाबा विश्वनाथ की महिमा का गुणगान किया। वैदिक और पौराणिक ग्रंथों में ऐसे आख्यानों का उल्लेख है। मुगलों ने अनेक बार इस मन्दिर पर आक्रमण किए लेकिन अनेक राजाओं ने मन्दिर का पुनर्निर्माण कराया। १७८० में वर्तमान विश्वनाथ मन्दिर को इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होल्कर ने बनवाया। पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह ने नौ क्विण्टल सोना काशी विश्वनाथ के शिखर पर मढ़वाया। १८६० में नेपाल के राजा ने वहां नन्दी की स्थापना की। १९वीं शताब्दी में बाबा विश्वनाथ मन्दिर का महत्व और प्रताप बढता गया। गंगा के किनारे ८४ घाटों का निर्माण हुआ। बाबा विश्वनाथ का यह मन्दिर रात्रि ढाई बजे खुलता है और रात्रि ११:१५ बजे बन्द होता है। पूरे वर्ष में सवा से डेढ़ करोड़ भक्त दर्शन करते हैं।
मां अन्नपूर्णा मन्दिर
काशी विश्वनाथ मन्दिर के समीप विश्वनाथ गली में ही मां अन्नपूर्णा देवी का अति प्राचीन मन्दिर है। पौराणिक कथा के अनुसार माता अन्नपूर्णा आदि काल से गंगा के पूर्व काल से ही यहां विराजमान हैं। माता अन्नपूर्णा का मुख उत्तर-पश्चिम दिशा में है। चैत्र महीने की मनोहर तिथि को विशेष पर्व के रूप में मनाया जाता है। माता अन्नपूर्णा का पूजन सती अनसूया एवं महालक्ष्मी देवी ने किया था। माता के विग्रह पर चांदी के पत्ते का आवरण चढ़ा हुआ है। माता का स्वरूप अति दिव्य और सौम्य है। मां अन्नपूर्णा की स्वर्णमयी प्रतिमा मन्दिर के ऊपरी भाग में अवस्थित है, जिनके दर्शन दीपावली, धनतेरस, अन्नकूट में कराए जाते हैं। इस प्रतिमा में भगवान शिव मां अन्नपूर्णा से भिक्षा मांग रहे हैं। यह दर्शन रंगभरी एकादशी के दिन विशेष रूप से होता है। मन्दिर में प्रतिदिन भण्डारा चलता है, जहां हजारों श्रद्धालु भोजन का प्रसाद ग्रहण करते हैं। वर्ष में एक दिन भक्तों के बीच खजाना लुटाया जाता है। इस शक्ति स्थल की गणना देवी पुराण के अनुसार १०८ दिव्य शक्ति स्थलों में की जाती है। प्रति वर्ष ३० से ३५ लाख से अधिक भक्त दर्शन करने यहां आते हैं।
संकटमोचन हनुमान मन्दिर
हनुमान जी के इस प्रसिद्ध मन्दिर का निर्माण १७वीं शताब्दी में गोस्वामी तुलसीदास ने कराया था। तब से अब तक इस मन्दिर का जीर्णोद्धार कई बार हो चुका है। यह मन्दिर अत्यन्त शक्तिशाली है। प्रतिदिन बडी संख्या में श्रद्धालु नियमित रूप से दर्शन करते हैं किन्तु मंगलवार और शनिवार को दर्शानार्थियों की संख्या अधिक रहती है। इस मन्दिर में हनुमान जी की विराट प्रतिमा है। गोस्वामी तुलसीदास हनुमान के भक्त थे और उन्होंने ही हनुमान चालीसा की रचना की है। तुलसीदास जहां भी रामकथा कहते थे वहां सिल्क का कपडा बिछाकर रख देते थे। उनका विश्वास था कि हनुमान जी रामकथा श्रवण करने के लिए वहां अवश्य आ जाते हैं। एक दिन जब वे कथा कर रहे थे तब उन्होंने एक कोढ़ी व्यक्ति को वहां बैठे हुए देखा, जो बहुत ध्यानपूर्वक कथा को सुन रहा था। तुलसीदास ने समझ लिया कि वे हनुमान के अतिरिक्त कोई नहीं हो सकता। कथा समाप्ति के बाद तुलसीदास जी उसके पीछे-पीछे चलने लगे। कुछ दूर जाने के बाद उन्होंने हनुमान जी को प्रणाम किया और दर्शन देने का आग्रह किया। हनुमान जी ने तुलसीदास को अपना दर्शन दिया। दर्शन मिलने के बाद तुलसीदास ने इसी स्थान पर हनुमान जी से प्रतिष्ठित होने का अनुरोध किया, जिसे हनुमान जी ने स्वीकार कर लिया। इसलिए मन्दिर की मूर्ति को स्वयंभू कहा जाता है। यहां निरन्तर भजन-कीर्तन का आयोजन चलता रहता है।
काशी के अन्य मन्दिर
इसके अतिरिक्त वाराणसी में अनेक और मन्दिर हैं जहां श्रद्धालु आस्था और विश्वास के साथ पूजन-अर्चन करते हैं। इन मन्दिरों में शनिदेव मन्दिर, दुर्ग विनायक मन्दिर, १००८ श्री पार्श्वनाथ मन्दिर, मां विशालाक्षी मन्दिर, महालक्ष्मी मन्दिर, कालभैरव, केदारेश्वर, महामृत्युंजय महादेव, तिलभाण्डेश्वर, ओंकारेश्वर, तुलसी मानस मन्दिर, श्री कूष्मांड दुर्गा मन्दिर, त्रिदेव मन्दिर, बडा गणेश मन्दिर, गुरुद्वारा बडी संगत, मार्कंडेश्वर महादेव मन्दिर आदि प्रमुख हैं। सारनाथ में बौद्ध मन्दिर और जैन धर्म के २४ तीर्थकरों में चार तीर्थंकरों की जन्मभूमि भी वाराणसी में हैं, जहां उनके मन्दिर बने हैं। संत कबीरदास और संत रविदास के मन्दिरों में भी श्रद्धालुओं का निरन्तर आगमन होता रहता है। वैसे तो काशी मन्दिरों की नगरी है जिनकी संख्या की गणना सम्भव नहीं है। काशी के कण-कण में शिव व्याप्त हैं।
मां विंध्यवासिनी धाम
वाराणसी के पडोसी जिले मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी देवी का धाम है, जो आस्था का प्रमुख केन्द्र है। देश के विभिन्न जिलों के श्रद्धालु मां का दर्शन-पूजन करने के लिए विंध्यधाम आते हैं। नवरात्रि में यहां श्रद्धालुओं की काड़ी भीड़ रहती है। लाखों दर्शनार्थी प्रतिदिन मां के दरबार में मत्था टेकते हैं। इसके अतिरिक्त यहां मुण्डन संस्कार भी सम्पन्न होता है। दूर-दूर से लोग अपने पुत्र और पुत्रियों का सविधि मुण्डन कराने के लिए यहां आते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश का यह प्रमुख उपासना स्थल है।
मां विंध्यवासिनी के प्राकट्य की अद्भुत कथा है। श्री ब्रह्मा के पुत्र स्वयाम्भुव मनु और उनकी पत्नी सतरूपा मंदाकिनी के तट पर आदि शक्ति के दर्शन के लिए अत्यन्त कठोर तपस्या कर रहे थे। उनकी मनोकामना मां विंध्यवासिनी देवी के प्रत्यक्ष दर्शन की थी। अविकल तपस्या के परिणामस्वरूप उन्हें मां के दिव्य और मनोहर छवि का भान हो गया था। उन्होंने मां विंध्यवासिनी की प्रतिमा की रचना की एवं श्रद्धा और विश्वास के साथ षोडपोपचार विधि से पूजन-अर्चन किया। सम्पूर्ण आराधना के दौरान मनु और सतरूपा ने उपवास और संयम के साथ मां के चरण कमलों पर अपना ध्यान एकाग्र किया। उनकी निष्ठा पर प्रसन्न होकर मां विंध्यवासिनी अपने ज्योतिर्मय रूप में प्रकट हुई और कहा-‘मैं तुम दोनों की साधना से प्रसन्न हूं। अब मैं विंध्यशिखर पर जा रही हूं जहां मैं विंध्यवासिनी के रूप में पूजित होऊंगी। इसके बाद त्रिपुर सुन्दरी आद्यशक्ति मां विंध्यधाम में अवतरित हुई।’
विंध्यधाम और आदि शक्ति का उल्लेख औसनस, मार्कण्डेय, देवी भागवत, स्कन्द, अग्नि तथा शिवपुराण में है। औसनस उपपुराण के १ से ४१ अध्याय तक विंध्यमाहात्म्य पर ही विस्तार से वर्णन है। लक्ष्मीस्वरूपा मां विंध्यवासिनी के आगमन पर महाकाली खोह तथा सरस्वती स्वरूपा योगमाया के अष्टभुजा पर आने से यहां ज्ञान, कर्म और इच्छाशक्ति का त्रिकोण बनता है। सांसारिक इच्छा से आने वाले साधक में ऊर्ध्वमुखी विचारधारा बनने लगती है इस त्रिकोण यात्रा से।
गोरखनाथ मन्दिर
पूर्वी उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहर गोरखपुर में गोरखनाथ का प्रसिद्ध ऐतिहासिक मन्दिर है। नगर के मध्य में इस मन्दिर की उस जगह स्थापना की गयी है, जहां त्रेतायुग में गुरु गोरखनाथ साधना किया करते थे। ५२ एकड़ भूमि के परिसर में इस भव्य मन्दिर का निर्माण किया गया है। यह मन्दिर इस क्षेत्र के सर्वाधिक सुन्दर और विशिष्ट मन्दिरों में से एक है। प्रत्येक वर्ष १४ जनवरी को यहां मकर संक्रांति मेले का आयोजन किया जाता है। लाखों की संख्या में भक्त और पर्यटक इस मेले में सम्मिलित होते हैं। मेले में खिचड़ी चढाने की परम्परा है। गोरखनाथ मठ एवं मन्दिर नाथ परम्परा की आस्था स्थली है। गोरखनाथ शिव के प्रतिरूप माने जाते हैं। गुरु गोरखनाथ के नाम पर ही गोरखपुर जिले का नामकरण किया गया है। मुगल शासन काल के दौरान इस मन्दिर को नष्ट करने के लिए कई बार हमले किए गए। स्वर्गीय महन्त दिग्विजय नाथ और महन्त अवैद्यनाथ के प्रयासों से मन्दिर का वर्तमान स्वरूप विकसित हो पाया। गोरखनाथ मन्दिर का इतिहास काफी पुराना है। ११वीं शताब्दी में प्रख्यात योगी गोरखनाथ ने भारत के विभिन्न क्षेत्रों की यात्रा की और नाथ सम्प्रदाय पर अनेक पुस्तकों की रचना की। गुरु मच्छेंद्रनाथ ने नाथ सम्प्रदाय की स्थापना की थी। इस मन्दिर के माध्यम से शिक्षा, संस्कृति और मानव कल्यण के लिए भी अनेक कार्य किये जाते हैं। धार्मिक गतिविधियों के अतिरिक्त गोरखनाथ मन्दिर के महन्तों की राजनीति के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। महन्त अवैद्यनाथ लम्बे समय तक गोरखपुर से सांसद चुने जाते रहे। वर्तमान में महन्त योगी आदित्यनाथ लोकसभा के सदस्य हैं।
देवीपाटन मन्दिर
पूर्वी उत्तर प्रदेश के देवीपाटन मण्डल के पूर्वी सम्भाग में देवीपाटन मन्दिर है, जो ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। मां पाटेश्वरी देवी के नाम पर देवीपाटन मण्डल का गठन किया गया है। बलरामपुर जिले के तुलसीपुर में देवी पाटन मन्दिर आस्था का प्रमुख केन्द्र हैं, जहां भारी संख्या में श्रद्धालु दर्शन-पूजन के लिए आते हैं। हिन्दू मान्यताओं के अनुसार मां दुर्गा के ५१ शक्ति पीठों में से एक देवी पाटन मन्दिर है। दुर्गा पूजा के अवसर पर यहां वृहद धार्मिक आयोजन होता है, जहां देशभर से श्रद्धालु आते हैं। प्रत्येक वर्ष चैत्र मास में मेले का आयोजन होता है और शोभा यात्रा निकाली जाती है। नेपाल के डंग जिले से श्रद्धालु इस शोभा यात्रा में भाग लेते हैं, जो इसकी परम्पराओं का हिस्सा है। मन्दिर की बायीं ओर विशाल सूर्य कुण्ड है जिसका निर्माण कर्ण ने अपने पिता के सम्मान में किया था। १८५७ की क्रान्ति में महारानी ईश्वरी देवी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभायी थी। यहां पर एक विशाल हनुमान मन्दिर भी है जहां हनुमान की सबसे ऊंची प्रतिमा है।
अयोध्या के मन्दिर
भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या में है, जो करोड़ों हिन्दुओं की आस्था का केन्द्र है। राम को विष्णु का सातवां अवतार माना जाता है। उत्तर प्रदेश में फैजाबाद जिले के अन्तर्गत अयोध्या सरयू तट पर स्थित है। अयोध्या हिन्दुओं की पवित्र तीर्थ स्थली है। अयोध्या का इतिहास अत्यन्त प्राचीन है कभी यह अवध क्षेत्र की राजधानी थी। अथर्ववेद के अनुसार अयोध्या का निर्माण स्वयं देवताओं ने किया था, जहां वैभव का साम्राज्य था। शताब्दियों तक यह कोशल देश की राजधानी रही। अनेक राजाओं ने यहां शासन किया था। इनमें इक्ष्वाकु, प्रिथू, मांधाता, हरिश्चन्द्र, सगर, भगीरथ, रघु, दिलीप, दशरथ और राम जैसे प्रतापी राजाओं के नाम आते हैं। अयोध्या के शासन और वहां की वैभव गाथाओं का विवरण रामायण और रामचरित मानस जैसी अमर कृतियों में वर्णित है। अयोध्या का धार्मिक महत्व बौद्ध, जैन और सिंख धर्मावलम्बियों के लिए भी है। पांच जैन तीर्थकरों की जन्मभूमि अयोध्या है। सिख गुरु नानक देव जी, गुरु तेग बहादुर और गुरु गोविन्द सिंह भी अयोध्या आ चुके हैं। अयोध्या में रामकोट का ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व है। मार्च-अप्रैल में पडने वाली रामनवमी को यहां देशभर से श्रद्धालु आते हैं। रामनवमी को भगवान राम का जन्म दिवस सोल्लास मनाया जाता है। हनुमान गढी अयोध्या का सर्वाधिक महत्वपूर्ण मन्दिर है। यह दसवीं शताब्दी का मन्दिर है। यहां हनुमान जी की भव्य प्रतिमाएं हैं। कनक भवन अत्यन्त ही आकर्षक और सुसज्जित मन्दिर है, जिसका निर्माण मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ की महारानी ने १८९१ में कराया था। नागेश्वर नाथ मन्दिर भी काफी प्रसिद्ध है। कथानक के अनुसार भगवान राम के पुत्र कुश ने इसका निर्माण कराया था। वर्तमान मन्दिर का निर्माण १७५० में कराया गया। त्रेता के ठाकुर, छोटी देवकली मन्दिर, मणि पर्वत, राम की पैड़ी के अतिरिक्त जैन मन्दिर और गुरुद्वारे भी दर्शनीय स्थल हैं।
तीर्थराज प्रयाग का कुम्भ
प्रयाग (इलाहाबाद) को तीर्थराज कहते हैं। यह भारत का प्राचीन तीर्थस्थल है। आध्यात्मिक दृष्टि से प्रयाग का विशेष महत्व है। यह देश का पवित्रतम तीर्थ है। इलाहाबाद तीन नदियों गंगा, यमुना, सरस्वती नदियों के संगम तट पर स्थित है। वर्ष पर्यन्त हजारों तीर्थ यात्री संगम पर स्नान करते हैं लेकिन महाकुम्भ पर अपार जनसैलाब यहां उमड़ पडता है। देश के विभिन्न क्षेत्रों और विदेशों से लोग यहां आते हैं। कुम्भ मेले की विश्व के प्रमुख धार्मिक मेलों में गणना होती है। प्रयाग में ज्ञान की पर्याय सरस्वती, ऋषि तपश्चर्या से उठी गंगा और प्रेम-रस से सराबोर यमुना भाव-विह्वल होती हैं। ऋग्वेद के कवि ‘इमे गंगे यमुने सरस्वती शुतुद्रि’ गाकर इनकी स्तुति करत हैं। प्रयाग यज्ञ की विशिष्ट भूमि है। प्रयाग में आयोजित कुम्भ पर्व के विविध आयाम हैं। इस पर्व के आयोजन के पीछे धार्मिक, सांस्कृतिक, राष्ट्रीय एवं सामाजिक उद्देश्य हैं। इस पर्व का उल्लेख ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद में हुआ है। स्कन्दपुराण, विष्णुपुराण, ब्रह्माण्डपुराण, शिवपुराण, मत्स्यपुराण आदि में इसके माहात्म्य का वर्णन है। कुम्भ भारत का धार्मिक-सांस्कृतिक पर्व है। पुराणों में उल्लिखित है कि कुम्भ में स्नान करने से व्यक्ति के दस पहले और दस बाद की पीढ़ियों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। कुम्भ हमारी धार्मिक और सांस्कृतिक एकता को अविच्छिन्न बनाए रखने के लिए किए गए सामूहिक प्रयत्नों का देदीप्यमान प्रतीक है। कुम्भ में मठों और अखाडों की सहभागिता की मजबूत परम्परा है। कुम्भ का आध्यात्मिक माहात्म्य तो है ही, यह राष्ट्रीय एकता का सशक्त माध्यम भी है। यह आस्था और विश्वास का महापर्व है।
उत्तर प्रदेश का सम्पूर्ण पूर्वांचल अपनी आध्यात्मिक, धार्मिक और सांस्कृतिक विशिष्टताओं से समृद्ध है। सभी जिलों में आस्था के केन्द्र हैं। कोई भी जनपद इससे अछूता नहीं है। इस आलेख में मात्र कुछ ही जिलों के प्रमुख उपासना स्थलों का उल्लेख किया गया है।