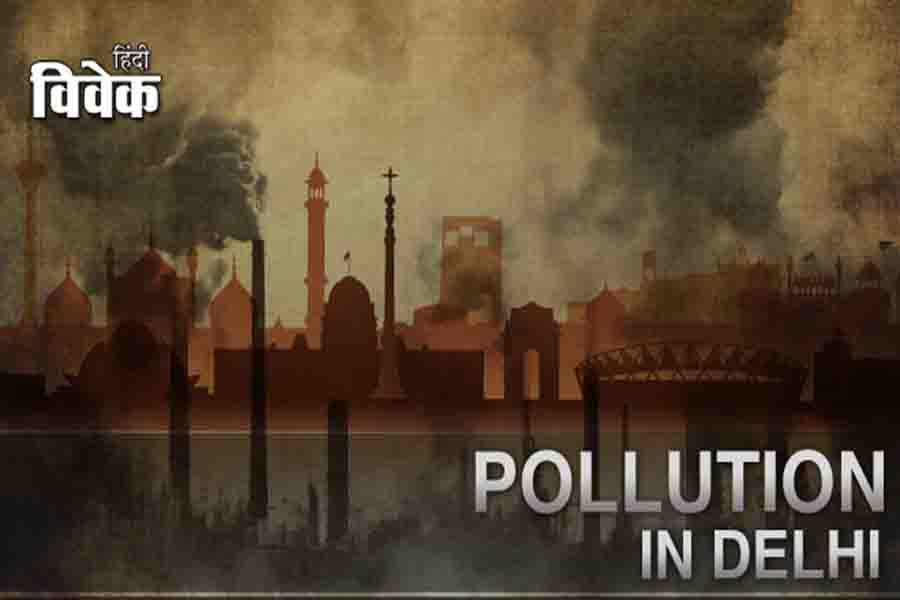देश की राजधानी दिल्ली में पिछले माहभर में हाहाकार था। लोगों की जान सांसत में पड़ गई थी। सांस लेना मुश्किल हो रहा था। प्रकृति से खिलवाड़ की सजा आदमी भुगत रहा था। हवा दूषित हो गई थी। पानी को आप शुद्ध कर लेंगे, भूमि को दूषित होने से रोक लेंगे, पेड़-पौधों को कीट-पतंगों से बचा लेंगे, मिलावटी अन्न से निजात पा लेंगे; लेकिन आसमानी हवा को आप कैसे शुद्ध कर लेंगे? न शुद्ध हवा होगी और न मनुष्य के प्राण बचेंगे। दिल्ली ने इस वर्ष यह भीषण ‘पर्यावरण संकट’ झेला । बुजुर्ग कहते हैं कि दिल्ली में इस तरह की धुंध कभी नहीं रही, न कभी सांस लेने में इतना कष्ट हुआ। यह स्थिति कमोबेश आज भी चल रही है।
यह संकट दिल्ली के लिए नया नहीं है। जिन लोगों ने दिल्ली और उत्तर भारत की सर्दियां एवं ठिठुरन देखी है उनके लिए कोहरा नया नहीं है। हफ्ते में एकाध बार ही सूर्य दर्शन या धूप खिल जाना भी नया नहीं है। इस बार नया यह है कि यह कोहरा नहीं, धुंध थी और यह धुंध पंजाब एवं हरियाणा के खेतों से उठी थी। खेतों में पड़े ठूंठ एवं घासफूस जलाने के कारण धुएं के बादल आकाश में उठे। कुंद हवा के कारण वे दिल्ली समेत आसपास के इलाके के आकाश में छा गए। जलने की तीव्र गंध भी वे अपने साथ ले आए। यह सब जहरीली गैसनुमा बन गया। इसीलिए लोग दिल्ली को ‘गैस चेम्बर’ कहने लगे। ‘गैस चेम्बर’ शब्द हिलटर के कारण प्रचलन में आया; क्योंकि हिटलर अपने दुश्मनों को कमरे में बंद कर उसमें जहरीली गैस छोड़ कर उन्हें मार डालता था। दिल्ली राजधानी परिक्षेत्र में वाहनों आदि से पहले से ही वायु प्रदूषण मौजूद है। उसके साथ खेतों से आया धुआं मिल जाने से वह खतरनाक स्तर तक पहुंच गया था।
पंजाब एवं हरियाणा में खरीफ की पहली फसल धान की होती है। उसकी कटाई मशीनों से करने का प्रचलन बढ़ गया है; क्योंकि यह सस्ता पड़ता है और फौरन होता है। मशीनें धान की बालियां ऊपर ही ऊपर काटती हैं। इससे पौधों के बड़े ठूंठ खेतों में बने रहते हैं। इन ठूंठों को मजदूर लगा कर सतह से काटना महंगा सौदा होता है। इसलिए किसान इन ठूंठों और घासफूस जैसे अन्य अवशिष्ट को जला देते हैं। इससे खेत समतल हो जाता है और रबी की अगली गेहूं की फसल के लिए जमीन तैयार होती है। देश के अन्य भागों में धान के ठूंठ पशुचारे के रूप में प्रयुक्त होते हैं, लेकिन पंजाब-हरियाणा में ऐसा करना बहुत महंगा पड़ता है। पहले कटाई के लिए मजदूर लगाए जाते थे, वे जमीनी सतह से पौधे काटते थे, फिर हलर में डाल कर चावल अलग व भूसी अलग निकलती थी। भूसी पशुओं के काम आती थी। सब कुछ प्राकृतिक था, अब कृत्रिम हो गया है। इसकी सजा तो भुगतनी पड़ेगी ही।
इस प्रदूषण ने गांव और शहर के बीच युद्ध का संकेत दे दिया है। शहर वाले कहते हैं कि गांव वालों के खेती में अवशिष्ट जलाए जाने के कारण यह जहरीली धुंध बनी, किसान कहते हैं, हम साल भर थोड़े ठूंठ जलाते हैं, फिर शहरों में धूल-धड़क्का और वायु प्रदूषण कहां से आता है? शहर वालों ने तो हमारी नदियां और जल स्रोत तक प्रदूषित कर दिए! इस धुंध के लिए हमें दोष न दें। ये आपकी ही देन है, भुक्तभोगी तो हम हैं। अपनी धूलभरी सड़कों, आलीशान वाहनों, ट्रकों, कनठैया आवाज को रोको; फिर हमें अक्ल सिखाना। पर्यावरण तो शहर वाले बिगाड़ते हैं, गांव वाले तो उसे बचाते हैं। खैर, यह इस आलेख का विषय नहीं है; लेकिन इस बहाने पंजाब-हरियाणा और दिल्ली वालों में जो तू तू-मैं मैं चली उससे भविष्य के संघर्ष के संकेत मिलते हैं।
देश भर में कोई ५-६०० मेट्रिक टन कृषि अवशिष्ट जलाया जाता है। इसमें उ.प्र. में ६० मेट्रिक टन, पंजाब में ५१ मेट्रिक टन तथा महाराष्ट्र में ४६ मेट्रिक टन कृषि कचरा हर साल जलाया जाता है। इसमें धान का ३४% और गेहूं का २२% हिस्सा है। अतः किसानों के प्रति बहुत कड़ा रुख अपनाना राज्य सरकारों के लिए मुश्किल रहा। फिर भी राज्यों ने ठूंठ या घासफूस जलाने लिए प्रति हेक्टर २५०० रु. जुर्माने की घोषणा की, पर किसान नहीं झुके। पंजाब में केवल महज १४०० मामलों में चालान होना इस बात का सबूत है। शहरी क्षेत्रों में भी कचरा जलाना अब प्रतिबंधित कर दिया गया है; लेकिन महानगरपालिकाओं के डम्पिंग ग्राउंड में जलने वाले कचरे पर कोई जवाब नहीं है।
किसानों की बात में दम है। निम्न तालिका में देखें कि शहर वालों ने वाहनों, उद्योगों, ईंट भट्टों, बिजली घरों और घरेलू कचरे से निकलने वाले धुएं से अपने शहरों को किस कदर जहरीला बना दिया है। इसमें कृषि जलावन का हिस्सा महज ८ फीसदी है।
दिल्ली में वायु प्रदूषण के स्रोत- प्रतिशत
| स्रोत | पीएम – २ . ५ | एसओ – २ | एनओ – एक्स |
| वाहन | १७ | 2 | ५३ |
| डीजल जनरेटर | ६ | ४ | २५ |
| ईंट – भट्ट | १५ | ११ | 2 |
| उद्योग | १४ | २३ | ११ |
| भवन – निर्माण | ५ | – | १ |
| कृषि जलावन | ८ | १ | १ |
| सड़कों की धूल | ६ | – | – |
| बिजली घर | १६ | ५५ | ७ |
| घरेलू | १२ | ६ | १ |
दिल्ली तो दुनिया का सब से जहरीला शहर बन गया है। चीन की राजधानी बीजिंग से भी दुगुना जहरीला। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट में विश्व के दस सर्वाधिक प्रदूषित शहरों के नाम दिए गए हैं, जिनमें दिल्ली पहले नम्बर पर है। इसके बाद पटना, ग्वालियर, रायपुर तथा अमदाबाद तथा लखनऊ नौवें व दसवें नम्बर पर है। पाकिस्तान के कराची, पेशावर व रावलपिंडी ५ से ७वें तथा ईरान का खोरादाबाद शहर ८वें नम्बर पर हैं। यह सर्वेक्षण २०१४ का है, जिसकी रिपोर्ट दिसम्बर २०१५ में जारी की गई। इस वर्ष यह स्तर ‘आपात् स्थिति’ तक पहुंच गया।
इस प्रदूषण को किस तरह नापते हैं, इसे यह जरा समझ लें। इससे वायु में जहरीले कणों की मात्रा का पता चलता है। इसे पीएम-२.५ एवं पीएम-१० कहते हैं। एसओ-२ का मतलब है सल्फरिक ऑक्साइड। विभिन्न तरीकों से गैसों के मिश्रण से बनने वाली हवा को वोलाटाइल आर्गेनिक कम्पाउंड (वीओसी) कहते हैं। इनसे भूमि पर ओजोन की परत नष्ट होती है। इसे ओजोन-३ कहते हैं। जमीनी सतह से ओजोन की परत नष्ट होने का मतलब है आक्सीजन की कमी। पीएम का अर्थ है पार्टिकल मैटर याने धूलि कण। पीएम-२.५ का अर्थ है एक वर्ग मीटर वायु में २.५ माइक्रोमीटर सूक्ष्मता के धूलि कण होना। ये कण मानवी बाल से २८ गुणा छोटे होते हैं। मानवी बाल लगभग ७० माइक्रोमीटर मोटा होता है, जबकि ये कण २.५ माइक्रोमीटर या उससे भी छोटे होते हैं। इससे इनकी सूक्ष्मता का हम अंदाजा लगा सकते हैं। पीएम-१० का मतलब इसी तरह है याने ऐसे कण हवा में मिल जाना जिनकी मोटाई १० माइक्रोमीटर या उससे भी कम है याने ये भी मानवी बाल से छोटे हो गए। पीएम-१० अधिकतर सड़क के किनारों की धूल, उद्योग की निकासी या वाहनों से निकलने वाले धुएं के सूक्ष्म कण होते हैं। पीएम-१० प्रदूषण में धूल का हिस्सा ५०%, उद्योगों के धुएं का हिस्सा २३% और वाहनों का हिस्सा ७% होता है। मोटी तौर पर यह मान सकते हैं कि पीएम-२.५ अत्यंत सूक्ष्म कण और पीएम-१० उससे चार गुणा मोटे कण होते हैं। इसलिए वायु प्रदूषण सूचकांक में पीएम-१० की संख्या पीएम-२.५ से हमेशा अधिक होती है। इस फर्क को प्रदूषण का अंदाजा लगाते समय हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। मिसाल के तौर पर पीएम-२.५ का सूचक अंक २५१ और पीएम-१० का सूचक अंक ४३१ से आगे बढ़ने पर ‘पर्यावरणीय आपात् स्थिति’ मानी जाती है। इस वर्ष दिल्ली में ये अंक क्रमशः ६१२ और ६७३ तक पहुंच गए थे। इसे ही वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) कहा जाता है। यह अंक जितना अधिक उतना ही मानवी जीवन को संकट अधिक। पशु-पक्षी भी इससे अछूते नहीं रहते। इसे प्राकृतिक नरसंहार की निचली सीढ़ी मान सकते हैं। परमाणु बम से भी अधिक यह ‘पर्यावरण बम’ विनाशक है। इससे श्वसन विकार, अस्थमा, फेफड़ों की बीमारियां, एलर्जी, कैंसर, हृदय-रोग, हड्डियों के रोग, रक्त विकार, चर्म-विकार, नस-तंत्र व गर्भ पर विपरीत असर और न जाने क्या-क्या हो हो सकता है। बच्चों, बूढ़ों और महिलाओं पर इसका सर्वाधिक असर पड़ता है।
पिछले तीन वर्षों में दिल्ली में प्रदूषण से पीड़ित बीमारों की संख्या में लगातार बढ़ोत्तरी हो रही है। देखें निम्न तालिका-
| अस्पताल | २०१२ | २०१३ | २०१४ |
| वीपीसी | १६६०४ | १६८५९ | १६७५९ |
| एम्स | ५१५९ | ८१३५ | ९३७८ |
(उपर्युक्त बड़े सरकारी अस्पताल हैं। मेदांता और सर गंगाराम जैसे निजी बड़े अस्पतालों में रोगियों की संख्या प्रति वर्ष ३० से ३५% से बढ़ रही है। छोटे अस्पतालों या निजी डॉक्टरों से इलाज करने वालों की संख्या जोड़ दें तो स्थिति ज्यादा गंभीर दिखाई देगी। )
इस वर्ष अक्टूबर के आरंभ से ही दिल्ली परिसर में वायु प्रदूषण महसूस होने लगा। अमुमन दीवाली के समय पटाखों आदि के कारण वैसे तो हर वर्ष प्रदूषण बढ़ता ही है, लेकिन इस वर्ष पटाखे कम चलाए जाने के बावजूद प्रदूषण की मात्रा खतरनाक स्तर पर पहुंच गई। दिल्ली उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय तक याचिकाएं दायर हुईं और ‘जनस्वास्थ्य आपात्काल’ घोषित करने की मांग की गई। अदालतों ने इस पर केंद्र से लेकर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, केंद्र से भी हलफनामे दाखिल करने के लिए कहा।
केवल दिल्ली ही नहीं, देश के अन्य शहरों की स्थिति दिन-ब-दिन किस तरह खराब होती जा रही है। मुंबई में सड़कों पर धूल एवं बिजली व अन्य कारखानों से ५०% से अधिक प्रदूषण होता है। चेन्नई में वाहन प्रदूषण सब से बड़ा कारण है। बेंगलुरू में प्रति वर्ष ५% की दर से प्रदूषण बढ़ रहा है। कोलकाता में ७०% प्रदूषण का कारण वाहनों से निकलने वाला धुआं है।
दुनिया में भी वही हालत
ऐसी स्थिति दुनिया के अन्य बडे शहरों में भी रही है और वहां इस समस्या से निजात पाने के लिए क्या उपाय किए जाते हैं यह भी गौर करने लायक है। इन शहरों में वायु प्रदूषण का स्तर खतरे के निशान तक पहुंचते ही सभी स्कूल बंद कर दिए जाते हैं। वाहनों को सड़कों पर आने से रोक दिया जाता है। कल-कारखाने बंद कर दिए जाते हैं। गैस-मास्क का सार्वजनिक वितरण किया जाता है।
ब्रिटेन ने वायु प्रदूषण पर कैसा नियंत्रण किया यह देखें- राजधानी लंदन में आने वाले वाहनों से ११.५० पौंड शुल्क लिया जाता है, यह न चुकाने पर १९५ पौंड का जुर्माना होता है, अगले वर्ष अर्थात २०१७ से उन वाहनों को १० पौंड अतिरिक्त देने पड़ेंगे जो २००५ के पूर्व बने हो, २०१९ से प्रदूषण मानक पूरे न करने वाले वाहनों को ६५० पौंड का भारी जुर्माना देना होगा।
इटली ने अपनी राजधानी मिलान में निजी कारों पर छह घंटों एवं दुपहिया वाहनों पर ३ दिन का प्रतिबंध लगाया, सार्वजनिक बसों पर केवल डेढ़ यूरो में दिन भर यात्रा करने की मोहलत दी गई। रोम में ऑड-ईवन योजना लागू की गई (याद रहे दिल्ली में भी इसका प्रयोग हो चुका है)। सेंट वितलियागो में लकड़ियां जलाने पर रोक लगा दी गई।
चीन ने अपने यहां ऑड-ईवन योजना लागू की। राज्य के बाहर के वाहनों के आने पर प्रतिबंध लगाया गया। प्रदूषण फैलाने वाले २,००० कारखानों को बंद किया गया। प्रदूषण फैलाने पर भारी जुर्माना एवं निर्माण-कार्य स्थल पर प्रदूषण की निगरानी के लिए बड़े पैमाने पर निरीक्षक नियुक्त किए गए। बीजिंग में २०१४ से ‘प्रदूषण के विरुद्ध युद्ध’ अभियान आरंभ किया गया। कोरिया में २००५ से वायु प्रदूषण के लिए विशेष कानून लागू है। उद्योगों और वाहनों के लिए कड़े प्रदूषण मानक लागू किए गए। प्रदूषण को नियंत्रित रखने वाले उद्योगों के लिए पुरस्कार की योजना लागू की गई।
भारत में भी राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल- एनजीटी) कार्यरत है। पिछले दस माह पूर्व प्रदूषण नियंत्रण के लिए विभिन्न उपायों की विस्तृत योजना बनाई गई थी। नया हरित कर भी लगाया गया है। लेकिन राज्यों ने इसे बहुत गंभीरता से नहीं लिया और योजना धरी की धरी रह गई। अब पुनः जोरशोर से बैठकें हो रही हैं। सरकार ने १५ वर्ष पुराने ट्रकों और अन्य वाहनों को रद्द कर दिया है। इनकी संख्या कोई पौने दो लाख है। बदरपुर इलाके में स्थित कोयले पर आधारित बिजली कारखाना बंद कर दिया गया है। ईंट भट्टों को बंद कर दिया गया है। पत्थर की खानों में काम रोक दिया गया है। इमारत निर्माण-कार्य रोक दिया गया था, लेकिन अब उपराज्यपाल ने पुनः शुरू कर दिया है, जिसे लेकर केजरीवाल और उपराज्यपाल के बीच नोंकझोंक चल रही है। सड़कों पर पानी छिड़कने का उपाय कुछ दिन चला, लेकिन अब रोक दिया गया है; क्योंकि इसे बहुत व्यावहारिक नहीं माना गया है। पंजाब सरकार ने धान के ठूंठ जलाने के लिए यंत्र मुहैया करने की १६०० करोड़ रु. की योजना बनाई है। अन्य राज्यों से भी इसी तरह की योजनाएं बनाने के लिए कहा गया है। कृषि अर्थशास्त्री एम.एस.स्वामिनाथन ने कृषि कचरे से बिजली निर्माण की योजना का सुझाव दिया है।
विश्व में हर साल वायु प्रदूषण से ७० लाख लोग मरते हैं। इनमें भारत में मरने वालों की संख्या सर्वाधिक है। वायु प्रदूषण का सर्वाधिक कहर तो भोपाल में १९८४ में हुआ था, जब यूनियन कार्बाइड नामक कारखाने से जहरीली गैस रिसी थी। इससे हजारों लोग पीड़ित हुए और अगली पीढ़ियों तक इसका प्रभाव झेलना पड़ रहा है। प्रकृति का अति दोहन एवं उससे खिलवाड़ मानव जाति के लिए संहारक बन कर उभर रहा है। मानवी व्यवहार में जब तक सुधार नहीं होता तब तक इसमें बदलाव की संभावना नहीं है। या तो मनुष्य को बदलना होगा या प्रकृति उसे बदल देगी- लूला-लंगड़ा बना देगी या संहार कर देगी। हमारे पौराणिक साहित्य में जल प्रलय का जिक्र है, लेकिन कभी वायु-प्रलय भी होगा इसकी शायद किसी ने कल्पना नहीं की होगी। दिल्ली का नरसंहारक वायु प्रदूषण हम नियंत्रित न कर सके तो भारत वायु-प्रलय की मिसाल बनेगा।