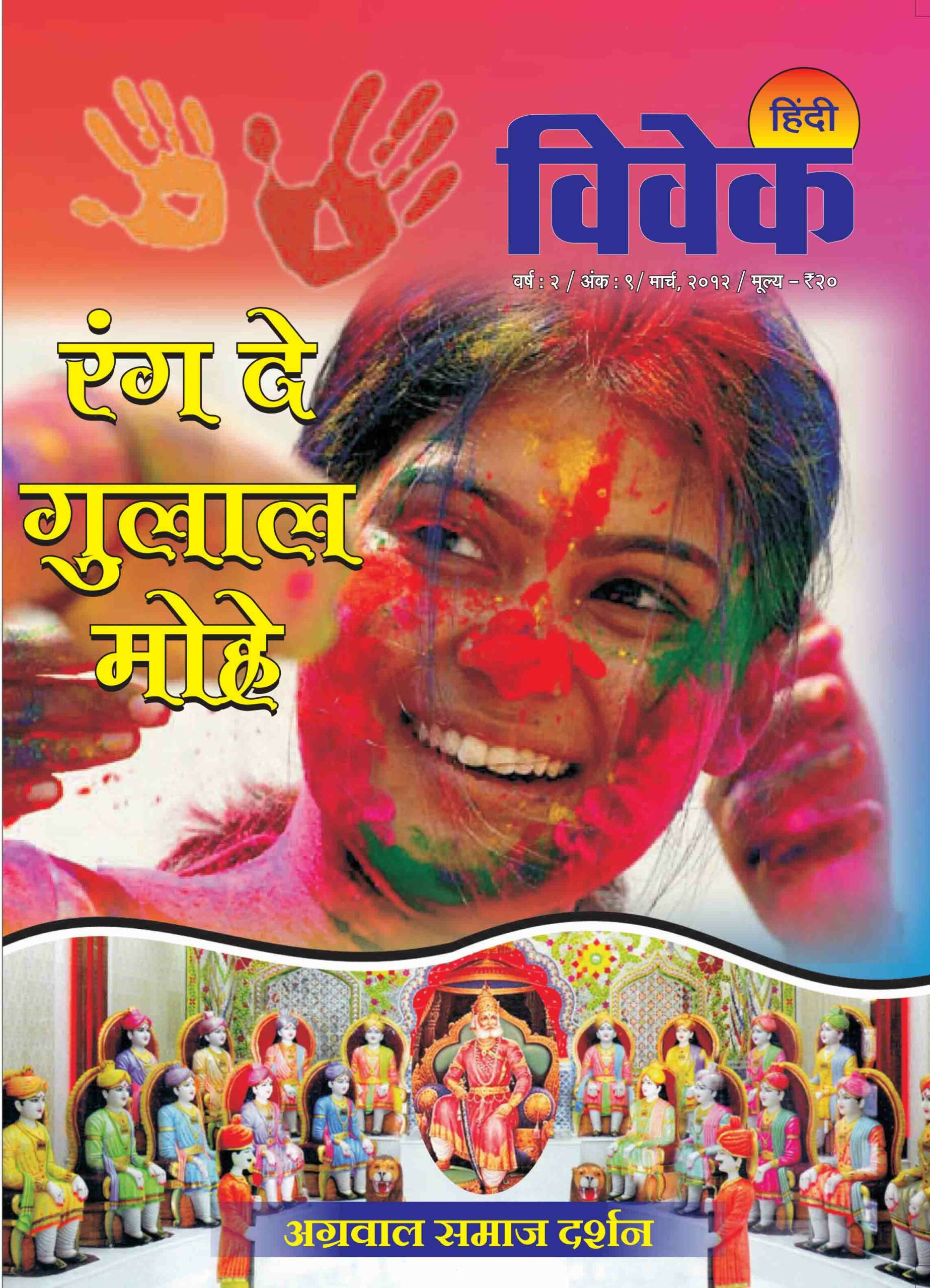क्या आपको अब्बासमस्तान निर्देशित ‘अग्निकाए’ नामक फिल्म याद है?
उसमें गुजरात के एक छोटे नगर के राजनीतिकसामाजिक.आपराधिक तानेबाने की फिल्मी कहानी थी। उस कहानी में चुनाव (?) आता है और खलनायक भारी वोटों से जीत जीतने के लिए वेश्याओं, हिजड़ों की बस्तियों में जाकर और आपराधिक लोगों से सांठगांठ कर विजयी बनाने की अपील करता है और उनके वोटों की बदौलत चुनाव जीत भी जाता है। वोटों के इस सहयोग के लिए खलनायक धन्यवाद देता है और अपने भाषण में कहता है, ‘मैं सही अर्थ में लोकतंत्र का समर्थक हूं। इसीलिए मैंने आम आदमी की तरह समाजकंटक समझ कर हिकारत से देखे जाने वाले वाले लोगों के भी वोट प्राप्त किए। मैं गुंडों का समर्थन करता हूं यह आरोप विरोधी मुझ पर करते हैं। लेकिन अपराधी भी मतदाता हैं। मैं उनकी सुरक्षा और उनके भविष्य के बारे में सोचता हूं इसे गलत कैसे कहा जा सकता है?’
सदाशिव अमरापुरकर किसी परिपक्व खलनायक को साकार करने में सफल हो गए।
कुल मिलाकर फिल्म महज फिल्म और उथली लगती है। इस फिल्म के कारण कुछ हिंदी फिल्म वालों की चुनाव प्रक्रिया के प्रति दृष्टि भी स्वैराचार जैसी दिखाई देने लगी।
गुलजार लेकिन इस लीक में नहीं बैठते। उन्हें लोकतंत्र का अर्थ और चुनाव का महत्व ज्ञात है। उसका प्रतिबिम्ब उनकी फिल्मों में दिखाई देता है। अब तब आपको गुलजार के निर्देशन और जे. ओमप्रकाश निर्मित फिल्म याद आ गई होगी। वास्तव में मैं ‘आंधी’ फिल्म को राजनीतिक फिल्म नहीं मानता। वह राजनीति की पार्श्वभूमि में गुलजार शैली की प्रेम कहानी थी। राजनीतिक महत्वाकांक्षा रखने वाली पत्नी के कारण (सुचित्रा सेन) पति (संजीव कुमार) को बौध्दिक स्तर पर विरह सहन करना पड़ता है। राजनीतिक दांवपेंचों में पत्नी उलझती जाती है। इस माहौल में चुनाव आ जाते हैां इसीके साथ प्रचार, घोषणाएं, रैलियां, आश्वासन, आरोप, अफवाहें का मिश्रण होता है। एक बार प्रचार सभा में हुई पत्थरबाजी में नायिका को चोट पहुंचती है। इस घटना पर राजनीति होती है। फलस्वरूप जनता की सहानुभूति पाकर वोट बटोरने का प्रयास भी होता है।
गुलजार ने भारतीय लोकतंत्र में चुनाव प्रक्रिया दिखाने का प्रयास किया है। यथार्थ को ठीकठाक पेश किया है। वह उनके स्वभाव के अनुकूल ही है।
फिल्मों चुनाव विषय पर ये दो भिन्न ‘फोकस’ है। पहले में कितना तो उथलापन है, जिससे खुल कर इनकार भी नहीं किया जा सकता। दूसरे में ‘यथार्थ’ है, जिसे सहजता से टाला भी नहीं जा सकता।
लेकिन समाज में व्याप्त बुराईभलाई की असंख्य घटनाओं के साथ चुनाव, मतदान, रैलियां, पराजय की चोट, उससे उपजने वाली हिंसा जैसी कई बातें फिल्मों में आती हैं। यह भी एक ‘रियलिटी शो’ है। इतनी विविधता शायद दुनिया की किसी फिल्म में दिखाई न देती होगी। यही तो हमारी हिंदी फिल्मों की विशेषता है।
गोविंद निहलानी निर्देशित ‘अर्ध सत्य’ का रामा शेट्टी (सदाशिव अमरापुरकर) आतंक के बल पर चुनाव जीत कर प्रतिष्ठित हो जाता है। उसका सामाजिक प्रभाव अस्वस्थ कर देता है।
के. सी. बोकाडिया की फिल्म ‘फूल बने अंगारे’ जैसी भडकीली फिल्म में राजनीति व फलस्वरूप मतदान का दर्शन होता है। बोकाडिया का वास्तव में किस राज्य की मतदान प्रक्रिया पर ‘फोकस’ था यह वे ही जाने। लेकिन उन्होंने मतदान की पहली रात को उम्मीदवारों से मतदाताओं को पैसा, कपड़े, कुछ घरेलू कीमती चीजों का बांटना, मतदान के दिन गुंडों का मतदान केंद्र पर कब्जा करना, फिर स्वयं ही मतपत्रिका पर मुहर लगाना, कभी तों मतपेटियां उठा लेना इस तरह की जबरन हिंसा भी दिखाई है। कुछ राज्यों में इसी तरह चुनाव लड़े और जीते जाते हैं। लेकिन परम्परागत लोकप्रिय फिल्मों में ये घटनाएं मिर्चमसाले के साथ पेश की जाती हैं। तब दुर्भाग्य से ये घटनाएं सच ही लगती हैं। ऐसे समय लोकतंत्र पर भरोसा रखने वालों का विश्वास भी डगमगा जाता है। हम कतार में खड़े रहकर अपने विवेक से मतदान करते हैं, जिससे कुछ राज्यों (अथवा कुछ छोटे शहर या गांव) में यह प्रक्रिया हिंसात्मक होती है इसे मानना कठिन हो जाता है। कई बार तो फिल्मों में मतदान इसी तरह गांव के स्तर का ही होता है।
निर्मातानिर्देशक एन. चंद्रा ने ‘प्रतिघात’ में इसी तरह एक राक्षसी महत्वाकांक्षा रखने वाले राजनीतिक नेता (चिरंजीवी) का दर्शन कराया। उस समय नासिक में चल रहे फिल्मीकरण के लिए मुंबई के हम कुछ पत्रकारों को निमंत्रित किया गया था। एन. चंद्रा ने चुनाव प्रचार रैली के लिए स्थानीय नागरिकों का खूबी से उपयोग किया था। एन. चंद्रा ने नासिक में फिल्मीकरण कर अच्छा लाभ उठाया यह स्पष्ट हुआ। चंद्रा के नासिक में फिल्मीकरण के समय भी वे पत्रकारों को वहां ले गए थे। इस समय उनकी फिल्मी कहानी राजनीति की ओर झुकने वाली थी। एक परिपक्व राजनीतिज्ञ (ओम पुरी) अपने एक निष्ठावान कार्यकर्ता (सनी देवल) का उपयोग कर अपना राजनीतिक दबदबा कायम करने का चालाकी से प्रयास करता है। उसके बल पर चुनाव जीतने का दांव लगाता है। लेकिन इस चुनाव में नेता का असली चेहरा ध्यान में आते ही वह क्रोधित होता है और अपने नेता के खिलाफ ही बगावत करता है।
मराठी फिल्मों और राजनीति का गहरा रिश्ता है। ‘सामना’, ‘सिंहासन’, ‘वजीर’, ‘सरकारनामा’, ‘घराबाहेर’, ‘गल्ली ते दिल्ली’, ‘पुढारी’, ‘तोतया आमदार’, ‘सहकार सम्राट’, ‘झेंडा’, ‘राज का रण’ जैसी कितनी तो फिल्मों में इसका दर्शन होता है। महाराष्ट्र में लम्बे समय तक सहकारिता आंदोलन और कांग्रेस संस्कृति का राजनीति पर दबदबा होने से फिल्मों में उसी परिस्थिति का दर्शन हुआ। ‘पुढारी’ जैसी फिल्मों में तालुका स्तर की राजनीति, दांवपेंच, रैलियां, आतंक, गुलालअबीर उड़ाना आदि का दर्शन हुआ। विशेष रूप से महाराष्ट्र में शहरी मराठी व्यक्ति को राजनीति पर चर्चा करना पसंद होता है। इसी तरह ग्रामीण इलाकों के लोग ‘गल्ली से दिल्ली’ तक की राजनीति पर चाव से गप लड़ाते हैं। अपने पसंदीदा दल और नेतृत्व का पक्ष लेकर वादविवाद करते हैं। इस तरह की सामाजिक परिस्थितियों के कारण ही मराठी में बड़े पैमाने पर राजनीतिक पार्श्वभूमि वाली फिल्में बनती होंगी और उन्हें भरपूर सफलता भी मिलती है। पिछले कुछ वर्षों में महाराष्ट्र में कांग्रेस का दबदबा कम हुआ है और भाजपाशिवसेना युति ने अपना स्थान और अस्तित्व पैदा किया। शिवसेना से टूट कर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना स्थापित हुई। इस पार्श्वभूमि में मराठी में कुल तीन फिल्में बनीं। वे हैं झेंडा, राज का रण व 2015 राज का रण। विषय के अनुसार घटनाएं इनमें आ ही गई हैं। कहीं दल के टूटने से हुई कार्यकर्ताओं की फजीहत और कहीं दल टूटने से मतविभाजन का दुष्परिणाम दिखाई दिया। फिल्म के कहानीकार, निर्माता, निर्देशक ने राजनीति के विवरण में न उतरते हुए अखबारी खबरों व विश्लेषणों पर अधिक भरोसा रखा दिखाई देता है। राजनीतिक खेल और उसका मतदान पर होने वाला भलापुरा परिणाम जितना लगता है उतना सरल नहीं होता। बाहर से राजनीति का जैसा और जितना दर्शन होता है या वह समझता है उसके मुकाबले प्रत्यक्ष में राजनीति बहुत गूढ़ होती है और उसका लक्ष्य बदलता रहता है। और यह सब मतदान पर प्रभाव डालने के लिए होता है। फिल्मवाले यदि इस गहराई में जाने में सफल हुए तो मराठी हो, हिंदी हो अथवा किसी भी भाषा की फिल्म हो उसकी विश्वसनीयता व स्तर बढ़ेगा।
 दक्षिण की ‘बॉडीगार्ड’ (तमिल) का ‘अंगरक्षक’ नाम से हिंदी में रिमेक हुआ है। उसमें चुनावी राजनीति का पृथक दर्शन होता है। उसमें राजनीति के कारण प्रचंड महत्वाकांक्षी बना नेता (कुलभूषण खरबंदा) चुनाव जीतने के लिए अपनी पुत्री (पूजा भट्ट) का अपहरण करने का स्वांग रचता है। तब उस पुत्री का अंगरक्षक (सनी देवल) उस पिता के इस इरादे का प्रयास विफल कर देता है। इससे उस नेता का असली चेहरा आने से वह चुनाव हारता है।
दक्षिण की ‘बॉडीगार्ड’ (तमिल) का ‘अंगरक्षक’ नाम से हिंदी में रिमेक हुआ है। उसमें चुनावी राजनीति का पृथक दर्शन होता है। उसमें राजनीति के कारण प्रचंड महत्वाकांक्षी बना नेता (कुलभूषण खरबंदा) चुनाव जीतने के लिए अपनी पुत्री (पूजा भट्ट) का अपहरण करने का स्वांग रचता है। तब उस पुत्री का अंगरक्षक (सनी देवल) उस पिता के इस इरादे का प्रयास विफल कर देता है। इससे उस नेता का असली चेहरा आने से वह चुनाव हारता है।
‘आज का एमएलए’, ‘रामअवतार’, ‘यह देश’, ‘इन्कलाब’, ‘हम’ जैसी कितनी तो फिल्मों में राजनीति की भलीबुरी बातों का दर्शन होता है। आपात्काल के दौरान अर्थात 1975 से 1977 के बीच विचार स्वातंत्र्य पर पाबंदी का फिल्मों पर असर पड़ा। तब थिएटरों में प्रदर्शित होकर रसिकों और समीक्षकों की सराहना पाने वाली ‘आंधी’ व ‘सामना’ जैसी फिल्मों का प्रदर्शन रोका गया। उनक पर कुछ समय तक पाबंदी लगाकर उन्हें फिर से सेंसर से पास कराने के लिए मजबूर किया गया। यही नहीं, ‘किस्सा कुर्सी का’ की सेंसर प्रिंट ही जब्त की गई और नए सिरे से फिल्मीकरण करना पड़ा। किसी फिल्म में फिल्मी नेता का किरदार पसंद न आने से उनके समर्थक उस पर पाबंदी की मांग करते हैं। कई बार थिएटरों को भी हानि पहुंचाई जाती है। ‘झेंडा’ के समय ऐसा ही हुआ।
एक महत्वपूर्ण प्रश्न। पांच साल बाद किसी भी तरह के चुनाव (मिसाल के तौर पर मनपा, नपा, ग्राम पंचायत, जिला परिषद, विधान सभा और लोकसभा) मतदान का प्रतिशत 40 से 55 के बीच होता है। लेकिन इस अवधि में आने वाली बड़ी फिल्मों को पहले कुछ दिन सौ फीसदी समर्थन मिलता है। इसका अर्थ यह कि मतदान केंद्र पर जाने की अपेक्षा थिएटर की टिकट खिड़की पर जाने में रसिकों की विशेष उत्सुकता होती है, यह आंकड़ों से साबित होता है।
फिल्मों दिखने वाली चुनावी राजनीति की ‘परम्परागत स्थिति’ में बहुत बदलाव क्यों नहीं होता? उसके प्रति मात्र मनोरंजन की दृष्टि से ही क्यों देखा जाता है?