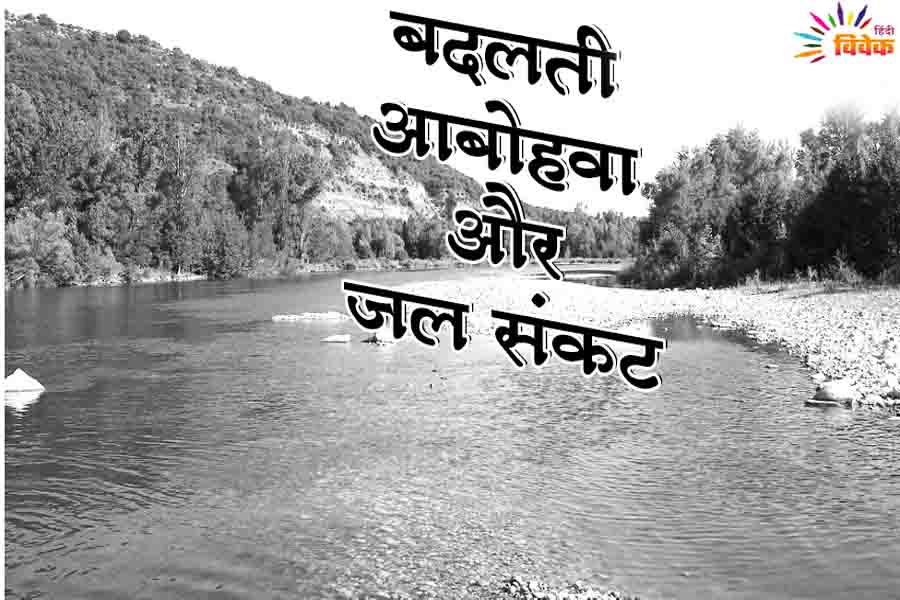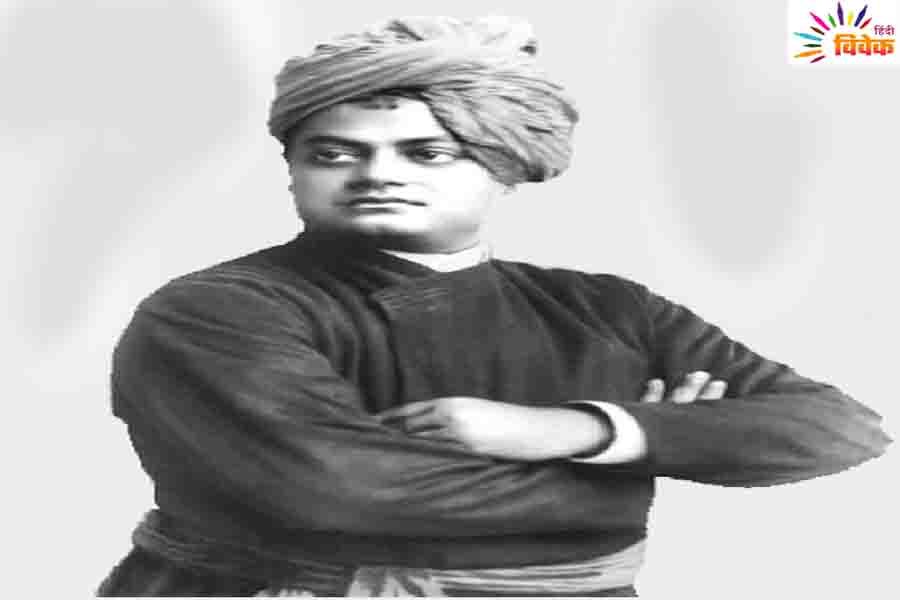अनुमान है कि इस सदी के मध्य तक अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर अधिक वर्षा होगी। यह अतिरिक्त पानी बह कर सागर में चला जाएगा। कुछ जगह बेहद बारिश होगी तो अन्य जगह बारिश का अभाव होगा। इससे 2050 तक पानी का संकट बढ़ने की संभावना है।
इसी माह 22 तारीख को विश्व जल दिन है। राष्ट्रसंघ 1992 से यह दिन मना रहा है। प्रति वर्ष एक केंद्रीय कल्पना लेकर विश्वभर में विविध कार्यक्रम किए जाते हैं। संबंधित वर्ष का नारा लेकर जनजागरण किया जाता है। इस वर्ष का नारा है ‘जल और अन्न सुरक्ष।’ पानी और अनाज का कितना संबंध है यह बताने की आवश्यकता नहीं है। इसी कारण इस वर्ष का जलदिन महत्वपूर्ण है। जनसंख्या का विस्फोट और सीमित प्राकृतिक संसाधन के बीच किस तरह सामंजस्य स्थापित करे यह एक बड़ा सवाल है। भविष्य में उसकी व्याप्ति और बढ़ने वाली है। केवल अनाज की पैदावार पर विचार करें तो विशेषज्ञ बताते हैं कि 2050 में विश्व में पर्याप्त अनाज, सब्जियों का उत्पादन करने के लिए 55 आस्वान बांध पानी लगेगा। आस्वान मिश्र का महाकाय बांध है। उसमें कितना पानी होता है? 111 घन किलोमीटर! अनुमान है कि इस तरह के प्रचंड जलसंग्रह वाले 55 बांधों का पानी 2050 में अनाज उत्पादन के लिए जरूरी होगा।
यह अनुमान हैरान करने वाला है। पिछले कुछ वर्षों में वायु प्रदूषण, पर्यावरण का असंतुलन, प्रकॄति के चक्र में हो रहा बदलाव, ऋतुओं में धीमी गति से होने वाला परिवर्तन कम होते जा रहे जंगल, भूगर्भ में पानी के स्तर में गिरावट, समुंदर के जल स्तर में होने वाली बढोतरी (समुंदर का जल स्तर बढ़ने से ओरिशा के तीन देहात समुंदर में समा चुके हैं। कोंकण में कई जगह समुद्री ऊफान अंदर तक आने लगा है। जल स्तर बढ़ने ये कुछ उदाहरण हैं।) इत्यादि अनेक बातों से विशेषज्ञों की चिंता बढ़ रही है। इस संबंध में पानी के बारे में विचार करें तो क्या दिखाई देता है?
औद्योगिक क्रांति के बाद के काल में अर्थात 1850 के बाद के डेढ़ सौ वर्षों में हमने भारी प्रगति की है। लेकिन वह करते समय आवश्यक बातों पर ध्यान नहीं दिया। कई बातें हम मान कर ही चले हैं। अर्थात उसके भी कारण थे। इतिहास पर गौर करें तो ध्यान में आएगा कि पिछले दस हजार वर्षों में हमारी धरती की आबोहवा में बहुत बदलाव नहीं हुआ है। आबोहवा लगभग स्थिर रही। उस समय में जीवन की कुल गति भी आज से अलग थी। जनसंख्या भी आज जितनी नहीं थी। सन 1800 में विश्व की जनसंख्या 100 करोड़ थी और उसके बाद के 200 सालों में वह 600 करोड़ से आगे बढ़ गई। 1960 के बाद जनसंख्या वृध्दि की गति तेज हो गई यह भी ध्यान रखना होगा। विज्ञान के सभी क्षेत्रों में अनुसंधानों को बल मिला और फलस्वरूप व्यक्ति की औसत आयु बढ़ने लगी। आयुर्विज्ञान की प्रगति के कारण लाइलाज बीमारियों का भी सफल यइलाज होने लगा। नई चिकित्सा पध्दतियां विकसित हुईं। जीवाणु और विषाणु का गहन अध्ययन होने लगा। उन्हें खत्म करने की नई दवाइयां विकसित करने में सफलता मिली। इस सब का परिणाम यह हुआ कि विश्व की जनसंख्या बढ़ने लगी। यूरोप में इसकी गति धीमी थी, लेकिन अफ्रीका और एशिया में वह बढ़ने लगी।
विश्व की इस बढ़ती जनसंख्या के कारण ही सारा गणित गड़बड़ा गया। इस संदर्भ में रामदास स्वीमी ने ‘दासबोध’ में (दशक सोलहवा, समास चौथा) पानी के बारे में विवेचना की है। वे कहते हैं, ‘पानी सभी का जन्मस्थान है। सभी जीवों का जीना उस पर निर्भर है।’ रामदास स्वामी के मराठी के पद इस प्रकार हैं
उदकतारकमाक । उदकनानासौख्यदायेक । पाहतां उदकाचा विवेक । अलोलीक ॥
ठाई ठाई डोहो तुंबती । विशाळ तळीं डबाबिती । चबाबिती थबाबिती । कालवे पाट ॥
येकी पालथ्या गंगा वाहती । उदके सन्निधचि असती । खळाळां झरे वाहती । भूमीचे पोटी ॥
भूगर्भी डोहो भरले । कोण्ही दखिले ना एैकिले । ठाई ठाई झोवीरे जाले । विदुल्यतांचे ॥
पृथ्वीतळीं पाणी भरले । पृथ्वीमधें पाणी खेळे । पृथ्वीवरी प्रकटलें । उदंड पाणी ॥
प्रा. के. वी. बेलसरे ने इसका अर्थ निम्न प्रकार से बताया है, ‘पानी जिस तरह तारक है, उसी तरह मारक भी है। पानी अनेक तरह से आदमी को सुख देता है। विचार करें तो ऐसा लगेगा कि पानी बड़ा अलौकिक है। जगह जगह भर जाता है। प्रचंड जलाशय भी पानी से लबालब हो जाते हैं। नहरें और नालें पानी से भरे होते हैं। कुछ जगह भूमिगत गंगा बहती हैं। उनका पानी भूमि के नीचे लेकिन करीब ही होता है। कुछ जगह भूमि के अंदर झरने बहते होते हैं। कभी किसी ने न देखे और सुने पानी के जलाशय धरती की पेट में होते हैं। कुछ जगह आसमानी बिजली गिरने से बड़ा गड्ढा हो जाता है और उसमें झरने फूट पड़ते हैं। इस तरह धरती के नीचे पानी भरा है। धरती के भीतर और बाहर भरपूर पानी बह रहा है।
समर्थ रामदास स्वामी के निरीक्षणों पर गौर करें तो दिखाई देगा कि उन दिनों पानी भरपूर मात्रा में था। यही क्यों, हाल के पिछले कुछ वर्षों में भी पानी की कमी महसूस नहीं होती थी और कभी यह समस्या आएगी ऐसा किसी ने सोचा भी नहीं था। लेकिन प्रगति के दौर में सब कुछ बदलइ गया और उसमें आबोहवा भी बदल गई। इससे पूरा ऋतुचक्र भी धीरेधीरे बदलने लगा। बारिश का भरोसा नहीं रहा। शुध्द पानी के भंडार खोजने पड़े। बर्फ के रूप में जमा पानी समुंदर में जाने लगा। रूस के अरल समुद्र का संकोच होने लगा। यह संकोच इतना था कि कभी समुद्र में डूबी नौकाएं भी दिखाई देने लगीं। अरल सागर की स्थिति अफ्रीका के छाड सरोवर जैसी होने लगी। यह सरोवर अब 90 प्रतिशत ही रह गया है। इस सरोवर पर दो करोड़ लोग निर्भर थे। इससे छाड के संकोच से उत्पन्न तीव्र संकट की कल्पना आ सकती है।
इन बातों से साफ है कि पानी की कमी अभी जो महसूस की जा रही है उसमें इस सदी में और 20 फीसदी की बढोतरी होगी। अनुमान है कि इस सदी के मध्य तक अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर अधिक वर्षा होगी। यह अतिरिक्त पानी बह कर सागर में चला जाएगा। कुछ जगह बेहद बारिश होगी तो अन्य जगह बारिश का अभाव होगा। इससे 2050 तक पानी का संकट बढ़ने की संभावना है। सब से बड़ी चिंता की बात यह है कि ग्लेशियरों और हिमखंडों में जमा पानी का संग्रह पिछले दस वर्षों से कम हो रहा है और आने वाले दस वर्षों में वह और कम होता जाएगा। इससे गंगा व ब्रह्मपुत्र जैसी नदियों के पानी पर असर होने वाला है। भारत, चीन, पाकिस्तान व अमेरिका के पश्चिम भाग पर इसका प्रभाव पड़ेगा। संख्या में बताना हो तो दुनिया की एक बटा छह जनसंख्या इससे प्रभावित होगी।
एक ओर पानी का संग्रह कम होगा तो दूसरी ओर कुछ इलाकों में सूखा पड़ जाएगा। वायु मंडल में आने वाले इन परिवर्तनों के कारण जीवजंतुओं की वृध्दि होगी और उपलब्ध जल की क्वालिटी खतरे में पड़ सकती है। इसमें बाढ़ के कारण अनेक प्रदूषक घटक पानी में घुल जाएंगे और जहां जहां ऐसा होगा वहां वहां पानी प्रदूषित हो जाएगा। (एक अनुमान के अनूसार सन 2030 में दुनियाभर में डायरिया की मात्रा 10 प्रतिशत की वृध्दि होगी।) सागर के जलस्तर में वृध्दि के कारण खारा पानी अधिकाधिक भूभाग पर फैलगा। जिस जमीन पर यह पानी फैलेगा वह फसलों के लिए निरुपयोगी हो जाएगी। बार बार आने वाले सूखे के कारण खेती के लिए पानी कहां से लाए यह समस्या रहेगी। बढ़ती जनसंख्या के कारण अधिक अनाज की जरूरत होगी और उसे पैदा करने के लिए जमीन का क्षेत्र विस्तारित होता जाएगा। यह अतिरिक्त जमीन कहां से उपलब्ध होगी यह भी एक समस्या ही होगी। कुल जमीन कितनी है यह सभी जानते हैं। यही नहीं, जो है भी उस सारी जमीन पर फसल लेना संभव नहीं है। सहारा जैसे रेगिस्तान दुनिया में हैं। आस्ट्रेलिया का बहुत बड़ा हिस्सा खेती के लिए उपयुक्त नहीं है। हमारे राजस्थान में भी थर जैसा रेगिस्तान है। इस संबंध में सर्वे बताते हैं कि रेगिस्तानी इलाका बढ़ रहा है। दूसरे शब्दों में कहे तो बिनउपजाऊ जमीन का क्षेत्र बढ़ रहा है। पानी के बारे में जब हम सोचते हैं तब इस वास्तविकता को भी ध्यान में रखना होगा।
खेती के लिए जिस तरह अधिक पानी लगने वाला है, उसी तरह वह कारखानों को भी लगने वाला है। पानी की जरूरत प्रक्रिया को शीत रखने के लिए होती है। कुल औसत तापमान जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे कारखानों के संयंत्र को शीत रखने के लिए अधिकाधिक पानी की जरूरत होगी। बड़े पैमाने पर स्थापित कारखानों व नए आने वाले कारखानों को बिजली की जरूरत होगी और उसे पैदा करने का मार्ग पानी ही है। पानी की बढ़ती मांग को पूरा करने का एक उपाय उपयोग में लाए गए जल का शोधन करना है। इसके लिए भी बिजली की जरूरत पड़ेगी ही। पानी को बार बार शोधित करना खर्चीला विकल्प है। लम्बे समय तक इसे चलाना मुश्किल है।
आर. के. मल्ल, अखिलेश गुप्ता जैसे लोगों ने पानी समस्या का गहन अध्ययन किया है। विशेषज्ञों की राय है कि इस सदी में सागर के औसत जलस्तर में एक मीटर से वृध्दि होगी। ओरिशा व प. बंगाल इन दो राज्यों के तटवर्ती क्षेत्रों की लगभग 1760 किलोमीटर जमीन पर पानी छा जाएगा। इसका असर 5763 किलोमीटर के तटवर्ती क्षेत्र पर होगा। 71 लाख लोग इससे प्रभावित होंगे। वहां वाष्पीकरण का वेग बढ़ेगा। मध्य भारत में वहां के सूखे इलाके की आबोहवा पर अधिक प्रभाव पड़ेगा। कोसी नदी में पानी कम होगा। देश की अन्य नदियों पर इसी तरह का असर होने से इनकार नहीं किया जा सकता। देश के वायु मंडल पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। हवा में कार्बन डायआक्साइड की मात्रा बढ़ेगी। तापमान कोई 2.33 से 4.78 सेल्शियस से बढ़ेगा। फलस्वरूप धुआंधार बारिश होगी। वार्षिक औसत बारिश में सात से दस प्रतिशत की वृध्दि होगी। फिर भी पानी की कमी महसूस की जाती रहेगी, क्योंकि पानी की मांग लगातार बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, खेती व उद्योगों के लिए अधिक पानी लगेगा। भूजल का स्तर कम होता जाएगा, क्योकि बारिश का पानी जमीन में झरने के बजाए बह जाएगा। बारिश की अवधि कम होने (15 दिन से) का अनुुभव आएगा। देश के पश्चिम और मध्य भाग में इसका ज्यादा प्रभाव दिखाई देगा। इसी समय उत्तरांचल व उत्तरपूर्वी इलाकों में बारिश की अवधि (5 से 10 दिन से) बढ़ेगी।
इससे आतंकित करना इस लेख का उद्देश्य नहीं है। हमेंं समय पर सतर्क होना पड़ेगा। इस संदर्भ में फिनलैण्ड जैसा छोटा देश काम कर रहा है। उससे हमें सबक लेना होगा।