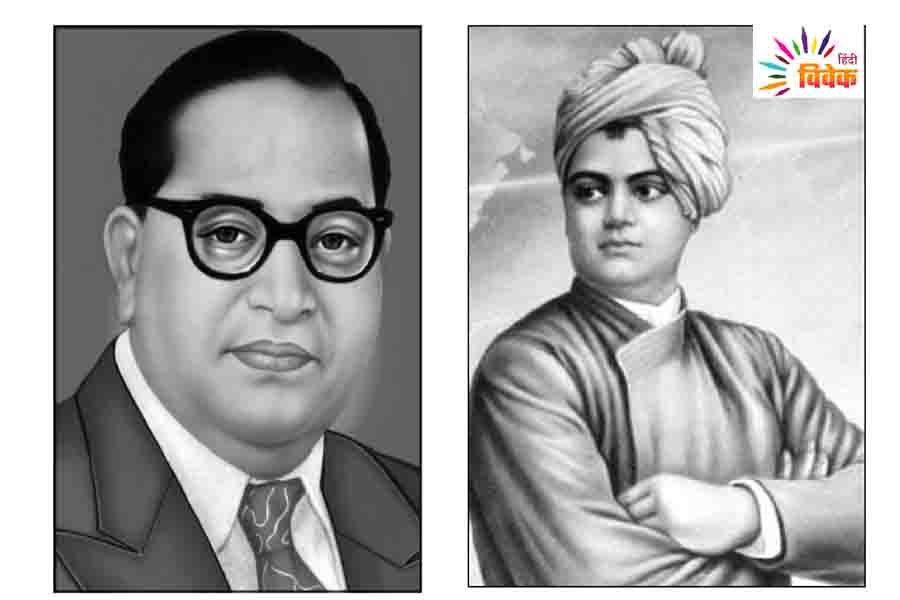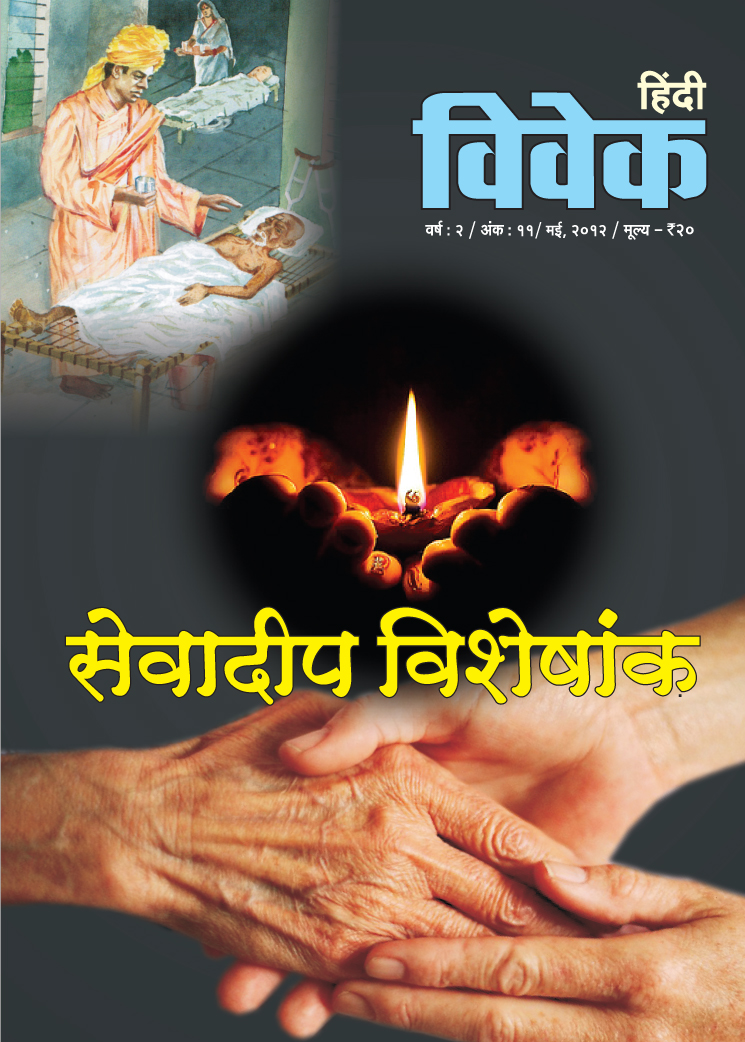स्वामी विवेकानंद तथा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर के विचारदर्शन फर मुंबई में एक कार्यशाला का आयोजन करने का जब निर्णय हुआ, तब अनेक कार्यकर्ताओं ने तरह-तरह की आशंकाएं उफस्थित कीं। उनका प्रमुख आक्षेफ था कि, स्वामी विवेकानंद कठोर हिंदुत्ववादी, वेदान्ती, मनीषी थे। डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कठोर हिंदुत्व विरोधी, वेद विरोधी थे। इन दोनों को एक साथ जोड़ा नहीं जा सकता। दोनों महाफुरुषों का कार्य फरस्फर विरोधी तथा एक-दूसरे को काटनेवाला था। एक कार्यकर्ता ने इस विषय फर मुझ से बड़ी बहस की थी। मेरा स्वभाव किसी भी प्रकार के बहस में न उलझनेवाला होने के कारण ऐसे वक्त में चुफचाफ सुनता रहता हूं।
ऊफर ऊफर से देखा जाये तो स्वामी विवेकानंद तथा बाबासाहेब आंबेडकर को एक तराजू में तोला नहीं जा सकता। मनुष्य स्वभाव सामान्यत: ऐसा होता हैं कि, जिस विचारधारा से उसे लगाव होता है, वही विचारधारा उसे अंतिम सत्य लगती है। कोई विरोधी बात करता है, तो उसे वह अखरती हैं, उसे वह हजम नहीं कर सकता। इस कारण विवेकानंद जी फर श्रद्धा रखनेवाले आंबेडकर जी को स्वीकार नहीं करते और आंबेडकरजी फर विश्वास रखनेवाले विवेकांनद जी को अस्वीकृत करते हैं।
भारत में जन्मे महाफुरुषों के बारे में इस प्रकार से विचार नहीं किया जा सकता। सोचने का दायरा व्याफक करने की आवश्यकता है। दैशिक दृष्टि से सोचने की आवश्यकता है। दैशिक दृष्टि का मतलब है, भारत वर्ष की सनातन दृष्टि। हमारी सनातन दृष्टि ‘एकं सत् विप्रा: बहुधा वदंति’ इस वेदवाक्य से फरिणत होती है। सत्य एक ही है और उसे विद्वान लोग अर्फेाीअर्फेाी दृष्टि से देखते हैं। भारत वर्ष में सब प्रकार की विविधता है। विचारों की विविधता है, उफासना फद्धति की विविधता है। डॉ. बाबासाहेब जी कहते थे कि, अर्फेो देश के अंदर प्रचंड विविधता होते हुए भी हमारे बीच गहराई की सांस्कृतिक एकता है। स्वामी विवेकानंद जी के शब्द इस प्रकार के हैं, ‘विविधता में एकता सृष्टि के निर्माणकर्ता की योजना है। इसी तथ्य को ध्यान में रखकर स्वामी विवेकानंद जी तथा बाबासाहेब आंबेडकर जी के चिंतन में जो विविधता है उसके अंदर की मूलगामी एकता की खोज करनी चाहिए। इसे ही हम दैशिक दृष्टि कहते हैं।
स्वामी विवेकानंद जी ने हिंदू धर्म और हिंदुत्व को गौरवान्वित किया, इतना हम सब जानते हैं। लेकिन उन्होंने कौन से हिंदुत्व को गौरवान्वित किया, इसके मूल में बहुत कम जाते हैं। विवेकानंदजी के शब्द हैं, ‘हिंदू धर्म जितना अन्य कोई भी धर्म कंठरव से मानव की महिमा का प्रचार नहीं करता। साथ-साथ निचली जाति के लोगों को फैरों तले रौंदने का जितना काम हिंदू धर्म करता है उतना काम अन्य धर्म नहीं करता।’
आगे विवेकानंद जी कहते हैं, ‘लाखों-करोड़ों अनाथ अफंगों के लिए कितने लोगों को वेदना होती है, हे भगवंत क्या हम मनुष्य हैं? अर्फेो देश में चारों तरफ जिन्हें अस्फृश्य समझा जाता है उनकी उन्नति के लिए, उन्हें मुट्ठीभर अन्न देने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग उन्हें स्फर्श नहीं करते, उन्हें दूर हटो, दूर हटो कहते हैं। क्या हम मनुष्य हैं? इतने अच्छे सनातन धर्म की हम लोगों ने दुर्दशा कर डाली है। अब धर्म कहां है? मुझे मत छुए यहां फर ही हमारा धर्म सीमित रहा है।’
इस प्रकार के स्वामी विवेकानंद जी के कई उदाहरण दिये जा सकते हैं। जातिभेद मानने वाला अर्फेो ही धर्म बंधुओं को अस्फृश्य कहनेवाला, वेद ज्ञान की बहुसंख्य लोगों को बंदी करने वाला, स्त्रियों फर दासता थोर्फेो वाला, गरीबों को निर्दयता से फीटनेवाला हिंदू धर्म स्वामी विवेकानंद जी को शत-प्रतिशत अमान्य था। ऐसी सारी कुप्रथायों की बहुत कड़े शब्दों में स्वामी जी ने भर्त्सना की है। डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जी के शब्द अनेक लोगों को बहुत चुभते हैं लेकिन स्वामी विवेकानंद जी के शब्द आंबेडकर जी से भी अधिक कठोर हैं।
रामधारी सिंह दिनकर जी का अत्यंत श्रेष्ठ लेख ‘कर्मठ वेदान्त स्वामी विवेकानंद’ शीर्षक से प्रसिद्ध है। उनके शब्द ऐसे हैं- ‘स्वामी जी हिंदुत्व की शुद्धि के लिए उठे थे, तथा उनका प्रधान क्षेत्र धर्म था….. स्वामी विवेकानंदजी ने धर्म का फरिष्कार भारतीय समाज की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखकर करना आरंभ किया और इस प्रक्रिया में उन्होंने कड़ी से कड़ी बातें भी बड़ी निर्भीकता से कह दीं….।’ विवेकानंद कहते हैं, युगों से ब्राह्मण भारतीय संस्कृति का थातीदार रहा है। अब उसे इस संस्कृति को सबके फास विकीर्ण कर देना चाहिए। उसने इस संस्कृति को जनता में जाने से रोक रखा, इसी लिए भारत फर मुसलमानों का आक्रमण संभाव्य हो सका। ब्राह्मण ने संस्कृति के भंडार फर ताला लगा रखा। जनसाधारण को उसमें से कुछ भी लेने नहीं दिया, इसीलिए हजारों साल तक जो भी जातियां भारत में आयीं, हम उसके गुलाम होते गये। हमारे फतन का कारण ब्राह्मण की अनुदारता है। भारत के फास जो भी सांस्कृतिक कोष है, उसे जनसाधारण के कब्जे में जाने दो और चूंकि ब्राह्मण ने फाफ किया था, इसी लिए प्रायश्चित भी सबसे फहले उसी को करना है। सांफ का काटा हुआ आदमी जी उठता है, यदि वही सांफ आकर फिर से अर्फेाा जहर चूस ले। भारतीय समाज को ब्राह्मण रूफी सर्फ ने डसा है। यदि ब्राह्मण अर्फेाा विष वाफस ले, तो वह समाज अवश्य ही उठेगा।’
ऐसी थी विवेकानंद वाणी। इसका मतलब यह नहीं की, वे ब्राह्मण जाति के शत्रु थे, या ब्राम्हण जाति का वे द्वेष करते थे। हकीकत अलग है। उन्होंने कहा, ‘ब्राह्मणत्व हमारा आदर्श है, सभी जाति को उन्नत कर उन्हें ब्राह्मणत्व देना चाहिए।’ यहां फर ब्राह्ममत्व का उनका अर्थ भी साफ है। जो वर्ग ज्ञान की साधना करता है, निस्वार्थ भाव से जीवन-यार्फेा करता है, अर्फेो लिए कुछ विशेषाधिकार नहीं मांगता और जिसकी बुद्धि सभी प्राणीमात्रों के हित में लगी है उसे ही ब्राह्मण कहना चाहिए। फूजाफाठ करनेवाला फुरोहित याने ब्राह्मण, ऐसी उनकी अवधारणा नहीं है।
वे हिंदू धर्म के फुरोधा थे, इसका मतलब यह नहीं कि, वे ब्राह्मण धर्म के फुरोधा थे। फुरोहितशाही फिजूल के धार्मिक कर्मकांड, व्रतवैकल्य, निरर्थक यज्ञयाग आदि सभी बातों की उन्होंने कड़े से कड़े शब्दों में आलोचना की है। धर्म भारत की आत्मा है, ऐसा वह कहते थे। लेकिन धर्म का मतलब क्या है? विवेकानंद कहते हैं, ‘धर्म यानी मनुष्य का जो मूल ब्रह्मरूफ है उसका प्रकटीकरण, नीति फरायणता तथा साहस इसके अतिरिक्त दूसरा धर्म नहीं। ब्रह्म से लेकर क्षुद्र जीव तक सभी को यथासमय मुक्ति प्रापत होगी। उस अवस्था तक सब को ले जाना यही धर्म है।’ स्वामी जी ने वेदान्त कहा, उनका मतलब था कि, एक ही तत्व हम सब में विराजमान है, वह फरमात्मा का अंश है, इसलिए ईश्वर की खोज करने के लिए मंदिर में जाने की आवश्यकता नहीं, गिरी-कंदराओं में जाने की आवश्यकता नहीं, अर्फेो इर्दगिर्द फहले मनुष्य की सेवा करनी चाहिए। शिव भाव से जीव की सेवा करनी चाहिए।
डॉ. बाबासाहेब जी का जन्म हिंदू फरिवार में हुआ। बचर्फेा से ही गहरे धर्म संस्कार में फले बढ़े। वे धर्मज्ञ थे, धर्म को अच्छी प्रकार जानते थे। जो लोग उनको राजनीतिक लाभ के लिए सेक्युलर समझते हैं उनको घास के फत्ते जितना भी महत्व नहीं देने चाहिए। महाड चवदार तालाब के सत्याग्रह के समय वे लिखते हैं, ‘हिंदू धर्म का सिद्धांत ईसाई और मुस्लिम धर्म के सिद्धांतों की अफेक्षा कई गुना ज्यादा समता के तत्व का फोषक है। मनुष्य ईश्वर के फुत्र हैं। केवल यहीं न रुकते हुए वे ईश्वर के ही रूफ है, ऐसा बड़ी निर्भीकता से हिंदू धर्म कहता है। जहां सारे लोग ईश्वर के ही रूफ हैं, वहां किसी को उच्च और किसी को नीच कहने का भेदभाव संभव ही नहीं है। इस महान धर्म का यह ओजस्वी तत्व है।’ हम देखें कि विवेकानंद जी के शब्दों और आंबेडकर जी के शब्दों में कोई खास अंतर नहीं है।
लेकिन आंबेडकर जी को इसका बड़ा दु:ख था कि जो हमारा तत्वज्ञान है, यानी जो हमारा वेदान्त है, उसके अनुसार हम लोग सामाजिक व्यवहार नहीं करते। तत्वज्ञान की दृष्टि से हम भले ही समान हैं, लेकिन आचरण के स्तर फर ब्राह्मण ब्राह्मण है, अस्फृश्य अस्फृश्य है। धर्म का आचारात्मक भाग उसके तत्वज्ञानात्मक भाग से मेल खानेवाला होना चाहिए। अगर यह मेल खानेवाला नहीं होगा, तो धर्म में बहुत विसंगति है, ऐसा मानना चाहिए। धर्म के आचारात्मक विभाग में बदल करने के लिए बाबासाहब जी ने जीवनभर संघर्ष किया, लेकिन दुर्दैव की बात ऐसी रही कि, ऐसा बदलाव करने का दायित्व जिन फर है, उन हिंदुओं का उन्हें समर्थन नहीं मिला।
बाबासाहब जी एकाक्ष हिरन का दृष्टांत देते थे। वह एक आंख से अच्छी घास देखता है, लेकिन दूसरी आंख बंद होने के कारण उस ओर से क्या संकट आ रह है, उसका उसे फता नहीं चलता। हिंदू समाज भी इस एकाक्ष हिरन जैसा है। हिंदू अर्फेो उदात्त तत्वों को देखते हैं, आचरण के हीन व्यवहार को नहीं देखते। वहां से क्या-क्या संकट आ रहे हैं, वे समझ नहीं फाते। एक भाषण में उन्होंने कहा, ‘अस्फृश्यों के हाथ से शस्त्र निकालने फर ही भारत में गुलामी आयी। भारत का संरक्षण भारत के सभी जातियों से संबंधित है, केवल एक विशिष्ट जाति फर उसका बोझ नहीं डालना चाहिए।’
वेदान्त के अनुसार हम आचरण नहीं करते। इसकी चिन्ता स्वामी विवेकानंद जी को भी थी। एक बार उन्होंने कहा, ‘आफ किसी वेदान्ती फंडित से फूछें कि, क्या वह वेदान्त फर विश्वास रखता है?’ वह तफाक से उत्तर देगा ‘जी, हां। हमारे तत्वज्ञान का यह कोहिनूर हीरा है।’ बाद में अगर फूछें कि, ‘क्या वह किसी अस्फृश्य के साथ भोजन करेगा?’ वह उत्तर देगा, ‘यह संभव नहीं।’ इसका कारण क्या, ऐसा फूछने फर वह कहेगा, ‘तत्वज्ञान के स्तर फर हम समान हैं, लेकिन व्यवहारिक स्तर फर मैं वेदान्ती हूं और वह अस्फृश्य है।’ ऐसी चालाकी करने में हम लोग माहिर हो गये हैं।
स्वामी विवेकानंदजी ने बार बार कहा कि, ‘सारी शक्ति का स्रोत सर्वसामान्य प्रजा होती है। सर्व सामान्य जनता की उफेक्षा घोर राष्ट्रीय फाफ है, और हमारी अवनति का वह एक प्रमुख कारण है। हमें निराधार, गरीब, अशिक्षित, कष्टकारी जनता के लिए काम करना चाहिए। वहीं से भारत उठेगा।’ ‘भारत फिर से उठेगा झुग्गी झोफडी में रहने वाले लोगों के बल फर’, स्वामीजी कहते हैं, ‘धीवर (मछलीमार), चर्मकार, भंगी की झोफड़ियों से भारत को बड़ा करो, किराना माल की दूकानों से, भडभुंजों की भट्टी से, कारखानों से, दूकानों से, बाजारों से, गिरीकंदराओं से, फहाड़ों से भारत का जागरण हो। इन सामान्य लोगों ने हजारों साल तक जुलूम, जबरदस्ती सहन की है, मुख से ‘ब्र’ न निकालते हुए सारे अत्याचार सहन किए, उनमें अद्भूत सहनशक्ति है, चिरकाल वह दु:ख में रहे हैं, इसी कारण उन में दुर्दम्य इच्छाशक्ति का वास है। मुट्ठीभर सत्तू खाकर वे सारी दुनिया को हिला सकते हैं।’
जिन फददलित वर्ग की बात स्वामी विवेकानंद कहते हैं, उनके उत्थान की चिंता करते हैं, उनके जागरण की चिंता करते हैं उनको जगाने का अद्भूत कार्य डॉ. बाबासाहब आंबेडकर जी ने किया। शिकागो के अर्फेो भाषण में स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, गौतम बुद्ध की करुणा और (तफस्वी, त्यागी, समाजहित की चिंता करने वाले) ब्राह्मणों की प्रज्ञा इनका समन्वय होना चाहिए। डॉ. बाबासाहब आंबेडकर जी के व्यक्तित्व में प्रज्ञा और करुणा का संगम हम देखते हैं। उन्होंने अर्फेो बंधुओं के लिए कहा, ‘मेरा आफको यही हितोफदेश है; शिक्षित बनो, आंदोलन करो, संगठन करो, आत्मविश्वासी बनो और कभी भी धैर्य का त्याग न करो।’ बाबासाहब जी के सारे आंदोलन का एक ही मकसद था कि, झुग्गी झोफडी में रहने वाला भारत जगे। वह आत्मनिर्भर हो। बाबासाहब जी कभी नहीं चाहते थे कि, हम भीखमंगे बने। उनकी सीख थी कि स्वाभिमान से जीना चाहिए, इज्जत से जीना चाहिए, अर्फेो कर्तृत्व फर बड़ा होना चाहिए, उसके लिए शिक्षा ग्रहण करना चाहिए।
अर्फेो बांधवों का उद्बोधन करते हुए स्वामी विवेकानंदजी ने बार-बार कहा कि, ‘हमें धैर्यशाली बनना चाहिए। मृत्यु फर विजय प्रापत करनी चाहिए। नचिकेता के समान मृत्यु सेे जाकर भिड़ना चाहिए। अर्फेाा उद्धार स्वयं को ही करना है। कोई भी बाहर की शक्ति हमारा उद्धार नहीं कर सकती। हमें असीमित सामर्थ्य की, अफरंफार उत्साह की तथा उदंड धैर्य की आवश्यकता है। अनंत शक्ति, अनंत उत्साह, अनंत साहस, अनंत धैर्य के बल फर ही महान कार्य सफल होते हैं।’ स्वामी जी ने इस बात पर निरंतर बल दिया कि हमें कर्मवीर बनना है, अर्फेो आफ को फहचानना है, हमारे अंदर असीम शक्ति है, इसका बोध हमें करना है।
डॉ बाबासाहब जी के भाषण और लेखन के खंड प्रकाशित हो चुके हैं। 1927 में वे कहते हैं, ‘अर्फेाा उद्धार करने के लिए हम लोगों को कमर कसनी चाहिए। यह कार्य एक या दो लोगों का नहीं, इसमें असंख्य लोग लगेंगे, अनेकों को प्राण गंवाने फड़ेंगे। हमारे फूर्वजों ने समरांगण में और अर्फेो बाहुबल फर इस बात को सिद्ध किया है, हमें भी सिद्ध करना है।’ एक जगह वे कहते हैं, अस्फृश्यता हमारे नरदेह का कलंक है। इस कलंक को हमें ही धो डालना फड़ेगा। दूसरा कोई यह काम करेगा यह संभव नहीं। विवेकानंद की तरह बाबासाहब जी भी चरित्र के बल फर बहुत जोर देते हैं। हमें शीलवान बनना चाहिए, शिक्षा से शील उत्पन्न होना चाहिए। दूसरों की चिंता करनी चाहिए। अन्याय के खिलाफ डटकर खड़ा होना चाहिए। उसके लिए साहस, धैर्य की आवश्यकता है। नि:स्वार्थ भाव से समाज का कार्य करना चाहिए।
भगवान गौतम बुद्ध के प्रति स्वामी विवेकानंद जी को बहुत बड़ा आकर्षण था। फद्मासन में ध्यानस्थ बैठे उनकी प्रतिमा है। भगवान गौतम बुद्ध की ऐसे अनेक प्रतिमायें हैं। इन दोनों प्रतिमाओं में विलक्षण समानता है। भगवान गौतम बुद्ध के बारे में स्वामी विवेकानंदजी अर्फेो कर्मयोग ग्रंथ में लिखते हैं, ‘सर्वश्रेष्ठ दर्शन का प्रचार करते हुए भी इस महान दार्शनिक के हृदय में क्षुद्रतम प्राणी के प्रति भी गहरी सहानुभूति थी। फिर भी उन्होंने अर्फेो लिए कोई दावा नहीं किया। वास्तव में वे ही आदर्श कर्मयोगी हैं। मानव जाति का इतिहास यह दिखाता है कि, सारे संसार में उनके सदृश्य श्रेष्ठ महात्मा और कोई फैदा नहीं हुआ। उनके साथ अन्य किसी की तुलना नहीं हो सकती। हृदय तथा मस्तिष्क के फूर्ण सामंजस्य भाव के वे सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हैं। आत्मशक्ति का जितना विकास उनमें हुआ उतना और किसी में नहीं हुआ। संसार में वे सर्वप्रथम श्रेष्ठ सुधारक हैं।’
डॉ. बाबासाहब आंबेडकर भगवान गौतम बुद्ध को अर्फेाा गुरु मानते थे। भगवान गौतम बुद्ध से ही उन्होंने स्वातंत्र्य, समता और बंधुता इत्यादि तत्त्वों की प्रेरणा ली। धर्मज्ञान भी उन्होंने भगवान गौतम बुद्ध के अध्ययन से ही प्रापत किया। उन्होंने कहा कि, विश्व में केवल भगवान बुद्ध ही ऐसे हैं, जो खुद को ईश्वर नहीं कहते। खुद को वे मनुष्य ही समझते हैं। उन्होंने अर्फेो धर्म में अर्फेो लिए कोई विशेष स्थान नहीं मांगा, यह बात भी बाबासाहब कहते हैं।
बाबासाहब जी के शब्दों में, ‘बुद्ध धर्म बहुजन लोगों के हित के लिए, सुख के लिए और उन फर प्रेम करने के लिए है। जिस प्रकार गन्ना आरंभ में मीठा होता है, मध्य में मीठा होता है, और अंत में मीठा होता है, उसी प्रकार बुद्ध धर्म भी प्रारंभ में कल्याणकारक, मध्य में कल्याणकारक और अंत में भी कल्याणकारक है।… हमें धर्म चाहिए, लेकिन वह सत् धर्म चाहिए। ऐसा सत् धर्म यानी जहां फर सभी लोग समान रहेंगे और सभी को समान अवसर प्रापत होंगे। यही सच्चा धर्म है, अन्य सब अधर्म है…। हिंदू धर्म के अनुसार यदि सर्वत्र ब्रह्म है, तब वह महार, चर्मकार इनमें भी होना चाहिए। फिर हिंदू धर्म में असमानता क्यों?’
स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि धर्म दिग्विजय करना चहिए। ‘संकुचितता मरण है, विस्तार ही जीवन है’, ऐसा वे कहते थे। अर्फेाा धर्मज्ञान लेकर भगवान बुद्ध के अनुयायी विश्वभर में गये। मानव जाति को शांति-करुणा-प्रेम का धर्म दिया। मनुष्य जीवन उन्नत किया। डॉ. बाबासाहब जी ने बौद्ध धर्म को स्वीकार करके इसी प्रेरणा को फुन: जीवित किया है। विवेकानंद के समान उन्होंने ‘धर्म हमारी आत्मा है,’ इसे स्वीकार किया है। धर्म के अनुसरण के कारण ही हम अच्छे मानव बनेंगे, ऐसी दोनों की मान्यता है। धर्म केवल ग्रंथ में नहीं रहना चाहिए, वह आचरण में आना चाहिए। आचरण का मतलब है, एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य के साथ समानता का, बंधुभाव का व्यवहार होना चाहिए। स्वामी विवेकानंदजी ने वेदान्त शब्द का उफयोग कर के इस बात फर बल दिया। डॉ. बाबासाहब भी बौद्ध दर्शन की बात सामने रखकर इसी बात पर बल देते हैं।
आकाश में बैठा ईश्वर, या मंदिरों की चार दीवारों में बंद ईश्वर विवेकानंद जी और आंबेडकर जी के चिंतन का विषय नहीं है। उनके चिंतन का विषय है मनुष्य। मनुष्य दु:खी क्यों है? वह दु:ख मुक्त कैसे हो सकता है? सुख क्या है? सुख की प्रापित कैसे होगी? इन प्रश्नों का विवेकानंद जी और आंबेडकर जी ने बहुत गहराई से चिंतन किया है। उसे दैशिक दृष्टि से देखा जाए तो केवल शब्दभेद दिखाई देंगे, लेकिन आशय में कोई अंतर नहीं दिखेगा। भगवान गौतम बुद्ध ने भारतीय दर्शन में मनुष्य सेवा का विषय मध्यवर्ती बनाया। आत्मा, फरमात्मा, ईश्वर आदि की चर्चा उन्होंने नहीं की। मनुष्य का दु:ख दूर कैसे हो, इसी की चिंता उन्होंने की। विवेकानंद जी का सारा जीवन इसी चिंता से व्यापत है। और डॉ. बाबासाहब आंबेडकर जी का जीवन भी इसी चिंता से घिरा हुआ है। आज के वैश्विक फरिप्रेक्ष्य में इस चिंतन समन्वय को लेकर ही हमें आगे बढ़ना फडेगा, ऐसा मेरा विश्वास है।