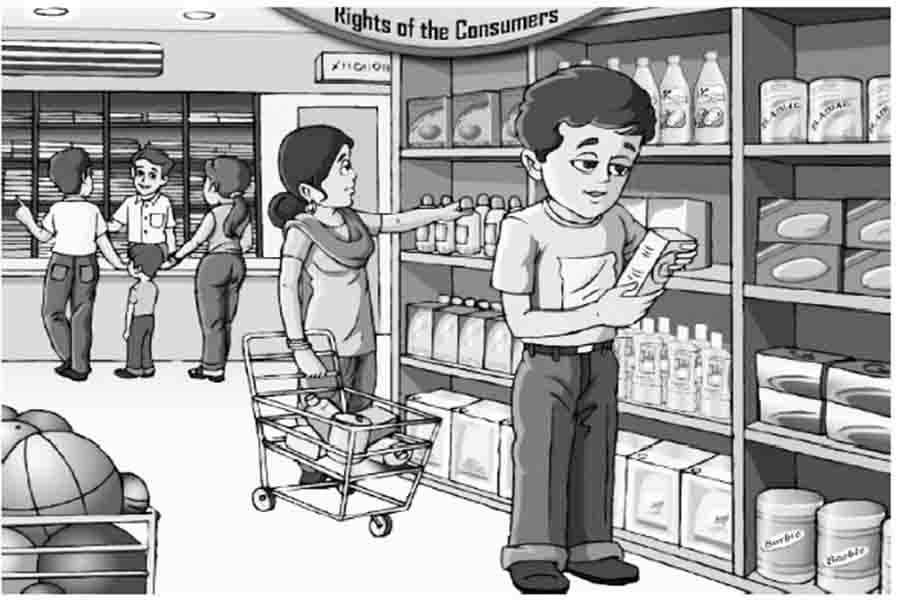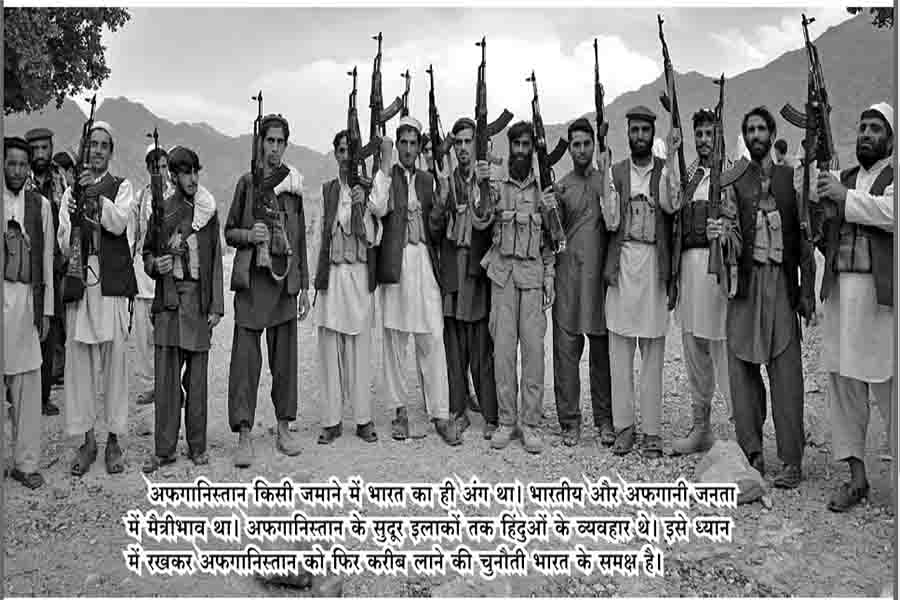भारत में हर साल 24 दिसम्बर राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत के राष्ट्रपति ने इस दिन ऐतिहासिक उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को स्वीकारा था। भारत सरकार ने 24 दिसम्बर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस घोषित किया है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक वर्ष 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। 1963 में इसी तारीख को अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जान एफ केनेडी ने ग्राहक मुहिम कार्यकर्ताओं के दबाव में अमेरिकी कांग्रेस के समक्ष उपभोक्ताओं के लिये ‘बिल ऑफ राइट्स’ की घोषणा की थी। इसके बाद 15 मार्च विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में मनाने की परंपरा चल पडी। भारत में यह दिवस पहली बार वर्ष 2000 में मनाया गया। इसके बाद प्रति वर्ष मनाया जाने लगा।
वैसे भारत में पारंपरिक तौर से वेदों में भी ग्राहकों के हितों का जिक्र मिलता है। व्यापारियों से व्यापार में ईमानदारी और सत्यनिष्ठा की अपेक्षा की जाती थी। चाणक्य के अर्थशास्त्र में उपभोक्ताओं के संरक्षण संबंधी प्रावधान हैं। सामानों की बिक्री को इस तरह संगठित किया गया था जिससे कि आम जनता को कोई दिक्कत न हो। यदि किसी व्यापारिक व्यवहार के उच्च मुनाफे से आम जनता को कोई दिक्कत होती थी तो उस व्यापार गतिविधि को तत्काल बंद कर दिया जाता था। व्यापारियों के लिये मुनाफे की सीमा निर्धारित थी। वजन और माप के निरीक्षण के लिये वाणिज्य निरीक्षक होता था। वजन और माप में गड़बड़ी करनेवाले विक्रेता को भारी जुर्माना किया जाता था। मिलावट करनेवाले विक्रेता को न केवल जुर्माना देना पड़ता था बल्कि उसे क्षतिपूर्ति भी करनी पडती थी। मनुस्मृति में लिखा है- क्रय-विक्रयानुशयी विवाद: सवामि पालयो:। अर्थात क्रय-विक्रय के किसी विवाद, उत्कृष्ट या निकृष्ट उत्पाद को लेकर किसी भी झगड़े का निपटारा मनुकाल में राजा द्वारा न्यायालय में होता था। लोभ आदि से मिथ्या गवाही देनेवाले और ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी करनेवाले को न्यायालय दंडित करता था। हालांकि आरंभ में अत्यंत सीमित व्यापार प्रथा का प्रचलन था। परंतु यह व्यापार ईमानदारी के साथ होता था और व्यापार विनिमय पद्धति पर आधारित था। गौरतलब है कि यदि व्यापारी व्यापार में पारदर्शिता नहीं बरतते तो उन्हें राजा का कोपभाजन बनना पड़ता था।
18वीं सदी के उत्तरार्ध और 19वीं सदी के प्रारंभ में पश्चिमी देशों में औद्योगिक और व्यापारिक क्रांति हुई। इन देशों ने एशिया, अफ्रीका और लातिन अमेरिका के अधिकांश देशों पर कब्जा कर उन्हें अपनी मंडी बना लिया। भारत पर ब्रिटेन ने कब्जा कर लिया। इस नए परिवर्तन से दुनिया भर में नये बाजारों का विकास हुआ तथा विभिन्न देशों के उत्पाद ग्राहकों को उपलब्ध होने लगे। उत्पादन के लिये बड़ी मशीनों का इस्तेमाल किया जाने लगा। इससे उत्पादन में संख्यात्मक और गुणात्मक दोनों ही दृष्टि से से वृद्धि हुई। पर इन बदलावों के साथ ग्राहकों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर से नये जोखिमों का सामना करना पड़ा। पुरानी अर्थव्यवस्था में माल का दर्जा, वर्गीकरण और उसका मूल्य निर्धारण आदि बातें तत्कालीन रीति-रिवाजों पर निर्भर रहा करती थीं। इन रीति-रिवाजों को समाज से एक तरह का समर्थन हासिल रहता था। पर इसके ठीक विपरीत बाजार पेठ आधारित बदली अर्थव्यवस्था में ग्राहक से आपेक्षा की जाने लगी कि वह स्वयं अच्छी तरह जांच-परख कर और सोच-समझकर बाजार में वस्तु का चयन करें।
20वीं शताब्दी के प्रारंभ तक अदालतें भी यह मान्यता स्वीकार करती थीं कि खरीदार को स्वयं सावधान रहना चाहिये। समय के साथ-साथ व्यापार में तेजी आई। बाजार पेठ में होनेवाले परिवर्तनों से अनभिज्ञ होने और उत्पादनों के स्तर तथा उसकी गुणवत्ता के बारे में अज्ञानता के कारण ग्राहक को हमेशा झुकना पड़ता था।
कुछ मालदार वितरक अपनी साधन सामग्री के बल पर कई ग्राहकों को गलत जानकारी देकर उसे गुमराह करने लगे। बिक्री करारनामों में धोखाधड़ी करके भी ग्राहकों को ठगा जाने लगा। उत्पादक और विक्रेता आपसी मिलीभगत कर माल की आपूर्ति और मूल्य वृद्धि के कुचक्र में ग्राहकों को फांसने लगे। आजकल तो विज्ञापनों के माध्यम से घटिया उत्पाद को भी अच्छे दामों में बेचा जा रहा है। विज्ञापनों से खरीदारों को लुभावने वादे और वस्तु/सेवा के गुणों को बढ़ा-चढ़ाकर प्रदर्शित किया जाता है।
बदली परिस्थितियों में उत्पादकों और व्यापारियों द्वारा शोषण और मनमानी से ग्राहकों के संरक्षण की जरूरत महसूस की जाने लगी। इंगलैंड, अमेरिका आदि औद्योगिक दृष्टि से विकसित देशों में उपभोक्ताओं के दबाव में उनके हितों की रक्षा के लिये कई कानून बनाने पड़े।
‘खरीदार को स्वयं सावधान रहना चाहिये’ वाली मान्यता फ ीकी पड़ने लगी। विक्रेता पर यह दायित्व डाला जाने लगा कि वह साबित करें कि उसने शर्तों के पालन या विज्ञापन के वायदों में किसी प्रकार की धोखाधड़ी नहीं की। अमेरिका में ग्राहक आंदोलन के कार्यकर्ताओं की सबसे बड़ी सफलता यह रही कि वे ग्राहक के हित के मुद्दे पर विचार करने के लिये सरकार को मजबूर करने में सफल रहे। ग्राहक हितों के मुद्दे पर 60 के दशक में ग्राहक आंदोलन के कार्यकर्ताओं ने इतना प्रभावी जनमत तैयार किया कि 1962 में अमेरिकी संसद को उपभोक्ता अधिकार का कानून बनाना पड़ा।
विश्व स्तर पर काम करनेवाले जागतिक संगठनों में ग्राहकों का प्रतिनिधित्व करनेवाले स्वैच्छिक संस्थाओं के एक विश्व संगठन की जरूरत महसूस की जाने लगी।
1960 में आईओसीयू यानी इंटरनेशनल आर्गनेशन ऑफ कंज्यूमर्स यूनियन्स की स्थापना की गयी। अब इस संस्था का नाम बदलकर कंज्यूमर्स इंटरनेशनल कर दिया गया। सीआई बहुत बड़ा संगठन है। इससे सौ से अधिक देशों के 240 संगठन जुड़े हुए हैं। इस संगठन ने अमेरिकी कानून में संलग्न उपभोक्ता अधिकार के घोषणा पत्र के तत्वों को बड़ाकर आठ कर दिया है जो कि इस प्रकार हैं- चयन का अधिकार, सूचित किये जाने का अधिकार, सुने जाने का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार, उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, स्वच्छ वातावरण तथा मूलभूत आवश्यकताओं जैसे भोजन, वस्त्र और आवास पाने का अधिकार।
सीआई के घोषणा पत्र के आधार पर संयुक्त राष्ट्र ने अप्रैल 1985 को उपभोक्ता संरक्षण के लिये अपना दिशा-निर्देश संबंधी एक प्रस्ताव पारित किया। भारत ने इस प्रस्ताव के हस्ताक्षरकर्ता देश के तौर पर इसके दायित्व को पूरा करने के लिये उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 बनाया जो कि 15 अप्रैल 1987 से लागू हो गया।
उपभोक्ता संरक्षण कानून 1986 सभी सामानों और सेवाओं पर लागू होता है। यह कानून उपभोक्ताओं के कुछ अधिकारों को कानूनी जामा पहनाता है। वे अधिकार हैं- सुरक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, चयन का अधिकार, अपनी बात कहने का अधिकार, शिकायत निवारण का अधिकार, तथा उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। इस कानून के तहत तीन स्तरों- जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तरों पर जिला फोरम, राज्य उपभोक्ता शिकायत निवारण आयोग और राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग जैसे अर्ध न्यायिक निकाय मशीनरी का प्रावधान है। जिला फोेरम उन मामलों में फैसले करता है जहां 20 लाख रुपये तक का दावा होता है, राज्य आयोग 20 लाख रुपये से ऊपर एक करोड़ रुपये तक के मामलों की सुनवाई करता है। जबकि राष्ट्रीय आयोग एक करोड़ रुपये से अधिक की राशि के दावेवाले मामले की सुनवाई करता है। इस कानून को और प्रभावी बनाने के लिये 1993 और 2002 में संशोधित किया गया।
कई मामलों में ग्राहक जागरूक न होने या कानूनी झंझट से बचने के लिये ही उपभोक्ता अदालत में शिकायत नहीं करते। पर इससे उत्पादकों व्यापारियों और सेवा प्रदान करनेवालों की मनमानी और बड़ती है। यदि ग्राहक मुस्तैदी दिखायें और उपभोक्ता अदालत में दस्तक देने लगे तो उत्पादकों, व्यापारियों और सेवा प्रदान करनेवालों की मनमानी पर काफी हद तक लगाम लग सकती है।
—————