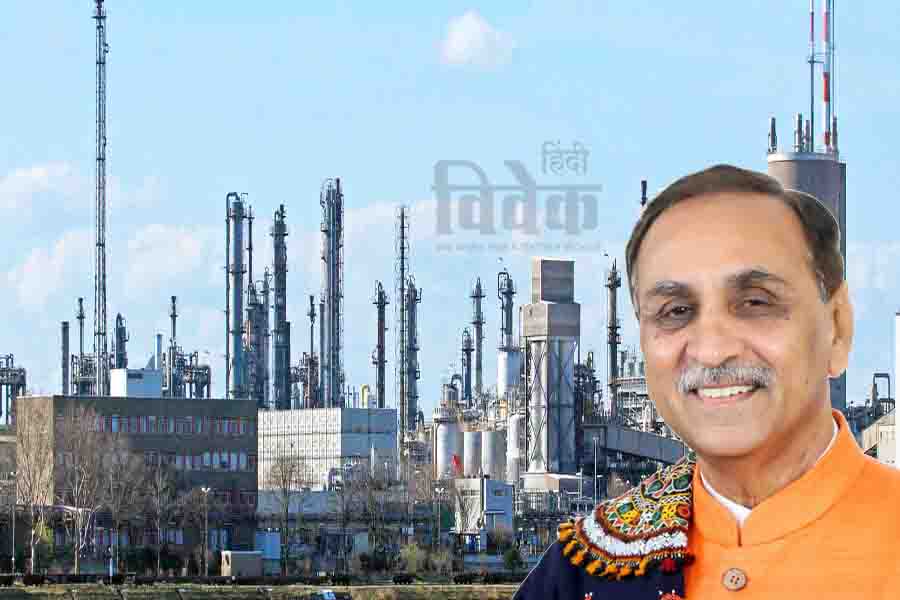भारतमाला चरण -1 में 24,800 किलोमीटर के कॉरिडोर नेटवर्क के उन्नयन से, निर्माण के चरण में लगभग 34 करोड़ श्रम दिवस उत्पन्न होंगे और आर्थिक गतिविधियों के बढ़ने के साथ लगभग 220 लाख स्थायी नौकरियों का सृजन होने की संभावना है।
आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 24 अक्टूबर, 2017 को आयोजित एक बैठक में भारतमाला परियोजना के चरण-1 के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। भारतमाला देश का एक व्यापक राजमार्ग विकास कार्यक्रम है। मौजूदा कमियों और परिवहन की बढ़ती जरूरतों के कारण भारत राजमार्ग क्षेत्र में महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा तैयार कर रहा है। भारतमाता राजमार्गों के बुनियादी ढांचे के लिए एक नए युग की शुरुआत का प्रतीक है।
राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना (एनएचडीपी) 1998 में एनडीए सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया देश का पहला प्रमुख राजमार्ग विकास कार्यक्रम था। योजना और निष्पादन के कॉरिडोर एप्रोच के आधार पर देश में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास, संचालन और अनुरक्षण के लिहाज से सड़क विकास में एक ऊंची छलांग लगाने की भारतमाला की परिकल्पना है। भारतमाला का उद्देश्य उपयुक्त पहल के जरिए पूरे देश के राष्ट्रीय राजमार्गों पर माल ढुलाई और यात्रियों, दोनों स्तर पर लॉजिस्टिक संबंधी दक्षता में सुधार करना है।
भारतमाला को डिजाइन करने का दृष्टिकोण
उच्च घनत्व वाले मूल-गंतव्य स्थान, दोनों के बीच माल की आवाजाही का एक व्यापक अध्ययन किया गया। इसके बाद नए आर्थिक गलियारों को पहचानने और विकसित करने के लिए एक नई रणनीति तैयार की गई ताकि आर्थिक क्षेत्र की लॉजिस्टिक संबंधी दक्षता को अधिकतम किया जा सके। इससे अर्थव्यवस्था पर बहुस्तरीय प्रभाव पड़ने की संभावना है। इस मूल गतंव्य स्थान अध्ययन ने एनएचडीपी के तहत संचालित परियोजनाओं के साथ आर्थिक गलियारों के एकीकरण ध्यान में रखा।
आर्थिक गलियारा
चिह्नित किए गए आर्थिक महत्व के गलियारों से आने वाले वर्षों में 25 प्रतिशत माल ढुलाई की संभावना है। एक बार निर्मित होने के बाद राष्ट्रीय और आर्थिक गलियारों, अपने अंतर-गलियारों और फीडर मार्गों के साथ, द्वारा माल ढुलाई के 80 प्रतिशत तक पहुंचने की संभावना है। लगभग 26,200 किलोमीटर लंबे खंडों को आर्थिक गलियारे के रूप में विकसित किया जाएगा, जिसमें से चरण -1 में 9,000 किलोमीटर पर काम किया जाएगा।
अतंर-गलियारा और फीडर मार्ग
लगभग 8,000 किलोमीटर अंतर-गलियारों और लगभग 7,500 किलोमीटर फीडर मार्गों को चिह्नित किया गया है जिनमें चरण -1 में 6,000 किलोमीटर पर काम किया जाएगा।
राष्ट्रीय गलियारा दक्षता सुधार
स्वर्ण-चतुर्भुज और उत्तर-दक्षिण और पूर्व-पश्चिम गलियारे भारत की 35 प्रतिशत माल ढुलाई करते हैं और उन्हें राष्ट्रीय गलियारा घोषित किए जाने का प्रस्ताव है। 6 राष्ट्रीय गलियारों में औसत यातायात 30,000 से अधिक पीसीयूज (पैसेंजर कार यूनिट) है। जैसी जरूरत हो, इन गलियारों की 6/8 लेनिंग की जाएगी। समय के साथ राष्ट्रीय गलियारों में चोक प्वाइंट्स बन गए हैं जो उनकी क्षमता को प्रभावित कर रहे हैं। इन गलियारों में भीड़ को कम करने के लिए िंंरग (रोडस )और बायपास व एलिवेटेड कॉरिडोर्स को बनाया जाना चाहिए। साथ ही सड़कों को विस्तार भी दिया चाहिए। इसके अतिरिक्त मोडल ट्रांसफर और माल ढुलाई को समूहबध्द एवं अलग-अलग करने के लिए रणनीतिक स्थानों पर लॉजिस्टिक्स पार्कों को विकसित करने की भी योजना बनाई गई है। चरण -1 में इस श्रेणी के अंतर्गत लगभग 5000 किलोमीटर पर काम किया जा रहा है।
सीमा और अंतरराष्ट्रीय कनेक्टिविटी सड़क
लगभग 3,300 किलोमीटर लंबी सीमा सड़कों को चिह्नित किया गया है जो अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर उनके रणनीतिक महत्व के कारण विकसित की जाएंगी। भारत के प्रमुख राजमार्ग गलियारे को अंतरराष्ट्रीय व्यापार बिंदुओं से जोड़ने के लिए लगभग 2,000 किलोमीटर लंबी सड़कों की जरूरत है ताकि पड़ोसी देशों जैसे नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार के साथ निर्यात-आयात को सुविधाजनक बनाया जा सके। चरण -1 में लगभग 2,000 किलोमीटर लंबी सड़कों पर काम किया जा रहा है।
 तटीय और बंदरगाह कनेक्टिविटी सड़क
तटीय और बंदरगाह कनेक्टिविटी सड़क
भारत के तटीय किनारों पर लगभग 2,100 किलोमीटर की तटीय सड़कों को चिह्नित किया गया है। इन सड़कों द्वारा तटीय क्षेत्रों में पर्यटन और औद्योगिक विकास के बढ़ने की संभावना है। गैर-प्रमुख बंदरगाहों की कनेक्टिविटी में सुधार के लिए लगभग 2,000 किलोमीटर की बंदरगाह कनेक्टिविटी सड़कों को चिह्नित किया गया है ताकि निर्यात-आयात को सहज किया जा सके। चिह्नित सड़कों को नौवहन मंत्रालय के सागरमाला कार्यक्रम के साथ सहयोग दिया गया है। चरण -1 में इस श्रेणी में करीब 2,000 किलोमीटर लंबी सड़कों पर काम किया जा रहा है।
ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे
राष्ट्रीय और आर्थिक गलियारों के कुछ हिस्सों में ट्रैफिक 50,000 पीसीयू से अधिक है और कई चोक (प्वाइंटस ) भी बन गए हैं। इनके 1,900 किलोमीटर हिस्से को ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के लिए चिह्नित किया गया है जिसके चरण -1में लगभग 800 किलोमीटर पर काम किया जा रहा है।
भारतमाला चरण-1-घटक और संभावित निवेश भारतमाला चरण -1 में लगभग 24,800 किलोमीटर लंबी सड़कें विकसित करने की योजना है। इसके अतिरिक्त चरण-1 में एनएचडीपी के तहत लगभग 10,000 किलोमीटर का शेष सड़क निर्माण कार्य भी शामिल है। चरण-1 के लिए पांच वर्षों में 5,35,000 करोड़ रूपये का परिव्यय अनुमानित है।
24,800 किलोमीटर से अधिक की सड़कों को चिह्नित करने के मामले में पर्याप्त लचीलापन है क्योंकि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री इस कुल लंबाई के 15 प्रतिशत हिस्से को दूसरी उपयुक्त परियोगनाओं में शामिल करने के लिए अधिकृत हैं। अगर किसी स्थिति में भूमि अधिग्रहण या अन्य अनपेक्षित कारणों से कुछ निश्चित हिस्सों को विकसित न किया जा सके।
परियोजनाओं का मूल्यांकन और अनुमोदन
इस कार्यक्रम की मुख्य विशेषता है एकल परियोजना का प्रभावी मूल्यांकन व अनुमोदन करना। इससे परियोजनाओं को समय पर लागू करना आसान होगा। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) को परियोजनाओं का मूल्यांकन और अनुमोदन करने का अधिकार दिया गया है। इसके अतिरिक्त इस बात को सुनिश्चित करने का प्रयास भी किया जा रहा है कि मूल्यांकन व अनुमोहन की प्रक्रिया में गुणवत्ता से कोई समझौता न किया जाए। सभी
परियोजनाओं का मूल्यांकन कुशल प्रॉजेक्ट एप्रेजल एंड टेक्निकल स्क्रूटनी कमिटियों द्वारा तकनीकी और आर्थिक स्तर पर किया जाए। इन कमिटियों का गठन प्राधिकरण और मंत्रालय में किया जाए और इनमें नीति आयोग में विशेष शामिल हों। ठेका देने की कार्रवाई में तेजी लाने के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा परियोजना संबंधी गतिविधियों को पहले ही शुरू किया गया है। नीति आयोग के सीईओ को एनएचएआई बोर्ड (प्राधिकरण) में अंशकालिक सदस्य के रूप में शामिल किया गया है।
बड़ी चुनौती की व्यवस्था
बड़ी चुनौती के माध्यम से विकास प्रक्रिया में भाग लेने के लिए राज्य सरकारों को प्रोत्साहित करना इस कार्यक्रम की एक और विशेषता है। इसके अंतर्गत, परियोजनाओं, जिसमें संबंधित राज्य सरकारों को एक सक्रिय भूमिका निभानी होती है, विशेष रूप से परियोजना के लिए जमीन उपलब्ध कराने के मामले में, को कार्यान्वयन के लिए प्राथमिकता दी जाएगी।
संस्थागत क्षमता में वृद्धि
कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय तथा उसकी कार्यान्वयन एजेंसियों की आंतरिक क्षमता को बढाने के लिए जागरूक प्रयास किये जा रहे हैं। “सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय तथा उसकी कार्यान्वयन एजेंसियों का संगठन और प्रक्रियागत परिवर्तन“ पर एक अध्ययन किया गया है और अध्ययन की कुछ सिफारिशें लागू की जा चुकी हैं जैसे भूमि अधिग्रहण से संबंधित सुधार, परियोजना डीपीआर की गुणवत्ता बढ़ाने से संबंधित सुधार, ऑनलाइन प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग सूचना प्रणाली (पीएमआईएस) और अन्य का निकास और कार्यान्वयन।
भारतमाला का प्रभाव
एक सुसंगत कॉरिडोर एप्रोच को अपनाते हुए पूरे देश में सड़कों पर यातायात की क्षमता में सुधार किया गया है। इस नेटवर्क से देश के विभिन्न जिलों में लगभग 80 प्रतिशत माल ढुलाई होने की संभावना है। इससे देश में वाहनों की औसत रफ्तार 20 से 25 प्रतिशत तक बढ़ जाएगी।
आर्थिक गलियारों और संबंधित अंतर -गलियारे और फीडर मार्गों के विकास के परिणामस्वरूप सड़कों के ढांचे में सुधार होगा, बाईपास, रिंग रोड्स के माध्यम से भीड़भाड़ समाप्त होगी। कॉरिडोर में प्रवेश व निकासी आधारित टोलिंग के साथ नियंत्रित प्रवेश वाले एक्सप्रेसवे जैसी पहल से राजमार्गों की औसत रफ्तार में अधिक सुधार होगा। माल ढुलाई वाले वाहनों की औसत रफ्तार में सुधार करने से तीन मुख्य लाभ होंगे- (क) वाहन उपयोग में सुधार होने से तेजी से बेक्रइवन (जब लागत-आय समान होती है) होगा और माल ढुलाई की लागत प्रति टन प्रति किलोमीटर कम होगी, (ख) फालतू समय न लगने के कारण वाहनों की ईधन क्षमता में सुधार होगा और माल ढुलाई की लागत कम होगी और (ग) तीव्र और विश्वसनीय माल पारगमन से माल ढुलाई के दौरान औसत इन्वेंटरी की खपत भी कम होगी। एक बार विकसित होने के बाद नेटवर्क की मदद से आपूर्ति श्रृंखला की लागत में कम होगी। यह लगभग 5-6 प्रतिशत कम हो जाएगी। देश के लॉजिस्टिक्स कुशलता सूचकांक (एलपीआई) पर भी इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
देश के 550 जिलों को एनएच लिंकेज से जोड़ा जा रहा है। वर्तमान में लगभग 300 जिलों में एनएच लिंक है।
राजमार्गों और संबंधित बुनियादी ढांचे के विकास, संचालन और रखरखाव से निवेश और निर्माण का रास्ता खुलेगा।
भारतमाला चरण -1 में 24,800 किलोमीटर के कॉरिडोर नेटवर्क के उन्नयन से, निर्माण के चरण में लगभग 34 करोड़ श्रम दिवस उत्पन्न होंगे और आर्थिक गतिविधियों के बढ़ने के साथ लगभग 220 लाख स्थायी नौकरियों का सृजन होने की संभावना है।