सच पूछिए तो अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर फिल्मों ने एक मीठे जहर की तरह हमें हमारे ही विरुद्ध कब खड़ा कर दिया गया पता ही नहीं चला। आज भगवान का मज़ाक उड़ाती ‘ओह माई गॉड’, ‘पीके’ जैसी फिल्मों को देख कर लोग ताली बजाते हैं। लेकिन क्या कभी अल्लाह का मज़ाक उड़ाती किसी फिल्म को आपने देखा है?
भारत में सिनेमा आम आदमी के जीवन का हिस्सा है। उसके सुख दुख का साथी है। अपने ख्वाबों को वह सिनेमा में देखता है। भारत में सिनेमा एक जुनून है, पागलपन है। यहां सिनेमा एक धीमा नशा है जो धीरे धीरे लोगों को अपनी गिरफ्त में लेता है और फिर उन्हें अपना आदी बना लेता है। हमारे देश में सिनेमा की शुरुआत 1913 में हुई। अगर हम उस समय की फिल्मों पर नज़र डालें तो उनकी कहानियां भारत की मिट्टी से जुड़ी हुई होती थीं। उस समय फिल्में धार्मिक, सामाजिक, ऐतिहासिक, स्टंट आदि श्रेणियों में बटी होती थीं। फिल्में समाज में परिवर्तन लाने का माध्यम भी बनीं। देश के लिए सिनेमा के सार्थक योगदान को नकारा नहीं जा सकता। लेकिन इसी के साथ सिनेमा में एक अलग विचार को भी स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा था। धीरे धीरे चल रहे ये प्रयास अब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर खुले आम हो रहे हैं।
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर आज देश की सनातन मान्यताओं, संस्कृति, सामाजिक मूल्यों और धार्मिक आस्थाओं पर प्रहार किया जा रहा है। देश में बदले राजनीतिक विचार के चलते अब इस प्रहार के विरोध में स्वर उठने लगे हैं। देश में राष्ट्रीय विचार के समर्थक अब फिल्मकारों के इस कृत्य को नकार रहे हैं। लेकिन एक खास विचारधारा के लोग इसे अभिव्यक्ति की आजादी पर प्रहार मान रहें हैं। यहां सवाल उठता है कि क्या अभिव्यक्ति की आजादी सिर्फ एक वर्ग विशेष के लिए है? इस आजादी का इस्तेमाल सिर्फ भारतीय मान्यताओं, संस्कृति, सामाजिक मूल्यों और हिंदुओं की आस्थाओं पर चोट पहुंचाने के लिए किया जाएगा?
 सिनेमा क्योंकि मनोरंजन का साधन था इसलिए आम जनता भी उसे उसी तरह से लेती थी। लेकिन धीरे धीरे आज़ादी के बाद या यूं कहें साझा गंगा जमुनी संस्कृति के नाम पर मनोरंजन के माध्यम से हमारे देश में एक खास विचार को प्रस्तुत करने का काम चल रहा था। 1947 में देश का विभाजन हुआ। विभाजन धर्म के नाम पर हुआ। इस देश के मुसलमानों को अपना मुल्क चाहिए था, इसलिए हुआ। देश के दो हिस्से हुए। एक हिस्से ने अपनी पहचान बनाए रखी वह मुस्लिम देश बना। लेकिन हमारे नेताओं ने देश को हिंदू राष्ट्र न बनाकर जो लोग विभाजन के जिम्मेदार थे उन्हें न केवल इसी देश में रखा, बल्कि उन्हें हिंदुओं के सिर पर बैठाया।
सिनेमा क्योंकि मनोरंजन का साधन था इसलिए आम जनता भी उसे उसी तरह से लेती थी। लेकिन धीरे धीरे आज़ादी के बाद या यूं कहें साझा गंगा जमुनी संस्कृति के नाम पर मनोरंजन के माध्यम से हमारे देश में एक खास विचार को प्रस्तुत करने का काम चल रहा था। 1947 में देश का विभाजन हुआ। विभाजन धर्म के नाम पर हुआ। इस देश के मुसलमानों को अपना मुल्क चाहिए था, इसलिए हुआ। देश के दो हिस्से हुए। एक हिस्से ने अपनी पहचान बनाए रखी वह मुस्लिम देश बना। लेकिन हमारे नेताओं ने देश को हिंदू राष्ट्र न बनाकर जो लोग विभाजन के जिम्मेदार थे उन्हें न केवल इसी देश में रखा, बल्कि उन्हें हिंदुओं के सिर पर बैठाया।
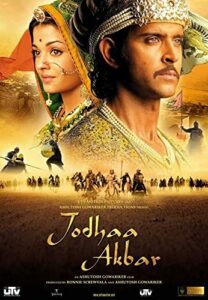 हम भारतीय सिनेमा का अगर एक सूक्ष्म विश्लेषण करें तो हमें ध्यान आएगा जो आज चल रहा है। उसकी भूमिका बहुत पहले से ही बन रही थी। कहीं सिनेमा के माध्यम से समाज में वर्ग विशेष के विरुद्ध जनमानस को खड़ा करने का प्रयास किया गया। सामाजिक कुरीतियों को सबके सामने लाने के नाम पर दो वर्गों में भेद खड़ा किया गया। अमीर के गरीब पर अत्याचार की कहानियां बनाकर दोनो वर्गों में दूरी बना दी गई। समांतर सिनेमा गढ़ा गया जिसमें वास्तविक सिनेमा के नाम पर खास तरह की फिल्मों का निर्माण किया गया। अगड़े-पिछडों के बीच दूरी बढ़ाई गई। सबसे बुरा यह किया गया कि धार्मिक भेदभाव की छोटी मोटी घटनाओं का चित्रण भी इस प्रकार किया गया जैसे ये सारे समाज की मानसिकता हो। सुनियोजित तरीके से सिनेमा का उपयोग एक ऐसे हथियार के रुप में किया गया जिससे देश का बहुसंख्यक समाज हमेशा टुकड़ों में बंटा रहे, कभी एक न हो पाए।
हम भारतीय सिनेमा का अगर एक सूक्ष्म विश्लेषण करें तो हमें ध्यान आएगा जो आज चल रहा है। उसकी भूमिका बहुत पहले से ही बन रही थी। कहीं सिनेमा के माध्यम से समाज में वर्ग विशेष के विरुद्ध जनमानस को खड़ा करने का प्रयास किया गया। सामाजिक कुरीतियों को सबके सामने लाने के नाम पर दो वर्गों में भेद खड़ा किया गया। अमीर के गरीब पर अत्याचार की कहानियां बनाकर दोनो वर्गों में दूरी बना दी गई। समांतर सिनेमा गढ़ा गया जिसमें वास्तविक सिनेमा के नाम पर खास तरह की फिल्मों का निर्माण किया गया। अगड़े-पिछडों के बीच दूरी बढ़ाई गई। सबसे बुरा यह किया गया कि धार्मिक भेदभाव की छोटी मोटी घटनाओं का चित्रण भी इस प्रकार किया गया जैसे ये सारे समाज की मानसिकता हो। सुनियोजित तरीके से सिनेमा का उपयोग एक ऐसे हथियार के रुप में किया गया जिससे देश का बहुसंख्यक समाज हमेशा टुकड़ों में बंटा रहे, कभी एक न हो पाए।
एक समय था भारत में मनाए जाने वाले त्यौहार दीवाली, होली, भाईदूज, व्रत, तीज आदि फिल्मों का एक अहम हिस्सा होते थे। कहीं ना कहीं फिल्म निर्माताओं के दिमाग में रहता था कि इनको दिखाने से दर्शक सिनेमा हाल में आएंगे। लेकिन धीरे धीरे न जाने कब ये हमारी फिल्मों से खत्म होते गए हमें पता ही नहीं चला। फिल्मों में से भजन, गीत का स्थान कब सूफी संगीत के नाम पर मज़ार पर गाए जाने वाले गीतों ने ले लिया पता ही नहीं चला। ईश्वर की जगह कब अल्लाह स्थापित हो गए पता ही नहीं चला। हिंदू त्यौहार सांप्रदायिक हो गए। ईद गंगा-जमुनी तहजीब का प्रतीक। दीवार जैसी फिल्म में नायक ईश्वर के प्रति आस्था नहीं रखता है लेकिन 786 नंबर का बिल्ला उसको हर मुसीबत से बचाता है, यह किस तरह का सिनेमा है? ऐसी अनेक फिल्में मिल जाएंगी जहां नायक को ईश्वर से बड़ी शिकायतें होंगी लेकिन उसी फिल्म में कोई न कोई ऐसा किरदार होगा जो अल्लाह या गॉड में आस्था रखता होगा और एक सच्चा इंसान होगा।
 कैसे अमर अकबर एंथनी में शिरडी के साईं बाबा की कव्वाली डालकर एक ऐसे व्यक्ति को लाखों लोगों की आस्था का प्रतीक बना दिया गया जिसका अपना धर्म मुस्लिम था। सच पूछिए तो एक मीठे जहर की तरह हमें हमारे ही विरुद्ध कब खड़ा कर दिया गया पता ही नहीं चला। आज भगवान का मज़ाक उड़ाती ‘ओह माई गॉड’, ‘पीके’ जैसी फिल्मों को देख कर लोग ताली बजाते हैं। लेकिन क्या कभी अल्लाह का मज़ाक उड़ाती किसी फिल्म को आपने देखा है? क्या सारा सुधार हिंदू समाज में होना है? क्या मुस्लिम समाज की कुरीतियों तीन तलाक, हलाला, कुरान, उनकी अपनी हालत पर कोई फिल्म नहीं बननी चाहिए? क्या सिर्फ हिंदू समाज ही जाति में बंटा है? क्या मुस्लिम समाज की जाति व्यवस्था में सुधार के लिए कोई फिल्म नहीं बननी चाहिए? इस बात पर हमें सोचना चाहिए कैसे हमें धीरे धीरे आधुनिकता के नाम पर, प्रोगेसिव होने के नाम पर भ्रमित करके हमें अपने संस्कारों से दूर करने का प्रयास किया गया।
कैसे अमर अकबर एंथनी में शिरडी के साईं बाबा की कव्वाली डालकर एक ऐसे व्यक्ति को लाखों लोगों की आस्था का प्रतीक बना दिया गया जिसका अपना धर्म मुस्लिम था। सच पूछिए तो एक मीठे जहर की तरह हमें हमारे ही विरुद्ध कब खड़ा कर दिया गया पता ही नहीं चला। आज भगवान का मज़ाक उड़ाती ‘ओह माई गॉड’, ‘पीके’ जैसी फिल्मों को देख कर लोग ताली बजाते हैं। लेकिन क्या कभी अल्लाह का मज़ाक उड़ाती किसी फिल्म को आपने देखा है? क्या सारा सुधार हिंदू समाज में होना है? क्या मुस्लिम समाज की कुरीतियों तीन तलाक, हलाला, कुरान, उनकी अपनी हालत पर कोई फिल्म नहीं बननी चाहिए? क्या सिर्फ हिंदू समाज ही जाति में बंटा है? क्या मुस्लिम समाज की जाति व्यवस्था में सुधार के लिए कोई फिल्म नहीं बननी चाहिए? इस बात पर हमें सोचना चाहिए कैसे हमें धीरे धीरे आधुनिकता के नाम पर, प्रोगेसिव होने के नाम पर भ्रमित करके हमें अपने संस्कारों से दूर करने का प्रयास किया गया।
हमारे इतिहास से छेड़छाड़ की गई। यह कैसे संभव है कि एक आक्रांता विजेता बना कहावतों का हिस्सा बना, सिनेमा का शीर्षक बना ‘जो जीता वहीं सिकंदर’ लेकिन उसके विश्व विजय के सपने को तोड़ने वाला राजा पुरू किसी कहावत का हिस्सा नहीं है। काल्पनिक कहानियों को आधार बनाकर जहांगीर को न्याय का दूसरा नाम बताया गया, पुकार जैसी फिल्म में जहांगीर के इंसाफ का बखान किया गया। जोधा- अकबर की प्रेम कहानी बताई गई। अकबर को इंसाफ पसंद बताया गया और सारा जीवन अपनी मातृभूमि के लिए जंगलों में भटकने वाले, अकबर की सेना को नाकों चने चबवाने वाले वीर महाराणा प्रताप, उनका त्याग, तपस्या हमारी कहानियों का हिस्सा क्यों नहीं हैं?
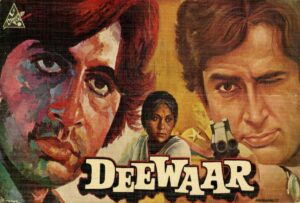 आखिर क्यों अधिकांश फिल्मों में हिंदू किरदार को खलनायक की तरह दिखाया जाता है। मंदिर का पुजारी धर्म के नाम पर लोगों को ठगने वाला, सूदखोर साहूकार, भ्रष्ट नेता, पुलिसवाला हिंदू ही क्यों होते हैं? क्यों नहीं किसी मस्जिद की सच्चाई दिखाई जाती है? कभी किसी ने चर्च में होने वाले व्यभिचार को दिखाने की हिम्मत की है?
आखिर क्यों अधिकांश फिल्मों में हिंदू किरदार को खलनायक की तरह दिखाया जाता है। मंदिर का पुजारी धर्म के नाम पर लोगों को ठगने वाला, सूदखोर साहूकार, भ्रष्ट नेता, पुलिसवाला हिंदू ही क्यों होते हैं? क्यों नहीं किसी मस्जिद की सच्चाई दिखाई जाती है? कभी किसी ने चर्च में होने वाले व्यभिचार को दिखाने की हिम्मत की है?
आज मनोरंजन के नए माध्यम वेब सीरिज में खुलेआम हिंदू देवी देवताओं का मज़ाक बनाया जा रहा है। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर हमारे सांस्कृतिक मूल्यों, आस्था पर प्रहार किया जा रहा है। कहानी के मुख्य पात्रों के नाम देवी देवताओं के नाम पर रखकर उन्हें गलत काम करते दिखाया जा रहा है। किसी को इसमें कोई बुराई नज़र नहीं आती। लेकिन अभी ईरानी फिल्म पैगबंर- द मैसेंजर ऑफ गॉड नाम की फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने की बात हुई तो महाराष्ट्र सरकार में मंत्री अनिल देशमुख ने सूचना प्रसारण मंत्री को पत्र लिखकर इसको रोकने के लिए कहा है। कुछ मुस्लिम नेताओं ने तो इसके प्रदर्शन पर कानून व्यवस्था खराब होने की भी चुनौती दे डाली है। अब क्या यह किसी की अभिव्यक्ति की आजादी पर प्रहार नहीं है? क्या इस तरह की जागरूकता तब भी नहीं दिखाई जानी चाहिए थी जब ‘पीके’ में भगवान शिव का मज़ाक उड़ाया जा रहा था?
सच तो यह है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर वामपंथी विचारधारा के लोगों ने समाज को एक दूसरे से काटने का काम किया है। सिनेमा हमेशा से असंगठित क्षेत्र रहा है। फिल्मों में पैसा कहां से लगता है, कौन है जो फिल्मों का कथानक तय करते हैं? कौन है जो संगठित होकर खानत्रयी को इस देश में महानायक बनाते हैं? कौन हैं वे लोग जो देश में सिनेमा पर अपना आधिपत्य बनाए हुए हैं? कौन लोग हैं जो पर्दे के पीछे से इस खेल को खेल रहें हैं? आज ये सवाल सबके सामने उठ रहे हैं। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत ने फिल्म उद्योग की गंदगी को सबके सामने लाकर रख दिया है। कैसे एक प्रतिभाशाली अभिनेता असमय अपने प्रशंसकों से जुदा हो गया। किस तरह से एक खास लॉबी ने सुशांत जैसे अनेक कलाकारों के लिए कोई विकल्प नहीं छोड़ा है।
 आज इंडस्ट्री की गंदगी बाहर आ रही है। पर्दे के पीछे की कहानियां सबके सामने आ रही हैं। आज तक जो ढंका छुपा था कि पैसा किसका लग रहा है, वह भी सबके सामने आ रहा है। यह सही समय है इनका सच सामने लाने का। जनता को जागरूक करने का। उसे इस धीमे ज़हर से बाहर निकालने का। अभिव्यक्ति की आज़ादी को परिभाषित करने का, उसकी मर्यादा तय करने का। सिनेमा की ताकत का उपयोग देश और समाज के लिए करने का। दर्शक होने के नाते यह हमारा दायित्व है कि इस तरह के सिनेमा को हम नकार दें। याद रखिए अगर इस तरह की फिल्में, वेब सीरिज अगर असफल होंगी तो इनके निर्माताओं का मनोबल टूटेगा। सकारात्मक सिनेमा का स्वागत कीजिए, उसे सफल बनाइए। अगर हम इस बार भी चूक गए तो वह दिन जल्द आएगा जब हम अपनी पहचान को भुला चुके होंगे। अपने गौरव को भुला चुके होंगे।
आज इंडस्ट्री की गंदगी बाहर आ रही है। पर्दे के पीछे की कहानियां सबके सामने आ रही हैं। आज तक जो ढंका छुपा था कि पैसा किसका लग रहा है, वह भी सबके सामने आ रहा है। यह सही समय है इनका सच सामने लाने का। जनता को जागरूक करने का। उसे इस धीमे ज़हर से बाहर निकालने का। अभिव्यक्ति की आज़ादी को परिभाषित करने का, उसकी मर्यादा तय करने का। सिनेमा की ताकत का उपयोग देश और समाज के लिए करने का। दर्शक होने के नाते यह हमारा दायित्व है कि इस तरह के सिनेमा को हम नकार दें। याद रखिए अगर इस तरह की फिल्में, वेब सीरिज अगर असफल होंगी तो इनके निर्माताओं का मनोबल टूटेगा। सकारात्मक सिनेमा का स्वागत कीजिए, उसे सफल बनाइए। अगर हम इस बार भी चूक गए तो वह दिन जल्द आएगा जब हम अपनी पहचान को भुला चुके होंगे। अपने गौरव को भुला चुके होंगे।
——–




Bycot