तमाम आर्थिक और तांत्रिक समस्यांओ को पार करते हुए 21 अप्रैल 1913 में धुंडिराज गोविंद फालके अर्थात दादा साहेब फालके ने पहली भारतीय फिल्म ‘‘राजा हरिश्चन्द्र’’ का प्रीमियर शो कुछ मान्यवर अतिथियों के सामने पेश किया। इसके पश्चात 3 मई 1913 को कोरोनेशन सिनेमाघर में उसका प्रदर्शन किया गया। इस वर्ष संपूर्ण भारत मे इसी घटना की सौंवी वर्षगांठ मनाई जा रही है।
इस संपूर्ण शतक मे ‘भारतीय सिनेमा’ की यात्रा यशस्वी बहुरंगी और समाज से जुडी रही। समाज और भारतीय सिनेमा का रिश्ता इतना पक्का है कि इन्हे एक दूसरे से अलग करना मुश्किल है। समय के साथ-साथ सिनेमा देखने की पद्धति में भी परिवर्तन होता रहा। एक पहदा सिनेमा घर से लेकर इंटरनेट तक का यह सफर बहुत मनोरंजक रहा। इस सफर में कभी सिनेमा का प्रभाव समाज पर पड़ा तो कभी समाज की आवश्यकता के अनुसार सिनेमा में परिवर्तन आया।
हमारे यहां जब सिनेमां की शुरुवात हुई तब उसे चित्रित किये गये नाटक के रूप में देखा जाता था। विशेषत: दादा साहब तोरणे द्वारा निर्मित ‘पुंडलिक’ कुछ इसी प्रकार का था। ‘राजा हरिश्चन्द्र’ चित्रपट जब समाज के सामने आया तो परदे पर चलने बोलनेवाले चित्र लोगों के लिये कौतुहल का विषय था। कुछ लोग तो इसे जादू-टोना समझने लगे। कई लोगो ने इसे समाज के लिये घातक, पाप, आदि शब्दो से भी संबोधित किया। परेश मोकोशी द्वारा दिग्दर्शित मराठी चित्रपट ‘हरिश्चन्द्राची फैक्टरी’ मे ‘राजा हरिश्चन्द्र’ सिनेमा के समय की समाज की मानसिकता के स्पष्ट दर्शन होते हैं। उस समय के लोग सीधे-साधे, सन्मार्ग पर चलनेवाले होते थे। उन लोगों द्वारा सिनेमा के लिये ऐसी प्रतिक्रिया देना स्वाभाविक लगता है। परंतु लोगों ने तब सिनेमा को स्वीकार किया और तब से वह समाज का अंग है इस विषय पर कुतुहल निर्माण होता है। किसी भी नये माध्यम के आने पर समाज ने उसके दुष्परिणाम ही पहले देखे। ‘टेलिफोन’ के आविष्कार के समय भी लोगों ने सोचा कि यह कैसा अजीब सा यंत्र है जिसमें दूर बैठे किसी व्यक्ति की आवाज हमें सुनाई देती है और हमारी आवाज उसे। टेलीफोन को दूर बैठे व्यक्ति से संवाद करने के उपयुक्त यंत्र के रूप में पहचान बनाने में बहुत समय लगा। सिनेमा का हाल भी कुछ ऐसा ही है। ‘बायोस्कोप से सिनेमास्कोप’ सिनेमा से थ्री डी सिनेमा तक’, ‘गली सिनेमा से मल्टीप्लैक्स तक’ और ‘मिनी थियेटर से चलते-फिरते सिनेमा घर तक’ की यात्रा के दौरान सिनेमा ने कई ऊंचे-नीचे स्तर देखे। सिनेमा की इस यात्रा मे दूरचित्रवाणी, व्हीडियो, उपग्रह चैनल, होम थियेटर, डीबीडी, जैसे अनेक घटक शामिल है। परंतु इस सभी की धुरी सिनेमा ही रहा।
सिनेमा और समाज का रिश्ता किसी लकीर के समान सीधा-सीधा नहीं है। यह एक इतिहास है। यह केवल ढाई तीन घंटे का मनोरंजन नही बल्कि एक सशक्त माध्यम है। 14 मार्च 1931 में प्रदर्शित ‘आलमआरा’ पहला चित्रपट था जिसे लोगों ने संवादों के साथ देखा। अर्थात अब लोगों को चलते-बोलते चित्रों के साथ-साथ पात्रों के संवाद भी सुनाई देने लगे। कुछ वर्षों के बाद ही पहला रंगीन चित्रपट ‘सौरंध्री’ लोगों के सामने पेश किया गया। इस चित्रपट के प्रिन्ट पर जर्मनी में तांत्रिक कारामात की गई थीं। ‘कृष्ण-धवल’ सिनेमा के युग में इस तरह के रंगीन चित्रपट को देखना लोगों के लिये उत्सुकता का विषय था।
जैसे-जैसे सिनेमा अपने प्रगतिपथ पर बढ़ता गया वैसे-वैसे समाज का सिनेमा के प्रति आकर्षण भी बढ़ता गया। शुरु में ‘संत ज्ञानेश्वर’ जैसे पौराणिक और ‘दुनिया न माने’ जैसे सामाजिक चित्रपट ने लोगों का भरपूर मनोरंजन किया। प्रभात प्रोडक्शन के ‘आदमी’ चित्रपट में एक पुलिस आफिसर और एक वेश्या की प्रेमकहानी है। वहीं मेहबूब खान का ‘आस’ चित्रपट पहला टेक्निकलर चित्रपट था।
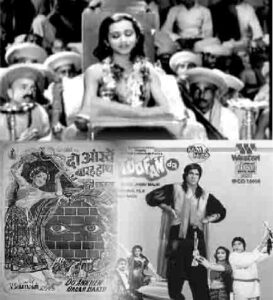 कई चित्रपटों में स्वतंत्रता की लढ़ाई का बहृत अच्छा प्रदर्शन किया गया है। इससे यह सिद्ध होता है कि भारतीय सिनेमा समाज के किसने करीब है। उदाहरण के लिये बाम्बे टीकाज प्रस्तुत ‘किस्मत’ (1943) का ‘‘दूर हटो ओ दुनियावालो हिन्दुस्तान हमारा है’’ गीत आज तक लोगों को याद आता है। ब्रिटिश शासन के खिलाफ किये गये आंदोलनों में सिनेमा ने भी समाज के कंधे से कंधा मिलाया और इसी कारण लोगों ने इसे बहुत पसंद किया। भारत का ‘आम आदमी’ हमेशा से ही सिनेमा के प्रति भावुक रहा है।
कई चित्रपटों में स्वतंत्रता की लढ़ाई का बहृत अच्छा प्रदर्शन किया गया है। इससे यह सिद्ध होता है कि भारतीय सिनेमा समाज के किसने करीब है। उदाहरण के लिये बाम्बे टीकाज प्रस्तुत ‘किस्मत’ (1943) का ‘‘दूर हटो ओ दुनियावालो हिन्दुस्तान हमारा है’’ गीत आज तक लोगों को याद आता है। ब्रिटिश शासन के खिलाफ किये गये आंदोलनों में सिनेमा ने भी समाज के कंधे से कंधा मिलाया और इसी कारण लोगों ने इसे बहुत पसंद किया। भारत का ‘आम आदमी’ हमेशा से ही सिनेमा के प्रति भावुक रहा है।
स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हमारे देश में अलवा वातावरण निर्माण होने लगा था। लोग देश को ‘अपना देश’ के रुप में देख रहे थे और उनके में आशावाद और नये स्वप्नों का उगम हो रहा था। बिलकुल इसी समय भारतीय सिनेमा में भी तीन महानायकों का उगम हो रहा था।’ ट्रेजडी किंग दिलीप कुमार ने सामाजिक स्तर की ‘नया दौर’ में अपनी छाप छोडी। अपने समय के चॉकलेटी हीरो देव आनंद ने पानी की समस्या पर आधारित चित्रपट गाइड से लोगों का मन लुभाया और प्रेम को बहुरंगी रुप में दर्शाने वाले राज कपूर के ‘श्री 420’ लोगों के आकर्षण का केन्द्र रहीं। इस तिकडी की लोकप्रियता का जादू लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा था।
सामाजिक समस्याओं पर प्रकाश डालने वाले चित्रपटों का निर्माण अपनी गीत से निरंतर होता रहा। सन 1938 में आई ‘डॉ कोटनीस की अमर कहानी’ एक युवा डॉक्टर के त्याग पर आधारित सत्य घटना को दिखाती है। 1946 में प्रदर्शित ‘नीचा नगर’ अमीर-गरीब के बीच की खाई और उससे उत्पन्न संघर्ष को दिखाते है। 1947 की ‘सिंदूर’ में विधवा पुनर्विवाह की समस्या, 1946 की ‘धरती के लाल’ मे बंगाल के एक गांव के मध्यमवर्गीय परिवार की समस्या, 1953 की ‘दो बीघा जमीन’ में अपने कर्ज से अपनी जमीन को छुडाने की जद्दोजहद, 1954 की ‘बूट पालिश’ में अनाथ बच्चों द्वारा बूट पालिश करके अपना जीवनयापन करना, 1956 की ‘जागते रहो’ में एक गांव का गायक अपने सपने पूरे करने हेतु शहर की इमारत में आता है जहां उसे चोर समझा जाता है, 1957 की ‘प्यासा’ में एक मित्र द्वारा दूसरे मित्र की दुर्घटना में मृत्यू की अफवाह के बाद उसकी शानदार कविताओं को अपने नाम पर समाज के सामने लाना 1957 की ‘दो आंखे’ बारह हाथ’ में एक जेलर द्वारा छ: खौफनाक कैदियो को इंसान बनाने का प्रयत्न, 1959 की ‘सुजाता’ में सुजाता नामक निम्न जाति की युवती का जीवन संघर्ष, 1960 की ‘अनुराधा’ में एक डॉक्टर द्वारा ग्रामीण भाग भाग में अपनी सेवाएं देना 1967 की ‘उपकार’ के गीत मेरे देश की धरती सोना उगले को लोगों द्वारा देशभक्ति गीत के रूप में अपनाना, 1970 की ‘दस्तक’ में एक नलदंपत्ति का घर ढूंढने की कोशिश में रेड लाईट एरिया में रहना और बडी सामाजिक समस्या का सामना करना, 1971 की ‘आनंद’ में कैंसर पीडित युवक द्वारा जीवन जीने कला सिखाते हुए कहना कि ‘जिंदगी बडी होनी चाहिये लंबी नहीं’ 1972 की ‘कोशिश’ में एक गूंगे बहरे दंपत्ति की कथा-व्यथा, 1973 की ‘गरम हवा’ में हिन्दु मुस्लिम एकता की कथा, 1974 की ‘अंकुर’ में जमींदार द्वारा आदिवासियों का किया जानेवाला शोषण, 1976 में आई घरौंदा में नवदंपत्ति द्वारा महानगर में घर लेने की कोशिश करना और फसना, 1979 की ‘स्पर्श’ में दृष्टिहीनों की भावनाओं की कथा, 1980 की ‘आक्रोश’ में आदिवासियों के शोषण की कहानी, 1980 की ‘अल्बर्ट पिन्टो को गुस्सा क्यों आता है’ में समाज और राजकीय परिस्थितियों में होनेवाले राजकीय बदलावों के कारण युवक की वैचारिक भावनिक स्थिति, 1983 की ‘अर्धसत्य’ में पुलिस के भ्रष्टाचार के विरोध में उठाये गये कदम, 1984 की ‘मोहन जोशी हो’ में चॉल में रहनेवाले मध्यमवर्गीय परिवारों की मतभिन्नता, 1985 की ‘नाचे मयूरी’ में प्रत्यक्ष जीवन में आनेवाले अनेक संकटों को पार करते हुए एक युवती के द्वारवा नृत्य के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचना, 1985 की ही ‘राम तेरी गंगा मैली’ में एक ग्रामीण युवती का अपने प्रेमी को ढूंढते हुए शहर में आना और इस दौरान कई समस्याओं का सामना करना, 1988 की ‘सलाम बॉम्बे’ में मुंबई के फुटपाथ पर रहनेवाले लोगों की कहानी, 1990 की दिशा में मुंबई के कपडा मिलो में काम करने वालों द्वारवा मिलजुल कर चाल में रहना और सभी त्यौहारों को मनाना, 1991 में आई ‘मैं आजाद हूं’ में राजनैतिक चालों के खिलाफ जनसामान्य को एकत्र करना, 1992 की ‘प्रहार’ में सैनिक प्रशिक्षण की कथा, 1992 की ‘रोजा’ में कश्मिर के आतंकवादियों द्वारा बंदी बनाये गये अपने पति को छुडाने के लिये एक पत्नि के द्वारा किये गये सभी प्रयत्न, 1994 की ‘हम आप के है कौन’ में देश के अमीर परिवार के सुख दुखो की झलक, 1994 में आई ‘1942 अ लव्ह स्टोरी’ में स्वतंत्रता संग्राम की पृष्ठभूमि पर एक प्रेम कथा, 1994 की ‘दिलवाले दुल्हनिया ले जायेंगे’ में इंग्लैंड स्थित भारतीय प्रेमी प्रेमिका की कहानी उस में भारतीय मिट्टी की याद, 1997 की ‘दिल तो पागल है’ में आधुनिक संगीत की पार्श्वभूमि पर आधारित प्रेम त्रिकोण, 2000 में आई ‘मिशन कश्मीर’ में आतंकवादियों द्वारा फैलाई जानेवाली दहशत, 2001 की ‘लगान’ में अंग्रेजों को उनके खेल क्रिकेट में मात करने की कहानी और ऑस्कर में नामांकन, 2002 में ‘चांदनी बार’ में मुंबई के बार में काम करने वाली युवतियों की कहानी, 2005 में ‘पेज थ्री’ के द्वारा मुंबई के ‘पार्टी सर्कल’ का प्रदर्शन, 2008 की ‘फैशन’ में फैशन की दुनिया के मुखौटे और उनके पीछे के चेहरों का प्रदर्शन, 2009 मे ‘पा’ मे अमिताभ द्वारा मेकअप की सहायता से किया गया अभिनय, 2011 में प्रदर्शित ‘देहली बोली’ में आज की युवा पीढी द्वारा प्रयोग में लाई जानेवाली भाषा का बेधडक प्रदर्शन ये सभी चित्रपट सिनेमा के सफर और उसके समाज के साथ रहने वाले जुडाव को दर्शाते हैं।
ऐसी ही अन्य कई फिल्मों के द्वारा समाज की अनेक समस्याओं और अच्छी बुरी बातों पर निरंठर प्रकाश डाला जाता रहा। अत: हमारे देश में सिनेमा ही आम जनता तक पहुंचने का सशक्त माध्यम रहा। अपने देश की विभिन्न जातियां, धर्म, भाषा, पंथ आदि से निर्माण होने वाली समस्यांए और इन सभी को पसंद आनेवाला चित्रपट बनाना बहुत कठिन है। परंतु हिन्दी सिनेमा इन सभी को मात करते हुए आगे बढ़ता गया और फलता-फूलता गया। हिन्दी सिनेमा की स्वत: की एक संस्कृति है। मनोरंजन के माध्यम से समाज प्रबोधन यही इसकी खास पहचान है। विश्व के अन्य किसी भी देश के फिल्मों में न मिलनेवाली गीत-संगीत-नृत्य इसकी पहचान है। भारतीयो के जीवन में जन्म से लेकर मृत्यू तक के सभी महत्वपूर्ण विधानों ने गीत व नृत्य सिनेमा में शामिल है। इनकी ताल पर सभी तीज त्यौहारों पइ अमीर-गरीब सभी नाचते-गाते हैं। अत: सिनेमा में गीत होने के सवाल पर कोई प्रश्नचिन्ह नही लग सकता। चित्रपट की पटकथा में गीत के लिये उपयुक्त जगह होनी चाहिये और दर्शकों को उस गीत का आनंद मिलना चाहिये यही कोशिश सदैव रहती है।
सौ वर्षों के इस लंबे अंतराल में भारतीय समाज ने अपने ‘स्टार’ को भरपूर प्यार दिया। राजेश खन्ना पहला सुपर स्टार था। दर्शको की एक पूरी पीढ़ी उसकी दीवानी थी। ‘आनंद’, ‘आराधना’, ‘बहारो के सपने’, ‘दो रास्ते’, ‘हाथी मेरे साथी’, ‘द ट्रेन’, ‘आप की कसम’, ‘मर्यादा’, ‘दुश्मन’, ‘अमर प्रेम’, जैसी कई फिल्मों को दर्शको ने खून सराता। इसके बाद एंग्री यंग मैन की छबि लेकर अमिताभ बच्चन का अवतार हुआ। यह नायक तात्कालिक समाज की स्थिती को समाज के सामने लाता है ऐसा माना जाने लगा। दीवार, जंजीर, खून पसीना, लावारिस, नमक हलाल, मुकद्दर का सिकंदर आदि चित्रपट महत्वपूर्ण रहे। शाहरूख खान कंप्यूटर-इंटरनेट की पीढ़ी का नायक है। स्वत: के गुणों से मार्केटिंग और प्रमोशन करने के लिये वह प्रसिद्ध है। ‘दीवाना’, कुछ कुछ होता है, वीर जारा, कभी अलविदा ना कहना, रा वन आदि चित्रपट महत्वपूर्ण है। भारतीय समाज कलाकारों से प्रेम करता है। परंतु केवल इसलिये उनके निम्न दर्जे का चित्रपट भी स्वीकार कर लें ऐसा नहीं है। दिलीप कुमार का बैराग, राजेश खन्ना का मेहबूबा, अमिताभ का तूफान, शाहरूख का डॉन लोगों ने अस्वीकार कर दिये। भारतीय समाज सिनेमा का दीवाना है परंतु अंधा नहीं है। उनकी यह दीवानगी अपने ‘फेवरेट’ कलाकार को कोई नाम देकर भी प्रदर्शित होती है। (प्राण खलनायक होने के कारण उसका किसी ने कोई नाम नहीं दिया।) कॉलेज में पढ़नेवाले बच्चे भी चित्रपटों से कल्पना प्राप्त करते हैं। हम आपके है ने सभी शादियो को संगीत प्रदान किया। सिनेमा के कारण ही शादी के बाद हनीमून पर जाने की प्रथा शुरू हुई। प्रेमभंग होने के बाद किसी विरहगीत की साथ भी फिल्मों से ही मिलती है। मनुष्य के जीवन से जुडी हुई प्रत्येक घटना से सिनेमा को संबद्ध किया जा सकता है। हमारे सिनेमा यथार्थ दूर केवल स्वप्न रंजन करते हैं ऐसी मिथ्याओं को भी सिनेमा ने पीछे धकेल दिया है। सत्य तो यह है कि प्रशंसा के स्थान पर सिनेमा पर टीका टिप्पणी ही अधिक हुई है। सिनेमा पर प्रेम करनेवाले मूर्ख लोग या फिर समीक्षा-चिकित्सा विश्लेषण करनेवाले सामान्य लोग ऐसी कई बातें कही गई। इन सारी प्रतिकूलताओं के बावजूद भी लोगो के दिलों पर सिनेमा ने रज किया। कई लोगों के लिये यह जीने का आधार बना। इस पूरे यात्रा में रमेश सिप्पी की ‘शोले का महत्वपूर्ण स्थान है। 1975 की यह फिल्म आज की युवा पीढ़ी को भी आकर्षित करती है।
सौ वर्षों की इस यात्रा में मराठी-बंगाली-मलयालम फिल्मों को भी सहयोग रहा।
भारतीय चित्रपट एक ऐसा वृक्ष है जिसकी कई टहनियां, फल, फूल और साथ ही साथ कांटे भी है इस सत्य को कोई नकार नहीं सकता।



