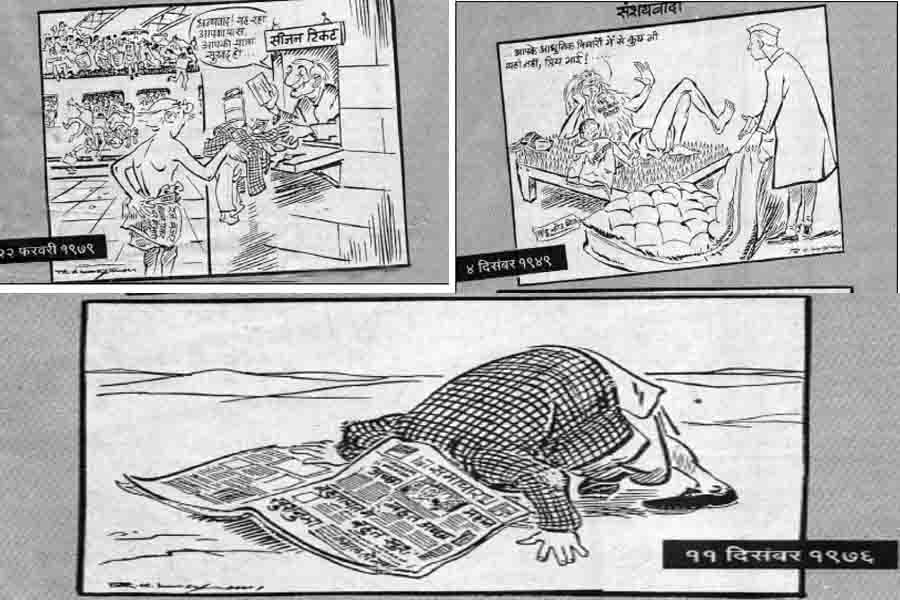ऑफिस से लौटकर आज भी वह पार्क के एक सुनसान कोने में अकेला आ बैठा। एक के बाद दूसरी सिगरेट फूँकता रहा। कभी खुद-ब-खुद धीरे से हंसकर अपने ‘जख्मों’ को सहलाता -सा लगता, तो कभी शून्य में निहार कर अपनी ही दुनिया में भटकता-सा। सम्भवत: तभी कुछ दूरी पर खेल रहे बच्चों का खेल उसे वर्तमान में न ला सका। न किसी युगल का हंस-हंस कर बातें करना ही।
‘‘आज भी यहां आ बैठे?’’ एक परिचित-सा स्वर उसके कानों से आ टकराता है। वह ऐसे चौंक पड़ता है, जैसे किसी ने उसे गहरी नींद में झक्झोर दिया हो। तभी उसकी भारी सूर्ख सी आँखें, सामने खड़े अपने पुराने एक लेखक मित्र की ओर उठती हैं। फिर पल-दो-पल बाद शरीर में तनाव बढ़ते ही झुक जाती हैं। और सिगरेट के धुएं में डूब जाती हैं।
‘‘जाना नहीं है?’’ लेखक मित्र का आत्मीयता भरा स्वर गूंजता है – ‘‘अभी तो किसी कर्जदार को भी तुम्हारे ट्रांसफर हो जाने का पता नहीं है।’’
वह कुछ नहीं बोलता। खामोशी से सिगरेट के लम्बे-लम्बे कश खींचने लगता है।
‘‘वास्तव में तुम पागल हो गए हो।’’ लेखक मित्र झुंझलाकर रवाना हो जाता है।
उसे सुकून मिलता है। एक लम्बे अर्से से एकान्त में मिलने वाला सुकून। काश! यदि सिगरेटों के बदलते ब्राण्डों की तरह उसके सोचने का ब्राण्ड भी बदल जाता, तो सुकून मिलने का उसका रास्ता भी बदल जाता, जिन्दगी का खाका पलट जाता। लेकिन न जाने कब से वह इस विषय पर सोचता ही नहीं। कुछ वर्षों से तो वह किसी भी विषय पर पूरी तरह सोच नहीं पाता। इसी वजह से अब उसके जीवन के किसी क्षेत्र का कार्य पूरा नहीं हो पाता। यहां तक कि बहुत दिनों तक मेहनत कर लिखी जा रही रचनाओं का कार्य भी नहीं।
उसने लिखा है। काफी लिखा व पढ़ा है। घर, रेस्टोरेन्ट, लाइब्रेरी, पार्क हर जगह बगल में पत्र-पत्रिकाओं व कागजों का पुलिन्दा दबाये हुए घंटों-घंटों बैठकर लिखा व पढ़ा है। परिणामस्वरूप डिग्रियां प्राप्त कर सका, न अच्छी नौकरी। फिर भी मॉडर्न ढंग से रहने का पूरा-पूरा प्रयत्न करता। मिलते-जुलने वालों पर दिल खोलकर खर्च करता। भले ही उसे कर्ज लेना पड़ता। कर्ज के बोझ से दबना पड़ता। इसके उपरांत भी वह चिन्ता नहीं करता। न आज की करता, न कल की। बस अपनी कलम पर विश्वास करता।
आखिर वह विकृत रात आ ही गयी, जब कुछ अर्से से आर्थिक संकट पर चली आ रही कटु वार्तालापों के बाद पत्नी उस पर गरजी – ‘‘ये लेखक-देखक बनने का चक्कर छोड़ दो।’’
‘‘क्या मतलब?’’ उसकी भी भौंहें तन गयीं।
‘‘हम भूखे नहीं मरना चाहते।’’ पत्नी के स्वर में एक भयंकर चीख थी।
‘‘तो केसे मरना चाहती हो?’’ वह क्रोध से कांपता हुआ बोला – ‘‘क्या मेरे अन्दर बैठे रचनाकार को पूरी तरह मारकर?’’
‘‘हां। हां।’’ पत्नी का क्रोध चरम सीमा को छू गया। परिणामस्वरूप अगले दिन पत्नी सीनों बच्चों को लेकर पिता के घर के लिए गाड़ी में चढ़ गयी।
उसे लगा जैसे एक भारी बोझ उसके सिर पर से हट गया। वह घर के सुनसान वातावरण में लिखने-पढ़ने लगा। लिखते-पढ़ते उसे प्रतीत हुआ कि वास्तव में उसके उल्लेख में शिथिलता का कारण उसका गृहस्थ जीवन था। अब वह पूर्ण रूप से आजाद है। जब मर्जी होगी तब लिखेगा, पढ़ेगा। यार-दोस्तों के साथ साहित्य पर खूब चर्चा करेगा, घूमेगा, फिरेगा, खायेगा-पियेगा। परन्तु जैसे-जैसे उसने अपनी इच्छाओं को नए ढंग से व तेजी से कार्य रूप में परिणित करना आरम्भ किया, वैसे -वैसे कर्ज का भूत उसके सिर पर अपने पंजों को मणबूती से गाड़ता गया। लेकिन वह एक दार्शनिक की तरह विचारों में डूबता गया। साधारण लोगों से नपीतुली बातें व बुद्धिजीवियों के सामने अपनी बात ऊंची रखने का प्रयत्न करने लगा। इससे मिलने-जुलने वाले लोग उससे क्रुद्ध हो गए। उससे दूर हटते गए। वह भी झुंझला उठा। क्रोध से भरता गया। एकान्तवासी हो गया। उसे विश्वास हो चला था कि एक दिन वह अपनी कलम की नोंक से अपने ऊपर पड़ा बाबूगीरी का चोला उतार फेंकेगा और प्रतिष्ठित व्यक्ति का चोला पहन लेगा। गिरने आर्थिक स्तर की होली जलाकर, ऊंचे स्तर की दीवाली मनाएगा।
लेकिन काफी कोशिशों के बावजूद भी इच्छा मुताबिक उसके दिन नहीं फिरे। हां, इच्छा के विरुद्ध शीघ्र ही वह दिन अवश्य आ गया, जब वह बहुत मेहनत से लिखी रचनाओं को भी साधारण पत्र-पत्रिकाओं में भेजने को मजबूर हो गया। अनुमान से बहुत कम पारिश्रमिक पाने लगा या बिलकुल न पा पाता। इतना ही नहीं उसका दो कमरों का मकान एक कोठरी में परिणित हो गया। हर माह मिलने वाला वेतन और शीघ्रता से झूठे-सच्चे कर्जदारों की झोलियों में, टुकड़े-टुकड़े होकर गिरने लगा। उसका बात-बात पर झुंझला जाना या क्रोधित हो जना आदम बन गयी। जिसके कारण उसकी चाय-सिगरेट की लत में बढ़ोत्तरी हो गयी। कभी-कभी ‘पैग’ भी लेने लगा वह।
एक दिन आया जब वह अपनी इन इच्छाओं की पूर्ति हेतु रोज कई किलोमीटर पैदल घूमता। नए-नए उधार गुहों का निर्माण करता। न ऑफिस की चिन्ता करता, न वहां के कार्य की। आखिर एक दिन सेक्शन इंचार्ज ने झुंझलाकर उसे टोक ही दिया – ‘‘क्यों जनाब कधिर मटरगस्ती करते रहते हो?… कई दिनों से देख रहा हूँ कि तुम अब ऑफिस के कार्य में तनिक भी रूचि नहीं लेते। तुम्हारे हक में यह ठीक नहीं होगा।’’
‘‘क्या ठीक है और क्या गलत है, मैं सब जानता हूँ।’’ वह उखड़ पड़ा – ‘‘कौन करता है यहाँ काम? सब एक-दूसरे को मूर्ख बनाने में लगे रहते हैं…’’
सेक्शन इंचार्ज तिलमिला गया। पर बोला कुछ नहीं। यह बोलता गया – ‘‘नहीं तो मैंने जितना कार्य इस सेक्शन का इंचार्ज रह कर एक वर्ष में किया, उतना आप दो वर्ष में भी क्यों न कर सके? सिर्फ इसलिए कि आप डिग्रियों के आधार पर इस कुर्सी पर ऊंचा पद लेकर बैठे हो, जबकि में डिग्रियां ना लेने के कारण साधारण पद लेकर बैठा था?’’
‘‘क्यों फालतू बक-बक कर रहे हो।’’ सेक्शन इंचार्ज गरजा – ‘‘अपनी औकात देखो।’’
यह सुनते ही क्रोध से उसका शरीर काँपने लगा। दांत पीसते हुए गालों की हड्डियां तनने लगीं। आँखों से ज्वाला फूटने लगी। लगा जैसे वह कुछ तोड़ देगा, फोड़ देगा।
सेक्शन इंचार्ज लौट गया। पर वह सिगरेट के धुएं व कड़क चाय में उमड़ते क्रोध को घोलने लगा।
उसके कुछ माह ऐसे ही गुजरे। उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। पर समय अपनी परिवर्तन शीलता के क्रम को न तोड़ सका। अचानक हैड ऑफिस में किसी को मजबूरन लाने के कारण डाईरेक्टर ने उसका तबादला, सेक्शन इंचाई की शिकायतों को आधार बनाकर, एक ब्रांच ऑफिस में कर दिया। कर्ज के बोझ से बुरी तरह दब जाने के कारण वह सबसे नजदीकी मित्र के पास गया। विश्वास भरे स्वर में बोला – ‘‘फुर्ती से कुछ रूपये निकालो दोस्त, आज ही गाड़ी चढ़ जाना चाहता हूं।’’
‘‘रूपये।’’ विश्वासी मित्र आश्चर्य भरे स्वर में बोला – ‘‘इस जमाने में हम जैसों के पास रूपया कहां?’’
‘‘सदा रहे हैं।’’ वह विश्वास भरे स्वर में बोला – ‘‘यदा-कदा दिए भी हैं। आखिर मुझसे अच्छा वेतन पाते हो। अनुवाद से भी खूब कमाते हो। और… खैर छोड़ो इन बातों को। फुर्ती से कम से कम साठ-सत्तर रुपये तो दे ही दो। मैं पैसे मिलते ही सबसे पहले तुम्हें भेज दूंगा।’’
उत्तर में विश्वासी मित्र ने ‘‘साँरी’’ कह कर अपनत्व भाव प्रकट कर उसे एक सिगरेट पेश कर विदा कर दिया। वह भी मन में एक और टूटन व ऐंठन लिये हुए, बहुत जरूरी सामान लेकर, चुपचाप शहर के सब स्टेशन से गाड़ी चढ़ गया। ऐसे ही दो-तीन बार चढ़ता रहा। एक बार फिर जब हैड ऑफिस आने के लिए गाड़ी चढ़ाया गया, तो वह टूट चुका था, रोगों से घिर गया था। मौंखिक दया का पात्र बन गया था। फिर भी किसी के पूछने पर कि इन दिनों क्यों नहीं लिखते-पढ़ते? वह दावे से कहता – ‘‘अब जब भी लिखूँगा अद्वितीय रचना का निर्माण करूंगा। पढूँगा तो अद्वितीय रचना पढूृँगा।’’ जबकि उसकी बगल से पत्र-पत्रिकाओं व कागजों का पुलिन्दा न जाने कब कहां गिर चुका था।
इस कारण साधारण व्यक्ति तक को उसका ऑफिस आकर अपनी सीट पर दोनों हाथों के बीच सिर छुपाए खामोश बैठे रहना या बाहर बगीचे व कैन्टीन के एक कोने में सिगरेट पर सिगरेट फँूकते रहना, पागलपन के अलावा कुछ नहीं लगा। फिर भी वह अपने विचारों का ताना-बाना बुनता रहता। भले ही उसके जीवन में कोई चटक रंग न रहा, भीतर दूर-दूर तक सख्त अँधेरा फैलता रहा।
करे भी तो क्या करे वह? वह किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुँच पाता। बस दिनभर चाय, सिगरेट व बिस्कुटों के बूते पर जिन्दगी को मंजिल तक खींच ले जाना ही, जैसे उसका विश्वास बन चुका है। भले ही अब उसका शरीर काला पड़ गया है, गालों की हड्डियां बाहर निकल आई हैं, जवानी में बूढ़ा लगने लगा है, जिन्दगी बनाने के लिए बुने ताने-बाने मौत का पैगाम लेकर देहरी पर आ खड़े हुए हैं।
आश्चर्य नहीं कि सिगरेट की तरह जल रहा उसका जिस्म एक दिन उसकी तरह ही बुझ जाएगा। वह राख का ढ़ेर होकर रह जाएगा। तब भी अब से कुछ देर पूर्व जबकि डाईरेक्टर ने दया कर उसका तबादला, बीबी-बच्चों के समीप स्थित विभाग के एक ब्रांच ऑफिस में कर दिया है, फिर भी वह पार्क में आ बैठा। … पता नहीं कब तक बैठा रहेगा।… तब तक ऐसे क्षणों का सिलसिला बनाए रखेगा? कब तक अपने को झूठी तसल्ली देता रहेगा?… कब तक?