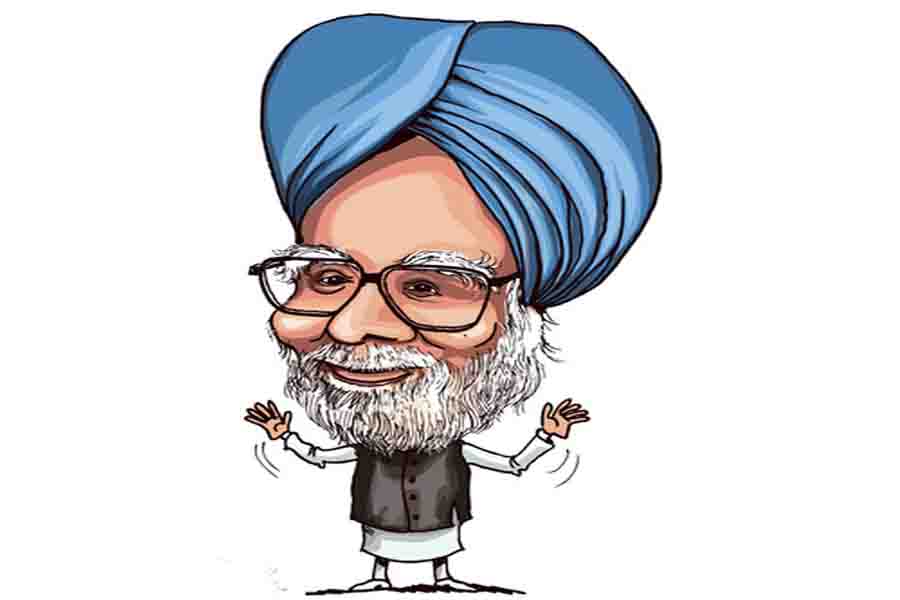कुम्भ हमारे देश का एक अति प्रसिद्ध पर्व है। बारह वर्षों के भीतर यह भारतवर्ष के चार परम् पवित्र स्थानों में से एक-एक स्थान पर आता है। और इसी प्रकार छठें वर्ष के अवसर पर अर्धकुम्भ पर्व मनाने की प्रथा भी परम् प्राचीन काल से चली आ रही है। यह चारों पवित्र स्थान हैं- प्रयाग (उ.प्र.), हरिद्वार (उत्तराखंड), नासिक (महाराष्ट्र) और उज्जैन (म.प्र.)। इनमें से दो स्थानों का पर्व कुछ अति प्रसिद्ध है, प्रयाग और हरिद्वार का। यहां प्रत्येक बारह वर्ष पर कुम्भ और कुम्भ के छठें वर्ष पर अर्धकुम्भ लगता है। कुम्भ पर्व के सुप्रसिद्ध ये चारों स्थान भारतवर्ष के प्राचीन तीर्थस्थल हैं और इनकी प्राचीन ऐतिहासिक स्थिति भी है।
इन पवित्र तीर्थ स्थलों पर यों तो प्रतिवर्ष अथवा प्रतिदिन स्नान-दान, कथा-कीर्तन, भजन-पूजन और यज्ञादि करने का महत्त्व हिन्दू धर्मशास्त्रों में बताया गया है, किन्तु अर्धकुम्भ और कुम्भ के अवसर पर तो इनकी महिमा बहुत बढ़ जाती है और उस समय समूचे देश के लाखों व्यक्ति एकत्र होते हैं। इस विशाल देश का कोई अंचल उस समय ऐसा नहीं रह जाता, जहां के लोग यहां न आते हों। यही नहीं, उस अवसर पर तो नेपाल, अफगानिस्तान, वर्मा, इण्डोनेशिया, श्रीलंका, मारीशस आदि सुदूर विदेशों के हिन्दू भी यहां एकत्र होते हैं और बड़ी श्रद्धा, भक्ति-भावना और प्रेम से स्नान-दान कर अपने जन्म को सफल मानते हैं और बड़ी ऊंची निष्ठा और प्रेरणा लेकर अपने-अपने घरों को वापस जाते हैं। बहुत प्राचीन काल से इन तीर्थों की यह परम्परा हमारे महान् देश की सांस्कृतिक एवं राजनैतिक एकता को पुष्टि प्रदान करती रही है और उसी का यह परिणाम है कि अनेक भाषा, वेशभूषा, रीतिनीतिक एवं भौगोलिक व्यवधानों के होते हुए भी हम न केवल संस्कारों एवं जीवनचर्या के क्रमों में ही एक हैं वरन् सहस्रों वर्षों की बाधक परिस्थितियों के विपरीत हमारे विचारों, भावनाओं, मतों और आदर्शों में भी अद्भुत एकता है।
छह अथवा बारह वर्षों पर लगने वाले इन धार्मिक पर्वों पर दूर-दूर प्रदेशों से आ-आकर एकत्र होने पर कुछ दिनों अथवा क्षणों के लिए ही सही हम अपने आपको भूल जाते हैं और इस महान राष्ट्र के विभिन्न अंचलों में निवास करने वालों को अपना भाई समझकर जनसंपर्क में आ जाते हैं। चिरन्तन काल से चले आने वाले इस संपर्क का ही यह सुपरिणाम है कि हिमालय की चोटियों पर बसने वालों से लेकर रामेश्वरम् के समीपवर्ती लोगों तक और द्वारिकापुरी के निवासियों से लेकर गंगासागर के मुहाने तक समूची हिन्दू जाति की समस्त ऐहिक और पारलौकिक मान्यताएं एक-सी हैं और उनके देवी-देवता और आराधना की पद्धति एक-सी है। भारत के चारों धाम इसीलिए एक-दूसरे से उतने ही दूर हैं कि किसी भी धर्मिक व्यक्ति को एक बार विराट् भारत के दर्शन हो जायें। इसी प्रकार अर्धकुम्भ अथवा कुम्भ पर्व के लिए महत्त्वपूर्ण ये चारों तीर्थ स्थल भी एक-दूसरे से पर्याप्त दूर हैं जहां छह अथवा बारह वर्षों पर विराट् मेले लगते हैं।
कुम्भ पर्व की पुराणों तथा धर्मशास्त्रों में बड़ी महिमा है। विशेषकर प्रयाग में उसकी महिमा इसलिए भी अत्यधिक हो जाती है कि वह हमारे देश के सभी तीर्थों का राजा है। लोक पावनी गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के इस पावन संगम स्थल की वेदों के काल से ही अपार महिमा गायी गई है और उसके इस कुम्भ पर्व की भी वेदों में चर्चा है, जिससे यह अनुमान होता है कि उस समय भी कुम्भ पर्व का प्रचलन था और देश के कोने-कोने से लोग यहां आते हैं। ऋग्वेद के दो मंत्रों में कुम्भ की चर्चा इस प्रकार की गयी है-
जघान वृत्रं स्वघितिवनैंव रूरोज पुरो अरदन्न सिन्थून।
विभेद गिरिं वनिन्नकुम्भ मागा तन्दो अकृणुतास्वयुग्मि:॥
तथा
कुम्भीवर्थो मा व्यषिष्ठा यज्ञाायुवेरज्यनतिषिक्ता।
अर्थात् कुम्भ पर्व में तीर्थयात्रा करने वाला मनुष्य स्वयं अपने फल रूप से प्राप्त होने वाले सत्कर्मों दान-यज्ञादि से, काष्ठ काटने वाले कुल्हाड़े की तरह अपने पापों का विनाश करता है। जिस प्रकार नदियां अपने तटों को नष्ट करती हुई प्रवाहित होती है। उसी प्रकार कुम्भ पर्व पर अपने पूर्वजन्मार्जित सत्कर्मों से मनुष्य अपने शारीरिक पापों को नष्ट करता है।
वेदों के परवर्ती साहित्य में तो प्रयाग और उसके कुम्भ पर्व की अत्यधिक चर्चा मिलती है। हिन्दुओं के धर्म ग्रन्थ के अतिरिक्त अन्य महाबलियों के ग्रंथों से भी इस बात के प्रमाण मिलते हैं कि कुम्भ का यह महान् मेला इस पुण्य स्थान पर अनेक वर्षों से इसी प्रकार लगता चला आ रहा है। यहां आकर बड़े-बड़े राजा-महाराजा अपना सर्वस्व दान कर अपने जीवन को सफल मानते थे। ऋषियों-मुनियों और साधु-सन्तों का भी यहां बराबर चलते ही रहते थे, जैसा कि इसके नाम प्रयाग से स्पष्ट मालूम पड़ता है। महर्षि भरद्वाज के स्थायी आश्रम होने के कारण कुम्भ अथवा मकर पर्व में एक महीने तक यहां देश के कोने-कोने से आकर ऋषि-महर्षि एकत्र होते थे और पारम्परिक विचार-विनिमय, शास्त्रचिंतन एवं अध्यात्म चर्चा के साथ-साथ संसार की ऐहलौकिक समस्याओं का भी वे लोग समाधान करते थे।
 कुम्भ एक राशि का नाम है। प्राय: माघ के महीने में सूर्य कुम्भ राशि पर आता है। सूर्य मकर संक्रान्ति पर प्राय: 14 जनवरी और कुम्भ राशि पर प्राय: 13 या 14 फरवरी को आता है, इन्हीं दोनों राशियों के मध्य में प्रयाग का मेला लगता है। प्रयाग के कुम्भ का यह योग प्रत्येक बारहवें वर्ष पर आता है। बहुत प्राचीन काल से यह मेला हमारे देश में प्रचलित है। इसी परम्परा का पता हवेनसांग के जिस वर्णन से लगता है उससे यह भी ज्ञात होता है कि प्रत्येक छठें वर्ष पर भी आज के अर्धकुम्भ जैसा मेला लगता था और उसमें भी लोग स्नान-दान करते थे। महाराज हर्षवर्धन के सम्बन्ध में यह उल्लेख है कि उन्होंने अपने पूर्वजों का अनुसरण करते हुए पांच वर्ष का संचित धन एक दिन में बांट दिया और उनके पुराने वस्त्रों के सिवा कुछ भी नहीं शेष रहा।
कुम्भ एक राशि का नाम है। प्राय: माघ के महीने में सूर्य कुम्भ राशि पर आता है। सूर्य मकर संक्रान्ति पर प्राय: 14 जनवरी और कुम्भ राशि पर प्राय: 13 या 14 फरवरी को आता है, इन्हीं दोनों राशियों के मध्य में प्रयाग का मेला लगता है। प्रयाग के कुम्भ का यह योग प्रत्येक बारहवें वर्ष पर आता है। बहुत प्राचीन काल से यह मेला हमारे देश में प्रचलित है। इसी परम्परा का पता हवेनसांग के जिस वर्णन से लगता है उससे यह भी ज्ञात होता है कि प्रत्येक छठें वर्ष पर भी आज के अर्धकुम्भ जैसा मेला लगता था और उसमें भी लोग स्नान-दान करते थे। महाराज हर्षवर्धन के सम्बन्ध में यह उल्लेख है कि उन्होंने अपने पूर्वजों का अनुसरण करते हुए पांच वर्ष का संचित धन एक दिन में बांट दिया और उनके पुराने वस्त्रों के सिवा कुछ भी नहीं शेष रहा।
पुराणों में कुम्भ पर्व के सम्बन्ध में जो कथा दी गयी है, वह बड़ी ही विचित्र है। उसका संक्षेप कुछ इस प्रकार है।
पृथ्वी पर एक बार देवताओं और असुरों में बड़ी मैत्री भावना थी। परस्पर की यह मैत्री जब कुछ दिनों चलती रही, तो दोनों जातियों के प्रमुखों ने एक बार आपस में मिलकर यह तय किया कि समुद्र को मथकर उसके रत्नों को निकालना चाहिए। रत्न ही नहीं, समुद्र में वह अमृत भी छिपा हुआ है, जिसे पीकर लोग अजर-अमर हो जाते हैं। बस निश्चय की देर थी। समुद्र-मंथन की जबरदस्त तैयारी की गयी। देवताओं और असुरों में पराक्रम की कमी तो थी नहीं। इस पारस्परिक सुमति से उनके उत्साह में वृद्धि हो गयी थी। समुद्र-मंथन की युक्तियां सोची गयीं और तत्काल कार्य आरम्भ हो गया। समुद्रतटवर्ती मन्दराचल को उपारकर मथानी बनाया गया, सर्पों के राजा वासुकि को रस्सी के रूप में प्रयुक्त किया गया। पूंछ की ओर देवता लोग, फणों की ओर असुर। समुद्र-मंथन आरम्भ हो गया। भयंकर मंथन हुआ और भयंकर मंथन के शब्दों से त्रैलोक्य कांप गया। बेचारे समुद्र की दुर्गति का कोई ठिकाना नहीं था। उसके भीतर रहने वाले सभी जीव-जन्तु विह्वल हो गये। हाहाकार मच गया। अन्तत: समुद्र शरणागत हुआ, अपनी समस्त मूल्यवान् निधियों के संग, वह अमृत का कलश लेकर जलराशि से बाहर निकला, तो दिशाएं प्रसन्न हो गयीं। अमृत कलश की चतुर्दिक बिखरी हुई सुगन्ध से देवताओं और असुरों की मूर्च्छित चेतना प्रफुल्लित हो उठी। उनके श्रमसीकर सूख गये। अमृत कलश के साथ उन्हें अन्यान्य रत्न भी प्राप्त हुए।
किन्तु जब अमृत के बंटवारे का प्रश्न सामने आया तो दोनों जातियों की प्रसुप्त वैराग्नि भीतर से धधक उठी। देवताओं के अधीश्वर इन्द्र के पुत्र जयन्त ने बड़ी त्वरा से अमृत कलश ले लिया और पूर्व दिशा की ओर भाग चले। असुर भी असावधान नहीं थे। उन्होंने पवन गति से जयन्त का पीछा किया। फिर क्या था, बारह दिनों तक भीषण युद्ध देवताओं और असुरों में निरन्तर चलता रहा। देवताओं का बारह दिन मनुष्यों का बारह वर्ष होता है। इन बारह दिनों में चार स्थानों पर चार बार दैत्यों ने जयन्त को पकड़कर अमृत कलश छीनने का प्रयास किया, किन्तु देवताओं के संयुक्त मोर्चे के कारण उन्हें विफलता ही हाथ लगी। किन्तु इस छीना-झपटी में अमृत की बहुतेरी बूंदें कलश से छलककर नीचे गिर पड़ीं। ये चारों स्थान यही थे-प्रयाग, हरिद्वार, नासिक और अवन्तिका (उज्जैन) जयन्त के हाथों से कलश की रक्षा में सूर्य, बृहस्पति और चन्द्रमा ने बड़ी सहायता की थी, फलत: जब ये तीनों ग्रह एक राशि पर एकत्र होते हैं तब इन स्थानों पर कुम्भ पर्व लगता है। धार्मिक जनता का विश्वास है कि इस अवसर पर इन स्थानों में स्नान-दान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। कलश को ही कुम्भ भी कहते हैं, अत: इस पर्व की प्रसिद्धि कुम्भ नाम से हुई है।
कुछ लोगों का मत है कि इस पर्व की आदिम प्रतिष्ठा का श्रेय आद्य जगद्गुरु श्री शंकराचार्य को है। भारत के चारों कोनों में स्थित अपने चारों आश्रमों की भांति देश के विभिन्न अंचलों में उन्होंने इन चार पर्वों पर कुम्भ की भी प्रतिष्ठा की थी। उनका उद्देश्य यही था कि इसी बहाने देश के कोने-कोने से लोग आ-आकर यहां एकत्र हुआ करें और कुछ दिनों के लिए ही सही अपने को छल-छिद्र एवं राग-द्वेष से रहित बनाकर परमार्थ एवं परलोक की भी चिन्ता करें और साथ ही इस विशाल देश की अखण्डता और एकात्मता का भी अनुभव करें।