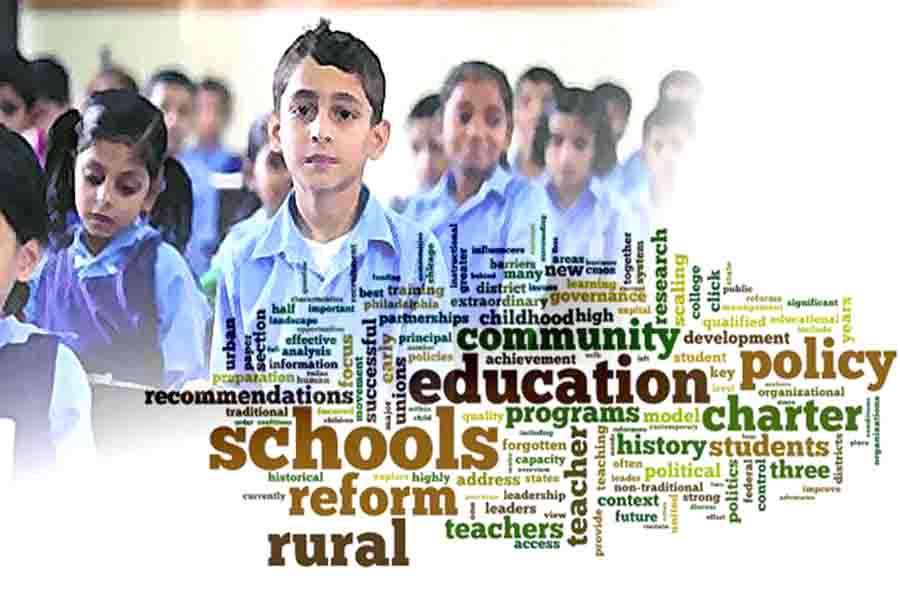प्रस्तावित राष्ट्रीय शिक्षा नीति नए भारत के निर्माण की कार्ययोजना का प्रभावी प्रारूप है …देश में शिक्षा की व्यवस्था संभालने वाली सभी संस्थाएं अपनी स्वायत्ता को क़ायम रखते हुए नई शिक्षा प्रणाली को लागू कर हम सबके सपनों के भारत को साकार कर सकती हैं।
मानव समाज की विशेषता है कि वह अपने भविष्य की कल्पना कर सकता है और उस संकल्पित भविष्य को साकार करने के लिए पुरूषार्थ करने की भी उसे प्रकृति ने शारीरिक, मानसिक व बौद्धिक क्षमताएं प्रदान की हैं। जो राष्ट्र अपनी नियति स्वयं निर्धारित कर सकता है वही तो स्वतंत्र है। हमारे मन में क्या है, कल का भारत कैसा होगा? या फिर कल का भारत कैसा बनाना है? ये सब हम यदि नियति पर छोड़ देते हैं तो यह पशुवत व्यवहार माना जाएगा। जो होगा सो देखा जाएगा। इस स्थिति में तो अन्य अधिक सक्षम देश ही हमारे भविष्य को बनाने में लग सकते हैं, शायद लगे भी हैं।
एक हजार से अधिक वर्षों तक विदेशी सत्ताओं ने हमारी नियति निर्धारण का प्रयास किया। भारत के मूल स्वरूप को बदलने का, इसके चित्त को अपने अनुसार ढालने के अनेक प्रयास हुए। साम, दाम, दण्ड, भेद आदि सभी हथकण्डे अपनाए। पर उन्हें केवल आंशिक सफलता ही मिली। सौभाग्य था कि हमारे समाज में हजारों वर्षों से ऋषि-मुनियों ने ऐसे सुदृढ़ संस्कारों की नींव रखी थी कि भारतीय समाज का अधिकांश भाग अपनी आस्थाओं और जीवन मूल्यों को सुरक्षित रखने में सफल हुआ।
स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् परकीय प्रयासों को निरस्त होना चाहिए था, परंतु दुर्भाग्य कि ऐसा नहीं हुआ। भारत के भविष्य की योजना वे लोग बनाने लगे जो प्राचीन भारतीय संस्कृति व ज्ञान-सम्पदा के प्रति श्रद्धा नहीं रखते थे। ऐसा वर्ग सत्ता में बारम्बार आया जो अपने देश को ‘इंडिया’ के नाम से जानता था, भारतीयता के नाम से ही उसके मन में हीनता उत्पन्न होती थी। उनके सपनों का भारत कभी ब्रिटेन की कार्बन-कापी, कभी रूस की प्रतिलिपि और फिर अमेरिकी समाज के अनुरूप भारतीय समाज को ढालने का था। जब वैश्विक संस्थाओं ने भारत सहित कुछ देशों को ‘तीसरे विश्व’ की पहचान दी तो हमारे देश के बड़े बुद्धिजीवियों ने इसका विरोध नहीं किया उल्टा स्वयं भी इस अपमानजनक शब्दावली का जमकर प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया।
परिणाम यह निकला कि अपना देश भारत तो बन ही नहीं पाया परंतु किसी अन्य समाज का पूर्ण अनुसरण करने में भी हमें सफलता नहीं मिली। हम दयानंद, विवेकानंद, अरविंद, गोखले, हेडगेवार, गांधी, नेहरू, पटेल, दीनदयाल किसी का भी भारत बनाने में असफल रहे हैं। इक्कीसवीं शताब्दी के आगमन पर टेक्नॉलाजी के माध्यम से युग परिवर्तन सा कुछ हुआ है। इंटरनेट, कम्प्यूटर और उपग्रह प्रौद्योगिकियों के संदर्भ में आज हमारा समाज फिर से नए भारत की संकल्पनाएं बनाता दिख रहा है। पहले योजना आयोग भविष्य की योजनाएं बनाता था जिसमें उन लोगों का बोलबाला था जो पश्चिम के अनुसरण को ही विकास मानते थे। नीति आयोग ने भारत को नई दृष्टि से देखना प्रारंभ किया है। नीति आयोग का प्रयास राष्ट्र के पुन:निर्माण का न होकर पुनरुत्थान का लगता है। दोनों में अंतर मूलत: विश्वास, धारणा और आस्था का है। नीति आयोग न तो पाश्चात्यकरण को और न ही देशानुकूल आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को भारत का विकास मानता है। इसके अनुसार विकास का आधार भारतीय प्राचीनता का युगानुकूल प्रकटीकरण ही भविष्य के भारत की संकल्पना है।
भविष्य में भारत की संकल्पना कौन करेगा? योजना कौन बनाएगा? क्रियान्वयन कौन करेगा? संसाधन कौन जुटाएगा? ये सब प्रश्न इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि सब कुछ निर्भर करेगा विकास की प्रक्रिया के दायित्ववान वर्ग के संस्कारों, धारणाओं एवं आस्थाओं पर, उनके वैचारिक अधिष्ठानों पर। हम सब जानते हैं कि मुख्यत: शिक्षा ही व्यक्ति के संस्कारों, धारणाओं व वैचारिक अधिष्ठानों के निर्माण का कार्य सम्पन्न करती है। अन्य शब्दों में, प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से भारत की शिक्षा नीति ही तय करेगी कि भविष्य का भारत कैसा होगा।
पिछले पांच वर्षों से सम्पूर्ण भारतीय समाज में शिक्षा नीति के विषय में अत्यंत विस्तृत विमर्श हुआ है। केन्द्रीय मानव संसाधन मंत्रालय के अनुसार ग्राम पंचायत से लेकर राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक लाख से अधिक विमर्शों की जानकारी संग्रहित की गई है। इन पांच वर्षों में विमर्श केवल शासकीय स्तर पर शासन द्वारा प्रायोजित हों ऐसा नहीं है। महाविद्यालय व विश्वविद्यालय स्तर पर भी सैंकड़ों सेमिनार और कार्यशालाएं हुई हैं। अनेक स्वयंसेवी संस्थाओं ने भी इस विमर्श में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। भारतीय शिक्षण मण्डल, संस्कृति उत्थान न्यास, पंचनद शोध संस्थान व पुनरुत्थान विद्या पीठ की इस संदर्भ में पारस्परिक विमर्श को योजनाबद्ध ढंग से परिणामकारी उपलब्धियां तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही है।
लोकसभा चुनाव 2019 से पूर्व मानव संसाधन मंत्रालय को सौंपी कस्तूरीरंगन समिति की रिपोर्ट में इन संस्थानों का योगदान भी रहा है, हालांकि कुछ मामलों में मतभेद अभी भी बने हुए हैं। यह भी उल्लेखनीय है कि केन्द्र की नई सरकार ने आते ही इस रिपोर्ट का संज्ञान लिया और इसे जनमानस मे विचार और सुझावों के लिए जारी किया। पहले 30 जून तक सुझाव देने की अंतिम तिथि थी, जो बाद में 31 जुलाई तक बढ़ा दी गई। वैसे तो कस्तूरीरंगन रिपोर्ट बहुत विस्तृत है फिर भी रिपोर्ट की उन महत्वपूर्ण अनुशंसाओं की चर्चा यहां प्रासंगिक लगती है जिनका सीधा-सीधा सम्बंध कल के भारत से है।
1. मंत्रालय का नामकरण: सबसे महत्वपूर्ण सुझाव कस्तूरीरंगन रिपोर्ट में है केन्द्र सरकार के मंत्रालये के नाम बदलने का। वर्तमान मे जो मंत्रालय देश की शिक्षा के विषयों का प्रबंधन करता है उसका नाम ‘मानव संसाधन विकास मंत्रालय’ है। आभास यह होता है कि मनुष्य धन, संपत्ति, खनिजों की तरह ही एक रिसोर्स है, संसाधन है और देश के हित में इसे प्रयोग करने की व्यवस्था बनाने का कार्य इस मंत्रालय का है। जैसे पशुधन का विकास करना, वैसे ही मनुष्य धन का भी। जैसे खनिजों को अधिकाधिक देशहित में प्रयोग करना वैसे ही अपने देश के बच्चों को इस प्रकार शिक्षित करना जिससे वे बढ़े होकर समाज के लिए लाभकारी संसाधन सिद्ध हों। 26 दिसम्बर 1985 से पूर्व इस मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय था। उस समय की सरकार को लगा कि मनुष्य को संसाधन मान कर उसका विकास करेंगे अर्थात शिक्षित करेंगे तो देश का भला होगा। सर्वविदित है कि साम्यवादी विचार में मनुष्य एक राजनैतिक प्राणी है जिसका अस्तित्व सामूहिकता में ही है। पूंजीवादी सोच में मनुष्य उपभोक्ता है जिसका होना उत्पादों के प्रयोग के लिए अनिवार्य है। यदि पूंजी का विकास होना है तो उत्पादों की विभिन्नता व उनका अधिकाधिक प्रयोग अनिवार्य है। यहां भी व्यक्ति के स्वत्व की पहचान नहीं है। एक तीसरा पक्ष यह है कि मनुष्य जीवन पशु जीवन से इस प्रकार से भिन्न है कि मानव को प्रकृति ने स्व के विकास की संभावनाएं प्रदान की हैं। सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक जीवन में सामूहिकता और पारस्परिक निर्भरता निभाता हुआ भी उसे अपने आप को समझने और मानव के विकसित रूप को प्राप्त करने के लिए सक्षम बनाना है। समाज की शिक्षा व्यवस्था ऐसी हो कि बच्चों, किशोरों व युवाओं को आवश्यक ज्ञान प्राप्त हो और वे परिस्थितियों के अनुसार जीविका उपार्जन के लिए योग्य बनें परंतु जीवन जीने की कला व विज्ञान भी उनको शिक्षा संस्थानों में दिया जाए। इसलिए कस्तूरीरंगन समिति की यह अनुशंसा कि मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय हो वैचारिक दृष्टि से परिपक्व एवं व्यवहारिक है, इसलिए सराहनीय भी है।
2. भाषा का प्रश्न: दो विषय हैं। एक, शिक्षा का माध्यम क्या हो और दूसरा, भविष्य के भारतीय नागरिक को कौन-कौन सी भाषाएं आनी चाहिए। हमने दोनों विषयों का वर्षों तक ऐसा घालमेल किया है कि भाषा का विषय भारतीय समाज के लिए नासूर बन चुका है। जैसे ही इस विषय को किसी भी रूप में उठाते हैं तो चारों ओर घमासान मच जाता है। यहां तक कि देश के विघटन की धमकियां प्रारंभ हो जाती हैं।
शिक्षा मुख्यत: कुछ सीखने का कार्य है। बच्चा पहले बोलना व सुनना सीखता है जिसकी भाषा वह होती है जो मां, पिता, भाई व बहन बोलते हैं। यह मां-भाषा है, जिसको सिखाने की आवश्यकता नहीं होती। स्वयं सहज भाव से निपुणता प्राप्त हो जाती है। जीवन जीने का प्रारंभिक ज्ञान भी बिना सिखाए, बिना पढ़ाए-लिखाए मां-भाषा में ही प्राप्त होता है। स्वाभाविक है कि कुछ भी सीखना हो तो मां-भाषा में सीखना सबसे सहज और सरल है। परंतु यहां दो समस्याएं सामने आती हैं। पहली यह कि मां-भाषा में उस ज्ञान-विज्ञान के ग्रंथ नहीं होते जो बच्चों को जानना व सीखना होता है। इसलिए एक भाषा जानना ज़रूरी है जिसमें ज्ञान उपलब्ध हो। सामान्यतः क्षेत्रीय भाषाओं में कक्षा बारहवीं तक की पुस्तकें आसानी से आज भी प्रचुर मात्रा मे उपलब्ध हैं। यह भी तथ्य है कि अधिकतर मां-बोलियां क्षेत्रीय भाषाओं से मेल खाती हैं। मां-बोली से अपनी क्षेत्रीय भाषा सीखने का कार्य सहज, सरल व स्वभाविक ही है। बच्चे के मस्तिष्क पर बिलकुलअपरिचित भाषा सीखने का दबाब या तनाव नहीं रहता। अपनी ही मां-बोली जैसी भाषा को लिखना-पढ़ना बच्चे के लिए अन्य ज्ञान प्राप्त करने का साधन बन जाता है। देश की अधिकांश जनसंख्या को अपना जीवन चलाने और आजीविका कमाने के लिए इतना ही पर्याप्त होता है। साधारण समझदारी है, प्रयोगात्मक प्रमाण भी है और अनुभव आधारित विवेक भी कि अपनी भाषा में सोचना व विश्लेषण करना सर्वाधिक सृजनात्मक व नवाचारों को उत्पन्न करने वाला होता है।
पूर्व राष्ट्रपति व मिसाइलमैन की ख्याति प्राप्त कलाम जी का यही मानना था कि आयु के शुरू में सीखी हुई भाषा में मस्तिष्क अधिकतम परिणाम का कार्य करता है। मंगलयान के कार्य को सम्पन्न करने वाली टीम के मुखिया ने एक साक्षात्कार में कहा कि वे अभी भी अपनी बचपन की ही भाषा में सोचते हैं। प्रश्न यह होना चाहिए कि जिस भाषा की जीवन में उपयोगिता नहीं है, नियम बनाकर उसे ज़बरदस्ती बच्चे पर क्यों थोपा जाए।
यहां यह कहना भी प्रासंगिक होगा कि यदि उच्च शिक्षा के लिए कोई अन्य भाषा सीखना अनिवार्य हो तो उसे सीखा जा सकता है। आज भी जो भारतीय विदेशों में पढ़ाई, शोध या नौकरी के लिए जाते हैं वे आवश्यकतानुसार रूसी, जर्मन, जापानी, कोरियन, स्पैनिश भाषा सीख ही लेते हैं। यदि उच्च शिक्षा अंग्रेज़ी में लेनी है तो अंग्रेज़ी सीख लें, पर जिनको जीवन में अंग्रेज़ी की आवश्यकता ही नहीं वह क्यों सीखें। मान लीजिए एक कुशल प्लम्बर, वाहन मैकेनिक या दुकानदार अपने गृह राज्य में ही काम कर रहा है तो उसको विदेशी भाषा सीखने का बड़ा लाभ नहीं होने वाला। एम.बी. ए. और एम. बी. बी. एस. किए हुए व्यक्तियों की पढ़ाई अंग्रेजी में होती है, परंतु कार्य करते हुए उन्हें डीलर या मरीज की बोली में ही बात करने से सफलता मिलती है।
अब बात आती है कि भविष्य के भारत का नागरिक कौन सी भाषा बोले।स्पष्ट है कि स्थानीय वातावरण में सफल होने के लिए उसे मां-भाषा व मां-भाषा से मिलती-जुलती क्षेत्रीय भाषा उसको बोलना, पढ़ना व लिखना आना ही चाहिए। क्षेत्रीय संस्कृति से सकारात्मक सम्बंध भी बनेगा और उसको समृद्ध करने में भी योगदान होगा। परंतु हम भविष्य का भारत ऐसा भी चाहते हैं जिसमें हर देशवासी हर अन्य देशवासी से खुलकर बात कर सके। देश को एक व एकात्म बनाने के लिए एक ऐसी भाषा तो चाहिए ही जो सबको व सर्वत्र स्वीकार्य हो। शासन-प्रशासन, उद्योग-व्यापार, मीडिया-साहित्य, पर्यटन-तीर्थाटन सबके लिए सम्पर्क भाषा तो चाहिए ही।
दुर्भाग्य यह है कि इस महत्वपूर्ण बौद्धिक विषय का राजनीति ने अपहरण कर लिया और ऐसा मुद्दा बना दिया जो वर्षों तक सुलझने में नहीं आया। विषय बौद्धिक है, हल भी बुद्धि से ही निकालना होगा। राजनीतिज्ञों को स्वीकार करवाना होगा। कस्तूरीरंगन समिति ने भी इस विषय पर बात की है परंतु उसने पुराने तीन भाषा सीखने के ही सूत्र को आगे बढ़ा दिया। जो फ़ार्मूला 1956 में प्रारंभ हुआ और समय-समय पर जिसको प्रशासनिक समर्थन भी प्राप्त हुआ। बार-बार जो फार्मूला असफल रहा उसे एक बार फिर से देश पर थोपना उचित नहीं है। शिक्षा की भाषा मातृभाषा व आवश्यकता पढने पर कोई दूसरी भाषा सीखने की मानसिकता सहज उपाय है। साथ ही बौद्धिक जगत सम्पर्क भाषा के विषय को सुलझाए। चीन ने मन्दारिन को समग्रता देकर उसे अपने देश की शिक्षा की भाषा 1920 में बनाई। हमारी सभी भाषाएं अंग्रेज़ी की अपेक्षा कहीं अधिक वैज्ञानिक और समृद्ध हैं। सबको मिलाकर एक नई भाषा बन सकती है जो शब्द और व्याकरण सभी भारतीय भाषाओं से ले और मूल रूप से संस्कृत का अनुसरण करे। हमारे आई. टी. विशेषज्ञ ऐसी भाषाएं बनाने में दक्ष हैं जो मशीनें समझ लेती हैं। क्या हम भविष्य के भारत के लिए एक नई भारतीय भाषा नहीं बना सकते। एक आधुनिक पाणिनी की आवश्यकता है।
3. शिक्षा का पोषण: वर्तमान शिक्षा में जो न्यूनताएं एवं विकृतियां हैं उनके मूल में शिक्षा के आर्थिक पोषण की कुव्यवस्थाएं हैं। विद्यालयीन शिक्षा हो या उच्च शिक्षा, शासन का योगदान बहुत होने के बाबजूद बहुत कम है। अनेक सामाजिक संस्थाएं सेवा के नाते करोड़ों रूपये प्रतिवर्ष शिक्षा में लगा रही हैं। तीसरे वर्ग में वे लोग या संस्थाएं हैं जो शिक्षा में निवेश करती हैं लाभ के लिए। देश में शिक्षा का एक बड़ा भाग लाभ के लिए व्यापार बन गया है। भारतीय समाज को तय करना है कि उसे शिक्षा को व्यापार बनाना स्वीकार्य है या नहीं। अनेक वर्षों से मांग की जा रही है कि सकल घरेलू उत्पाद का 6 प्रतिशत शिक्षा में लगाया जाए तो ही शिक्षा सर्वव्यापी व सर्वसुलभ होगी। वर्तमान में सकल घरेलू उत्पाद का केवल 2.3 प्रतिशत ही शिक्षा में लग रहा है। कस्तूरीरंगन समिति ने शिक्षा में अर्थव्यवस्था के लिए नवाचारी सुझाव दिया है। अनुशंसा की गई है कि सरकार के कुल ख़र्च का 20 प्रतिशत शिक्षा में जाना चाहिए। वर्तमान में सरकारी ख़र्च का लगभग 10 प्रतिशत ही शिक्षा के कार्यों में जाता है। रिपोर्ट में अनुशंसा है कि यह बढ़ौतरी क्रमश: उपलब्ध साधनों के अनुसार की जाए। इसके अतिरिक्त, कार्पोरेट जगत, स्वयंसेवी संस्थाओं, धार्मिक अधिष्ठानों, पूर्व विद्यार्थियों आदि से भी हर स्तर की शिक्षा के लिए धन संग्रह करने की बात भी कही गई है।
अन्य महत्वपूर्ण परंतु व्यवहारिक रूप से कठिन अनुशंसा यह है कि किसी भी शिक्षा संस्थान के ख़र्च की भरपाई शुल्क के माध्यम से 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। निजी शिक्षण संस्थान कैसे चल पाएंगे यह प्रश्न तो है ही परंतु यह भी सही है कि यदि इस बात को सख़्ती से लागू किया जाता है तो शिक्षा के व्यापारीकरण की प्रक्रिया पर अवश्य ही लगाम लगेगी। हमारे कल के भारत की शिक्षा पूर्णत: शासन व समाज पोषित हो यही उचित है और संभव भी है।
कुल मिलाकर प्रस्तावित राष्ट्रीय शिक्षा नीति नवीन भारत के निर्माण की कार्ययोजना का प्रभावी प्रारूप है, इसीलिए सब ओर से इसको समर्थन प्राप्त हो रहा है। सावधानी की आवश्यकता यह है कि जिन नई संस्थाओं (जैसे, केन्द्र स्तर पर राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, उच्च शिक्षा अनुदान आयोग व राज्य स्तर पर राज्य शिक्षा आयोग आदि) का प्रस्ताव रिपोर्ट में किया है वे वास्तव में कितनी स्वायत रह पाती हैं। हमारे देश में स्वायत्ता का असफल मॉडल प्रसार भारती है और सफल मॉडल चुनाव आयोग है। आशा करनी चाहिए कि देश में शिक्षा की व्यवस्था संभालने वाली सभी संस्थाएं अपनी स्वायत्ता को क़ायम रखते हुए नवीन शिक्षा प्रणाली को लागू कर हम सब के सपनों के भारत को साकार करेंगी।
————-