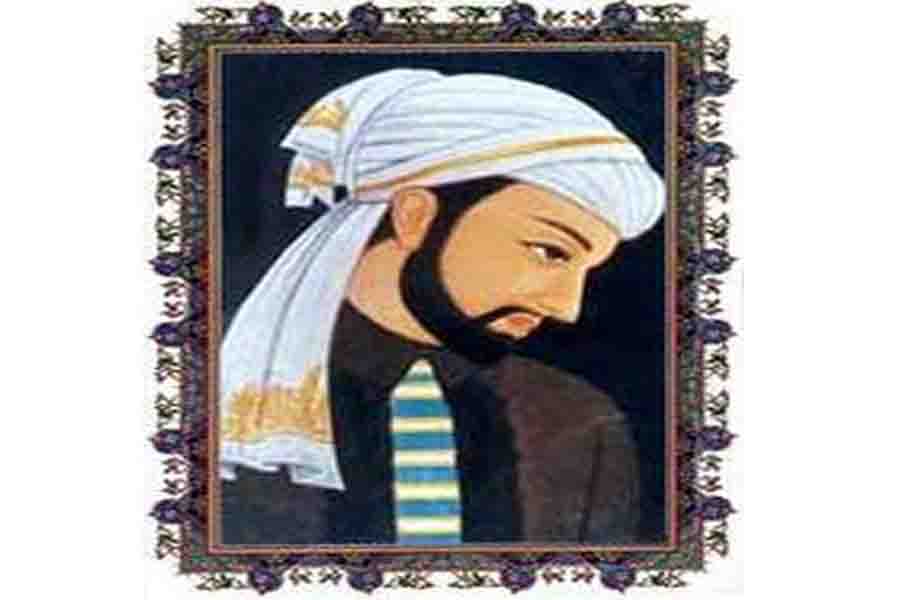संगीत -शिक्षा संस्थाओं के प्रारंभ से पूर्व संगीत की तथा संगीतज्ञों की क्या स्थिति रही होगी, समाज के हृदय में संगीत के प्रति सम्मान भाव जागृत करने के लिए कैसी तपस्या करनी पड़ी होगी, यह जानना और विशेष रूप से उन महान संगीतज्ञों के कष्टमय प्रयत्नों को जानना उन संगीत प्रचारकों को अधिक आवश्यक था, जिन्होंने स्वयं इस सबके लिए अपना जीवन समर्पित किया।
रत कला एवं संस्कृति का विश् व प्रसिद्ध वह राष्ट्र रहा है जिसने जगत को नाद के अमृत रस का आस्वाद दिया है। वस्तुत : भारत ने सदैव एक परंपरा का संरक्षण कर उस आधार पर अपना मार्ग निर्धारित किया है। भारत के वैदिक युग की ओर दृष्टि डालें तो ऋषियों -मुनियों ने भारत की शिक्षा पद्धति को लेकर एक उदाहरण प्रस्तुत किया था। वैदिक ऋचाओं का गान शिक्षा पद्धति का मौलिक स्वरूप माना जा सकता है।
भारत में संगीत शिक्षा के पहलू पर विचार करते समय एक तथ्य सामने आता है कि यहां धर्म, अध्यात्म, भक्ति तथा अन्य प्रकार की उपदेशात्मक शिक्षा या प्रेरणा संगीत से दी जाती रही है। संगीत शिक्षा उत्तम नागरिक अर्थात सुसंस्कृत व्यक्ति निर्माण में सहायक मानी जाती रही है।
भारत की सामाजिक व्यवस्था में प्राचीन काल में वर्णाश्रम व्यवस्था के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार वर्ण विशेष को प्राप्त था जो सामाजिक स्तर पर सुसंस्कृत नागरिक को बनाने में सहायक होते थे। यद्यपि मध्य युग के आते -आते वर्णाश्रम व्यवस्था कमजोर पड़ गई, परंतु तब भी सभ्य नागरिक के निर्माण में संगीत को आधार माना गया। इसका एक कारण यह भी है कि संगीत का उद्देश्य ही मानव का आत्मिक विकास है। जीवनोपयोगी यदि ६४ कलाएं हैं तो ललित कलाओं की संख्या मात्र ५ हैं, उनमें से भी संगीत कला आदर्श कला है, क्योंकि श्रवण के साथ -साथ यह भारत के योग विज्ञान पर भी आधारित है।
आइए, इस संगीत शिक्षा पद्धति के रूपों को जानें –
भारत में सामूहिक शिक्षा प्रारंभ होने से पूर्व प्रत्येक स्थान पर गुरु -शिष्य परंपरा ही थी। शिष्य, व्यक्तिगत रूप से गुरु के पास जाकर शिक्षा ग्रहण करता था। उन दिनों शिक्षा अमूल्य दान था। ज्ञान और कला के कर्णधारों को उन दिनों राजाओं और नवाबों का उदार संरक्षण प्राप्त था। वे अपने छात्रों से प्रशिक्षण के लिए किसी प्रतिदान की आशा नहीं करते थे और न ही उन्हें इसकी आवश्यकता थी।
वास्तव में वे शाही संरक्षकों के उपहार और चंदे के रूप में प्राप्त भूमि और धन से अपने छात्रों के लिए वस्त्र तथा भोजन की पूरी व्यवस्था करते थे। यह सत्य है कि वे अपने छात्रों से कठोर परिश्रम भी करवाते थे और कभी -कभी तो छात्रों को गुरु की कष्टप्रद निजी सेवा भी करनी पड़ती थी। हो सकता है कि वह सब प्रशिक्षण का ही अंग हो। शिक्षक की यह प्रेम -श्रम के रूप में शिक्षा देने की भावना और छात्र की निष्ठा, शाही संरक्षण शिथिल होने के साथ ही समाप्त हो गई और शिक्षक को अपनी जीविका -निर्वाह की खोज करने पर बाध्य होना पड़ा।
यद्यपि संगीतज्ञ को शाही संरक्षणों के कारण जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं की चिंता से मुक्त रखा जाता था, जिससे उन्हें अपने दैनंदिन जीवनोपयोगी साधनों की चिंताएं कष्ट नहीं देती थीं, तथापि समाज का व्यवहार उनके प्रति बेहद कष्टप्रद था। एक संगीतज्ञ के रूप में राजा और जनसमुदाय से मान -सम्मान प्राप्त होने पर भी समाज के एक अंग या घटक के रूप में उन्हें उचित सम्मान नहीं मिलता था। विशिष्ट सामाजिक समारोहों में उन्हें आमंत्रित करना टाला जाता था। यह स्थिति उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध की थी।
भारतीय संगीत के इतिहास में कई नरेशों ने और संतों ने भी संगीत की सेवा की, ऐसा उल्लेख मिलता है, परंतु ये सभी संगीतानुरागी या तो समाज के आश्रयदाता, सत्ताधारी थे, या ऐसे संत थे जिन्हें सामान्य जनजीवन से कोई तात्पर्य नहीं था। वह केवल आनंद या उपासना हेतु संगीत साधना करते थे। ऐसे नरेशों में सुलतान हुसैन शाह शर्की, मानसिंह तोमर, रामपुर दरबार के नवाब, ग्वालियर के सिंधिया वंश तथा संतों में स्वामी हरिदास, अष्टछाप के कवि आदि थे। इनके संगीतज्ञों नवाबों, राजाओं को समाज में पर्याप्त सम्मान था, परंतु ऐसे संगीतज्ञ जिन्हें किसी सत्ता की विशेष कृपा प्राप्त नहीं थी और जीवन -यापन के लिए पर्याप्त धन की आवश्यकता थी, उन्हें समाज में प्रोत्साहन मिलना तो दूर उनकी सामान्य से सामान्य आवश्यकताओं के लिए भी उन्हें समाज की ओर ताकना पड़ता था।
अपने शिक्षा काल में यही संगीतज्ञ कठिनतम परिश्रम से गुरुगृह में अपार कष्ट सहन करके संगीत विद्या प्राप्त करते थे। दूर -दूर तक भ्रमण करके इसे वृद्धिगत करने की चेष्टा करते थे, तथापि इसके उपरांत उन्हें समाज से प्रताड़ना ही मिलती।
मध्य काल में संगीत यद्यपि शिक्षा के क्षेत्र में सहायक रूप में इतना प्रचलित नहीं था, तथापि संगीत को मनोरंजन का साधन मानकर तथा उसका केवल कलात्मक रूप मानकर उसे पारंपरिक रूप से प्रवाहित करने के लिए संगीत की शिक्षा को विशेष महत्व प्राप्त हुआ। संगीत में निहित सौंदर्य तत्वों की वृद्धि करना, उनमें विविधता लाने की दृष्टि से विचार हुआ और अपनी परंपरागत गायन -वादन शैली तथा उसके वैशिष्ट्य का संरक्षण -संवर्धन करने हेतु गुरु -शिष्य परंपरा और घरानेदार गायकी तथा वादन शैली का जन्म हुआ।
घरानेदार संगीत शिक्षा के गुण -दोषों को ध्यान में रखते हुए तथा यह शिक्षा, जो सामान्य संगीत प्रेमियों के लिए सहजता से उपलब्ध नहीं होती थी, आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में इसे भी स्वतंत्र स्थान प्राप्त हुआ, जिससे यह कला शिक्षा आधुनिक समाज के सभी संगीत प्रेमी शिक्षार्थियों को सरल रूप से उपलब्ध हो सके तथा संगीत को शिक्षा के क्षेत्र में अन्य विषयों के समकक्ष सम्मान भी प्राप्त हो सके।
संगीत की बढ़ती हुई महत्ता को ध्यान में रखकर और उसके गुणों की पहचान कर ही शिक्षाविदों ने संगीत शिक्षा का महत्व समझा। संगीत के कुछ अनुरागी तथा विद्वानों ने, जिन्हें शिक्षित तथा सभ्य समाज में सम्मान प्राप्त हुआ था, संगीत के शास्त्र तथा विद्या को जन -जन तक पहुंचाने हेतु संगीत शिक्षा का प्रचार -प्रसार किया और संगीत संस्थाएं खोलकर सामूहिक रूप से शिक्षा देना प्रारंभ किया। तथापि इन सभी प्रक्रियाओं में कई वर्ष लगे।
कई संगीतज्ञों की कठोर तपस्या इसके पीछे थी। इसी कारण संगीत -शिक्षा संस्थाओं के प्रारंभ से पूर्व संगीत की तथा संगीतज्ञों की क्या स्थिति रही होगी, समाज के हृदय में संगीत के प्रति सम्मान भाव जागृत करने के लिए कैसी तपस्या करनी पड़ी होगी, यह जानना और विशेष रूप से उन महान संगीतज्ञों के कष्टमय प्रयत्नों को जानना उन संगीत प्रचारकों को अधिक आवश्यक था, जिन्होंने स्वयं इस सबके लिए अपना जीवन समर्पित किया।
वस्तुत : संगीत की सामाजिक अप्रतिष्ठा के साथ -साथ संगीत -शिक्षा सामान्य जन के लिए सहजता से उपलब्ध न होना भी खेदजनक बात थी। परंतु यह वास्तविकता थी कि आम संगीत प्रेमियों के लिए संगीत सीखना इतना सरल नहीं था।
संगीत शिक्षा की इस समस्या को पं . दिगंबर जी ने समझा था वैसे ही बड़ौदा के उ . मौलाबख्श ने तथा मुंबई के विष्णु नारायण भातखंडे जी ने भी इस समस्या पर चिंतन -मनन कर इसका निराकरण करने का निश् चय किया। संगीत -शिक्षा के तत्कालीन स्वरूप में तथा संगीत के भिन्न क्षेत्रों से पनपते मतभेदों को मिटाया एवं संगीत का एक आदर्श स्वरूप हो और उसी की एक विशिष्ट पद्धति से शिक्षा हो, जिससे सभी समस्याओं का समाधान हो सके, इन बातों पर सोचने -विचारने के लिए प्रेरित किया। पं . भातखंडे स्वयं एक जाने माने वकील थे, परंतु अपनी बाल्यावस्था से ही संगीत के प्रति लगाव होने के कारण घर के लोगों से छिपकर संगीत सीखते रहे। भातखंडे जी के वकालत करने के समय ही ई . १८९० से पूर्व मुंबई में ‘गायन उत्तेजक मंडली ’ नाम से एक संगीत संस्था का प्रारंभ हो चुका था। इस संस्था में अच्छे नामांकित गुणी गायक वादकों के कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। इसी संस्था में संगीत सीखने की इच्छा रखने वालों के लिए संगीत -शिक्षक की भी व्यवस्था की गई थी।
संगीत शिक्षक के महान उद्देश्य को ध्यान में रखकर भातखंडे संगीत के क्रियात्मक एवं सैद्धांतिक पक्ष का अध्ययन करते रहे। संगीत के विभिन्न ग्रन्थों का अध्ययन तथा परंपरागत रागदारी और बंदिशों का संग्रह करते रहे। यद्यपि भातखंडे जी को ऐसा संग्रह करने में अनेक कठिनाइयां आईं। कई बार किसी उस्ताद को वेतन देकर भी उनसे बंदिशें प्राप्त करनी पड़ीं, तो कई बार छल -कपट से भी बंदिशें निकलवानी पड़ीं।
इसके बाद उन्होंने अपनी संग्रहित बंदिशों तथा उनके नियमों के आधार पर राग के लक्षण गीतों की रचनाएं की, जिसमें राग के सामान्य नियमों का वर्णन उन्हीं राग के गीतों के द्वारा स्पष्ट होता है।
१९वीं शताब्दी के उत्तरार्ध का समय सामूहिक शिक्षण संस्थाओं की नींव मजबूत करने और समाज के अंतर्गत संगीत -शिक्षा के प्रति जागृत होने, संगीत की प्रतिष्ठा बढ़ाने, संगीतकारों को उचित सम्मान प्राप्त कराने के लिए योग्य सिद्ध हो रहा था। संपूर्ण देश में संगीत की इस शिक्षा क्रांति तथा प्रतिष्ठा का मजबूत जाल बुनना आरंभ हो गया था।
भिन्न -भिन्न संगीत शिक्षा -संस्थाएं, विद्यालयों के रूप में उभरने लगी। इस पद्धति से एक ही समय एक ही घंटे में, एक ही शिक्षक से अनेक विद्यार्थी संगीत सीखने लगे। वर्तमान युग में हिंदुस्तानी संगीत की आधुनिक शिक्षा पद्धति गत साठ -सत्तर वर्षों से ही प्रचलित हुई है। इन साठ -सत्तर वर्षों में हिंदुस्तानी संगीत में अनेक परिवर्तन हुए।
पं . भातखंडे, संगीत शिक्षा को विश् वविद्यालयीन पाठ्यक्रम का सम्मान दिलाना चाहते थे। किसी भी विद्या की उन्नति के लिए जिस बुनियादी साहित्य की आवश्यकता होती है, वह सब उन्होंने संगीत के लिए उपलब्ध करा दिया था।
संगीत शिक्षा को प्राप्त कर विद्यार्थी केवल गायक ही नहीं अपितु, अच्छा गायक, अच्छा शिक्षक, प्रशासक तथा शास्त्रकार बने यह पं . भातखंडे जी की कामना थी और इसी दृष्टि से वे प्रयत्नशील भी रहे। उनके पश् चात उनसे प्रभावित संगीत प्रेमी भी इस दिशा में प्रयत्नशील रहे। उनके अनंत परिश्रमों तथा उत्कट इच्छा के फलस्वरूप ही भारत में सर्वप्रथम बड़ौदा विश् वविद्यालय में संगीत का समावेश हुआ।
इसके बाद सन १९५२ में बनारस हिंदू विश् वविद्यालय में . पं . ओंकारनाथ ठाकुर ने अत्यधिक प्रयत्नों से कॉलेज आफ म्यूजिक एंड फाइन आटर्स विभाग शुरू किया और उसे स्थायी रूप प्रदान किया। इस प्रकार से भारत के दो विश् वविद्यालयों में अन्य विषयों की भांति ही संगीत की शिक्षा का प्रारंभ हुई।
संगीत को विश् वविद्यालय में स्थान प्राप्त हो जाने से अन्य सभी विषयों के समान ही संगीत में भी विश् वविद्यालयों द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम, कक्षाएं, परीक्षाएं तथा उपाधियां इत्यादि बातों को महत्व प्राप्त हुआ। संगीत को एक शैक्षणिक दर्जा प्राप्त हो जाने से संगीत के क्षेत्र में एक अनोखी क्रांति आ गई और इससे संगीत का समूचा क्षेत्र लाभान्वित हुआ। इसी तरह, इंदिरा कला संगीत विश् वविद्यालय खैराग़ढ एवं राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला वि . वि . ग्वालियर वर्तमान संगीत शिक्षण पद्धति के प्रगति के सर्वश्रेष्ठ सोपान माने जा सकते हैं।
संगीत शिक्षा के तीन प्रमुख उद्देश्य भी माने जा सकते हैं –
१ . संगीत द्वारा व्यक्तित्व का विकास करना।
२ . संगीत की भिन्न -भिन्न शाखाओं में अनुसंधान करना।
३ . संगीत शिक्षा द्वारा मंच प्रदर्शक का निर्माण करना।
वर्तमान युग में संगीत शिक्षा के प्रसार एवं प्रचार से संगीत की एवं संगीतज्ञों की महत्ता बढ़ी है। छात्रों को संगीत शिक्षा अत्यंत सुलभता से प्राप्त होने लगी है। संगीत का ज्ञान और उपाधि दोनों ही बातें उन्हें विश् वविद्यालयीन शिक्षा द्वारा सरलता से उपलब्ध होने लगी है, इसी कारण उन्हें अन्य शिक्षित, उपाधिधारी व्यक्तियों के समान ही नियुक्तियां, वेतनमान और प्रतिष्ठा मिलने लगी।
वास्तव में संगीत एक ऐसा विषय है जिसमें राग के स्वरूप को समझने की आवश्यकता होती है। राग की प्रकृति को समझकर उसे गाना केवल पाठ्यक्रम पूर्ण करने से ही संभव नहीं हो पाता। शिक्षक या गुरु के सन्मुख बैठकर बार -बार सुनने समझने तथा अन्य भी अनेकों कलाकारों का गायन -वादन सतत रूप से सुनते रहने से ही विद्यार्थी राग की प्रकृति की विविध छटाएं समझ सकता है। गुरुकुल या घरानेदार शिक्षा पद्धति में राग की बंदिशों का अनगिनत बार अभ्यास करने, आलाप के ढंग को समझकर उसका बार -बार अभ्यास करते रहने से, एक -एक तान को कई -कई बार रटने से, जहां पाठ्य सामग्री का पाठांतर हो जाता है, वहीं गले की तैयार भी होती है तथा गायन में परिपक्वता आती है। वैसे तो ‘कला ’ का कोई अंत नहीं है, परिश्रम से उसके स्वरूप में नवीनता और वृद्धि होती है। अत : ऐसे विषय में यदि किसी भी कारण से अनियमितता होने पर छात्र की प्रगति में, उन्नति में बाधा उत्पन्न होती है, साथ ही एक कर्तव्यनिष्ठ अध्यापक को इस प्रकार के विशिष्ट विषय का पाठ्यक्रम पूर्ण करने में भी असमंजस्यता उत्पन्न होती है।
वही दूसरी ओर संगीत शिक्षकों की सृजनशीलता का प्रश् न सचमुच चिंतनीय है। कलाकार प्रवृत्ति का शिक्षक नित्य नई सृजनाओं से प्रेरित रहता है। अपनी नई परिकल्पनाओं को वह अपने छात्रों में ढालना चाहता है। परंतु अधिकांशतया उसे योग्य विद्यार्थियों के संबंध में निराश होना पड़ता है। कमजोर विद्यार्थियों को सिखाने में उसे इतनी मेहनत करनी पड़ती है कि नई कल्पना तो छोड़ ही दें, उस शिक्षक का रहा -सहा संगीत ज्ञान भी कुंठित हो जाता है। ज्ञान का आदान -प्रदान शिक्षक और विद्यार्थी की क्षमता पर निर्भर करता है। इस आदान -प्रदान की गति ही नई कल्पनाओं को जन्म देती है और ये नई कल्पनाएं आपस में मिल जुलकर ही सृजन का रूप लेती हैं।
वस्तुत : आज विज्ञान का युग है। वैज्ञानिक उपकरणों की सहायता से भी आज का संगीत शिक्षण अध्ययन -अध्यापन की नवीन आशा का संचार कर रहा है, यह भारतीय संगीत के सुनहरे भविष्य की ओर इंगित करता है।