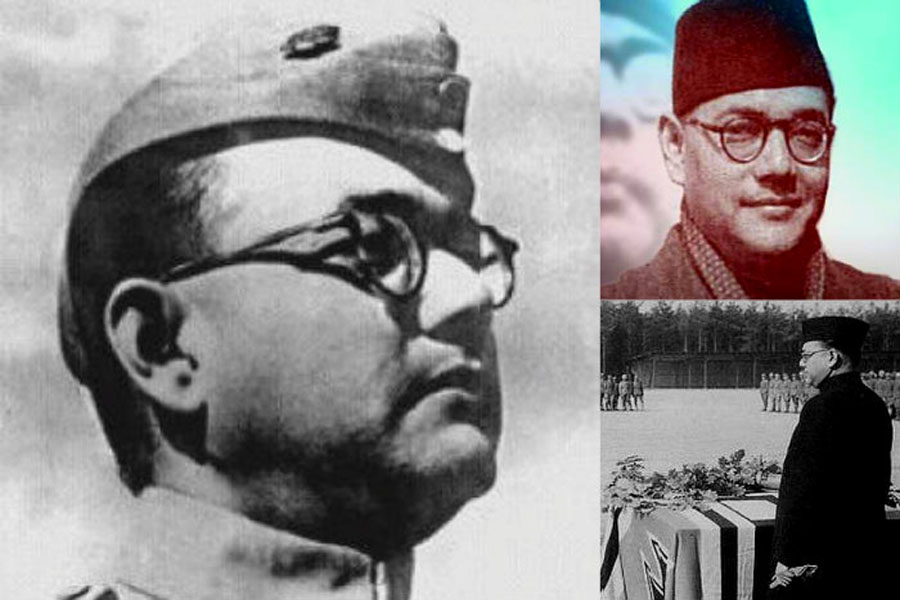भारत की न्यायपालिका की संवेदना भारत के जनमानस के साथ जुड़ी दिखाई नहीं देती। उसका अपना एक सामंती चरित्र है, जो हर प्रकार से शक्तियों से परिपूर्ण किन्तु किसी के प्रति जवाबदेह नहीं है और बड़ी आत्ममुग्ध और स्व-संचालित है। वह अपने बारें में किसी समीक्षा को पसंद नहीं करता।
इस वर्ष अपना देश आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। भारत सरकार द्वारा इस उपलक्ष्य को अमृत-महोत्सव का नाम दिया है। केंद्र व राज्य सरकारें तथा तमाम सामाजिक व राजनीतिक संगठन इस अवसर पर विविध तरह के कार्यक्रम आयोजित करके देश की स्वतंत्रता में योगदान देने वालों, बलिदानीं वीरों व स्वतन्त्रता सेनानियों को याद कर उन्हे अपनी श्रद्धांजलि दे रहें है किन्तु एक अति-आवश्यक बात जो इस अवसर पर अवश्य होनी चाहिए वह होती नहीं दिख रही है, वह है इन 75 वर्षों में अपने देश की लोकतांत्रिक यात्रा की चर्चा। इस अवसर पर हमें अपने देश के संविधान व इनके अंग-उपांगो की उपयोगिता-उपादेयता की चर्चा व समीक्षा अवश्य करनी चाहिए। यद्यपि जब लोकतंत्र की यात्रा की बात होगी तो उसमें संविधान व सरकार के सभी अंगों के साथ-साथ स्वतंत्रता के पश्चात देश की सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक प्रगति सब कुछ शामिल है और तब इसका क्षेत्र फ़लक बहुत बड़ा हो जाता है।
उत्कृष्ट लोकतान्त्रिक देशों की तरह भारत की एक अत्यंत शक्तिशाली व स्वतंत्र न्यायपालिका है। राजनीति विज्ञान में सरकार के अंगों की जो बड़ी सरल परिभाषा बताई जाती है वो ये है कि विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका उसे लागू करती है और न्यायपालिका उसका उल्लंघन करने वालों को दंड देती है। विधि के उल्लंघन पर ऐसे उल्लंघनकर्ता को दंडित करना न्यायालय का द्वितीयक कार्य है, बल्कि न्यायपालिका का मूल कार्य तो कार्यपालिका और व्यवस्थापिका की निरंकुशता व उसके अन्याय -अत्याचार से समाज को बचाना और इन सबसे जनमानस में व्यवस्था के प्रति उपजे विषाद व असंतोष को संभालना होता है। इस विचार के आलोक में जब हम भारत की न्यायपालिका की भूमिका का दर्शन करते हैं तो बड़ी निराशा होती है। कुछ उदाहरणों को छोड़ दिया जाए तो भारत की न्यायपालिका की संवेदना भारत के जनमानस के साथ जुड़ी दिखाई नहीं देती। उसका अपना एक सामंती चरित्र है, जो हर प्रकार से शक्तियों से परिपूर्ण किन्तु किसी के प्रति जवाबदेह नहीं है और बड़ी आत्ममुग्ध और स्व-संचालित है। वह अपने बारें में किसी राय व समीक्षा को भी पसंद नहीं करती। भारत में न्यायपालिका का उच्च-स्वरूप जिन्हें हम संवैधानिक न्यायालय कहते हैं इनका गठन बड़ा अलोकतांत्रिक व दोषपूर्ण है। न्याय- व्यवस्था जिसके द्वारा न्यायपालिकाएं अपने कार्य संचालन करती है वह अत्यंत महंगी, अतिविलंबकारी और अप्रत्याशित निर्णय देने वाली है। ‘न्याय प्राप्त करना और इसे समय से प्राप्त करना किसी भी राज्य व्यवस्था के व्यक्ति का नैसर्गिक अधिकार होता है।’ लेकिन भारत के न्यायालयों के संबंध में यह तीनों ही बातें लागू नहीं होती। यह कटु- सत्य है कि आप अपनी किसी पीड़ा के संबंध में कैसे भी पैसे की व्यवस्था करके अपनी क्षमता से ज्यादा एक महंगा वकील करिए, मुकदमा फाइल करिए और भूल जाइए (File Forget)। आपके मुकदमें का परिणाम आपके भाग्य और प्रारब्ध पर निर्भर करेगा। तुच्छ से विषय पर कानूनी लड़ाई के लिए इतने फोरम और स्तर हैं कि लड़ने में पीढ़ियां खप जा रही हैं। यदि इस पर कोई अध्ययन हो तो निश्चित रूप से यही निकल कर आएगा कि राजस्व व सिविल विवाद के 90% से अधिक मामलों में कम से कम 2 पीढ़ियां मुकदमा लड़ने में गुजार देती हैं। बाकी मामलों में भी स्थिति बहुत बेहतर नहीं है। भारत के अपराध-विचारण प्रणाली (ट्रायल) के मामले में तो यह आम धारणा बन गई है कि यह अपराध कर बच निकलने का उपक्रम है, जहां विचारण के दौरान पीड़ित को और अधिक पीड़ा सहनी पड़ती है। बेल तक की जेल ही अधिकांश अपराधों की सजा है। उसके बाद का तो सब एक दिखावा है, उसके बाद तो मुकदमें के स्वतः समाप्ति के लिए ट्रायल या फिर अपील के नाम पर सिर्फ समय बीतने का इंतजार किया जाता है ताकि वादी या अपराधी में से कोई एक समाप्त हो जाए, और केस खत्म हो।
सभी प्रकार के मामलों में विचारण न्यायालय में जो समय लगता है वो तो वर्षों वर्ष है ही, सिविल व राजस्व मामलों के कई मामलों में अपील, रिविज़न, रिट, विशेष अनुमति याचिका आदि के मामलों के कई कई साल तक लंबित रहने के बाद ऊपरी न्यायालय से अचानक से कह दिया जाता है कि मामला उसके समक्ष पोषणीय ही नहीं था, और उसे फिर किसी अन्य सक्षम फोरम में जाने के लिए कह दिया जाता है। इसमें समय का कितना नुकसान होता हैं, ये दर्द वही समझ सकते हैं, जिसका इन्हें कटु अनुभव है। बहुत लंबे समय तक लंबित रहने के कारण बहुतायत मुकदमें औचित्यहीन हो जाते हैं किंतु सुनवाई का नंबर न आने पर लंबित मुकदमों की सूची में उनकी गिनती चलती रहती है। किसी भी मामलें में दूसरे पक्ष को नोटिस सर्व करने की प्रक्रिया ही इतनी सुस्त है कि कई वर्ष तो सिर्फ इसमें गुजर जाते हैं। कभी-कभी तो इसी में 10-10 साल लग जाते हैं और जब तक किसी पर नोटिस सर्व हो पाती है और कार्यवाही आगे बढ़ने की कुछ गुंजाइश बनती तब तक उस पक्षकार की मृत्यु हो जाती है, फिर उनके विधिक उत्तराधिकारियों को जोड़ने का अंतहीन सिलसिला चल पड़ता है। निचली अदालत के निर्णय के विरुद्ध ऊपरी अदालत में गए हुए अधिकांश मामलों में एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को नोटिस सर्व करने या उसके विधिक उत्तराधिकारियों को वाद में पक्षकार बनाने में सारा समय निकल जाता है और अंततोगत्वा उस मुकदमे की परिणीति पक्षकारों द्वारा थक हार कर घर बैठ जाने से मुकदमे की स्वतः समाप्ति से होती है ।
स्वतंत्रता के समय जिस प्रकार की न्याय-व्यवस्था हमको अंग्रेजों ने दी थी हमने उसे उसी भांति स्वीकार कर लिया, और फिर हमने सुधार करने की फिर कभी कोई हिम्मत नहीं दिखाई। यद्यपि मैं इसके मूल में न्यायपालिका की हठधर्मिता, विधायिका और कार्यपालिका का न्यायिक सुधार के संबंध में उपेक्षात्मक रुख साथ-साथ भारतीय जनमानस की भूमिका देखता हूं, जिसने अपार पीड़ा को सहते हुए भी न्यायिक सुधार की दिशा में कदम उठाने के लिए सरकारों पर दबाव बनाने का कार्य कभी नहीं किया, जो मिला उसे नियति मानकर स्वीकार कर लिया। भारत को अपनी सामाजिक, सांस्कृतिक परिस्थिति और अपने इतिहास बोध के अनुसार एक वैकल्पिक न्याय तंत्र ही स्थापित करना चाहिए, किंतु जब तक यह नहीं होता वर्तमान व्यवस्था में ही कुछ आवश्यक सुधार करके हमें इसे समसामयिक और उपयोगी बनाए रखना चाहिए।
सर्वप्रथम तो भारत के न्यायपालिका का संस्थागत चरित्र बदलने की जरूरत है। यह सामंती है और इसे इसके स्थान पर लोकतांत्रिक बनाना होगा। संवैधानिक जजों की चयन प्रक्रिया बहुत ही अलोकतांत्रिक है, जिसमें संविधान में वर्णित ‘हम भारत के लोग’ इनकी कोई भूमिका नहीं है। यहां पहले से पदासीन चले आ रहे लोग अपनी पसंद के लोगों को चुनकर पदों पर बिठा देते हैं, देखते ही देखते कुछ ही वर्षों में भारत का पूरा न्यायिक तंत्र कुछ परिवारों के कब्जे में आ गया है। वर्तमान सरकार ने इसमें सुधार का जो थोड़ा सा प्रयास किया उसे भी न्यायिक पुनर्विलोकन की अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए न्यायपालिका ने खारिज कर दिया।
एक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सभी उच्च संस्थाओं के गठन में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जन की भूमिका अवश्य होनी चाहिए। क्या ये उत्तम नहीं होगा कि भारत के संवैधानिक न्यायालय अपने सदस्यों के नियुक्ति के लिए अपनी आवश्यकता से कुछ गुना अधिक अच्छे विधिवेत्ताओं का एक पैनल तैयार करे, जिससे अतीत और आचरण के बारें में कार्यपालिका जांच करें और फिर यह नाम उच्च सदन (राज्यसभा) के पटल पर कुछ निश्चित समय के लिए रखे जाएं, जिस किसी सदस्य को आपत्ति हो तो वो प्रकट करें, और फिर उस पर मतदान हो। यहां प्रसंगवश लेखक एक बात और कहना चाहेगा कि आदर्श लोकतान्त्रिक व्यवस्था के क्रम में कम से कम संसद के उच्च सदन को दलीय लोकतन्त्र से मुक्त रखना चाहिए। इसके सदस्यों के चुनाव में भी मतदाताओं को दलीय अनुशासन में नहीं बांधना चाहिए और चुनकर आने वालों राज्यसभा सांसदों को किसी भी विषय पर स्वतंत्र मतदान का अधिकार होना चाहिए। इसी क्रम में यदि न्यायमूर्ति बनाए जाने के लिए प्रस्तावित किसी नाम पर यदि मतदान में भाग लेने वाले आधे से अधिक सदस्य आपत्ति कर दे तो उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाना चाहिए। भावी मुख्य न्यायाधीश का पद वर्तमान मुख्य न्यायाधीश- भारत सरकार और मुख्य विपक्षी दल के एक-एक प्रतिनिधि से बनी समिति द्वारा पूर्ण सहमति के आधार पर भरा जाना चाहिए। हालांकि अंत में यह कहने से मैं फिर नहीं चुकूंगा कि भारत की सम्पूर्ण न्याय व्यवस्था का भारतीयकरण होना चाहिए।