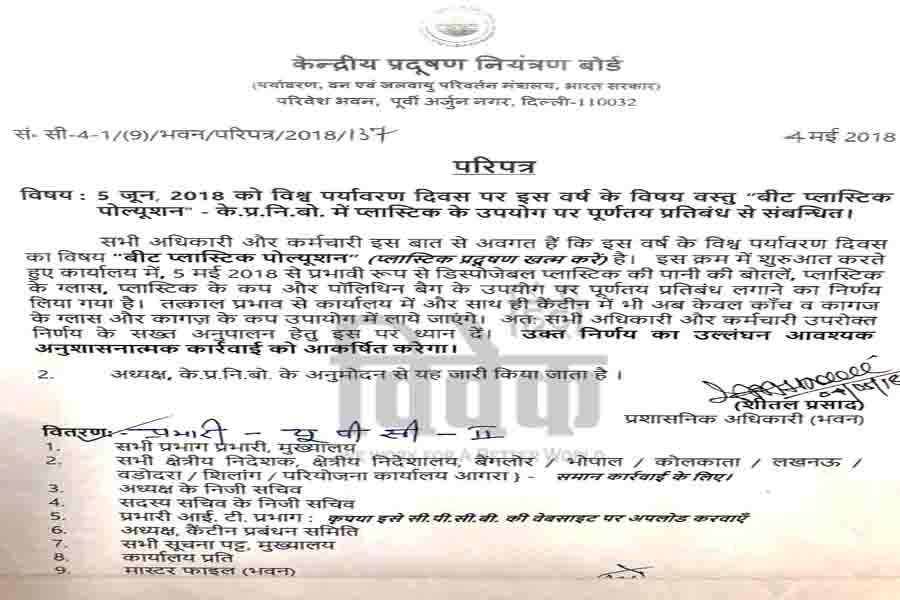प्लास्टिक ने भूतल पर ही नहीं, समुंदरों और अंतरिक्ष में भी हाहाकार मचा दिया है। सारी दुनिया में इसे रोकने के प्रयास चल रहे हैं, विभिन्न विकल्पों पर ध्यान दिया जा रहा है, कई नए अनुसंधान हो रहे हैं। इससे आनेवाले समय में अवश्य ही कोई माकूल जवाब खोज लिया जाएगा, लेकिन तब तक हमें सावधानी बरतना जरूरी है।
विश्व में प्लास्टिक के बढ़ते उपयोग से प्रत्येक देश चिंतित और पीड़ित है। बावजूद प्लास्टिक है कि आम से खास लोगों की दिनचर्या में शुमार हो गया है। दैनिक उपयोग की वस्तुओं से लेकर संचार, वाहन, भवन निर्माण और अंतरिक्ष यानों तक में इसका भरपूर इस्तेमाल हो रहा है। अंतरिक्ष यानों में लूरोप्लास्टिक का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह 275 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर भी पिघलता नहीं है। पैकेजिंग के लिए जिस प्लास्टिक का प्रयोग होता है, उसे पॉलिस्टरीन कहते हैं। थैलियां, पैकेट और डिब्बे इसी पॉलिस्टरीन से बनते हैं। विनाइल प्लास्टिक का प्रयोग हैंड बैग, शॉवर, पर्दे और शीट कवर में किया जाता है। फार्मिका प्लास्टिक टेबल पर लगाई जाती है, जिससे टेबल ताप अवरोधक बन जाती है। दीवारों पर जो प्लास्टिक पेंट होता है, वह अल्काइड और एक्रिलिक प्लास्टिक होता है। इसी के प्रयोग से दीवारें चमकदार और वाटरप्रूफ बनती हैं। पारदर्शी प्लास्टिक को पर्सपेक्स प्लास्टिक कहते हैं। यह काँच की जगह प्रयोग में लाया जाता है। सिनेमा की फिल्म और कैसेट की रील जिस प्लास्टिक से बनती है, उसे सेल्युलॉयड प्लास्टिक कहते हैं। साफ है, प्लास्टिक का उपयोग हर जगह बढ़ गया है, इसलिए जरूरी है कि हम इसके निर्माण की प्रक्रिया को जान लें।
प्लास्टिक ऐसा पदार्थ है, जिसे गर्म करने पर उसमें मुलामियत आ जाती है। इस स्थिति में उस पर दबाव डालकर उसे मनचाहे आकार-प्रकार में ढाल लिया जाता है। ठंडा होने पर इसका आकार स्थिर रहता है। प्लास्टिक का मुख्य तत्व कॉर्बन है। कॉर्बन एक ऐसा तत्व है, जो लंबी श्रृखंला वाले विभिन्न तरह के अनेक कॉर्बनिक का निर्माण करता है। मनुष्य ने पहला प्लास्टिक आज से लगभग 125 वर्ष पहले बनाया था, जिसे सेल्युलॉयड नाम दिया गया। सेल्युलाइड प्लास्टिक का यही आरंभिक स्वरूप है। इसे प्रकृति प्रदत्त प्लास्टिक भी कहते हैं। प्लास्टिक का ठीक से उपयोग 1940 से शुरू हुआ।
अंतरिक्ष में प्लास्टिक का कचरा
एक अनुमान के मुताबिक प्रति वर्ष 31.1 करोड़ टन प्लास्टिक का उत्पादन किया जाता है। यही वजह है कि समूचा ब्रह्माण्ड प्लास्टिक कचरे की चपेट में है। मानव विकास और उन्नत विज्ञान की चाहत में हर देश अंतरिक्ष में उपग्रह भेजने में लगा है। भारत ने तो एक साथ अतंरिक्ष में 104 उपग्रह स्थापित कर विश्व कीर्तिमान स्थापित किया है। यही लालसा और होड़ मनुष्य को भारी पड़ रही है। पुराने अंतरिक्ष यान और उपग्रह कबाड़ के रूप में आकाश में भटक रहे हैं। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि अंतरिक्ष का यह कबाड़ खतरा साबित हो सकता है। एक अनुमान के अनुसार अंतरिक्ष में कबाड़ के रूप में 17 करोड़ टुकड़े तैर रहे हैं, जो किसी भी समय सक्रिय उपग्रहों से टकराकर उन्हें नष्ट कर सकते हैं। इन टुकड़ों से अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के नष्ट होने का भी खतरा है। ऐसा होने पर यह विश्व अर्थव्यवस्था को विनाशकारी साबित हो सकता है। दरअसल अंतरिक्ष यानों में लूरोप्लास्टिक का प्रयोग किया जाता है। इसकी यह विशिष्टता होती है कि यह 275 डिगी सेंटीगे्रड उच्च तापमान पर भी पिघलता नहीं है। इसलिए इनका अस्तित्व रॉकेट के नष्ट हो चुकने के बाद भी बना रहता है।
पुराने रॉकेटों और व्यर्थ हो चुके उपग्रहों का मलबा बहुत तेज गति से पृथ्वी की कक्षा में घूमता है। इसमें वातावरण की ऊपरी सतह को बेकार करने की क्षमता होती है। वर्तमान समय में अंतरिक्ष की कक्षा में 3000 से अधिक उपग्रह सक्रिय हैं। ये मानव समाज के लिए आवश्यक हैं, क्योंकि इनके माध्यम से जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को देखने से लेकर रक्षा प्रयोजनों की निगरानी भी की जाती है। कक्षा में सक्रिय इन उपग्रहों की कीमत लगभग 33 लाख करोड़ रूपए है। ऑस्ट्रेलियाई ‘स्पेस एनवायरमेंट रिसर्च सेंटर‘ के सीईओ बेन ग्रीन का कहा है, ‘वहां इतना मलबा है कि वह आपस में ही टकरा रहा है। साथ ही इकट्ठा होकर कबाड़ की संख्या बढ़ा रहा है। अब यह आशंका बढ़ रही है कि कचरा आपस में टकराकर अंतरिक्ष की कक्षा में परिक्रमा कर रहे उपग्रहों को कहीं नष्ट न कर दें ?’ अंतरिक्ष कबाड़ के रूप में 17 करोड़ टुकड़ों में से अब तक महज 22000 टुकड़ों की ही पहचान हुई है।
समुद्र में प्लास्टिक कचरा
जब भी हम प्लास्टिक के खतरनाक पहलुओं के बारे में सोचते हैं, तो एक बार अपनी उन गायों की ओर जरूर देखते हैं, जो कचरे में मुंह मारकर पेट भरती दिखाई देती हैं। पेट में पॉलिथीन जमा हो जाने के कारण मरने वाले पशुधन की मौत की खबरें भी आए दिन आती ही रहती हैं। यह समस्या भारत की ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की है। यह बात भिन्न है कि यह हमारे यहां ज्यादा और खुलेआम दिखाई देती है। एक तो इसलिए कि स्वच्छता अभियान कई रूपों में चलाए जाने के बावजूद प्लास्टिक की थैलियों में भरा कचरा शहर, कस्बा और गांव की बस्तियों के नुक्कड़ों पर जमा मिल जाता है। यही बचा-खुचा कचरा नालियों से होता हुआ नदी, नालों, तालाबों से बहकर समुद्र में पहुंच जाता है। इसीलिए आर्कटिक सागर के बारे में आया ताजा अध्ययन चौंकाता है। इस अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि 2050 तक इस सागर में मछलियों की तुलना में प्लास्टिक के टुकड़े कहीं ज्यादा संख्या में तैरते दिखाई देंगे।
प्लास्टिक की समुद्र में भयावह उपलब्धि की चौंकाने वाली रिपोर्ट ‘यूके नेशनल रिसोर्स डिफेंस काउंसिल’ ने भी जारी की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक प्रत्येक वर्ष दुनिया भर के सागरों में 14 लाख टन प्लास्टिक विलय हो रहा है। सिर्फ इंगलैंड के ही समुद्रों में 50 लाख करोड़ प्लास्टिक के टुकड़े मिले हैं। प्लास्टिक के ये बारीक कण (पार्टीकल) कपास-सलाई (कॉटन-बड्स) जैसे निजी सुरक्षा उत्पादों की देन हैं। ये समुद्री सतह को वजनी बनाकर इसका तापमान बढ़ा रहे हैं। समुद्र में मौजूद इस प्रदूषण के सामाधान की दिशा में पहल करते हुए इंग्लैंड की संसद ने पूरे देश में पर्सनल केयर प्रोडक्ट के प्रयोग पर प्रतिबंध का प्रस्ताव पारित किया है। इसमें खासतौर से उस कपास-सलाई का जिक्र है, जो कान की सफाई में इस्तेमाल होती है। प्लास्टिक की इस सलाई में दोनों और रूई के फोहे लगे होते हैं। इस्तेमाल के बाद फेंक दी गई यह सलाई सीवेज के जरिए समुद्र में पहुंच जाती हैं। गोया, ताजा अध्ययनों से जो जानकारी सामने आई है, उसमें दावा किया गया है कि दुनिया के समुद्रों में कुल कचरे का 50 फीसदी इन्हीं कपास-सलाइयों का है। इंग्लैंड के अलावा न्यूजीलैंड और इटली में भी कपास-सलाई को प्रतिबंधित करने की तैयारी शुरू हो गई है।
भारतीय राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान (एनआईओ) के एक अध्ययन के अनुसार मानसून के दौरान समुद्री तटों से बहकर समुद्र में समा जाने वाला प्लास्टिक कबाड़ समुद्री जीवों के लिए खतरा बन रहा है। गोवा स्थित एनआईओ के वैज्ञानिकों और शोधार्थियों की ओर से एक शोध-पत्र प्रस्तुत किया गया है। इसके अनुसार जहाजरानी मार्गों से गुजरने के दौरान जहाजों से गिरने वाला प्लास्टिक और भूल से समुद्र में गिर जाने वाला सामान, तटीय पर्यावरण को बड़ा नुकसान पहुंचा रहा है। मानसून के दौरान बरसात के पानी के साथ बहकर चला आने वाला प्लास्टिक कचरा समुद्री जीवों के लिए बड़ा हानिकारक है। इस प्लास्टिक की वजह से दुनिया में 1200 से ज्यादा समुद्री जीवों की प्रजातियां खतरें में हैं। भोजन के धोखे में इन्हें खा लेने से प्रति वर्ष एक लाख समुद्री जीवों की मौत हो जाती है। भारत के मुंबई, अंडमान-निकोबार और केरल के समुद्री तट सबसे ज्यादा प्रदूषित हैं।
प्लास्टिक कबाड़ से छुटकारे के उपाय
प्लास्टिक के यौगिकों की यह खासियत है कि ये करीब 400 साल तक नष्ट नहीं होते हैं। इनमें भी प्लास्टिक की ‘पोली एथलीन टेराप्थलेट‘ ऐसी किस्म है, जो इससे भी ज्यादा लंबे समय तक जैविक प्रक्रिया शुरू होने के बावजूद नष्ट नहीं होती है। इसलिए प्लास्टिक का पुनर्चक्रण कर इससे नए उत्पाद बनाने और इसके बाद भी बचे रह जाने वाले अवशेषों को जीवाणुओं के जरिए नष्ट करने की जरूरत है।
यदि भारत में कचरा प्रबंधन सुनियोजित और कचरे का पुनर्चक्रण उद्योगों की श्रृंखला खड़ी करके शुरू हो जाए तो इस समस्या का निदान तो संभव होगा ही रोजगार के नए रास्ते भी खुलेंगे। भारत में जो प्लास्टिक कचरा पैदा होता है, उसमें से 40 प्रतिशत का आज भी पुनर्चक्रण नहीं हो पा रहा है। यही नालियों सीवरों और नदी-नालों से होता हुआ समुद्र में पहुंच जाता है। प्लास्टिक की विलक्षणता यह भी है कि इसे तकनीक के मार्फत पांच बार से भी अधिक मर्तबा पुनर्चक्रित किया जा सकता है। इस प्रक्रिया के दौरान इससे वैक्टो ऑयल भी सह उत्पाद के रूप में निकलता है, इसे डीजल वाहनों में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और जापान समेत अनेक देश इस कचरे से ईंधन प्राप्त कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलियाई पायलेट रॉसेल ने तो इसी ईंधन को विमान में डालकर 16 हजार 898 किमी का सफर करके विश्व-कीर्तिमान स्थापित किया है। इस यात्रा के लिए पांच टन बेकार प्लास्टिक को विशेष तकनीक द्वारा गलाकर एक हजार गैलन में तब्दील किया गया। फिर एकल इंजन वाले 172 विमान द्वारा सिडनी से आरंभ हुआ सफर एशिया, मध्य एशिया और यूरोप को नापते हुए छह दिन में लंदन पहुंचकर समाप्त हुआ। प्रति दिन लगभग 2500 किमी का सफर 185 किमी प्रति घंटे की रतार से तय किया गया। भारत में भी प्लास्टिक से ईंधन बनाने का सिलसिला शुरू हो गया है। किंतु अभी प्रारंभिक अवस्था में है।
ग्वालियर के जीवाजी विश्वविद्यालय के अभियांत्रिकी विभाग ने प्लास्टिक कचरे से पेट्रोल निर्माण में सफलता प्राप्त की है। प्रयोगशाला में किए प्रयोग से प्राप्त निष्कर्ष की मानें तो 10 किलोग्राम उपयोग में लाई जा चुकी पॉलिथीन से एक से डेढ़ लीटर पेट्रोल बनाया जा सकता है। यह आज के पेट्रोल मूल्य से करीब चार गुना सस्ता होगा। ‘इंटरनेशनल जनरल ऑफ केमिकल रिसर्च‘ में प्रकाशित हुए इस शोध के प्रमुख डॉ. डी सी तिवारी ने तो यहां तक दावा किया है कि यह पेट्रोल करीब-करीब सौ-सौ फीसदी प्रदूषण मुक्त है।
प्लास्टिक से सड़क का निर्माण
मदुरै के अभियांत्रिकी महाविद्यालय में रसायन-शास्त्र के प्राध्यापक राजगोपाल वासुदेवन ने प्लास्टिक अपशिष्ट से सड़क निर्माण के लिए चूर्ण का आविष्कार किया है। 2002 में उन्होंने इस प्रौद्योगिकी का पेंटेट भी करा लिया है। राष्ट्रीय ग्राम सड़क विकास अभिकरण ने इसी चूर्ण से सड़कें बनाने का निर्णय लिया है। अब तक मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र और झारखंड में 16 हजार किमी से ज्यादा लंबी सड़कें बन भी चुकी हैं। भारतीय ग्रामों में कुल 24.5 लाख किमी सड़के हैं। यदि प्लास्टिक के अपशिष्ट से ये सड़कें बनें तो 24.5 लाख टन डामर बचेगा। इससे 12,250 करोड़ रुपए की बचत होगी। हर साल ग्रामीण सड़कों पर 22,500 करोड़ रुपए खर्च होते हैं, लेकिन 20,000 करोड़ की सड़कें ध्वस्त हो जाती हैं। प्लास्टिक से बनी सड़कों से यह नुकसान भी कम हो जाएगा। भारत में प्लास्टिक के पुनर्चक्रण की प्रक्रिया शुरू होने के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि 2018 में प्लास्टिक का बाजार, प्रसंस्करण सामग्री के रूप में 18 लाख मीट्रिक टन तक पहुंच जाएगा।
जीवाणु दिलाएगा प्लास्टिक के अपशिष्ट से मुक्ति-
हम सब यह भली-भांति जानते हैं कि अंतत: हम किसी नई वस्तु का निर्माण प्रकृति में उपलब्ध तत्वों का कायांतरण करके ही करते हैं। इसलिए इन तत्वों से निर्मित वस्तु के बाद जो भी अपशिष्ट बचते हैं, प्रकृति भी उसे प्राकृतिक रूप से नष्ट करने की व्यवस्था करती है, जिससे प्रकृति का संतुलन बना रहे। कुछ साल पहले वैज्ञानिकों ने ऐसे फंगस पाए थे, जो प्लास्टिक को नष्ट करने की क्षमता रखते थे। अब जापानी वैज्ञानिकों ने ऐसे जीवाणु (बैक्टीरिया) खोजे हैं, जो प्लास्टिक अपशिष्ट को और तीव्रता से नष्ट करते हैं।
जापान के क्योटो इंस्टीट्यूट ऑफ प्रौद्योगिकी के कोडियो-ओडा के समूह ने इस जीवाणु की खोज की है। ‘साइंस’ जनरल के मुताबिक इसका नाम इडियोनेला सेकेन्सिस है। ये जीवाणु पतली फिल्म वाली प्लास्टिक को 30 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर छह सप्ताह में खत्म कर देते हैं। इनके शरीर से निकलने वाले एंजाइम इसे टेरेप्थौलिक अम्ल और एथलीन ग्यालकोल में बदल देते हैं। इस रूप में ये पर्यावरण के लिए हानिकारक नहीं रह जाते हैं। जीवाणु इन्हें पचाने में भी सक्षम होते हैं। बहरहाल प्लास्टिक अपशिष्ट का सुनियोजित व वैज्ञानिक ढंग से व्यापाक स्तर पर निष्पादन शुरू हो जाता है, तो इससे होने वाले प्रदूषण से तो निजात मिलेगी ही, नए रोजगार का सृजन भी होगा। प्लास्टिक को जैविक तरीके से खत्म किया जाना इसलिए आवश्यक है, क्योंकि इसे जलाकर नष्ट करने से कॉर्बन डाइऑक्साइड, कॉर्बन मोनोऑक्साइड एवं डाईऑक्सीन्स जैसी विषैली गैसें उत्सर्जित होती हैं। जो अनेक तरह की बीमारियों को जन्म देती है, इसलिए इसका जैविक रूप से नष्ट किया जाना जरूरी है।