“समाज का जाति अनुसार विचार करने वाले प्रगतिशील महानुभावों द्वारा संघ को मनुवादी कहते देखकर मेरे क्रोध की सीमा न रही। हिंदू समाज का अस्तित्व उन्हें स्वीकार नहीं था। परंतु जातीय अहंकार, जातीय भावना भड़काने से उन्हें कोई एतराज नहीं था। जातीय भावना भड़काकर समता पर आधारित समाज रचना करने का उपदेश करना यह उनके ढोंगीपन की सीमा थी।”
1975 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा की। उसी वर्ष मई महीने में संघ शिक्षा वर्ग के तृतीय वर्ष की शिक्षा के लिए मैं नागपुर गया था।
नागपुर का शिक्षा वर्ग पूरा होने के बाद संघ कार्य से समय निकालकर अर्थार्जन की दृष्टि से कुछ करना आवश्यक था। सिलाई का काम मुझे अच्छी तरह आता था। एम. ए. तक की पढ़ाई भी पूरी हो चुकी थी। अपनी सिलाई की दुकान खोलना या नौकरी करना यही दो विकल्प मेरे सामने थे। मेरी बहनें भी बड़ी हो गई थीं। उनके विवाह की भी जिम्मेदारी थी।
हम कई बार कुछ करने की सोचते हैं परंतु विधाता के मन में कुछ और ही होता है। जून में शिक्षा वर्ग पूरा होने के बाद मैं वापस आया और 26 जून को आपातकाल की घोषणा हुई। उसके तुरंत बाद संघ पर पाबंदी लगाई गई। मुंबई के सब प्रमुख संघ कार्यकर्ता मीसा के अंतर्गत बंदी बनाए गए। दूसरी श्रेणी के मेरे जैसे कार्यकर्ता जेलों के बाहर थे। ऐसे समय अर्थार्जन के लिए संघ कार्य छोड़ना कायरता का लक्षण होता। अपने संगठन पर संकट आया है और उसका सामना करना ही चाहिए, ऐसा पक्का निश्चय मैंने किया और उसी हेतु भूमिगत हो गया। आपातकाल की घोषणा के विरुद्ध कड़ा संघर्ष करने का निश्चय संघ ने किया था। सर्वव्यापी सत्याग्रह हुआ। भूमिगत रहकर मैं सत्याग्रही जुटाने में लग गया। उनकी टुकड़ियां बनाकर सत्याग्रह के लिए भेजना, धन इकट्ठा करना, स्वयंसेवकों का मानसिक बल बनाए रखना, इन सब कामों में मैं व्यस्त रहने लगा।
संघ के अनेक वरिष्ठ अधिकारी भी भूमिगत थे। उनके रहने के लिए मेरे क्षेत्र में सुरक्षित निवास की व्यवस्था करना, उनकी बैठकों की योजना बनाना, आदि कार्य भी मैं ही करता था। उस समय पुलिस का बड़ा डर लगता था। यदि पकड़ा गया तो वे मारेंगे, जानकारी उगलवाने के लिए शारीरिक अत्याचार करेंगे, इसका डर सदैव लगा रहता था। उन दिनों पुलिस के मतलब की बहुत सी बातें मुझे ज्ञात होती थीं। संघ के सरकार्यवाह माधवराव मुले का निवास स्थान कहां है? मोरोपंत पिंगले कहां ठहरे हैं? दत्तोपंत ठेंगड़ी कहां हैं? संघ की केन्द्रीय समिति की बैठक कहां होने वाली है? आदि बातों की जानकारी मुझे होती थी। यदि पुलिस ने पकड़ा तो उनके द्वारा किए जाने वाले अत्याचारों को सहन करने की आत्मिक शक्ति भगवान मुझे दे, ऐसी प्रार्थना मैं रोज करता था।
आपातकाल का मानसिक दबाव कभी-कभी असह्य हो जाता था और उससे छुटकारा पाने के लिए मैं एक ही दिन में दो-दो सिनेमा देखता था। इन्हीं दिनों श्री दत्तोपंत ठेंगड़ी से अत्यंत निकट का परिचय हुआ। उनकी व्यवस्था करने के निमित्त उनके साथ दीर्घकाल तक रहने का भी अवसर मिला।
दत्तोपंत जी की संगत में भी मैंने उनसे विचार-विनिमय कभी नहीं किया। आपातकाल के बारे में मैंने उनसे सिर्फ एक बार और वह भी एक ही प्रश्न पूछा था। “आपातकाल कब तक समाप्त होगा?” और आपातकाल यदि लम्बे समय तक जारी रहा तो संघ का क्या होगा?” इस पर दत्तोपंत का जो उत्तर था, उसने मुझे गंभीरता से विचार करने पर बाध्य किया। उन्होंने कहा था, “आपातकाल दीर्घ समय तक नहीं चलेगा और उसमें संघ विजयी होगा। संघ का क्या होगा, इसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कार्यकर्ता को, अपना क्या होगा, इसकी चिंता रहती है और अपनी चिंता को ही वह संगठन की चिंता समझता है। अपना कार्य ईश्वरीय कार्य है। उसकी विजय की चिंता हमें नहीं करनी चाहिए। हमें सिर्फ हमारे कंधों पर डाली गई जिम्मेदारी की ही चिंता करनी चाहिए, वह अधिक उपयुक्त है।” उसके बाद संघ का क्या होगा? ऐसी निरर्थक चिंता करना मैंने छोड़ दिया।
जिस बात का मुझे सबसे अधिक डर लग रहा था, वह आखिर हो ही गई। मैं पुलिस के जाल में फंस गया। जनसंघर्ष समिति के मुख्य सचिव श्री रवींद्र वर्मा को एक बैठक के लिए अंधेरी से पार्ला ले जाने का काम मुझे सौंपा गया था। रवींद्र वर्मा घाटकोपर से आने वाले थे। रवींद्र वर्मा नियोजित जगह पहुंचे। उन्हें दूसरी टैक्सी से ले जाना था। मैं टैक्सी की तलाश में था तभी 15-16 पुलिस वालों ने हमें घेर लिया। वे सब सादे वेश में थे। सहायक पुलिस आयुक्त श्री मोकाशी ने रवींद्र वर्मा का हाथ पकड़कर कहा, “वर्मा साहब आपको गिरफ्तार किया जाता है।”
मुझे आने में देर क्यों हो रही है, यह देखने के लिए पार्ला से श्री भीमसेन राणे आए। वे उस समय प्रचारक थे। पुलिस ने उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया। हम सबको पहले अंधेरी के आई. बी. कार्यालय व वहां से क्रॉफर्ड मार्केट पुलिस मुख्यालय ले जाया गया। मेरा और श्री भीमसेन का बयान लिया गया। रवींद्र वर्मा को अलग बैठाया गया।
मेरी और भीमसेन की अब अच्छी धुलाई होगी ऐसा लगता था। परंतु पता नहीं क्यों पुलिस ने अधिक पूछताछ की ही नहीं। मेरे बयान पर भी उन्होंने आगे कोई विशेष जांच नहीं की। मैं दिन भर क्रॉफर्ड मार्केट पुलिस मुख्यालय में रहा। पुलिस का बर्ताव अत्यंत सभ्य था। रवींद्र वर्मा जैसा बड़ा असामी हाथ लगने का उन्हें आनंद हुआ होगा या शायद उन्हें भी हमारे संघर्ष के प्रति सहानुभूति रही होगी।
सायंकाल हम तीनों को, यानी मैं, रवींद्र वर्मा और भीमसेन को ठाणे कारागृह भेज दिया गया। हमारे विरुद्ध ‘मीसा’ लगाया गया था।
ठाणे कारागृह में मैं चौदह महीने रहा। इन चौदह महीनों का कालखण्ड सच्चे अर्थ में मेरे जीवन में समग्र परिवर्तन लाने वाला सिद्ध हुआ। समाजवादियों का भी एक बड़ा गुट हमारे साथ था। दत्ताजी ताम्हणे उसी गुट में थे। समाजवादी साथी भाइयों की असलियत क्या है, इसका दर्शन ठाणे कारागृह में अत्यंत निकट से करने का सौभाग्य मुझे मिला। संघ का द्वेष प्रत्येक समाजवादी के रक्त और हड्डियों में अंदर तक बैठ गया है। संघ द्वेष यदि उनके जीवन से निकाल दिया जाए तो उनके अस्तित्व का कोई आधार ही नहीं रह जाता। कारागृह की छोटी-छोटी बातों में भी उनकी द्वेष भावना उभरकर सामने आती थी।
हम सब जन संघर्ष समिति के कार्यकर्ता होने के नाते कारागृह में डाले गए थे। आपातकाल के खिलाफ हम सबको एकत्रित होकर लड़ना था। इस कारण प्रारंभ में कारागृह के कुछ कार्यक्रम एकत्रित रूप से करने का प्रयत्न किया गया। वहां संघ के स्वयंसेवकों की संख्या सबसे अधिक होने के कारण कार्यक्रमों पर हमारा प्रभाव तो रहता ही था। एक कार्यक्रम में संघ की पद्धति के अनुसार प्रारंभ में एक गीत होने वाला था। गीत मुझे ही गाना था। जैसे ही मैं गीत गाने के लिए खड़ा हुआ, चार समाजवादी साथी भी उनकी योजनानुसार उठ खड़े हुए और उन्होंने गीत गाने का विरोध किया। इस कार्यक्रम में गीत नहीं होगा, यह उनका आग्रह था। अंत में बिना गीत गाये ही कार्यक्रम हुआ।
प्रत्येक वार्ड का रसोई खाना अलग था। परंतु सबका भोजन एक साथ ही होता था। प्रारंभ करते समय हम ‘सहनाववस्तु’ मंत्र का उच्चारण करते थे। लेकिन सबकी पंगत में भोजन के लिए बैठा हुआ समाजवादी भाई नमक परोसते ही (महाराष्ट्र में थाली में पहले नमक परोसा जाता है।) भोजन की शुरुआत कर देता था। ‘सहनाववस्तु’ मंत्र से उसे छूत लग जाती थी। ऐसी छोटी-मोटी बातों के कारण हमारे और उनके बीच एक प्रकार का तनाव सदैव बना रहता था। संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी पांडुरंग शास्त्री क्षीरसागर, बाबासाहब घटाटे, दत्ता ताम्हणे, रवींद्र वर्मा सामंजस्य बनाए रखने का पूरा प्रयास करते रहते थे; फिर भी एकसाथ कार्यक्रम करने का आग्रह हमें छोड़ देना पड़ा व संघ तथा समाजवादी भाइयों के कार्यक्रम अलग-अलग होने लगे। समाजवादियों ने जनता पार्टी क्यों तोड़ी, इसका उत्तर कारागृह में जनता पार्टी की स्थापना होने के पहले ही मिल गया था।
महाराष्ट्र के समाजवादियों में संघ के प्रति इतनी घृणा, इतनी अधिक द्वेष भावना, असीम अहिष्णुता क्यों निर्माण हुई, यह शोध का विषय है। तात्त्विक भूमिका के आधार पर हर समाजवादी, मानवतावादी होता है, इसमें सर्वधर्म समभाव होता है, प्रेम से सारा संसार जीतने की उसकी इच्छा होती है, परंतु संघ के बारे में वह फासिस्ट होता है। संघ को समूल नष्ट करने की उसकी प्रबल इच्छा होती है। उसमें यह वैचारिक अंतर्विरोध क्यों होता है?
अपनी दृष्टि से मैं इस प्रश्न का उत्तर ढूंढ़ने का प्रयत्न करता हूं। समाजवादी साथी साने गुरुजी को बहुत मानते हैं। उनके वैचारिक संस्कारों से प्रभावित ऐसे लोगों की एक पूरी की पूरी पीढ़ी महाराष्ट्र के सामाजिक और राजनैतिक क्षेत्रों में कार्यरत रही। साने गुरुजी का साहित्य, उनका जीवन, उनका तत्त्वज्ञान आदि बातों का परिणाम इन समाजवादियों पर बहुत गहराई तक हुआ है। संघ के बारे में साने गुरुजी की राय अच्छी नहीं थी। साने गुरुजी के विचारों का बहुत गहरा वैचारिक संस्कार समाजवादी साथियों के मन पर हुआ है।
कारागृह में कोई काम न होने के कारण मैंने पुस्तकें पढ़ना शुरू किया। परीक्षा की तैयारी करते समय रूसी राज्य क्रांति, अमेरिकी राज्य क्रांति, फ्रेंच राज्य क्रांति के बारे में पाठ्यपुस्तकों में थोड़ा बहुत पढ़ा था। अब फिर से, अधिक विस्तार से इन विषयों को पढ़ा। अपने देश की वैचारिक परम्परा पर इन घटनाओं का परिणाम हुआ है, इस कारण उनका अध्ययन करना आवश्यक था।
ठाणे कारागृह में ही मैंने सर्वप्रथम डॉ. बाबासाहब आंबेडकर का चरित्र पढ़ा। उस समय तक मेरे मन में उनके लिए कोई विशेष श्रद्धा नहीं थी। जिसने हिंदू धर्म का त्याग किया, उसके प्रति एक कट्टर हिंदुत्चवादी के मन में प्रेम क्यों होगा? धनंजय कीर लिखित डॉ. बाबासाहब का चरित्र पढ़कर मैं दहल सा गया। डॉ. बाबासाहब का चरित्र पढ़ने के बाद ही मेरे भीतर का चिंतक जागृत हुआ। जिस हिंदू समाज का संगठन करने के लिए मैं अपनी पूरी शक्ति लगाकर काम कर रहा था, उस हिंदू समाज की मुझे सच्ची पहचान नहीं थी। डॉ. बाबासाहब के चरित्र ने मेरे मन में इसका भान कराया। हिंदू समाज की भयानक अस्पृश्यता का दर्शन डॉ. बाबासाहब के जीवन में होता है।
हिंदू समाज विघटित क्यों हुआ? जातिभेद ने समाज को दुर्बल कैसे बनाया? अस्पृश्यता के कारण समाज की क्या हानि हुई? जातीय अहंकार, राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न करने के काम में कैसे बाधक होता है? जातिभेद का तत्त्वज्ञान कैसे विकसित हुआ? उच्च वर्ण के लोगों का ही अधिकार बना रहे इसलिए धर्मशास्त्र में कैसी व्यवस्था की गई? यह सब बातें डॉ. आंबेडकर का चरित्र पढ़ने के बाद ही ध्यान में आती हैं।
डॉ. बाबासाहब का चरित्र पढ़ने के बाद एक और बात ने मुझे बड़ा व्यथित किया। कारागृह में जाने तक मैं मुंबई शाखा का एक प्रमुख संघ कार्यकर्ता हो गया था। जब मेरे जैसे एक प्रमुख कार्यकर्ता को डॉ. बाबासाहब और अपने ही समाज के बारे में इतना असीम अज्ञान है तो सामान्य स्वयंसेवक की क्या अवस्था होगी? यह प्रश्न बहुत व्यथित करने वाला था। यदि मन में कोई प्रश्न ही नहीं उठता तो उसका उत्तर ढूंढ़ने की कोई आवश्यकता भी नहीं होती। ऐसा होने पर आत्मसंतुष्टि, अथवा अल्प संतुष्टता अपने आप निर्माण होती है। डॉ. बाबासाहब के चरित्र ने मेरे मन में असंख्य प्रश्न निर्माण किए और मुझे उनका उत्तर ढूंढ़ने के लिए प्रेरित किया।
कारागृह में डॉ. आंबेडकर का चरित्र पढ़ने के बाद मैंने संघ प्रचारक बालासाहब दीक्षित से पूछा था कि क्या गांवों में आज भी अस्पृश्यता है? बालासाहब मराठवाड़ा के प्रचारक थे। उन्होंने बताया कि ग्रामीण भागों में आज भी अस्पृश्यता है और बड़ी कठोरता से उसका पालन किया जाता है। होटलों में अस्पृश्यों के लिए चाय की प्याली-तश्तरी वगैरह अलग रखी जाती है। यह सब सुनने के बाद मैंने उनसे पूछा कि हम अस्पृश्यों के लिए क्या करते हैं? क्या हम उन्हें शाखा में लाने का कोई विशेष प्रयत्न करते हैं? अस्पृश्यों के प्रति समाज में होने वाली भावना को बदलने के लिए हम क्या करते हैं? कारण संघ के नाते अस्पृश्यता निवारण के लिए हम विशेष रूप से कुछ भी नहीं कर रहे थे।
मेरी एक आदत है कि किसी का भी चरित्र पढ़ने के बाद मैं मन ही मन उसकी तुलना डॉ. हेडगेवार के जीवन से करने लगता हूं। किसी अन्य स्वयंसेवक की तरह डॉ. हेडगेवार का जीवन मेरे लिए भी प्रेरणा का एक महत्त्वपूर्ण स्रोत है। उनके जीवन कार्य के विषय में मन में सतत चिंतन होता रहता है। डॉक्टर साहब के बारे में मेरे मन की स्थिति संत तुकाराम के शब्दों में “जेथे जातो तेथे तू माझा सांगाती। चालविशी हाती धरोनिया” (मैं जहां जाता हूं वहां तेरा ही साथ रहता है। मेरा हाथ पकड़कर तू मुझे चलाता है।) ऐसी होती है।
डॉ. हेडगेवार ने हिंदुओं की कर्म चेतना को जगाया तो, डॉ. बाबासाहब ने हिंदुओं की विचार शक्ति जागृत की। उसे विचार करना, बोलना, अपने विचार अभिव्यक्त करना सिखाया। यह सब मेरा व्यक्तिगत मत अथवा चिंतन है। डॉ. बाबासाहब का जीवन चरित्र हमें क्यों नहीं सिखाते? हम उनकी उपेक्षा क्यों करते हैं? कारागृह में ऐसे प्रश्न मुझ तक ही सीमित रहते थे। आयु से बड़ा न होने पर भी संघ कार्य की जिम्मेदारी के हिसाब से मैं एक ज्येष्ठ कार्यकर्ता था, इसलिए मेरे जैसे व्यक्ति द्वारा ऐसे प्रश्न रखना तर्कसंगत नहीं लगता। सच पूछा जाए तो एक कार्यकर्ता होने के नाते मुझसे तो ऐसे प्रश्नों का उत्तर अपेक्षित था।
मेरे मन में उठने वाले प्रश्न केवल मुझ तक ही सीमित नहीं थे। ऐसे ही प्रश्न उस समय और भी अनेक कार्यकर्ताओं के मन में थे।
संघ ब्राह्मणों का है, संघ विषमतावादी है, संघ वर्ण व्यवस्था का समर्थक है, ये वाक्य मुझे कारागृह में जाने के पहले से ही मालूम थे। परंतु संघ ब्राह्मणों का है, इस वाक्य में कौन सा जहर मिला है, यह उस समय तक मेरी समझ में नहीं आया था। कारागृह में समाजवादी साथियों की संगत में रहने और उनका साहित्य पढ़ने के बाद इन सब वाक्यों का जातीय संदर्भ मेरी समझ में आता गया।
ब्राह्मण-अब्राह्मण विवाद की यह पार्श्वभूमि समझने का प्रयास मैं धीरे-धीरे कर रहा था। उसी समय अन्य अनेक बातें भी मेरे ध्यान में आने लगीं। समाजवादी प्रेरणा स्वीकार करने वालों का तर्कशास्त्र भी धीरे-धीरे मेरी समझ में आने लगा। समाजवादी विचारों वाले लोग खुद को प्रगतिशील याने मानवतावादी, जातीय विचार न करने वाला, सांसारिक बातों का विचार करने वाला-इहवादी, धर्म को अस्वीकार करने वाला तार्किक, धर्म प्रत्येक व्यक्ति के लिए व्यक्तिगत बात है, सब धर्म एक समान हैं, यह सब बातें मानने वाला प्रगतिशील विचारों का होता है, ऐसा अर्थ लगाया जाता है।
समाजवादी तर्कशास्त्र के अनुसार सारे हिंदुत्ववादी-जातीयवादी, फासिस्ट मनोवृत्ति के, मध्य युगीन मानसिकता वाले, धार्मिक पागलपन निर्माण करने वाले, हिंसा में विश्वास रखने वाले होते हैं और इसलिए वे मानवता के शत्रु और मानवता के संहारक हैं। संघ में ब्राह्मण बहुसंख्यक हैं। संघ के प्रमुख अधिकारी पदों पर ब्राह्मण हैं और ब्राह्मणत्व एक महाभयानक बात है। संघ में ब्राह्मण हैं, विषमतावादी, अपना धार्मिक और जातीय वर्चस्व अबाधित रखने वाले ऐसे ब्राह्मण संघ चलाते हैं इसलिए संघ भी विषमतावादी, जातीय भेद बढ़ाने वाला, शूद्रों को गुलामी में रखने वाला है। वामपंथियों का यह तर्कशास्त्र किसी गंवार, मूर्ख व्यक्ति को ही धोखे में डाल सकता है।
हॅट्स ऑफ हंसराज खन्ना
आपातलाकाल के दौरान मीसा बंदी में मैं जेल तो गया, परंतु मीसा कानून क्या है, आपातकाल किस धारा के अंतर्गत लगाई गई, वह लादने के प्रमुख कारण क्या थे, ये बातें मुझे संविधान का अध्ययन करने के बाद समझीं। इंदिरा गांधी नहीं यह नहीं जानती थीं कि संविधान की धारा 352 आपातकाल की है। यह धारा लगाने की सलाह उन्हें वकील तथ पं.बंगाल के तत्कालीन मुख्य मंत्री के सिद्धार्थ शंकर रे ने दी थी। इंदिरा गांधी का लोकसभा चुनाव अलाहबाद उच्चन्यायालय ने रद्द कर दिया था। 6 साल तक उन्हें चुनाव लडने की अनुमति नहीं थी। सर्वोच्च न्यायालय में इस निर्णय के विरुद्ध इंदिरा गांधी ने स्टे की मांग की, जिसे न्यायाधीश कृष्णा अय्यर ने 24 जून को नकार दिया। सर्बोच्च न्यायालय कर द्वारा भी चुनाव रद्द किए जाने की आशंका को देखते हुए इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगा दिया और आपातकाल में व्यक्ति के जीने का अधिकार भी समाप्त कर दिया। इसके विरोध में सर्वोच्च न्यायालय में जो मुकदमा चला उसे एडीएम जबलपुर विरुदध शिवकांत शुक्ला के नाम से जाना जाता है। 5 न्यायाधीशों के न्यायपीठ के सामने सुनवाई हुई। 5 में से 4 न्यायाधीशों ने मीसा में जीवन समाप्त किया जा सकता है ऐसा निर्णय दिया परंतु हंसराज खन्ना ने अपना अलग निर्णय दिया। उनके निर्णय का सार था कि व्यक्ति के जीने का अधिकार प्राचीन है, पवित्र है। ऐसा नहीं कि केवल संविधान में उसे मान्यता है, वह तो स्वयंभू है। इसका अर्थ हुआ कि मीसाबंदियों को मारा नहीं जा सकता। ऐसा निर्णय देने के कारण हंसराज खन्ना की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश के रूप में नहीं हो पाई। मेरे मन में हंसराज खन्ना के प्रति उच्चकोटि का श्रद्धाभाव अपने आप निर्माण हो गया। क्योंकि हंसराज खन्ना किसी भी मीसा बंदी को नहीं पहचानते थे। इस प्रकार अपरिचित लोगों के जीवन की रक्षा के लिए जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, वे थे हंसराज खन्ना।
इस कुतर्क को तात्त्विक आधार देने के लिए महात्मा ज्योतिबा फुले व डॉ. बाबासाहब का बड़ी कुशलता से उपयोग किया जाता है। महात्मा फुले अथवा डॉ. बाबासाहब आंबेडकर ने इन दिनों में ब्राह्मणों पर अत्यंत कठोर हमले किए हैं, यह सत्य है। परंतु अब ऐसा लगता है कि इन दोनों महापुरुषों का उपयोग, हिंदुत्व द्वेष निर्माण करने के लिए तथा हिंदू समाज का जातियों के आधार पर विभाजन करने के लिए बड़ी खूबी से किया जा रहा है। मैं जैसे-जैसे महात्मा फुले तथा डॉ. बाबासाहब का लिखित साहित्य पढ़ने लगा वैसे-वैसे मेरी यह धारणा पक्की होती गई कि महाराष्ट्र के इन दोनों महापुरुषों को प्रगतिशील लोगों ने, प्रगतिशील जेलों में बंदी बना रखा है। उनके द्वारा प्रतिपादित तत्त्वों को विकृत किया जा रहा है। हमें, अर्थात संघ को कोसने के लिए उनका दुरुपयोग किया जा रहा है और संघ के नाते हम उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं करते। हम निष्क्रिय होकर सारे आघात चुपचाप सहन करते जा रहे हैं।
समाज का जाति अनुसार विचार करने वाले प्रगतिशील महानुभावों द्वारा संघ को मनुवादी कहते देखकर मेरे क्रोध की सीमा न रही। हिंदू समाज का अस्तित्व उन्हें स्वीकार नहीं था। परंतु जातीय अहंकार, जातीय भावना भड़काने से उन्हें कोई एतराज नहीं था। जातीय भावना भड़काकर समता पर आधारित समाज रचना करने का उपदेश करना यह उनके ढोंगीपन की सीमा थी। इसके विरुद्ध तो वैचारिक आंदोलन करना चाहिए, ऐसा लगता था। परंतु केवल मुझे ऐसा लगने का कुछ उपयोग नहीं था। संघ के अधिकारी, कार्यकर्ताओं को भी वैसा लगना आवश्यक था। आपातकाल समाप्त हो गया। हम सब विजयी होकर कारागृह से बाहर आए।

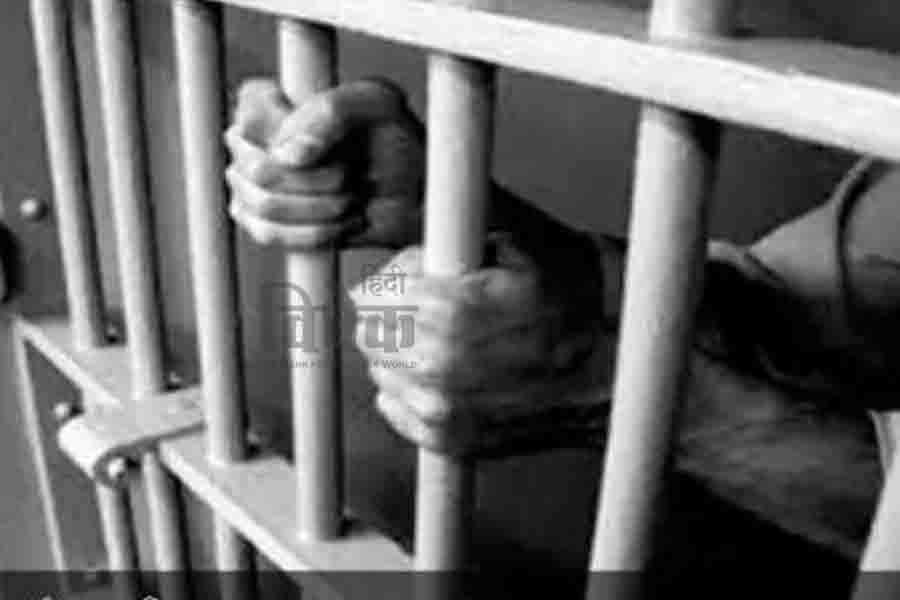


बढीया
सुंदर विवेचन
बहुत ही सुन्दर ।