शरीरी तौर पर मनुष्य और सृष्टि के अन्य जीवों में भेद नहीं है। लेकिन मनुष्य की चेतना में शेष प्रति जिज्ञासा भाव उसमें गुणात्मक अंतर उत्पन्न कर उसमें पृथ्वी के अन्य जीवों की तुलना में उर्ध्व स्थान पर प्रतिष्ठित कर देता है। आदि मानव से आधुनिक मनुष्य तक की विकास यात्रा का यही निष्कर्ष है कि अन्य जीवों की भांति मनुष्य नामक प्राणी की दिनचर्या जन्म से मृत्यु के बीच केवल खाने-सोने तक सीमित नहीं रही। उसकी उर्ध्वगामी चेतना ने प्रकृतिक सदस्यों, जन्म-मृत्यु के कारणों तथा जीवन के उद्देश्यों पर सोचने के लिए विवश किया। एक वर्ग, जिसमें जिज्ञासा रूप में यह चेतना अपने प्रबलतम स्वरूप में उपस्थित रही, उसने स्वयं को प्रकृति और जीवन के उद्देश्यों पर सोचने के लिए विवश किया। उसने स्वयं को प्रकृतिक और जीवन के रहस्यों के चिंतन में ही संलग्न कर लिया। मानवीय प्रज्ञा का उर्ध्वतम रूप वेदों में मिलता है। वेद भारतीय साहित्य के ही नहीं, वरन् विश्व साहित्य के आदि ग्रंथ हैं। वैदिक ऋृषियों ने अपनी असाधारण अध्यात्मिक मेघा से जिन सत्यों का साक्षात्कार किया, कालांतर में वही विस्तार पाकर विभिन्न दार्शनिक सिद्धांतों का आधार बने। वैदिक प्रज्ञात्मकता उपनिषद, आरणयक और शतपथ ब्राम्हण मार्गों को ग्रहण करती हुई दर्शन का विषय बनी। जैसे हर सैद्धांतिकी का एक व्यवहारिक पक्ष होता है, वैदिक प्रज्ञात्मकता के साथ तत्कालीन समाज के कुछ धार्मिक यज्ञ, अनुष्ठान भी जुड़े हुए थे। वेदों का समस्त चिंतन विश्वकल्याण के वृहत्तर उद्देेश्य से जुड़ा है। वृहत्तर समाज दार्शनिक, अध्यात्मिक, धार्मिक चिंतन के मूल स्वरूपों तक यज्ञ याग, यम नियम आदि बाह्य अनुष्ठानों के माध्यम से पहुंचता है। परम्परा से प्राप्त ज्ञान की स्वानुभूत युगानुरूप व्याख्याएं करने वाले आदर्श महापुरुषों का योगदान भी समाज को मिलता रहता है। पूर्णत: आत्मनिष्ठता के साथ समाज में रहते हुए विश्व कल्याण में प्रवृत्त रहने वाले महात्माओं और महापुरुषों को ‘संत’ संज्ञा से अभिहित किया गया है, हमारे शास्त्र-ग्रंथों में आध्यात्मिकता के जो रत्न विद्यमान हैं और जो कुछ भी मनुष्य के अधिकार में मठों और अरण्यों में छिपे हुए हैं, सबसे पहले उन्हें निकालना होगा। जिन लोगों के अधिकार में ये छिपे हुए हैं, केवल वहीं से इस ज्ञान का उद्धार करने से काम न होगा, किंतु उससे भी दुर्भेद्य पेटिका, अर्थात जिस भाषा में ये सुरक्षित हैं, उस शताब्दियों के संस्कृत शब्दों के जाल से उन्हें निकालना होगा। तात्पर्य यह है कि मैं उन्हें सब के लिए सुलभ कर देना चाहता हूं। मैं इन तत्वों को निकालकर सबकी भारत के प्रत्येक मनुष्य की सम्पति बना देना चाहता हूं, चाहे वह संस्कृत जानता हो या नहीं।
उपर्युक्त उदाहरण में स्वामी विवेकानंद जन सामान्य के कल्याण हेतु प्राचीन भारतीय ग्रंथों में बंद गूढ़ ज्ञान के व्यापक प्रचार की आवश्यकता का अनुभव करते हैं। यह कार्य जनता की बोली बानी में ही हो सकता था। भारतीय संतों ने यही तो किया है। आलोच्य ग्रंथ ‘उत्तरी भारत की संत परम्परा’ की भूमिका में लेखक ने स्पष्ट किया है, ‘‘उत्तरी भारत के संतों ने जिस मत का प्रचार किया और जिसे उन्होंने विश्व कल्याण के लिए अव्यक्त आवश्यक समझा, वह कोई नितांत नवीन संदेश न था और न भारतीयों के लिए उसका कोई अंश अपरिचित ही था। उसके प्राय: प्रत्येक अंग का मूल रूप हमारे प्राचीन साहित्य के किसी न किसी भाग में विद्यमान हैं।’’ स्वामीजी के अपेक्षा के अनुसार इन संतों ने अपने मतों का प्रचार-प्रसार भी जनभाषा में ही किया है। उत्तर भारत के संतों ने अधिकतर फुटकर पदों की रचना की है, जो इनकी बानियों के नाम से प्रसिद्ध है। दक्षिण भारत के संतों में ज्ञानदेव और एकनाथ ने प्राचीन संस्कृत ग्रंथों पर अपनी सरल व प्रचलित भाषा में ही टीकाएं व पाली भाषा में रची है। सूफी संतों की भाषा फारसी मिश्रित बोलचाल की हिंदी है। कबीर, जिनको केंद्र में रखकर उक्त ग्रंथ की रचना की गयी है, की भाषा इतनी बोलियों व प्रांतीय भाषाओं मिलकर बनी है कि उसे सधुक्कड़ी भाषा कहा जाता है।
हिमालय से निकलने वाली गंगा अपनी हजारों मील की यात्रा में राह के छोटे-बड़े सभी नदी नालों को समेटती हुई अंतत: गंगासागर में समाहित हो जाती है। किंतु प्राचीन भारतीय आध्यात्मिक ज्ञान की गंगा अपनी अनंत यात्रा में स्वयं को सहस्त्र धाराओं में बांटकर करोड़ों भारतवासियों के हृदयों को रससिक्त करती आ रही है। विभिन्न धार्मिक सम्प्रदाय और संत मत ही ज्ञान गंगा की सहस्त्र धाराएं हैं। संतों द्वारा प्रवर्तित इन्हीं पंथ व सम्प्रदायों की परम्परा का विस्तृत विवेचन श्री परशुराम चतुर्वेदी ने अपने ग्रंथ ‘उत्तरी भारत की संत परम्परा’ में किया है। संत जयदेव से प्रारंभ कर महात्मा गांधी तक संतों के चुनाव में लेखक की दृष्टि की उदारवादी रही है। स्वयं लेखक का वक्तव्य है, ‘‘संत परम्परा के अंतर्गत सम्मिलित किए जाने वाले संतों का चुनाव करते समय सबसे अधिक ध्यान स्वाभवत: उन लोगों की ओर ही दिया गया है जिन्होंने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष ढंग से कबीर साहब अथवा उनके किसी अनुयायी को अपना पथ-प्रदर्शक माना था अथवा जिन्होंने उनके द्वारा स्वीकृत सिद्धांतों और साधनाओं को किसी न किसी प्रकार अपनाया था। फिर भी यहां कुछ ऐसे लोगों को भी स्थान देना पड़ गया है जो सूफियों, सगुणोपासकों, नाथपंथियों व अन्य ऐसे सम्प्रदायों के साथ सम्बद्ध रहते हुए भी संत-परम्परा में गिने जाते आए हैं और जो अपने संतमतानुकूल सिद्धांतों वाली रचनाओं के आधार पर भी उक्त संतों के अत्यंत निकटवर्ती समझे जा सकते हैं। संतों की ‘रहनी ’ में रचित होने वाला ‘सहजभव’ एक ऐसी विशेषता है जो किसी भी असाधरण व्यक्ति के जीवन स्तर को बहुत ऊंचा कर देती है। महात्मा गांधी ने कबीर साहब आदि संतों की भांति पदों या सखियों की रचना नहीं की और न उनकी भांति उपदेश देते फिरने का ही कोई कार्यक्रम रखा। परंतु जिस प्रकार उन्होंने अपने निजी अनुभवों के आधार पर अपने सिद्धांत स्थिर किए और उन्हें अपने जीवन के प्रत्येक दल में व्यवहार कर दिखलाया, वह ठीक उन संतों के ही अनुसार था।’’
भारत में संत परम्परा की देन और ‘उत्तरी भारत की संत परम्परा’ ग्रंथ के महत्व को जानने के लिए भारतीय साधना के इतिहास को खंगालना ही पड़ेगा। प्राचीन वाड मय के अध्ययन से पता चलता है कि हमारे पूर्वजों का जीवन अत्यंत सरल था। उनके धार्मिक अनुष्ठानों के प्रधान अंग देव-पूजन, पितृ पूजन व यज्ञ थे तथा प्रार्थना के द्वारा वे अपनी अभीष्ट ऐहिक सुख के लिए प्राकृतिक शक्तियों में निहित कल्पनात्मक देवरूपों से याचना भी किया करते थे। 8वीं-9वीं शताब्दी तक आते-आते वेदकालीन साधना पद्धतियां अनेक संशयों, मिथ्याचार व पाखंडों में फंस गईं जिससे साधना के क्षेत्र में अराजकता सी लक्षित होने लगी। ऐसे ही अवसर पर स्वामी शंकराचार्य ने अपने अद्वैतवाद के अंतर्गत अवैदिक मतों के अमान्य ठहराया, वैदिक मतों में भी उपलब्ध दोषों की निंदा कर उन्हें वेद विरुद्ध घोषित किया। बौद्धों व जैनों के सुधारक सम्प्रदायों, नाथयोगियों तथा वैष्णव सहजिया संतों ने बिना प्रामाण्य ग्रंथों का सहारा लिए स्वतंत्र रूप से प्रचलित बुराइयों को सरल व व्यवहारिक बातों द्वारा बदलने की चेष्टा की। वारकरी सम्प्रदाय ने बीच का रास्ता अपनाते हुए प्राचीन धर्मग्रंथों को आधार बनाकर उनके मतव्यों को व्यापकता प्रदान की। सूफी सम्प्रदाय में अपने मूल धार्मिक ग्रंथ ‘कुरान शरीफ’ व ‘हदीस’ के प्रति पूरी आस्था लक्षित होती है, किंतु उनकी बातों को एक विशेष दृष्टिकोण से व्याख्या करते हुए ‘इश्क मजाजी’ को आवश्यक माना । संत-परम्परा जिसका विवेचन ‘उत्तरी भारत की संत-परम्परा’ ग्रंथ में किया गया है का सूत्रपात ‘गीत गोविंद’ के रचयिता मस्त कवि जयदेव के समय 13वीं शताब्दी में हो चुका था, किंतु इसकी निश्चित रूपरेखा उसने दो सौ वर्ष पीछे कबीर साहब के जीवन काल में उनके क्रांतिकारी विचारों द्वारा प्रकट हुई। कबीर तथा उनके पूर्ववर्ती एवं समसामायिक संतों की प्रवृत्ति अपने मत को किसी वर्ग विशेष के साम्प्रदायिक रूप में ढालने की नहीं थी। वे अपने विचारों को व्यक्तिगत अनुभवों पर आश्रित समझते थे। परिस्थिति की निष्पक्ष आलोचना उसके आधार पर निश्चित किए गए स्वतंत्र विचार और उसी के द्वारा वे विश्व कल्याण में भी सहायता पहुंचाने में विश्वास रखते थे। इस संत परम्परा में मनुष्य मात्र के प्रति समदर्शिता का जो भाव और दृष्टि है वह वैदिक ऋषि की ‘सर्वे भवन्तु सुखिन:’ का परिवर्तित लोक-स्वर ही है।
संत कबीर, नानक, रविदास, कमाल, धन्ना भगत आदि संत कवि एक ओर भारतीय जनता को उसकी मूल धार्मिकता, आध्यात्मिकता एवं सांस्कृतिकता से जोड़ने में लगे थे तो दूसरी ओर साम्प्रदायिक आडंबरों, असामजिक उच्छृंखलताओं, आडंबरों, टोनो-टोटकों व अंधविश्वासों के खिलाफ भी उन्हें लड़ना पड़ना। धर्मांतरण और राज्य-साम्राज्य स्थापना के उद्देश्य से जड़े जमा चुकी मुस्लिम सेमेटिक आक्रमणकारी शक्तियां भारतीय समाज को संस्कृतिच्युत व पूर्णत: अस्मिताहीन करने पर आमदा थीं। संत कवियों ने पूरी शक्ति से इस आंधी का सामना किया तथा भारतीय आस्था को डिगने नहीं दिया। यही कारण ह भारतीय इतिहास और राजनीति की पराजय संस्कृति या अस्मिता की पराजय नहीं बन सकी। अपने दर्शन, चिंतन, काव्य, कला, समाज और राजनीति आदि को समेटने में हमें बड़ी मशक्कत करनी पड़ी। हम लंबे समय तक अंधकार में रहे, परंतु नि:शेष नहीं हुए थे। इस सबका श्रेय हमारे भक्त कवियों एवं संत परम्परा को जाता है। कुछ यही परिस्थितियां बीसवीं सदी में गांधीजी के समय में उपस्थित हुई थीं। गांधी ने भी नरसी मेहता इकतारे के क्षीण स्वर और अहिंसा सत्याग्रहियों के पैरों की आहट के सहारे सांस्कृतिकता के महायज्ञ में जिसमें कबीर-नानक आदि ने शब्द के प्रथम आहुति दी थी, कर्म की पूर्णाहुति प्रदान की।
कबीर और गांधी के युग में सेमेटिक इस्लाम व ईसाइयत के आक्रमणों की प्रकृति जहां धर्मांतरण या राज्य स्थापना तक सीमित थी, वहां आज यह अर्थ और विज्ञान के नए आयुधों के साथ सक्रिय है। साम्राज्य की अवधारणा अब बाजार या विश्वव्यापी बाजार के रूप में मूर्त की जाने लगी है। इस परिवर्तन का प्रभाव शिक्षा, आचार-विचार, कला, साहित्य, संगीत सब पर आश्चर्यजनक रूप से होने लगा है। वस्तुत: वह सब प्रकार की अस्मिताओं के अपहरण का सर्वभक्षी सेमेटिक षडयंत्र है। इसलिए आधुनिक काल में मनुष्य जाति में से मनुष्यत्व का बोध ही समाप्त कर दिए जाने का षडयंत्र है। इस कुटिलता के बाद भी यदि मनुष्य बचा भी रहता है, तो उसमें और पशु में कितना और कैसा अंतर होगा, यह कह पाना कठिन है। श्री परशुराम चतुर्वेदी का ग्रंथ ‘उत्तरी भारत की संत परम्परा’ का अध्ययन निश्चित ही हमें मनुष्यता के सामने खड़े अस्तित्वहीनता के संकट से जूझने की शक्ति और मार्गदर्शन दोनों ही प्रदान करेगा।

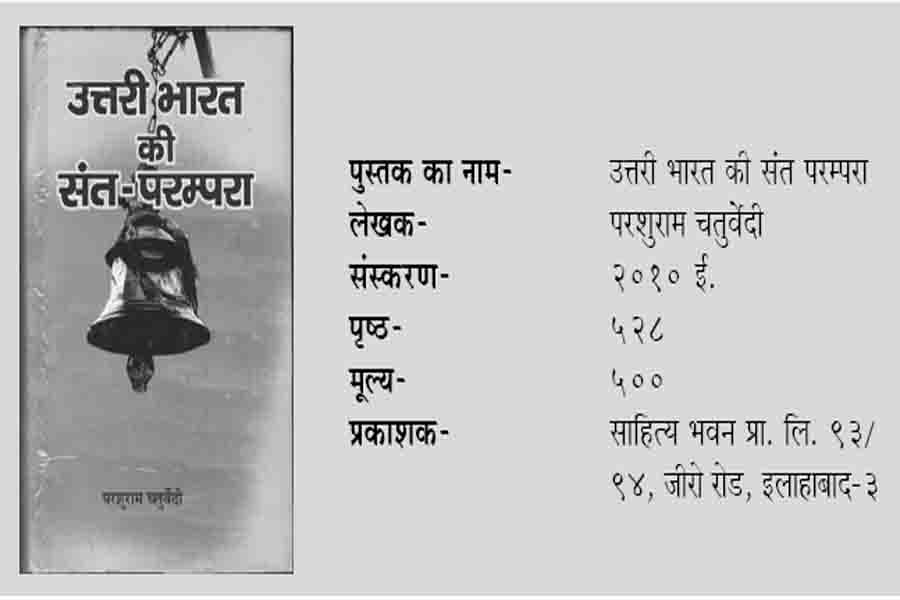
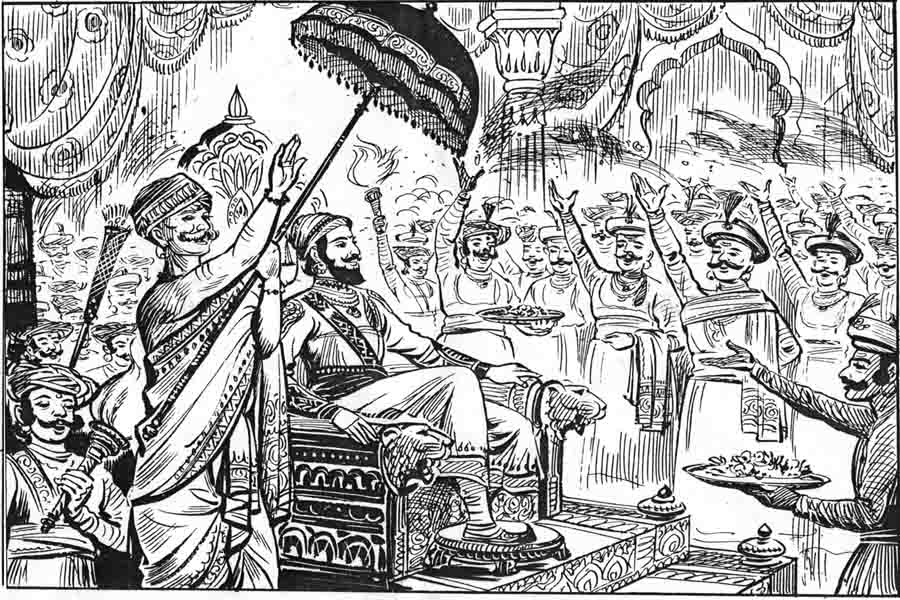

खेद पूर्वक कहना चाहता हूँ कि इस ग्रंथ में श्री प्राणनाथ जी के संदर्भ में लिखा हुआ बहुत कुछ यथार्थ सत्य नहीं है | अधिक जानकारी के लिए श्री निजानंद (प्रणामी) संप्रदाय के इतिहासकार कुंज बिहारी सिंह इटावा का संपर्क करें: +919411239277 | श्री प्राणनाथ टीवी सीरीअल, छत्रसाल वेब सीरीज देखें | श्री प्राणनाथ वैश्विक चेतन अभियान : मनुकूमार पटेल: +917874151371