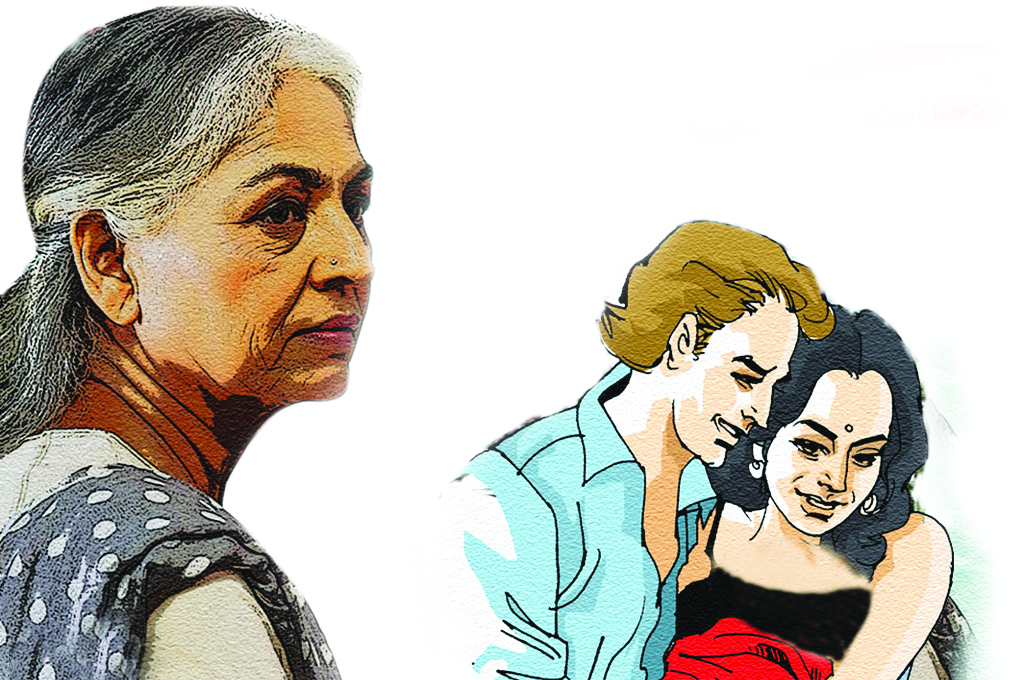वैज्ञानिकों ने तकनीकी जांच में पाया कि इन पत्थरों को बनाने के लिए एक आयताकार खाई तैयार की गई, जिसमें ग्रेनाइट पत्थर का चूर्ण, गन्ने से निर्मित चीनी (केन शुगर), नदी की रेत और कुछ अन्य यौगिक डालकर एक मिश्रण तैयार किया। इस मिश्रण से नींव भरी गई और विभिन्न आकार के छिद्रयुक्त पत्थर तैयार किए गए।
भारत ही नहीं वर्तमान दुनिया में केवल पांडुलिपियों और पुस्तकों को ज्ञानार्जन का आधार माना जाता है। इसीलिए भारत में जब आक्रांता आए तो उन्होंने मंदिरों और पुस्तकालयों का एक साथ विनाश किया। नालंदा विश्वविद्यालय इसका प्रमुख उदाहरण है। यहां के पुस्तकालय में करीब दो लाख पांडुलिपियां सुरक्षित थीं। इनमें खगोल विज्ञान, गणित, ज्योतिष, वास्तुशास्त्र, आयुर्वेद, युद्धकला, पशु चिकित्सा और धर्म संबंधी पांडुलिपियां थीं, जिनमें ज्ञान का अकूत भंडार था। इसी तरह जो भी भारत के प्राचीन मंदिर हैं, वे खगोल विज्ञान, भौतिकी, प्रकृति और ब्रह्मांड के रहस्यों की खुली किताब को मूर्तियों के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं। मूर्ति और स्थापत्य कला के भी ये मंदिर अद्भुत नमूने हैं। भारत ज्ञान के क्षेत्र में अग्रणी न रहने पाए, इसलिए आक्रांता जो भी रहे हों, उन्होंने इन दोनों ही प्राचीन धरोहरों को नष्ट करने का काम निर्ममतापूर्वक किया।
तुर्की शासक बख्तियार खिलजी ने 1199 में इस पुस्तकालय में आग लगाई थी। ये दो लाख पुस्तकें और पांडुलिपियां करीब तीन माह तक सुलगती रही थीं। आग लगाने के जिस कारण को लेकर खिलजी को भारतीय वैद्याचार्य के प्रति कृतज्ञता जताने की जरूरत थी, उसके बदले में उसने पुस्तकालय को तो अग्नि को होम किया ही, अनेक वैद्यों और हिंदू व बौद्ध धर्म के लोगों की भी हत्या कर दी थी। इसी समय खिलजी ने बौद्धों द्वारा शासित राज्यों को अपने आधिपत्य में ले लिया था। इतिहासकार बताते हैं कि खिलजी एक समय बहुत अधिक बीमार पड़ गया था। उसके साथ आए हकीम उसका उपचार करने में असफल रहे। तब उसने नालंदा विवि के आयुर्वेद विभाग के प्रमुख राहुल श्रीभद्रजी से इलाज कराया। खिलजी ठीक भी हो गया। लेकिन जब उसे यह ज्ञात हुआ कि उपचार की ये पद्धतियां विवि के पुस्तकालय की पांडुलिपियों में सुरक्षित हैं, तब उसने इसे आग के हवाले कर दिया।
कोणार्क का सूर्य मंदिर
इन मुगल शासकों ने कलिंग राज्य को आधिपत्य में लेकर यहां के सूर्यमंदिर को भी नष्ट करने की कोशिश की थी। लेकिन इस कालखंड में यहां गंगवंश के सूर्यवंशी शासक थे। पूरे राज्य की मंदल-पंजी के अनुसार 1278 ईंसवीं के ताम्रपत्रों से पता चला कि यहां 1238 से लेकर 1282 तक यही लोग शासक रहे थे। ये शक्तिशाली सम्राट होने के साथ कुशल योद्धा भी थे। भारत में नरसिंह देव के पिता अनंगदेवभीम ऐसे बिरले शासकों में से एक हुए हैं, जिन्होंने तुर्क-अफगानी हमलावरों को कलिंग (प्राचीन ओडीशा) में न केवल घुसने से रोका, बल्कि इस्लामी शासन के विस्तार पर भी अंकुश लगा दिया था। अनंगभीम देव ने मुस्लिमों को पराजित करने की प्रसन्नता में कोणार्क मंदिर की नींव रखी, जिसे उनके पुत्र नरसिंह देव ने आगे बढ़ाया और फिर अनंगभीम के पोते नरसिंह देव द्वितीय ने इस मंदिर को चुंबकीय तत्व मिश्रित पत्थरों और इस्पात की पट्टियों से कुछ इस विलक्षण ढंग से निर्मित कराया कि भगवान सूर्यदेव की प्रतिमा अधर में स्थापित करने में सफलता प्राप्त कर ली थी। यह प्रतिमा भौतिकी के सिद्धांत पर वायु में प्रतिष्ठित की गई थी। इस मंदिर का निर्माण 1250 में शुरू होकर 1262 में समाप्त हुआ।
कोणार्क का संधि-विच्छेद करने पर ‘अर्क’ का अर्थ ‘सूर्य’ और ’कोण’ के मायने ’कोना’ निकलता है। इस मंदिर की विशेषता मंदिर के गुंबद पर 52 टन का रखा चुंबकीय तत्वों से मिश्रित पत्थर का शिखर था। साथ ही मंदिर की चौड़ी दीवारों में लोहे की ऐसी पट्टिकाएं लगाई गईं थीं, जिनमें प्रभावशाली चुंबक था। इन पट्टियों और शिखर को स्थापित करने में कुछ ऐसी अनूठी तकनीक अपनाई गई थी, जिस कारण भगवान सूर्यदेव की मुख्य प्रतिमा बिना किसी सहारे के हवा में तैरती रहती थी। उस कालखंड में सूर्यमंदिर इसलिए बनाए जाते थे, क्योंकि हिंदू मान्यता के अनुसार सूर्य एकमात्र ऐसे देवता हैं, जो प्रत्यक्ष रूप में आंखों से दिखाई देते हैं। सूर्य की अराधना से श्रृद्धालुओं को साकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है।
 इस मंदिर की कल्पना सूर्यरथ से की गई है। रथ में 12 जोड़े विशाल पहिये लगे हुए हैं, इनमें आठ तीलियां हैं। इस रथ को सात शक्तिशाली घोड़े तीव्र गति से खींच रहे हैं। इस रथ के प्रतीकों को समझने से पता चलता है कि 12 जोड़ी पहिये दिन और रात के 24 घंटे दर्शाते हैं। ये पहिये वर्ष में 12 माह होने के भी द्योतक हैं। पहियों में लगी आठ तीलियां दिन और रात के आठों प्रहर की प्रतीक हैं। मंदिर में सूर्य भगवान की तीन प्रतिमाएं हैं। उदित सूर्य, यह मूर्ति सूर्य की बाल्यावस्था की प्रतीक है, जिसकी ऊंचाई आठ फीट है। युवावस्था के रूप में मध्यान्ह सूर्य की प्रतिमा है, जिसकी ऊंचाई 9.5 फीट है। तीसरी प्रतिमा प्रौढ़ावस्था यानी अस्त होते सूर्य की है, जिसकी ऊंचाई तीन फीट है। साफ है, यह मंदिर प्रकृति की दिनचर्या को मूर्त रूप में अभिव्यक्त करता है।
इस मंदिर की कल्पना सूर्यरथ से की गई है। रथ में 12 जोड़े विशाल पहिये लगे हुए हैं, इनमें आठ तीलियां हैं। इस रथ को सात शक्तिशाली घोड़े तीव्र गति से खींच रहे हैं। इस रथ के प्रतीकों को समझने से पता चलता है कि 12 जोड़ी पहिये दिन और रात के 24 घंटे दर्शाते हैं। ये पहिये वर्ष में 12 माह होने के भी द्योतक हैं। पहियों में लगी आठ तीलियां दिन और रात के आठों प्रहर की प्रतीक हैं। मंदिर में सूर्य भगवान की तीन प्रतिमाएं हैं। उदित सूर्य, यह मूर्ति सूर्य की बाल्यावस्था की प्रतीक है, जिसकी ऊंचाई आठ फीट है। युवावस्था के रूप में मध्यान्ह सूर्य की प्रतिमा है, जिसकी ऊंचाई 9.5 फीट है। तीसरी प्रतिमा प्रौढ़ावस्था यानी अस्त होते सूर्य की है, जिसकी ऊंचाई तीन फीट है। साफ है, यह मंदिर प्रकृति की दिनचर्या को मूर्त रूप में अभिव्यक्त करता है।
इस मंदिर की चुंबकीय शक्ति इतनी ताकतवर थी कि जब इस मंदिर के निकट से अंग्रेजों के समुद्री जहाज गुजरते हुए मंदिर के चुंबकीय परिधि में आ जाते थे, तो उनके ’दिशा निरूपण यंत्र’ काम करना बंद कर देते थे। परिणामस्वरूप जहाज दिशा बदलकर मंदिर की ओर खिंचे चले आते थे। इस कारण इन सागरपोतों को भारी नुकसान होता था। अतएव अंग्रेज शासकों ने जब इस रहस्य को जान लिया तब उन्होंने मंदिर के शिखर को हटा दिया। चूंकि यह शिखर केंद्रीय चुंबकत्व का केंद्र था, इसलिए इसके हटते ही मंदिर की दीवारों से जो चुबंक-पट्टिकाएं आबद्ध थीं, उनका संतुलन बिगड़ गया और मंदिर के पत्थर खिसकने लगे। गोया, मंदिर का मूलस्वरूप तितर-बितर हो गया।
सूर्यरथ से जुड़ा मिथक
आमतौर से सूर्य को प्रकाश और गर्मी का अक्षुण्ण स्रोत माना जाता है। परंतु जब सूर्य दक्षिणायन रहते हैं, तब मौसम ठंडा रहता है और जब मकर संक्रांति के दिन से सूर्य उत्तरायण होने लगते हैं, यानी उत्तर की ओर गमन करने लगते हैं, तो ठंड कम होने लगती है और दिन बड़े होने लगते हैं। इस स्थिति के निर्माण का कारक पुराणों में सूर्य के रथ में एक पहिए के होने से जुड़ा है। सूर्य की गतिशीलता से जुड़ा यह मिथक नितांत सार्थक और निरंतर प्रासंगिक बना रहने वाला है। यदि सूर्य रथ में दो पहिए होते तो उसमें ठहराव आ सकता था। सूर्य की गति में स्थिरता का अर्थ था, सृष्टि का सर्वनाश।
अब वैज्ञानिक भी मान रहे हैं कि यदि सूर्य की गति में ठहराव आ जाए तो पृथ्वी पर विचरण करने वाले सभी जीव-जंतु तीन दिन के भीतर मर जाएंगे। सूर्य के स्थिर होने के साथ ही वायुमंडल में उपलब्ध समूची जलवाष्प ठंडी होकर बर्फ में बदल जाएगी और समूचे ब्रह्मांड में शीतलता छा जाएगी। फलतः कोई भी प्राणी जीवित नहीं रह पाएगा। करीब पचास करोड़ वर्ष पहले अस्तित्व में आए इस प्रकाशित सूर्य की प्राणदायिनी ऊर्जा की रहस्मयी शक्ति को भारतीय ऋषियों ने छह हजार साल पहले ही समझ लिया था। अतएव वे ऋग्वेद में लिख गए थे, ’आप्रा द्यावा पृथिवी अंतरिक्षः सूर्य आत्मा जगतस्थश्च।’ अर्थात विश्व की चर तथा अचर वस्तुओं की आत्मा सूर्य ही है। इसीलिए वैदिक काल के पूर्व से ही ज्ञान और प्रकाश को अंतर में एकत्र करने के लिए मनुष्य सूर्योपासना करता आ रहा है। चंद्रमा की चमक भी सूर्य के आलोक में अंतर्निहित है।
एक चक्रीय सूर्य की कल्पना काल (संक्रांति) की गति के रूप में भी की गई है। अतएव सूर्य का महत्व खगोल और ज्योतिष के साथ अध्यात्म में भी है। खगोल विज्ञानियों का मानना है कि उत्तरी व दक्षिणी छोर के अंतिम बिंदु अर्थात कर्क व मकर रेखा तक सूर्य की रोशनी एकदम सीधी (लंबवत) पड़ती है। पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा से सूर्य जब दक्षिण की ओर बढ़ता है तो दक्षिणायन और जब मकर रेखा से उत्तर हो जाता है तो उत्तरायण कहलाता है। इन दोनों स्थितियों के निर्माण में छह मास का समय लगता है। महाभारत के योद्धा पितामाह भीष्म ने सूर्य के उत्तरायण होने पर ही प्राण छोड़े थे। वैदिक मान्यता है कि देवताओं का निवास उत्तरी धु्रव और दैत्यों का आवास दक्षिणी धु्रव है। इसलिए भी उत्तरायण सूर्य को जीव-जगत के लिए शुभ माना जाता है।
सूर्य के एक चक्रीय रथ में सात घोड़ों के जुते होने की कल्पना ऋषियों ने की हैं। इन अश्वों को नियंत्रित करने में जो वल्गाएं सौर-रश्मियां परिलक्षित होती हैं, वही सात प्रकार की किरणें हैं। अब विज्ञान ने इन सात किरणों के अस्तित्व को मान लिया है और इनके पृथक-पृथक महत्व को समझने में लगा है। अब तक के शोधों से ज्ञात हुआ है कि सूर्य किरणों के अदृश्य हिस्से में अवरक्त और पराबैंगनी किरणें होती हैं। भूमंडल को गर्म रखने और जैव-रासायनिक क्रियाओं को तेज बनाए रखने का काम अवरक्त किरणें और जीवधारियों के शरीर में रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढ़ाने का काम पैराबैंगनी किरणें करती हैं। हालांकि इनमें पैराबैंगनी-सी किरणें अत्यंत घातक होती हैं। इस घातक विकिरण से बचने के लिए ही उगते सूर्य की ओर मुख करके तांबे के पात्र में भरे जल से मकर संक्रांति के दिन सूर्य को अर्घ्य देने का विशेष विधान है। ओजोन परत भी इन किरणों को अवरुद्ध करती हैं। कुल मिलाकर सूर्य रथ का एक चक्रीय होना गतिशील बने रहने का द्योतक है। गतिशीलता ही मनुष्य की मूल प्रकृति है। ठहराव का अर्थ जीवन का शुष्क व निष्क्रिय हो जाना है। स्थिरता एक तरह का विकार है, जो जीवन और प्रकृति को जड़ता में बदल सकता है। जड़ता, ऐसी सडांध है, जो मृत्यु का पर्याय बन जाती है। अतएव गतिशीलता जीवन की अनिवार्य चर्या बनी रहनी चाहिए।
सोमनाथ मंदिर का विज्ञान
इसी शैली में काठियावाड़ गुजरात का सोमनाथ मंदिर था। इस मंदिर में शिवलिंग चुंबकीय प्रभाव से अधर में झूलता रहता था। यह एक आश्चर्य के विषय के साथ वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण भी था। हवा में तैरते इस चुंबकीय शिवलिंग और मंदिर में उपलब्ध सोने-चांदी के अकूत भंडार की जानकारी जब महमूद गजनवी को लगी तो वह हतप्रभ रह गया। मंदिर के किवाड़ भी सोने के थे। गजनवी को यह जानकारी अरब यात्री अलबरुनी के यात्रा वृतांत से मिली थी। लुटेरे गजनवी ने सन् 1025 में पांच हजार सशस्त्र सैनिकों के साथ मंदिर को लूटने और तोड़ने की मंशा के साथ सोमनाथ की ओर कूच कर अचानक आक्रमण कर दिया। मंदिर को संकट में देख नगर के हजारों निहत्थे लोग मंदिर की रक्षा के लिए दौड़ पड़े। लेकिन सशस्त्र सैनिकों के हाथ निष्ठुरतापूर्वक मारे गए। मंदिर में पूजा-अर्चना कर रहे 50 हजार श्रद्धालुओं और पुजारियों को भी मार दिया गया। अंततः गजनवी की मंशा पूरी हुई, उसने मंदिर तो तोड़ा ही टनों धन-संपदा भी लूटकर ले गया।
स्वतंत्र भारत में तोड़े गए मंदिर के प्रतीकस्वरूप नया मंदिर सरदार वल्लभभाई पटेल की दृढ़ इच्छाशक्ति के चलते अस्तित्व में लाया गया। इसकी आधारशिला आठ मई 1950 को सौराष्ट्र के पूर्व राजा दिग्विजय सिंह ने रखी। 11 मई 1951 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉ राजेंद्र प्रसाद ने मंदिर में ज्योतिर्लिंग स्थापित किया। यह मंदिर 1962 में पूर्ण रूप से निर्मित हो गया था। यह मंदिर अरब सागर तट पर स्थित है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से इसे पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। भगवान श्रीकृष्ण ने इसी प्रभाष क्षेत्र में जरा नाम के व्याध के बाण से प्राण त्यागे थे। इस मंदिर में गर्भग्रह, सभामंडप और नृत्यमंडप तीन प्रमुख भाग हैं। मंदिर का 150 फीट ऊंचा शिखर है। शिखर पर 10 टन भार का कलश रखा हुआ है। इसी स्थल पर जो प्राचीन मंदिर था, उस पर एक शिलालेख लगा था, जो संकेत देता था कि यहां से दक्षिणी ध्रुव बिना किसी बाधा के पहुंचा जा सकता है। इसे बाद में समुद्र विज्ञानियों ने सही पाया। इससे पता चलता है कि हमारे प्राचीन ऋषि-मुनियों ने पूरे विश्व का भौगोलिक ज्ञान प्राप्त कर लिया था। ॠगवेद के अनुसार इस मंदिर का निर्माण चंद्रदेव सोमराज ने किया था। इस मंदिर को मुस्लिम अक्रांताओं ने अनेक बार तोड़ा और हिंदू राजाओं ने हर बार इसका पुर्ननिर्माण कराया।
तैरने वाले पत्थरों से बने रामप्पा मंदिर का विज्ञान
वाल्मीकि रामायण में चित्रित रामसेतु को सभी जानते हैं कि यह तैरने वाले पत्थरों से बना है। ऐसे ही पत्थरों से बना आंध्र-प्रदेश के ग्राम पालमपेट का ’रामप्पा’ मंदिर है। इसे काकतिया वंश के महाराजा गणपति देव ने सन् 1213 में बनवाया था। इस मंदिर के शिल्प को देखकर गणपति देव इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने मंदिर का नाम इसके वास्तुशिल्पी रामप्पा के नाम से रख दिया। भारत ही नहीं विश्व में शायद यह इकलौता मंदिर है, जो भगवान के नाम से न होकर शिल्पकार के नाम से है। इस क्षेत्र में भूकंपों से इसके समकालीन अन्य मंदिर और भवन तो जर्जर हो गए, लेकिन यह भूकंप के प्रभाव से अछूता, यथारूप में खड़ा है। इस मंदिर को संयुक्त राष्ट्रसंघ ने 2021 में विश्व-धरोहर की सूची में शामिल किया है।
पुरातत्व विज्ञानियों ने जब इस मंदिर को खंडहरों के बीच सुरक्षित पाया तो इसके निर्माण की विधि जानने की जिज्ञासा हुई। प्रयोग में लाए गए कुछ पत्थरों को निकालकर उनका तकनीकी परीक्षण किया गया। इन पत्थरों का वजन बहुत कम था। अतएव इन्हें जब पानी में डाला गया तो ये डूबने की बजाय तैरते रहे। तब जाकर मंदिर की मजबूती का रहस्य उजागार हुआ। दरअसल अन्य मंदिर व भवन ठोस व कठोर पत्थरों से बने थे। इसलिए वे सतह पर कंपन होने से टूट गए। लेकिन रामप्पा मंदिर में लगे पत्थरों का भार बहुत कम था, इसलिए भूकंप को चुनौती देते हुए मंदिर खड़ा रहा। हालांकि अब तक वैज्ञानिक इन पत्थरों का यह रहस्य नहीं जान पाए हैं कि ये पत्थर कहां से लाए गए या फिर किस तकनीक से बनाए गए? क्योंकि ये पत्थर दुनिया में प्राकृतिक रूप में कहीं मिलते नहीं हैं। रामसेतु जरूर ऐसे ही पत्थरों से बना है। रामसेतु को नासा ने सबसे प्राचीन मानव निर्मित सरंचना माना है। अब औद्योगिक अनुसंधान परिषद् रामसेतु पर भूगर्भीय हलचल के पड़े असर की जांच कर रही है।
वैसे इस क्षेत्र में ऐसे छिद्रयुक्त कम दबाव व भार वाले पत्थर भी पाए जाते हैं, जो पानी में नहीं डूबते। इन्हें इसी सेतु का भाग बताकर लोग आजीविका भी चलाते हैं। पुराविदों का मानना है कि ज्वालामुखी फूटने के समय ऐसे पत्थर प्राकृतिक रूप से निर्मित हो जाते हैं, जिनके भीतर हवा भरी रहती है। लेकिन 48 किमी लंबा सेतु इन प्राकृतिक पत्थरों से बनाया गया हो, यह मुश्किल है। रामप्पा मंदिर में जो बलुआ पत्थर जड़े हैं, उन्हें मानव निर्मित माना जा रहा है। इस मंदिर की नींव, आधार और गुंबद ऐसे ही पत्थरों से बने हैं।
वैज्ञानिकों ने तकनीकी जांच में पाया कि इन पत्थरों को बनाने के लिए एक आयताकार खाई तैयार की गई, जिसमें ग्रेनाइट पत्थर का चूर्ण, गन्ने से निर्मित चीनी (केन शुगर), नदी की रेत और कुछ अन्य यौगिक डालकर एक मिश्रण तैयार किया। इस मिश्रण से नींव भरी गई और विभिन्न आकार के छिद्रयुक्त पत्थर तैयार किए गए। इन पत्थरों को जब आधार और दीवारों पर जोड़ा गया तब इनके बीच में अंतर रखा गया, जैसा कि रेल पटरियों के बीच में रखा जाता है। गोया, 1 अप्रैल 1843 को जब इस क्षेत्र में भूकंप आया तो आस-पास के भवन तो ढह गए, लेकिन मंदिर सुरक्षित रहा। हालांकि मंदिर के आधार के पत्थरों के बीच जो अंतराल रखा गया था, वहां से वे कुछ इंच ऊपर जरूर उठ गए थे। दरअसल निर्माण की इस अनूठी तकनीक की वजह से जो मिश्रण नींव और आयताकार आधार में भरा गया था, वह छिद्रयुक्त कम भार का मिश्रण था। इसलिए उसने भूकंप के कंपन को अवशोषित कर लिया।
लगभग ऐसी ही तकनीक से वर्तमान में बहुमंजिला इमारतें बनाई जा रही हैं। राम मंदिर के आधार में भी ऐसी ही तकनीक इस्तेमाल की जा रही है। इस तकनीक को ’ब्लॉक ऐरिटेड कांकरीट इंजेक्ट टेक्नोलॉजी’ कहते हैं। इस विधि से नींव व आधार में गैस भरी जाती है। जिससे भूकंप का असर भवन पर न पड़े। साफ है, हमारे वास्तुशिल्पी भूकंपरोधी तकनीक का प्रयोग जानते थे, इसलिए रामप्पा मंदिर भूकंप से अछूता रहा। भयंकर बाढ़ और भूस्खलन से केदारनाथ मंदिर भी शायद इसीलिए बचा रहा। ओड़ीसा का कोणार्क मंदिर भी इसी तकनीक से निर्मित बताया जाता है। प्राचीन मंदिरों में यह तकनीक प्रयोग करने के अन्य प्रमाण भी मिले हैं।